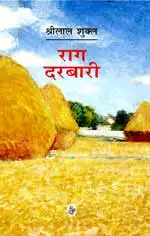|
उपन्यास >> राग दरबारी राग दरबारीश्रीलाल शुक्ल
|
221 पाठक हैं |
|||||||
डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि को विशेष स्थान पर जाकर रामाधीन की तरफ़
से रुपये की एक थैली एकान्त में रख दी जाए। डाका डालने की यह पद्धति आज भी
देश के कुछ हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय है। पर वास्तव में है यह मध्यकालीन
ही, क्योंकि इसके लिए चाँदी या गिलट के रुपये और थैली का होना आवश्यक है,
जबकि आजकल रुपया नोटों की शक्ल में दिया जा सकता है और पाँच हजार रुपये
प्रेम-पत्र की तरह किसी लिफ़ाफ़े में भी आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चेक से
भी रुपये का भुगतान किया जा सकता है। इन कारणों से परसों रात अमुक टीले पर
पाँच हजार रुपये की एक थैली रखकर चुपचाप चले जाओ, यह आदेश मानने में
व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। टीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफ़ाफ़ा हवा
में उड़ सकता है, चेक जाली हो सकता है। संक्षेप में, जैसे कला, साहित्य,
प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में, वैसे ही डकैती के क्षेत्र में भी
मध्यकालीन पद्धतियों को आधुनिक युग में लागू करने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ
पैदा हो सकती हैं।
जो भी हो, डकैतों ने इन बातों पर विचार नहीं किया था क्योंकि रामाधीन के यहाँ
डाके की चिट्ठी भेजनेवाले असली डकैत न थे। उन दिनों गाँव-सभा और कॉलिज की
राजनीति को लेकर रामाधीन भीखमखेड़वी और वैद्यजी में कुछ तनातनी हो गई थी। अगर
शहर होता और राजनीति ऊँचे दर्जे की होती तो ऐसे मौके पर रामाधीन के खिलाफ़
किसी महिला की तरफ़ से पुलिस में यह रिपोर्ट आ गई होती कि उन्होंने उसका में
शीलभंग करने की सक्रिय चेष्टा की, पर महिला के सक्रिय विरोध के कारण वे कुछ
नहीं कर पाए और वह अपना शील समूचा-का-समूचा लिये हुए सीधे थाने तक आ गई। पर
यह देहात था जहाँ अभी महिलाओं के शीलभंग को राजनीतिक युद्ध में हैण्डग्रिनेड
की मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए वहाँ कुछ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया
गया था और बाबू रामाधीन के ऊपर डाकुओं का संकट पैदा करके उन्हें कुछ दिन
तिलमिलाने के लिए छोड़ दिया गया था।
पुलिस, रामाधीन भीखमखेड़वी और वैद्यजी का पूरा गिरोह-ये सभी जानते थे कि डाके
की चिट्ठी फ़र्जी है। ऐसी चिट्ठियाँ कई बार कई लोगों के पास आ चुकी थीं।
इसलिए रामाधीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि वह नियत तिथि और समय पर रुपये के साथ
टीले पर पहुँच ही जाए। चिट्ठी फ़र्जी न होती, तब भी रामाधीन शायद चुपचाप
रुपया दे देने के मुक़ाबले घर पर डाका डलवा लेना ज्यादा अच्छा समझते। पर
चूँकि रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो गई थी, इसलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ करने के
लिए मजबूर थी। उस दिन टीले से लेकर गाँव तक का स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर
दिया गया और उसमें वे 'डाकू-डाकू' का खेल खेलते रहे। टीले पर तो एक
थाना-का-थाना ही खुल गया। उन्होंने आसपास के ऊसर, बंजर, जंगल, खेत-खलिहान
सभी-कुछ छान डाले, पर डाकुओं का कहीं निशान नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने
पेड़ों की टहनियाँ हिलाकर, लोमड़ियों के बिलों में संगीनें घुसेड़कर और
सपाट जगहों को अपनी आँखों से हिप्नोटाइज करके इत्मीनान कर लिया कि वहाँ जो
हैं, वे डाकू नहीं हैं; वे क्रमशः चिड़ियाँ, लोमड़ियाँ और कीड़े-मकोड़े हैं।
रात को जब बड़े जोर से कुछ प्राणी चिल्लाए तो पता चला कि वे भी डाकू नहीं,
सियार हैं और पड़ोस के बाग में जब दूसरे प्राणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में
आ गया कि वे कुछ नहीं, सिर्फ़ चमगादड़ हैं। उस रात डाकुओं वे और रामाधीन
भीखमखेड़वी के बीच की कुश्ती बराबर पर छूटी, क्योंकि टीले पर न डाकू रुपया
लेने के लिए आए और न रामाधीन देने के लिए गए।
थाने के छोटे दारोगा को नौकरी में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। टीले पर
डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हें ही सौंपा गया था, पर सबकुछ करने पर भी वे
अपनी माँ को भेजी जानेवाली चिट्ठियों की अगली किस्त में यह लिखने लायक नहीं
हुए थे कि माँ, डाकुओं ने मशीनगन तक का इस्तेमाल किया, पर इस भयंकर गोलीकाण्ड
में भी तेरे आशीर्वाद से तेरे बेटे का बाल तक बाँका नहीं हुआ। वे रात को लगभग
एक बजे टीले से उतरकर मैदान में आए; और चूँकि सर्दी होने लगी थी और अँधेरा था
और उन्हें अपनी नगरवासिनी प्रिया की याद आने लगी थी और चूँकि उन्होंने बी.ए.
में हिन्दी-साहित्य भी पढ़ा था; इन सब मिले-जुले कारणों से उन्होंने
धीरे-धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और आखिर में गाने लगे, “हाय मेरा दिल !
हाय मेरा दिल !" 'तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर' वाली कहावत को
चरितार्थ करते उनके आगे भी दो सिपाही थे और पीछे भी। दारोगाजी गाते रहे और
सिपाही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएँगे। मैदान पार
करते-करते दारोगाजी का गाना कुछ बुलन्दी पर चढ़ गया और साबित करने लगा कि जो
बात इतनी बेवकूफ़ी की है कि कही नहीं जा सकती, वह बड़े मजे से गायी जा सकती
है।
सड़क पास आ गई थी। वहीं एक गड्ढे से अचानक आवाज आयी, “कौन है सफ़र्कीला ?"
दारोगाजी का हाथ अपने रिवाल्वर पर चला गया। सिपाहियों ने ठिठककर राइफलें
सँभाली; तब तक गड्ढे ने दोबारा आवाज दी, "कौन है सफ़र्कीला ?" एक सिपाही ने
दारोगाजी के कान में कहा, “गोली चल सकती है। पेड़ के पीछे हो लिया जाए हुजूर
!"
पेड़ उनके पास से लगभग पाँच गज की दूरी पर था। दारोगाजी ने सिपाही से
फुसफुसाकर कहा, “तुम लोग पेड़ों के पीछे हो जाओ। मैं देखता हूँ।"
इतना कहकर उन्होंने कहा, “गड्ढे में कौन है ? जो कोई भी हो बाहर आ जाओ।" फिर
एक सिनेमा में देखे दृश्य को याद करके उन्होंने बात जोड़ी, “तुम लोग घिर गए
हो। तुम आधे मिनट में बाहर न आए, तो गोली चला दी जाएगी।"
गड्ढे में थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आवाज आयी, “मर्फ़र गये सफ़र्कीले, गोली
चर्फलानेवाले।"
प्रत्येक भारतीय, जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है, भाषा के मामले में पत्थर
हो जाता है। इतनी तरह की बोलियाँ उसके कानों में पड़ती हैं कि बाद में हारकर
वह सोचना ही छोड़ देता है कि यह नेपाली है या गुजराती। पर इस भाषा ने
दारोगाजी को चौकन्ना बना दिया और वे सोचने लगे कि क्या मामला है ! इतना
तो समझ में आता है कि इसमें कोई गाली है, पर यह क्यों नहीं समझ में आता कि यह
कौन-सी बोली है ! इसके बाद ही जहाँ बात समझ के बाहर होती है वहीं गोली चलती
है-इस अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का शिलपालगंज में प्रयोग करते हुए दारोगाजी
ने रिवाल्वर तान लिया और कड़ककर बोले, “गड्ढे से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं
गोली चलाता हूँ।" पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के
पीछे से निकलकर कहा, “गोली मत चलाइए हुजूर, यह जोगनथवा है। पीकर गड्ढे में
पड़ा है।"
|
|||||


 i
i