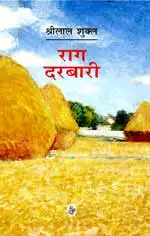|
उपन्यास >> राग दरबारी राग दरबारीश्रीलाल शुक्ल
|
221 पाठक हैं |
|||||||
8
शिवपालगंज गाँव था, पर वह शहर से नजदीक और सड़क के किनारे था। इसलिए
बड़े-बड़े नेताओं और अफ़सरों को वहाँ तक आने में कोई सैद्धान्तिक एतराज नहीं
हो सकता था। कुओं के अलावा वहाँ कुछ हैण्डपम्प भी लगे थे, इसलिए बाहर से
आनेवाले बड़े लोग प्यास लगने पर, अपनी जान को खतरे में डाले बिना, वहाँ का
पानी पी सकते थे। खाने का भी सुभीता था। वहाँ के छोटे-मोटे अफसरों में
कोई-न-कोई ऐसा निकल ही आता था जिसके ठाठ-बाट देखकर वहाँवाले उसे परले सिरे का
बेईमान समझते, पर जिसे देखकर ये बाहरी लोग आपस में कहते, कितना तमीजदार है।
बहुत बड़े खानदान का लड़का है। देखो न, इसे चीको साहब की लड़की ब्याही है।
इसलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग वहाँ खाना भी
खा सकते थे। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में शिवपालगंज में जननायकों और
जनसेवकों का आना-जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको शिवपालगंज के विकास
की चिन्ता थी और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते थे।
वे लेक्चर गँजहों के लिए विशेप रूप से दिलचस्प थे, क्योंकि इनमें प्रायः शुरू
से ही वक्ता श्रोता को और श्रोता वक्ता को बेवकूफ़ मानकर चलता था जो कि
बातचीत के उद्देश्य से गँजहों के लिए आदर्श परिस्थिति है। फिर भी लेक्चर इतने
ज्यादा होते थे कि दिलचस्पी के बावजूद, लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चर का
मजा तो तब है जब सुननेवाले भी समझें कि यह बकवास कर रहा है और बोलनेवाला भी
समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। पर कुछ लेक्चर देनेवाले इतनी गम्भीरता से चलते
कि सुननेवाले को कभी-कभी लगता था यह आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ही ईमानदार
है। ऐसा सन्देह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फ़ीका बन जाता था और उसका असर
श्रोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ़ पड़ता है। यह सब देखकर गँजहों ने अपनी-अपनी
तन्दुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय चुन लिया था, कोई सबेरे खाना
खाने के पहले लेक्चर लेता था, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद । ज्यादातर लोग
लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जागने के बीच
में लेते थे।
उन दिनों गाँव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि
पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले कई सालों से गाँववालों को फुसलाकर बताया जा
रहा था कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है। गाँववाले इस बात का विरोध नहीं करते
थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही यह मानकर चलता था कि गाँववाले इस बात का
विरोध करेंगे। इसीलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूँढ़कर लाते थे और यह साबित
करने में लगे रहते थे कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है। इसके बाद वे यह बताते थे
कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। फिर आगे की बात बताने के पहले ही
प्रायः दोपहर के खाने का वक़्त हो जाता और वह तमीजदार लड़का, जो बड़े सम्पन्न
घराने की औलाद हुआ करता था और जिसको चीको साहब की लड़की ब्याही रहा करती थी,
वक्ता की पीठ का कपड़ा खींच-खींचकर इशारे से बताने लगता कि चाचाजी, खाना
तैयार है। कभी-कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता ले जाते थे और तब मालूम
होता कि उनकी आगे की और पीछे की बात में कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि
घूम-फिरकर बात यही रहती थी कि भारत एक खेतिहर देश है, तुम खेतिहर हो, तुमको
अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता इसी सन्देह
में गिरफ्तार रहता था कि काश्तकार अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहते।
लेक्चरों की कमी विज्ञापनों से पूरी की जाती थी और एक तरह से शिवपालगंज में
दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहाँ की समस्याओं और उनके समाधानों का
सच्चा परिचय देते थे। मिसाल के लिए, समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है
और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान यह था कि
किसानों के आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी-अच्छी तस्वीरें दिखायी जाएँ।
उनके द्वारा उन्हें बताया जाय कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते
तो देश के लिए करो। इसी से जगह-जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश
के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला-जुला
असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता था और भोले-से-भोला काश्तकार भी मानने
लगता था कि हो-न-हो, इसके पीछे भी कोई चाल है।
शिवपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खासतौर से मशहूर हो रहा था जिसमें एक
तन्दुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बाँधे, कानों में बालियाँ लटकाए और बदन पर
मिर्जई पहने गेहूँ की ऊँची फसल को हँसिये से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे
खड़ी हुई, अपने-आपसे बहुत खुश, कृषि-विभाग के अफ़सरोंवाली हँसी हँस रही थी।
नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिन्दी अक्षरों में लिखा था, “अधिक अन्न उपजाओ।'
मिर्जई और बालीवाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे, उन्हें
अंग्रेजी इबारत से और जो हिन्दी के विद्वान थे, उन्हें हिन्दी से परास्त करने
की बात सोची गई थी; और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे, वे भी
कम-से-कम आदमी और औरत को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के
पीछे हँसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह
अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। यह तस्वीर शिवपालगंज में आजकल कई जगह चर्चा
का विषय बनी थी, क्योंकि यहाँवालों की निगाह में तस्वीरवाले आदमी की शक्ल
कुछ-कुछ बद्री पहलवान से मिलती थी। औरत की शक्ल के बारे में गहरा मतभेद था।
वह गाँव की देहाती लड़कियों में से किसकी थी, यह अभी तय नहीं हो पाया था।
|
|||||


 i
i