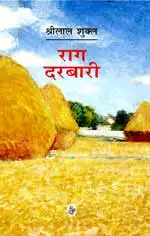|
उपन्यास >> राग दरबारी राग दरबारीश्रीलाल शुक्ल
|
221 पाठक हैं |
|||||||
7
छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य-पुस्तक-जैसा खुला
पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुगदरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि
सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे, परिवार के दूसरे प्राणी भी
कमरे का अपने-अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएँ काँच और मिट्टी के
बरतनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थीं और शाम होते-होते कमरे
में जमा कर देती थीं। यही हाल छत पर सूखनेवाले कपड़ों का भी था। कमरे के
आर-पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लँगोट और चोलियाँ, अंगोछे और
पेटीकोट साथ-साथ झूलते नजर आते थे। वैद्यजी के दवाखाने की अनावश्यक शीशियाँ
भी कमरे की एक आलमारी में जमा थीं। प्रायः सभी शीशियाँ खाली थीं। उन पर चिपके
हुए सचित्र विज्ञापन ‘इस्तेमाल के पहले' शीर्षक पर एक अर्धमानव की तस्वीर से
और 'इस्तेमाल के बाद' शीर्षक के अन्तर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से, जिसकी
मूंछे ऐंठी हुई हैं, लँगोट कसा हुआ है और परिणामतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा है,
पता चलता था कि ये वही शीशियाँ हैं जो हजारों इन्सानों को शेर के मानिन्द बना
देती हैं; यह दूसरी बात है कि वे अपने गुसलखाने और शयन-कक्ष में ही कमर
लपलपाते हुए शेर की तरह घूमा करते हैं, बाहर बकरी-के-बकरी बने रहते हैं।
एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज' जैसी पुस्तकों
से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छापना 1947 के पहले तो जुर्म था ही, आज
भी जुर्म है, जो बहुत-सी दफ्तरी बातों की तरह गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहता,
जो आहार-निद्रा-भय आदि में फँसे हुए आदमियों की जिन्दगी में एक बड़े सुखद
लिटरेरी सप्लीमेण्ट का काम करता है और जो विशिष्ट साहित्य और जन-साहित्य की
बनावटी श्रेणियों को लाँघकर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठित है।
वैसे उसमें कोई खास बात नहीं होती, सिर्फ यही बताया जाता है कि किसी आदमी ने
किसी आदमी या किसी औरत के साथ किसी तरह से क्या बर्ताव किया; यानी उसमें,
सुमित्रानन्दन पन्त की दार्शनिक भाषा में कहा जाए तो, ‘मानव मानव के चिरन्तन'
सम्बन्धों का वर्णन होता है इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए
भी होता था और वह अध्ययन, जाहिर है, परिवार में अकेले विद्यार्थी होने के
नाते, रुप्पन बाबू ही करते थे। रुप्पन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए
भी करते थे। जिस सुख के लिए दूसरे लोगों को रोटी के टुकड़े, पेड़ की छाँव,
कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उमरखैयामी पदार्थों की जरूरत होती है,
वह सुख रुप्पन बाबू इस कमरे में अपने-आप ही खींच लेते थे।
परिवार के सभी लोगों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का नारा बुलन्द करनेवाले इस
कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए श्रद्धा पैदा हो सकती
थी। इसे देख लेने पर कोई भी समाजशास्त्री यह नहीं कह सकता था कि पूर्वी
गोलार्द्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को कहीं से कोई खतरा है यही कमरा
रंगनाथ को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ चार-पाँच महीने रहना था।
वैद्यजी ने ठीक ही बताया था। एम.ए. करते-करते किसी भी सामान्य विद्यार्थी की
तरह वह कमजोर पड़ गया था। उसे बुखार रहने लगा था। किसी भी सामान्य
हिन्दुस्तानी की तरह उसने डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास न रहते हुए भी
डॉक्टरी दवा खायी थी। उससे वह अभी विलकुल ठीक नहीं हो पाया था। किसी भी
सामान्य शहराती की तरह उसकी भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर
होती है। इसलिए वह यहाँ रहने के लिए चला आया था। किसी भी सामान्य मूर्ख की
तरह उसने एम.ए. करने के वाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी
थी, पर किसी भी सामान्य बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए
विश्वविद्यालय में रहना और नित्यप्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं है।
इसीलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन वह गाँव में रहकर आराम करेगा, तन्दुरुस्ती
बनाएगा, अध्ययन करेगा, जरूरत पड़ने पर शहर जाकर किताबों की अदला-बदली कर आएगा
और वैद्यजी को हर स्टेज पर शिप्ट भाषा में यह कहने का मौक़ा देगा कि काश !
हमारे नवयुवक निकम्मे न होते तो हम बुजुर्गों को ये जिम्मेदारियाँ न उठानी
पड़तीं।
ऊपर का कमरा काफ़ी बड़ा था और उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना
व्यक्तिवाद फैला दिया था। उसकी सफ़ाई कराके एक चारपायी स्थायी रूप से डाल दी
गई थी, उस पर एक स्थायी बिस्तर पड़ गया था। पास की आलमारी में उसकी किताबें
लग गई थीं और उनमें जेबी जासूस या गुप्त साहित्य के प्रवेश का निषेध कर दिया
गया था। वहीं एक छोटी-सी मेज और कुर्सी भी कॉलिज से मँगाकर लगा दी गई थी।
चारपायी के पास ही दीवाल में एक खिड़की थी, जो खुलने पर बागों और खेतों का
दृश्य पेश करती थी। यह दृश्य रंगनाथ की जिन्दगी को कवित्वमय बनाने के काम आता
था और वहाँ उसे सचमुच ही कभी-कभी लगता था कि उसके सामने न जाने कितने
वर्डस्वर्थ, कितने राबर्ट फ्रास्ट, कितने गुरुभक्तसिंह एक आर्केस्ट्रा बजा
रहे हैं और उनके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुँह में तुरही लगाए, साँस फुलाए
खड़े हुए हैं। रुप्पन बाबू कहीं से कुछ ईंट-रोड़ा उठा लाए थे और उसे
जोड़-गाँठकर उन्होंने एक रेडियो-जैसा तैयार कर दिया था। कमरे के ऊपर वाँसों
और आस-पास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लम्बे-लम्चे तार दौड़ा दिए थे जिससे
लगता था कि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमिशन सेण्टर है। पर अन्दर का
रेडियो एक हेड-फोन के सहारे ही सुना जा सकता था, जिसे कान पर चिपकाकर रंगनाथ
कभी-कभी स्थानीय खबरें और वैष्णव सन्तों के शोकपूर्ण भजन सुन लेता था और
इत्मीनान कर लेता था कि आल इण्डिया रेडियो अब भी वैसा ही है जैसा कि पिछले
दिनों में था और हजार गालियाँ खाकर भी वह बेहया अपने पुराने ढर्रे से
टस-से-मस नहीं हुआ है।
रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्यजी की सलाह से बना था; बहुत सबेरे उठना, उठकर सोचना
कि कल का खाया हजम हो चुका है। (ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् जीर्णाजीर्ण
निरूपयेत्), ताँबे के लोटे में रखा हुआ ठण्डा पानी पीना, दूर तक टहलने निकल
जाना, नित्यकर्म (क्योंकि संसार में वही एक कर्म नित्य है, बाक़ी अनित्य
हैं), टहलते हुए लौटना (पर चंक्रमणं हितम्), मुँह-हाथ धोना, लकड़ी चबाना और
उसी क्रम में लगे हाथ दाँत साफ़ करना (निम्बस्य तिक्तके श्रेष्ठः कपाये
बब्बुलस्तथा), गुनगुने पानी से कुल्ले करना (सुखोष्णोदकगण्ड्पैः जायते
वक्त्रलाघवम्), व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर को भोजन करना,
विश्राम, अध्ययन, सायंकाल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम,
बादाम-मनक्के आदि के द्रव का प्रयोग, अध्ययन, भोजन, अध्ययन, शयन।
रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया था। इसमें सिर्फ इतना
संशोधन हुआ था कि अध्ययन की जगह वैद्यजी की बैठक में गँजहों की सोहबत ने ले
ली थी। चूंकि इससे रंगनाथ के वीर्य की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं था और कुल
मिलाकर उसके पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता था, इसलिए वैद्यजी
को इस संशोधन में कोई ऐतराज न था। बल्कि एक तरह से वे इसे पसन्द करते थे कि
एक पढ़ा-लिखा आदमी उनके पास बैठा रहता है और हर बाहरी आदमी के सामने परिचय
कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है।
कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत
की तरह, जो कहीं नहीं है वह यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है।
उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक-सी है। उसने
देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे-मोटे
अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिसके सहारे बड़े-बड़े निगम, आयोग और
प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घिसटते हैं, वही दाँव-पेंच और पैंतरेबाजी की
अखिल भारतीय प्रतिभा यहाँ कच्चे माल के रूप में इफ़रात से फैली पड़ी है। ऐसा
सोचते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई।
पर कमजोरी सिर्फ एक बात को लेकर थी। उसने देखा था कि शहरों में वाद-विवाद का
एक नया रूप पुरानी और नयी पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी
पीढ़ी का यह विश्वास था कि हम बुद्धिमान हैं और हमारे बुद्धिमान हो चुकने के
बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्त्व खत्म हो गया है और नयी पीढ़ी के लिए उसका
एक कतरा भी नहीं बचा है। वहीं पर नयी पीढ़ी की यह आस्था थी कि पुरानी पीढ़ी
जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाती थी और अपने और समाज के प्रति ईमानदार न थी,
जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालत में खुश नहीं होते हैं और अपने प्रति ईमानदार
हैं और समाज के प्रति कुछ नहीं हैं, क्योंकि समाज कुछ नहीं है।
यह वाद-विवाद खास तौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में ही चल रहा था,
क्योंकि औरों के मुक़ाबले वाद-विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र ही
ज्यादा-से-ज्यादा फैलावदार और कम-से-कम हानिकारक हैं। पिछली पीढ़ी के मन में
अगली पीढ़ी को मूर्ख और अगली के मन में पिछली को जोकर समझने का चलन वहाँ इतना
बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या कला का न होता, तो अब तक गृहयुद्ध हो
चुका होता रंगनाथ कुछ दिन तक समझता रहा कि शिवपालगंज में अभी तक ऐसे
पीढ़ी-संघर्ष का उदय नहीं हुआ है । पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देख
लिया कि यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वह समझ गया कि यहाँ की राजनीति इस
पहलू से भी कमजोर नहीं है।
बात एक चौदह साल के लड़के को लेकर चली थी। एक शाम बैठक में किसी आदमी
ने शिवपालगंज के उस लड़के का जीवन-चरित बताना शुरू किया। उससे प्रकट हुआ कि
लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी थी कि बड़े-बड़े
मनोवैज्ञानिक और समाज-वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो
गए थे । सुना जाता है कि अमरीका से पढ़कर लौटे हुए कई विद्वानों ने उस लड़के
के बारे में छानवीन की। उन्होंने टूटे हुए परिवार, बुरी सोहवत, खराव बातावरण,
अपराधशील वंश-परम्परा आदि रटी-रटायी कितावी थ्योरियों को उस पर खपाना चाहा,
पर लड़के ने खपने से इंकार कर दिया और वाद में वे विद्वान इसी नतीजे पर
पहुँचे कि हो-न-हो, यह प्रभु का चमत्कार है।
वास्तव में इससे इन विद्वानों की अयोग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता ही
प्रमाणित होती है जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति-विज्ञान,
मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी-ऐसी व्यावहारिक समस्याएँ चुटकियों में
पैदा कर सकता है कि अमरीका में क़ीमती कागजों पर छपी हुई किताबों के वेशक़ीमत
सिद्धान्त पोच सावित होने लगते हैं और उनका हल निकालने के लिए बड़े-बड़े
भारतीय विद्वानों को घबराकर फिर अमरीका की ओर ही भागना पड़ता है। इस लड़के की
केस-हिस्ट्री ने भी कुछ ऐसा तहलका मचाया था कि एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी
अगली अमरीका-यात्रा में उसका समाधान ढूँढ़ने की प्रतिज्ञा कर डाली थी।
लड़का शिवपालगंज के इतिहास में अचानक ही दो-तीन साल के लिए उदित हुआ, चमका और
फिर पुलिस के झापड़, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निस्संग
भाव से हजम करता हुआ वाल-अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग वन गया। वहीं
पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना
हुआ है और उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमरीका की मित्रता का सहारा लिया
जानेवाला है। यह बात शिवपालगंज में आते-आते लोक-कथा बन गई थी और तव से वहाँ
उस लड़के का लीला-संवरण बड़े अभिमान के साथ किया जाने लगा था।
रंगनाथ को बताया गया कि वह लड़का दस साल की उम्र में ही इतना तेज दौड़ने लगा
था कि पन्द्रह साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। ग्यारह साल की उम्र
में वह रेल में बिना टिकट चलने और टिकट-चेकर को धता देने में उस्ताद हो गया
था। एक साल बाद वह मुसाफ़िरों के देखते-देखते उनका सामान कुछ इस तरह से गायब
करने लगा जैसे लोकल अनीस्थीशिया देकर होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डालते हैं और
मेज पर लेटे हुए आदमी को पता ही नहीं चलता कि शरीर का एक हिस्सा कहाँ चला
गया। इस तरह की चोरी में उसकी ख्याति सबसे ज्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी
पकड़ा नहीं गया। बाद में, चौदह वर्ष की अबस्था में, जब वह पकड़ा गया, तो पता
चला कि वह ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे की भीतरी सिटकनी खोलने की कला में दक्ष
हो चुका है, बँगलों में चोरियाँ करता है और चोरियाँ भी रोशनदान से नहीं,
बल्कि उपर्युक्त तरकीब से दरवाजा खोलकर, भले आदमियों की तरह क़ायदे के रास्ते
मकान में घुसकर करता है।
इस लड़के की प्रशंसा करते-करते किसी आदमी ने वहराम चोट्टा का भी जिक्र किया
जो किसी जमाने में उस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्त्व का चोर माना जाता था। पर
उसका नाम सुनते ही एक लड़के ने बड़े जोर-शोर से विरोध किया और बतर्ज
विधान-सभा की स्पीचों के, बिना किसी तर्क के, सिर्फ़ आवाज ऊँची करके, साबित
करने की कोशिश की कि "बहराम चोट्टा भी कोई चोट्टा था ! रामस्वरूप ने बारह साल
की उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया, वह बहराम चोट्टा के जनम-भर भी हिलाए न
हिलेगा।"
रंगनाथ को इस बातचीत में पीढ़ी-संघर्ष की झलक दीख पड़ी। उसने सनीचर से पूछा,
“क्या आजकल के चोट्टे सचमुच ही ऐसे तीसमारखाँ हैं? पहले भी तो एक-से-एक
खतरनाक चोट्टे हुआ करते थे।"
सनीचर उस उम्र का था जिसे नयी पीढ़ीवाले पुरानी के साथ और पुरानी पीढ़ीवाले
नयी के साथ लगाते हैं और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन न होने
के कारण जिसे दोनों वर्ग अपने से अलग समझते हैं। इसी कारण उसके ऊपर किसी भी
पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। साहित्य और कला के सैकड़ों अर्ध-प्रौढ़
आलोचकों की तरह सिर हिलाकर, अपनी राय देने से कतराते हुए, वह बोला, "भैया
रंगनाथ, पहले के लोगों का हाल न पूछो। यहीं ठाकुर दुरबीनसिंह थे। मैंने उनके
दिन भी देखे हैं। पर आजकल के लौण्डों के भी हाल न पूछो !"
आज से लगभग तीस साल पहले, जब आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी और हुई भी थी तो :
यशस्वी रहें हे प्रभो ! हे मुरारे !
चिरंजीव रानी व राजा हमारे !
या
'खुदाया, जार्ज पंजुम की हिफ़ाजत कर, हिफ़ाजत कर' का कोरस गाने के लिए हुई
थी, शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गँजहा का नाम ठाकुर दुरबीनसिंह था। उनके
माँ-बाप ने उनके नाम के साथ 'दुरबीन' लगाकर शायद चाहा था कि उनका लड़का हर
काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा ही किया भी। जिस चीज में
उन्होंने दिलचस्पी दिखायी, उसे बुनियाद से पकड़ा। उन्हें अंग्रेजी कानून कभी
अच्छा नहीं लगा। इसलिए जब महात्मा गाँधी सिर्फ़ नमक-कानून तोड़ने के लिए
दाण्डी-यात्रा की तैयारी कर रहे थे उन दिनों दुरबीनसिंह ने इण्डियन पेनल कोड
की सभी दफाओं को एक-एक करके तोड़ने का बुनियादी काम शुरू कर दिया था।
स्वभाव से वे बड़े परोपकारी थे। परोपकार एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे
में हर व्यक्ति की अपनी-अपनी धारणा होती है। कोई चींटियों को आटा खिलाता है,
कोई अबिवाहित प्रौढ़ाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अपने मत्थे पर
'प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार' की तख्ती लगाकर घूमता है, कोई किसी को सीधे
रिश्वत न लेनी पड़े, इसलिए रिश्वत देनेवालों से खुद सम्पर्क स्थापित करके
दोनों पक्षों के बीच दिन-रात दौड़-धूप करता रहता है। ये सब परोपकार-सम्बन्धी
व्यक्तिगत धारणाएँ हैं और दुरबीनसिंह की भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा
थी। वे कमजार आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे। इसीलिए
लड़ाई-भिड़ाई के हर मौके पर वे बिना बुलाए पहुँच जाते थे और कमजोर की तरफ़ से
लाठी चला दिया करते थे। उन शान्तिपूर्ण दिनों में ये सब बातें बँधी दर से
चलती थीं और सारे इलाके में मशहूर था कि शहर में जैसे बाबू जयरामप्रसाद वकील
मारपीट के मुक़दमे में खड़े होने के लिए पचास रुपया हर पेशी पर लेते हैं, उसी
तरह दुरबीनसिंह भी मुक़दमे के पहलेवाली मारपीट के लिए पचास रुपया लेते हैं।
बड़ी लड़ाइयों में, जहाँ आदमी जमा करने पड़ते, यह रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब
से बढ़ती जाती थी, पर उसकी भी दरें निश्चित थीं और उसमें कोई धोखेवाजी नहीं
थी। उनके आदमियों को गोश्त और शराब भी देनी पड़ती थी, पर वे स्वयं इन मौक़ों
पर गोश्त नहीं खाते थे और शराब नहीं पीते थे। इससे उनका पेट हल्का और दिमाग
साफ़ रहता था जो कि युद्ध के समय बड़ी ही वांछनीय स्थिति है; और चूँकि गोश्त
और शराब देखकर भी 'नहीं' कहनेवाला आदमी सदाचारी कहलाता है, इसलिए वे सदाचारी
कहलाते थे।
दुरबीनसिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे सेंध नहीं लगाते थे। वे दीवार
फाँदने के उस्ताद थे। और कहीं भी आसानी से पोल जम्प के चैम्पियन हो सकते थे
शुरू में रुपये की कमी होने पर वे कभी-कभी दीवार फाँदने का काम करते थे। बाद
में वे ऐसा काम सिर्फ कभी-कभी अपने नये चेलों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने
की नीयत से ही करने लगे थे। यह वह जमाना था जब चोर चोर थे और डाकू डाकू। चोर
घर में सिर्फ़ चोरी करने के लिए घुसते थे और एक पाँच साल का बच्चा भी पैर
फटफटा दे तो वे जिस सेंध से अन्दर आए थे उसी से विनम्रतापूर्वक बाहर निकल
जाते थे डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट में ज्यादा होती थी, माल लूटने में कम। इस
परिप्रेक्ष्य में दुरबीनसिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग
जानेवालों को पीटने का चलन चलाया और यह तरीक़ा उनके समसामयिक चोरों में बड़ा
ही लोकप्रिय हो गया, इस तरह दुरबीनसिंह ने चोरों और डकैतों के बीच के फ़ासले
को कम करने का एक बुनियादी काम किया और उनकी पद्धतियों (मेथडालॉजी) में
क्रान्तिकारी परिवर्तन किए।
पर वक्त की बात ! (शिवपालगंज में जो बात भी वक्त के खिलाफ़ पड़ती थी, वक्त की
बात हो जाती थी) यही ठाकुर दुरबीनसिंह अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा
वुढ़ापे में खाकर कुएँ की जगत से नीचे गिर गए। उनकी रीढ़ टूट गई। कुछ दिनों
तक कोने में रखी हुई अपनी लाठी को देख-देखकर दुरबीनसिंह अपने भतीजे के मुँह
में उसे ढूंस देने का संकल्प करते रहे और अन्त में लाठी और भतीजे के मुँह को
यथावत् छोड़कर वे शिवपालगंज की मिट्टी को वीर-विहीन बनाते हुए वीरगति को
प्राप्त हुए, यानी, 'टें' हो गए।
सनीचर ने दुरबीनसिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया ;
"भैया रंगनाथ, अँधेरी रात थी और मैं भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ
रहा था। तब हमारा भी बचपना था और हम बाघ-बकरी को एक निगाह से देखते थे। देह
में ऐसा जोश कि हवा में डण्डा मारते और पत्ता भी खड़क जाए तो छिटककर माँ की
गाली देते थे। तो, अँधेरी रात थी और हम हाथ में डण्डा लिये सटासट चले आ रहे
थे, तभी एक पेड़ के पीछे से किसी ने कहा, 'खबरदार !'
"हमने समझा कि कोई जिन्न आ गया। उनके सामने तो लाठी-डण्डा सभी बेकार। मैंने
लाल लँगोटवाले का ध्यान किया, पर भैया, लाल लँगोटवाला तो तभी काम देगा जब
भूत, प्रेत, जिन्न से मुचेहटा हो। यहाँ पेड़ के पीछे से एक काला-कलूटा, गँठी
देह का जवान निकलकर मेरे सामने आया और बोला, 'जो कुछ हो, चुपचाप रख दो।
धोती-कुरता भी उतार दो।"
“मैंने मारने को डण्डा ताना तो क्या देखा कि चारों तरफ़ से पाँच-छः आदमी घेरा
डाले हुए हैं । सब बड़ी-बड़ी लाठियाँ और भाले लिये हुए। हमने भी कहा कि चलो
सनीचर, तुम्हारी भी जोड़-बाक़ी आज से फिस्स। डण्डा मेरा तना-का-तना रह गया,
चलाने की हिम्मत न पड़ी !
“एक बोला, 'तान के रह क्यों गया ? चलाता क्यों नहीं ? असल बाप की औलाद हो तो
चला दे डण्डा।"
"बड़ा गुस्सा लगा। पर भैया, मैं जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने
कहा, 'जान न लो, माल ले लो।'
"दूसरे ने कहा, 'साले की अधेला-भर की जान, उसके लिए सियार-जैसा फें-फें कर
रहा है। इतना माल छोड़े दे रहा है। अच्छी बात है। धर दे सब माल।'
"बस भैया, एक झोला था, उसमें सत्तू था। एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था। मामा
के घर से मिला था। फस्ट किलास सूत की डोरी। लोटा क्या था, बिलकुल बाल्टी था।
कुएँ से दो सेर पानी खींचता था। पूड़ियाँ थीं असली घी की। तब यह बनास्पती
साला कहाँ चला था ! सब उन्होंने गिनकर धरा लिया। फिर धोती उतरवायी, टेंट में
एक रुपया था, उसे भी छीन लिया। कुरता और लँगोटा पहने हुए जब मैं खड़ा हो गया,
तो एक ने कहा, 'अब मुँह में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ। चूँ-भर किया
तो इसी बाग में खोदकर गाड़ दूंगा।'
“मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा, 'कहाँ रहता है ?'
"मैंने कहा, 'गँजहा हूँ।"
“फिर न पूछो, भैया ! सब लुटेरे खड़े-खड़े मुँह तकने लगे। किसी एक ने मुझसे
शिवपालगंज के मुखिया का नाम पूछा, दूसरे ने लम्बरदार का, तीसरे ने कहा,
'दुरबीनसिंह को जानते हो ?'
"मैंने कहा, 'दुरबीनसिंह की तरफ़ से लाठी भी चलाने जा चुका हूँ। जब रंगपुर
में जमावड़ा हुआ था! सुलह न होती तो हजारों लोग वहीं खेत हो जाते। दुरबीनसिंह
को गाँव के रिश्ते काका कहता हूँ।'
"बस ! राम-राम सीताराम ! जैसे काले आदमियों में कोई गोरा फ़ौजी पहुँच गया हो।
भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस ला रहा है, कोई कुरता, एक ने जूता दिया, एक
ने मेरे हाथ में झोला पकड़ाया। एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वोला,
'तुम्हारी दो पूड़ियाँ खा ली हैं। इनके दाम ले लो। पर दुरबीनसिंह से न बताना
कि हमने तुम्हें घेरा था। चाहे कुछ पैसा ले लो। और कहा तो पेट फाड़कर पूड़ी
निकाल दूं। हमें क्या पता कि भैया, तुम गॅजहा हो !'
"फिर तो सब हमें गाँव के पास के ताल तक पहुँचाने आए। बहुत रिरियाते रहे।
मैंने भी समझाकर उनके आँसू पोंछ दिए। कहा कि जब तुम घर के आदमी निकले तो फिर
पूड़ी खाने का क्या अफ़सोस ! लो, दो-एक और खाओ।
"वह आदमी भागा। कहा, 'दादा, हमने भर पाया। हमें क्या पता था कि तुम गँजहा हो
! बस दादा, दुरबीनसिंह से न कहना।'
"हमने कहा, 'घर चलो, पानी-पत्ता करके जाना। भूखे होओ तो भोजन-भाव कर लेना।'
पर उन्होंने कहा, 'दादा, अब हमें जाने दो। तुम भी जाकर सोओ। कल सबेरे तक यह
सब भूल जाना। किसी से कहना नहीं।'
“सो भैया, मैं घर आकर पड़ रहा। सबेरा होते ही मैंने दुरबीनसिंह के जाकर पैर
पकड़े कि काका, तुम्हारे नाम में लाल लँगोटवाले का जोर बोल रहा है। तुम्हारा
नाम लेकर जान बचा पाया हूँ। दुरबीनसिंह ने पाँव खींच लिए। बोले, ‘जा सनिचरा,
कोई फिकिर नहीं। जब तक मैं हूँ, अँधेरे-उजेले में जहाँ मन हो वहाँ घूमा कर।
किसी का डर नहीं है। साँप-बिच्छू तू खुद ही निबटा ले, बाक़ी को हमारे लिए
छोड़ दे' ।" यहाँ सनीचर साँस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया कि घटिया
कहानी-लेखकों की तरह मुख्य बात पर आते-आते वह हवा बाँध रहा है। उसने पूछा,
“फिर तो जब तक दुरबीनसिंह थे, गँजहा लोगों के ठाठ कटते रहे होंगे ?"
तब रुप्पन बाबू बोले । उन्होंने रंगनाथ की जानकारी में पहली बार एक साहित्यिक
बात कही। साँस भरकर कहा :
कि पुरुस बली नहिं होत है, कि समै होत बलवान।
कि भिल्लन लूटी गोपिका, कि वहि अरजुन वहि बान॥
रंगनाथ ने पूछा, “क्या हो गया रुप्पन बाबू ? क्या शिवपालगंज से कोई तुम्हारी
गोपिकाएँ लूट ले गया ?"
रुप्पन बाबू ने कहा, “सनीचर, दूसरावाला क़िस्सा भी सुना दो।"
सनीचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया :
"भैया, लठैती का काम कोई असेम्बली का काम तो है नहीं। असेम्बली में जितने ही
बूढ़े होते जाओ, जितनी ही अकल सठियाती जाए, उतनी ही तरक्की होती है। यही
हरनामसिंह को देखो। चलने को उठते हैं तो लगता है कि गिरकर मर जाएँगे। पर
दिन-पर-दिन वहाँ उनकी पूछ बढ़ रही है। यहाँ लठैती में कल्ले के जोर की बात
है। जब तक चले, तब तक चले। जब नहीं चले, तब हलाल हो गए।
"अभी पाँच-छः साल हुए होंगे, मैं कातिक के नहान के लिए गंगा घाट गया था।
लौटते-लौटते रात हो गई। यही भोलूपुर के पास रात हुई। बढ़िया चटक चाँदनी। बाग़
के भीतर हम मौज में आ गए तो एक चौबोला गाने लगे। तभी किसी ने पीछे से पीठ पर
दायें से लाठी मारी। न राम-राम, न दुआ-सलाम, एकदम से लाठी मार दी। अब भैया,
चौबोला तो जहाँ का तहाँ छूटा, झोला बीस हाथ पर जाकर गिरा। डण्डा अलग छिटक
गया। मैं चिल्लाने को हुआ कि तीन-चार आदमी ऊपर आ गए। एक ने मुँह दबाकर कहा,
'चुप बे साले ! गरदन ऐंठ दूंगा !' मैंने तड़फड़ाकर उठने की कोशिश की, पर
भैया, अचकचे में कोई गामा पहलवान पर लाठी छोड़ दे तो वहीं लोट जाएगा, हमारी
क्या बिसात ? वहीं मुँह बन्द किए पड़े रहे। थोड़ी देर में हाथ-पाँव जोड़ता
रहा। इशारा करके कहा कि मैं चिल्लाऊँगा नहीं। तब कहीं उन्होंने मुँह से कपड़ा
निकाला। एक ने मुझसे पूछा, 'रुपया कहाँ है ?'
"मैंने कहा, 'बापू, जो कुछ है, इसी झोले में है।'
"झोले में डेढ़ रुपये की रेजगारी थी। एक लुटेरे ने उसे हाथ में खनखनाकर कहा,
'लँगोटा खोलकर दिखाओगे ?'
"मैंने कहा, 'बापू, लँगोटा न खुलवाओ। उसके नीचे कुछ नहीं है। नंगा हो
जाऊँगा।'
"बस भैया, वे बिगड़े। उन्होंने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर तो उन्होंने
देह पर से सभी कुछ उतरवाकर तलाशी ली। गाँजा-भाँग की खोज में पुलिसवाले भी ऐसी
तलाशी नहीं लेते। जब कुछ नहीं निकला तो उनमें से एक ने मेरे पीछे एक लात मारी
और कहा कि अब चुपचाप मुँह बन्द किए नाक के सामने चले जाओ और अपने दरबे में
घुस जाओ।
“अब तक मेरी बोली लौट आयी थी। मैंने कहा, 'बापू, तुम लोगों ने हमारी जान छोड़
दी, यह ठीक ही किया है। माल ले लिया तो ले लिया, उसकी फिकिर नहीं। हम भी
तुमको बता दें कि तुम नमक से नमक खा रहे हो। तुम हो सरकार के, तो हम भी हैं
दरबार के।'
“वे लोग मेरे पास सिमट आए। पूछने लगे, ‘कौन हो तुम ? कहाँ रहते हो ?
किसके साथ हो ?'
“मैंने कहा, 'मैं गँजहा हूँ। ठाकुर दुरबीनसिंह के साथ रहता आया हूँ।'
"फिर न पूछो भैया रंगनाथ ! सब ठिल्लें मार-मारकर हँसने लगे। एक ने मेरा हाथ
पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं सोच भी नहीं पाया था कि वह क्या करने जा रहा है,
और उसने एक लँगड़ी मारकर मुझे वहीं चित्त कर दिया।
"मैं फिर देह से घास-फूस झाड़कर खड़ा हुआ। एक लुटेरे ने जो नयी उमिर का सजीला
जवान था, कहा, 'यह दुरबीनसिंह किस चिड़िया का नाम है ?' सब फिर ठी-ठी करके
उसी तरह हँसने लगे।
"मैंने कहा, 'दुरबीनसिंह के नहीं जानते बापू ? क्या बाहर से आए हो ? यहाँ दस
कोस के इर्द-गिर्द कोई गँजहा लोगों को नहीं टोकता। दुरबीनसिंह के गाँववालों
को सभी छोड़कर चलते हैं। मगर बापू, तुम नहीं मानते तो ले जाओ मेरा झोला। कोई
बात नहीं।'
"लुटेरे फिर ठी-ठी करने लगे। एक बोला, 'मैं जानता हूँ। अब दुरबीनसिंह के दिन
लद गए। ये जितने पुराने लोग थे, थोड़ी लठैती दिखाकर तीसमारखाँ बन जाते थे।
इनके दुरबीनसिंह लाठी चलाकर, दो-चार दीवारें फाँदकर बहादुर बन गए। अब बाँस के
सहारे दीवारें फाँदना तो स्कूलों तक में सिखा देते हैं।'
“एक लुटेरा वोला, 'लाठी चलाना भी तो सिखाते हैं। मैंने खुद वहीं लाठी चलाना
सीखा था।'
“पहलेवाला नौजवान बोला, 'तो यही दुरबीनसिंह बड़े नामवर हो गए। तमंचा तक तो
साले के पास है नहीं। चले हैं जागीरदारी फैलाने !'
“एक दूसरा लुटेरा हाथ में चोर-वत्ती लिये खड़ा था। जेब से उसने एक तमंचा
निकाला। कहा, 'देख लो बेटा, यही है छः गोलीवाला हथियार । देसी कारतूस तमंचा
नहीं, असली विलायती,' कहते-कहते उसने तमंचे की नली हमारी छाती पर ठोक दी।
कहता रहा, 'जाकर बता देना अपने बाप को। अन्धों में काना राजा बनने के दिन लद
गए। अब वे पड़े-पड़े खटिया पर रोते रहें। कभी अँधेरे-उजेले में दिख गए तो
खोपड़ी का गूदा निकल जाएगा। समझ गए बेटा फकीरेदास !'
"इसके बाद भैया, मैं अपने को रोक न पाया। देह में इतना जोश बढ़ा कि डण्डा तक
वहीं फेंककर बड़े जोर से हिरन की तरह भागा। मेरे पीछे उन लोगों ने फिर ठहाका
लगाया। एक चिल्लाकर बोला, 'मार साले दुरबीनसिंह को। खड़ा तो रह, अभी
मारते-मारते दुरबीन वनाए देता हूँ।'
"मगर भैया, भागने में कोई हमारा आज तक मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ स्कूल-
-कॉलिज में लड़कों को सीटी बजा-बजाकर भागना सिखाते हैं। हम बिना सीखे ही ऐसा
भाग के दिखा दें कि खरगोश तक खड़ा-खड़ा पछताता रहे। तो भैया, गाली-वाली
उन्होंने बहुत दी, पर हमें वे पकड़ नहीं पाए। किसी तरह से मैं घर आ पहुँचा।
दुरबीनसिंह के दिन तब तक गिर गए थे। पुलिस भी भीतर-ही-भीतर उनके खिलाफ़ रहने
लगी थी। दूसरे दिन हमारा मन बहुत कुलबुलाया, पर हमने यह बात उनसे कही नहीं।
कह देते तो दुरबीन काका उसी की ठेस में टें बोल जाते।"
रुप्पन बाबू दुखी चेहरे को वजनी झोले की तरह लटकाए बैठे थे। साँस खींचकर
बोले, “अच्छा ही होता। तव टें हो जाते तो भतीजे के हाथ से तो न मरते।"
|
|||||


 i
i