|
नारी विमर्श >> कृष्णकली कृष्णकलीशिवानी
|
16660 पाठक हैं |
|||||||
हिन्दी साहित्य जगत् की सशक्त एवं लोकप्रिय कथाकार शिवानी का अद्वितीय उपन्यास
बाईस
"हम भी बड़ी लम्बी यात्रा पर निकली
हैं।" वह कली के बिना कुछ पूछे ही
कहने लगी, “पहले रामेश्वरम्, फिर
तिरुवल्ली, काँची, मदुराई और वापस
दिल्ली। बस, इस ओर की यात्रा में
कुल्हड़ की चाय के लिए तरस कर रह जाती
हूँ। बड़ा बुरा अभ्यास है चाय का।
सुबह उठते ही गला सूख जाता है। तुमने
तो रात भी कुछ नहीं खाया, भूख लग आयी
होगी। रुको, थोड़ा प्रसाद धरा है।"
आधुनिका सन्तनी ने अपना चौकोर बटुआ
खोलकर एक रेशमी थैली निकाली और
डोरियाँ खींचकर थैली का खुला मुँह कली
की ओर कर दिया। "मुझे तो इतनी सुबह कुछ खाने का अभ्यास ही नहीं है, फिर ब्रश भी नहीं किया," कली ने संकुचित स्वर में कहा।
"तो क्या हो गया बेटी ! यह तो बालगोपाल का भोग है। गंगाजल को घुटकने से पहले क्या कोई साधारण जल से कुल्ला करता है ? पगली, ले खा। मुँह में धरते ही मंजन-वंजन सब आप ही हो जाएगा।" वह बड़ी आत्मीयता से 'तुम' छोड़ 'तू'
पर उतर आयी थी।
"ले ना, ठाकुर भोग के लिए नाहीं नहीं करते।" खुली थैली में छिले बादाम, काजू और पिश्ते देख दो दिन पूर्व की स्मृति कली के कण्ठ में गह्वर बनकर अटक गयी।
"काबुली वाले, देखू तुम्हारी झोली में क्या है ?" थैली में निर्जीव मेवों पर धस कली का हाथ काँप उठा।
"क्या नाम है बेटी तुम्हारा ?"
कली को संकोच से एक ही काजू निकालते देख सन्तनी ने मुट्ठी-भर मेवे निकालकर उसकी गोदी में धर दिये।
"कृष्णकली।"
इस बार मेवों पर पड़ा दूसरा हाथ काँप गया। वह कली के चेहरे पर टकटकी बाँधकर ऐसे देखने लगी जैसे निर्ममता से चिथड़े-चिथड़े कर फाड़ दी गयी किसी अमूल्य चिट्ठी के टुकड़ों को जोड़-जोड़कर पढ़ रही हो। अस्पष्ट धूमिल स्याही अचानक स्पष्ट होकर निखर आयी, अर्थहीन, लुंजपुंज अक्षरों की लिखावट की पंक्ति साकार होकर कानों में गूंजने लगी-
कृष्णकली आमी तारेई बोली-
कालो तारे बोले गायेरलोक
'कृष्णकली' 'कृष्णकली' वह होंठों ही में बड़बड़ाती कली को उसी रिक्त दृष्टि से देख रही थी, "तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटी ?" वह डरती-डरती ऐसे पूछ रही थी जैसे अप्रिय उत्तर उसे पहले ही मिल गया हो।
"कृष्णकली मजूमदार।"
यल से की गयी तारुण्य की कलई देखते-ही-देखते उतर गयी। चेहरा सिकुड़कर विषाद की झुर्रियों से भर गया। होंठ काटकर रोकने पर भी, नीचे को बह गये। होंठों से दबी सिसकी फिसलकर निकल गयी।
दोनों लम्बे हाथ फैलाकर उसने कली को छाती से लगा लिया।
आश्चर्य से स्तब्ध कली अनजान कठोर वक्षस्थल से लगकर भी तनकर काठ ही बनी रही, उस स्नेहपूर्ण आकस्मिक आलिंगन का सामान्य भद्रतापूर्ण प्रत्युत्तर भी नहीं दे पायी। कैसी सनकी थी यह सन्तनी ! न जान, न पहचान और लगी छाती से लगाकर रोने जैसे बरसों पहले खो गयी सगी बिटिया को किसी गोदने या तावीज़ का सूत्र पकड़कर पहचान लिया हो ! महानाटकीय सिसकियों से कली सहसा झुंझला उठी
और उसी झुंझलाहट के बीच एक शंकाशूल ने उसे तड़पाकर रख दिया। अपने कन्धे पर टिकी लम्बी अँगुलियों को उसने बड़ी नम्रता से नीचे उतारते-उतारते गौर से देख लिया। नहीं, उसकी धारणा निर्मूल निकली। वे अँगुलियाँ रोगमुक्त होने पर भी क्या
वैसी हो सकती थीं। एक पल को उसने उस जोड़े को अपने ही बिछुड़े माँ-बाप का जोड़ा समझ लिया था, पर अंगुलियाँ मिल भी जाती तो उसकी अभागी जननी को आँखें कौन देता ? अपने को सन्तनी के बाहुपाश से मुक्त कर कली पीछे हो गयी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






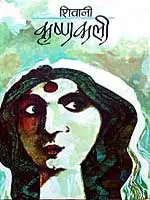

_s.jpg)

