|
नारी विमर्श >> कृष्णकली कृष्णकलीशिवानी
|
16660 पाठक हैं |
|||||||
हिन्दी साहित्य जगत् की सशक्त एवं लोकप्रिय कथाकार शिवानी का अद्वितीय उपन्यास
पर कली के जग जाने का ऐसा क्या भय ! ओह,
अब समझ में आया। कली ने करवट बदलकर हँसी
रोक ली। स्वामीजी ने कटोरदान से दो उबले
अण्डे निकालकर मुख में धर लिये थे और
फिर दूसरे कटोरदान में किसी
प्रागैतिहासिक युग के-से जीव का विराट्
हड्डा निकालकर चिंचोड़ने लगे थे। सचमुच
ही तो संगिनी का सहमना उचित था ! सिर पर
जटाजूट, ठुड्डी पर लम्बी दाढ़ी, गैरिक
वसन, कण्ठ में रुद्राक्ष की माला,
सिरहाने कमण्डलु और अण्डो-हड्डियों का
फलाहार ! देखनेवाला भी आखिर क्या कहेगा
! पर खानेवाले को किसी की चिन्ता नहीं
थी। करवट बदलने पर भी कली बड़ी देर तक
उनके सुदीर्घ भोजन की कचर-कचर सुनती रही
थी। फिर उसने स्वामीजी के गटागट घुटके
गये किसी रहस्यमय पेय की गटगट का ध्वनि
संगीत भी सुना।
"क्यों जी, पीली पत्तियों वाला ज़र्दा
नहीं लायी क्या ?' उनका झुंझलाया स्वर
ही उनके क्रोधी असंयमी स्वभाव का स्वयं
परिचय दे गया।
शान्त सहचरी से निश्चय ही भूल हो गयी
थी। वह बड़ी देर तक नम्र स्वर में क्षमा
माँगती जा रही थी, पर उनकी बिड़बिड़
बन्द नहीं हुई—“क्यों खायें हम तुम्हारा
काला तम्बाकू, जानती हो कि हमें
तुम्हारा वह काला बारूद एकदम नापसन्द
है। अपनी चीज़ रखना तो नहीं भूलीं,
हमारी चीज़ भूल गयीं। अब किसी स्टेशन पर
उतरकर हमें किसी पान वाले से खरीदकर ला
देना। बिना पीली पत्ती के हमें नींद
नहीं आती।" फिर शायद किसी उदार पानवाले
ने उनकी खुराक जुटा दी थी क्योंकि तड़के
ही कली की नींद टूटी तो स्वामीजी
खर्राटे ले रहे थे, खर्राटे भी ऐसे कि
आरोह से अवरोह तगड़ा।
पौ नहीं फटी थी। कली खिड़की खोलकर बैठ
गयी। भागते वृक्ष और खेत-खलिहानों के
बीच रेल की खुली खिड़की से उसे ऐसे ही
अस्पष्ट लुकाछिपी खेलते म्लान सूर्य की
किरणों को ढूँढ़ने में बड़ा आनन्द आता
था। दूर-दूर तक फैले ताड़ के पेड़ों का
झुरमुट और झोंपड़ियों का क्षण-क्षण
बदलता शिल्प आँखें बाँध रहा था। कैसा
विचित्र था भारत ! प्रत्येक दिशा के
शिल्प में बहुरूपी शिल्पी की विभिन्न
शैली—उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो
शायद वह शिल्पी पेस्टल रंगों से बनाकर
चित्र प्रस्तुत करता। उस प्रातःकालीन
सूर्य की रक्ताभ किरणों के, सरसों के
पीताभ पुष्पों से संगम में रंग भरने के
लिए रंगभीनी तूलिका से ही काम नहीं
चलता। पल-पल में रंग बदलते सरसों के
खेत, हवा में झूमती गेहूँ की बालियाँ,
तराई के संगम से हाथ हिला-हिलाकर विदा
लेती कुमाऊँ की दुर्गम पर्वत श्रेणियाँ,
नहरों का क्षीण कलेवर, जैसा ही बहुरंगी
वैभव वैसा ही मेल खाता प्रकृतिदत्त
अनुपम पेस्टल रंग ! पर एक ही बात थी।
उत्तर प्रदेश की यात्रा होती तो वह क्या
इतने तड़के ऐसे खिड़की खोलकर देख पाती ?
क़तार की क़तार में लोटा लेकर बैठी
निर्लज्ज गँवारू भीड़ प्रकृति के उस
सुरम्य चित्र में कोलतार पोतकर रख देती।
लगता था ससुरे रेलवे टाइम टेबल देखकर ही
लोटा लेकर जम गये हैं। जितनी बार वह
मन्दस्मिता उषा का स्वागत करने ट्रेन की
खिड़की खोलकर मुँह बाहर निकालती, उतनी
ही बार मीलों तक फैली लोटाधारी निर्लज्ज
पंगत करारा थप्पड़ मारकर उसका मुँह
खिड़की के भीतर कर देती। कभी-कभी बचकाने
क्रोध से वह बौखला जाती। पर इस ओर के
ग्रामवासियों में शायद ऐसी कुव्यवस्था
नहीं थी, अचानक कली को उन्हीं प्रातः
स्मरणीय लोटाधारी ग्रामीणों की निर्लज्ज
मुद्रा की स्मृति गुदगुदा गयी। वह हँसने
लगी।
"क्यों हँस रही हो बेटी ?" मीठी आवाज़
से चौंककर कली मुड़ गयी। वही हँसमुख
सन्तनी उसकी सीट पर आकर बैठ गयी थी।
कली खिसिया गयी, जिस बात को याद कर उसे
हँसी आयी थी वह क्या बतलाने की थी ?
उसने कुछ नहीं कहा।
"कहाँ तक जा रही हो ?" मुखरा वैरागिनी
ने चट से दूसरा प्रश्न पूछ दिया।
"अभी तो धनुषकोटि जा रही हूँ, वैसे
जाऊँगी सीलोन।''
"अरे बड़ी दूर जा रही हो और वह भी
अकेली..."
“मुझे वहाँ नौकरी मिल गयी है।" कली ने
उतनी दूर जाने की कैफियत-सी दी।
"अच्छा, नौकरी करती हो ! हमने तो सोचा
कि किसी फ़िल्म कम्पनी में काम करती
होगी।"
"क्यों, क्या वैसी ही लगती हूँ मैं ?"
कली ने हँसकर पूछा।
"हाँ, एकदम चेहरा-मोहरा तो हमें याद
रहता है पर नाम याद नहीं रहता। कुछ दिन
पहले एक फ़िल्म देखी थी—'बालिका बधू।'
जाने उस लड़की का नाम क्या था, पर सूरत
एकदम तुम्हारी थी बेटी।"
कली ने देखा, वैरागिनी के वेश होने पर
भी उन बड़ी-बड़ी आँखों में विलास की
स्पष्ट छाया थी, वैराग्य की नहीं। आई
ब्रो पेन्सिल से सँवरी चपल मुखरा दृष्टि
की नुकीली भंगिमा मौलिक नहीं थी। गेरुआ
कमीज़ के भीतर पहना गया नन्हा परिधान भी
कली की अनुसन्धानी दृष्टि से बच नहीं
सका। सुघड़ बैसाखियों पर टिका यौवन कली
को छल नहीं सकता था। चाँदी की अंगूठी
में पहना गया बड़ा-सा प्रवाल सम्भवतः
किसी दुष्ट ग्रह की शान्ति के लिए ही
चाँदी में मढ़ा गया था क्योंकि उसी कलाई
में बँधी गोल घड़ी की सुवर्ण चोटी-सी
गुंथी मोटी चेन कम-से-कम तीन तोले की
थी। क्या उस वैरागिनी के लिए भी समय की
उपादेयता थी ?
|
|||||


 i
i 






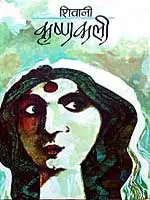

_s.jpg)

