|
नारी विमर्श >> कृष्णकली कृष्णकलीशिवानी
|
16660 पाठक हैं |
|||||||
हिन्दी साहित्य जगत् की सशक्त एवं लोकप्रिय कथाकार शिवानी का अद्वितीय उपन्यास
ऐसी ही पहली डुबकी दी थी स्वयं उसकी
जन्मदायिनी जननी ने, जब उसका नन्हा गला
घोटकर उसे एक अनजानी गोदी में पटक दिया
था। दूसरी डुबकी खिलायी थी नियति ने जब
पीली कोठी, बडी माँ, वाणी मौसी और
काकातआ का पिंजरा सब हाथ हिलाकर एक साथ
किसी धुंधले परदे के पीछे छिप गये थे.
तीसरी डबकी उसने स्वयं ली थी इस महानगरी
में, जहाँ न फिर अम्मा उसे ढूँढ़ पायी
थी, न रोज़ी आण्टी! पर इस डुबकी को किसी
पेशेवर गोताखोर के चातुर्य से ही लेना
होगा, जिससे ऊपर उठते बुलबुले देखकर
गहरे जल के अतल-तल में डूब गयी उसकी
सुकुमार देह के लिए सब मातम मना लें। न
अब इसे इलाहाबाद जाना होगा, न
पाण्डिचेरी। चंचल मन में उठ रही
तर्क-वितर्क की आँधी को उसने अपने
अविवेक के वातायन द्वार को यल से मूंदकर
बाहर ठेल दिया। अब वह भारत नहीं लौटेगी।
गाड़ी चलने लगी तो
पल-भर को जी न जाने कैसा हुआ। कुछ देर
तक वह जगमगाती रोशनियों के उस विराट
कार्निवल से शहर को देखती रही। फिर उसने
खिड़की बन्द कर दी। अचानक उसकी दृष्टि
ऊपर और नीचे के बर्थ पर सिर से पैर तक
एक-सी नारंगी चादर ओढ़े जोड़े पर पड़ी।
ऊपर के बर्थ पर सो रहे व्यक्ति के
सिरहाने एक काला कमण्डलु धरा था और खूटी
पर लटकी एक लम्बी सुपारी के-से दानों की
रुद्राक्ष की माला रेल के
साथ झटकती ताल-सी दे रही थी। चादर का
रंग भी नारंगी नहीं, गेरुआ था। इतना
लम्बा सफ़र और साथ में साधुओं का यह
एरिस्टोक्रैटिक जोड़ा !
फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे उस मुरदा
बने सिर-मुँह ढाँप-दूंपकर सोनेवाले
सहयात्रियों की रहस्यमय उपस्थिति से कली
सहमी हो, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी
सहमनेवाली लड़की वह नहीं थी, बल्कि देखा
जाये तो उसी की उपस्थिति आज तक ऐसे
बीसियों निद्रामग्न यात्रियों को सहमा
चुकी थी। इतने बड़े स्टेशन में गाड़ी
रुकी, फिर भी दोनों क्या चरस की दम
लगाकर सो रहे थे ? ऊपर के सो रहे यात्री
का गोरा अँगूठा उसे एक बार दिखा और वह
समझ गयी कि यह कोई विदेशी नया-नया
दीक्षित स्वामी है। चलो अच्छा ही हुआ,
चें-चें-पें-पें करते बच्चोंवाला कोई
परिवार साथ चलता या कोई नव-विवाहिता
जोड़ा ही सहयात्री बन गया होता तो वह
बौखला जाती। जैसा उखड़ा मूड लेकर वह
कलकत्ता छोड़ रही थी, उसके लिए ऐसा
साहचर्य ही उसे शोभा देता था। अगल-बगल
में सो रहे उन लम्बतडंग खबीस-से साधुओं
के जोड़े को देख उसे किसी भी संशय ने
सशंकित नहीं किया। वह तकिया ठीक से
लगाकर सोने ही जा रही थी कि ऊपर बर्थ पर
पड़ी चादर हिली और पलक झपकाते ही वह
व्यक्ति नीचे उतर गया। लग रहा था कि
नीचे उतरने में उसे विशेष प्रयत्न नहीं
करना पड़ा। शायद उसकी भयावह रूप से
लम्बी टाँगें उसके बैठते ही स्वयं ज़मीन
को छू गयी थीं। धुंधले नीले बल्ब की
रोशनी में उसके फिक्सो से सँवारे गये
जटाजूट को कली ने कनखियों से देख लिया।
गोरे चेहरे पर यत्न से छंटी सँवरी दाढ़ी
और चिकनी मूंछे रामलीला के बनवासी
रामचन्द्रजी की ही-सी नकली
दाढ़ी-मूंछों-सी बनावटी लग रही थीं।
उसने एक बार उडती दष्टि से कली की ओर
देखा. फिर नीचे सो रहे अपने साथी का
कन्धा पकडकर हिलाने लगा।
"खाना निकालो जी, बड़ी भूख लगी है।"
नींद का बहाना बनाये, आँखों तक चादर की
यवनिका को सुविधानुसार उठाती-गिराती कली
चुपचाप पड़ी उस राजसी सन्त-समागम का
आनन्द ले रही थी। दूसरी चादर का आवरण
हटा और कली ने देखा कि जगकर बैठनेवाली
सन्त नहीं सन्तनी थी। ऊपर की बर्थ से
नीचे उतर उसे जगानेवाला गैरिकवसनधारी
स्वामी उसके पास बैठ गया और धीमे स्वर
में फुसफुसाने लगा। कभी-कभी रात्रि की
निस्तब्धता में ऐसी फुसफुसाहट
नगाड़े-दमाड़े की चोट से भी अधिक स्पष्ट
होकर कानों में बजने लगती है।
"कौन है यह ? कहाँ से चढ़ी ?" पुरुष के
कण्ठ ने पूछा।
"पता नहीं, मैं तो सो गयी थी। लगता है,
सियालदह से ही बैठी है, तुम हाथ-मुँह धो
लो, मैं खाना लगाती हूँ।"
वह उठी और कली ने फिर पतली चादर के
ताने-बाने के औदार्य से देखा कि
उठनेवाली भी अपने गैरिकधारी साथी की
भाँति कद्दावर, ऊँची, हृष्ट-पुष्ट महिला
है। रंग साँवला होने पर भी बनावट अनुपम
थी। गेरुए रंग की चुस्त सलवार और किसी
साईं बाबा के-से ढीले कुरते में छिपी
स्वामिनी की कलात्मक रुचि को कली की
मॉडल की दृष्टि ने पल-भर में भाँप लिया।
उस संन्यासिनी ने अपने डल ड्रेस को जैसा
स्मार्ट बनाकर पहन लिया था, उसे शायद
विदेश के किसी मॉडलिंग स्कूल की छात्रा
भी वैसी लुभावनी सज्जा में नहीं साध
सकती। शरीर की कृशता स्वाभाविक नहीं थी।
इसमें कोई सन्देह नहीं था कि पोलो की
कृशता की भाँति वह चाबुक से साधकर बनायी
गयी थी। चेहरे की वयस चालीस से ऊपर,
बड़े-बड़े चप्पल खंजन नयनों की बीस के
आस-पास और कसी कमीज़ में यत्न से कसकर
घटायी गयी कृशता की वयस देखनेवालों को
अनायास ही अपने वर्ष के कैशोर्य की
मरीचिका में बाँध सकती थी। स्टील का
कटोरदान खोलकर वह बड़े धैर्य से बार-बार
सामने की बर्थ पर पतली चादर से मुँह
ढाँपकर पड़ी कली की ओर सहमकर देखती
कटोरदान के डिब्बे को साथी के सामने
सजाती जा रही थी। उसके हाथ से डिब्बे एक
प्रकार से अधैर्य से छीनने को तत्पर
उसका बुभुक्षित साथी इधर-उधर देखे बिना
किसी भुखमरे कँगले भिक्षुक की भाँति
कचर-कचर खाये जा रहा था। बीच-बीच में
उसकी गम्भीर संगिनी उसे कटोरदान का
जलतरंग बजाने पर या गिलास लुढ़का देने
पर धीमे स्वर में टोकती भी जा रही
थी—“शोर मत करो प्लीज़, कहीं वह जग न
जाये !''
|
|||||


 i
i 






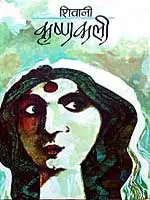

_s.jpg)

