|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
नदी जो मरुस्थल में खो गई
मेरा यह मत रहा है कि किसी प्रियजन के संस्मरण सँजोने हों तो उसके जीवनकाल में
ही यह कार्य करना चाहिए, किन्तु हममें से कितनों की दुःसाहसी लेखनी, ऐसा कर
पाती है? कहीं उस व्यक्ति की किसी दुर्बलता का उल्लेख उसे रुष्ट न कर दे, कहीं
वह कुछ का कुछ अर्थ न लगा बैठे। मैं स्वयं कई बार इस प्रयोग के गर्म दूध की आँच
से झुलस चुकी हूँ। इसी से अब वास्तविकता का मठा भी फूंक-फूंककर पीती हूँ। मेरी
इसी लेखनी ने न जाने कितने आत्मीय स्वजनों से, मुझे विलग किया है।
मैं ‘जो कुछ कहूँगी, सच कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी,' यह कहना तो बहुत सरल है, किन्तु लिखना उतना ही कठिन। सत्य की कड़वी औषधि में कभी-कभी काल्पनिक शहद भी मिलाना पड़ता है, वह मैं आज तक न कर पाई, न कभी कर पाऊँगी। शायद, यही कारण है कि इष्ट मित्रों की शाप-वृष्टि से सदा त्रस्त ही रही। मायके के लौहर्गल युक्त कपाट तक मेरे लिए सदा के लिए मुंद गए, फिर भी यह मुँहफट लेखनी, किसी अल्ट्रासाउंड की प्रखरता से एकदम अन्दर छिपी व्याधि का अवकिल चित्र उतारकर रख देती है। इतना अवश्य जान गई हूँ कि अपनों ही पर, कलम की गुलेल साधना, सहज नहीं होता। आज, जब बन्धु-बान्धवी, सहपाठी, समवयसी आत्मीयों में से अधिकांश, इहलोक के बन्धन काट, ऊपर जा चुके हैं, स्मृति दंश कभी-कभी दुर्वह हो उठता है।
जहाँ बैठकर लिख रही हूँ, वहाँ पिछवाड़े की सँकरी गली से, प्रायः ही महाप्रस्थान के यात्री, चार कन्धों पर हुलसते जाते हैं। पिपराघाट के श्मशान को, यही सड़क जाती है। अभी-अभी एक भाग्यवान गुजरा है 'राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है।' यह सत्य किसी को झकझोर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता-मन अचानक अशान्त हो गया। सामने गुलमोहर का लाल-लाल फूलों से लदा वृक्ष, कामोन्मत्त वृषभ-सा मस्ता रहा है। आषाढ़ आधा बीत गया है, बाहर सामान्य वर्षा ने तप्त धरणी की प्यास ऐसी बढ़ा दी है कि धरित्री, निधूम, अग्निकुंड बनी, आग फंक रही है-मुझे, इस वर्षासिक्त धरणी की सौंधी महक, आज अनायास ही उस चेहरे की स्मृति में आकंठ डुबो रही है जिसके पास बैठकर, कभी मेघदूत पढ़ा था-
मैं ‘जो कुछ कहूँगी, सच कहूँगी। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी,' यह कहना तो बहुत सरल है, किन्तु लिखना उतना ही कठिन। सत्य की कड़वी औषधि में कभी-कभी काल्पनिक शहद भी मिलाना पड़ता है, वह मैं आज तक न कर पाई, न कभी कर पाऊँगी। शायद, यही कारण है कि इष्ट मित्रों की शाप-वृष्टि से सदा त्रस्त ही रही। मायके के लौहर्गल युक्त कपाट तक मेरे लिए सदा के लिए मुंद गए, फिर भी यह मुँहफट लेखनी, किसी अल्ट्रासाउंड की प्रखरता से एकदम अन्दर छिपी व्याधि का अवकिल चित्र उतारकर रख देती है। इतना अवश्य जान गई हूँ कि अपनों ही पर, कलम की गुलेल साधना, सहज नहीं होता। आज, जब बन्धु-बान्धवी, सहपाठी, समवयसी आत्मीयों में से अधिकांश, इहलोक के बन्धन काट, ऊपर जा चुके हैं, स्मृति दंश कभी-कभी दुर्वह हो उठता है।
जहाँ बैठकर लिख रही हूँ, वहाँ पिछवाड़े की सँकरी गली से, प्रायः ही महाप्रस्थान के यात्री, चार कन्धों पर हुलसते जाते हैं। पिपराघाट के श्मशान को, यही सड़क जाती है। अभी-अभी एक भाग्यवान गुजरा है 'राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है।' यह सत्य किसी को झकझोर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता-मन अचानक अशान्त हो गया। सामने गुलमोहर का लाल-लाल फूलों से लदा वृक्ष, कामोन्मत्त वृषभ-सा मस्ता रहा है। आषाढ़ आधा बीत गया है, बाहर सामान्य वर्षा ने तप्त धरणी की प्यास ऐसी बढ़ा दी है कि धरित्री, निधूम, अग्निकुंड बनी, आग फंक रही है-मुझे, इस वर्षासिक्त धरणी की सौंधी महक, आज अनायास ही उस चेहरे की स्मृति में आकंठ डुबो रही है जिसके पास बैठकर, कभी मेघदूत पढ़ा था-
धूम्रज्योतिः सलिलमरुता सन्निपातः क्व मेघः।
हम सात बहनों में वयः ज्येष्ठा थी जयन्ती। इस वर्ष उसकी बीमारी का समाचार सुन
उससे मिलने गई तो वर्षों पूर्व उन्हीं से पढ़े शिवपुराण की चेतावनी स्मरण कर
आँखें भर आईं। आँखों में जमकर ठहर गया पानी, कानों की पलट गई लोड़ियाँ, किंचित
तिर्यक् बनी नासिका। समझ गई कि 'दिवस का अवसान समीप था'।
कहाँ गई वह भरी-भरी देह, वह पीतवर्णी आभा, तेजोदृप्त कंठस्वर? मुझे बाँहों में भर, वह रोने लगी, वह जिसे मैंने कभी किसी के सामने रोते नहीं देखा था। शायद, वह जान गई थी, कि यह दोनों बहनों का अंतिम आलिंगन है, विच्छेद की भूमिका। मेरे क्षुब्ध चित्त में, विक्षोभ का तूफ़ान उठ रहा था। अपराधी चित्त, बार-बार पानी में भीगे चाबुकी अदृश्य मार से, मुझे आहत कर रहा था। न जाने कितनी बार, मैंने उसके हृदय को दुखाया है, छात्र जीवन में अपनी अबाध्यता से उसे विचलित किया है। और आज तक, कभी क्षमा भी नहीं माँग पाई। आज आई हूँ, जब दीपशिखा बुझ चुकी है, केवल क्षीण अवसन्न धूम्ररेखा प्राणों का संकेत बनी रह गई है। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, वह अब, अपने को संयत कर चुकी थी, खिसियाए स्वर में बोली, “पता नहीं क्यों, आजकल ऐसा ही गह्वर आ जाता है, कैसी है तू?' एक हाथ मेरी पीठ पर था, दूसरा शिथिल लता-सा, पलंग के नीचे झूल रहा था-हाथ का कंकण, न जाने कब बाँहों का अनन्त बन गया था-
मोतियाबिन्द से लगभग दृष्टिहीन आँखें, जितनी ही बार, मुझे निकट से देखने की चेष्टा कर रही थीं, उतनी ही बार यत्न से रोकी गई रुलाई मेरा कंठ अवरुद्ध कर रही थी। फिर उसने एक दीर्घ निश्वास लेकर दोनों हाथ अपनी छाती पर धर, आँखें मूंद लीं। पहले भी जब कभी वह ऐसी ध्यानस्थ हो जाती, तो उसका मुख-मंडल एक दैवी तेज से दीप्त हो उठता था। लगता था साक्षात् वाग्देवी ही आविर्भूत हो गई हैं। उसका वैदुष्य ज्ञान अगाध था। कभी बनारस विश्वविद्यालय ने, उसे साहित्य मनीषिणी की उपाधि से विभूषित किया था, जीवन में तब ही उसकी प्रतिभा का उचित मूल्यांकन हुआ था। बचपन से ही, पितामह के साथ रह संस्कृत की घुट्टी पी, अनेक भाषाएँ सीखीं-गुजराती, बाँग्ला, मराठी, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत-प्राकृत, पाली। शान्तिनिकेतन में चीनी भाषा सिखाने प्रो. तान जैसे स्नेही गुरु मिले। संस्कृत तो जैसे उसकी मातृभाषा थी। हिन्दी-अंग्रेज़ी लिखती तो मोती से अक्षर, साँचे में ढले निकलते। वृद्धावस्था में वे ही मोती बिखर गए, टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखे उसके पत्र पढ़ती तो कलेजा कसमसा उठता। आँखों से ठीक से दिखता नहीं था, पढ़ने ही में उसके प्राण बसते थे, वही छूट गया। कहानी लिखना न छोड़ा होता तो आज हिन्दी की शीर्षस्थ लेखिका होती, जैसे ही भाषा वैसे ही भाव। पता नहीं क्यों स्वयं ही इस विधा से उदासीन हो गई। 'चाँद', में 'हंस' में कई कहानियाँ छपी-'शराबी, 'ठाकर की रोमा।' एक कहानी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी आई, किन्तु न जाने क्यों, उसने स्वेच्छा से ही लिखना छोड़ दिया। पत्रों का, उसके पास अमूल्य संकलन था, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, रवीन्द्रनाथ, नन्दलाल बोस, एलिस बोर्नर, आचार्य कृपलानी, मालवीयजी, बलराज साहनी। काश, उसकी मृत्यु से पूर्व मैंने उसकी वह अमूल्य निधि बटोर ली होती। हजारीप्रसादजी के तो न जाने कितने पत्र थे उसके पास गुरुदेव के बनाए चित्र, जिनके लिए पहाड़ी रंगों को, जयन्ती ने स्वयं अमर-कोश के वनौषधि पर्व से पढ़ जंगली फूलों को ढूँढ-ढूँढ़कर तैयार किया था। गत वर्ष 'देश' पत्रिका में प्रकाशित रवीन्द्रनाथ के एक पत्र में उनकी अपनी प्रिय छात्रा जयन्ती का उल्लेख था कि कैसे उसने हरिद्रा, खदिर, पलाश, बुरुश से अभिनव रंग बनाए थे। मैंने, तत्काल काटकर, कटिंग जयन्ती को भेज दी। जब मिली तो मैंने पूछा-'कटिंग मिली?'
'हाँ, मिली तो थी, मैंने सिरहाने रख दी थी कि फुर्सत से पढूंगी-पता नहीं कहाँ चली गई-क्या लिखा था?'
उसका सिरहाना भानुमती का पिटारा था। दाडिम, अखरोट के दाने, खाँड के खिलौने, पुड़ियों में रखे पहाड़ी मसालों-जम्बू ‘गभैणी' कस्तूरी के बीड़े। हमारे बचपन की तस्वीरें, दिवंगत जीजाजी का रूमाल। उस बहुरंगी भीड़ में भला रवीन्द्रनाथ के पत्र की क्या बिसात?
अपनी प्रतिभा का मूल्य जयन्ती स्वयं कभी नहीं आँक पाई। उसे तो आँका था गुरुदेव ने, आश्रम के गुरुजनों ने, हजारीप्रसादजी ने, जो कहते थे 'कभी मेरी क़लम की उत्तराधिकारी जयन्ती ही होगी।' गुरुदेव ने उसका नाम रखा था 'भारत माता'। आश्रम में उसकी खिल्ली उड़ाई जाती। खद्दर की मोटी-मोटी साड़ियाँ बाँधती हैं, वह भी कितनी ऊँची। सिर ढाँपती है, नीचे आँखें किए चलती है, किसी से अनावश्यक बात नहीं करती-गुरुदेव के अनन्य स्नेह ने ही, उन्हें अहंकारी बना दिया है, आदि-आदि, किन्तु बात ऐसी नहीं थी। अहंकार से तो वह कोसों दूर थी-यद्यपि अहंकार करने को उसके पास बहुत कुछ था। रंग हम सबसे दबा होने पर भी यौवनावस्था में उसका आकर्षक व्यक्तित्व कैसा था, यह वही बता सकते हैं, जिन्होंने उसे तब देखा है।
इन्टर किया ही था कि दनादन रिश्ते आने लगे, किन्तु वह बहुत पहले ही आजन्म कुँआरी रहने की घोषणा कर चुकी थी। उसकी जिद को सब जानते थे, फिर भी माँ ने लाख समझाया, 'देख, ऐसे रिश्ते बार-बार नहीं आते, इतना अच्छा घर-वर, फिर कहाँ मिलेगा-तू अट्ठारह की हो गई है, तेरी बड़ी बहन तो चौदह वर्ष में ही माँ बन गई थी-लड़का आई.सी.एस. की परीक्षा देने विलायत गया है...।' पर जयन्ती का मुँह से छूटा 'नहीं' ब्रह्म वाक्य था।
उधर उसके एक प्रशंसक जिन्हें लॉर्ड कहा जाता था, हमारे गृह की निरन्तर परिक्रमा किए जा रहे थे। एक दिन, हम गरमी की छुट्टियों में घर आए तो देखा, बढ़िया ट्वीड का ओवरकोट पहने, मुँह में सिगार लगाए, लार्ड सीटी में कोई अंग्रेज़ी धुन, गुनगुना रहा था। उसके दुःसाहस से जयन्ती के तनबदन में आग लग गई। कहने लगी, 'देख तू मेरा एक काम करेगी, तो पाँच रुपये दूंगी-' उन दिनों उत्कोच की वह राशि पर्याप्त थी- 'कहो।'
-देख, कल जब यह पट्ठा, खड़ा होकर सीटी बजाए, तो दीवार पर चढ़ तू इस बुलबुलिया के, इन ब्रिलैंटीन की जुल्फ़ों पर पिच्च से थूककर कहना-‘जा भाग, मेरी बहन ने कहा है, वह तुझसे कभी शादी नहीं करेगी...'
दूसरे दिन सन्ध्या प्रगाढ़ होते ही कृष्ण की बंकिम मुद्रा में खड़ा लॉर्ड सीटी बजाने लगा। मैं दीवार पर बैठी बड़ी देर से, थूक का गोला बना रही थी। मुझे देख, भावी साली के रूप में उसने बड़े मोहक स्मित से मेरा स्वागत किया। बड़ी देर से मुख में संचित थूक प्रक्षेपण में, मैंने फिर विलम्ब नहीं किया। मेरा अचूक निशाना पलभर में, उन यन्त्र से सँवरी जुल्फों का सन्तुलन विकृत कर बैठा।
कहाँ गई वह भरी-भरी देह, वह पीतवर्णी आभा, तेजोदृप्त कंठस्वर? मुझे बाँहों में भर, वह रोने लगी, वह जिसे मैंने कभी किसी के सामने रोते नहीं देखा था। शायद, वह जान गई थी, कि यह दोनों बहनों का अंतिम आलिंगन है, विच्छेद की भूमिका। मेरे क्षुब्ध चित्त में, विक्षोभ का तूफ़ान उठ रहा था। अपराधी चित्त, बार-बार पानी में भीगे चाबुकी अदृश्य मार से, मुझे आहत कर रहा था। न जाने कितनी बार, मैंने उसके हृदय को दुखाया है, छात्र जीवन में अपनी अबाध्यता से उसे विचलित किया है। और आज तक, कभी क्षमा भी नहीं माँग पाई। आज आई हूँ, जब दीपशिखा बुझ चुकी है, केवल क्षीण अवसन्न धूम्ररेखा प्राणों का संकेत बनी रह गई है। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, वह अब, अपने को संयत कर चुकी थी, खिसियाए स्वर में बोली, “पता नहीं क्यों, आजकल ऐसा ही गह्वर आ जाता है, कैसी है तू?' एक हाथ मेरी पीठ पर था, दूसरा शिथिल लता-सा, पलंग के नीचे झूल रहा था-हाथ का कंकण, न जाने कब बाँहों का अनन्त बन गया था-
मोतियाबिन्द से लगभग दृष्टिहीन आँखें, जितनी ही बार, मुझे निकट से देखने की चेष्टा कर रही थीं, उतनी ही बार यत्न से रोकी गई रुलाई मेरा कंठ अवरुद्ध कर रही थी। फिर उसने एक दीर्घ निश्वास लेकर दोनों हाथ अपनी छाती पर धर, आँखें मूंद लीं। पहले भी जब कभी वह ऐसी ध्यानस्थ हो जाती, तो उसका मुख-मंडल एक दैवी तेज से दीप्त हो उठता था। लगता था साक्षात् वाग्देवी ही आविर्भूत हो गई हैं। उसका वैदुष्य ज्ञान अगाध था। कभी बनारस विश्वविद्यालय ने, उसे साहित्य मनीषिणी की उपाधि से विभूषित किया था, जीवन में तब ही उसकी प्रतिभा का उचित मूल्यांकन हुआ था। बचपन से ही, पितामह के साथ रह संस्कृत की घुट्टी पी, अनेक भाषाएँ सीखीं-गुजराती, बाँग्ला, मराठी, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत-प्राकृत, पाली। शान्तिनिकेतन में चीनी भाषा सिखाने प्रो. तान जैसे स्नेही गुरु मिले। संस्कृत तो जैसे उसकी मातृभाषा थी। हिन्दी-अंग्रेज़ी लिखती तो मोती से अक्षर, साँचे में ढले निकलते। वृद्धावस्था में वे ही मोती बिखर गए, टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखे उसके पत्र पढ़ती तो कलेजा कसमसा उठता। आँखों से ठीक से दिखता नहीं था, पढ़ने ही में उसके प्राण बसते थे, वही छूट गया। कहानी लिखना न छोड़ा होता तो आज हिन्दी की शीर्षस्थ लेखिका होती, जैसे ही भाषा वैसे ही भाव। पता नहीं क्यों स्वयं ही इस विधा से उदासीन हो गई। 'चाँद', में 'हंस' में कई कहानियाँ छपी-'शराबी, 'ठाकर की रोमा।' एक कहानी कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी आई, किन्तु न जाने क्यों, उसने स्वेच्छा से ही लिखना छोड़ दिया। पत्रों का, उसके पास अमूल्य संकलन था, प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, रवीन्द्रनाथ, नन्दलाल बोस, एलिस बोर्नर, आचार्य कृपलानी, मालवीयजी, बलराज साहनी। काश, उसकी मृत्यु से पूर्व मैंने उसकी वह अमूल्य निधि बटोर ली होती। हजारीप्रसादजी के तो न जाने कितने पत्र थे उसके पास गुरुदेव के बनाए चित्र, जिनके लिए पहाड़ी रंगों को, जयन्ती ने स्वयं अमर-कोश के वनौषधि पर्व से पढ़ जंगली फूलों को ढूँढ-ढूँढ़कर तैयार किया था। गत वर्ष 'देश' पत्रिका में प्रकाशित रवीन्द्रनाथ के एक पत्र में उनकी अपनी प्रिय छात्रा जयन्ती का उल्लेख था कि कैसे उसने हरिद्रा, खदिर, पलाश, बुरुश से अभिनव रंग बनाए थे। मैंने, तत्काल काटकर, कटिंग जयन्ती को भेज दी। जब मिली तो मैंने पूछा-'कटिंग मिली?'
'हाँ, मिली तो थी, मैंने सिरहाने रख दी थी कि फुर्सत से पढूंगी-पता नहीं कहाँ चली गई-क्या लिखा था?'
उसका सिरहाना भानुमती का पिटारा था। दाडिम, अखरोट के दाने, खाँड के खिलौने, पुड़ियों में रखे पहाड़ी मसालों-जम्बू ‘गभैणी' कस्तूरी के बीड़े। हमारे बचपन की तस्वीरें, दिवंगत जीजाजी का रूमाल। उस बहुरंगी भीड़ में भला रवीन्द्रनाथ के पत्र की क्या बिसात?
अपनी प्रतिभा का मूल्य जयन्ती स्वयं कभी नहीं आँक पाई। उसे तो आँका था गुरुदेव ने, आश्रम के गुरुजनों ने, हजारीप्रसादजी ने, जो कहते थे 'कभी मेरी क़लम की उत्तराधिकारी जयन्ती ही होगी।' गुरुदेव ने उसका नाम रखा था 'भारत माता'। आश्रम में उसकी खिल्ली उड़ाई जाती। खद्दर की मोटी-मोटी साड़ियाँ बाँधती हैं, वह भी कितनी ऊँची। सिर ढाँपती है, नीचे आँखें किए चलती है, किसी से अनावश्यक बात नहीं करती-गुरुदेव के अनन्य स्नेह ने ही, उन्हें अहंकारी बना दिया है, आदि-आदि, किन्तु बात ऐसी नहीं थी। अहंकार से तो वह कोसों दूर थी-यद्यपि अहंकार करने को उसके पास बहुत कुछ था। रंग हम सबसे दबा होने पर भी यौवनावस्था में उसका आकर्षक व्यक्तित्व कैसा था, यह वही बता सकते हैं, जिन्होंने उसे तब देखा है।
इन्टर किया ही था कि दनादन रिश्ते आने लगे, किन्तु वह बहुत पहले ही आजन्म कुँआरी रहने की घोषणा कर चुकी थी। उसकी जिद को सब जानते थे, फिर भी माँ ने लाख समझाया, 'देख, ऐसे रिश्ते बार-बार नहीं आते, इतना अच्छा घर-वर, फिर कहाँ मिलेगा-तू अट्ठारह की हो गई है, तेरी बड़ी बहन तो चौदह वर्ष में ही माँ बन गई थी-लड़का आई.सी.एस. की परीक्षा देने विलायत गया है...।' पर जयन्ती का मुँह से छूटा 'नहीं' ब्रह्म वाक्य था।
उधर उसके एक प्रशंसक जिन्हें लॉर्ड कहा जाता था, हमारे गृह की निरन्तर परिक्रमा किए जा रहे थे। एक दिन, हम गरमी की छुट्टियों में घर आए तो देखा, बढ़िया ट्वीड का ओवरकोट पहने, मुँह में सिगार लगाए, लार्ड सीटी में कोई अंग्रेज़ी धुन, गुनगुना रहा था। उसके दुःसाहस से जयन्ती के तनबदन में आग लग गई। कहने लगी, 'देख तू मेरा एक काम करेगी, तो पाँच रुपये दूंगी-' उन दिनों उत्कोच की वह राशि पर्याप्त थी- 'कहो।'
-देख, कल जब यह पट्ठा, खड़ा होकर सीटी बजाए, तो दीवार पर चढ़ तू इस बुलबुलिया के, इन ब्रिलैंटीन की जुल्फ़ों पर पिच्च से थूककर कहना-‘जा भाग, मेरी बहन ने कहा है, वह तुझसे कभी शादी नहीं करेगी...'
दूसरे दिन सन्ध्या प्रगाढ़ होते ही कृष्ण की बंकिम मुद्रा में खड़ा लॉर्ड सीटी बजाने लगा। मैं दीवार पर बैठी बड़ी देर से, थूक का गोला बना रही थी। मुझे देख, भावी साली के रूप में उसने बड़े मोहक स्मित से मेरा स्वागत किया। बड़ी देर से मुख में संचित थूक प्रक्षेपण में, मैंने फिर विलम्ब नहीं किया। मेरा अचूक निशाना पलभर में, उन यन्त्र से सँवरी जुल्फों का सन्तुलन विकृत कर बैठा।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






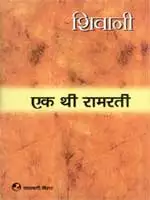


_s.jpg)
