|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
मैंने तो भय से आँखें ही बन्द कर लीं-हाय, अब इसे कुछ हो गया, तो इसके चाचा से
क्या कहूँगी!
सहसा चन्दन ने बाबर की तुलुगमा रणनीति अपना ली। जैसे ही बैल पीछे जाकर, सिर झुकाकर हमला करने बढ़ता, वह पत्थरों की बौछार से उसे फिर पीछे ढकेल देता। पत्थरों का बारूद जनता बराबर सप्लाई किए जा रही थी। सहसा विजय-ध्वनि से एक बार फिर घाटी गूंज उठी। शत्रु दुब दबाकर तेजी से भागा जा रहा था।
“अरे वाह-वाह, क्या मारा है! खून से लथपथ हो गया।" अब समझ में आया कि कुश्तीप्रेमी क्यों रुपया खर्च करके पशु और मानव की यह कुश्ती देखने स्पेन जाते हैं।
इधर संयोग से जब कभी मेरे पति खाना खाने बैठते और मुख में पहला कौर धरते कि किसी-न-किसी मन्त्रीजी का फोन आ जाता। कुछ दिनों बाद, जब यह असमय का कॉल नित्य का नियम बन गया. तो चन्दन ने किसी प्रधानमन्त्री के रूखे पी.ए. की ही कर्तव्यपरायणता से उस मुखर फोन का अपने संरक्षण में ले लिया। पहले-पहल बातों का क्रम कुछ-कुछ ऐसा रहता :
"मैं मन्त्री बोल रहा हूँ।”
“मैं चन्दन बोल रहा हूँ।"
“अरे भई, मैं मन्त्री बोल रहा हूँ।"
"अरे भई, मैं चन्दन बोल रहा हूँ।"
(कुछ झल्लाकर)- “पंतजी हैं?"
“जी, नहा रहे हैं।"
“कब तक नहा लेंगे?"
“यह मैं कैसे बता सकता हूँ जी?"
"क्या?"
“जी...बता तो वही सकते हैं जी, जो नहा रहे हैं।"
लपककर उसके हाथ से फोन छीनने पर भी मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़
रहे अपने राजनयिक सम्बन्धों को फिर सुधार नहीं पाती।
“ऐसे क्यों बोलता है तू, चन्दन? कह देता अभी आ जायेंगे।” मैं डाँटती तो वह दुष्टता से मुस्कराकर कहता-“रोज-रोज बाबू का खाना ठंडा हो जाता है।”
“भलेमानुस, यह तो कह सकता था कि खाना खा रहे हैं," मैंने कहा। दुर्भाग्य से दूसरे दिन, ठीक उसी समय पहले कौर के मुँह में रखते ही फिर वही घंटी बजी। मैं उसी तेजी से भागी जैसे कोई खिलाड़ी बालक पतंग की कटी डोर पकड़ने लपकता है। पर तब तक रिसीवर चन्दन के हाथ में जा चुका था। अपना अचूक निशाना साध फिर गोली दागने में उस निर्भीक सैनिक ने एक पल का भी विलम्ब न किया।
फोन फिर किसी मन्त्रीजी का ही था।
“क्यों भई, पंतजी हैं?”
“जी हैं, पर खाना खा रहे हैं।” शायद पहली बार उसने ईमानदारी से उत्तर दिया था।
“अरे भई, मैं मन्त्री बोल रहा हूँ।" मैं वहीं पर खड़ी उनके आदेश को स्पष्ट सुन रही थी। मैं समझ गयी कि परिचय का उल्लेख केवल इसीलिए किया गया था कि खाना खा रहे हों तो भी उन्हें फोन दे दिया जाए। “सुना, मैं मन्त्री बोल रहा हूँ!" इस बार स्वर पंचम से धैवत में पहुँच गया था।
“तो बोलिए फिर।” और उसने रिसीवर नीचे रख दिया, फिर मेरी ओर देखकर बड़े गर्व से मुस्कराया, जैसे कह रहा हो- 'देखा दीदी, कैसा जवाब दिया।'
“छी चन्दन, तू क्या कभी ढंग से बातें करना नहीं सीखेगा?” मैंने उसे बुरी तरह फटकारा, पर मेरी फटकार सदा की भाँति चिकने घड़े पर पड़े जलबिन्दु-सी ही ढुलक गई। एक-एक करके वह अब तक शायद प्रदेश के पूरे मन्त्रिमंडल को ही रुष्ट कर चुका है। इसी से बत्तीस दाँतों के बीच सहमी जिह्वा-सी मैं अपने अन्धकारमय भविष्य की कल्पना करके कभी स्वयं सिहर उठती हूँ। लक्ष्मण की भाँति यह अभागा क्या एक ही परशुराम को अप्रसन्न कर चुप बैठ पाया है? इसके अपराध को देख यदि कभी मेरे पति का तबादला अण्डमान भी कर दिया गया तो भी समझूँगी कि हम सस्ते ही छूटे।
एक दिन किसी मन्त्रीजी के कुछ गर्वीले पी.ए. महोदय का फोन आया, "देखो जी, मैं फलाँ मन्त्रीजी का पी.ए. बोल रहा हूँ। साहब को फोन दो।"
कुछ अकड़कर ही उसने कहा।
“नहीं दे सकता।” उस स्वाभाविक निर्भीकता की गूंज ही मुझे वहाँ खींच लाई।
"क्या?"
“जी, नहीं दे सकता। क्योंकि साहब हैं ही नहीं, घूमने गए हैं।"
"तुम कौन बोल रहे हो?" स्वर में रपट लिख रहे किसी अनुभवी थानेदार की-सी ही कठोरता 'किर्र' से गूंजती निकली।
“जी मैं?" पूछनेवाले को चिढ़ाने के लिए ही वह अबोध बना, अनावश्यक किस्तों में अपना विलम्बित उत्तर दे रहा था।
"और क्या मैं?”
खु-खु करके हँसी, फिर वही प्रश्न-“जी मैं?'' फिर हँसी और फिर वही-“जी मैं?”
“बेवकूफ, जंगली हो तुम।” स्वर इस बार ऐसे गरजा जैसे रिसीवर को ही चकनाचूर कर देगा-“मैं पी.ए. बोल रहा हूँ।"
“ओह तभी ही तो, यह मैं समझ ही गया था जी, कि आप पिये हैं। पिये ' न होते तो ऐसे थोड़े ही बोलते...एक दिन हमारा धोबी भी पीकर ऐसे ही गरज रहा था...” फोन रखकर वह हँसता-हँसता दोहरा हो गया। “खूब पीकर बोल रहे थे हजरत, इसी से तो अकड रहे थे!"
“चल हट!” मैंने उसे डाँटकर कहा, “पी.ए. मन्त्रीजी का सेक्रेटरी होता है मूर्ख!”
बस उसी क्षण, उस संक्षिप्त संबोधन की महत्ता ने उसे मोह लिया। दो अक्षरों में कैसी महिमा भरी थी, कैसी गरिमा! अब किसी का फोन आता है, “कौन बोल रहा है?" तो वह अपने उत्तर को स्वाभाविक “जी” से नहीं सँवारता। “मैं पंतजी का पी.ए. बोल रहा हूँ, चन्दन।” कहकर पीठ सतर कर खड़ा हो जाता है।
सहसा चन्दन ने बाबर की तुलुगमा रणनीति अपना ली। जैसे ही बैल पीछे जाकर, सिर झुकाकर हमला करने बढ़ता, वह पत्थरों की बौछार से उसे फिर पीछे ढकेल देता। पत्थरों का बारूद जनता बराबर सप्लाई किए जा रही थी। सहसा विजय-ध्वनि से एक बार फिर घाटी गूंज उठी। शत्रु दुब दबाकर तेजी से भागा जा रहा था।
“अरे वाह-वाह, क्या मारा है! खून से लथपथ हो गया।" अब समझ में आया कि कुश्तीप्रेमी क्यों रुपया खर्च करके पशु और मानव की यह कुश्ती देखने स्पेन जाते हैं।
इधर संयोग से जब कभी मेरे पति खाना खाने बैठते और मुख में पहला कौर धरते कि किसी-न-किसी मन्त्रीजी का फोन आ जाता। कुछ दिनों बाद, जब यह असमय का कॉल नित्य का नियम बन गया. तो चन्दन ने किसी प्रधानमन्त्री के रूखे पी.ए. की ही कर्तव्यपरायणता से उस मुखर फोन का अपने संरक्षण में ले लिया। पहले-पहल बातों का क्रम कुछ-कुछ ऐसा रहता :
"मैं मन्त्री बोल रहा हूँ।”
“मैं चन्दन बोल रहा हूँ।"
“अरे भई, मैं मन्त्री बोल रहा हूँ।"
"अरे भई, मैं चन्दन बोल रहा हूँ।"
(कुछ झल्लाकर)- “पंतजी हैं?"
“जी, नहा रहे हैं।"
“कब तक नहा लेंगे?"
“यह मैं कैसे बता सकता हूँ जी?"
"क्या?"
“जी...बता तो वही सकते हैं जी, जो नहा रहे हैं।"
लपककर उसके हाथ से फोन छीनने पर भी मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़
रहे अपने राजनयिक सम्बन्धों को फिर सुधार नहीं पाती।
“ऐसे क्यों बोलता है तू, चन्दन? कह देता अभी आ जायेंगे।” मैं डाँटती तो वह दुष्टता से मुस्कराकर कहता-“रोज-रोज बाबू का खाना ठंडा हो जाता है।”
“भलेमानुस, यह तो कह सकता था कि खाना खा रहे हैं," मैंने कहा। दुर्भाग्य से दूसरे दिन, ठीक उसी समय पहले कौर के मुँह में रखते ही फिर वही घंटी बजी। मैं उसी तेजी से भागी जैसे कोई खिलाड़ी बालक पतंग की कटी डोर पकड़ने लपकता है। पर तब तक रिसीवर चन्दन के हाथ में जा चुका था। अपना अचूक निशाना साध फिर गोली दागने में उस निर्भीक सैनिक ने एक पल का भी विलम्ब न किया।
फोन फिर किसी मन्त्रीजी का ही था।
“क्यों भई, पंतजी हैं?”
“जी हैं, पर खाना खा रहे हैं।” शायद पहली बार उसने ईमानदारी से उत्तर दिया था।
“अरे भई, मैं मन्त्री बोल रहा हूँ।" मैं वहीं पर खड़ी उनके आदेश को स्पष्ट सुन रही थी। मैं समझ गयी कि परिचय का उल्लेख केवल इसीलिए किया गया था कि खाना खा रहे हों तो भी उन्हें फोन दे दिया जाए। “सुना, मैं मन्त्री बोल रहा हूँ!" इस बार स्वर पंचम से धैवत में पहुँच गया था।
“तो बोलिए फिर।” और उसने रिसीवर नीचे रख दिया, फिर मेरी ओर देखकर बड़े गर्व से मुस्कराया, जैसे कह रहा हो- 'देखा दीदी, कैसा जवाब दिया।'
“छी चन्दन, तू क्या कभी ढंग से बातें करना नहीं सीखेगा?” मैंने उसे बुरी तरह फटकारा, पर मेरी फटकार सदा की भाँति चिकने घड़े पर पड़े जलबिन्दु-सी ही ढुलक गई। एक-एक करके वह अब तक शायद प्रदेश के पूरे मन्त्रिमंडल को ही रुष्ट कर चुका है। इसी से बत्तीस दाँतों के बीच सहमी जिह्वा-सी मैं अपने अन्धकारमय भविष्य की कल्पना करके कभी स्वयं सिहर उठती हूँ। लक्ष्मण की भाँति यह अभागा क्या एक ही परशुराम को अप्रसन्न कर चुप बैठ पाया है? इसके अपराध को देख यदि कभी मेरे पति का तबादला अण्डमान भी कर दिया गया तो भी समझूँगी कि हम सस्ते ही छूटे।
एक दिन किसी मन्त्रीजी के कुछ गर्वीले पी.ए. महोदय का फोन आया, "देखो जी, मैं फलाँ मन्त्रीजी का पी.ए. बोल रहा हूँ। साहब को फोन दो।"
कुछ अकड़कर ही उसने कहा।
“नहीं दे सकता।” उस स्वाभाविक निर्भीकता की गूंज ही मुझे वहाँ खींच लाई।
"क्या?"
“जी, नहीं दे सकता। क्योंकि साहब हैं ही नहीं, घूमने गए हैं।"
"तुम कौन बोल रहे हो?" स्वर में रपट लिख रहे किसी अनुभवी थानेदार की-सी ही कठोरता 'किर्र' से गूंजती निकली।
“जी मैं?" पूछनेवाले को चिढ़ाने के लिए ही वह अबोध बना, अनावश्यक किस्तों में अपना विलम्बित उत्तर दे रहा था।
"और क्या मैं?”
खु-खु करके हँसी, फिर वही प्रश्न-“जी मैं?'' फिर हँसी और फिर वही-“जी मैं?”
“बेवकूफ, जंगली हो तुम।” स्वर इस बार ऐसे गरजा जैसे रिसीवर को ही चकनाचूर कर देगा-“मैं पी.ए. बोल रहा हूँ।"
“ओह तभी ही तो, यह मैं समझ ही गया था जी, कि आप पिये हैं। पिये ' न होते तो ऐसे थोड़े ही बोलते...एक दिन हमारा धोबी भी पीकर ऐसे ही गरज रहा था...” फोन रखकर वह हँसता-हँसता दोहरा हो गया। “खूब पीकर बोल रहे थे हजरत, इसी से तो अकड रहे थे!"
“चल हट!” मैंने उसे डाँटकर कहा, “पी.ए. मन्त्रीजी का सेक्रेटरी होता है मूर्ख!”
बस उसी क्षण, उस संक्षिप्त संबोधन की महत्ता ने उसे मोह लिया। दो अक्षरों में कैसी महिमा भरी थी, कैसी गरिमा! अब किसी का फोन आता है, “कौन बोल रहा है?" तो वह अपने उत्तर को स्वाभाविक “जी” से नहीं सँवारता। “मैं पंतजी का पी.ए. बोल रहा हूँ, चन्दन।” कहकर पीठ सतर कर खड़ा हो जाता है।
किन्तु समस्त ब्रह्मांड से अकेले ही मोर्चा लेनेवाले मेरे पति के इस दुःसाहसी
पी.ए. की उग्र नक्सलवादी गतिविधियों ने इधर मेरी उलझनें विकट रूप से बढ़ा दी
हैं। घर से बाहर निकलता है, तो हवा से लड़ता है। पत्रिकाएँ पढ़ता है और जब कहीं
किसी आलोचक ने मेरी किसी कहानी को बुरा-भला कह दिया, तो बाँहें समेट लेता है,
“चिन्ता मत करो दीदी, आने दो कभी ससुर को लखनऊ, मैं निबट लूँगा।" एक लम्बी साँस
खींच, चुप रहने के अलावा मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं रह जाता। चाहने पर भी अब
क्या मैं आँगनकुटी छवाकर 'निंदक नियरे' रख सकती हूँ?
किन्तु इसी क्रोधी, दुर्वासा रूपी अनाथ उदंड किशोर के स्वभाव का एक दूसरा पक्ष भी है-बुलडॉग की ही भाँति शायद विधाता ने उसे केवल ‘वन मैन्स डॉग' बनाया है। हमारे परिवार के प्रति उसकी निष्ठा, स्वामिभक्ति और प्रेम स्वयं अपने में एक अनूठी मिसाल है। किन्तु यदि किसी और ने उस पर रोब जमाने की चेष्टा की तो वह पैंतरा बदल लेता है।
कपड़ों के चयन में उसकी रुचि सर्वथा मौलिक है। कभी-कभी तो अपना पूरा वेतन ही वह कपड़ों में फूंक डालता है। डैनम के बैलबॉटम, गुरु कुरते, नैनीताल के तिब्बती बिसातियों से खरीदी हुई अनोखी मालाएँ, सुमरनियाँ, एक-एक बालिश्त चौड़ी 'आई लव यू' लिखी कमर की पेटियाँ और कन्धे तक झूलती अत्याधुनिक अयाल! फरमाइश भी उसकी मौलिक रहती है। मैं गत वर्ष आकाशवाणी की एक परिचर्चा में भाग लेने बम्बई जाने लगी तो मैंने पूछा, “क्यों रे, तुझे क्या चाहिए बम्बई से?"
“धर्मेन्द्र से कहिएगा, अपने चौखाने ट्वीड का नमूना मुझे भेज दें।"
"धर्मेन्द्र से?” मैं जैसे आकाश से गिरी।
“हाँ, मैंने उनके इंटरव्यू में पढ़ा था कि उन्हें आपकी कहानियाँ बहुत पसन्द हैं।”
दुर्भाग्य से मेरी भेंट धर्मेन्द्र से नहीं हो पायी। मिलते, तो शायद मेरे इस विचित्र दत्तक पुत्र की अनोखी फरमाइश पूरी भी कर देते।
जो चन्दन को नहीं जानता, उसकी वेशभूषा, गतिविधि देख उसे मेरा ही पुत्र समझता है। कुछ दिन पूर्व, मेरे एक ब्रिगेडियर मित्र मिलने आए। खिड़की पर चन्दन को देखा, तो हँसकर पूछने लगे, “अच्छा, तो यह तुम्हारा बेटा है!"
नहीं, यह मेरा बेटा नहीं, मेरा नौकर है। यह मैं चाहने पर भी नहीं कह पायी।
जो मेरे बच्चों के साथ उन्हीं की भाँति मुझे दीदी और मेरे पति को 'बाबू' कहता आया है; जिसे मेरी बेटी अपने भाई की ही जैसी अविकल जुड़वाँ राखी भेजना कभी नहीं भूलती; जो मेरे पति के ऑपरेशन के पश्चात्, उन्हें होश में आने के लिए यन्त्रणा से छटपटाते देख अपना रुआँसा सफ़ेद चेहरा अधमुंदे द्वार की दरार से सटा घंटों खड़ा रहा था-उसे मैं अब नौकर कहूँ भी, तो किस मुँह से?
किन्तु इसी क्रोधी, दुर्वासा रूपी अनाथ उदंड किशोर के स्वभाव का एक दूसरा पक्ष भी है-बुलडॉग की ही भाँति शायद विधाता ने उसे केवल ‘वन मैन्स डॉग' बनाया है। हमारे परिवार के प्रति उसकी निष्ठा, स्वामिभक्ति और प्रेम स्वयं अपने में एक अनूठी मिसाल है। किन्तु यदि किसी और ने उस पर रोब जमाने की चेष्टा की तो वह पैंतरा बदल लेता है।
कपड़ों के चयन में उसकी रुचि सर्वथा मौलिक है। कभी-कभी तो अपना पूरा वेतन ही वह कपड़ों में फूंक डालता है। डैनम के बैलबॉटम, गुरु कुरते, नैनीताल के तिब्बती बिसातियों से खरीदी हुई अनोखी मालाएँ, सुमरनियाँ, एक-एक बालिश्त चौड़ी 'आई लव यू' लिखी कमर की पेटियाँ और कन्धे तक झूलती अत्याधुनिक अयाल! फरमाइश भी उसकी मौलिक रहती है। मैं गत वर्ष आकाशवाणी की एक परिचर्चा में भाग लेने बम्बई जाने लगी तो मैंने पूछा, “क्यों रे, तुझे क्या चाहिए बम्बई से?"
“धर्मेन्द्र से कहिएगा, अपने चौखाने ट्वीड का नमूना मुझे भेज दें।"
"धर्मेन्द्र से?” मैं जैसे आकाश से गिरी।
“हाँ, मैंने उनके इंटरव्यू में पढ़ा था कि उन्हें आपकी कहानियाँ बहुत पसन्द हैं।”
दुर्भाग्य से मेरी भेंट धर्मेन्द्र से नहीं हो पायी। मिलते, तो शायद मेरे इस विचित्र दत्तक पुत्र की अनोखी फरमाइश पूरी भी कर देते।
जो चन्दन को नहीं जानता, उसकी वेशभूषा, गतिविधि देख उसे मेरा ही पुत्र समझता है। कुछ दिन पूर्व, मेरे एक ब्रिगेडियर मित्र मिलने आए। खिड़की पर चन्दन को देखा, तो हँसकर पूछने लगे, “अच्छा, तो यह तुम्हारा बेटा है!"
नहीं, यह मेरा बेटा नहीं, मेरा नौकर है। यह मैं चाहने पर भी नहीं कह पायी।
जो मेरे बच्चों के साथ उन्हीं की भाँति मुझे दीदी और मेरे पति को 'बाबू' कहता आया है; जिसे मेरी बेटी अपने भाई की ही जैसी अविकल जुड़वाँ राखी भेजना कभी नहीं भूलती; जो मेरे पति के ऑपरेशन के पश्चात्, उन्हें होश में आने के लिए यन्त्रणा से छटपटाते देख अपना रुआँसा सफ़ेद चेहरा अधमुंदे द्वार की दरार से सटा घंटों खड़ा रहा था-उसे मैं अब नौकर कहूँ भी, तो किस मुँह से?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






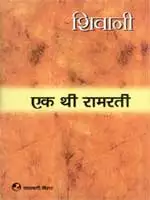


_s.jpg)
