|
नारी विमर्श >> भैरवी (अजिल्द) भैरवी (अजिल्द)शिवानी
|
358 पाठक हैं |
|||||||
पति-व्रता स्त्री के जीवन पर आधारित उपन्यास
क्या वह रणधीर सिंह ही तो नहीं था? कुछ-न कुछ बहाना बनाकर वह ऐसे ही आ जाता,
कभी अखबार लेकर और कंभी दियासलाई माँगने। आकर फिर क्या वह कभी सहज में टलता
था? अगर अब भी वही होगा तो वह उसे द्वार से ही गर्दन मरोड़कर टरका देगी। पर
इस बार वह नहीं था। जो गर्दन मरोड़ने का संकल्प कर उठ गई थी, उसे शायद पूरी
एक ही ऊँचाई और एक दर्जन गर्दनें ही मरोड़नी पड़तीं, क्योंकि वहाँ तो पूरे एक
दर्जन लगभग एक ही ऊँचाई और एक ही वर्दी के दस-बारह लड़के कन्धे पर बैग लटकाए
ऐसे खड़े थे, जैसे पर्वतारोही दल के शेरपा हों।
पहले तो वह भौचक्की-सी उन्हें देखती ही रह गई।
यह क्या कोई फौजी टुकड़ी ही इधर भटककर आ गई थी?
"क्षमा कीजिएगा माँजी!" उनकी टुकड़ी का एक सुदर्शन आगे बढ़ आया। "हमारा
पर्वतारोही दल दिल्ली से आया है, और अचानक इस अंधड़ में फँस गया है। क्या
कृपा कर थोड़ी देर हमें अपने यहाँ सुस्ताने देंगी?"
उसकी बात पूरी भी नहीं निकली थी कि प्रबल प्रभंजन के एक साइक्लोनी तेजी से आए
झोंके से उनकी विचित्र पोशाक को पैराशूट-सा फुला दिया। बरसाती के कपड़े से
बने कोट, जिसमें मशीनी शकरपारे काटकर शायद रुई की मोटी-मोटी तहें बिछा दी गई
थीं, हवा से फूलकर गैस के गुब्बारों से तन गए। साथ ही शिलावृष्टि और भी तेजी
से ताबड़तोड़ छत पीटने लगी। झर-झार पाँगर के कठोर दाने ढालू छत से
लुढ़कते-पुढ़कते धरा पर कत्थई चादर-सी बिछा गए और गुलावी पुष्पों से लदा
पंय्या का वृक्ष पल-भर में अंग झाड़, पुष्पों से गदराए यौवन को खोकर 'नीरस
तरुवर विलसति पुरतः' बन गया। राजेश्वरी पल-भर को यह भी भूल गई कि कमरे के
भीतर उसकी रूपवती राजकन्या बैठी है और दीवानखाने में जाते ही एकसाथ चौबीस
तरुण आँखें उसे देख लेंगी। बरसते आकाश और गरजती शिलावृष्टि के नीचे खड़े बारह
कमनीय चेहरे देखकर उसका सुप्त मातृत्व जग गया। उनकी वर्दी अब इतनी अधिक फूल
गई थी कि राजेश्वरी को लगा, दूसरा प्रबल झोंका आते ही बारह के बारह छोकड़े
हवा में उड़ जाएंगे। बेचारे परदेशी लड़के इतनी रात को-क्या वह द्वार से लौटा
देगी?
“आ जाइए।" अब तक कार्पण्य से खोले गए द्वार उसने पूर्ण औदार्य से खोल दिए।
वर्षा में भीगे लड़के, बैंक्स, बैंक्स से दिशाएँ [जाते, जूते खोलकर दीवानखाने
के गुदगुदे गलीचे में धंस गए।
जहाँ अपनी माँ को छोड़, जिसने कभी कोई दूसरा कंठ-स्वर सुना भी था तो शायद
रणधीर सिंह का या पीताम्बर नाना का, वहाँ एकसाथ उतने गलों का ताजा कंठ-स्वर
सुन चन्दन अपना कुतूहल नहीं रोक पाई। द्वार पर परदा तो था नहीं; वह भागकर
द्वार पर खड़ी हो गई, साथ ही चौबीस आँखें उसके औत्सुक्य-मिश्रित कुतूहल से और
भी भोले बन गए, कमनीय चेहरे पर नग-सी जड़ गईं। अचकचाकर राजेश्वरी उठकर भीतर
गई और पुत्री को भी न जाने क्या कहकर साथ लेती गई। माँ-बेटी के जाते ही उस
पुराने ढंग से बने दीवानखाने की नई भीड़ में द्वार पर पल-भर को खड़ी उर्वशी
को लेकर गरमागरम बहस चल पड़ी।
कोई कहता-यह निश्चय ही उसकी बेटी है।
दूसरा कहता-अरे आशावादियो! क्यों बालू में किला बाँधते हो, हो सकता है, हम
सबकी बदनसीबी से वह मकान-मालकिन की बहू हो! पहाड़ में तो ऐसी छोटी कच्ची उमर
की बहुएँ होती हैं।
साथ ही एक दबा ठहाका गूंज उठा। उसी ठहाके को उसके कमरे में आते ही पुनः कंठ
में खींच लिया गया है, यह चतुरा राजी समझ गई।
तब क्या उसी की हँसी उड़ाने लगे थे ये छोकरे! वह अब कर ही क्या सकती थी? 'जब
कभी कुछ विवशता से ही करना पड़े, राजेश्वरी!' उसकी पथप्रदर्शिका शारदा बहनजी
कहा करती थीं, 'डू इट विद ग्रेस ? क्या फायदा है मुँह लटकाकर, झुंझलाकर, उस
विवशता को निभाने में? हँस-खेलकर भी तो वह विवशता झेली जा सकती है?' वह अपनी
अदर्शी गुरुआइन की सीख को सिर-आँखों पर झेलती, बड़ी-सी अष्टकोणी पहाड़ी
सग्गड़ में धधकाते बाज के सूखे फूल और दहकते कोयले सजा लाई।
“आप लोग आराम से हाथ-पैर तापें, मैं अभी चाय बनाकर ले आती हूँ।" थोड़ी देर
में वह बारह गिलास गर्म, नमकीन मक्खन डली चाय लेकर आ गई, “इस चाय को पीते ही
आप अपनी थकान भूल जाएँगे।" उसने हँसकर एक-एक को गिलास थमा दिया और फिर खाली
थाली लेकर उठ गई। “मैं थोड़ा पानी और चढ़ा आऊँ, आपमें से कोई शायद दूसरा
गिलास पीना पसन्द करे।" वह चली गई।
"बड़ी पक्की है यार!" वही अगुआ अपने साथियों को फिर एक कहकहे के जलजले में
धंसा गया, “लगता है, चाय का दूसरा राउंड देने भी सुसरी खुद आएगी। उस लड़की को
क्या चूल्हे में गाड़ आई है?" रसिक प्रश्न अभी सबको गुदगुदाकर शान्त नहीं हुआ
था कि सचमुच ही वह दूसरी बार भी स्वयं ही चाय भरी केतली लेकर आ गई। वर्षा रुक
गई थी, दो-तीन बार आकर राजेश्वरी उन्हें हिंट भी दे गई थी, पर, वे अनजान बने
गुदगुदे गलीचे पर गठरियाँ बने लुढ़कने लगे। रात के दस बज गए थे, अब वह इतनी
रात गए उन्हें जाने के लिए कह भी कैसे सकती थी? पल-भर की मूर्खता का अब उसे
गहरा मूल्य चुकाना पड़ रहा था। वह तीसरी बार उन्हें देखने आई तो वे पीठ के
बँधे झोले उतार, स्वयं ही जीन-लगाम-काठी-विहीन अश्वदल की भाँति अस्तबल की
जुगाली में रम चुके थे। कोई सिगरेट फूंक रहा था, कोई पैर पर पैर धरे गुनगुना
रहा था, और कोई हाथ-पैर फैलाकर चारों खाने चित्त हो गया था।
|
|||||


 i
i 






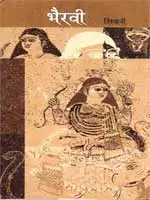


_s.jpg)
