|
नारी विमर्श >> भैरवी (अजिल्द) भैरवी (अजिल्द)शिवानी
|
358 पाठक हैं |
|||||||
पति-व्रता स्त्री के जीवन पर आधारित उपन्यास
क्या रंग था लड़की का! और कैसी अपूर्व आँखें- एक तो इधर उसकी गुंइयाँ ताहिरा
ने, उन शरबती आँखों में सुरमे के स्याह डोरे डाल, उन्हें और भी सरस बना दिया
था, उस पर पारदर्शी त्वचा पर मुसलमानी धानी-ऊदे लच्छे की शोभा, लहरें-सी
मारने लगी थीं।
"चची ने जिद कर एकसाथ इतनी चूड़ियाँ पहना दीं, अम्माँ! पूरे चार रुपये की
हैं।" वह चची के औदार्य का बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख करती, रूठी माँ को मनाने का
प्रयत्न करती। वह जानती थी कि अम्माँ, चाहे मुँह से कुछ न कहे, किन्तु अपनी
खतरनाक आँखों के डमरू बजाकर, उसे शाखामृगी-सी ही उठा-बैठा सकती है।
प्रतिवेशी मुसलमान परिवार के लड़के भी, सब नहले पर दहला थे। एक से एक बाँके,
सजीले जवान, कभी कोई पाकिस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेज से छुट्टियाँ बिताने आ
जाता, कभी कोई अलीगढ़ का अधूरा डॉक्टर ही, बारजे में सीटियाँ बजाता, निरर्थक
चक्कर लगाने लगता। जब-जब उनके छुट्टियों में घर आने की खबर राजेश्वरी को
मिलती, वह स्वयं गेस्टापो बनी पुत्री के पीछे, छाया-सी डोलने लगती। वह स्वयं,
प्रेमदुर्ग की एक-एक गुप्त सुरंग से परिचित थी, कब और कैसे पुत्री माँ को छल
सकती है, वह सब सूंघकर ही बता सकती थी, किन्तु इतना वह जान गई थी कि पुत्री
की निर्दोष दृष्टि में, अभी कहीं भी छल-कपट की धोखाधड़ी नहीं उभरी है, किन्तु
कभी भी डाइनामाइट का धड़ाका, उनकी गृहस्थी की सुदृढ़ चट्टान को ढहा सकता है।
तब क्यों न वह स्वयं आग की जली, समय रहते ही मठा भी फूंककर पी ले!
लम्बी नीरस नौकरी के क्रम में उसने कभी एकसाथ दस दिन की भी छुट्टी नहीं ली
थी। दूसरे ही दिन दो महीने की लम्बी छुट्टी लेकर, वह यह कहकर पहाड़ चली गई कि
माँ-बाप का, बड़े शौक से बनवाया घर एकदम बँडहर हो गया है, ऐसी चिट्ठी घर से
आई है, वह उसी की देखभाल करने जा रही है।
पुत्री के उत्साह का अन्त नहीं था, किन्तु जैसे-जैसे अलमोड़ा निकट आता जाता,
उसकी माँ अस्वाभाविक रूप से गुमसुम बनी जा रही थी। लाल-कुआँ का स्टेशन आते ही
राजेश्वरी को न जाने कैसी दहशत होने लगी। उसे अभी भी यही लग रहा था, जैसे
कनेर की घनी छाँह में, साक्षात् दुर्वासा बने उसके क्रोधी बाबूजी थरथरा रहे
हैं और लैंपपोस्ट की कुहरे में काँपती लौ में उसके वर्षों के विस्मृत प्रेमी
का सफेद पड़ गया चेहरा, किसी अदृश्य प्रस्तर मूर्ति में, वहाँ सदा के लिए
खुदकर रह गया है।
अलमोड़ा पहुँचने का तार उसने अपने आत्मीय स्वजनों को न देकर अपनी एक परिचिता
स्नेही प्रधानाध्यापिका को दिया था, जो अपनी अध्यापिकाओं की, एक छोटी-मोटी
फौज ही लेकर बसस्टैंड पर माता-पुत्री की प्रतीक्षा में खड़ी थी। दोनों ने
एकसाथ एल. टी. किया था। फिर रिश्ते में शान्ति, शारदा बहन की मौसेरी बहन भी
लगती थी। बड़े स्नेह से, वह माँ-बेटी को लेकर अपने जिस बँगले में पहुँची,
वहाँ राजराजेश्वरी पल भर को, ठिठककर खड़ी रह गई। अचानक जैसे किसी ने, पैरों
में लोहे की बेड़ियाँ डाल दी हों।
"कितना बढ़िया बँगला है न, अम्माँ? एकदम किसी राजा का महल लगता है यह तो!"
चन्दन चहकती जा रही थी, पर उसकी माँ को तो क्रूर नियति, पग-पग पर अँगूठा
दिखाती, चिढ़ाती जा रही थी।
"हाँ-हाँ, ठीक ही कह रही है बेटी!" शान्ति ने कहा। वह उन्हें जिस तेजी से
लेकर दीवानखाने में पहुँची, उसके लिए राजेश्वरी प्रस्तुत नहीं थी।
“क्षमा करना शान्ति, मोटर की लम्बी यात्रा के घुमार से मेरा सिर अभी भी चकरा
रहा है।" वह, सामने धरी एक मखमली कुर्सी पर ही धम्म से बैठ गई। कुर्सी वहाँ
बड़े मौके से धरी न मिलती तो शायद वह नीचे ही बैठ जाती। सचमुच ही कोई उसे
बाँहों में लिए तेजी से चक्कर खिला रहा था। पर वह क्या मोटर-घुमार था?
कमरे की एक-एक कुर्सी, एक-एक मेज, झाड़फानूस के लटकनों में लिपटी-स्मृतियों
के प्रेत कंकाल, उसे घेरकर मंडलाकार नृत्य में घूमने लगे। अब तक अवश पड़ी
सहस्र स्मृतियाँ, जिन्हें उसने हलवाई पति की उबलती चाशनी में, गृहस्थी के पाग
में पागकर रख दिया था, वे एकसाथ सहस्र भाले तानकर खड़ी हो गईं। दीवार पर लगे
राजा साहब के निर्जीव चित्र में भी जैसे किसी ने पल-भर को जान फूंक दी
थी-व्यंग्य से पूँछे बंकिम स्मित में तनी, उसे छेदने लगीं।
“तुम चलकर आराम से मेरे कमरे में लेट जाओ, राजेश्वरी!" शान्ति बोली, “लगता
है, बेहद थक गई हो, एक नींबू डालकर गर्म चाय पिलाऊँगी तो तुम्हारी सब घुमारी
दूर हो जाएगी।"
पर उस कोठी का कौन-सा कमरा ऐसा था, जहाँ वह आराम से लेट सकती थी? किस कमरे
में, उसके प्रेमी का प्रेत उसकी छाती पर सवार हो, उसका गला नहीं दबा बैठेगा?
शान्ति के कमरे में जाकर वह और व्याकुल हो उठी। यही तो था कुन्दन का कमरा।
अपने पिता की खुकरी से उसने, इसी कमरे की दीवार पर लता-पत्रांकित एक पान का
पत्ता खोद, दो अक्षर, खजुराहो की मिथुन मूर्तियों से गूंथकर रख दिए थे-'के'
और 'आर'। शायद अभी भी वहीं हों।
शान्ति, चाय बनाने चली गई थी और पहली बार पहाड़ को देखकर मुग्ध हो गई उसकी
चपला पुत्री कभी भाग-भागकर, झूमते, देवदार-द्रुमों को देख रही थी, कभी
हिमाच्छादित कामेत और त्रिशूल की चोटियों को। वह एकान्त के अलभ्य क्षण पाकर
सहसा बौराकर, दीवार को घूम-घूमकर देखती, अपनी स्मृतियों का खोया खजाना
ढूँढ़ने लगी।
रंग-चूने की अनेक परतों के नीचे, सहसा एक-दूसरे से गुंथे दो अक्षर उसे मिल
गए। भावुक कैशोर्य की लिखावट की स्याही क्या ऐसी ही अमिट होती होगी? अंग्रेजी
की एक कहावत को वह मन-ही-मन दुहराने लगी-'प्रथम प्रेम की कभी मृत्यु नहीं
होती। फिर वह तो उसका प्रथम और अन्तिम प्रेम था।
|
|||||


 i
i 






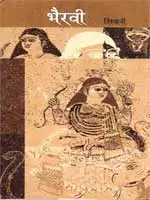


_s.jpg)
