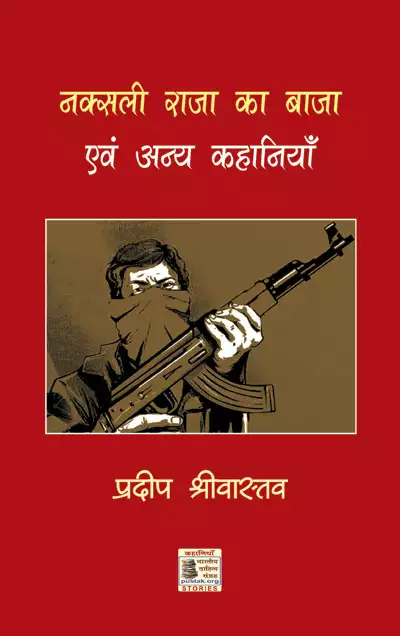|
उपन्यास >> बेनजीर - दरिया किनारे का ख्वाब बेनजीर - दरिया किनारे का ख्वाबप्रदीप श्रीवास्तव
|
|
||||||||||
प्रदीप जी का नवीन उपन्यास
कमरे की लाइट जल रही थी। फ्रेम में लगा कढ़ाई वाला कपड़ा दूर पड़ा था। मेरे तन के सारे कपड़े सामने दीवार के पास उनसे टकरा-टकरा कर इधर-उधर पड़े हुए थे। अपने को उस हाल में देख कर मैं खुद से ही शर्मा गई। जल्दी-जल्दी कपड़े पहन कर अम्मी के पास गई। सवेरे-सवेरे ही झूठ बोल दिया कि, देर तक कढ़ाई करती रही। बंद कमरे में कल गर्मी बहुत थी, इसीलिए सो नहीं पाई। सवेरे राहत मिली तो आँख लग गई। थोड़ी देर बाद आकर मैंने कमरे का बाकी हुलिया ठीक किया। सारा दिन बिना रुके मैं रात में छूटा काम पूरा करती रही।'
अपने ही शरीर के ऐसे बिंदास वर्णन से बेनज़ीर मुझे जितनी गजब की किस्सागो नज़र आई उतनी ही गजब की बोल्ड लेडी भी। मैं सच में उनसे इतना इंप्रेस हुआ कि, मंत्रमुग्ध होकर उन्हें एकटक देखता-सुनता, एकदम खो सा गया, तो उसने कहा, 'कहाँ खो गए, आप ऐसे क्या देख रहे हैं?' उनके इन प्रश्नों से मैं जैसे नींद से लौट आया। मैंने कहा, 'मैं आपकी कमाल की किस्सागोई में खो गया था। आपकी बोल्ड पर्सनॉलिटी ने ऐसा जादू कर दिया कि आपको एकटक देखता रह गया। यह भी भूल गया कि लाइफ में मैनर्स की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है।'
मेरी यह बात पूरी होने से पहले ही वह खिलखिला कर हँस पड़ीं। उनकी हंसी से मैंने बड़ी शर्मिंदगी महसूस की। उससे मुक्ति पाने के लिए मैंने जल्दी से वह प्रश्न पूछ लिया जो मन में तब खड़ा हुआ था, जब वह अपनी बातें बिना संकोच कहे जा रही थीं। मैंने भी उन्हीं की तरह बोल्ड होते हुए पूछा, 'तो यह वह क्षण थे जिसमें आप जीवन में पहली बार स्त्री-पुरुष संबंधों को पहली बार जान-समझ और हाँ, देख भी रही थीं।'
|
|||||


 i
i