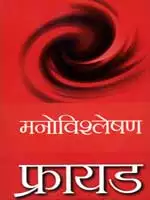|
विविध >> मनोविश्लेषण मनोविश्लेषणसिगमंड फ्रायड
|
286 पाठक हैं |
|||||||
‘ए जनरल इन्ट्रोडक्शन टु साइको-अनालिसिस’ का पूर्ण और प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद
मैं अपना कथन इन उदाहरणों से खत्म करूंगा। ये सिर्फ उदाहरण हैं। हम इस विषय
के बारे में और अधिक जानते हैं और आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे जैसे
अनाड़ियों के बजाय पुराणविद्या, नृतत्त्व-विज्ञान, भाषातत्त्व और लोककथाओं के
सच्चे विशेषज्ञों द्वारा इस तरह की सामग्री का संग्रह किया जाए तो वह कितना
अधिक विस्तृत और मनोरंजक होगा। हमें मजबूरन कुछ निष्कर्षों पर आना पड़ता है
जो इस तरह सारे-के-सारे हमारे सामने नहीं आ सकते, पर फिर भी जो हमें सोचने के
लिए बहुत कुछ मसाला दे जाएंगे।
प्रथम तो हमारे सामने यह तथ्य आता है कि स्वप्नद्रष्टा के पास अपने मन की बात
कहने की प्रतीकात्मक रीति है जिसके बारे में वह जाग्रत जीवन में कुछ नहीं
जानता और जिसे वह पहचानता भी नहीं। इससे उतना ही आश्चर्य होता है जितना आपको
यह पता लगने पर होगा कि आपकी नौकरानी संस्कृत भाषा जानती है, यद्यपि आपको यह
मालूम है कि वह बोहेमिया के एक गांव में पैदा हुई थी और उसने वह भाषा कभी
नहीं सीखी। इस तथ्य का हमारे मनोविज्ञान-विषयक विचारों से मेल बिठाना आसान
काम नहीं। हम इतना ही कह सकते हैं कि स्वप्नद्रष्टा का प्रतीकात्मकता का
ज्ञान अचेतन है और उसके अचेतन मानसिक जीवन में रहता है, पर यह धारणा भी हमारे
लिए अधिक उपयोगी नहीं होती। अब तक हमें सिर्फ यह कल्पना करनी पड़ी थी कि
अचेतन प्रवृत्तियों का अस्तित्व है, जो हमें स्थायी या . अस्थायी रूप से
अज्ञात होती हैं, पर अब कुछ बड़ा सवाल है और हमें ऐसी चीजों में सचमुच
विश्वास करना है, जैसे अचेतन ज्ञान, विचार-सम्बन्ध और विभिन्न वस्तओं में
साम्य, जिनके द्वारा एक मनोबिम्ब के स्थान पर दसरा मनोबिम्ब नियत रूप में
स्थापित किया जा सकता है। ये साम्य हर बार नये सिरे से नहीं शुरू होते, बल्कि
हमेशा के लिए तैयार की हुई हमारी सूची में होते हैं। यह हम विभिन्न
व्यक्तियों में सम्भवतः भाषा-सम्बन्धी भेदों के होते हुए भी उनके अभिन्न होने
का अनुमान करते हैं।
इसी प्रतीकात्मकता का ज्ञान हमें कहां से होता है? भाषा में प्रयुक्त शब्दों
में बहुत थोड़े प्रतीक आते हैं और दूसरे क्षेत्रों से बहुत सारे सादृश्य
स्वप्नद्रष्टा को अधिकतर अज्ञात होते हैं। सबसे पहले हमें स्वयं उन्हें मेहनत
से क्रमबद्ध करना होगा।
दूसरी बात यह कि ये प्रतीकात्मक सम्बन्ध स्वप्नद्रष्टा के लिए अलग नहीं होते,
या उसी स्वप्न-रचना के लिए अलग नहीं होते जिसमें ये प्रकट होते हैं, क्योंकि
हमने देखा है कि वही प्रतीक पुराणकथाओं में और परियों की कहानियों में, आम
लोगों की भाषा में और गीतों में, बोलचाल की भाषा और काव्य की कल्पना में
प्रयोग में आते हैं। प्रतीकात्मकता का क्षेत्र सामान्य रूप से विस्तृत है;
स्वप्न-प्रतीकात्मकता उसका एक छोटा-सा अंश-मात्र है। सारी समस्या पर स्वप्नों
के पहल से विचार करना उचित भी नहीं होगा। और जगह आमतौर से काम आने वाले
बहुत-से प्रतीक या तो स्वप्नों में बिलकुल ही नहीं आते और या बहुत कम आते
हैं। दूसरी ओर, बहुतसे स्वप्न-प्रतीक दूसरे हर क्षेत्र में नहीं मिलते, बल्कि
जैसा कि आप देख चुके हैं, सिर्फ कहीं-कहीं मिलते हैं। हम पर यह असर पड़ता है
कि यह कोई प्राचीन, और अब अप्रचलित भाव-प्रकाशन की रीति होगी, जिसके विभिन्न
टुकड़े विभिन्न क्षेत्रों में, कोई कहीं और कोई कहीं, मामूली हेर-फेर के साथ
बचे हुए हैं। यहां मुझे एक बड़े मनोरंजक पागल रोगी की कल्पना की याद आती है
जो कहता था कि एक 'आद्य भाषा' रही होगी जिसके अवशेष ये सब प्रतीक हैं।
तीसरी बात यह है कि आपको यह महसूस होगा कि ऊपर बताए गए अन्य क्षेत्रों में
होने वाली प्रतीकात्मकता यौन विषयों तक ही सीमित नहीं है। पर स्वप्नों में इन
प्रतीकों का प्रयोग सिर्फ यौन वस्तुओं और सम्बन्धों को सूचित करने के लिए
होता है। इसका कारण बताना भी कठिन है। क्या यह माना जाए कि पहले यौन या
मैथुन-सम्बन्धी अर्थ रखने वाले प्रतीक बाद में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त
हुए और शायद इसी कारण प्रतीकात्मक निरूपण का ह्रास हो गया और निरूपण की दूसरी
रीतियां अपना ली गईं? सिर्फ स्वप्न-प्रतीकात्मकता पर विचार करके इन प्रश्नों
का उत्तर देना स्पष्टतः असम्भव है; हम इतना ही कर सकते हैं कि इस कल्पना को
दृढ़ता से मान रहें कि सच्चे प्रतीकों और मैथुन में विशेष रूप से नज़दीकी
सम्बन्ध है।
इस सिलसिले में हमें हाल में ही एक महत्त्वपूर्ण संकेत एक भाषातत्त्वज्ञ
(अपस्ला के एच० स्पर्बर, जो मनोविश्लेषण से बिलकुल अलग कार्य करते हैं) के इस
विचार से मिला है कि भाषा की उत्पत्ति और परिवर्धन में मैथुन-सम्बन्धी
आवश्यकताओं का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपने लिखा है कि जो सबसे पहली ध्वनि
मनुष्य के मुख से निकली वह अपनी बात कहने का साधन और मैथुन के साथी को बुलाने
का साधन थी और बाद में भाषण के अवयवों का प्रयोग आदिमकाल के मनुष्य द्वारा
किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के साथ होने लगा। यह कार्य तालबद्ध रीति से
दोहराए गए वचनों की ध्वनि के साथ किया जाता था और इसका असर यह होता था कि
मैथुन-सम्बन्धी दिलचस्पी कार्य में बदल जाती थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है
कि आदिमकाल के मनुष्य ने अपने कार्य को मैथुन-सम्बन्धी कार्यों के समान और
उनका स्थानापन्न मानकर सुखदायक बनाया। इसलिए सामाजिक कार्य में प्रयुक्त
शब्दों के दो अर्थ होते थे-एक तो मैथुन-सम्बन्धी कार्य को सूचित करता था और
दूसरा उस परिश्रम को सूचित करता था जिसके तुल्य इसे मान लिया गया। धीरे-धीरे
उस शब्द का मैथुन-सम्बन्धी अर्थ खत्म हो गया। और उनका प्रयोग सिर्फ कार्य के
लिए होने लगा। अनेक पीढ़ियों बाद यही बात नये शब्द के बारे में हुई-वह भी
पहले मैथुन-सम्बन्धी अर्थ का वाचक बना और फिर किसी नये तरह के कार्य के लिए
प्रयोग में आने लगा। इस प्रकार अनेक मूल शब्द बन गए जो सब मैथुन-सम्बन्धी
प्रसंग से पैदा हुए थे पर बाद में अपना मैथुन-सम्बन्धी अर्थ खो बैठे। यदि
उपर्युक्त कथन सही है, तो स्वप्न-प्रतीकों को समझने की एक सम्भावना हमें
दिखाई देने लगती है। हमको समझना चाहिए कि स्वप्नों में, जिनमें उन आदिम
अवस्थाओं का कुछ अंश बाकी है, इतने अधिक मैथुन-सम्बन्धी प्रतीक क्यों होते
हैं, और आमतौर से हथियार और औजार पुरुष के, तथा जिन वस्तुओं और सामान को
बनाया-संवारा जाता है, वे स्त्री के प्रतीक क्यों होते हैं। तब प्रतीकात्मक
सम्बन्ध इसी बात के अवशेष होंगे कि पहले दोनों के लिए एक शब्द प्रयोग होता
था। जिन वस्तुओं का वाचक पहले जननेन्द्रियवाचक शब्द था वे अब स्वप्न में
जननेन्द्रिय की प्रतीक बन सकती हैं।
इसके अतिरिक्त, स्वप्न-प्रतीकात्मकता से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है
कि मनोविश्लेषण क्यों इतना आम दिलचस्पी का विषय बन जाता है, जितना मनोविज्ञान
और मनश्चिकित्सा नहीं बन सकते। मनोविश्लेषण-कार्य विज्ञान की और बहुत-सी
शाखाओं के साथ अच्छी तरह गुंथा हुआ है, और इन शाखाओं की जांच-पड़ताल करने से
बहुत कीमती नतीजे निकल सकते हैं, जैसे पुराणविद्या, भाषातत्त्व और
भाषा-विज्ञान, लोककथाएं, लोकमनोविज्ञान और धर्मशास्त्र। आपको यह जानकर
आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मनोविश्लेषण के आधार पर एक ऐसी पत्रिका का
प्रकाशन आरम्भ हुआ है कि जिसका एकमात्र उद्देश्य इन सम्बन्धों को बढ़ाना है।
मेरा संकेत ईभेगो की ओर है जो सबसे पहले 1912 में प्रकाशित हुई थी और जिसके
सम्पादक हैन्स सैक्श और ओटो रैंक थे। इन दूसरे विषयों के साथ सम्बन्ध रखते
हुए मनोविश्लेषण ने इनसे जितना पाया है उससे अधिक इन्हें दिया है। यह सच है
कि मनोविश्लेषण अपने ही परिणामों की पुष्टि इन दूसरे क्षेत्रों में करता है,
जो बड़ी विचित्र बात मालूम होती है, पर कुल मिलाकर मनोविश्लेषण द्वारा दी हुई
तकनीकी विधियों और दृष्टिकोणों का प्रयोग ही दूसरे क्षेत्रों में सफल सिद्ध
होता है। मनुष्य का मानसिक जीवन मनोविश्लेषण की जांच-पड़ताल के द्वारा ऐसी
व्याख्याएं पेश करता है जो मनुष्य जाति के जीवन की बहुत-सी पहेलियों को हल कर
देती हैं, या कम-से-कम उन्हें ठीक रूप में सामने ले आती हैं।
अब तक मैंने उन परिस्थितियों के बारे में आपको कुछ नहीं बताया जिसमें हम उस
परिकल्पित 'आद्य भाषा' की गहराई में पहुंच सकते हैं, या उस क्षेत्र में पहुंच
सकते हैं जिसमें यह आद्य भाषा अधिकतर जैसी की तैसी मौजूद होती है। जब तक आपको
यह पता न चले तब तक आप सारे विषय का वास्तविक महत्त्व नहीं समझ सकते। मेरा
आशय स्नायुरोगों के क्षेत्र से है। इसकी सामग्री स्नायुरोगियों के लक्षणों और
अभिव्यक्ति की दूसरी रीतियों में मिलती है-इन स्नायुरोगियों के लक्षणों की
व्याख्या और इलाज के लिए ही असल में मनोविश्लेषण की रीति निकाली गई थी।
मेरा चौथा दृष्टिकोण हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हम चले थे, बल्कि
हमें उस मार्ग पर चलाता है जो हमने पहले ही देख लिया है। हमने कहा था कि यदि
स्वप्न की काट-छांट न हो, तो भी स्वप्नों का अर्थ लगाना हमारे लिए कठिन होगा
क्योंकि तब हमारे सामने यह सवाल होगा कि स्वप्नों की प्रतीकात्मक भाषा का
जाग्रत जीवन की भाषा में अनुवाद किया जाए। इस प्रकार प्रतीकात्मकता
स्वप्नविपर्यास में दूसरा और स्वतन्त्र कारण है, जो सेन्सरशिप या काट-छांट के
साथ-साथ होता है, पर यह नतीजा तो सीधा ही है कि सेन्सरशिप को प्रतीकात्मकता
का उपयोग करने में सहूलियत होती है, क्योंकि दोनों का एक ही प्रयोजन होता है
कि स्वप्न को विचित्र और दुर्बोध बना दिया जाए।
स्वप्न के और आगे अध्ययन से हमें विपर्यास के किसी और कारण का पता चलेगा या
नहीं यह अभी हम देखेंगे। पर स्वप्न-प्रतीकात्मकता के विषय को छोड़ने से पहले
मैं इस अजीब तथ्य का उल्लेख एक बार और कर देना चाहता हूं कि इसका शिक्षित
व्यक्तियों में बड़ा प्रबल विरोध हुआ है, यद्यपि पुराणकथाओं, धर्म, कला और
भाषा मे असंदिग्ध रूप से प्रतीकात्मकता मौजद है। क्या यहां भी यही सम्भव नहीं
है कि मैथुन से इसका सम्बन्ध ही इसका कारण हो?
|
|||||


 i
i