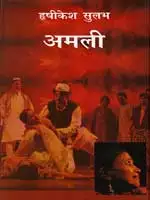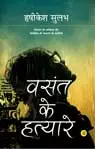|
नाटक-एकाँकी >> अमली अमलीहृषीकेश सुलभ
|
252 पाठक हैं |
|||||||
अमली में हास्य और रोमांस के क्षणों के बीच शोषण और अत्याचार के विभिन्न चरित्रों को उभारा है
Amli Yuvaon Ke Liye - A Hindi Book - by Hrishikesh Sulabh
हृषीकेश सुलभ ने लोकनाट्य शैली बिदेसिया में अन्तर्निहित शक्ति को पहचाना और उसे आधुनिक रंगदृष्टि के साथ जोड़कर उसकी स्थानीयता का अतिक्रमण कर और उसके स्वरूप तथा संरचना में बदलावकर नई अर्थ सम्भावनाएँ पैदा कीं। इस अर्थ में उन्होंने हमारी पश्चिमाभिमुखी प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया और साथ ही हिन्दी रंगदृष्टि को उसकी जड़ों से जोड़ रखकर भी एक विशिष्ट प्रकार की आधुनिकता प्रदान की और उसे फिर सन्दर्भवान बनाया। अन्तर्वस्तु के धरातल पर यथार्थ अंकन से जोड़ने के साथ ही भिखारी ठाकुर की नाट्यकल्पना और रंगयुक्तियों को सुरक्षित रखते हुए भी उसे संस्कारित किया और उसे एक मानक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की। उन्होंने एक भारतीय पारम्परिक रंगदृष्टि का नया आयाम प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
अमली में हास्य और रोमांस के क्षणों के बीच शोषण और अत्याचार के विभिन्न चरित्रों को उभारा है। कथा में एक अनिवार्य तनाव के द्वारा हमारे सामाजिक विद्रूप के चेहरों की परत-दर-परत उघड़ती है और हमारे समय तथा समाज की जटिल और विडम्बनापूर्ण स्थितियों का बड़ी बेचैनी तथा तल्ख़ी के साथ सघन रूप से यह कृति अहसास कराती है। केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा भुवनेश्वर में सफल मंचन।
बिहार की विदेसिया शैली में लिखित अमली नाटक आधुनिक भी है और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी। नाटक में प्रचुर पारम्परिक गीतों एवं नृत्यों का समन्वय किया गया है जो नाटक के कथ्य एवं विदेसिया शैली दोनों के अभिन्न अंग हैं। सूत्रधार और गड़बड़िया जैसे पात्र अमली को एक ओर संस्कृत परम्परा से जोड़ते हैं तो दूसरी ओर लोक परम्परा से। नाटक रोचक होने के साथ ही हमें सोचने को मजबूर करता है और कहीं वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति पाने-दिलाने के लिए उन्मुख करता है। टोटल थिएटर को रूपायित करनेवाली हृषीकेश सुलभ की यह कृति हिन्दी नाट्य साहित्य एवं रंगमंच की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
अमली में हास्य और रोमांस के क्षणों के बीच शोषण और अत्याचार के विभिन्न चरित्रों को उभारा है। कथा में एक अनिवार्य तनाव के द्वारा हमारे सामाजिक विद्रूप के चेहरों की परत-दर-परत उघड़ती है और हमारे समय तथा समाज की जटिल और विडम्बनापूर्ण स्थितियों का बड़ी बेचैनी तथा तल्ख़ी के साथ सघन रूप से यह कृति अहसास कराती है। केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा भुवनेश्वर में सफल मंचन।
बिहार की विदेसिया शैली में लिखित अमली नाटक आधुनिक भी है और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी। नाटक में प्रचुर पारम्परिक गीतों एवं नृत्यों का समन्वय किया गया है जो नाटक के कथ्य एवं विदेसिया शैली दोनों के अभिन्न अंग हैं। सूत्रधार और गड़बड़िया जैसे पात्र अमली को एक ओर संस्कृत परम्परा से जोड़ते हैं तो दूसरी ओर लोक परम्परा से। नाटक रोचक होने के साथ ही हमें सोचने को मजबूर करता है और कहीं वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति पाने-दिलाने के लिए उन्मुख करता है। टोटल थिएटर को रूपायित करनेवाली हृषीकेश सुलभ की यह कृति हिन्दी नाट्य साहित्य एवं रंगमंच की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
–प्रतिभा अग्रवाल
दरअसल अमली भारत के किसी भी पिछड़े प्रान्त के किसी भी ज़िले के किसी भी गाँव में मिल जाएगी। इस मायने में अमली समकालीन समाज की जीवन्त पुनर्रचना है। अमानवीय अर्थतंत्र और सामन्ती समाज की विद्रूपताओं में पिसते व्यापक समाज की दारुण स्थितियाँ अमली को एक समकालीन रचना बनाती हैं। सूत्रधार, विदूषक और समाजी ब्रेख़्त के थियेटर की शैली में यातना और बेचैनी के आवेगों में बहते नाट्य-दर्शकों की चेतना को झकझोरते हैं और उन्हें नाटक के बजाय समाज की विराट सच्चाइयों से जोड़ते हैं।
–उर्मिलेश, नवभारत टाइम्स, पटना, 1 जनवरी, 1988
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हिन्दी रंगमंच का नवोन्मेष तो हुआ, पर उसमें भारतीय रंग परम्परा विलुप्त-सी रही। पिछले-दो-तीन दशकों से भारतीय रंगदृष्टि की तलाश चल रही है। इस दिशा में एक सार्थक क़दम है बिदेसिया शैली में हृषीकेश सुलभ लिखित अमली नाटक का मंचन। –
श्रीप्रकाश, दैनिक हिन्दुस्तान, पटना, जुलाई 1988
अमली उस पीड़ित समाजकी प्रतिनिधि है जिसे सत्ता, सम्पत्ति और षड्यंत्र ने सदा लूटा है।
–जनसत्ता, कोलकाता, 26 दिसम्बर, 1991
हृषीकेश सुलभ द्वारा लिखिति इस नाटक का मंचन वर्तमान में राँची रंगमंच के ठहरी हुई झील में एक बड़ा पत्थर था। यह बहुख्यात नाटक भिखारी ठाकुर के बिदेसिया से उदभुत शैली पर आधारित प्रयोग है। सीधे-सादे कथ्य के साथ जुड़ा शिल्प इस नाटक की मूल ताक़त है।
–प्रियदर्शन, राँची एक्सप्रेस, राँची, 25 जून, 1992
अमली में बिदेसिया शैली की सार्थक रंगयुक्तियों का नए तरीके से कुशलता के साथ इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी रंगमंच के भीतर यह एक नया प्रयोग था। इस प्रयोग ने पटना रंगमंच को नया आकाश दिया।
–चंद्रेश्वर, दैनिक हिन्दुस्तान, पटना, 17 मार्च, 1993
[हारमोनियम, ढोलक, हुड़का, ताशा, बाँसुरी, झाल और करताल आदि वाद्यों के साथ नाटक के सारे पात्र मंच पर प्रवेश करते हैं। मंच के पिछले हिस्से पर दर्शकों के आमने-सामने बैठते हैं। मंच के बदले चौकोर शामियाना के नीचे एक तरफ की धरती का सुविधानुसार उपयोग किया जा सकता है। समाजियों (कोरस) सहित सारे पात्रों के बैठने के बाद उनके आगे की धरती या मंच का उपयोग अभिनय-स्थल के रूप में होगा। मंच पर प्रवेश के बाद सब शीश झुकाकर अभिवादन करते हुए बैठ जाते हैं। समाजी अपने वाद्य-यन्त्रों को मिलाते हैं और सुमिरन गाते हैं। सुमिरन में नाटक के सारे पात्र शामिल होते हैं।]
समाजी : सुमिरन
आहो गननायक देवता,
आहो गननायक, आहो गननायक देवता।
सुमिरन में होखऽ ना सहाय, आहो गननायक देवता।
शंकर सुवन भवानी के नन्दन, आहो गननायक देवता।
लडुवा के भोगवा बा तोहार, आहो गननायक देवता।
हथिया के सूँड़वा पवलऽमूस के सवरिया,
मानुस शरीरवा बा तोहार, आहो गननायक देवता।
सुमिरन में होखऽना सहाय, आहो गननायक देवता।
आहो गननायक, आहो गननायक देवता।
सुमिरन में होखऽ ना सहाय, आहो गननायक देवता।
शंकर सुवन भवानी के नन्दन, आहो गननायक देवता।
लडुवा के भोगवा बा तोहार, आहो गननायक देवता।
हथिया के सूँड़वा पवलऽमूस के सवरिया,
मानुस शरीरवा बा तोहार, आहो गननायक देवता।
सुमिरन में होखऽना सहाय, आहो गननायक देवता।
[नाट्यदल अन्य पारम्परिक वन्दना का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुमिरन समाप्त होते ही सूत्रधार उठता है। वह पारम्परिक वेशभूषा (घाघरानुमा पेशवाज, तंग मोहरी का पाजामा या धोती-मिरजई और कमरबन्द, दुपट्टा तथा पगड़ी) में है। वह मंच के अगले भाग में आता है और लोकधुन पर नृत्य के टुकड़े प्रस्तुत करता है। नृत्य के बाद सिर झुकाकर दर्शकों को नमस्कार करता है।]
सूत्रधार : दूर-दूर से पधारे दरसक देवता लोगन को बारा-बार परनाम। आज आप सब नाच-तमासा देखे खातिर पधारे हैं। नाच-तमासा से दुखी मन को सुख मिलता है। अगर देखनिहार की ई सुख मिल जावे, तो नाच-तमासा वाले लोगन की मेहनत सुफल। पर एक अरज है हमारी कि...ई पल का सुख...छिन भर की हँसी...मायाजाल है।
सूत्रधार : दूर-दूर से पधारे दरसक देवता लोगन को बारा-बार परनाम। आज आप सब नाच-तमासा देखे खातिर पधारे हैं। नाच-तमासा से दुखी मन को सुख मिलता है। अगर देखनिहार की ई सुख मिल जावे, तो नाच-तमासा वाले लोगन की मेहनत सुफल। पर एक अरज है हमारी कि...ई पल का सुख...छिन भर की हँसी...मायाजाल है।
[पारम्परिक निरगुन]
काहे, गइले मायापुर बाजार रे अनाड़ी मनवा।
एहिजा बइठल ठग दुकानदार रे अनाड़ी मनवा।।
दिन देख चलिह ऽरतिया बितरहऽ तुहूँ जाग।
डेगे-डेगे चोर-बटमार रे अनाड़ी मनवा।।
एहिजा बइठल ठग दुकानदार रे अनाड़ी मनवा।।
दिन देख चलिह ऽरतिया बितरहऽ तुहूँ जाग।
डेगे-डेगे चोर-बटमार रे अनाड़ी मनवा।।
तो भइया लोग ! नाच-तमासा से घर लौट के फिर दुख...फिर माया...फिर झंझट। सो, देवतासरूप दरसक लोग। आज के तमासा में सुख ना है...हँसी ना है। आज के तमासा में जिनगी के साँच-साँच किस्सा है।
सिरी गनेस पद नाऊँ माथा।
तब गाऊ अमली के गाथा।।
तब गाऊ अमली के गाथा।।
भाई लोग ! आज के तमासा में अमली का किस्सा है।
नावत बानी सब केरू माथा।
चित दे सुनहु अमली के गाथा।।
चित दे सुनहु अमली के गाथा।।
अमली का किस्सा केवल हमारे गाँव का किस्सा ना है। हर गाँव में है अमली अउर देस के हर गाँव में है अमली का किस्सा।...जिला सीवान का गाँव मनरौली। गाँव मनरौली की अमली। मनरौली के अछूत-हरिजन परिवार की अमली। बुधिया के टुटडे घर के आँगन में मंगल-बधाव बज रहा था,...गीत-गवनई चल रहा था।
[बुधिया कुछ औरतों के साथ बेटा और बहू के स्वागत की रस्म कर रही है। सूत्रधार सहित सारे समाजी भी इस समूहन-दृश्य में शामिल होते हैं और गायन में साथ देते हैं।]
[बुधिया कुछ औरतों के साथ बेटा और बहू के स्वागत की रस्म कर रही है। सूत्रधार सहित सारे समाजी भी इस समूहन-दृश्य में शामिल होते हैं और गायन में साथ देते हैं।]
विवाह-गीत
आवेले कवन बाबू हथिया से घोड़वा हे,
आवेले कवन दुलहा बहू लेहले डोलिया हे।
आवेले रमेसर बाबू हथिया से घोड़वा है,
आवेले रमेसर दुलहा बहू लेहले डोलिया हे।
पहिरीं ना बुधिया माई इयरी से पियरी है,
बहुआ परिछीं घरे मंगल गावहु हे।
सासऽ के अँखियाँ लागेली मधुमखिया हे,
निरखि-निरखि बिहँसे बहू रसरंगिलिया हे।
आवेले कवन दुलहा बहू लेहले डोलिया हे।
आवेले रमेसर बाबू हथिया से घोड़वा है,
आवेले रमेसर दुलहा बहू लेहले डोलिया हे।
पहिरीं ना बुधिया माई इयरी से पियरी है,
बहुआ परिछीं घरे मंगल गावहु हे।
सासऽ के अँखियाँ लागेली मधुमखिया हे,
निरखि-निरखि बिहँसे बहू रसरंगिलिया हे।
[निर्देशक स्थानीय रस्म-रिवाज के अनुसार किसी अन्य गीत का भी उपयोग कर सकते हैं। गीत समाप्त होते ही प्रकाश सिमट जाता है और समाजियों पर पूर्ववत् केन्द्रित होता है।]
समाजी एक : भाई ! खुशी-खुशी विवाह निबट गया। कनिया घर आ गई अउर किस्सा खत्म हो गया ?
सूत्रधार : ना भाई, किस्सा तो अब चालू हुआ है।
समाजी दो : तो आगे का किस्सा कवन बयान करेगा ?
सूत्रधार : सब लोग मिल-जुलकर करेंगे भाई। एतनी बड़ी, एतनी भारी जिनगी का किस्सा अकेले हमरे बस का ना है।...तो भाई दरसक देवता लोग...! दिन बीता...मास बीते...बीत गया विवाह का उछाह। धतूरे के फूल जइसी मदमाती जवानी का नशा उतरते देर ना लगी। विवाह के बाद नयका जोड़े की देह फूलती-फलती है...लहराती है खेत की जवान फसल की तरह। पर रमेसर-अमली के साथ अइसा कुछ भी न हुआ। जइसी सूखी-कँटीली जिनगी पहिले थी, वइसी ही रही। साँच कहें तो...।
समाजी एक : अरे भाई, खाली किस्सा-कथा सुनाओगे कि आगे भी दिखाओगे ?
समाजी दो : गप्प में सगरी रात बीत गई। जल्दी करो, जल्दी।
सूत्रधार : दिखा रहे हैं भाई।
समाजी एक : अरे तुम तो बस गपियाए चले जा रहे हो।
सूत्रधार : लो भइया, देखो।
[मंच के एक भाग में प्रकाश होता है। अमली जाँता से अन्य पीस रही है। थोड़ी
समाजी एक : भाई ! खुशी-खुशी विवाह निबट गया। कनिया घर आ गई अउर किस्सा खत्म हो गया ?
सूत्रधार : ना भाई, किस्सा तो अब चालू हुआ है।
समाजी दो : तो आगे का किस्सा कवन बयान करेगा ?
सूत्रधार : सब लोग मिल-जुलकर करेंगे भाई। एतनी बड़ी, एतनी भारी जिनगी का किस्सा अकेले हमरे बस का ना है।...तो भाई दरसक देवता लोग...! दिन बीता...मास बीते...बीत गया विवाह का उछाह। धतूरे के फूल जइसी मदमाती जवानी का नशा उतरते देर ना लगी। विवाह के बाद नयका जोड़े की देह फूलती-फलती है...लहराती है खेत की जवान फसल की तरह। पर रमेसर-अमली के साथ अइसा कुछ भी न हुआ। जइसी सूखी-कँटीली जिनगी पहिले थी, वइसी ही रही। साँच कहें तो...।
समाजी एक : अरे भाई, खाली किस्सा-कथा सुनाओगे कि आगे भी दिखाओगे ?
समाजी दो : गप्प में सगरी रात बीत गई। जल्दी करो, जल्दी।
सूत्रधार : दिखा रहे हैं भाई।
समाजी एक : अरे तुम तो बस गपियाए चले जा रहे हो।
सूत्रधार : लो भइया, देखो।
[मंच के एक भाग में प्रकाश होता है। अमली जाँता से अन्य पीस रही है। थोड़ी
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i