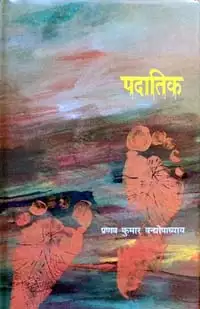|
उपन्यास >> अधूरे-से कुछ दिन अधूरे-से कुछ दिनप्रणव कुमार वन्द्योपाध्याय
|
49 पाठक हैं |
|||||||
वह शख्स था तो मुसलमान लेकिन उसके ही घर में पनाह मिली थी हिंदू दुकानदार को...
भारत के विभाजन के समय की कहानी है अधूरे-से कुछ दिन। पूर्वी बंगाल
(बांग्लादेश) के उखाड़-पछाड़ के बीच हिंदुओं और मुसलमानों की त्रासद
स्थिति में एक छोटे हिंदू दुकानदार का घर उजड़ गया। सिर्फ वही अंततः जीवित
रह गया था। बचाया था, अक अकेले रिक्शेवाले ने। वह शख्स था तो मुसलमान
लेकिन उसके ही घर में पनाह मिली थी हिंदू दुकानदार को।
अपनी इच्छा के विरुद्ध वह व्यक्ति अंततः जरूर कोलकाता आ खड़ा हुआ, लेकिन उसके पांवों के नीचे शायद कोई ज़मीन थी ही नहीं। कोलकाता उस समय पूर्वी बंगाल से आए लोगों से दहक रहा था।
आखिर में पूर्वी बंगाल का वह पुरुष आसाम पहुंच गया। बहुत कुछ सोच विचार कर नहीं, खड़े होने लायक थोड़ी जगह पाने के लिए। वह फिर कुछ समय बाद पांडू चला आया तो दो बच्चों को पढ़ाते हुए शायद अपने भीतर बहुत दूर तक चला गया था। लेकिन वह परिवार इसके कुछ समय बाद आसाम छोड़कर गोरखपुर के लिए रवाना हो गया। रेलवे की सरकारी नौकरी में यह एक आम बात थी।
पूर्वी बंगाल से आया व्यक्ति अब पांडू से बाहर तो चला नहीं गया, लेकिन एकदम अकेला हो गया था। अकेला और निर्बल।
इस कथा के माध्यम से प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय ने एक नयी ज़मीन की खोज की है, जिसमें एक ओर मनुष्य की त्रासदी है और दूसरी ओर है उसके नये रिश्ते। आसाम की पटभूमि में हिंदी का पहला उपन्यास।
अपनी इच्छा के विरुद्ध वह व्यक्ति अंततः जरूर कोलकाता आ खड़ा हुआ, लेकिन उसके पांवों के नीचे शायद कोई ज़मीन थी ही नहीं। कोलकाता उस समय पूर्वी बंगाल से आए लोगों से दहक रहा था।
आखिर में पूर्वी बंगाल का वह पुरुष आसाम पहुंच गया। बहुत कुछ सोच विचार कर नहीं, खड़े होने लायक थोड़ी जगह पाने के लिए। वह फिर कुछ समय बाद पांडू चला आया तो दो बच्चों को पढ़ाते हुए शायद अपने भीतर बहुत दूर तक चला गया था। लेकिन वह परिवार इसके कुछ समय बाद आसाम छोड़कर गोरखपुर के लिए रवाना हो गया। रेलवे की सरकारी नौकरी में यह एक आम बात थी।
पूर्वी बंगाल से आया व्यक्ति अब पांडू से बाहर तो चला नहीं गया, लेकिन एकदम अकेला हो गया था। अकेला और निर्बल।
इस कथा के माध्यम से प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय ने एक नयी ज़मीन की खोज की है, जिसमें एक ओर मनुष्य की त्रासदी है और दूसरी ओर है उसके नये रिश्ते। आसाम की पटभूमि में हिंदी का पहला उपन्यास।
अधूरे-से कुछ दिन
नदी के किनारे बांस की चटाई से बने दो कमरों के दरबे रेलवे में काम करने
वाले लोगों को मिले हैं। दफ़्तर में काम करनेवाला बाबू हो या चौकीदार,
सबको बराबर आकार का ही घर हासिल हुआ है। रेलवे में नौकरी और नौकरी के साथ
घर कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन बात आज की नहीं है। सन् सैंतालीस में
भारत आज़ाद हुआ तो कई मुसलमान पाकिस्तान चले गये और ढेर सारे हिंदू इस पार
आकर दाल-भात के साथ बसेरे का कोई न कोई इंतज़ाम करते रहे। बस गये कहना सच
नहीं होगा। वे सब बस इधर चले आये। ज़्यादातर आनेवालों के हाथ ख़ाली थे और
किसी तरह जान बचाकर एक धोती या साड़ी पहने वे बस चले आये थे। वे नहीं
जानते थे कि अब अगली रात कैसे गुज़रेगी ?
प्रबोधबाबू आने वाले लोगों में एक थे। पहले वह चटगांव में एक दुकान चलाते थे। घर-गृहस्थी की छोटी-छोटी चीज़ों की एक मामूली-सी दुकान। उनका और घरवालों का गुज़ारा उसी से चलता था। लेकिन जब वह पाकिस्तान छोड़ कर भारत आ गये तो अकेले थे। घर के तमाम लोग एक ही रात ख़त्म कर दिये गये थे। प्रबोधबाबू को मुसलमानों ने लाश समझ कर ज़्यादा कुचल नहीं दिया तो रात के अंधेरे में होश आने पर वह एकदम ख़ामोश बैठे रहे। पूरा जिस्म सुन्न हो गया था।
आख़िर में सुबह होने को हुई तो अचानक सामने राशिद मियां आ खड़ा हुआ। साठ-पैंसठ या सत्तर की उम्र का एक सांवला आदमी। सिर में किसी ज़माने में बाल तो थे लेकिन अब इस पर बस यक़ीन भर किया जा सकता है। राशिद चटगांव में रिक्शा चला कर अपना गुज़र-बसर कर लेता है। कई बार वह प्रबोधबाबू की दुकान से चाय की पत्ती के अलावा गुड़ वगैरह कुछ न कुछ ख़रीद लेता और सामने के बांस के मोढ़े पर बैठ कर ज़्यादा नहीं तो कम से कम घंटा भर छत्तीस तरह की बातें सुन लेता। वह ज़्यादा कुछ पूछ तो नहीं पाता, लेकिन बाबू की बातें सुन कर दिमाग़ में बिठाने की कोशिश करता रहता। उसे मालूम था कि बाबू तरह-तरह की किताबें उलटते रहते। दुकान में बैठ कर गुड़-तेल बेचने के अलावा जब भी घड़ी-दो घड़ी मिलती, कोई न कोई किताब के पन्ने वह ज़रूर उलट-पलट लेते।
लाशों के बीच प्रबोधबाबू को देख कर राशित मियां की आंखें भर आयीं और गला रुंध-सा गया।
प्रबोधबाबू की आंखों में शायद कोई दृष्टि नहीं थी। सिर्फ़ एक उचाट ख़ालीपन था। पता नहीं चलता कि यह ख़ालीपन कहां से शुरू हो कर किस मुक़ाम तक पहुंचता है।
राशिय मियां ने कंधे पर पड़ा अंगोछा अपनी गीली आंखों पर फेर लिया। आसापास के तमाम घर तुड़-मुड़ कर ज़मीन पर फैले पड़े थे। लग ही नहीं रहा था कि इनमें कभी कोई बसता भी था। किसी भी घर पर पक्की छत नहीं थी। छत की जगह या तो खपरैल थे या धान के सूखे पौधे। उस ज़माने में ईंट की छत एक आध लोगों की ही होती थी। ज़ाहिर है, प्रबोधकुमार ऐसे लोगों में कभी नहीं थे।
राशिद मियां थोड़ा आगे बढ़ा और आहिस्ते से अपनी दाहिनी हथेली प्रबोधबाबू के कंधे पर रखी।
चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा था, उसके साथ था सन्नाटा। कोई आसपास नहीं था।
राशिद ने अब और इंतज़ार नहीं किया। उसने प्रबोधबाबू से कुछ भी नहीं कहा और उनके जिस्म को कंधे पर डाल लिया।
प्रबोधबाबू को शायद कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। कहने को वह ज़िंदा ज़रूर थे, लेकिन थे एक मुर्दे के बराबर ही।
अपने घर में ला कर राशिद प्रबोधबाबू की देखभाल करता रहा। इस तरह शायद दसेक दिन गुज़रे थे। उनमें अब होश-ओ-हवास थोड़ा-बहुत आ गया। तब एक दिन राशिद समझ गया कि हालत अब बद से बदतर हो रही है। लिहाज़ा अब बाबू का, उस पार के बंगाल जाने के अलावा, कोई रास्ता नहीं था। बहुत सोचने-समझने के बाद राशिद मियां इसी नतीजे पर पहुंचा था।
तब एक शाम चुप बैठे बाबू के सामने राशिद ने कह ही दिया, ‘‘एक बार कहूं बाबू ? वैसे मुझे हिम्मत तो नहीं होता।’’
प्रबोधबाबू निरुत्तर थे।
‘‘कहते हुए मेरा कलेजा तो फटता है, लेकिन यहां शायद अब आपको बचा नहीं पाऊंगा। चारों तरफ़ सिर्फ़ ज़हरीले सांस फैले पड़े हैं।’’
प्रबोधबाबू चुप रहे। जवाब देने लायक़ कुछ सूझ नहीं रहा था।
‘‘सुनने में आया, यहां से ट्रकों पर बैठ कर लोग ढाका की तरफ़ निकल जायेंगे और वहां से स्यालदा की रेलगाड़ी पकड़ लेंगे।’’ बहुत डरते हुए राशिद बोला। उसका गला कांप रहा था।
‘‘उधर तो मेरा कोई भी नहीं है। कौन पहचानेगा मुझे ?’’ प्रबोधबाबू की अधूरी-सी आवाज़ में सवाल था। लड़खड़ाता-सा।
‘‘लेकिन यहां कि मिट्टी तो अब बदल गयी है, बाबू। लगता है, हिंदुओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची। मैं तो यही देख रहा हूं।’’
‘‘तुम पागल हो, मियां ? हमारे बाप-दादा जिस ज़मीन को स्वर्ग से कम नहीं मानते थे, वहां से तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें भी रिश्तेदार मानता हूं, मियां। हमारे घर के तमाम लोग तो ख़त्म हो गये लेकिन फिर भी मेरा मन यहां से चले जाने को तैयार नहीं है।’’ प्रबोधबाबू की आंखों से दो नदियां बह रही थीं।
‘‘मेरे पास बहुत बुरी ख़बर है, बाबू।’’
‘‘कौन-सी नयी बुरी ख़बर, मियां ? हमें यहां के लोग काट डालेंगे, यही न ?’’
‘‘बिहारी मुसलमानों ने बंगाल के मुसलमानों का दिमाग ज़हर से भर दिया है। अब वे कहते हैं कि पूर्वी बंगाल के एक-एक हिंदू को ज़मीन के नीचे दफ़ना दिया जायेगा।’’
‘‘इस पूर्वी बंगाल के अलावा मैं तो कोई और मुल्क नहीं जानता। क़िस्मत अगर यही रही, चलो मैं भी यहीं ख़त्म हो जाऊंगा। कहीं बाहर जा कर मरने से यही बेहतर होगा।’’
‘‘ऐसा न बोलें, बाबू। आप तो बड़े आदमी हैं। किताब वग़ैरह पढ़ कर तो आप ढेर सारा समझ लेते हैं। दुनिया को आप जितना समझते हैं, उतना और कौन समझेगा ?’’
‘‘चलो, अगर मैं थोड़ा समझता हूं तो वही सही, लेकिन तुम भी तो पढ़े-लिखे बिना भी कुछ न कुछ समझ ही लेते हो। हर किसी में यह गुण थोड़े ही होता है ?’’
‘‘आप तो हंसी-ठट्ठा कर रहे हैं। असल में हम तो बुर्बक हैं, बाबू। लेकिन अच्छा है कि मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है, वरना वह भी एक और बुर्बक ही रह जाता।’’ राशिद की आवाज़ में थोड़ी कंपकंपी उतर आयी थी।
प्रबोधबाबू ने पूछा, ‘‘तुम्हें जानता तो इतने दिनों से हूं, लेकिन कभी नहीं जानाता कि तुम्हारे साथ और हैं कौन-कौन आख़िरकार ? लेकिन अब देख रहा हूं, तुम्हारे इस दरबे में कोई और रहता भी नहीं है।’’
राशिद चुप हो गया।
प्रबोधबाबू ने कहा, ‘‘कुछ बोलोगे नहीं, मियां ?’’
‘‘बोलने लायक़ अब रहा ही क्या है, बाबू ? सब कुछ तो कब का ख़त्म हो गया। अब तो मैं भूल भी गया अपने बारे में।’’
प्रबोधबाबू ने कुछ नहीं कहा। आंखें कहीं दूर चली गयी थीं।
कुछ देर बाद राशिद बोला, ‘‘आप तो चुप रह कर बहुत कुछ कह देते हैं, बाबू। मैं बुर्बक तो हूं लेकिन थोड़ा-बहुत समझ ही लेता हूं।’’
प्रबोधबाबू ने जवाब नहीं दिया।
‘‘चलिए, अब बता ही देता हूं।’’ राशिद मियां बोला, ‘‘अब तो मेरी उम्र पैंसठ या सत्तर ज़रूर हो गयी है, लेकिन कभी मैं भी बाईस साल का एक लड़का था। जब बिमला को पहली बार देखा तो सिर फिर गया था। बिमला थी तो हिंदू मल्लाहों की बेटी, लेकिन वह मुसलमान बन गयी और मुझसे उसका निकाह हो गया। निकाह के बाद अपनी औरत के साथ मैं ढाका की एक गली में बहुत ख़ुश रह रहा था। लेकिन सिर्फ़ चार महीने। इस बीच मेरी औरत के पैर भारी हो गये थे और मैं जाने क्या-क्या ख़्वाब देखने लगा।’’ राशिद का गला काफ़ी भारी हो गया था।
प्रबोधबाबू थोड़ा-बहुत समझ गये कि हिंदू-मुसलमान की शादी का अंजाम आख़िर क्या हुआ होगा।
कुछ देर चुप रहने के बाद राशिद मियां बोला, ‘‘कोई नयी बात नहीं है, बाबू। ऐसी बातें मुझसे पहले तो हुई ही हैं, आगे भी होती रहेंगी। आप जानते हैं न, ढाका के शाखारी (शंख की चूड़ी बनाने वाले) बहुत मशहूर हैं। लेकिन लोग उनसे डरते भी हैं। बिहारी मुसलमान तो उन्हें देखते ही भाग खड़े होते हैं। मैं दो दिनों के लिए काम से चटगांव आया था तो मेरी बीवी को चार हिंदू शाखारी जाकर ख़त्म कर आये। तब से मैं कभी ढाका नहीं जा पाया। मेरी बीवी चील-कौओं का खाना बन गया और उसका साथ साथ पल रहा पेट का बच्चा भी। तब से मैं चटगांव में ही रह रहा हूं। बाबू, बस इतनी भर मेरी कहानी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं।’’
प्रबोधबाबू आसमान की तरफ़ देख रहे थे। उन्होंने आंखें बिना फेरे ही मियां से कहा, ‘‘इतना प्यार था बीवी से ?’’ वैसे दोनों जानते थे, यह कोई सवाल नहीं था।
राशिद ने उत्तर नहीं दिया।
‘‘तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी बहुत लंबी है, मियां। शायद उसकी लंबाई का अंदाज़ा किसी को भी न हो।’
‘‘है ही कौन मेरा, जो बैठ कर अंदाज़ा लगायेगा, बस मैं एक बैलगाड़ी भर हूं, जो जैसे-तैसे चल रही है।’’
‘‘तुम्हारे अंदर भोलोबसा (प्रेम) बहुत है, मियां। यह मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं चला। वरना तुम घर तो बसा ही लेते। इससे अलग तो कुछ भी तुमने नहीं मांगा था।’’
राशिद हंसा, ‘‘आप बोलेत क्या हैं बाबू, कई बार तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। मान लेता हूं, वक़्त आने पर शायद कभी न कभी मतलब थोड़ा-बहुत शायद पकड़ लूं।’’
प्रबोधबाबू ने सिलसिला एकदम से बदल दिया था बोले, ‘‘मुझे अब रहने यहीं दो। उस पार के बंगाल भेज कर तुम्हें क्या मिलेगा, मियां ? मैं अब जिऊंगा भी कितना ? दो साल या चार साल ? कुछ भी हो, मुझे तो अब यहीं रहने दो।’’
प्रबोधबाबू आने वाले लोगों में एक थे। पहले वह चटगांव में एक दुकान चलाते थे। घर-गृहस्थी की छोटी-छोटी चीज़ों की एक मामूली-सी दुकान। उनका और घरवालों का गुज़ारा उसी से चलता था। लेकिन जब वह पाकिस्तान छोड़ कर भारत आ गये तो अकेले थे। घर के तमाम लोग एक ही रात ख़त्म कर दिये गये थे। प्रबोधबाबू को मुसलमानों ने लाश समझ कर ज़्यादा कुचल नहीं दिया तो रात के अंधेरे में होश आने पर वह एकदम ख़ामोश बैठे रहे। पूरा जिस्म सुन्न हो गया था।
आख़िर में सुबह होने को हुई तो अचानक सामने राशिद मियां आ खड़ा हुआ। साठ-पैंसठ या सत्तर की उम्र का एक सांवला आदमी। सिर में किसी ज़माने में बाल तो थे लेकिन अब इस पर बस यक़ीन भर किया जा सकता है। राशिद चटगांव में रिक्शा चला कर अपना गुज़र-बसर कर लेता है। कई बार वह प्रबोधबाबू की दुकान से चाय की पत्ती के अलावा गुड़ वगैरह कुछ न कुछ ख़रीद लेता और सामने के बांस के मोढ़े पर बैठ कर ज़्यादा नहीं तो कम से कम घंटा भर छत्तीस तरह की बातें सुन लेता। वह ज़्यादा कुछ पूछ तो नहीं पाता, लेकिन बाबू की बातें सुन कर दिमाग़ में बिठाने की कोशिश करता रहता। उसे मालूम था कि बाबू तरह-तरह की किताबें उलटते रहते। दुकान में बैठ कर गुड़-तेल बेचने के अलावा जब भी घड़ी-दो घड़ी मिलती, कोई न कोई किताब के पन्ने वह ज़रूर उलट-पलट लेते।
लाशों के बीच प्रबोधबाबू को देख कर राशित मियां की आंखें भर आयीं और गला रुंध-सा गया।
प्रबोधबाबू की आंखों में शायद कोई दृष्टि नहीं थी। सिर्फ़ एक उचाट ख़ालीपन था। पता नहीं चलता कि यह ख़ालीपन कहां से शुरू हो कर किस मुक़ाम तक पहुंचता है।
राशिय मियां ने कंधे पर पड़ा अंगोछा अपनी गीली आंखों पर फेर लिया। आसापास के तमाम घर तुड़-मुड़ कर ज़मीन पर फैले पड़े थे। लग ही नहीं रहा था कि इनमें कभी कोई बसता भी था। किसी भी घर पर पक्की छत नहीं थी। छत की जगह या तो खपरैल थे या धान के सूखे पौधे। उस ज़माने में ईंट की छत एक आध लोगों की ही होती थी। ज़ाहिर है, प्रबोधकुमार ऐसे लोगों में कभी नहीं थे।
राशिद मियां थोड़ा आगे बढ़ा और आहिस्ते से अपनी दाहिनी हथेली प्रबोधबाबू के कंधे पर रखी।
चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा था, उसके साथ था सन्नाटा। कोई आसपास नहीं था।
राशिद ने अब और इंतज़ार नहीं किया। उसने प्रबोधबाबू से कुछ भी नहीं कहा और उनके जिस्म को कंधे पर डाल लिया।
प्रबोधबाबू को शायद कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। कहने को वह ज़िंदा ज़रूर थे, लेकिन थे एक मुर्दे के बराबर ही।
अपने घर में ला कर राशिद प्रबोधबाबू की देखभाल करता रहा। इस तरह शायद दसेक दिन गुज़रे थे। उनमें अब होश-ओ-हवास थोड़ा-बहुत आ गया। तब एक दिन राशिद समझ गया कि हालत अब बद से बदतर हो रही है। लिहाज़ा अब बाबू का, उस पार के बंगाल जाने के अलावा, कोई रास्ता नहीं था। बहुत सोचने-समझने के बाद राशिद मियां इसी नतीजे पर पहुंचा था।
तब एक शाम चुप बैठे बाबू के सामने राशिद ने कह ही दिया, ‘‘एक बार कहूं बाबू ? वैसे मुझे हिम्मत तो नहीं होता।’’
प्रबोधबाबू निरुत्तर थे।
‘‘कहते हुए मेरा कलेजा तो फटता है, लेकिन यहां शायद अब आपको बचा नहीं पाऊंगा। चारों तरफ़ सिर्फ़ ज़हरीले सांस फैले पड़े हैं।’’
प्रबोधबाबू चुप रहे। जवाब देने लायक़ कुछ सूझ नहीं रहा था।
‘‘सुनने में आया, यहां से ट्रकों पर बैठ कर लोग ढाका की तरफ़ निकल जायेंगे और वहां से स्यालदा की रेलगाड़ी पकड़ लेंगे।’’ बहुत डरते हुए राशिद बोला। उसका गला कांप रहा था।
‘‘उधर तो मेरा कोई भी नहीं है। कौन पहचानेगा मुझे ?’’ प्रबोधबाबू की अधूरी-सी आवाज़ में सवाल था। लड़खड़ाता-सा।
‘‘लेकिन यहां कि मिट्टी तो अब बदल गयी है, बाबू। लगता है, हिंदुओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची। मैं तो यही देख रहा हूं।’’
‘‘तुम पागल हो, मियां ? हमारे बाप-दादा जिस ज़मीन को स्वर्ग से कम नहीं मानते थे, वहां से तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें भी रिश्तेदार मानता हूं, मियां। हमारे घर के तमाम लोग तो ख़त्म हो गये लेकिन फिर भी मेरा मन यहां से चले जाने को तैयार नहीं है।’’ प्रबोधबाबू की आंखों से दो नदियां बह रही थीं।
‘‘मेरे पास बहुत बुरी ख़बर है, बाबू।’’
‘‘कौन-सी नयी बुरी ख़बर, मियां ? हमें यहां के लोग काट डालेंगे, यही न ?’’
‘‘बिहारी मुसलमानों ने बंगाल के मुसलमानों का दिमाग ज़हर से भर दिया है। अब वे कहते हैं कि पूर्वी बंगाल के एक-एक हिंदू को ज़मीन के नीचे दफ़ना दिया जायेगा।’’
‘‘इस पूर्वी बंगाल के अलावा मैं तो कोई और मुल्क नहीं जानता। क़िस्मत अगर यही रही, चलो मैं भी यहीं ख़त्म हो जाऊंगा। कहीं बाहर जा कर मरने से यही बेहतर होगा।’’
‘‘ऐसा न बोलें, बाबू। आप तो बड़े आदमी हैं। किताब वग़ैरह पढ़ कर तो आप ढेर सारा समझ लेते हैं। दुनिया को आप जितना समझते हैं, उतना और कौन समझेगा ?’’
‘‘चलो, अगर मैं थोड़ा समझता हूं तो वही सही, लेकिन तुम भी तो पढ़े-लिखे बिना भी कुछ न कुछ समझ ही लेते हो। हर किसी में यह गुण थोड़े ही होता है ?’’
‘‘आप तो हंसी-ठट्ठा कर रहे हैं। असल में हम तो बुर्बक हैं, बाबू। लेकिन अच्छा है कि मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है, वरना वह भी एक और बुर्बक ही रह जाता।’’ राशिद की आवाज़ में थोड़ी कंपकंपी उतर आयी थी।
प्रबोधबाबू ने पूछा, ‘‘तुम्हें जानता तो इतने दिनों से हूं, लेकिन कभी नहीं जानाता कि तुम्हारे साथ और हैं कौन-कौन आख़िरकार ? लेकिन अब देख रहा हूं, तुम्हारे इस दरबे में कोई और रहता भी नहीं है।’’
राशिद चुप हो गया।
प्रबोधबाबू ने कहा, ‘‘कुछ बोलोगे नहीं, मियां ?’’
‘‘बोलने लायक़ अब रहा ही क्या है, बाबू ? सब कुछ तो कब का ख़त्म हो गया। अब तो मैं भूल भी गया अपने बारे में।’’
प्रबोधबाबू ने कुछ नहीं कहा। आंखें कहीं दूर चली गयी थीं।
कुछ देर बाद राशिद बोला, ‘‘आप तो चुप रह कर बहुत कुछ कह देते हैं, बाबू। मैं बुर्बक तो हूं लेकिन थोड़ा-बहुत समझ ही लेता हूं।’’
प्रबोधबाबू ने जवाब नहीं दिया।
‘‘चलिए, अब बता ही देता हूं।’’ राशिद मियां बोला, ‘‘अब तो मेरी उम्र पैंसठ या सत्तर ज़रूर हो गयी है, लेकिन कभी मैं भी बाईस साल का एक लड़का था। जब बिमला को पहली बार देखा तो सिर फिर गया था। बिमला थी तो हिंदू मल्लाहों की बेटी, लेकिन वह मुसलमान बन गयी और मुझसे उसका निकाह हो गया। निकाह के बाद अपनी औरत के साथ मैं ढाका की एक गली में बहुत ख़ुश रह रहा था। लेकिन सिर्फ़ चार महीने। इस बीच मेरी औरत के पैर भारी हो गये थे और मैं जाने क्या-क्या ख़्वाब देखने लगा।’’ राशिद का गला काफ़ी भारी हो गया था।
प्रबोधबाबू थोड़ा-बहुत समझ गये कि हिंदू-मुसलमान की शादी का अंजाम आख़िर क्या हुआ होगा।
कुछ देर चुप रहने के बाद राशिद मियां बोला, ‘‘कोई नयी बात नहीं है, बाबू। ऐसी बातें मुझसे पहले तो हुई ही हैं, आगे भी होती रहेंगी। आप जानते हैं न, ढाका के शाखारी (शंख की चूड़ी बनाने वाले) बहुत मशहूर हैं। लेकिन लोग उनसे डरते भी हैं। बिहारी मुसलमान तो उन्हें देखते ही भाग खड़े होते हैं। मैं दो दिनों के लिए काम से चटगांव आया था तो मेरी बीवी को चार हिंदू शाखारी जाकर ख़त्म कर आये। तब से मैं कभी ढाका नहीं जा पाया। मेरी बीवी चील-कौओं का खाना बन गया और उसका साथ साथ पल रहा पेट का बच्चा भी। तब से मैं चटगांव में ही रह रहा हूं। बाबू, बस इतनी भर मेरी कहानी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं।’’
प्रबोधबाबू आसमान की तरफ़ देख रहे थे। उन्होंने आंखें बिना फेरे ही मियां से कहा, ‘‘इतना प्यार था बीवी से ?’’ वैसे दोनों जानते थे, यह कोई सवाल नहीं था।
राशिद ने उत्तर नहीं दिया।
‘‘तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी बहुत लंबी है, मियां। शायद उसकी लंबाई का अंदाज़ा किसी को भी न हो।’
‘‘है ही कौन मेरा, जो बैठ कर अंदाज़ा लगायेगा, बस मैं एक बैलगाड़ी भर हूं, जो जैसे-तैसे चल रही है।’’
‘‘तुम्हारे अंदर भोलोबसा (प्रेम) बहुत है, मियां। यह मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं चला। वरना तुम घर तो बसा ही लेते। इससे अलग तो कुछ भी तुमने नहीं मांगा था।’’
राशिद हंसा, ‘‘आप बोलेत क्या हैं बाबू, कई बार तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाता। मान लेता हूं, वक़्त आने पर शायद कभी न कभी मतलब थोड़ा-बहुत शायद पकड़ लूं।’’
प्रबोधबाबू ने सिलसिला एकदम से बदल दिया था बोले, ‘‘मुझे अब रहने यहीं दो। उस पार के बंगाल भेज कर तुम्हें क्या मिलेगा, मियां ? मैं अब जिऊंगा भी कितना ? दो साल या चार साल ? कुछ भी हो, मुझे तो अब यहीं रहने दो।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i