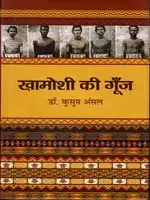|
ऐतिहासिक >> खामोशी की गूँज खामोशी की गूँजकुसुम अंसल
|
430 पाठक हैं |
|||||||
यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले उन सभी भारतीयों के इतिहास की दास्तान है जिन्होंने वर्षों पूर्व लगभग अठारह सौ साठ (1860) में उस धरती पर अपने कदम रखे थे।...
हिन्दी साहित्य में शायद यह पहला उपन्यास है जो दक्षिण अफ्रीका की
पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इस उपन्यास में कथानक की रोचकता को सुरक्षित
रखते हुए लेखिका ने एक ऐसे रंगभेदी समाज से हमें परिचित कराया है जहाँ
कष्टसाध्य गुलामी तथा दुर्व्यवहार के दर्द की एक ख़ामोशी की गूँज हर समय
सरसराती है।
यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले उन सभी भारतीयों के इतिहास की दास्तान है जिन्होंने वर्षों पूर्व लगभग अठारह सौ साठ (1860) में उस धरती पर अपने कदम रखे थे। ‘गोरी सरकार’ ने उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अनुबंधित किया था, परन्तु बदले में दिया था एक अमानवीय यातनापूर्ण जीवन और जातिभेद या ‘रेसिज़्म’ के नाम पर और जातिभेद या ‘रेसिज़्म’ के नाम पर अनेकानेक अत्याचार। वर्षों तक उनकी शिनाख्त मात्र एक ‘कुली’ जैसी थी जो उनकी अंतर आत्मा में आज भी कहीं गहरी धंसी हुई है। अपने चार वर्षों के शोध के पश्चात् लेखिका ने बड़ी सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टि से वहाँ के भारतीयों के दुःखद इतिहास और मानसिकता को उपन्यास का रूप दिया है।
स्वतन्त्रता पा जाने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर तीन प्रकार के नागरिक हैं। वह ‘गोरे’ जो पहले शासन करते थे, और लोकल ‘काले’ जो आज शासन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं वह भारतीय जो अपने को ‘शत-प्रतिशत दक्षिण अफ्रीकन भारतीय’ कहते हैं।’ यह भी सच है कि इन भारतीयों ने इतनी पुश्तों के बीत जाने के बाद भी अपनी मूल भारतीय संस्कृति, संस्कार और मूल्यों को सुरक्षित रखा है। श्री नेल्सन मंडेला ने इस मिली-जुली नागरिकता को ‘रेनबो नेशन’ या ‘इन्द्रधनुषी सभ्यता’ का नाम दिया था। उसके साथ-साथ महात्मा गाँधी ने भी अपने जीवन के इक्कीस वर्ष उस धरती पर व्यतीत किये थे और न केवल भारतीयों को बल्कि काले ‘अपार्थियों’ को भी संघर्षपूर्ण जीवन से उबार कर वोट दिलवाने का अधिकार दिलवाया और उन्हें एक मनुष्यत्व की पहचान या ‘आईडेंटिटी’ दी थी।
यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले उन सभी भारतीयों के इतिहास की दास्तान है जिन्होंने वर्षों पूर्व लगभग अठारह सौ साठ (1860) में उस धरती पर अपने कदम रखे थे। ‘गोरी सरकार’ ने उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए अनुबंधित किया था, परन्तु बदले में दिया था एक अमानवीय यातनापूर्ण जीवन और जातिभेद या ‘रेसिज़्म’ के नाम पर और जातिभेद या ‘रेसिज़्म’ के नाम पर अनेकानेक अत्याचार। वर्षों तक उनकी शिनाख्त मात्र एक ‘कुली’ जैसी थी जो उनकी अंतर आत्मा में आज भी कहीं गहरी धंसी हुई है। अपने चार वर्षों के शोध के पश्चात् लेखिका ने बड़ी सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टि से वहाँ के भारतीयों के दुःखद इतिहास और मानसिकता को उपन्यास का रूप दिया है।
स्वतन्त्रता पा जाने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर तीन प्रकार के नागरिक हैं। वह ‘गोरे’ जो पहले शासन करते थे, और लोकल ‘काले’ जो आज शासन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं वह भारतीय जो अपने को ‘शत-प्रतिशत दक्षिण अफ्रीकन भारतीय’ कहते हैं।’ यह भी सच है कि इन भारतीयों ने इतनी पुश्तों के बीत जाने के बाद भी अपनी मूल भारतीय संस्कृति, संस्कार और मूल्यों को सुरक्षित रखा है। श्री नेल्सन मंडेला ने इस मिली-जुली नागरिकता को ‘रेनबो नेशन’ या ‘इन्द्रधनुषी सभ्यता’ का नाम दिया था। उसके साथ-साथ महात्मा गाँधी ने भी अपने जीवन के इक्कीस वर्ष उस धरती पर व्यतीत किये थे और न केवल भारतीयों को बल्कि काले ‘अपार्थियों’ को भी संघर्षपूर्ण जीवन से उबार कर वोट दिलवाने का अधिकार दिलवाया और उन्हें एक मनुष्यत्व की पहचान या ‘आईडेंटिटी’ दी थी।
1
शाम के पाँच बज रहे थे, आकाश के एक छोर पर सूरज डूब रहा था और दूसरी ओर
हमारा हवाई जहाज़ जोहानसबर्ग की धरती पर उतर रहा था। जैसे-जैसे हमारे
वायुमान की गति धीमी होती गई मेरे हृदय की धड़कन बढ़ती गई। वह मेरी पहली
हवाई यात्रा थी जो अनेकों मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के साथ समाप्त हो रही
थी। हाथ का सामान सँभालती मैं जीवेश के पीछे-पीछे यन्त्रवत चलती चली जा
रही थी। यात्रियों की लम्बी कतार में इमीग्रेशन वाले खण्ड में खड़े होने
पर अपने आसपास दृष्टि डाली तो देखा बहुत से लोग थे, चेहरे पर चेहरा भीड़,
परन्तु अपना तो कोई नहीं था जिसकी भावात्मक गंध से तन-मन खिल उठता। परन्तु
बिल्कुल सामने एक पुरुष, अधेड़ उम्र, सफेद कमीज़ और काली पतलून पहने हमारी
ओर देखकर धीमे-धीमे मुस्करा रहा था। जाने क्यों मुझे लगा, यही होंगे जीवेश
के पिता श्री प्रताप सिंह। इससे पहले मैं कुछ कहती जीवेश आगे बढ़कर उनसे
लिपट गया। उन्होंने भी उसे उतने ही स्नेह से बाँहों में समेट लिया था। फिर
उन्होंने मुड़कर मुझे देखा–‘‘अरे तुम हो,
हमारे जीवेश की पत्नी हमारी बहु, गॉड ब्लैस यूँ !’’
उनका गला भर्रा-सा गया था, आँखों में नमी छलछला आई
थी–‘‘जीवेश, बहुत सुन्दर है बहू, क्या नाम
बताया था तुमने, हाँ अन्विता, नाम भी कितना प्यारा है। आओ बेटा, हमारे देश
में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है।’’ उन्होंने स्नेह से
मेरा आह्वान किया। परन्तु मैं, अपनी उलझनों के ऊहापोह में गुम आसपास के
परिवेश से पहचान बनाना चाह रही थी। एक अनजान शहर, अजनबी पिता...और जो लोग
वहाँ घूम रहे थे, वह रंगों का एक अजीब
सम्मिश्रण–‘काले’ वहाँ के लोकल लोग,
‘गोरे’, अंग्रेज और मटमैले परिवेश के बहुत से यात्री।
‘‘कहाँ आ गई मैं सरे-राह चलते-चलते
?’’ एकाएक मन में धड़कन ठहर-सी गई। परन्तु तभी जीवेश
की सान्त्वनापूर्ण बाँह मेरी कमर में लिपट गई, तो मैं अपने विचारों की
उड़ान से छिटककर पुनः उस धरती पर लौट आई, जो अब मेरी वास्तविक कर्मभूमि
बनने जा रही थी। प्रताप जी के लिए मैं क्या करूँ ? सोच रही थी, झुककर पैर
छू लूँ ? पता नहीं कितनी भारतीयता बची थी यहाँ ? मैंने बस हाथ जोड़ दिए
‘नमस्कार’। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, एक मौन-सा
आशीर्वाद दिया, पता नहीं किस भाषा में। अब तक हम सामान के साथ बाहर कार
पार्किंग एरिया में आ गए थे। एक सफेद कार में जीवेश, प्रताप जी के साथ आगे
बैठ गया था और पीछे की सीट पर मैं, और मेरे साथ छोटा-बड़ा असबाब, पुस्तकों
का बैग, मिठाई की छोटी पेटी और थी, तो, मेरी अपनी मिली-जुली अनुभूतियों की
एक गठरी जिसे सँभालकर मैं चुपचाप दम साधे थी।
‘‘रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई
?’’ ‘‘यात्रा सुखद थी
?’’ जैसे वाक्यों के बाद प्रताप जी जीवेश अपने किसी
वार्तालाप में उलझ गए थे। अपने से उबर कर मैंने शहर के बाहरी परिवेश को
ध्यान से देखा। खाली सपाट साफ-सुथरी सड़कें जहाँ दूर-दूर तक कोई आदमी, न
आदमी की जात, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जबकि भारत में भिखारियों की
कतार के साथ हर कदम पर धक्कम-धक्का होते रिक्शे-स्कूटरों या यात्रियों से
ठसाठस भरी बसें, धुआँ उगलते ट्रक, घोड़ागाड़ी सभी कुछ एकसाथ देखा जा सकता
था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कहीं भी कूड़े का कोई ढेर नहीं था। बेहद सफाई
और तरतीबवार लगाए गए लगभग एक जैसी ऊँचाई के पेड़ सड़क के किनारों पर शान
से तने खड़े थे। मैं अपने शरीर, अपनेपन को समेट रही थी। चाह रही थी सहज
होकर इस समूचे परिवेश को अपने भीतर समोहित कर लूँ। हाँ, अब यहीं तो रहना
है मुझे—मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य इन्हीं हवाओं में तय किया
जाएगा ? जाने क्या होगा पता नहीं ? सभी कुछ तो इतनी जल्दी में हुआ, मैं
कुछ समझने-परखने की स्थिति में होती, इससे पहले—इतना कुछ घटित
हो गया था। बुआ और जो. जो. अंकल की असमय मृत्यु और वैसे समय में, जीवेश का
सामने आ खड़े होना। ‘‘मैं संजू का मित्र हूँ, जीवेश,
जीवेश सिंह, साउथ अफ्रीका में रहता हूँ...’’ एक अजनबी
अनजान युवक दबे कदमों से मेरे भय के उस मंजर में प्रवेश कर गया जहाँ उस
समय दुख का एक क्रूर बवण्डर बाहर-भीतर हिचकोले खा रहा था। मैं
भीतर-ही-भीतर पथरा-सी गई थी ऐसे मौत के सन्नाटे में, अपने अस्तित्व या
अपने भविष्य के बारे में सोच पाना तो बहुत दूर की बात थी। और यह अजनबी ?
यह था, कि अपनी मीठी मुस्कान से मेरे हृदय की धड़कनों पर दस्तक दिए जा रहा
था। जाने कैसे मैंने निर्णय ले लिया। चंडीगढ़ में अपनी लगी-लगाई नौकरी
छोड़ दी, बुआ के उस घर के धुआँ-धुआँ अतीत से एक मौन विदा ले ली और वती
आँटी के कन्यादान से, जीवेश का हाथ पकड़ कर विवाह-सूत्र में बँध गई। और अब
यहाँ पहुँच गई हूँ विदेश की उस धरती पर जो मेरे लिए नितान्त अजनबी है।
बहुत सोचने पर अफ्रीका के नाम पर स्मृतियों के पटल पर खुदा एक अमरीकन
टेलीविजय सीरियल ‘रूट्स’ का चित्र उभरता था। दासता की
नितान्त काली तस्वीर, विशेष रूप से वह दृश्य जहाँ, उस खरीदे हुए दास के
पैरों की उंगलियाँ काट दी गई थीं, कि वह दासता की गुलाम ज़ँजीरें तोड़ भाग
न सके। उस दृश्य की क्रूर अमानवीय इंटेसिटी को मैं कभी भी भूल नहीं पाई
थी। आज भी पता नहीं क्यों वहीं पुरानी सिहरन शरीर में एक शीत कम्पन भर रही
थी। अपने को उस समूची स्मृति से उबारने के लिए मैंने फिर से खिड़की से
बाहर देखने का प्रयास किया; आकाश में, एक ओर सूरज डूब चुका था रचयिता की
ईश्वरीय आभा। दूसरी ओर लाल छतों वाले कतारबद्ध मकान शहर की उपस्थिति
परिभाषित करते मेरे सामने उभर रहे थे। मैंने उनकी दृश्यात्मकता को और गौर
से देखा। मेरा भविष्य मेरे समकक्ष था, एक नवनिर्मित वास्तुशिल्पी
आर्कीटेक्ट का भविष्य। जिसे मेरी उंगलियाँ शहर के फलक पर उकेरेंगी, हाँ
मुझे अपने भीतर के कलात्मक रचयिता को यहाँ प्रतिष्ठापित करना है यहाँ, इस
अनजान शहर की अजनबी बस्तियों में।
मेरे हाथ में एक ‘पैम्फलेट’ था जिसे, यहाँ के हवाई अड्डे के एक रेक पर से मैंने उठा लिया था। उसे खोलकर पढ़ने लगी, लिखा था, 1886 में इस शहर जोहरसबर्ग को स्थापित किया गया था। ‘‘एक सौ अठारह वर्ष पुराना यह शहर, संसार का सबसे छोटी उम्र का शहर है। संसार की चालीस प्रतिशत सोने की खदानें यहाँ खोज निकाली गई थीं और उन्हें के लिए यह शहर अपने-आप स्थापित होता चला गया। अब यह शहर यहाँ के ‘बिज़नेस कैपिटल’ (व्यावसायिक राजधानी) के रूप में पनप गया है। पर्यटक और व्यापारी यहाँ समान रूप से आते-जाते हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही थी वहाँ के मकानों या अन्य इमारतों पर पूरी तरह ब्रिटिश आर्कीटेक्ट का प्रभाव था। सारी निर्माण कला पर गोरों की अर्थगणित एक छाप जैसी थी जो भी नाम दें, ‘युनाइटर किंगडम’ की या व्हाइट नौबैलिटी’ की। मेरा आर्कीटेक्ट मन अपने भारतीय झरोखे-छज्जे, कलात्मक प्रतिमाओं के प्रति सजग हो रहा था। स्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं अन्विता, मैंने सोचा, मुझे अब इसी रूपान्तरित परिवेश में नए सिरे से जीना होगा। एक सान्त्वना जैसी मेरे आन्तरिक स्त्रोत में उपज ही रही थी कि...जीवेश का स्वर ‘‘अन्विता, कहाँ खो गई, कब से पुकार रहा हूँ, आओ मन्दिर आ गया है।’’
मैंने देखा, जीवेश कार का द्वार खोले खड़ा था, ‘‘मन्दिर और यहाँ ?’’
‘‘हाँ, यह स्वामीनारायण मन्दिर, आओ, अपना नया जीवन आरम्भ करने से पहले हम दोनों भगवान का आशीर्वाद ले लें।’’ जीवेश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था जिसे थामकर जब मैं उतरी तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, मेरी आँखों के सामने नितान्त भारतीय भव्य मंदिर था। गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित, जिसमें भारतीय निर्माण कला पूरी तरह झलक रही थी। प्रवेश द्वार पर ही दो हाथियों की प्रतिमाएँ सूँड माथे से छुआकर जैसे स्वागत कर रही थीं। सामने छोटा-सा आँगन जैसा था वहाँ अपने चप्पल-जूते उतार कर हम भीतर चले गए। सामने थी, नयनाभिराम श्वेत संगमरमर की प्रतिमाएँ, भगवान कृष्ण, राधिका और बलराम। उनके वस्त्र ही नहीं उनके आभूषण और सारी सज्जा सुन्दर और कलात्मक थी। भगवान को अपने निकट पाकर आश्वासन सा हुआ। लगा उनकी मुस्कुराहट में मेरे लिए कोई गोपनीय सन्देश है, क्या ? इससे पहले मैं कुछ और सोच पाती, एक धोती धारी पण्डित निकट आ खड़ा हुआ। मुझे पता ही नहीं चला वह लकड़ी के किस रहस्यात्मक दरवाज़े से निकलकर आया था ?
‘‘पण्डित जी, यह हमारी पुत्रवधू है अन्विता, अभी भारत से आई है। आप आशीर्वाद दें यहाँ इस धरती पर इसका जीवन मंगलमय हो।’’
‘‘ओह, तुम इतने समुद्र पार करके आई हो, यहाँ, इस धरती पर ? रास्ते के उजाले और अन्धकार सभी को फलाँग कर ? जिस सत्य के अनुसंधान के हेतु आई हो, प्राप्त होगा अवश्य प्राप्त होगा बेटा क्योंकि सत्य तो एक ही है, चाहे इस धरती पर रहो या उस, तद...एकम्...।’’
उन्होंने चन्दन का टीका मेरे माथे पर फिर जीवेश और प्रताप जी के माथे पर लगा दिया। मैंने उन्हें भरपूर देखा अधेड़ उम्र के स्वामी जी के साधारण से चेहरे पर कुछ था, एक चमक उनकी आँखों में थी, एक असाधारण चमक, जिसे मैं अपने चेहरे पर फैलता महसूस कर रही थी।...‘‘जी स्वामी जी, मैं इतनी दूर से आई हूँ यहाँ परन्तु नहीं जानती कि मेरी तलाश क्या है ? पता नहीं मैं अपने ध्येय की खोज में आई हूँ यहाँ, या शायद जीवन सुख ?’’ मुझे अपने शब्दों पर ही आश्चर्य हुआ था। अपनी माँ की तरह भगवान पर कभी विश्वास नहीं किया था मैंने। स्वामीजी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, परन्तु हाँ, मेरी फैली हुई खाली हथेली पर चरणामृत रख दिया जिसे मैं पी गई थी। मेरा प्रश्न मेरे विचारों का उद्घोषण ही तो था दो मुझे परेशान कर रहा था। मुझे खुद को खोज निकालना है अपने उत्तर को। अपने में ही उजागर करना है अपना गन्तव्य। प्रताप जी, बुआ की तरह, धरती पर लेटकर दण्डवत प्रणाम कर रहे थे और जीवेश, वह भी प्रार्थना की मुद्रा में झुका था।
मेरे हाथ में एक ‘पैम्फलेट’ था जिसे, यहाँ के हवाई अड्डे के एक रेक पर से मैंने उठा लिया था। उसे खोलकर पढ़ने लगी, लिखा था, 1886 में इस शहर जोहरसबर्ग को स्थापित किया गया था। ‘‘एक सौ अठारह वर्ष पुराना यह शहर, संसार का सबसे छोटी उम्र का शहर है। संसार की चालीस प्रतिशत सोने की खदानें यहाँ खोज निकाली गई थीं और उन्हें के लिए यह शहर अपने-आप स्थापित होता चला गया। अब यह शहर यहाँ के ‘बिज़नेस कैपिटल’ (व्यावसायिक राजधानी) के रूप में पनप गया है। पर्यटक और व्यापारी यहाँ समान रूप से आते-जाते हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही थी वहाँ के मकानों या अन्य इमारतों पर पूरी तरह ब्रिटिश आर्कीटेक्ट का प्रभाव था। सारी निर्माण कला पर गोरों की अर्थगणित एक छाप जैसी थी जो भी नाम दें, ‘युनाइटर किंगडम’ की या व्हाइट नौबैलिटी’ की। मेरा आर्कीटेक्ट मन अपने भारतीय झरोखे-छज्जे, कलात्मक प्रतिमाओं के प्रति सजग हो रहा था। स्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं अन्विता, मैंने सोचा, मुझे अब इसी रूपान्तरित परिवेश में नए सिरे से जीना होगा। एक सान्त्वना जैसी मेरे आन्तरिक स्त्रोत में उपज ही रही थी कि...जीवेश का स्वर ‘‘अन्विता, कहाँ खो गई, कब से पुकार रहा हूँ, आओ मन्दिर आ गया है।’’
मैंने देखा, जीवेश कार का द्वार खोले खड़ा था, ‘‘मन्दिर और यहाँ ?’’
‘‘हाँ, यह स्वामीनारायण मन्दिर, आओ, अपना नया जीवन आरम्भ करने से पहले हम दोनों भगवान का आशीर्वाद ले लें।’’ जीवेश ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था जिसे थामकर जब मैं उतरी तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, मेरी आँखों के सामने नितान्त भारतीय भव्य मंदिर था। गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित, जिसमें भारतीय निर्माण कला पूरी तरह झलक रही थी। प्रवेश द्वार पर ही दो हाथियों की प्रतिमाएँ सूँड माथे से छुआकर जैसे स्वागत कर रही थीं। सामने छोटा-सा आँगन जैसा था वहाँ अपने चप्पल-जूते उतार कर हम भीतर चले गए। सामने थी, नयनाभिराम श्वेत संगमरमर की प्रतिमाएँ, भगवान कृष्ण, राधिका और बलराम। उनके वस्त्र ही नहीं उनके आभूषण और सारी सज्जा सुन्दर और कलात्मक थी। भगवान को अपने निकट पाकर आश्वासन सा हुआ। लगा उनकी मुस्कुराहट में मेरे लिए कोई गोपनीय सन्देश है, क्या ? इससे पहले मैं कुछ और सोच पाती, एक धोती धारी पण्डित निकट आ खड़ा हुआ। मुझे पता ही नहीं चला वह लकड़ी के किस रहस्यात्मक दरवाज़े से निकलकर आया था ?
‘‘पण्डित जी, यह हमारी पुत्रवधू है अन्विता, अभी भारत से आई है। आप आशीर्वाद दें यहाँ इस धरती पर इसका जीवन मंगलमय हो।’’
‘‘ओह, तुम इतने समुद्र पार करके आई हो, यहाँ, इस धरती पर ? रास्ते के उजाले और अन्धकार सभी को फलाँग कर ? जिस सत्य के अनुसंधान के हेतु आई हो, प्राप्त होगा अवश्य प्राप्त होगा बेटा क्योंकि सत्य तो एक ही है, चाहे इस धरती पर रहो या उस, तद...एकम्...।’’
उन्होंने चन्दन का टीका मेरे माथे पर फिर जीवेश और प्रताप जी के माथे पर लगा दिया। मैंने उन्हें भरपूर देखा अधेड़ उम्र के स्वामी जी के साधारण से चेहरे पर कुछ था, एक चमक उनकी आँखों में थी, एक असाधारण चमक, जिसे मैं अपने चेहरे पर फैलता महसूस कर रही थी।...‘‘जी स्वामी जी, मैं इतनी दूर से आई हूँ यहाँ परन्तु नहीं जानती कि मेरी तलाश क्या है ? पता नहीं मैं अपने ध्येय की खोज में आई हूँ यहाँ, या शायद जीवन सुख ?’’ मुझे अपने शब्दों पर ही आश्चर्य हुआ था। अपनी माँ की तरह भगवान पर कभी विश्वास नहीं किया था मैंने। स्वामीजी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, परन्तु हाँ, मेरी फैली हुई खाली हथेली पर चरणामृत रख दिया जिसे मैं पी गई थी। मेरा प्रश्न मेरे विचारों का उद्घोषण ही तो था दो मुझे परेशान कर रहा था। मुझे खुद को खोज निकालना है अपने उत्तर को। अपने में ही उजागर करना है अपना गन्तव्य। प्रताप जी, बुआ की तरह, धरती पर लेटकर दण्डवत प्रणाम कर रहे थे और जीवेश, वह भी प्रार्थना की मुद्रा में झुका था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i