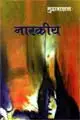|
कहानी संग्रह >> मुद्राराक्षस संकलित कहानियां मुद्राराक्षस संकलित कहानियांमुद्राराक्षस
|
2 पाठक हैं |
|||||||
कथाकार द्वारा चुनी गई सोलह कहानियों का संकलन...
मुठभेड़
कितनी लंबी और तीखी मार होती है फिर वह चाहे मौसम की हो या सिपाही की। चीखकर
उड़ी फड़फड़ाती हुई चील की तरह रज्जन की तकलीफ-भरी हुई एक सदा-सुन पड़ी-“ओ
मां..."
नत्थू के हाथ कमर में बंधे कपड़े के छोर से बनाई छोटी-सी पोटली पर इस कदर
ढीले पड़ गए कि पोटली उसके बदन का हिस्सा जैसा न बनी होती तो जरूर सरक गिरती।
आवाज, बांस जैसी तड़कती हुई तकलीफ-भरी वह चीख, ज्यादा लंबी नहीं थी लेकिन
नत्थू की पसलियों के अंदर बहुत दूर तक और देर तक लकीर-सी खींचती चली गई।
कितनी लंबी और तीखी मार होती है फिर चाहे वह मौसम की हो या सिपाही की।
जून की इस बहुत तीखी और बहुत ज्यादा चढ़े बुखार की तरह बेआवाज धूप में नत्थू
जहां ठिठक गया था, वहां से सिर्फ कुछ कदम आगे ही उसके मकान की पिछली दीवार
थी। कच्ची मिट्टी से खड़ी की गई उस दीवार पर सफेद सीपियां और घोंघे इस तरह
उभर आए थे गोया वे वहां जड़ दिए गए हों। उस सफेद पच्चीकारी के बीच पानी की
धार से कटी मिट्टी की संकरी खड़ी धारियां जाहिर कर रही थीं कि मौसम की अगली
मार पड़ते ही दीवार गलकर गिर जाएगी। शायद इस दीवार के गिरने पर भी वैसी ही
दहलानेवाली और भद्दी आवाज हो जैसी आवाज इस बार रज्जन की सनाई दी थी। नत्थू
ठहर गया था। हो सकता है वह अगली चीख का इंतजार कर रहा हो या फिर पहली ही चीख
के अपने अंतर में डूबने का समय लेना चाहता हो। रज्जन की आवाज दुबारा नहीं आई।
मौसम की मार से छिली हई दीवार की तरह ही शायद डंडे के सिर्फ एक और आघात से वह
भी गिरा हो तालाब की मिट्टी से बनी काली-भूरी दीवार-सा।
इतने समय में पोटली उसने दुबारा सावधानी से पकड़ ली थी। पोटली में काफी तादाद
में तोड़ी अरहर की फलियां थीं। इन्हें छिलके साहित उबाल लेने के बाद थोड़े से
नमक की मदद से खासे स्वादिष्ट भोजन के रूप में काम में लाया जा सकता था। खाने
के मामले में उसके लिए यह मौसम लगभग समृद्धि काल होता था। हर किसी के लिए यह
जानना आसान नहीं होता कि दुनिया का सबसे उम्दा खाना क्या होता है लेकिन नत्थू
को यह जरूर मालूम था कि मिट्टी और सड़े पत्तों के बीच टपकनेवाले महुए के रस
भरे हुए सफेद फूलों या फलों के बाद सबसे जायकेदार खाना अरहर की उबली हुई
फलियां होती थीं। अरहर एक ऐसी बदतमीज फसल है जो बिना किसी खाद या पानी के,
बगैर किसी सही देखरेख के खेत में बेतरतीबी से खड़ी रहती है और इतने लंबे अरसे
तक खड़ी रहती है कि लगता है वह वहां हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। खेत की हिफाजत
करनेवाला ही नहीं, उसे चर जानेवाला जानवर भी अक्सर उसकी तरफ से उदासीन हो
जाता था। ऐसे में झुलसाकर सुखाए आदमियों की खड़खड़ाती बेजान भीड़ की तरह खड़े
उस खेत से दो पाव फलियां तोड़ लेना मामूली बात थी।
रज्जनलाल की उस कातर चीख के बाद सब खामोश हो गया। सिर्फ एक ऐसे परिंदे की
आवाज आती रही जिसके बारे में नत्थू ने ही नहीं, गांव के हर आदमी ने एक ही
वीभत्स और जुगुप्साजनक कहानी सुनी थी। सच तो यह है कि बहुत स्वादिष्ट महुए
एकत्र करते हुए अक्सर वह परिंदा बोलता जरूर था और उसे वही कहानी याद भी आती
थी। कहते हैं कभी एक बूढ़ी औरत ने घर के बाहर धूप में महुए फैलाए और लकड़ी
बीनने जाते वक्त अपने एकमात्र पोते से कह गई कि वह महुओं की हिफाजत करे। धूप
से सूखकर महुए बहुत कम हो गए। बुढ़िया ने वापस लौटकर समझा कि बच्चा चोरी से
महुए खा गया। बुढ़िया ने बच्चे को सिल के पत्थर से मारा। बच्चा मर गया। लोगों
ने बुढ़िया को बताया कि महुए चोरी नहीं गए थे, सूखकर कम हो गए थे। इसके बाद
बुढ़िया एक चिड़िया बन गई और हर दोपहर आवाज लगाने लगी-उठो पुत्तू, पूर, पूर,
पूर-रज्जन को वे लोग सुबह कोई आठ बजे ले गए थे। उनमें से एक छोटा थानेदार था,
बाकी सिपाही थे। रज्जन से उन्हें क्या जानना था यह शायद ही किसी को मालूम रहा
हो।
रज्जन को जिस वक्त पुलिस ले चली, उसके पीछे बच्चों की खासी ही भीड़ थी लेकिन
मर्द या औरत कोई नहीं था। बच्चे शायद वहां बहुत देर तक रहे हों। गांव के बाहर
प्रधान के खेतों से कटकर आनेवाले अनाज के इकट्ठा करने की जगह और छोटे से एक
कमरे के स्कूल के पीछे से होकर रास्ता कुछ बेढंगी कब्रों के बीच से गुजरता
हुआ एक टीले जैसी जगह की तरफ निकल जाता था। इस टीले पर पलाश की धूल से अंटी
झाड़ियां और मकड़ी के जाले जैसे फूल उगानेवाली लंबी सूखी घास थी।
बच्चों और रज्जन को उधर जाते देखनेवालों में नत्थू भी था। जाने कैसे उसे लगा
था कि उसे वहां उस वक्त दिखाई नहीं देना चाहिए। शायद उसी अपरिभाषेय आशंका के
कारण उसने सोचा था कि फलियां तोड़ने में ज्यादा वक्त लगाना चाहिए और फिर जहां
तक बने, सीधे रास्ते घर नहीं लौटना चाहिए।
लंबा रास्ता तय करके गांव के करीब आते-आते उसने वह आवाज सुनी, बहुत दूर से और
बहुत ज्यादा तकलीफ में छटपटाती आवाज। वह रज्जन की आवाज थी। कुछ ऐसी जैसे
कीचड़ के बीच नोकदार लकड़ी से छेद दी गई मछली हो। रज्जन की उस चीख के साथ ही
बबूल के झीने बेडौल दरख्तों के बीच कहीं से उस परिंदे की आवाज आने लगी-उठो
पुत्तू, पूर, पूर, पूर-
रज्जन की आवाज के साथ बच्चों का वह हुजूम भागता हुआ स्कूल नाम के उस अधगिरे
सायबान के पास आ गया। शायद उन्हें पुलिसवालों ने धमकाकर भगा दिया था। बच्चों
के उस हूजूम में ही रज्जन का बेटा भी था। स्कूल के पास ठहरकर बच्चों ने उसकी
तरफ देखा। उनकी निगाहों में न कोई कुतूहल था न करुणा। उसे देखकर वे अपनी-अपनी
व्यस्तता का साधन खोजने लगे। रज्जन का बेटा अभी तक सामान्य दीख रहा था पर वह
एकाएक कमजोर और बीमार दिखने लगा। उसका सांवला चेहरा ऐसा हो आया जैसे उस पर
राख की एक परत आ जमी हो। वह धीरे से सखे हए गोबर के एक ढेर पर बैठ गया।
बच्चों को अपनी व्यस्तता खोजने में ज्यादा देर नहीं लगी। एक बहुत ऊंचे बीमार
आम के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लटके एक सूखे से कच्चे आम को तोड़ने के लिए
वे मिट्टी और पत्थर के ढेले उछालने लगे।
वह आम शायद बहुत दिनों से वहीं था। या फिर एक गिर जाने पर दूसरा प्रकट हो
जाता था। बच्चे लंबे अरसे से उस पर ढेले चला रहे थे। किसी को पता नहीं वह आम
कभी गिरा भी था या नहीं और गिरा था तो खाया गया था या नहीं। हां, बच्चों की
इस कोशिश पर उस स्कूल के ऊपर रखी गई टिन की चादरें गिरते टेलों की वजह से
खासा शोर करती थीं। काफी पत्थर गिर चुकने के बाद अंदर से स्कूल के एकमात्र
अध्यापक किशन बाबू की आवाजें सुनाई देती थीं-"ठहर जाओ सालो!"
इस ललकार के बाद बच्चे ईटें फेंकना बंद करके किसी और काम में लग जाते थे।
आम के उस दरख्त पर फेंके गए दो-तीन ढेलों के बाद ही इस बार अध्यापक किशन बाबू
की आवाज नहीं, आकृति बाहर आ गई। यह काफी अनहोनी घटना थी। बच्चे सहमकर खड़े हो
गए।
"भाग जाओ..." किशन बाबू भारी आवाज में बोले। बच्चे भाग गए। किशन बाबू स्कूल
के अंदर नहीं गए। गर्द और धूप से पीलिया के रोगी जैसे दीखते क्षितिज पर आंखें
गड़ाकर उस तरफ देखने लगे जिधर से रज्जन के चीखने की आवाजें आ रही थीं। अब वे
चीखने की आवाजें नहीं कुछ ऐसी ध्वनियां थीं जैसे वे गले से नहीं सीधे फेफड़े
से उबलकर बाहर आ रही हों।
स्कूल के आसपास एकदम सन्नाटा था। वह स्कूल था, इस बात पर शायद ही कोई विश्वास
कर सके। कच्चे फर्श और टीन की छतवाले उस लंबोतरे कमरे में दूसरे से चौथे
दर्जे तक की कक्षाएं एक साथ लगती थीं, कमरे के तीन कोनों में और चौथे कोने
में एक मेज के सहारे किशन बाबू बैठते थे। वे इस स्कूल के अध्यापक भी थे और
पोस्टमास्टर भी। कुछ गालियों के साथ बच्चों को लगातार लिखते रहने का कोई काम
देने के बाद वे सो जाते थे। कभी-कभी खीझ के साथ एक पोस्टकार्ड देने या खत
लिखने के लिए उन्हें जागना होता था।
जागने पर किशन बाबू बहुत जोर से खीझते थे। लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए।
जगानेवाला उनकी खीझ से परेशान होने के बजाय हंसता था। वे अजीब चरित्र थे।
उनकी चरित्रगत विशिष्टता ही थी कि वे या तो सिर्फ अध्यापक के रूप में जाने
जाते थे या डाकखाना के नाम से। पोस्टमास्टर शब्द वैसे भी सहज नहीं था पर उनके
स्वभाव के कारण लोगों को उन्हें डाकखाना कहना अच्छा लगता था। इसकी खासी मसखरी
वजह थीं। गांववालों का विश्वास था कि खत ही नहीं तार से भी ज्यादा जल्दी
पहुंचती हैं वे बातें, जोकि किशन बाबू को बता दी जाती हैं। इसीलिए वे डाक
बाबू नहीं डाकखाना माने जाते थे।
लेकिन इसमें कसूर किशन बाबू का नहीं था। वे जिंदगी में शायद ही कभी किसी ऐसी
जगह गए होंगे जहां कोई मनोरंजन कर सकता हो। मन लगाने के लिए उम्र बढ़ने के
साथ-साथ उन्होंने वह तरीका खोज लिया था जिसे, भद्दी भाषा में, अक्सर लोग
चुगली खाना कह लेते हैं।
उस छोटे से गांव में यह एकमात्र सबसे सुलभ और लोकप्रिय मनोरंजन था। इस
मनोरंजन की खूबी यह थी कि अक्सर कई रोज निरंतर मन बहल सकता था। पड़ोस के गांव
में नौटंकी होती थी। उससे आगे एक कस्बा पड़ता था जिसमें एक अदद सिनेमा था।
मगर ये दोनों ही बहुत सीमित मनोरंजन थे। अक्सर सिनेमा या नौटंकी देखनेवाले को
बाद में मनोविनोद जारी रखने के लिए खासे झूठ बोलने होते थे जो कभी-कभी पकड़े
भी जाते थे। मसलन एक बार पंडित राधेश्याम ने एक सिनेमा देखा और वापस लौटकर
बताया, "बड़ी गंदी तस्वीर है। उसमें खुलेआम औरत-मर्द गड़बड़ करते हैं।"
"खुलेआम गड़बड़ करते हैं?" पड़ोसियों में अचानक उत्सुकता जाग पड़ी।
“अरे बड़े गंदे होते हैं ये, मत पूछो।" पंडित ने थूका भी।
"मगर होता क्या है?" उत्सुक पड़ोसियों ने सहसा कल्पनाएं करनी शुरू कर दी।
"अरे क्या नहीं होता, पूछो। रंडियां होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं।"
“मतलब कपड़े-कपड़े सब उतार कर?"
"लो, इस लल्लू की सुनो।"
सबने विश्वास कर लिया कि परदे पर पंडित राधेश्याम वह कुछ देखकर आए हैं, जो
दुर्लभ होता है और वह भी इतने सुंदर सजे-धजे लोगों के बीच होता हुआ।
|
|||||


 i
i