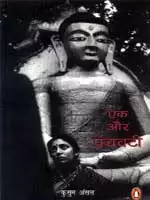|
नारी विमर्श >> एक और पंचवटी एक और पंचवटीकुसुम अंसल
|
75 पाठक हैं |
|||||||
नारी मन को परत दर परत उधेड़ता कुसुम अंसल का समसामायिक उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
कुसुम अंसल का यह उपन्यास नारी मन को परत दर
परत उधेड़ता
है। उपन्यास की नायिका साधवी की पृष्ठभूमि, मानसिकता और मानसिक द्वंद्व
उसे उस मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां सामाजिक-पारिवारिक मर्यादाएं बुरी
तरह चरमरा उठती हैं और वह निश्चय नहीं कर पाती कि जिस दिशा की ओर वह चल
पड़ी है, क्या वही उसकी दिशा है, उसकी मंज़िल है ?
पारिवारिक संबंधों की सीमा में होते हुए भी सीमाओं का अतिक्रमण करने वाली इस कहानी में उस नारी की व्यथा को मूर्त किया गया है जो न पत्नी रह पाती है, न रखैल बन पाती है और न परित्यक्ता का जीवन जी पाती है।
ऐसी स्थिति में एक नाटकीय मोड़ उसकी ज़िंदगी को आमूलचूल बद़ल कर रख देता है।
पारिवारिक संबंधों की सीमा में होते हुए भी सीमाओं का अतिक्रमण करने वाली इस कहानी में उस नारी की व्यथा को मूर्त किया गया है जो न पत्नी रह पाती है, न रखैल बन पाती है और न परित्यक्ता का जीवन जी पाती है।
ऐसी स्थिति में एक नाटकीय मोड़ उसकी ज़िंदगी को आमूलचूल बद़ल कर रख देता है।
बात एक और पंचवटी की
‘पंचवटी’ का पहला
संस्करण 1977 में
‘उसकी पंचवटी’ के नाम से, फिर दूसरा ‘एक और
पंचवटी’ के नाम से 1985 में ‘अभिव्यंजन’ से
प्रकाशित
हुआ था। 1999 में ‘पंचवटी’ पैनोरमा फ़िल्म के रूप में
देश-विदेश में दिखाई गई। ‘पचंवटी’ के कलाकार थे
दीप्ति नवल,
सुरेश ओबरॉय और अकबर ख़ान–स्वर्गीय श्री बासु भट्टाचार्य ने
उसका
निर्देशन किया था और शोभा डॉक्टर उसकी प्रोड्यूसर थीं।
उस समय जब मैंने लिखना आरंभ किया था तब कल्पना भी नहीं की थी कि लेखन मेरे जीवन का गहरा चिंतन बन जाएगा। जाने-अनजाने जो क़लम मेरे हाथों ने उठा ली थी, उसने मुझे एक सार्थक सा अस्तित्व प्रदान किया था। मुझे लगने लगा कि मेरे बेमानी, बेअर्थ जीवन को जैसे एक अर्थ प्राप्त हो गया था, और मैं जो नहीं हो सकी थी, वह मैं हो रही थी, एक अदना सी उपन्यास लेखिका। ‘पंचवटी’ फ़िल्म की ‘पटकथा’ और ‘संवाद’ की लेखिका के रूप में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फ़ेस्टीवल के दौरान दिल्ली और ताशकंद के मंच पर बासु भट्टाचार्य और पूरी ‘कास्ट’ के साथ बैठी हुई मैं, जैसे एक नई योनि में प्रवेश कर गई थी।
1985 में ‘एक और पंचवटी’ की भूमिका में मैंने लिखा था ‘पंचवटी के सहारे मैं एक गंध विशेष अपने समाज तक ला सकी, वह विचार श्रृंखला जहां मनुष्य अपने को सच के शीशे में ढाल कर जैसा है वैसा का वैसा प्रदर्शित करने की सामर्थ्य रखता है। उसके सच के सम्मुख सांसारिक बंधनों का, आदर्शों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। सांसारिक मान्यताओं को नकार कर मेरी साधवी पारदर्शी होकर खड़े हो सकने की सामर्थ्य रख सकी। खजुराहो की मूर्तियां भी तो मनुष्य की मानसिकता का जैसे का तैसा प्रदर्शन नहीं तो और क्या हैं ? कितना सच, कितना साहसिक, बनावट का कोई जामा नहीं। जब भी लॉन के उस कोने तक जाती हूं, आम के वृक्ष की मीठी सी तुर्श–खट्टी गंध मेरे आसपास बहती है और खजुराहो का सच उसमें घुल जाता है।’ उस समय मैंने प्रेम की मांसलता में डूबी खजुराहो की ‘इरौटिक’ प्रतिमाओं की कल्पना की थी। मुझे यह नहीं पता था कि जब ‘पंचवटी’ फ़िल्म में रूपांतरित होगी तो उसमें प्रतिबिंबित होगी नेपाल के ‘स्वयंभू’ मंदिर की भगवान बुद्ध की अनगिनत सात्विक प्रतिमाएं, जिनके मध्य मेरी साधवी प्रेमिका से परिवर्तित होकर वास्तव में ‘साधवी’ की चेतना को आत्मसात कर लेगी कि वह अपने लिए... अपने में पूर्ण होकर अपना अस्तित्व जी सके।
पता नहीं वे कैसे दिन थे, जब दूरदर्शन पर पहले ‘तितलियां’ फिर ‘इसी बहाने’ और ‘इंद्रधनुष’ सीरियल मेरी क़लम से निकलकर मेरे सृजनात्मक लेखन को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं दिनों शोभा डॉक्टर के साथ एक दिन बासु भट्टाचार्य और दीप्ति नवल से भेंट हो गई। मेरे सामने की मेज़ पर मेरी पुस्तकें पड़ी थीं। ‘एक और पंचवटी’ को हाथ में उठाकर दीप्ति ने कहा–‘ आपने लिखा है यह उपन्यास...?’ ‘हां’ मैंने कंपकंपाते स्वर में कहा, बस बात आरंभ हो गई, बासु दा को ‘पंचवटी’ की कहानी भा गई और बात आगे बढ़ती चली गई... उपन्यास परावर्तन से परावर्तित रूप में ढलने के लिए।
पुस्तक और फ़िल्म दोनों के मध्य खड़े होकर मुझे लगा कि पुस्तक एक बंद दरवाज़ा है, जिसके पृष्ठ खोलने पर हाथ लगते हैं उनके दृश्य। वे दृश्य जहां फूल खिल रहे हैं, सूर्य उग रहा है, चांद आकाश पर टंगा है, और फ़िल्म एक ऐसा द्वार है, जहां खोलने को कुछ नहीं है, सभी कुछ आंखों के सम्मुख है, सामने घटित होता हुआ। उपन्यास पर बनी फ़िल्म कुछ ऐसी होती है कि झरने के ऊपर से कोई पत्थर उठा दे और झरना प्रपात बन जाए, या एक ऐसा दरवाज़ा बाहर-भीतर के दृश्य को समूची लैंडस्केप प्रदान करने में सफल हो जाए। आज के संदर्भ में सिनेमा ही एक ऐसा मीडिया है, जिसके माध्यम से अपनी बात हर वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है, ये बात अलग है कि उसका विवेचन या इंटरप्रटेशन सबका अपना-अपना होता है। जैसे कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के समय किसी पदार्थ के भीतर प्रवेश करता है, उसका विश्लेषण करता है। वैज्ञानिक का अनुसंधान बताता है पदार्थ, पदार्थ नहीं परमाणु है, दर्शक की सोच कहती है संसार जो दिखता है वह वैसा नहीं है, भ्रम है, धोखा है। ‘मैं’ के परमाणु हैं समूचे मानसिक अनुभव। ‘एक और पंचवटी’ कुछ ऐसी ही मानसिकता का उपन्यास है, जो समाज के मान्यता प्रधान नियमों (विवाह आदि) पर प्रश्न चिह्न ही नहीं लगाता हमें विचार करने को बाध्य करता है।
‘पंचवटी’ उपन्यास, फ़िल्म में परिवर्तित होकर जैसे सजीव हो उठा, जीवन के समानांतर बह निकला। उपन्यास के कथानक में नेपाल का कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु शोभा को नेपाल के साथ एक फ़िल्म बनानी थी। ‘पंचवटी’ की बात आने पर अपनी कहानी को किसी दूसरी धरती को सौंपना पहले मुझे अटपटा लगा, पर फिर समझौता तो मुझे करना ही था, क्योंकि ‘ना’ कहने में मैं बहुत कमज़ोर हूं, इंकार करना मैंने सीखा नहीं। तभी अपनी आदतों के कटघरे में, मैं क़ैद, चुपचाप खड़ी रह गई और पंचवटी के पात्र नेपाल की धरती पर पैर रख कर चलने लगे, उन्हें देखती तो लगता चरित्र तो मात्र क्रिएशन है–कल्पना की स्त्री और कल्पना का पुरुष यहां तक कि भगवान की आकृति भी वास्तविक नहीं है, वह भी हमारी इच्छानुसार की गई कल्पना के आधार पर रूप धरती है, इस समय भगवान पशुपतिनाथ के रूप में वे हमारे इष्ट थे।
‘पंचवटी’ के विक्रम और साधवी भी उस धरती पर उतर कर कल्पना से निकल वास्तविक हो गए थे–नेपाल की धरती उन्हें नए अर्थ दे रही थी। नेपाल से जुड़ते ही कथानक में इतना कुछ आ मिला था, मंदिर, बौद्ध भिक्षु, भगवान बुद्ध की अनगिनत प्रतिमाएं, और एक ऐसा अद्भुत चित्रकार, ‘कर्मसिद्धि जी’, जो अपनी कला को प्रार्थना के मंत्रों जैसा सुच्चा मानकर अपने चित्र फूलों की तरह भगवान के चरणों में अर्पित कर देता था। ऐसे श्रद्धा के अहसास से लिपटा समूचा कथानक अपने आप ही एक विशेष मानसिकता जीने लगा, नेपाल का प्राकृतिक सौंदर्य उसे एक सशक्त पृष्ठभूमि प्रदान करने में सार्थक हो गया और प्रकृति, प्रकृति न रहकर कहानी की एक ‘पात्र’ हो गई थी।
शूटिंग आरंभ होने के पहले दिन मैं ज़बरदस्ती, बासु दा और शोभा को पशुपतिनाथ के मंदिर ले गई–बासु दा लोकेशन खोज रहे थे और मैं भगवान का आशीर्वाद। बाहर द्वार पर मैंने पूजा की एक थाली ख़रीदी–हाथ में फल-फूल, होठों पर बुदबुदाते मंत्र लिए जैसे ही मंदिर के आंगन में प्रवेश किया, पता नहीं कहां से एक भारी-भरकम बंदर कूद कर आया और झपट्टा मारकर मेरी थाली का नैवेद्य उठा ले गया था–मैं चकराई सी खड़ी देखती रही, मेरा पात्र ख़ाली था, पदार्थ विहीन, इम्मेटीरियल...
मैंने पंचवटी को मात्र लिखा ही नहीं शिद्दत से जिया भी, झेला भी–मात्र लेखिका ही नहीं बची थी मैं, कभी सुरेश जी से उनके चरित्र की बात करती, कभी दीप्ति को अपने गहने-कपड़े ला देती और कभी अकबर के विवाह की पार्टी का आयोजन करती। आधी से अधिक फ़िल्म अपने ही फ़ार्म पर शूट हुई थी–अतः मेरे काम भी अनगिनत थे, कभी कमरे का फ़र्नीचर ठीक करती, क़ालीन बिछवाती, कभी ‘इकेबाना’ पद्घति से फूल सजाती, कभी ‘बौन्साई’ समेट लाती कि उनके बौना हो आए स्वरूप के माध्यम से अपनी नायिका की आंतरिक घुटन को बयान कर सकूं। फ़िल्म के हर दृश्य के साथ गुंथकर, मैं भी, जैसे अस्तित्ववान हो रही थी, या शायद होश में नहीं थी, इसलिए कि मुझे उन दिनों ‘पंचवटी’ से अलग कुछ भी सुझाई नहीं देता था। शायद इस कारण भी कि, अपने पात्रों को उपन्यास के पन्नों पर से उठकर सजीव हो जाने का अनुभव बहुत रोमांचक होता है। तभी तो उन दिनों मेरा अपना समूचा अस्तित्व एक अद्भुत अनुभूति से थरथराता रहता है। स्वप्न और इच्छाओं के मध्य एक बहुत महीन विभाजक रेखा होती है। ‘पचंवटी’ के कथानक से अनेकों प्रश्न उस रेखा से बाहर फिसल आए थे, जैसे कि, क्या किसी मनुष्य को जीते जी सुख का ऐसा कोई अपूर्व पल हाथ लग सकता है ? और यदि हां, तो क्या उस पल के सहारे पूरी पहाड़ जैसी उम्र को जिया जा सकता है ? क्या वास्तव में सुख का पल इतना बड़ा होता है ? ऐसी कोई ‘पचंवटी’ धरती पर है क्या ?
उस समय जब मैंने लिखना आरंभ किया था तब कल्पना भी नहीं की थी कि लेखन मेरे जीवन का गहरा चिंतन बन जाएगा। जाने-अनजाने जो क़लम मेरे हाथों ने उठा ली थी, उसने मुझे एक सार्थक सा अस्तित्व प्रदान किया था। मुझे लगने लगा कि मेरे बेमानी, बेअर्थ जीवन को जैसे एक अर्थ प्राप्त हो गया था, और मैं जो नहीं हो सकी थी, वह मैं हो रही थी, एक अदना सी उपन्यास लेखिका। ‘पंचवटी’ फ़िल्म की ‘पटकथा’ और ‘संवाद’ की लेखिका के रूप में अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म फ़ेस्टीवल के दौरान दिल्ली और ताशकंद के मंच पर बासु भट्टाचार्य और पूरी ‘कास्ट’ के साथ बैठी हुई मैं, जैसे एक नई योनि में प्रवेश कर गई थी।
1985 में ‘एक और पंचवटी’ की भूमिका में मैंने लिखा था ‘पंचवटी के सहारे मैं एक गंध विशेष अपने समाज तक ला सकी, वह विचार श्रृंखला जहां मनुष्य अपने को सच के शीशे में ढाल कर जैसा है वैसा का वैसा प्रदर्शित करने की सामर्थ्य रखता है। उसके सच के सम्मुख सांसारिक बंधनों का, आदर्शों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। सांसारिक मान्यताओं को नकार कर मेरी साधवी पारदर्शी होकर खड़े हो सकने की सामर्थ्य रख सकी। खजुराहो की मूर्तियां भी तो मनुष्य की मानसिकता का जैसे का तैसा प्रदर्शन नहीं तो और क्या हैं ? कितना सच, कितना साहसिक, बनावट का कोई जामा नहीं। जब भी लॉन के उस कोने तक जाती हूं, आम के वृक्ष की मीठी सी तुर्श–खट्टी गंध मेरे आसपास बहती है और खजुराहो का सच उसमें घुल जाता है।’ उस समय मैंने प्रेम की मांसलता में डूबी खजुराहो की ‘इरौटिक’ प्रतिमाओं की कल्पना की थी। मुझे यह नहीं पता था कि जब ‘पंचवटी’ फ़िल्म में रूपांतरित होगी तो उसमें प्रतिबिंबित होगी नेपाल के ‘स्वयंभू’ मंदिर की भगवान बुद्ध की अनगिनत सात्विक प्रतिमाएं, जिनके मध्य मेरी साधवी प्रेमिका से परिवर्तित होकर वास्तव में ‘साधवी’ की चेतना को आत्मसात कर लेगी कि वह अपने लिए... अपने में पूर्ण होकर अपना अस्तित्व जी सके।
पता नहीं वे कैसे दिन थे, जब दूरदर्शन पर पहले ‘तितलियां’ फिर ‘इसी बहाने’ और ‘इंद्रधनुष’ सीरियल मेरी क़लम से निकलकर मेरे सृजनात्मक लेखन को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं दिनों शोभा डॉक्टर के साथ एक दिन बासु भट्टाचार्य और दीप्ति नवल से भेंट हो गई। मेरे सामने की मेज़ पर मेरी पुस्तकें पड़ी थीं। ‘एक और पंचवटी’ को हाथ में उठाकर दीप्ति ने कहा–‘ आपने लिखा है यह उपन्यास...?’ ‘हां’ मैंने कंपकंपाते स्वर में कहा, बस बात आरंभ हो गई, बासु दा को ‘पंचवटी’ की कहानी भा गई और बात आगे बढ़ती चली गई... उपन्यास परावर्तन से परावर्तित रूप में ढलने के लिए।
पुस्तक और फ़िल्म दोनों के मध्य खड़े होकर मुझे लगा कि पुस्तक एक बंद दरवाज़ा है, जिसके पृष्ठ खोलने पर हाथ लगते हैं उनके दृश्य। वे दृश्य जहां फूल खिल रहे हैं, सूर्य उग रहा है, चांद आकाश पर टंगा है, और फ़िल्म एक ऐसा द्वार है, जहां खोलने को कुछ नहीं है, सभी कुछ आंखों के सम्मुख है, सामने घटित होता हुआ। उपन्यास पर बनी फ़िल्म कुछ ऐसी होती है कि झरने के ऊपर से कोई पत्थर उठा दे और झरना प्रपात बन जाए, या एक ऐसा दरवाज़ा बाहर-भीतर के दृश्य को समूची लैंडस्केप प्रदान करने में सफल हो जाए। आज के संदर्भ में सिनेमा ही एक ऐसा मीडिया है, जिसके माध्यम से अपनी बात हर वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है, ये बात अलग है कि उसका विवेचन या इंटरप्रटेशन सबका अपना-अपना होता है। जैसे कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के समय किसी पदार्थ के भीतर प्रवेश करता है, उसका विश्लेषण करता है। वैज्ञानिक का अनुसंधान बताता है पदार्थ, पदार्थ नहीं परमाणु है, दर्शक की सोच कहती है संसार जो दिखता है वह वैसा नहीं है, भ्रम है, धोखा है। ‘मैं’ के परमाणु हैं समूचे मानसिक अनुभव। ‘एक और पंचवटी’ कुछ ऐसी ही मानसिकता का उपन्यास है, जो समाज के मान्यता प्रधान नियमों (विवाह आदि) पर प्रश्न चिह्न ही नहीं लगाता हमें विचार करने को बाध्य करता है।
‘पंचवटी’ उपन्यास, फ़िल्म में परिवर्तित होकर जैसे सजीव हो उठा, जीवन के समानांतर बह निकला। उपन्यास के कथानक में नेपाल का कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु शोभा को नेपाल के साथ एक फ़िल्म बनानी थी। ‘पंचवटी’ की बात आने पर अपनी कहानी को किसी दूसरी धरती को सौंपना पहले मुझे अटपटा लगा, पर फिर समझौता तो मुझे करना ही था, क्योंकि ‘ना’ कहने में मैं बहुत कमज़ोर हूं, इंकार करना मैंने सीखा नहीं। तभी अपनी आदतों के कटघरे में, मैं क़ैद, चुपचाप खड़ी रह गई और पंचवटी के पात्र नेपाल की धरती पर पैर रख कर चलने लगे, उन्हें देखती तो लगता चरित्र तो मात्र क्रिएशन है–कल्पना की स्त्री और कल्पना का पुरुष यहां तक कि भगवान की आकृति भी वास्तविक नहीं है, वह भी हमारी इच्छानुसार की गई कल्पना के आधार पर रूप धरती है, इस समय भगवान पशुपतिनाथ के रूप में वे हमारे इष्ट थे।
‘पंचवटी’ के विक्रम और साधवी भी उस धरती पर उतर कर कल्पना से निकल वास्तविक हो गए थे–नेपाल की धरती उन्हें नए अर्थ दे रही थी। नेपाल से जुड़ते ही कथानक में इतना कुछ आ मिला था, मंदिर, बौद्ध भिक्षु, भगवान बुद्ध की अनगिनत प्रतिमाएं, और एक ऐसा अद्भुत चित्रकार, ‘कर्मसिद्धि जी’, जो अपनी कला को प्रार्थना के मंत्रों जैसा सुच्चा मानकर अपने चित्र फूलों की तरह भगवान के चरणों में अर्पित कर देता था। ऐसे श्रद्धा के अहसास से लिपटा समूचा कथानक अपने आप ही एक विशेष मानसिकता जीने लगा, नेपाल का प्राकृतिक सौंदर्य उसे एक सशक्त पृष्ठभूमि प्रदान करने में सार्थक हो गया और प्रकृति, प्रकृति न रहकर कहानी की एक ‘पात्र’ हो गई थी।
शूटिंग आरंभ होने के पहले दिन मैं ज़बरदस्ती, बासु दा और शोभा को पशुपतिनाथ के मंदिर ले गई–बासु दा लोकेशन खोज रहे थे और मैं भगवान का आशीर्वाद। बाहर द्वार पर मैंने पूजा की एक थाली ख़रीदी–हाथ में फल-फूल, होठों पर बुदबुदाते मंत्र लिए जैसे ही मंदिर के आंगन में प्रवेश किया, पता नहीं कहां से एक भारी-भरकम बंदर कूद कर आया और झपट्टा मारकर मेरी थाली का नैवेद्य उठा ले गया था–मैं चकराई सी खड़ी देखती रही, मेरा पात्र ख़ाली था, पदार्थ विहीन, इम्मेटीरियल...
मैंने पंचवटी को मात्र लिखा ही नहीं शिद्दत से जिया भी, झेला भी–मात्र लेखिका ही नहीं बची थी मैं, कभी सुरेश जी से उनके चरित्र की बात करती, कभी दीप्ति को अपने गहने-कपड़े ला देती और कभी अकबर के विवाह की पार्टी का आयोजन करती। आधी से अधिक फ़िल्म अपने ही फ़ार्म पर शूट हुई थी–अतः मेरे काम भी अनगिनत थे, कभी कमरे का फ़र्नीचर ठीक करती, क़ालीन बिछवाती, कभी ‘इकेबाना’ पद्घति से फूल सजाती, कभी ‘बौन्साई’ समेट लाती कि उनके बौना हो आए स्वरूप के माध्यम से अपनी नायिका की आंतरिक घुटन को बयान कर सकूं। फ़िल्म के हर दृश्य के साथ गुंथकर, मैं भी, जैसे अस्तित्ववान हो रही थी, या शायद होश में नहीं थी, इसलिए कि मुझे उन दिनों ‘पंचवटी’ से अलग कुछ भी सुझाई नहीं देता था। शायद इस कारण भी कि, अपने पात्रों को उपन्यास के पन्नों पर से उठकर सजीव हो जाने का अनुभव बहुत रोमांचक होता है। तभी तो उन दिनों मेरा अपना समूचा अस्तित्व एक अद्भुत अनुभूति से थरथराता रहता है। स्वप्न और इच्छाओं के मध्य एक बहुत महीन विभाजक रेखा होती है। ‘पचंवटी’ के कथानक से अनेकों प्रश्न उस रेखा से बाहर फिसल आए थे, जैसे कि, क्या किसी मनुष्य को जीते जी सुख का ऐसा कोई अपूर्व पल हाथ लग सकता है ? और यदि हां, तो क्या उस पल के सहारे पूरी पहाड़ जैसी उम्र को जिया जा सकता है ? क्या वास्तव में सुख का पल इतना बड़ा होता है ? ऐसी कोई ‘पचंवटी’ धरती पर है क्या ?
-डॉ. कुसुम अंसल
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i