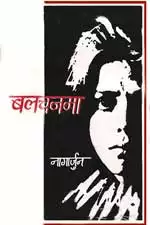|
विविध उपन्यास >> बलचनमा बलचनमानागार्जुन
|
288 पाठक हैं |
|||||||
बलचनमा प्रख्यात कवि और कथाकार नागार्जुन की एक सशक्त कथा-कृति और हिन्दी का पहला आंचलिक उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘बलचनामा’ के पिता का यही कसूर था कि वह जमींदार के बगीचे से
एक कच्चा आम तोड़कर खा गया। और इस एक आम के लिए उसे अपनी जान गँवानी पड़ गई।
गरीब जीवन की त्रासदी देखिए कि पिता की दुखद मृत्यु के दर्द से आँसू अभी सूखे भी नहीं थे कि उसी कसाई जमींदार की भैंस चराने के लिए बलचनमा को बाध्य होना पड़ा। पेट की आग के आगे पिता की मृत्यु का दर्द जैसे बिला गया !
उस निर्मम जमींदार ने दया खाकर उसे नौकरी पर नहीं रखा था...बेशक उसे ‘अक्षर’ का ज्ञान नहीं था, लेकिन ‘सुराज’, ‘इन्किलाब’ जैसे शब्दों से उसके अन्दर चेतना व्याप्त हो गई थी। और फिर शोषितों को एकजुट करने का प्रयास शुरु होता है-शोषकों से संघर्ष करने के लिए।
गरीब जीवन की त्रासदी देखिए कि पिता की दुखद मृत्यु के दर्द से आँसू अभी सूखे भी नहीं थे कि उसी कसाई जमींदार की भैंस चराने के लिए बलचनमा को बाध्य होना पड़ा। पेट की आग के आगे पिता की मृत्यु का दर्द जैसे बिला गया !
उस निर्मम जमींदार ने दया खाकर उसे नौकरी पर नहीं रखा था...बेशक उसे ‘अक्षर’ का ज्ञान नहीं था, लेकिन ‘सुराज’, ‘इन्किलाब’ जैसे शब्दों से उसके अन्दर चेतना व्याप्त हो गई थी। और फिर शोषितों को एकजुट करने का प्रयास शुरु होता है-शोषकों से संघर्ष करने के लिए।
एक
चौदह बरस की उम्र में मेरा बाप मर गया। परिवार में माँ, दादी और छोटी बहन
थी। नौ हाथ लम्बा, सात हाथ चौड़ा घर था-दो छप्परों वाला। सामने छोटा-सा
आँगन था। बाईं ओर आठ-दस धूर बाड़ी थी। उसमें साल के बारहों महीने
कुछ-न-कुछ उपजा लिया जाता। पिछवाड़े गिरहथ का इनारा था, पक्की जगत वाला।
सामने इन्हीं के खेत फैले पड़े थे। दाईं ओर कुछ हटकर उन्हीं लोगों का
पोखरा पड़ता था।
कहना न होगा कि वह थोड़ी सी जमीन, जिस पर हम बसे थे, गिरहथ लोगों की ही थी। अपने जीवन की सबसे पहली घटना जो मुझे याद है, वह खूब साफ नहीं है....मालिक के दरवाजे पर मेरे बार को एक खंभेली के सहारे कसकर बाँध दिया गया है। जाँघ, चूतर, पीठ और बाँह-सभी पर बाँस की हरी कैली के निशान उभर आये हैं। चोट से कहीं-कहीं खाल उधड़ गई है और आँखों से बहते आँसुओं के टंघार गाल और छाती पर से सूखते नीचे चले गये हैं...चेहरा काला पड़ गया है। होंठ सूख रहे हैं। अलग कुछ दूर छोटी चौकी पर यमराज की भाँति मझले मालिक बैठे हुए हैं। दाएँ हाथ की उँगलियाँ रह-रह मूँछों पर फिर जाती हैं...उनकी वह लाल और गहरी आँख कितनी डरावनी है, बार रे ! मेरी दादी काँपते हाथों मालिक के पैर छाने हुए हैं। उसके मुँह से बेचैनी में बस यही एक बात निकल रही है कि ‘‘दुहाई सरकार की, मर जायेगा ललुआ ! छोड़ दीजिए सरकार ! अब कभी ऐसा न करेगा ! दुहाई मालिक की। दुहाई माँ-बाप की...’’ और माँ रास्ते पर बैठी हाय-हाय करके रो रही है, और मैं भी रो रहा हूँ। मेरी छोटी बहन की तो डर के मारे हिचकी बँध गयी है।
सुना है मेरा बाप दोपहर के समय बाग से दो किसुनभोग तोड़ लाया था। किसुनभोग कच्चा भी खाने में खूब स्वादिष्ट होता है। ठीक वैसा ही जैसा भिगोया हुआ चावल। तोड़ते तो किसी ने देखा नहीं, मगर पुराने बखारों की ओट में बैठ-बैठ वह जब आम के छिलके उतार रहा था तो किसी ने देखा और जाकर चुगली कर दी। फिर क्या था, मँझले मालिक आग-बबूला हो गये और...
बाबू जब मरा तो दादी को चौठइया बुखार लग रहा था। कुछ मालिक से लेकर, कुछ इधर-उधर से जैसे-तैसे किरिया-करम हुआ और मेरे गले की उतरी टूटी। उसके बाद दादी और माँ की राय हुई कि मैं मालिकों की किसी पट्टी में चरवाहे का काम करूँ। दादी ने मना किया था-‘‘अभी खाने-खेलने के दिन हैं, इसी समय जोत दोगी तो कलेजा सूख जायेगा’’, इस पर माँ बोली थी कि ‘‘अभी से पेट की फिकर नहीं करेगा तो बहतरा हो जायेगा...’’
कुछ ही दिन बाद छोटे मालिक के यहाँ भैंस चराने का काम मिला है। भगवान ! कितनी कठिनाई से और कितना गिड़गिड़ाने पर छोटी मलिकाइन मुझे रखने को राजी हुई ! उनके यहाँ जब हम पहुँचे तो अपना मुलायम और गुलाबी हाथ चमकाकर दादी से उन्होंने कहा-‘‘अरे, यह तो मेरे बखारों को खुक्ख कर देगा। डेढ़ सेर इस जून, डेढ़ सेर उस जून। छोकड़े का पेट तो देखो, कमर से लेकर गले तक मानो बखिया है। कैसा बेडोल कितना भयानक है, मइया री मइया।’’
मेरी ओर सिनेह-भरी निगाहें डालती हुई शादी ने कहा-‘‘नहीं मलिकाइन, ऐसी बात न कहिए। मेरी बालचन मुट्ठी-भर से से अधिक भात नहीं खाता कोदो, मड़ुआ, मकई, साँवाँ, काँवन चाहे जिसकी भी रोटी दे दो, खुशी-खुशी खा लेगा और दो चुल्लू भर पानी पीकर सन्तोष की साँस लेता उठ जायेगा, बड़ा ही सुभर है, तनिक भी नहीं खलेगा, मलिकाइन !’’
मेरी कमर से फटी-सी मैली-सी बिस्ठी झूल रही थी। बिस्ठी न तो लँगोटी है न कच्छा, कपड़े के लीरे को अगर तुम कोपीन की भाँति पहन लो तो वही हमारे यहाँ बिस्ठी कहलायेगी। मलिकाइन ने बिस्ठी की ओर इशारा करके कहा-‘‘कपड़ा-वपड़ा हमसे पार नहीं लगेगा।’’ यह सुनकर दादी ने दाँत निपोड़ दिये। चेहरे की झुर्रियों और लकीरों में बल पड़ गया दोनों हाथ जोड़कर वह गिड़िगिड़ाई-‘‘क्या कमी मलिकाइन, आप लोगों के यहाँ ? आप ही का तो आसरा है, नहीं तो हम गरीब जनमते ही बच्चों को नमक न चटा दें ! अरे, अपना जूठन खिलाकर, अपना फेरन-फारन पहनाकर ही तो हमारा पर्तपाल करती हैं...’’
छोटी मलिकाइन का चेहरा खिल गया, उनके दाँत दनुफ के फूल जैसे झकझक कर रहे थे। होठों की लाली बड़ी भली लगती थी। मेरी दादी पर अहसान कर मनो भार लादती हुई वह बोलीं-‘खाना पीना, लत्ता कपड़ा और ऊपर से दो आना महीना ! कौन देगा इतना ? अभी सारा काम इसे सिखाना पड़ेगा। समझाते-समझाते दिमाग का गूदा चट हो जायेगा।’’
दादी ने मलिकाइन के पैर पकड़ लिये-‘‘आज से आप ही इस निभागे की माँ-बाप हुई गिरहथनी ! आपका जूठन खाकर इसका भाग चमकेगा...’’
अगले दिन से मैं काम करने लगा। बतला ही चुका हूँ, चौदह साल की उमर थी। यों खास काम मेरा भैंस चराना था, फिर भी और कई काम थे जैसे कि बच्चे को खेलाना, पानी भरना, बाहर बैठक में झाड़ू लगाना, दुकान से नून, तेल, मसाला लाना और मलिकाइन के पैर चाँपने...
चौधरी लोगों का यह घराना किसी जमाने बहुत ही भरापूरा और अकबाली था। अब इनकी जमीनदारी तो नहीं थी, लेकिन रोब-दाब रहन-सहन चाल ढाल और बातचीत से हूकुमत की बड़ी बिकट बू आती थी। चार पट्टियों में बँटे थे लोग। अलग-अलग हवेलियाँ थीं। बची-खुची जमीन-जायदाद बँटी हुई थी। गाछी, कमलबाग बाँस, पोखर, खढ़ोर और चरागाह यह सब साझा चला आ रहा था। बीजू या शरही (देशी) आमों का बाग गाछी कहलाता है। बीस बीघा में फैले हुए थे। उनके बाग, हजार के लगभग पेड़ होंगे। कलमबाग भी काफी बड़ा था। बाँस भी तीन सौ बीट थे-तीन बीघे में फैले हुए। पोखर उनके तीन थे। खढ़ोर इतना बड़ा था कि सभी पटीदारों को अपने मकान छवाने लायक खर उसी से निकल आता। चरागाह थी तो बड़ी, लेकिन ऊसर हो गई थी। इसके अलावा सीसम, महुआ, तूत, इमली, जीमड़ जैसे तरह-तरह के सैकड़ों पेड़ों से भरा एक जंगल था।
पहले दिन सुबह-सुबह भैंस खोलकर जब मैं चराने ले चला तो अभी काफी सबेरा था। मुझे डर लगा। दादी के मुँह से भूत-प्रेत की कहानियाँ रोज ही सुनी थीं। गाँव के बाहर का हर एक बूढ़ा पीपल या बरगद मेरे लिए भूतों का रैन बसेरा था। भैंस सीधी-सादी थी, नाकों में नकेल थी। नकेल की रस्सी को हाथ में लपेटकर भैंस की पीठ पर मैं बैठ गया और वह अपनी इच्छा से पूरब की ओर चल पड़ी। जेठ का महीना था। इस साल आम नहीं फरे थे। इसलिए चरवाहे बागों में ले जाकर अपनी भैसों को छोड़ देते थे और खुद भैंस की पीठ पर पड़े-पड़े सुबह की मीठी नींद के झोंके लेते रहते। उन्हें इस तरह सोते देखकर मुझे कई बार डाह हुई थी, पर आज तो मैं खुद भैंस की पीठ पर सवार था।
छोटे मालिक किसी राजा के यहाँ मनेजरी करते थे। परिवार को कभी उन्होंने साथ नहीं रक्खा। मलिकाइन बहुत बड़े घर की बेटी थीं। बिना दूध दही का खाना। उनके कहने के मुताबिक बालू गोबर निगलना था। दो सौ रुपये लगाकर गुजराती नसल की यह भैंस उन्होंने मालिक से खरीदवाई। सेवा नहीं होने से भैंस बड़ी दुबली हो रही थी। पड़िया मर जाने से बिसुक गई थी। पुट्ठों का हाड़ और रीढ़ निकल आई थी। पुराना चरवाहा भागकर कटिहार चला गया था, चटकल में। फिर उन्होंने एक जवान दुसाध को इस काम के लिए रक्खा। उसकी एक ग्वालिन से साँठ-गाँठ हो गई तो मझले मालिक को इस बात का पता लग गया। पकड़े जाने पर उन्होंने उसे जूतों से इतना पीटा कि आधा पहर तक बेचारा आह-ऊह भी न कर सका, भाग तो गया ही..
अब भैंस मेरे सुपुर्द थी। पहले दिन मालिक के बाग में ही मैं उसे चरा ले आया। दूसरे दिन से तो वह मुझे पहचानने लगी। अभी तक माँ, दादी और रेबनी (छोटी बहन) से ही हिला-मिला हुआ था। बाबू चल ही बसा था। उन चारों के बाद वह भैंस ही थी जिसकी गीली आँख और गरम साँस मुझ पर अपना असर डाल सकी। सुबह-सुबह मैं रोज उसे चरा लाता। पहर दिन उठने पर मलिकाइन मुझे कलेवा देतीं, मड़ुआ की लाल रोटी। नोन और सरसों के तेल साथ में जब वह रोटी खा लेता, तो छोटा बच्चा मेरे जिम्मे कर दिया जाता। यह लड़का मानो रोना ही जानता था। घड़ी भर में ही उसकी रुलाई से मेरा माथा दुखने लगता। चुप करने की सारी कोशिशें बेकार जातीं और तब खस की कूची से बाल झारती हुई मलिकाइन सिर नीचा किये ही डपटकर मुझे कहतीं-‘‘कंधे के सहारे बच्चे को ले-ले और घूमघाम, माँ ने तुझे ठूँस-ठूँसकर खाना तो खूब सिखला दिया है, मगर फूल सा हलका बच्चा भी तुझसे नहीं सँभलता कोढ़िया !’’
गालियाँ सुनकर पहले दो चार दिन तो मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ हुई पर बाद में कान खूब पक्के हो गये। गदहा, सुअर, कुत्ता उल्लू...क्या नहीं कहती थीं वह मुझे ? उनका गुस्सा चुपचाप सह जाना मुझे सीखना पड़ा। एक बार दोपहर को घास लाने में जरा देर हो गई। बैसाख जेठ की जलती धरती हो तो घास छीलने में बड़ी कठिनाई होती है। पचीसों जगह खुरपी चला-चलाकर तंग आ जाओगे फिर भी टोकरी भर घास नहीं होगी। लेकिन जो देवी कई-कई डेवढ़ियों वाली हवेलियों के भीतर छाँह में आराम से बैठी हुई हों, उन्हें अपनी यह दिक्कत तुम समझा पाओगे भैया ? उनके लिए सारी धरती हरी-हरी, नरम-नरम दूबों में भरी होती है। सो उस रोज घास लेकर जब मैं जरा देर से पहुँचा तो मलिकाइन हुहुआ उठीं-‘‘मर क्यों न गया ? बड़े नवाब के नाती हुए हैं। कहीं बैठकर बाप के साथ कौड़ी खेल रहा होगा और देर हो गई तो घास नहीं मिलती है, खुरपी भोथी है, बेट ढीला पड़ गया था...पचास बहाने बनाता है। कलमुँहा !’’ इतना बक चुकने पर जब उन्हें सन्तोष न हुआ तो झाड़ू उठा लाई और मेरी पीठ पर कई बार झट झट बरसा दिये। मैं तिलमिलाकर वहीं बैठ गया-बाप-बाप कर उठा।
वह जब बहुत खुश होती तो सूखा या बासी पकवान, सड़ा आम, फटे दूध का बदबूदार छेना या जूठन की बची हुई कड़वी तरकारी देती हुई मुझे कहतीं-‘‘बलचनमा, ऐसी अच्छी चीज तेरे बाप-दादे ने भी नहीं खाई होगी।’’
किसी चीज की कमी नहीं थी। मालिक ढाई सौ रुपया महीना कमाते थे। मलिकाइन के मायके से भी महीने में दो एक भार आ ही जाता था। यो तो भार का मतलब है बोझा, मगर सौगात में एक गाँव से दूसरे गाँव भेजे जाने वाले ये भार मामूलीढंग के नहीं होते। बाँस की लचकदार बहँगी कंधे पर होती है, उसके दोनों छोर से लटकते छिक्कों पर दही का छाछ, चिवड़ा से भरा चँगेरा, केले की घौद पकवानों या मिठाइयों से भरी डालियाँ, धोती-साड़ी लहठी ऐसा ही और भी कुछ डाल दिया जाता है; बस यही भार कहलाता है। इसको लेकर चलने वाले भरिया कहलाते हैं। तुम इन्हें बोझ ढोनेवाले मजूर समझ लो। मलिकाइन के मायके से कभी-कभी ऐसा ही भार आता था सौगात की सारी चीजों को वह टोला-पड़ोस के छोटे-बड़े घरों में बायना के तौर पर बँटवा देती थीं। हाँ, चावल, चिवड़ा साड़ी, लहठी जैसी वस्तुएँ बायने में नहीं दिया जाता।
दही जब बहुत खट्टा हो जाता था, उससे बदबू आने लगती थी और वह उनके अपने या किसी पड़ोसी के खाने लायक न रह जाता तब मुझे मिलता। मैं उस दही को खुशी-खुशी खा लेता। याद आता है कि एक बार जास्ती खट्टा और बदबूदार रहने से उस दही को नहीं खा पाया तो मालिकाइन ने सजा दी थी-अगले दिन खाना नहीं मिला था।
भैंस चराना मुझे खूब पसन्द था। गाँव के बाहर मेरी ही उमर के जब और चरवाहे इकट्ठे होते तो हम अपना-अपना दुःख भूलकर खेलते। कभी कौड़ी उछालते, कभी बकरी की सूखी मींगणियों से सतधरा खेलते, कभी कंकडों से कौवाठुट्ठी मोगल पठान या बाघ गोटी का भी खेल चलता। हमारी भैंसे दूब भरे मैदान या चरागाह में चरती होती और हम अपने मालिकों की बुरी भली कहते सुनते और खेला करते। बड़े मालिक का चरवाहा बूढ़ा था, सबूरीमंडल। ठिगने कद का बूढ़ा धानुक। कान दोनों बुच थे। कपार छोटा। आँखें चमकदार मगर धँसी हुईं। बाल सन जैसे सफेद। अपने पशु की सेवा वह बड़ी ही लगन से करता। हमें अपने बीते दिनों की कहानियाँ सुनाते कभी न थकता था। खेल में मशगूल पाकर बहुधा हमको वह फटकारता भी।
और जो कुछ हो, सबूरी काका की दो बातें मैं अभी तक नहीं भूल पाया। एक तो यह कि अपनी भैंस को वह शायद ही पीटता और दूसरी यह कि सगी सन्तान की तरह उनकी सेवा। उसकी भैंस की आँखों में कभी किसी ने कीचड़ नहीं देखा। हर तीसरे दिन वह उसे तालाब में ले जाकर नहलाता, मुलायम दूबों की नूड़ी से भैंस की पीठ, पेट, पुट्ठे, जाँघ, गर्दन, माथ और पैर को भली भाँति रगड़ता। इस तरह अपनी भैंस को वह साफ सुथरी रखता...हम तो खैर थोड़ी ही उमर के थे, जिनकी उमर बड़ी थी उन चरवाहों से भी अपनी भैंसों की ऐसी सेवा पार नहीं लगती।
एक दिन मैं दोपहर के वक्त बड़े मालिक के बथान पर गया। उनके सोलह बैल थे और चार भैंसे थीं। चरवाहे तीन थे। सबूरी के जिम्मे दो भैंसे थीं। वहीं अलग एक झोंपड़ी में रहते थे। जिस समय मैं उनके पास गया तब वह हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। नारियल की पेंदी वाला इसी तरह का हुक्का मेरा भी बाप पीता था। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। आँखें उठाकर अपने नजदीक बैठने को उन्होंने इशारा किया। थोड़ी देर बाद बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा-‘‘तुम्हारी भैंस का यह सातवाँ महीना चल रहा है न ?’’
‘‘हाँ’’, मैंने कहा-‘‘बाबा, यह तुम कैसे जान गये ?’’
इस पर पतली मूँछों वाले उनके होंठ खिल उठे। सच, जोर से ठहाका लगाते उन्हें कभी नहीं देखा। बहुत हुआ तो खिलखिला पड़े, और तब बिना दाँत के उनके वे लाल मसूड़ें बड़े ही सुन्दर लगते। हुक्के को खूँटे से टिकाकर और चिलम को उलटाकर मंडल ने कहा-‘जिन्दगी भर तो भैंस ही चरायी है बलचनमा ! मैं जब ननिहाल से भागकर यहाँ आया तो बाइस साल का था। तेरा बाप लालचन्द तेरी ही उमर का रहा होगा..लच्छन से मालूम होता है कि तेरी भैंस के पेट में सात महीने की पड़िया है।’’
यह सुनकर मैं दंग रह गया। वह उठकर भैंस के पास जा बैठे। थनों से ऊपर वाली उसकी नसों को सहलाते हुए काका बोले-‘‘खाली बखत में इधर-उधर भटकना ठीक नहीं। चरवाहे को चाहिए कि अपने पशु के रोएँ-रोएँ को गौर से देखें। लापरवाही से कई तरह के कीड़े पड़ जाते हैं-अठौड़ी, किलनी, जूँ, चिल्लड़ कभी-कभी कुकुरमाछी भी इन्हें तंग करती है। इन बातों का ख्याल चरवाहा न रक्खेगा तो कौन रक्खेगा। इसके अलावा उनके रहने की जगह को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है....आजकल के चरवाहे हराम का खाते हैं, तभी तो उनका जानवर कलफ्ता रहता है।’’
उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सबूरी काका भैंस की सेवा करने में बड़े ही होशियार हैं, इनके पास घड़ी-आध रोज आकर बैठूँ तो बहुत सी बातें यों ही समझ में आ जायेंगी। और तब से जब कभी मुझे मौका मिलता तभी जाकर सबूरी मंडल के पास जा बैठता। हम एक बिरादरी के नहीं थे। वह थे धानुक मैं ठहरा ग्वाला। वह थे सबूरी मंडल मैं था बालचंद राउत, फिर भी दादा परदादा की तरह वह मुझे प्यार करते। कहीं कोई खाने-वाने की अच्छी चीज मिल जाती तो उसमें से थोड़ा कुछ मेरे लिए सँजोकर रखते। मुझसे और तो कुछ नहीं होता मगर रात को कभी –कभी जाकर पैर चाँप आता था।
मालिक की नौकरी ऐसी थी कि छुट्टी का नाम नहीं। तब भी छठे-छमाहे आ वह जरूर जाते। दो-चार दिन रहकर वह विदा होते तो इसटीसन तक सामान मुझे ही पहुँचाना पड़ता। चमड़े का छोटा सा सूटकेस होल्डाल में बँधा हुआ बिस्तरा-यह दोनों सिर पर और हाथ में टिफिन का डिब्बा। रामपुर से मधुबनी ढाई कोस पक्का पड़ता है। उठते-बैठते किसी तरह मैं पहुँचता। गरदन टूट जाती। पसीने से सारी देह तर हो होकर सूख चुकी होती। और इतने पर भी जब मालिक की गाड़ी पलेटफारम छोड़कर खिसकने लगती तो दो पैसा मेरी ओर फेंककर वह कहते-‘‘ले मूढ़ी या चना खरीद लेना, फाँकते-फाँकते घंटे भर में पहुँच जायेगा।’’
मन करता कि उन पैसों को वहीं पलेटफारम पर ही छोड़कर चल दूँ ! आखिर मैं वह पैसा उठा लेता। पैसे के चने और पैसे की बीड़ी, किसी तरह घर पहुँचता और माँ के पास धम्म से जा गिरता।
माँ मेरे बाप की ब्याही औरत नहीं थी। पहले ब्याह की औरत जब मर गई तो बाप कुछ रोज कलकत्ता रह आया था। बाद में जिस विधवा से संबंध हुआ वही थी मेरी माँ। दादी को भैंस चराने का मेरा यह काम पसन्द नहीं था। बहन थी छोटी, उसकी राय का कोई सवाल ही नहीं। हमारे पास कुल सात कट्ठा जमीन थी। मझले मालिक सौ कमाई के एक कसाई थे। बाबू के मरने पर बारह रुपये उन्होंने माँ को कर्ज दिये थे। बदले में सादे कागज पर अँगूठे का निशान ले लिया था। सूद देते-देते हम थक गये, मूल ज्यों-का-त्यों खड़ा था। छोटी मलिकाइन दुअन्नी के हिसाब से साल भर का दरमहा डेढ़ रुपैया देती थीं, उतने से क्या होता...
जाड़े की एक-एक रात हमारे लिए परलय की डुगडुगी बजाती आती थी। गर्मी के दिन जैसे-तैसे कट जाते, लेकिन जाड़ा से निबटना बड़ा ही मुश्किल होता। गुदड़ी कथड़ी भी ओढ़ने को अगर काफी न हो तो पूस माघ की ठंडी रात यमराज की बहन साबित होती है। जलावन के लिए लड़की भला हम लाते ही कहाँ से, हाँ, दादी ने दो बकरियाँ पाल रक्खी थीं, उनकी सूखी मींगणियाँ ताप-तापकर हम रात काटते। मालिकों के पास न लड़की की कमी, न घास फूस की। गोइठा, गोहरा भी उन्हीं के पास होता जिनके माल जाल हों। माल जाल के नाम पर हमारे यहाँ दो बकरियाँ थीं। आम, तलाम, जामुन, कटहर, बेर, कुसियार, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा...हमारा पेट भरने में इनसे काफी मदद मिलती। दादी अँधेरे में निकल जाती और मालिक के बाग से आम ले आती। गन्ना और दूसरे मौसमी फलों का यही हाल था। छोटी चीजें चुराने में मेरी दादी कमाल करती थी। वह कभी नहीं पकड़ी गई। माँ से यह काम नहीं होता था।
गाँव के बाहर जाड़े के दिनों में हर साल मालिकों का कोल्हू गड़ता। उनके यहाँ गन्ने की खेती कम नहीं होती। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर रात को कोल्हूआड़ में ही बिताया करता। गन्ना खा-खाकर पेट भर लेना और भट्ठी की आँच से गरमाकर सो जाना। डेढ़-दो महीने हर साल जाड़ों में हम ऐसा ही करते।
मझले मालिक की निगाह हमारे उन थोड़े से खेतों पर थी जिनमें मडुवा उपजाकर तीन चार महीने का खर्च हम निकालते आये थे। उन्होंने सोचा-लौंडा अभी छोटा है। जमाने का रंग-ढंग अच्छा नहीं। कमाने लायक होने पर कटिहार या कलकत्ता कहीं-न-कहीं जरूर भाग जायेगा, फिर कोई इसका क्या कर लेगा ! अभी तो खैर इस औरतिया का अँगूठा निशान अपने कब्जे में है..
सोच-समझकर एक दिन मझले मालिक ने हम तीनों को बुलाया। वहाँ गाँव के बूढ़े पंडित भी बैठे थे। आधा पीतल और आधा लोहे से बना सरौता मालिक के हाथ में था। वह सुपारी कतर रहे थे। कुछ बारीक कतरा पंडितजी की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा-‘‘ललचनमा जब तक जिया, जी जान से मेरी सेवा उसने की और इनको तो देखिए।’’
पंडित जी ने सुपारी फाँक लिया। फिर टूटे डंठल वाले चश्मे को नाक पर से हटाकर कपार पर चढ़ाया। मेरी ओर तनिक देर गौर से ताकते रहे। तब जाकर बोले-‘‘जसोधर बाबू, छोकड़े के रोआँ-रोआँ से नमक-हरामी टपकती है। देखो न, कैसे मुलुर-मुलुर ताकता है।’’
इस पर मझले मालिक ने कहा-‘‘हाँ गुरु, बड़ा ही पाती है। कभी पकड़ में नहीं आता। पाहुना आये थे, उनका नौकर बीमार पड़ गया। मैंने इस ससुर को कहला भेजा कि आकर मेहमान की मालिश कर जाय। साला आया ही नहीं...’’
कहना न होगा कि वह थोड़ी सी जमीन, जिस पर हम बसे थे, गिरहथ लोगों की ही थी। अपने जीवन की सबसे पहली घटना जो मुझे याद है, वह खूब साफ नहीं है....मालिक के दरवाजे पर मेरे बार को एक खंभेली के सहारे कसकर बाँध दिया गया है। जाँघ, चूतर, पीठ और बाँह-सभी पर बाँस की हरी कैली के निशान उभर आये हैं। चोट से कहीं-कहीं खाल उधड़ गई है और आँखों से बहते आँसुओं के टंघार गाल और छाती पर से सूखते नीचे चले गये हैं...चेहरा काला पड़ गया है। होंठ सूख रहे हैं। अलग कुछ दूर छोटी चौकी पर यमराज की भाँति मझले मालिक बैठे हुए हैं। दाएँ हाथ की उँगलियाँ रह-रह मूँछों पर फिर जाती हैं...उनकी वह लाल और गहरी आँख कितनी डरावनी है, बार रे ! मेरी दादी काँपते हाथों मालिक के पैर छाने हुए हैं। उसके मुँह से बेचैनी में बस यही एक बात निकल रही है कि ‘‘दुहाई सरकार की, मर जायेगा ललुआ ! छोड़ दीजिए सरकार ! अब कभी ऐसा न करेगा ! दुहाई मालिक की। दुहाई माँ-बाप की...’’ और माँ रास्ते पर बैठी हाय-हाय करके रो रही है, और मैं भी रो रहा हूँ। मेरी छोटी बहन की तो डर के मारे हिचकी बँध गयी है।
सुना है मेरा बाप दोपहर के समय बाग से दो किसुनभोग तोड़ लाया था। किसुनभोग कच्चा भी खाने में खूब स्वादिष्ट होता है। ठीक वैसा ही जैसा भिगोया हुआ चावल। तोड़ते तो किसी ने देखा नहीं, मगर पुराने बखारों की ओट में बैठ-बैठ वह जब आम के छिलके उतार रहा था तो किसी ने देखा और जाकर चुगली कर दी। फिर क्या था, मँझले मालिक आग-बबूला हो गये और...
बाबू जब मरा तो दादी को चौठइया बुखार लग रहा था। कुछ मालिक से लेकर, कुछ इधर-उधर से जैसे-तैसे किरिया-करम हुआ और मेरे गले की उतरी टूटी। उसके बाद दादी और माँ की राय हुई कि मैं मालिकों की किसी पट्टी में चरवाहे का काम करूँ। दादी ने मना किया था-‘‘अभी खाने-खेलने के दिन हैं, इसी समय जोत दोगी तो कलेजा सूख जायेगा’’, इस पर माँ बोली थी कि ‘‘अभी से पेट की फिकर नहीं करेगा तो बहतरा हो जायेगा...’’
कुछ ही दिन बाद छोटे मालिक के यहाँ भैंस चराने का काम मिला है। भगवान ! कितनी कठिनाई से और कितना गिड़गिड़ाने पर छोटी मलिकाइन मुझे रखने को राजी हुई ! उनके यहाँ जब हम पहुँचे तो अपना मुलायम और गुलाबी हाथ चमकाकर दादी से उन्होंने कहा-‘‘अरे, यह तो मेरे बखारों को खुक्ख कर देगा। डेढ़ सेर इस जून, डेढ़ सेर उस जून। छोकड़े का पेट तो देखो, कमर से लेकर गले तक मानो बखिया है। कैसा बेडोल कितना भयानक है, मइया री मइया।’’
मेरी ओर सिनेह-भरी निगाहें डालती हुई शादी ने कहा-‘‘नहीं मलिकाइन, ऐसी बात न कहिए। मेरी बालचन मुट्ठी-भर से से अधिक भात नहीं खाता कोदो, मड़ुआ, मकई, साँवाँ, काँवन चाहे जिसकी भी रोटी दे दो, खुशी-खुशी खा लेगा और दो चुल्लू भर पानी पीकर सन्तोष की साँस लेता उठ जायेगा, बड़ा ही सुभर है, तनिक भी नहीं खलेगा, मलिकाइन !’’
मेरी कमर से फटी-सी मैली-सी बिस्ठी झूल रही थी। बिस्ठी न तो लँगोटी है न कच्छा, कपड़े के लीरे को अगर तुम कोपीन की भाँति पहन लो तो वही हमारे यहाँ बिस्ठी कहलायेगी। मलिकाइन ने बिस्ठी की ओर इशारा करके कहा-‘‘कपड़ा-वपड़ा हमसे पार नहीं लगेगा।’’ यह सुनकर दादी ने दाँत निपोड़ दिये। चेहरे की झुर्रियों और लकीरों में बल पड़ गया दोनों हाथ जोड़कर वह गिड़िगिड़ाई-‘‘क्या कमी मलिकाइन, आप लोगों के यहाँ ? आप ही का तो आसरा है, नहीं तो हम गरीब जनमते ही बच्चों को नमक न चटा दें ! अरे, अपना जूठन खिलाकर, अपना फेरन-फारन पहनाकर ही तो हमारा पर्तपाल करती हैं...’’
छोटी मलिकाइन का चेहरा खिल गया, उनके दाँत दनुफ के फूल जैसे झकझक कर रहे थे। होठों की लाली बड़ी भली लगती थी। मेरी दादी पर अहसान कर मनो भार लादती हुई वह बोलीं-‘खाना पीना, लत्ता कपड़ा और ऊपर से दो आना महीना ! कौन देगा इतना ? अभी सारा काम इसे सिखाना पड़ेगा। समझाते-समझाते दिमाग का गूदा चट हो जायेगा।’’
दादी ने मलिकाइन के पैर पकड़ लिये-‘‘आज से आप ही इस निभागे की माँ-बाप हुई गिरहथनी ! आपका जूठन खाकर इसका भाग चमकेगा...’’
अगले दिन से मैं काम करने लगा। बतला ही चुका हूँ, चौदह साल की उमर थी। यों खास काम मेरा भैंस चराना था, फिर भी और कई काम थे जैसे कि बच्चे को खेलाना, पानी भरना, बाहर बैठक में झाड़ू लगाना, दुकान से नून, तेल, मसाला लाना और मलिकाइन के पैर चाँपने...
चौधरी लोगों का यह घराना किसी जमाने बहुत ही भरापूरा और अकबाली था। अब इनकी जमीनदारी तो नहीं थी, लेकिन रोब-दाब रहन-सहन चाल ढाल और बातचीत से हूकुमत की बड़ी बिकट बू आती थी। चार पट्टियों में बँटे थे लोग। अलग-अलग हवेलियाँ थीं। बची-खुची जमीन-जायदाद बँटी हुई थी। गाछी, कमलबाग बाँस, पोखर, खढ़ोर और चरागाह यह सब साझा चला आ रहा था। बीजू या शरही (देशी) आमों का बाग गाछी कहलाता है। बीस बीघा में फैले हुए थे। उनके बाग, हजार के लगभग पेड़ होंगे। कलमबाग भी काफी बड़ा था। बाँस भी तीन सौ बीट थे-तीन बीघे में फैले हुए। पोखर उनके तीन थे। खढ़ोर इतना बड़ा था कि सभी पटीदारों को अपने मकान छवाने लायक खर उसी से निकल आता। चरागाह थी तो बड़ी, लेकिन ऊसर हो गई थी। इसके अलावा सीसम, महुआ, तूत, इमली, जीमड़ जैसे तरह-तरह के सैकड़ों पेड़ों से भरा एक जंगल था।
पहले दिन सुबह-सुबह भैंस खोलकर जब मैं चराने ले चला तो अभी काफी सबेरा था। मुझे डर लगा। दादी के मुँह से भूत-प्रेत की कहानियाँ रोज ही सुनी थीं। गाँव के बाहर का हर एक बूढ़ा पीपल या बरगद मेरे लिए भूतों का रैन बसेरा था। भैंस सीधी-सादी थी, नाकों में नकेल थी। नकेल की रस्सी को हाथ में लपेटकर भैंस की पीठ पर मैं बैठ गया और वह अपनी इच्छा से पूरब की ओर चल पड़ी। जेठ का महीना था। इस साल आम नहीं फरे थे। इसलिए चरवाहे बागों में ले जाकर अपनी भैसों को छोड़ देते थे और खुद भैंस की पीठ पर पड़े-पड़े सुबह की मीठी नींद के झोंके लेते रहते। उन्हें इस तरह सोते देखकर मुझे कई बार डाह हुई थी, पर आज तो मैं खुद भैंस की पीठ पर सवार था।
छोटे मालिक किसी राजा के यहाँ मनेजरी करते थे। परिवार को कभी उन्होंने साथ नहीं रक्खा। मलिकाइन बहुत बड़े घर की बेटी थीं। बिना दूध दही का खाना। उनके कहने के मुताबिक बालू गोबर निगलना था। दो सौ रुपये लगाकर गुजराती नसल की यह भैंस उन्होंने मालिक से खरीदवाई। सेवा नहीं होने से भैंस बड़ी दुबली हो रही थी। पड़िया मर जाने से बिसुक गई थी। पुट्ठों का हाड़ और रीढ़ निकल आई थी। पुराना चरवाहा भागकर कटिहार चला गया था, चटकल में। फिर उन्होंने एक जवान दुसाध को इस काम के लिए रक्खा। उसकी एक ग्वालिन से साँठ-गाँठ हो गई तो मझले मालिक को इस बात का पता लग गया। पकड़े जाने पर उन्होंने उसे जूतों से इतना पीटा कि आधा पहर तक बेचारा आह-ऊह भी न कर सका, भाग तो गया ही..
अब भैंस मेरे सुपुर्द थी। पहले दिन मालिक के बाग में ही मैं उसे चरा ले आया। दूसरे दिन से तो वह मुझे पहचानने लगी। अभी तक माँ, दादी और रेबनी (छोटी बहन) से ही हिला-मिला हुआ था। बाबू चल ही बसा था। उन चारों के बाद वह भैंस ही थी जिसकी गीली आँख और गरम साँस मुझ पर अपना असर डाल सकी। सुबह-सुबह मैं रोज उसे चरा लाता। पहर दिन उठने पर मलिकाइन मुझे कलेवा देतीं, मड़ुआ की लाल रोटी। नोन और सरसों के तेल साथ में जब वह रोटी खा लेता, तो छोटा बच्चा मेरे जिम्मे कर दिया जाता। यह लड़का मानो रोना ही जानता था। घड़ी भर में ही उसकी रुलाई से मेरा माथा दुखने लगता। चुप करने की सारी कोशिशें बेकार जातीं और तब खस की कूची से बाल झारती हुई मलिकाइन सिर नीचा किये ही डपटकर मुझे कहतीं-‘‘कंधे के सहारे बच्चे को ले-ले और घूमघाम, माँ ने तुझे ठूँस-ठूँसकर खाना तो खूब सिखला दिया है, मगर फूल सा हलका बच्चा भी तुझसे नहीं सँभलता कोढ़िया !’’
गालियाँ सुनकर पहले दो चार दिन तो मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ हुई पर बाद में कान खूब पक्के हो गये। गदहा, सुअर, कुत्ता उल्लू...क्या नहीं कहती थीं वह मुझे ? उनका गुस्सा चुपचाप सह जाना मुझे सीखना पड़ा। एक बार दोपहर को घास लाने में जरा देर हो गई। बैसाख जेठ की जलती धरती हो तो घास छीलने में बड़ी कठिनाई होती है। पचीसों जगह खुरपी चला-चलाकर तंग आ जाओगे फिर भी टोकरी भर घास नहीं होगी। लेकिन जो देवी कई-कई डेवढ़ियों वाली हवेलियों के भीतर छाँह में आराम से बैठी हुई हों, उन्हें अपनी यह दिक्कत तुम समझा पाओगे भैया ? उनके लिए सारी धरती हरी-हरी, नरम-नरम दूबों में भरी होती है। सो उस रोज घास लेकर जब मैं जरा देर से पहुँचा तो मलिकाइन हुहुआ उठीं-‘‘मर क्यों न गया ? बड़े नवाब के नाती हुए हैं। कहीं बैठकर बाप के साथ कौड़ी खेल रहा होगा और देर हो गई तो घास नहीं मिलती है, खुरपी भोथी है, बेट ढीला पड़ गया था...पचास बहाने बनाता है। कलमुँहा !’’ इतना बक चुकने पर जब उन्हें सन्तोष न हुआ तो झाड़ू उठा लाई और मेरी पीठ पर कई बार झट झट बरसा दिये। मैं तिलमिलाकर वहीं बैठ गया-बाप-बाप कर उठा।
वह जब बहुत खुश होती तो सूखा या बासी पकवान, सड़ा आम, फटे दूध का बदबूदार छेना या जूठन की बची हुई कड़वी तरकारी देती हुई मुझे कहतीं-‘‘बलचनमा, ऐसी अच्छी चीज तेरे बाप-दादे ने भी नहीं खाई होगी।’’
किसी चीज की कमी नहीं थी। मालिक ढाई सौ रुपया महीना कमाते थे। मलिकाइन के मायके से भी महीने में दो एक भार आ ही जाता था। यो तो भार का मतलब है बोझा, मगर सौगात में एक गाँव से दूसरे गाँव भेजे जाने वाले ये भार मामूलीढंग के नहीं होते। बाँस की लचकदार बहँगी कंधे पर होती है, उसके दोनों छोर से लटकते छिक्कों पर दही का छाछ, चिवड़ा से भरा चँगेरा, केले की घौद पकवानों या मिठाइयों से भरी डालियाँ, धोती-साड़ी लहठी ऐसा ही और भी कुछ डाल दिया जाता है; बस यही भार कहलाता है। इसको लेकर चलने वाले भरिया कहलाते हैं। तुम इन्हें बोझ ढोनेवाले मजूर समझ लो। मलिकाइन के मायके से कभी-कभी ऐसा ही भार आता था सौगात की सारी चीजों को वह टोला-पड़ोस के छोटे-बड़े घरों में बायना के तौर पर बँटवा देती थीं। हाँ, चावल, चिवड़ा साड़ी, लहठी जैसी वस्तुएँ बायने में नहीं दिया जाता।
दही जब बहुत खट्टा हो जाता था, उससे बदबू आने लगती थी और वह उनके अपने या किसी पड़ोसी के खाने लायक न रह जाता तब मुझे मिलता। मैं उस दही को खुशी-खुशी खा लेता। याद आता है कि एक बार जास्ती खट्टा और बदबूदार रहने से उस दही को नहीं खा पाया तो मालिकाइन ने सजा दी थी-अगले दिन खाना नहीं मिला था।
भैंस चराना मुझे खूब पसन्द था। गाँव के बाहर मेरी ही उमर के जब और चरवाहे इकट्ठे होते तो हम अपना-अपना दुःख भूलकर खेलते। कभी कौड़ी उछालते, कभी बकरी की सूखी मींगणियों से सतधरा खेलते, कभी कंकडों से कौवाठुट्ठी मोगल पठान या बाघ गोटी का भी खेल चलता। हमारी भैंसे दूब भरे मैदान या चरागाह में चरती होती और हम अपने मालिकों की बुरी भली कहते सुनते और खेला करते। बड़े मालिक का चरवाहा बूढ़ा था, सबूरीमंडल। ठिगने कद का बूढ़ा धानुक। कान दोनों बुच थे। कपार छोटा। आँखें चमकदार मगर धँसी हुईं। बाल सन जैसे सफेद। अपने पशु की सेवा वह बड़ी ही लगन से करता। हमें अपने बीते दिनों की कहानियाँ सुनाते कभी न थकता था। खेल में मशगूल पाकर बहुधा हमको वह फटकारता भी।
और जो कुछ हो, सबूरी काका की दो बातें मैं अभी तक नहीं भूल पाया। एक तो यह कि अपनी भैंस को वह शायद ही पीटता और दूसरी यह कि सगी सन्तान की तरह उनकी सेवा। उसकी भैंस की आँखों में कभी किसी ने कीचड़ नहीं देखा। हर तीसरे दिन वह उसे तालाब में ले जाकर नहलाता, मुलायम दूबों की नूड़ी से भैंस की पीठ, पेट, पुट्ठे, जाँघ, गर्दन, माथ और पैर को भली भाँति रगड़ता। इस तरह अपनी भैंस को वह साफ सुथरी रखता...हम तो खैर थोड़ी ही उमर के थे, जिनकी उमर बड़ी थी उन चरवाहों से भी अपनी भैंसों की ऐसी सेवा पार नहीं लगती।
एक दिन मैं दोपहर के वक्त बड़े मालिक के बथान पर गया। उनके सोलह बैल थे और चार भैंसे थीं। चरवाहे तीन थे। सबूरी के जिम्मे दो भैंसे थीं। वहीं अलग एक झोंपड़ी में रहते थे। जिस समय मैं उनके पास गया तब वह हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। नारियल की पेंदी वाला इसी तरह का हुक्का मेरा भी बाप पीता था। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। आँखें उठाकर अपने नजदीक बैठने को उन्होंने इशारा किया। थोड़ी देर बाद बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा-‘‘तुम्हारी भैंस का यह सातवाँ महीना चल रहा है न ?’’
‘‘हाँ’’, मैंने कहा-‘‘बाबा, यह तुम कैसे जान गये ?’’
इस पर पतली मूँछों वाले उनके होंठ खिल उठे। सच, जोर से ठहाका लगाते उन्हें कभी नहीं देखा। बहुत हुआ तो खिलखिला पड़े, और तब बिना दाँत के उनके वे लाल मसूड़ें बड़े ही सुन्दर लगते। हुक्के को खूँटे से टिकाकर और चिलम को उलटाकर मंडल ने कहा-‘जिन्दगी भर तो भैंस ही चरायी है बलचनमा ! मैं जब ननिहाल से भागकर यहाँ आया तो बाइस साल का था। तेरा बाप लालचन्द तेरी ही उमर का रहा होगा..लच्छन से मालूम होता है कि तेरी भैंस के पेट में सात महीने की पड़िया है।’’
यह सुनकर मैं दंग रह गया। वह उठकर भैंस के पास जा बैठे। थनों से ऊपर वाली उसकी नसों को सहलाते हुए काका बोले-‘‘खाली बखत में इधर-उधर भटकना ठीक नहीं। चरवाहे को चाहिए कि अपने पशु के रोएँ-रोएँ को गौर से देखें। लापरवाही से कई तरह के कीड़े पड़ जाते हैं-अठौड़ी, किलनी, जूँ, चिल्लड़ कभी-कभी कुकुरमाछी भी इन्हें तंग करती है। इन बातों का ख्याल चरवाहा न रक्खेगा तो कौन रक्खेगा। इसके अलावा उनके रहने की जगह को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है....आजकल के चरवाहे हराम का खाते हैं, तभी तो उनका जानवर कलफ्ता रहता है।’’
उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सबूरी काका भैंस की सेवा करने में बड़े ही होशियार हैं, इनके पास घड़ी-आध रोज आकर बैठूँ तो बहुत सी बातें यों ही समझ में आ जायेंगी। और तब से जब कभी मुझे मौका मिलता तभी जाकर सबूरी मंडल के पास जा बैठता। हम एक बिरादरी के नहीं थे। वह थे धानुक मैं ठहरा ग्वाला। वह थे सबूरी मंडल मैं था बालचंद राउत, फिर भी दादा परदादा की तरह वह मुझे प्यार करते। कहीं कोई खाने-वाने की अच्छी चीज मिल जाती तो उसमें से थोड़ा कुछ मेरे लिए सँजोकर रखते। मुझसे और तो कुछ नहीं होता मगर रात को कभी –कभी जाकर पैर चाँप आता था।
मालिक की नौकरी ऐसी थी कि छुट्टी का नाम नहीं। तब भी छठे-छमाहे आ वह जरूर जाते। दो-चार दिन रहकर वह विदा होते तो इसटीसन तक सामान मुझे ही पहुँचाना पड़ता। चमड़े का छोटा सा सूटकेस होल्डाल में बँधा हुआ बिस्तरा-यह दोनों सिर पर और हाथ में टिफिन का डिब्बा। रामपुर से मधुबनी ढाई कोस पक्का पड़ता है। उठते-बैठते किसी तरह मैं पहुँचता। गरदन टूट जाती। पसीने से सारी देह तर हो होकर सूख चुकी होती। और इतने पर भी जब मालिक की गाड़ी पलेटफारम छोड़कर खिसकने लगती तो दो पैसा मेरी ओर फेंककर वह कहते-‘‘ले मूढ़ी या चना खरीद लेना, फाँकते-फाँकते घंटे भर में पहुँच जायेगा।’’
मन करता कि उन पैसों को वहीं पलेटफारम पर ही छोड़कर चल दूँ ! आखिर मैं वह पैसा उठा लेता। पैसे के चने और पैसे की बीड़ी, किसी तरह घर पहुँचता और माँ के पास धम्म से जा गिरता।
माँ मेरे बाप की ब्याही औरत नहीं थी। पहले ब्याह की औरत जब मर गई तो बाप कुछ रोज कलकत्ता रह आया था। बाद में जिस विधवा से संबंध हुआ वही थी मेरी माँ। दादी को भैंस चराने का मेरा यह काम पसन्द नहीं था। बहन थी छोटी, उसकी राय का कोई सवाल ही नहीं। हमारे पास कुल सात कट्ठा जमीन थी। मझले मालिक सौ कमाई के एक कसाई थे। बाबू के मरने पर बारह रुपये उन्होंने माँ को कर्ज दिये थे। बदले में सादे कागज पर अँगूठे का निशान ले लिया था। सूद देते-देते हम थक गये, मूल ज्यों-का-त्यों खड़ा था। छोटी मलिकाइन दुअन्नी के हिसाब से साल भर का दरमहा डेढ़ रुपैया देती थीं, उतने से क्या होता...
जाड़े की एक-एक रात हमारे लिए परलय की डुगडुगी बजाती आती थी। गर्मी के दिन जैसे-तैसे कट जाते, लेकिन जाड़ा से निबटना बड़ा ही मुश्किल होता। गुदड़ी कथड़ी भी ओढ़ने को अगर काफी न हो तो पूस माघ की ठंडी रात यमराज की बहन साबित होती है। जलावन के लिए लड़की भला हम लाते ही कहाँ से, हाँ, दादी ने दो बकरियाँ पाल रक्खी थीं, उनकी सूखी मींगणियाँ ताप-तापकर हम रात काटते। मालिकों के पास न लड़की की कमी, न घास फूस की। गोइठा, गोहरा भी उन्हीं के पास होता जिनके माल जाल हों। माल जाल के नाम पर हमारे यहाँ दो बकरियाँ थीं। आम, तलाम, जामुन, कटहर, बेर, कुसियार, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा...हमारा पेट भरने में इनसे काफी मदद मिलती। दादी अँधेरे में निकल जाती और मालिक के बाग से आम ले आती। गन्ना और दूसरे मौसमी फलों का यही हाल था। छोटी चीजें चुराने में मेरी दादी कमाल करती थी। वह कभी नहीं पकड़ी गई। माँ से यह काम नहीं होता था।
गाँव के बाहर जाड़े के दिनों में हर साल मालिकों का कोल्हू गड़ता। उनके यहाँ गन्ने की खेती कम नहीं होती। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर रात को कोल्हूआड़ में ही बिताया करता। गन्ना खा-खाकर पेट भर लेना और भट्ठी की आँच से गरमाकर सो जाना। डेढ़-दो महीने हर साल जाड़ों में हम ऐसा ही करते।
मझले मालिक की निगाह हमारे उन थोड़े से खेतों पर थी जिनमें मडुवा उपजाकर तीन चार महीने का खर्च हम निकालते आये थे। उन्होंने सोचा-लौंडा अभी छोटा है। जमाने का रंग-ढंग अच्छा नहीं। कमाने लायक होने पर कटिहार या कलकत्ता कहीं-न-कहीं जरूर भाग जायेगा, फिर कोई इसका क्या कर लेगा ! अभी तो खैर इस औरतिया का अँगूठा निशान अपने कब्जे में है..
सोच-समझकर एक दिन मझले मालिक ने हम तीनों को बुलाया। वहाँ गाँव के बूढ़े पंडित भी बैठे थे। आधा पीतल और आधा लोहे से बना सरौता मालिक के हाथ में था। वह सुपारी कतर रहे थे। कुछ बारीक कतरा पंडितजी की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा-‘‘ललचनमा जब तक जिया, जी जान से मेरी सेवा उसने की और इनको तो देखिए।’’
पंडित जी ने सुपारी फाँक लिया। फिर टूटे डंठल वाले चश्मे को नाक पर से हटाकर कपार पर चढ़ाया। मेरी ओर तनिक देर गौर से ताकते रहे। तब जाकर बोले-‘‘जसोधर बाबू, छोकड़े के रोआँ-रोआँ से नमक-हरामी टपकती है। देखो न, कैसे मुलुर-मुलुर ताकता है।’’
इस पर मझले मालिक ने कहा-‘‘हाँ गुरु, बड़ा ही पाती है। कभी पकड़ में नहीं आता। पाहुना आये थे, उनका नौकर बीमार पड़ गया। मैंने इस ससुर को कहला भेजा कि आकर मेहमान की मालिश कर जाय। साला आया ही नहीं...’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i