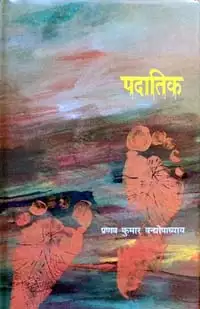|
कहानी संग्रह >> 10 प्रतिनिधि कहानियाँ (प्रणव कुमार वन्द्योपाध्याय) 10 प्रतिनिधि कहानियाँ (प्रणव कुमार वन्द्योपाध्याय)प्रणव कुमार वन्द्योपाध्याय
|
54 पाठक हैं |
|||||||
प्रणव कुमार वन्द्योपाध्याय की 10 प्रमुख कहानियां
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
किशोरावस्था में मैं इलाहाबाद पहुँचा था। बरेली में स्कूल की पढ़ाई खत्म
कर आया एक नए नगर में। इस शहर का नाम खूब सुनता रहा हूँ। दो कारण थे।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। दूसरी बात थी, इस
शहर में ढेर सारे कवि लेखक रहते थे। उनकी चर्चाएँ सुनता था। हालाँकि बहुत
कुछ समझ नहीं पाता था। ढेर सारी बातें सिर के ऊपर से फिसलकर निकल जाती
थीं। सोचता था, पहले मैं एक तरह से आदिकाल के पर्वत प्रदेश असम में था।
फिर पूर्वोत्तर प्रदेश छोड़कर पहुँचा था गोरखपुर। फिर बरेली। बरेली के बाद
प्रयाग पहुँच तो गया, लेकिन इस नगर की धाराओं से मैं बहुत दूर था। बात
शायद यही थी कि इससे पहले मैं साहित्य या संस्कृति के माहौल में कभी था ही
नहीं। एक तरह से प्रयाग आने के बाद ही संभवतः मेरा जन्म हुआ था। खैर, सिर से
पाँव तक अपनी अनगढ़ता के बावजूद अपनी कमियों के बीच ही सही, कम से कम
ज़रूरी मुद्दों को मैं समझना चाहता था। वैसे तब तक कई जगह मेरी कविताएँ
प्रकाशित हो रही थीं। एक नए कवि के रूप में मेरी खास पहचान तो नहीं बनी
थी, लेकिन मेरा नाम थोड़ा-ऊपर सामने आ ही रहा था।
संयोग से मैंने स्कूल की पढ़ाई समाप्त की और मेरा पहला कविता-संग्रह प्रयाग आते ही प्रकाशित हो गया। ‘धर्मयुग’ में छप गई मेरी एक कविता ‘इलाहाबाद’। मुझे एक पड़ाव तो मिल गया, लेकिन मात्र कविता के क्षेत्र में। मैं चाहता था कहानी—लेखन की शुरुआत करना। कविताएँ तो एक तरह से लिख ही रहा था और पूरे मन से कहानियाँ पढ़ता भी था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मेरी कहानी की ज़मीन बने कैसे ! कई बार कोशिश की, लेकिन असफल ही रहा। इसके बावजूद कई छोटी-मोटी पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ छप गईं। छपीं, लेकिन मेरे भीतर ज़बरदस्त खालीपन था।
उन्हीं दिनों कमलेश्वर पहुँचे थे मुंबई। ‘सारिका’ के संपादक नियुक्त होकर। उन्हें एक कहानी भेज दी—‘तीसरा आदमी’। संपादक ने वह कहानी तत्काल छाप दी तो मेरे तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। जानता थोड़े ही था कि कमलेश्वर बी.ए. में पढ़ रहे इस बालक की कथा स्वीकार करेंगे और तत्काल छाप भी देंगे। खैर, वह कहानी थी एक अयाचित संबंध की। ऐसा नहीं कि ऐसे किसी रिश्ते पर मैंने पहली बार लिखा था। लिखी तो ज़माने से जाती रहीं ऐसे रिश्तों पर कथाएँ लेकिन मैं समझ लेना चाहता था यह सब। यह चाह ज़रूरी रही है, लेकिन मैं भीतर से महसूस करना चाहता था प्रेम का उतावलापन और एक भय। मेरे भीतर सामर्थ्य कितनी थी, नहीं जानता। निश्चित ही वह अपूर्ण थी। इसके बावजूद मैं चाहता था मनुष्य की ग्रंथियों की परतों के भीतर घुसना। देखना चाहता था वह सब जो खुली आँखें से देख पाना संभव नहीं था।
इलाहाबाद पहुँचने के बाद धीरे-धीरे मैंने जानना चाहा वर्ग-संघर्ष का वास्तविक स्वरूप। यह इसलिए ज़रूरी था कि 1947 में स्वतंत्र होने के बाद देश ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आगे का रास्ता जैसे-तैसे तय करने की कोशिश में लगा था। यह तय नहीं था कि इस रास्ते से हम कहाँ तक पहुँच पाएँगे। इस मुद्दे का संघर्ष कर रहे लोग ईमानदार तो थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हिंदुस्तान की कार्य-प्रणाली क्या होनी चाहिए...
भारत में मार्क्सवाद की जड़ बहुत गहरी नहीं हो पाई। स्वतंत्रता की आधी शताब्दी के बाद भी इस देश की राजनीति में वह सामग्रिक रूप में इसलिए कुछ पीछे ही है कि इसमें वर्ग-संघर्ष का कोई प्रभावशाली नेता नहीं है। कम से कम भारत के नक्शे के ऊपर। दूसरी बात यह है कि भारत में मार्क्सवाद इस देश की संस्कृति और धर्म की परिसीमा के बाहर संभवतः बहुत आगे नहीं जा सकता। कम से कम फिलहाल ऐसी संभावना तो नहीं है।
इस देश के हिंदी कहानीकार समय की चढ़ाई के साथ देश, समाज और परिस्थितियों को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें मैं भी शरीक था। लेकिन ज़्यादातर कहानीकारों की तरह मेरी समझ की भी एक सीमा थी। फलस्वरूप कई बार में यथार्थ की वास्तविकता की बजाय अन्य रास्तों पर किसी न किसी रूप में चलता रहा। औरों की तरह। इसके बावजूद समय-समय पर बहुत सशक्त कहानियाँ सामने आती रही हैं। और उभरकर सामने आता रहा हिंदी कहानी का खाका।
इलाहाबाद जाने के बाद मैं हॉस्टल के कैलाश जोशी और हम लोगों से पहले के नीलकांत के साथ अकसर बहस करता था। मेरे साथ उन मित्रों की असहमति तो अनेक मुद्दों पर थी, लेकिन मेरी मार्क्सवाद की समझ किसी सीमा तक तय करने में उन लोगों का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस तथ्य को मैं बखूबी याद करता हूँ।
मार्क्सवाद का प्रभाव मन में इस तरह फैल गया कि भारत का भविष्य मुझे कुछ और नज़र आया। लेकिन मैंने अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं में चारू मजूमदार की बातें पढ़कर अंततः उनके मार्क्सवाद को ही वैचारिक धरातल पर कबूल कर लिया।
थोड़े समय बाद मैंने एक लंबी कहानी लिखी, ‘बारूद की सृष्टिकथा’। कहानी की कोई नायिका नहीं थी। मुख्य पात्र था निचले मध्यम वर्ग का एक किशोर। वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई समाप्त करने के बाद इलाहाबाद आकर विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी बना था। हॉस्टल में रहने लायक पैसे उसके पास तो नहीं थे, इस कारण वह बाहर रहकर पढ़ाई करता था। उन्हीं दिनों वह क्रान्तिकारी मार्क्सवाद के संपर्क में आया और चारू मजूमदार के विचारों से प्रभावित होकर स्वतः एक मार्क्सवादी कार्यकर्ता बन गया। अब उसकी पढ़ाई छूटनी ही थी और वह घर से भी बहुत दूर हो गया। यह कहानी उस किशोर के संघर्ष का बयान है। वह नहीं मानता कि कई बार हारते रहने के बावजूद हमारे काम अभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। यानी अभी तो मीलों चलना है।
‘बारूद की सृष्टिकथा’ लिख तो ली, लेकिन उसे छापने के लिए कौन तैयार होता ! आखिर में कहानी भेज दी ‘सारिका’ के संपादक को। साधाराण बुक-पोस्ट से। चंद दिनों बाद संपादक कमलेश्वर का अपेक्षाकृत बड़ा पत्र आ पहुँचा। उस कहानी की तारीफ में जो बातें उन्होंने लिखी थीं, वे आज तो याद नहीं हैं, लेकिन उस समय वे शब्द पढ़कर मन फैल गया था। संपादक ने इलाहाबाद के अंग्रेज़ी दैनिक ‘द लीडर’ का नाम मात्र बदल दिया था। इसके लिए भी संपादक ने मुझे तत्काल सूचना दी थी। इसके अलावा कहानी ज्यों-की त्यों छपी थी।
‘बारूद की सृष्टिकथा’ का मूल्यांकन मेरा मकसद नहीं है। वैसे भी मैं कोई कहानी-आलोचक नहीं हूँ। एक कथाकार की हैसियत से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आज से तीस-पैंतीस साल पहले एक अलग माहौल में अनेक कथाकार देश के बारे में बहुत सारी बातें सोचते थे। शायद उनमें से एक मैं खुद भी था। वास्तविक रास्तों पर चलते हुए देश को बदलने का एक मकसद आँखों में और दिल के भीतर था। तब तो नहीं समझ पाया था, लेकिन कह सकता हूँ कि कई मामलों में हमारी समझ बहुत कम थी। आदर्शवादी की संज्ञा देकर सामने न सही, पीछे ही से अनेक पाठक शायद हमारा मज़ाक भी करते हों। जो भी हो, स्थिति की समझ के बारे में लेखक और मार्क्सवादी लोगों की धारणा बहुत अपूर्व थी। यही नहीं, उनकी संख्या थी बहुत छोटी। आम लोगों को प्रभावित करने की उनकी शक्ति इतनी सीमित थी कि शायद ज़्यादातर लेखक समय को समझ पाने में असमर्थ थे। फिर आखिर में ढेर सारे सच्चे मार्क्सवादी चलते-चलते आकर खड़े हो गए एक चौराहे पर। सामने बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था।
इसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक और कहानी लिखी ‘आत्मज’। एक नक्सल युवक की कहानी। पिछली कहानी ‘बारूद’ की सृष्टिकथा के मुख्य पात्र की तरह वह भी था निम्न-मध्यमवर्ग का ही। बेटा नक्सलवादी संघर्ष करते रहने के कारण था परिवार से दूर। परिवार के लिए कुछ भी करने की सामर्थ्य, ज़ाहिर है, उसके भीतर नहीं थी। उसकी खबर लेने पुलिस जब तब आ जाती थी। उसके साथियों में पुरुष तो थे ही, युवतियाँ भी थीं। पिता समझता रहा, बेटा चरित्र-भ्रष्ट है। इस समझ के कारण पिता के भीतर था क्रोध और घृणा का एक अस्पृश्य तालाब। एक दिन माँ की आँखें बन्द हो गईं तो मृत शरीर के चरण-स्पर्श करने कहीं से आ गया था बेटा। कोई उम्मीद किसी के भी मन में कहाँ रह गई थी ! उस मुकाम पर बेटे का चेहरा देखकर पिता को लगा कि उसका पुत्र एकदम पवित्र। बाप का क्रोध क्षमा में एकदम घुलकर स्नेह में बदल गया था। वह थोड़ा भयभीत हो गया कि पुलिस सुराग पाकर एकदम से आ धमक सकती है। ऐसी हालत में युवा बेटे कि परिणति क्या होगी, पिता को स्वाभाविक रूप में तत्काल समझ में आ गई थी। तब बाप ने बेटे से कहा कि उसकी सच्चाई अब समझ में आ रही है, लेकिन पुलिस के हाथों बचने के लिए वह तत्काल यहाँ से भाग जाए।
इस कहानी में यथार्थ के होने से ज़्यादातर पाठक शायद असहमत नहीं होंगे। इसके बावजूद पिता के चरित्र के अंतिम भाग से शायद कुछ लोग सहमत न भी हों। मुझे ऐसी आलोचना की कोई जानकारी ज़रूर नहीं है, लेकिन लेखक की हैसियत से मैं यह कह सकता हूँ कि तमाम विरोधाभासों के एक बिंदु पर पहुँचने के बाद पिता की दृष्टि एकदम से बदल गई थी। इस सत्य को मैं कभी भी नकार नहीं सकता।
ऐसी कहानियाँ हिंदी में कितनी लिखी गईं, मैं यह तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाऊँगा। इसके बावजूद मैं देखता हूँ चरित्रों को। ये चरित्र आज भी जब-तब मुझे उकसाते रहते हैं। मेरा कहानीकार आगे कहाँ तक जाएगा, यह तो नहीं मालूम, लेकिन आगे के समय के बारे में मैं लगातार सोचता रहता हूँ। इस सोच में पिछले तीस-पैंतीस सालों में अनेक परिवर्तन तो आए, लेकिन भीतर के कई चौखट आज भी लगभग वैसे ही हैं। बदलता समय आगे बताएगा कि कई तरह से हो रहे जद्दोजहद के बीच मैं कहाँ खड़ा हूँ !
यह कहानी स्वाभाविक रूप में ! ‘सारिका’ में ही प्रकाशित हुई थी। इसकी वजह यही थी वरना यह ‘आत्मज’ पाठकों तक पहुँचने की बजाय मेरे पास ही कैद रह जाती।
इसी कड़ी में ‘सारिका’ में ही एक और कहानी प्रकाशित हुई थी--‘असंबोधित देवदास’। वतन को बदलने वाले कुछेक लोगों की कथा। इन कहानियों के साथ मैं दिन-रात लगातार चलता रहा। वह यात्रा एक लेखक में इस कदर आत्मसात् होती रही कि मेरी ज़मीन एकदम बदल गई थी। इस ज़मीन के बाहर मेरे लिए होना संभव नहीं था। एक तरह से इसी में मेरा अपना एक संसार बन गया था।
हमारी ज़िंदगी है तो निहायत छोटी, लेकिन हम गिरते-पड़ते ही चल सके हैं। ऐसा सभी के साथ हुआ। विज्ञान, साहित्य, राजनीति, खेल या कुछ भी हो, एक जगह स्थिर कभी नहीं रहा। हम लोगों ने जो भी बातें कीं, वे एक समय के बाद परिवर्तित हुई हैं। मैं ग्रह-नक्षत्रों का वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि सूर्य में भी वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कई दरारें आ गई हैं। पृथ्वी और समुद्र की आज की स्थिति तो काफी कुछ बदल ही चुकी है। साहित्य या कहानी इस संसार में है ही कल की। लेकिन कल और आज के दरमियान जो बदलाव आ चुके हैं, उनसे कहानी में बदलाव तो आना ही था।
संसार आज इतना बदल गया कि हमारे पैरों तले की ज़मीन पहले के समय से कई अंशों में मेल नहीं खाती। इस बदलाव का सब कुछ हम समझ नहीं सकते। यह संभव नहीं है। हमारी लेखकीय हैसियत अब किस बिंदु पर आ खड़ी हुई है, हम निर्णायक रूप में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन सोच रहे हैं कि हम कहाँ हैं ! मन के इस उतार-चढ़ाव के बीच भीतर का लेखक आज भी जीवित है। फिर हमने जो कहानियाँ लिखीं, उनमें ‘वृंदावन कथा, ‘पार’ आदि के पाठक अनेक रहे। कहानियाँ प्रकाशित होने के बाद पाठकों की प्रतिक्रियाएँ एक लंबे समय तक चलती रहीं। यह एक छोटा-सा तथ्य है, मेरी कहानियों का कोई विज्ञापन नहीं।
‘वृंदावन कथा’ एक छोटे-मोटे चोर-उचक्के की कहानी है। यह व्यक्ति जाना जाता था ‘बिंद्रावन’ नाम से। वह था गाँव का निवासी। नितांत निरादृत। काम-काज के नाम पर उसे करने को कुछ नहीं सूझा। ऐसे व्यक्ति पर लिखने के लिए मुझे मिला कि वह नितांत स्थितिहीन है। वह चोर ज़रूर है, लेकिन बहुत अक्लमंद नहीं। किसी तरह वह गुज़ारा-भर कर लेता है। कोई और विकल्प उसे दिखाई नहीं पड़ा।
यहाँ मैं समझ गया कि ‘बिंद्रावन’ जिस अवहेलना और तिरस्कार का शिकार है, उसका कुछ कारण निश्चित ही खुद वह भी है, लेकिन उसकी यह नियति एक लेखक को परेशानी करती ही है।
मैं देखता हूँ कि ‘बिंद्रावन’ नाम और परिचय के बाहर एक ऐसा प्राणी है, जिसकी मौत कहीं भी अंकित नहीं होगी। भारत में बिंद्रावन अनेक हैं। असंख्य। उन्हें लोग मौकों पर सज़ा दे देते हैं, लेकिन उनके होने और खत्म होने को कोई घटना नहीं मानता।
जब मैंने ‘पार’ लिखी, दो साल अमेरिका में रहकर वापस भारत लौटा था। अमेरिकी अनुभवों पर बस दो-चार कविताएँ ही सिर्फ लिख सका था। वहाँ ट्रॉय में शोध करता और पढ़ाता ज़रूर था, लिखने के नाम पर एकदम ज़ीरो हो गया था। मैं तब इस कदर खाली हो गया था कि लगता था, अब आगे कभी भी लिख ही नहीं पाऊँगा। बस, एक लेखक को उसका अंत स्वीकार कर लेना था। इस नियति के बाहर निकल आने की सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं थी। 1984 से ’86 तक मैं हर दिन अपना विराम सामने देखता रहा। पहले सोचा था, अभी दो-चार सालों में ही भारत लौटकर नहीं आऊँगा। अंततः कब लौटूँगा, अनिर्णय में था। कभी-कभी लगता था, मेरा मुकाम अब मुमकिन है, भारत न भी हो। लेकिन अन्ततः अपने सामने ज़बरदस्त अनिर्णय था। इसके बीच लगभग दो साल बाद मैंने बोरिया बिस्तर बाँधें और चिड़िया की तरह उड़कर लौट आया। एक अनिर्णय से एक और अनिर्णय में आ तो गया, लेकिन अंततः राहत शुरू हो गई थी। इस बात में सच्चाई कितनी थी, नाप तौलकर कुछ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मेरा मन अपने तमाम संकटों के बावजूद दिल्ली वापस आकर थोड़ा-बहुत हल्का हो गया था।
अब मसला है—अरसे से रुके पड़े लेखन को फिर से शुरू करने का। मन में एक लंबी कहानी की रूपरेखा बनी तो वह थी एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी। उसकी उम्र बहुत हो गई थी। पत्नी की मृत्यु काफी समय पहले की एक घटना थी। छोटी-सी। वह रहता था अपने बेटे और उसके परिवार के साथ। वह वृद्ध व्यक्ति पहले पहलवानी करता था। उसकी ख्याति दूर-दूर तक व्याप्त थी। लेकिन उसकी उम्र जब बहुत ज़्यादा हो गई, उसे चाहने वाले भी धीरे-धीरे छँटते गए। अब उसके इर्द-गिर्द रह गए थे सिर्फ उसका बेटा और उसकी पत्नी। वृद्ध का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं था। यह व्यक्ति के घर के लोगों के लिए अत्यंत उत्पाती बन गया था। बेटा समझ गया था कि पिता की मृत्यु संभवतः बहुत शीघ्र नहीं होगी और उसके तमाम खुराफात कहीं से भी कम नहीं हो जाएँगे। बेटा उधेड़बुन में था। निर्णय नहीं ले पा रहा था कि पिता से मिल रही निरंतर परेशानियों से अब मुक्ति का रास्ता क्या हो ! निर्णय लेना सहज तो नहीं था, लेकिन पिता की स्थिति का कोई समाधान भी नहीं रह गया था। अंततः एक दिन उसने पिता को नए कपड़े पहनाए और एक झोले में ज़रूरी सामान भरकर उसके साथ शहर के लिए चल पड़ा। शहर पहुँचकर वह सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचा। एक टिकट लेकर पिता के हाथ में उसने झोला और टिकट थमाया तो बूढ़े को लेकर गाड़ी चलने लगी। रेलगाड़ी के चलते ही बूढ़ा तो बहुत खुश था, लेकिन बेटा चलती हुई ट्रेन को चुप आँखों से देखता रहा थोड़ी ही देर में गाड़ी आगे बढ़ गई तो अब आखिरी डिब्बे का सिर्फ पीछे का हिस्सा-भर दिखाई दे रहा था। पिता के पार होने का मात्र यही रास्ता अब रह गया था।
यह कहानी लंबी तो थी, लेकिन लिखने का समय बहुत ज़्यादा नहीं था। कहानी मैंने झटपट लिख तो ली, लेकिन लंबाई के कारण यही सोचता रहा कि अंततः किसे दिया जाए ! आखिर में कहानी जब ‘सारिका’ में प्रकाशित हो गई, कितने लोगों ने इसे पढ़ा, न जान पाने के बावजूद कई पाठकों से मेरी यदा-कदा बातचीत हो जाती है। कहानी-लेखन के मामले में जब भी मैं सोचता हूँ, मुझे मनुष्य का संत्रास सामने दिखाई पड़ता है। संत्रास की यह कथा मनुष्य के भीतर आज भी ऐसे उमड़ती है कि वह निर्धनता के शिकंजे में जकड़े जाने के बाद एकदम असहाय है। और इसके बाद उसकी छोटी-सी संभावना भी समाप्त हो जाती है।
जाने-अनजाने मनुष्य का संसार आरंभ होते ही कहानी भी शुरू हो गई थी। किसी न किसी रूप में। वहीं लाखों साल के बाद बनते बिगड़ते आज की कहानी के रूप में अलग-अलग तरीकों से पाठकों के सामने पहुँच रही है। स्पष्ट है, कहानी मानव-सभ्यता का इतिहास दर्शाती है। इस इतिहास में दर्शन तो हैं ही, विज्ञान भी है। कला, संस्कृति और राजनीतिक आधार भी हैं। कुल मिलाकर यह कहना सत्य होगा कि साहित्य, मनुष्य और मनुष्य का विवेचन वैज्ञानिक रूप में है और कहानी की भूमिका इसमें अत्यंत प्रखर है।
इस संसार का अपना एक इतिहास है। तमाम-उखाड़-पछाड़ों के बाद आज भी हम जिस बिंदु तक पहुँचे हैं, हमारे पास जानकारी का दायरा इसके अन्तर्गत बहुत ही नगण्य है। अब जब हम कहानी की बात शुरू करते हैं, हमारी विस्तृति ज़रूर बहुत नहीं हो पाती है, लेकिन शायद हम कुछ गहराई तक पहुँच सकते हैं। हम काफी हद तक जान पाते मनुष्य की संक्रमण और अंतर्मन की कथा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आज की कहानी जिस सामर्थ्य के साथ आ खड़ी हुई है, स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा होना अस्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन हिंदी की कहानियाँ हमेशा ही इस तथ्य को पुष्ट नहीं करतीं। जो भी हो, मैं कहानी का एक सामान्य लेखक-भर हूँ, कोई आलोचक या विश्लेषक नहीं।
हमेशा तो नहीं, लेकिन कई बार कहानी लिखते हुए मैं अपने भीतर शायद किसी सीमा का प्रवेश देख पाता हूँ। संसार के कई टुकड़ों में। उन्हीं में मैं शायद स्वयं को छू भी पाया हूँ। कम से कम अनुभव ऐसा ही हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि पाठकों की इस बारे में क्या राय है ! उनकी राय अगर इससे आंशिक रूप में या मुमकिन है, पूरी तरह भिन्न भी हुई, मैं चुप रहूँगा। फिर से अपने भीतर घुसने की कोशिश कर, ज़्यादा न सही, दो अंगुली की दूरी लाँघने का प्रयास करता रहूँगा। और जहाँ भी मैं असमर्थ हूँ, अपने पाठकों से कबूल करने में मुझे कोई हिचक नहीं होगी।
संयोग से मैंने स्कूल की पढ़ाई समाप्त की और मेरा पहला कविता-संग्रह प्रयाग आते ही प्रकाशित हो गया। ‘धर्मयुग’ में छप गई मेरी एक कविता ‘इलाहाबाद’। मुझे एक पड़ाव तो मिल गया, लेकिन मात्र कविता के क्षेत्र में। मैं चाहता था कहानी—लेखन की शुरुआत करना। कविताएँ तो एक तरह से लिख ही रहा था और पूरे मन से कहानियाँ पढ़ता भी था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि मेरी कहानी की ज़मीन बने कैसे ! कई बार कोशिश की, लेकिन असफल ही रहा। इसके बावजूद कई छोटी-मोटी पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ छप गईं। छपीं, लेकिन मेरे भीतर ज़बरदस्त खालीपन था।
उन्हीं दिनों कमलेश्वर पहुँचे थे मुंबई। ‘सारिका’ के संपादक नियुक्त होकर। उन्हें एक कहानी भेज दी—‘तीसरा आदमी’। संपादक ने वह कहानी तत्काल छाप दी तो मेरे तो पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। जानता थोड़े ही था कि कमलेश्वर बी.ए. में पढ़ रहे इस बालक की कथा स्वीकार करेंगे और तत्काल छाप भी देंगे। खैर, वह कहानी थी एक अयाचित संबंध की। ऐसा नहीं कि ऐसे किसी रिश्ते पर मैंने पहली बार लिखा था। लिखी तो ज़माने से जाती रहीं ऐसे रिश्तों पर कथाएँ लेकिन मैं समझ लेना चाहता था यह सब। यह चाह ज़रूरी रही है, लेकिन मैं भीतर से महसूस करना चाहता था प्रेम का उतावलापन और एक भय। मेरे भीतर सामर्थ्य कितनी थी, नहीं जानता। निश्चित ही वह अपूर्ण थी। इसके बावजूद मैं चाहता था मनुष्य की ग्रंथियों की परतों के भीतर घुसना। देखना चाहता था वह सब जो खुली आँखें से देख पाना संभव नहीं था।
इलाहाबाद पहुँचने के बाद धीरे-धीरे मैंने जानना चाहा वर्ग-संघर्ष का वास्तविक स्वरूप। यह इसलिए ज़रूरी था कि 1947 में स्वतंत्र होने के बाद देश ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आगे का रास्ता जैसे-तैसे तय करने की कोशिश में लगा था। यह तय नहीं था कि इस रास्ते से हम कहाँ तक पहुँच पाएँगे। इस मुद्दे का संघर्ष कर रहे लोग ईमानदार तो थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हिंदुस्तान की कार्य-प्रणाली क्या होनी चाहिए...
भारत में मार्क्सवाद की जड़ बहुत गहरी नहीं हो पाई। स्वतंत्रता की आधी शताब्दी के बाद भी इस देश की राजनीति में वह सामग्रिक रूप में इसलिए कुछ पीछे ही है कि इसमें वर्ग-संघर्ष का कोई प्रभावशाली नेता नहीं है। कम से कम भारत के नक्शे के ऊपर। दूसरी बात यह है कि भारत में मार्क्सवाद इस देश की संस्कृति और धर्म की परिसीमा के बाहर संभवतः बहुत आगे नहीं जा सकता। कम से कम फिलहाल ऐसी संभावना तो नहीं है।
इस देश के हिंदी कहानीकार समय की चढ़ाई के साथ देश, समाज और परिस्थितियों को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनमें मैं भी शरीक था। लेकिन ज़्यादातर कहानीकारों की तरह मेरी समझ की भी एक सीमा थी। फलस्वरूप कई बार में यथार्थ की वास्तविकता की बजाय अन्य रास्तों पर किसी न किसी रूप में चलता रहा। औरों की तरह। इसके बावजूद समय-समय पर बहुत सशक्त कहानियाँ सामने आती रही हैं। और उभरकर सामने आता रहा हिंदी कहानी का खाका।
इलाहाबाद जाने के बाद मैं हॉस्टल के कैलाश जोशी और हम लोगों से पहले के नीलकांत के साथ अकसर बहस करता था। मेरे साथ उन मित्रों की असहमति तो अनेक मुद्दों पर थी, लेकिन मेरी मार्क्सवाद की समझ किसी सीमा तक तय करने में उन लोगों का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस तथ्य को मैं बखूबी याद करता हूँ।
मार्क्सवाद का प्रभाव मन में इस तरह फैल गया कि भारत का भविष्य मुझे कुछ और नज़र आया। लेकिन मैंने अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं में चारू मजूमदार की बातें पढ़कर अंततः उनके मार्क्सवाद को ही वैचारिक धरातल पर कबूल कर लिया।
थोड़े समय बाद मैंने एक लंबी कहानी लिखी, ‘बारूद की सृष्टिकथा’। कहानी की कोई नायिका नहीं थी। मुख्य पात्र था निचले मध्यम वर्ग का एक किशोर। वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई समाप्त करने के बाद इलाहाबाद आकर विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी बना था। हॉस्टल में रहने लायक पैसे उसके पास तो नहीं थे, इस कारण वह बाहर रहकर पढ़ाई करता था। उन्हीं दिनों वह क्रान्तिकारी मार्क्सवाद के संपर्क में आया और चारू मजूमदार के विचारों से प्रभावित होकर स्वतः एक मार्क्सवादी कार्यकर्ता बन गया। अब उसकी पढ़ाई छूटनी ही थी और वह घर से भी बहुत दूर हो गया। यह कहानी उस किशोर के संघर्ष का बयान है। वह नहीं मानता कि कई बार हारते रहने के बावजूद हमारे काम अभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। यानी अभी तो मीलों चलना है।
‘बारूद की सृष्टिकथा’ लिख तो ली, लेकिन उसे छापने के लिए कौन तैयार होता ! आखिर में कहानी भेज दी ‘सारिका’ के संपादक को। साधाराण बुक-पोस्ट से। चंद दिनों बाद संपादक कमलेश्वर का अपेक्षाकृत बड़ा पत्र आ पहुँचा। उस कहानी की तारीफ में जो बातें उन्होंने लिखी थीं, वे आज तो याद नहीं हैं, लेकिन उस समय वे शब्द पढ़कर मन फैल गया था। संपादक ने इलाहाबाद के अंग्रेज़ी दैनिक ‘द लीडर’ का नाम मात्र बदल दिया था। इसके लिए भी संपादक ने मुझे तत्काल सूचना दी थी। इसके अलावा कहानी ज्यों-की त्यों छपी थी।
‘बारूद की सृष्टिकथा’ का मूल्यांकन मेरा मकसद नहीं है। वैसे भी मैं कोई कहानी-आलोचक नहीं हूँ। एक कथाकार की हैसियत से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आज से तीस-पैंतीस साल पहले एक अलग माहौल में अनेक कथाकार देश के बारे में बहुत सारी बातें सोचते थे। शायद उनमें से एक मैं खुद भी था। वास्तविक रास्तों पर चलते हुए देश को बदलने का एक मकसद आँखों में और दिल के भीतर था। तब तो नहीं समझ पाया था, लेकिन कह सकता हूँ कि कई मामलों में हमारी समझ बहुत कम थी। आदर्शवादी की संज्ञा देकर सामने न सही, पीछे ही से अनेक पाठक शायद हमारा मज़ाक भी करते हों। जो भी हो, स्थिति की समझ के बारे में लेखक और मार्क्सवादी लोगों की धारणा बहुत अपूर्व थी। यही नहीं, उनकी संख्या थी बहुत छोटी। आम लोगों को प्रभावित करने की उनकी शक्ति इतनी सीमित थी कि शायद ज़्यादातर लेखक समय को समझ पाने में असमर्थ थे। फिर आखिर में ढेर सारे सच्चे मार्क्सवादी चलते-चलते आकर खड़े हो गए एक चौराहे पर। सामने बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था।
इसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक और कहानी लिखी ‘आत्मज’। एक नक्सल युवक की कहानी। पिछली कहानी ‘बारूद’ की सृष्टिकथा के मुख्य पात्र की तरह वह भी था निम्न-मध्यमवर्ग का ही। बेटा नक्सलवादी संघर्ष करते रहने के कारण था परिवार से दूर। परिवार के लिए कुछ भी करने की सामर्थ्य, ज़ाहिर है, उसके भीतर नहीं थी। उसकी खबर लेने पुलिस जब तब आ जाती थी। उसके साथियों में पुरुष तो थे ही, युवतियाँ भी थीं। पिता समझता रहा, बेटा चरित्र-भ्रष्ट है। इस समझ के कारण पिता के भीतर था क्रोध और घृणा का एक अस्पृश्य तालाब। एक दिन माँ की आँखें बन्द हो गईं तो मृत शरीर के चरण-स्पर्श करने कहीं से आ गया था बेटा। कोई उम्मीद किसी के भी मन में कहाँ रह गई थी ! उस मुकाम पर बेटे का चेहरा देखकर पिता को लगा कि उसका पुत्र एकदम पवित्र। बाप का क्रोध क्षमा में एकदम घुलकर स्नेह में बदल गया था। वह थोड़ा भयभीत हो गया कि पुलिस सुराग पाकर एकदम से आ धमक सकती है। ऐसी हालत में युवा बेटे कि परिणति क्या होगी, पिता को स्वाभाविक रूप में तत्काल समझ में आ गई थी। तब बाप ने बेटे से कहा कि उसकी सच्चाई अब समझ में आ रही है, लेकिन पुलिस के हाथों बचने के लिए वह तत्काल यहाँ से भाग जाए।
इस कहानी में यथार्थ के होने से ज़्यादातर पाठक शायद असहमत नहीं होंगे। इसके बावजूद पिता के चरित्र के अंतिम भाग से शायद कुछ लोग सहमत न भी हों। मुझे ऐसी आलोचना की कोई जानकारी ज़रूर नहीं है, लेकिन लेखक की हैसियत से मैं यह कह सकता हूँ कि तमाम विरोधाभासों के एक बिंदु पर पहुँचने के बाद पिता की दृष्टि एकदम से बदल गई थी। इस सत्य को मैं कभी भी नकार नहीं सकता।
ऐसी कहानियाँ हिंदी में कितनी लिखी गईं, मैं यह तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाऊँगा। इसके बावजूद मैं देखता हूँ चरित्रों को। ये चरित्र आज भी जब-तब मुझे उकसाते रहते हैं। मेरा कहानीकार आगे कहाँ तक जाएगा, यह तो नहीं मालूम, लेकिन आगे के समय के बारे में मैं लगातार सोचता रहता हूँ। इस सोच में पिछले तीस-पैंतीस सालों में अनेक परिवर्तन तो आए, लेकिन भीतर के कई चौखट आज भी लगभग वैसे ही हैं। बदलता समय आगे बताएगा कि कई तरह से हो रहे जद्दोजहद के बीच मैं कहाँ खड़ा हूँ !
यह कहानी स्वाभाविक रूप में ! ‘सारिका’ में ही प्रकाशित हुई थी। इसकी वजह यही थी वरना यह ‘आत्मज’ पाठकों तक पहुँचने की बजाय मेरे पास ही कैद रह जाती।
इसी कड़ी में ‘सारिका’ में ही एक और कहानी प्रकाशित हुई थी--‘असंबोधित देवदास’। वतन को बदलने वाले कुछेक लोगों की कथा। इन कहानियों के साथ मैं दिन-रात लगातार चलता रहा। वह यात्रा एक लेखक में इस कदर आत्मसात् होती रही कि मेरी ज़मीन एकदम बदल गई थी। इस ज़मीन के बाहर मेरे लिए होना संभव नहीं था। एक तरह से इसी में मेरा अपना एक संसार बन गया था।
हमारी ज़िंदगी है तो निहायत छोटी, लेकिन हम गिरते-पड़ते ही चल सके हैं। ऐसा सभी के साथ हुआ। विज्ञान, साहित्य, राजनीति, खेल या कुछ भी हो, एक जगह स्थिर कभी नहीं रहा। हम लोगों ने जो भी बातें कीं, वे एक समय के बाद परिवर्तित हुई हैं। मैं ग्रह-नक्षत्रों का वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि सूर्य में भी वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कई दरारें आ गई हैं। पृथ्वी और समुद्र की आज की स्थिति तो काफी कुछ बदल ही चुकी है। साहित्य या कहानी इस संसार में है ही कल की। लेकिन कल और आज के दरमियान जो बदलाव आ चुके हैं, उनसे कहानी में बदलाव तो आना ही था।
संसार आज इतना बदल गया कि हमारे पैरों तले की ज़मीन पहले के समय से कई अंशों में मेल नहीं खाती। इस बदलाव का सब कुछ हम समझ नहीं सकते। यह संभव नहीं है। हमारी लेखकीय हैसियत अब किस बिंदु पर आ खड़ी हुई है, हम निर्णायक रूप में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन सोच रहे हैं कि हम कहाँ हैं ! मन के इस उतार-चढ़ाव के बीच भीतर का लेखक आज भी जीवित है। फिर हमने जो कहानियाँ लिखीं, उनमें ‘वृंदावन कथा, ‘पार’ आदि के पाठक अनेक रहे। कहानियाँ प्रकाशित होने के बाद पाठकों की प्रतिक्रियाएँ एक लंबे समय तक चलती रहीं। यह एक छोटा-सा तथ्य है, मेरी कहानियों का कोई विज्ञापन नहीं।
‘वृंदावन कथा’ एक छोटे-मोटे चोर-उचक्के की कहानी है। यह व्यक्ति जाना जाता था ‘बिंद्रावन’ नाम से। वह था गाँव का निवासी। नितांत निरादृत। काम-काज के नाम पर उसे करने को कुछ नहीं सूझा। ऐसे व्यक्ति पर लिखने के लिए मुझे मिला कि वह नितांत स्थितिहीन है। वह चोर ज़रूर है, लेकिन बहुत अक्लमंद नहीं। किसी तरह वह गुज़ारा-भर कर लेता है। कोई और विकल्प उसे दिखाई नहीं पड़ा।
यहाँ मैं समझ गया कि ‘बिंद्रावन’ जिस अवहेलना और तिरस्कार का शिकार है, उसका कुछ कारण निश्चित ही खुद वह भी है, लेकिन उसकी यह नियति एक लेखक को परेशानी करती ही है।
मैं देखता हूँ कि ‘बिंद्रावन’ नाम और परिचय के बाहर एक ऐसा प्राणी है, जिसकी मौत कहीं भी अंकित नहीं होगी। भारत में बिंद्रावन अनेक हैं। असंख्य। उन्हें लोग मौकों पर सज़ा दे देते हैं, लेकिन उनके होने और खत्म होने को कोई घटना नहीं मानता।
जब मैंने ‘पार’ लिखी, दो साल अमेरिका में रहकर वापस भारत लौटा था। अमेरिकी अनुभवों पर बस दो-चार कविताएँ ही सिर्फ लिख सका था। वहाँ ट्रॉय में शोध करता और पढ़ाता ज़रूर था, लिखने के नाम पर एकदम ज़ीरो हो गया था। मैं तब इस कदर खाली हो गया था कि लगता था, अब आगे कभी भी लिख ही नहीं पाऊँगा। बस, एक लेखक को उसका अंत स्वीकार कर लेना था। इस नियति के बाहर निकल आने की सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं थी। 1984 से ’86 तक मैं हर दिन अपना विराम सामने देखता रहा। पहले सोचा था, अभी दो-चार सालों में ही भारत लौटकर नहीं आऊँगा। अंततः कब लौटूँगा, अनिर्णय में था। कभी-कभी लगता था, मेरा मुकाम अब मुमकिन है, भारत न भी हो। लेकिन अन्ततः अपने सामने ज़बरदस्त अनिर्णय था। इसके बीच लगभग दो साल बाद मैंने बोरिया बिस्तर बाँधें और चिड़िया की तरह उड़कर लौट आया। एक अनिर्णय से एक और अनिर्णय में आ तो गया, लेकिन अंततः राहत शुरू हो गई थी। इस बात में सच्चाई कितनी थी, नाप तौलकर कुछ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मेरा मन अपने तमाम संकटों के बावजूद दिल्ली वापस आकर थोड़ा-बहुत हल्का हो गया था।
अब मसला है—अरसे से रुके पड़े लेखन को फिर से शुरू करने का। मन में एक लंबी कहानी की रूपरेखा बनी तो वह थी एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी। उसकी उम्र बहुत हो गई थी। पत्नी की मृत्यु काफी समय पहले की एक घटना थी। छोटी-सी। वह रहता था अपने बेटे और उसके परिवार के साथ। वह वृद्ध व्यक्ति पहले पहलवानी करता था। उसकी ख्याति दूर-दूर तक व्याप्त थी। लेकिन उसकी उम्र जब बहुत ज़्यादा हो गई, उसे चाहने वाले भी धीरे-धीरे छँटते गए। अब उसके इर्द-गिर्द रह गए थे सिर्फ उसका बेटा और उसकी पत्नी। वृद्ध का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं था। यह व्यक्ति के घर के लोगों के लिए अत्यंत उत्पाती बन गया था। बेटा समझ गया था कि पिता की मृत्यु संभवतः बहुत शीघ्र नहीं होगी और उसके तमाम खुराफात कहीं से भी कम नहीं हो जाएँगे। बेटा उधेड़बुन में था। निर्णय नहीं ले पा रहा था कि पिता से मिल रही निरंतर परेशानियों से अब मुक्ति का रास्ता क्या हो ! निर्णय लेना सहज तो नहीं था, लेकिन पिता की स्थिति का कोई समाधान भी नहीं रह गया था। अंततः एक दिन उसने पिता को नए कपड़े पहनाए और एक झोले में ज़रूरी सामान भरकर उसके साथ शहर के लिए चल पड़ा। शहर पहुँचकर वह सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचा। एक टिकट लेकर पिता के हाथ में उसने झोला और टिकट थमाया तो बूढ़े को लेकर गाड़ी चलने लगी। रेलगाड़ी के चलते ही बूढ़ा तो बहुत खुश था, लेकिन बेटा चलती हुई ट्रेन को चुप आँखों से देखता रहा थोड़ी ही देर में गाड़ी आगे बढ़ गई तो अब आखिरी डिब्बे का सिर्फ पीछे का हिस्सा-भर दिखाई दे रहा था। पिता के पार होने का मात्र यही रास्ता अब रह गया था।
यह कहानी लंबी तो थी, लेकिन लिखने का समय बहुत ज़्यादा नहीं था। कहानी मैंने झटपट लिख तो ली, लेकिन लंबाई के कारण यही सोचता रहा कि अंततः किसे दिया जाए ! आखिर में कहानी जब ‘सारिका’ में प्रकाशित हो गई, कितने लोगों ने इसे पढ़ा, न जान पाने के बावजूद कई पाठकों से मेरी यदा-कदा बातचीत हो जाती है। कहानी-लेखन के मामले में जब भी मैं सोचता हूँ, मुझे मनुष्य का संत्रास सामने दिखाई पड़ता है। संत्रास की यह कथा मनुष्य के भीतर आज भी ऐसे उमड़ती है कि वह निर्धनता के शिकंजे में जकड़े जाने के बाद एकदम असहाय है। और इसके बाद उसकी छोटी-सी संभावना भी समाप्त हो जाती है।
जाने-अनजाने मनुष्य का संसार आरंभ होते ही कहानी भी शुरू हो गई थी। किसी न किसी रूप में। वहीं लाखों साल के बाद बनते बिगड़ते आज की कहानी के रूप में अलग-अलग तरीकों से पाठकों के सामने पहुँच रही है। स्पष्ट है, कहानी मानव-सभ्यता का इतिहास दर्शाती है। इस इतिहास में दर्शन तो हैं ही, विज्ञान भी है। कला, संस्कृति और राजनीतिक आधार भी हैं। कुल मिलाकर यह कहना सत्य होगा कि साहित्य, मनुष्य और मनुष्य का विवेचन वैज्ञानिक रूप में है और कहानी की भूमिका इसमें अत्यंत प्रखर है।
इस संसार का अपना एक इतिहास है। तमाम-उखाड़-पछाड़ों के बाद आज भी हम जिस बिंदु तक पहुँचे हैं, हमारे पास जानकारी का दायरा इसके अन्तर्गत बहुत ही नगण्य है। अब जब हम कहानी की बात शुरू करते हैं, हमारी विस्तृति ज़रूर बहुत नहीं हो पाती है, लेकिन शायद हम कुछ गहराई तक पहुँच सकते हैं। हम काफी हद तक जान पाते मनुष्य की संक्रमण और अंतर्मन की कथा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आज की कहानी जिस सामर्थ्य के साथ आ खड़ी हुई है, स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा होना अस्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन हिंदी की कहानियाँ हमेशा ही इस तथ्य को पुष्ट नहीं करतीं। जो भी हो, मैं कहानी का एक सामान्य लेखक-भर हूँ, कोई आलोचक या विश्लेषक नहीं।
हमेशा तो नहीं, लेकिन कई बार कहानी लिखते हुए मैं अपने भीतर शायद किसी सीमा का प्रवेश देख पाता हूँ। संसार के कई टुकड़ों में। उन्हीं में मैं शायद स्वयं को छू भी पाया हूँ। कम से कम अनुभव ऐसा ही हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि पाठकों की इस बारे में क्या राय है ! उनकी राय अगर इससे आंशिक रूप में या मुमकिन है, पूरी तरह भिन्न भी हुई, मैं चुप रहूँगा। फिर से अपने भीतर घुसने की कोशिश कर, ज़्यादा न सही, दो अंगुली की दूरी लाँघने का प्रयास करता रहूँगा। और जहाँ भी मैं असमर्थ हूँ, अपने पाठकों से कबूल करने में मुझे कोई हिचक नहीं होगी।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






_m.jpg)