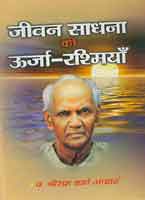|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटरश्रीराम शर्मा आचार्य
|
17 पाठक हैं |
||||||
शरीर से भी विलक्षण मस्तिष्क...
न घुटते रहिये, न भयभीत होइये
मस्तिष्क को मानसिक शक्तियों के केंद्र को आज व्यस्त और असंतुलित करने वाले
कारणों में दो बहुत भयंकर हैं—पहला घुटन और दूसरा भय। यों ये दोनों विकृतियाँ
लगभग एक जैसी हैं। इनमें बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। घुटन में परिस्थितियों की
प्रतिक्रिया होती है, उनसे होने वाली हानि के कारण घबड़ाहट भी होती है, परंतु
व्यक्ति उन परिस्थितियों के कारण इतना भयभीत रहता है कि वह भीतर ही भीतर
घुलता-जलता रहता है। भय में इसी प्रकार की दुर्बलता है। ये दोनों स्थिति
मानसिक असंतुलन के ही दुष्परिणाम हैं।
मस्तिष्क का पूरा नियंत्रण सारे शरीर पर है, उसकी इच्छा से ही नाड़ी संस्थान
काम करता है और ज्ञान तंतुओं के माध्यम से ही उसी का वर्चस्व छोटे से लेकर
बड़े अंगों पर छाया रहता है। ऐसे उद्गम केंद्र में असंतुलन पैदा हो तो वह
स्थानीय नहीं हो सकता, उसका प्रभाव ज्ञान तंतुओं के माध्यम से अन्य अंगों तक
भी पहुँचेगा और वहाँ भी रुग्णता की संभावना उत्पन्न होगी।
मानसिक घुटन को वाणी द्वारा या क्रिया द्वारा फूट कर बाहर निकलने का अवसर
मिलना चाहिए। अन्यथा वह दबाव अनैच्छिक संस्थान की ओर मुड़ जाता है और शरीर
में जो स्वसंचालित क्रियाएँ होती रहती हैं, उनमें वह घुटन वाला विष जा घुलता
है। इससे संबंधित अंगों में सिकुड़न एवं अकड़न पैदा होती है। यदि यह घुटन पेट
की ओर मुड़ जाए तो आमाशय पर अकारण ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है और पाचन
क्रिया में गड़बड़ी मच जाती है। रक्त संचार रुकता है और पाचन रसों की सप्लाई
रुक जाती है। उस गड़बड़ी से पहले आमाशय में सूजन होती है फिर जख्म बन जाते
हैं। अल्सर इसी प्रकार का रोग है, जिसमें शारीरिक कारण कम और मानसिक अधिक
रहते हैं।
यदि शोक-संताप का कोई कारण हो तो जोर से रो पड़ने या फूट-फूटकर बिलखने की
इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। मानसिक आघात से उत्पन्न घुटन बाहर निकाल देने का
यही सरल और स्वाभाविक तरीका है। यदि लोक-लाजवश उस इच्छा को दबाकर अपने वीतराग
या मनस्वी होने का ढोंग किया जाएगा, तो मानव स्वभाव की कमजोरियों पर तो विजय
पाई न जा सकेगी, वह घुटन भी दबकर भीतर बैठ जाएगी और अनेक गड़बड़ियाँ पैदा
करेगी। कोई विषैली चीज पेट में पहुंच जाए तो सीधा तरीका यही है कि उल्टी या
दस्त द्वारा बाहर निकल जाने दिया जाए। यदि उसे निकलने का अवसर न मिला तो वह
विष फिर अनेक भयंकर तरीकों से फूटकर निकलेगा और दस्त-उलटी जैसी कठिनाई की
तुलना में अधिक कष्ट साध्य और समय साध्य होगा।
क्रोध में बकझक कर, जी की जलन शांत कर लेना अच्छा है। पर यदि उस आवेग को मन
में दबा लिया जाए तो वह घृणा या द्वेष के रूप में जड़ जमा कर बैठ जाएगा और
शत्रुता का रूप धारण करके किसी अवसर पर विकराल प्रतिहिंसा का रूप धारण कर
सकता है।
कामुक आकांक्षाओं को होली जैसे त्यौहार पर एक दो दिन उच्छृंखल
नाच-कूदकर-गा-बजाकर निकाल देते हैं और जी हल्का कर लेते हैं, इसके विपरीत मन
में काम विकार घुमड़ते रहें और बाहर से ब्रह्मचारी बनकर बैठा रहा जाए तो भीतर
ही भीतर वह घुटन दूसरे रूप में फूटती है और कई प्रकार के शारीरिक-मानसिक रोग
उत्पन्न करती है।
अच्छा यही है कि मन को ऐसा प्रशिक्षित किया जाए कि उसमें सौम्य सज्जनता ही
स्वाभाविक हो जाए और विकार-विकृतियों के लिए गुंजाइश ही न रहे। पर यदि क्रोध,
शोक आदि आवेग उठ रहे हों तो उन्हें प्रकट होकर बाहर निकल जाने देना चाहिए।
कोई तो ऐसा सच्चा एवं विश्वस्त मित्र होना ही चाहिए, जिसके सामने पेट के छिपे
हुए हर रहस्य और भेद को प्रकट कर दिया जा सके। पिछले पापों को भी किसी ऐसे
विश्वस्त से कह ही देना चाहिए, जो उन्हें हर किसी से कहकर निंदा का वातावरण
तो न बनाये, पर स्वयं सहानुभूतिपूर्वक सुन ले। बदले में घृणा भी न करे। छिपी
शांत को कह सकने योग्य उसे विश्वस्त समझा जाए, इसके लिए मित्र की उदारता और
आत्मीयता को सराहे। ऐसे मित्रों का होना मनोविकारों की घुटन से पीछा छुड़ाने
का अच्छा तरीका है। अपने किये हुए पाप का प्रायश्चित्त कर लेना तो सबसे ही
उत्तम है। उससे घुटन द्वारा होने वाली भयंकर संभावनाओं की तुलना में कहीं कम
कठिनाई उठाकर, न केवल मन हलका कर लिया जाता है, वरन् कितने ही शारीरिक और
मानसिक रोगों की जड़ भी कट जाती है।
मनःसंस्थान में उत्पन्न घुटन विकृतियाँ अथवा भावनात्मक रोग उत्पन्न करती हैं।
उन रोगों के अलग से लक्षण नहीं होते वरन् वे शारीरिक रोगों में मिलकर ही
फूटते हैं। शारीरिक रोग यदि कायगत हों तो मामूली दवा-दारू ही अच्छा कर देती
है। पुराने समय में जब लोग सरल जीवन जिया करते थे, मन में प्रसन्नता,
निष्कपटता और निर्द्वद्वता का संतुलन बनाये रहते थे-तब आज जैसी मानसिक रोगों
की बाढ़ न थी। उस जमाने में केवल काय कष्ट ही होता था, अस्तु उनके उपचार में
कोई कठिनाई नहीं होती थी। अब प्रत्यक्षतः तो शारीरिक रोग ही दीखते हैं, पर
उनके पीछे मानसिक रोगों की जटिल ग्रंथियाँ उलझी होती हैं; जब तक वे न सुलझें,
दवा क्या काम करे। मानसिक रोगों की दवाएँ अभी निकली नहीं हैं। ऐसी स्थिति में
यदि चिकित्सकों को चक्कर में डाल रखने वाले और दवाओं को झुठलाते रहने वाले
रोगों का बाहुल्य औषधि उपचार की परिधि से बाहर निकलने लगे तो उसमें आश्चर्य
की कुछ बात नहीं है।
भावनाएँ यदि निर्मल, उदात्त और उच्चस्तरीय हों तो उनसे हर दृष्टि में लाभ ही
लाभ है। अंतःकरण, मस्तिष्क और शरीर इन तीनों की ही पुष्टि होती है।
परिस्थितिवश यदि शोक, क्रोध जैसे अवसर आ जाएँ और विवेक उनके समाधान में समर्थ
न हो तो उसे स्वाभाविक रीति से प्रकट हो जाने देना चाहिए। जितना संभव हो उतना
मर्यादाओं का पालन किया जाए, विवेक द्वारा बड़ी दीखने वाली बात को छोटी करके
उपेक्षा में डाल दिया जाए, पर यदि वैसा न बन पड़े तो उसके प्रकटीकरण में भी
हर्ज नहीं है।
कामवासना के पीछे मूलवृत्ति हास्य, विनोद और क्रीड़ाकलोल की-कोमल भावनाओं की
उत्तेजना का आनंद लेने की होती है। उसे दूसरे रूप में प्रकट और परिणत किया जा
सकता है। छोटे बालकों को खिलाने, दुलारने से भी सौंदर्य, वासना और निर्मल
हास-विलास की आवश्यकता पूरी हो जाती है। संगीत, साहित्य जैसी ललित कलाओं का
निर्माण ही इस आधार पर हुआ है कि उनसे भावनात्मक नीरसता को सरसता में परिणत
होने का अवसर मिले। नर-नारी में भी निष्पाप हास्य-विनोद चलता रह सकता है।
कुटुंब में बहिन-भाई, देवर-भौजाई, चाची-भतीजे जैसे कई रिश्ते नर-नारी के बीच
रहते हैं। इनमें परस्पर विचार-विनिमय, हास्य-परिहास, वार्तालाप चलता रहे तो
नर-नारी की पूरक आकांक्षाएँ पवित्र स्तर पर पूरी होती रह सकती हैं और
कामेच्छा का उदात्तीकरण होने से उन्हें भावनात्मक तृप्ति मिलती रह सकती है।
पति-पत्नी के बीच भी शरीरों को न्यूनतम मात्रा में ही गलाकर-व्यंग-विनोद,
उपहास-परिहास की शालीन प्रक्रिया अपनाकर मनःक्षेत्र को उल्लास से भरा जा सकता
है और वासनाजन्य घुटन का सहज निष्कासन होता रह सकता है। इस स्थिति में
ब्रह्मचर्य पालन कठिन नहीं पड़ता वरन् सरल हो जाता है।
भावनाओं का अनियंत्रित उभार ठीक शरीर में चढे हए बुखार की तरह है। बुखार में
पाचन तंत्र लड़खड़ा जाता है। कोई अवयव उत्तेजित होकर, अधिक काम कर रहा होता
है तो कोई एकदम शिथिलं पड़ गया होता है। ऐसे असंतुलन में रोगी को दाह, प्यास,
बेचैनी, दर्द आदि कितने ही कष्ट अनुभव होते हैं। भावनात्मक उभार को एक
मस्तिष्कीय बुखार कहना चाहिए। कई बार वह तीव्र होता है, कई बार मंद। क्रोध,
शोक और बेकाबू होकर प्रकट होने वाले आवेग तीव्र बुखार है। चिंता, निराशा,
कुढ़न, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियाँ मंद ज्वर हैं। आकांक्षाओं को इतनी बढ़ा
लेना कि वर्तमान परिस्थिति में कार्यान्वित-फलीभूत न हो सकें तो भी उनसे
अतृप्ति जन्य क्षोभ उत्पन्न होता है और मानसिक संतुलन बिगड़ता है। उन्नति के
लिए प्रयत्न करना बात अलग है और महत्त्वाकांक्षाओं का पहाड़ खड़ा करके हर
घड़ी असंतोष अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है। कितने ही व्यक्ति उपलब्धियों के
लिए व्यवस्थित प्रयास तो कम करते हैं किंतु कामनाओं के रंग-बिरंगे स्वप्न ही
देखते रहते हैं। शेखचिल्ली की तरह लंबी-चौड़ी बातें सोचते रहना तो सरल है, पर
उन्हें फलीभूत बनाने के लिए योग्यता, साधन और परिस्थिति तीनों का ही तालमेल
रहना चाहिए। इसके बिना महत्त्वाकांक्षाएँ-ऐषणाएँ केवल मानसिक विक्षोभ ही दे
सकती हैं। इस प्रकार की उड़ानें उड़ते रहने वाले अंतत: निराशाजन्य मानसिक
रोगों के जाल-जंजाल में जा फँसते हैं।
भावनात्मक विकृतियाँ शरीर के उपयोगी अंगों पर तथा जीवन-संचार की क्रियाओं पर
बुरा असर डालती हैं, उनके सामान्य क्रम को लड़खड़ा देती हैं और वह अवरोध किसी
न किसी शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होता है। पापी मनुष्य दूसरों की जितनी
हानि करता है, उससे ज्यादा अपनी करता है। दुष्कर्म कर लेना अपने हाथ की बात
है, पर उसकी प्रतिक्रिया जो कर्ता के ऊपर होती है और आत्म-धिक्कार की
आत्म-प्रताड़ना की जो भीतर ही भीतर मार पड़ती है, उसे रोकना किसी के बस में
नहीं रहता। पाप-पुण्य के भले-बुरे फल मिलने की यही तो स्वसंचालित प्रक्रिया
है। पाप कर्म के बाद अंतःकरण में अनायास ही पश्चात्ताप और धिक्कार की
प्रतिक्रिया उठती है। उससे शरीर और मन का संतुलन बिगड़ता है। दोनों क्षेत्र
रुग्ण होते हैं। उसके फलस्वरूप जनसहयोग का अभाव, असम्मान मिलता है और संतुलन
बिगड़ा रहने से हाथ में लिए हुए काम असफल होते हैं। इस सबका मिला-जुला स्वरूप
शारीरिक-मानसिक कष्ट के रूप में आधि-व्याधि बनकर सामने आता है। कर्मफल भोग की
यही मनोवैज्ञानिक पद्धति है। इससे बचाव करने के लिए निष्पाप जीवनक्रम अपनाने
की आवश्यकता है। जो पाप पिछले दिन बन पड़े हैं, उनके प्रायश्चित्त के लिए
किसी सूक्ष्मदर्शी आत्मविद्या विज्ञानी से परामर्श लेने की आवश्यकता है।
'साइकोसोमेटिक' रोगों की बाढ़ इन दिनों बौद्धिक विकास के दुरुपयोग ने उत्पन्न
की है। होना यह चाहिए कि यदि प्रबद्धता के दुरुपयोग का खतरा हो तो वहाँ
मानसिक विकास का प्रयास न किया जाए; यदि वह अनुचित लगता है और मस्तिष्कीय
विकास आवश्यक लगता है तो उसे सन्मार्गगामी बनाये जाने की समुचित तैयारी पहले
से ही रखनी चाहिए। विकसित मस्तिष्क यदि दुष्प्रवृत्तियों से भरा रहा तो
निश्चित रूप से वह अभिशाप सिद्ध होगा और उसका दंड जटिल, कष्टसाध्य, दुराग्रही
साइकोसोमेटिक रोगों के रूप में भुगतना पड़ेगा। यह मानसिक रोग झक्कीपन, आवेश,
मतिभ्रम, अर्धविक्षिप्तावस्था, पागलपन आदि के रूप में भी हो सकते हैं और अन्य
शारीरिक अवयवों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं।
घुटन एक—न दीखने वाली न समझ में आने वाली बीमारी है, पर इसका कुप्रभाव किसी
भी भयंकर रोग से कम नहीं होता। अतृप्त और असंतुष्ट मनुष्य अपने आप ही अपने को
खाता, खोता और खोखला करता रहता है। घुटन से बचा जाए। यदि अपनी भूल है-स्थिति
का सही मूल्यांकन न करके काल्पनिक जाल-जंजाल बुन लिया गया है, तो मकड़ी के
जाले को तोड़कर यथार्थता के धरातल पर आना चाहिए और परिस्थितियों के साथ
तालमेल बिठाकर मन का बोझ हल्का करना चाहिए। यदि अपनी मान्यता सही है और दबाव
डालकर आत्मा की आवाज का हनन किया जा रहा है तो फिर ऐसे आधिपत्य से इनकार करके
अपना स्वतंत्र रास्ता बनाना चाहिए; फिर चाहे वह कितना ही असुविधाजनक क्यों न
हो। घुटन में दिन काटते हुए अंतरात्मा को दिन-दिन दुर्बल बनाते जाने से तो
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही बल नष्ट होते हैं। इस प्रकार आत्महत्या
की स्थिति से तो निकलना ही चाहिए भले ही उसमें कुछ बड़ा जोखिम उठाना पड़े।
घुटन यदि आत्मप्रताड़ना की है तो उसे किसी विश्वस्त मित्र के आगे जी खोलकर कह
ही देना चाहिए, इस प्रकार वह धुआँ बाहर निकाल देने पर ही जी हल्का हो सकता
है।
|
|||||


 i
i