|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
दो वर्ष बाद गई तो देखा वही कृतज्ञ मरीज, अपनी जुड़ी नाक के नीचे दगदगाती हँसी
बिखेरता, बहन के द्वार पर खड़ा है। हाथ में, कार्तिकी श्वेत मधु का लबलबाता
पात्र और गोघृत।
ऐसे ही एक बार उनका एक्स-रे लेनेवाला कर्मचारी जुए में अपनी परमा सुन्दरी पत्नी को हार गया। रोती-कलपती पत्नी जयन्ती के द्वार पर आ खड़ी हुई। 'मुझे बचा लो डॉक्टरनी ज्यू, हरामी मुझे जुए में हार आया है, कुल तीन हजार में।' निर्लज्ज पिटा जआरी खडा-खडा टसए बहा रहा था। जयन्ती ने उसे छुड़ा तो लिया पर फिर वह द्रौपदी स्वयं ही पतिगृह नहीं गई। नर्स की ट्रेनिंग दिला, जयन्ती ने ही उसे नौकरी दिला दी और शायद आज भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसी पर मैंने कभी कहानी लिखी थी 'पिटी हुई गोट'। फिर आई सुजाता-बड़ी-बड़ी आँखें, छरहरी देह, सलोनी चितवन और वन्यहरिणी-सी विस्फारित दृष्टि। अधेड़ दुहेजू, शराबी पति दिन-रात ढोल दमामे-सा पीट-पीटकर दिन-रात ताने देता, 'बाँझिन राँड, चार साल में चूहे का बच्चा भी नहीं जन पाई।' वह ससुराल से भागकर भुवाली, जयन्ती के पास आ गई। एकदम पहाड़ी वेशभूषा, काला इटैलीन का मक्खी बेल लगा सात पाट का लहँगा, क्रेप की नीली कुर्ती और कसी-मसी वास्कट। मेरी माँ ने अपनी अनुभवी दृष्टि से, उसे पल भर में तौल दिया-'जयन्ती, विदा कर दे इसे, बहुत पछताएगी, इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते, लहँगे का नाड़ा लटकाकर चलती है-नाड़ा लटकाकर तो वेश्याएं चलती हैं।'
पर जयन्ती ने जो ठान ली, ठान ली। एक वर्ष में ही उसका काया-कल्प हो गया। चेहरे का लावण्य अब सौन्दर्य की देहरी पर खड़ा था-काजल से चिरी आँखें, जूड़े में दाडिम का फूल, उलटे पल्ले की साड़ी और सधे कटाक्ष।
मैंने ही उसका नया नाम धरा था सुजाता। उन्हीं दिनों सुजाता फ़िल्म देखी थी और नैन-नक्श नूतन का-सा ही लगता था।
माँ की भविष्यवाणी शत-प्रतिशत सही निकली। सुजाता के काँटे में पहली मछली फँसी मेरे ही मायके में। बड़े भाई का नौकर गोरा-उजला गबरू जवान था। सजाता पर ऐसा रीझा, कि नित्य सब्जी जलकर कोयला बनने लगी। फलतः जयन्ती को अपना आपका प्रवास, समय से पूर्व ही समाप्त करना पड़ा। सुजाता तो आग लगा, दामन बचाकर बेदाग़ निकल गई थी पर प्रणयी नहीं बचा। एक दिन सुना उसने आत्महत्या कर ली। जयन्ती को आत्मीय स्वजनों, पति और बच्चों की प्रताड़ना ने धैर्यच्युत कर दिया-फिर भी उसने सुजाता को असहाय नहीं रहने दिया। किसी सुदूर ग्राम में, ग्राम-सेविका बनाकर भेज दिया। फिर एक दूसरी आई, उसके प्रणय प्रसंग भी एकाध नहीं रहे। हारकर जयन्ती ने कसम खा ली-अब किसी लड़की को आश्रय नहीं दूंगी। फिर उसकी कसम तोड़ने विधाता ने एक पगली को भेज दिया। लाख खदेड़ा गया पर वह नहीं गई-कभी गाना गाती. कभी नाचती. बरामदे में पड़ी रहती। देखने में गोरी-उजली थी, किन्तु पति किसी और के चक्कर में था-अपने पति की इस प्रवंचना से वह पागल हो गई। एक दिन उसने एकान्त में जयन्ती से कहा- 'सारा गहना चुरा, लँगोट बाँधकर चलती हूँ-हा-हा-हा!'
अभागिनियों का ऐसा विचित्र लॉकर शायद ही संसार में अन्यत्र हो। फिर एक दिन वह पगली बिना किसी से कुछ कहे भाग गई-तीसरे दिन किसी ने काट-कूटकर, लाश सड़क पर फेंक दी थी। फिर शरण ग्रहण करने एक वीभत्स कुष्ठ रोगी आ गया-सेब के पेड़ के नीचे उसे भी शरण मिली। जयन्ती को मैंने समझाया--'डॉक्टर मोजेज को तो मैं जानती हूँ, कहो तो मैं अल्मोड़ा कुष्ठाश्रम में भिजवाने का प्रबन्ध करूँ-तेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जीजाजी भी बड़बड़ा रहे हैं।'
'नहीं।'
उसकी समाज-सेवा आरम्भ हुई, जब वह स्कूल में पढ़ती थी। हमारी माँ ने बाढ़ में बह रही एक अनाथ कोली कन्या को पाल-पोसकर बड़ा किया था, नाम था पाँची बाई। ग्राम के सरपंच ने ही उसका नाम, जाति बताकर उसे माँ के पैरों में डाल दिया था।
पाँची बाई, चौदह वर्ष की हुई तो रवीन्द्रनाथ की कविता की पंक्ति साकार हो उठी, ‘कटाक्षेर बे मम पंचम शर। वह मेरी माँ से 'बा' अर्थात माँ कहती थी, 'बा', उसने कहा, 'मुझे दूल्हा चाहिए।' घर भर उसके निर्लज्ज प्रस्ताव से स्तब्ध था। जयन्ती उसके लिए उसी का-सा एक अनाथ, अनाम कुलगोत्र का सुपात्र ढूँढ़ लाई।
‘जीवाराम'। केसरिया साफ़ा पहने, वह अम्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
जीवाराम का न घर-द्वार था न नौकरी। 'इसे पालेगा कैसे?' अम्मा ने पूछा तो उसने शरमाकर कहा, 'अन्नदाता, तमे छो ने।' (अन्नदाता, आप तो हैं ना!)
बस फिर क्या था, पाँची बाई को दान-दहेज गहना गुरिया देकर स्वयं अम्मा ने उसके पैर पूजे-बारात हमारे घर से विदा हुई और पिछवाड़े-हमारे सागर पेशे में समा गई। मथुरा की बेटी, गोकुल ब्याही। जीवाराम को ड्राइवरी सिखा, ड्राइवर बनाकर ही जयन्ती ने साँस ली। फिर टीकमगढ़ गए तो एक गड़रिया-दुहिता, पति-परित्यक्ता ललिता पधारी। एक आँख की कानी थी इसी से पति ने छोड़ दिया था। पर हमारे साथ चार वर्ष तक रही तो रंगरूप ही बदल गया। पति ने एक दिन मेले में देखा और मुग्ध हो गया। ललिता भी विदा हुई।
हम राजकोट में थे, जीवाराम पाँची की युगल जोड़ी ने, कुछ ही वर्षों में परिवार नियोजन की ऐसी धज्जियाँ उड़ाईं कि प्रत्येक वर्ष एक पाँचीबाई की गोद में तो दूसरा पेट में। राधाबाई, पोपट भाई आदि-आदि। एक दिन जब भरे-पूरे परिवार को छोड़ जीवाराम टी.बी. की चपेट में आ स्वर्ग सिधारे तो उसके बाद पूरा परिवार हमारे साथ रहा। कभी पहाड़, कभी बेंगलूर, पूरे तीस वर्ष रहकर पाँचीबाई को भी सौराष्ट्र के मोह ने खींच लिया।
ऐसे ही एक बार उनका एक्स-रे लेनेवाला कर्मचारी जुए में अपनी परमा सुन्दरी पत्नी को हार गया। रोती-कलपती पत्नी जयन्ती के द्वार पर आ खड़ी हुई। 'मुझे बचा लो डॉक्टरनी ज्यू, हरामी मुझे जुए में हार आया है, कुल तीन हजार में।' निर्लज्ज पिटा जआरी खडा-खडा टसए बहा रहा था। जयन्ती ने उसे छुड़ा तो लिया पर फिर वह द्रौपदी स्वयं ही पतिगृह नहीं गई। नर्स की ट्रेनिंग दिला, जयन्ती ने ही उसे नौकरी दिला दी और शायद आज भी अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसी पर मैंने कभी कहानी लिखी थी 'पिटी हुई गोट'। फिर आई सुजाता-बड़ी-बड़ी आँखें, छरहरी देह, सलोनी चितवन और वन्यहरिणी-सी विस्फारित दृष्टि। अधेड़ दुहेजू, शराबी पति दिन-रात ढोल दमामे-सा पीट-पीटकर दिन-रात ताने देता, 'बाँझिन राँड, चार साल में चूहे का बच्चा भी नहीं जन पाई।' वह ससुराल से भागकर भुवाली, जयन्ती के पास आ गई। एकदम पहाड़ी वेशभूषा, काला इटैलीन का मक्खी बेल लगा सात पाट का लहँगा, क्रेप की नीली कुर्ती और कसी-मसी वास्कट। मेरी माँ ने अपनी अनुभवी दृष्टि से, उसे पल भर में तौल दिया-'जयन्ती, विदा कर दे इसे, बहुत पछताएगी, इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते, लहँगे का नाड़ा लटकाकर चलती है-नाड़ा लटकाकर तो वेश्याएं चलती हैं।'
पर जयन्ती ने जो ठान ली, ठान ली। एक वर्ष में ही उसका काया-कल्प हो गया। चेहरे का लावण्य अब सौन्दर्य की देहरी पर खड़ा था-काजल से चिरी आँखें, जूड़े में दाडिम का फूल, उलटे पल्ले की साड़ी और सधे कटाक्ष।
मैंने ही उसका नया नाम धरा था सुजाता। उन्हीं दिनों सुजाता फ़िल्म देखी थी और नैन-नक्श नूतन का-सा ही लगता था।
माँ की भविष्यवाणी शत-प्रतिशत सही निकली। सुजाता के काँटे में पहली मछली फँसी मेरे ही मायके में। बड़े भाई का नौकर गोरा-उजला गबरू जवान था। सजाता पर ऐसा रीझा, कि नित्य सब्जी जलकर कोयला बनने लगी। फलतः जयन्ती को अपना आपका प्रवास, समय से पूर्व ही समाप्त करना पड़ा। सुजाता तो आग लगा, दामन बचाकर बेदाग़ निकल गई थी पर प्रणयी नहीं बचा। एक दिन सुना उसने आत्महत्या कर ली। जयन्ती को आत्मीय स्वजनों, पति और बच्चों की प्रताड़ना ने धैर्यच्युत कर दिया-फिर भी उसने सुजाता को असहाय नहीं रहने दिया। किसी सुदूर ग्राम में, ग्राम-सेविका बनाकर भेज दिया। फिर एक दूसरी आई, उसके प्रणय प्रसंग भी एकाध नहीं रहे। हारकर जयन्ती ने कसम खा ली-अब किसी लड़की को आश्रय नहीं दूंगी। फिर उसकी कसम तोड़ने विधाता ने एक पगली को भेज दिया। लाख खदेड़ा गया पर वह नहीं गई-कभी गाना गाती. कभी नाचती. बरामदे में पड़ी रहती। देखने में गोरी-उजली थी, किन्तु पति किसी और के चक्कर में था-अपने पति की इस प्रवंचना से वह पागल हो गई। एक दिन उसने एकान्त में जयन्ती से कहा- 'सारा गहना चुरा, लँगोट बाँधकर चलती हूँ-हा-हा-हा!'
अभागिनियों का ऐसा विचित्र लॉकर शायद ही संसार में अन्यत्र हो। फिर एक दिन वह पगली बिना किसी से कुछ कहे भाग गई-तीसरे दिन किसी ने काट-कूटकर, लाश सड़क पर फेंक दी थी। फिर शरण ग्रहण करने एक वीभत्स कुष्ठ रोगी आ गया-सेब के पेड़ के नीचे उसे भी शरण मिली। जयन्ती को मैंने समझाया--'डॉक्टर मोजेज को तो मैं जानती हूँ, कहो तो मैं अल्मोड़ा कुष्ठाश्रम में भिजवाने का प्रबन्ध करूँ-तेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जीजाजी भी बड़बड़ा रहे हैं।'
'नहीं।'
उसकी समाज-सेवा आरम्भ हुई, जब वह स्कूल में पढ़ती थी। हमारी माँ ने बाढ़ में बह रही एक अनाथ कोली कन्या को पाल-पोसकर बड़ा किया था, नाम था पाँची बाई। ग्राम के सरपंच ने ही उसका नाम, जाति बताकर उसे माँ के पैरों में डाल दिया था।
पाँची बाई, चौदह वर्ष की हुई तो रवीन्द्रनाथ की कविता की पंक्ति साकार हो उठी, ‘कटाक्षेर बे मम पंचम शर। वह मेरी माँ से 'बा' अर्थात माँ कहती थी, 'बा', उसने कहा, 'मुझे दूल्हा चाहिए।' घर भर उसके निर्लज्ज प्रस्ताव से स्तब्ध था। जयन्ती उसके लिए उसी का-सा एक अनाथ, अनाम कुलगोत्र का सुपात्र ढूँढ़ लाई।
‘जीवाराम'। केसरिया साफ़ा पहने, वह अम्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
जीवाराम का न घर-द्वार था न नौकरी। 'इसे पालेगा कैसे?' अम्मा ने पूछा तो उसने शरमाकर कहा, 'अन्नदाता, तमे छो ने।' (अन्नदाता, आप तो हैं ना!)
बस फिर क्या था, पाँची बाई को दान-दहेज गहना गुरिया देकर स्वयं अम्मा ने उसके पैर पूजे-बारात हमारे घर से विदा हुई और पिछवाड़े-हमारे सागर पेशे में समा गई। मथुरा की बेटी, गोकुल ब्याही। जीवाराम को ड्राइवरी सिखा, ड्राइवर बनाकर ही जयन्ती ने साँस ली। फिर टीकमगढ़ गए तो एक गड़रिया-दुहिता, पति-परित्यक्ता ललिता पधारी। एक आँख की कानी थी इसी से पति ने छोड़ दिया था। पर हमारे साथ चार वर्ष तक रही तो रंगरूप ही बदल गया। पति ने एक दिन मेले में देखा और मुग्ध हो गया। ललिता भी विदा हुई।
हम राजकोट में थे, जीवाराम पाँची की युगल जोड़ी ने, कुछ ही वर्षों में परिवार नियोजन की ऐसी धज्जियाँ उड़ाईं कि प्रत्येक वर्ष एक पाँचीबाई की गोद में तो दूसरा पेट में। राधाबाई, पोपट भाई आदि-आदि। एक दिन जब भरे-पूरे परिवार को छोड़ जीवाराम टी.बी. की चपेट में आ स्वर्ग सिधारे तो उसके बाद पूरा परिवार हमारे साथ रहा। कभी पहाड़, कभी बेंगलूर, पूरे तीस वर्ष रहकर पाँचीबाई को भी सौराष्ट्र के मोह ने खींच लिया।
हमारे पिता की मृत्यु हुई तो जयन्ती ने पूरे गृह की बागडोर थाम ली।
हमारी शिक्षा, बेंगलूर से पहाड़ की सुदीर्घ यात्रा। अब सोचती हूँ, उसने कैसे यह सब किया होगा? मैं जानती थी कि एक न एक दिन वह गृहस्थी के बन्धन में अवश्य बँधेगी। बहुत पहले हमारे घर आई एक विलक्षण सिद्ध भैरवी ने, चावल की मूठ फेंक, लाल-लाल आँखें कपाल पर चढ़ा, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था-'हाँ-हाँ, तेरी बहन शादी करेगी, अवश्य करेगी।'
वही हुआ, विवाह अचानक ही हुआ वह भी घर भर के विरोध के बावजूद। उसने स्वयं अपना वर चुना। जीजाजी सुदर्शन थे। उच्चपदस्थ चिकित्सक थे। रुचि में, पहनावे में सौ फीसदी अंग्रेज़ किन्तु यक्ष्मा की विकट व्याधि भोग चुके थे। उन दिनों क्षय रोग का अर्थ ही था आसन्न मृत्यु, किन्तु जयन्ती ने साक्षात् सावित्री बन अपने सत्यवान को बचा लिया-गृहस्थ सुख भी भोगा, सन्तान सुख भी। किन्तु वृद्धावस्था में जीजाजी की मृत्यु के बाद वह स्वयं जीने की इच्छा खो बैठी। फिर भी अन्त तक उसकी प्राणशक्ति अदम्य थी-दिन भर रसोई में नाना पकवान बनाती, खाती, खिलाती, अचार-मुरब्बे न जाने क्या-क्या! अतिथियों से घर भरा रहता, अतिथि भी ऐसे कि 'चित्त भी मेरी पट में मेरी, अंटा मेरे बाप का।'
मेरे पास वह एक-दो बार ही आ पाई। हिन्दी संस्थान का पुरस्कार ग्रहण करने आई, तो एक बार फिर वही पुराने दिन लौट आए, ‘याद है तुझे, याद है?'
उसके दो पूर्व परिचित बौद्धभिक्षु गोरखपुर से, उससे खरोष्ठी लिपि के लिखे भोज-पत्र पढ़वाने चले आए और पल भर में उसने उनका संस्कृत अनुवाद कर थमा दिया। काठमांडू गई तो पशुपतिनाथ के दर्शन कर, तत्काल सुन्दर श्लोक लहरी, रचकर चढ़ा आई। फिर पचहत्तर वर्ष की उम्र में जराजीर्ण देह सैकड़ों सीढ़ियाँ पारकर पहुँची, 'तुंगनाथ' -वहाँ भी उनकी महिमा में धाराप्रवाह श्लोक, पहाड़ी झरने से उसके पोपले मुँह से झरते रहे। पुजारी अवाक् खड़ा देखता रहा–'धन्य हो माँ सरस्वती।'
'सरस्वती नहीं हूँ पुजारीजी, सरस्वती की सेविका' ऐसी विदुषी और ऐसी प्रतिभा, किन्तु रवीन्द्रनाथ के ही शब्दों में-जयन्ती रही-'जे नदी मरुस्थले हारालौधारा' (वह नदी जो मरुप्रान्त में खो गई।)
मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उसने असह्य पीड़ा सही। बीच-बीच में कोमा से डूबती-उतराती लौटती तो असहाय अनचीन्ही दृष्टि से इधर-उधर देखती। पैर सूजकर कुप्पा हो गए थे। मैं कुछ दिनों तक रुकी, फिर जब उससे अन्तिम विदा लेकर चलने लगी, तो आँखें भर आईं। वह मुझे पहचान रही थी पर उसकी आँखों में अब आँसू नहीं रहे। अन्तर्वर्ती शोकाग्नि ने अँख के आँसुओं को शायद सुखा दिया था। आखिरी बार देखा तो वह शान्त, निःस्पंद प्रतिमासी एकटक छत को निहार रही थी और मेरा कलेजा फटा जा रहा था।
मुझे कभी-कभी लगता है, समय के साथ-साथ अब रिश्ते भी बदल गए हैं। जो प्रेम, हमारी पीढ़ी के भाई-बहनों में था, वैसा प्रेम इस पीढ़ी में नहीं रहा। हम लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, एक-दूसरे को जली-कटी भी सुनाते थे पर हममें से एक भी हमसे बिछुड़ता तो लगता था, स्वयं हमारा एक अंग विलग हो गया। आज कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जो समृद्ध हैं जो समृद्ध होने पर भी, पैतृक सम्पत्ति के बँटवारे के लिए, साँप-नेवले से एक-दूसरे के खून के प्यासे बन उठते हैं।
'जयन्ती, मैं जा रही हूँ,' मैंने रुंधे गले से कहा-मैं जान गई थी कि यह हमारी अन्तिम भेंट है। उसकी स्थिर दृष्टि, शून्य ही में निबद्ध रही-तब क्या - वह निर्मोह वैराग्य का सूत्र पकड़ चुकी थी?
सुना मृत्यु से तीन-चार दिन पहले, वह फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आई थी। मैं दिन भर उसके पास बैठी रही-एकान्त का सुअवसर पा, वह मुझे अपने हृदय में गोपनीय कक्ष में खींच ले गई थी। मेरी छोटी बहन मंजुला, अपने पति के साथ रात-दिन उसकी सेवा में खड़ी रहती। पर उस दिन हम दोनों ही अकेली थीं। जयंती के छोटे पुत्र पुष्पेश ने उसकी अन्त तक ममतामयी सेवा की। पर उसकी नौकरी भी थी। वह काम पर जाता तो वह प्रायः अकेली पड़ी रहती-असहाय-विवश। जननी के हृदय में यत्न से छिपाए गए नासूरों पर सन्तान की दृष्टि पड़ती भी कम है। तिस पर रोग ने उसे चिड़चिड़ी बना दिया था, नवीन पीढ़ी की उदासीनता, अबाध्यता, अशिष्टता झेलती वह अवश हो गई थी।
'तूने अपनी किसी कहानी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है पुत्र की नाल दो बार कटती है, एक बार जब वह माँ के गर्भ से विलग होता है, दूसरी बार तब, जब उसका विवाह होता है।' फिर हँसकर उसने मेरा हाथ धीरे से दबा दिया।
एक वयस के बाद, वाणी लाख समर्थ होने पर भी जो नहीं कह पाती, स्पर्श अपने सामान्य दबाव से ही बहुत कुछ कह जाता है।
उस दिन उसका वह स्पर्श मुझसे बहुत कुछ कह गया था। दिन भर अकेली पड़ी-पड़ी, पुरानी बातें याद करती रहती हूँ। कॉलेज की, शिलांग की, बेंगलूर की, ओरछा की, राजकोट की, याद है तुझे, अम्मा कितनी मीठी आवाज में गरबा गाती थी-
'आज तो सपना मा मने
डोलता डुंगर दीव्याजो'
(अरी आज सपने में मुझे डोलते पहाड़ दिखे)
शायद, उसके सिरहाने खड़ी मौत उसे कुमाऊँ की वे ही विस्मृत गिरि श्रेणियाँ दिखा रही थी जो कभी हम अपने आँगन की ऊँची दीवार पर बैठ कर देखती थीं-कामेत, नन्दा देवी, त्रिशूल, बानड़ी...।
मुझे उसके हृदय में गड़े एक-एक गोखरू कंटक की अभिज्ञता थी किन्तु फाँस को, आज तक कौन निकालकर दूर फेंक सका है? वह तो जितना निकालने की चेष्टा करो, उतनी ही गहराई में धंसती जाती है। शायद यही कसक, उसको विपरीत दिशा में खींच ले गई थी। परनिन्दा में उसे परम आनन्द आने लगा था। सगे-सम्बन्धियों ने उसकी इस दुर्बलता को जमकर भुनाया। पहले उसे खूब बकाते, फिर उसकी अविवेकी बतकही में नमक-मिर्च लगा, इधर-उधर फैलाते-
'वह ऐसा कह रही थी'-
'तुम्हारी निन्दा करते नहीं अघा रही थी।'
'सठिया गई है, हर वक्त खाँऊ-खाँऊ...'
'अरे हमेशा से ही लोगों को असली मुर्गों-सा लड़ाती थी, आज कौन नई बात है', आदि-आदि।
किन्तु कैसा है उसका वैदुष्य। उसका अकपट हृदय कैसा दर्पण-सा स्वच्छ है। वह कितनी परम् करुणामयी भी तो हैं, सर्वस्व त्यागकर अपना खजाना लुटानेवाली औघड़ दानी। यह सब किसी ने नहीं देखा-अन्त में उसका खज़ाना एकदम खाली हो चुका था। घरवाले जानबूझकर हाथ में रुपया नहीं देते थे कि लाख रुपया भी देंगे तो लुटा देगी। पूरी पेंशन तक वह पहले ही दान कर चुकी थी। एक चमत्कारी कछुआ अवश्य उसके साथ अन्तिम साँस तक रहा। सत्तर वर्ष पूर्व, महासिद्ध नारद बाबा का उसे दिया किसी धातु का बना कछुआ।
'एक ताँबे का पैसा भी इसे छुआएगी तो चाँदी का रुपया बनकर, तेरे बटुए में स्वयं आ जाएगा।' उन्होंने कहा था-हम भाई-बहन भले ही उस चमत्कारी कछुए की पीठ-पीछे हँसी उड़ाते हों, लुकछिपकर, अपना-अपना बटुआ उसके कलेवर से हम एक न एक बार छुआ ही आते थे। स्वयं मैंने कई बार ऐसा किया और फिर मेरा बटुआ कभी खाली नहीं हुआ। प्रातः छुआया तो सन्ध्या होते-होते या रॉयल्टी या कोई साहित्यिक पुरस्कार या किसी कहानी का अप्रत्याशित पारिश्रमिक मिला अवश्य।
उसकी मृत्यु से सात-आठ दिन पहले उससे कहा-'जयन्ती, भुवाली में तेरा अपना बँगला है, चली क्यों नहीं जाती, थोड़ा बदलाव हो जाएगा, यहाँ दिन भर पड़ी-पड़ी सोचती रहती है। तुझसे बहुत छोटी हूँ पर इतना बता दूँ आदमी को बीमारी नहीं मारती, मारती हैं यादें।'
वह हँसी, सूखे पपड़ी पड़े ओठों पर क्षण भर को तिरती वह करुण हँसी, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी-मेरा हाथ पकड़ उसने अपने ज्वरतप्त हाथों में दबाकर, क्षीण स्वर में कहा-
सर सूखे पच्छी उडै और सरन समाय।
दीन मीन बिन पच्छ के कह रहीम कहँ जाय?
हमारी शिक्षा, बेंगलूर से पहाड़ की सुदीर्घ यात्रा। अब सोचती हूँ, उसने कैसे यह सब किया होगा? मैं जानती थी कि एक न एक दिन वह गृहस्थी के बन्धन में अवश्य बँधेगी। बहुत पहले हमारे घर आई एक विलक्षण सिद्ध भैरवी ने, चावल की मूठ फेंक, लाल-लाल आँखें कपाल पर चढ़ा, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था-'हाँ-हाँ, तेरी बहन शादी करेगी, अवश्य करेगी।'
वही हुआ, विवाह अचानक ही हुआ वह भी घर भर के विरोध के बावजूद। उसने स्वयं अपना वर चुना। जीजाजी सुदर्शन थे। उच्चपदस्थ चिकित्सक थे। रुचि में, पहनावे में सौ फीसदी अंग्रेज़ किन्तु यक्ष्मा की विकट व्याधि भोग चुके थे। उन दिनों क्षय रोग का अर्थ ही था आसन्न मृत्यु, किन्तु जयन्ती ने साक्षात् सावित्री बन अपने सत्यवान को बचा लिया-गृहस्थ सुख भी भोगा, सन्तान सुख भी। किन्तु वृद्धावस्था में जीजाजी की मृत्यु के बाद वह स्वयं जीने की इच्छा खो बैठी। फिर भी अन्त तक उसकी प्राणशक्ति अदम्य थी-दिन भर रसोई में नाना पकवान बनाती, खाती, खिलाती, अचार-मुरब्बे न जाने क्या-क्या! अतिथियों से घर भरा रहता, अतिथि भी ऐसे कि 'चित्त भी मेरी पट में मेरी, अंटा मेरे बाप का।'
मेरे पास वह एक-दो बार ही आ पाई। हिन्दी संस्थान का पुरस्कार ग्रहण करने आई, तो एक बार फिर वही पुराने दिन लौट आए, ‘याद है तुझे, याद है?'
उसके दो पूर्व परिचित बौद्धभिक्षु गोरखपुर से, उससे खरोष्ठी लिपि के लिखे भोज-पत्र पढ़वाने चले आए और पल भर में उसने उनका संस्कृत अनुवाद कर थमा दिया। काठमांडू गई तो पशुपतिनाथ के दर्शन कर, तत्काल सुन्दर श्लोक लहरी, रचकर चढ़ा आई। फिर पचहत्तर वर्ष की उम्र में जराजीर्ण देह सैकड़ों सीढ़ियाँ पारकर पहुँची, 'तुंगनाथ' -वहाँ भी उनकी महिमा में धाराप्रवाह श्लोक, पहाड़ी झरने से उसके पोपले मुँह से झरते रहे। पुजारी अवाक् खड़ा देखता रहा–'धन्य हो माँ सरस्वती।'
'सरस्वती नहीं हूँ पुजारीजी, सरस्वती की सेविका' ऐसी विदुषी और ऐसी प्रतिभा, किन्तु रवीन्द्रनाथ के ही शब्दों में-जयन्ती रही-'जे नदी मरुस्थले हारालौधारा' (वह नदी जो मरुप्रान्त में खो गई।)
मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उसने असह्य पीड़ा सही। बीच-बीच में कोमा से डूबती-उतराती लौटती तो असहाय अनचीन्ही दृष्टि से इधर-उधर देखती। पैर सूजकर कुप्पा हो गए थे। मैं कुछ दिनों तक रुकी, फिर जब उससे अन्तिम विदा लेकर चलने लगी, तो आँखें भर आईं। वह मुझे पहचान रही थी पर उसकी आँखों में अब आँसू नहीं रहे। अन्तर्वर्ती शोकाग्नि ने अँख के आँसुओं को शायद सुखा दिया था। आखिरी बार देखा तो वह शान्त, निःस्पंद प्रतिमासी एकटक छत को निहार रही थी और मेरा कलेजा फटा जा रहा था।
मुझे कभी-कभी लगता है, समय के साथ-साथ अब रिश्ते भी बदल गए हैं। जो प्रेम, हमारी पीढ़ी के भाई-बहनों में था, वैसा प्रेम इस पीढ़ी में नहीं रहा। हम लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, एक-दूसरे को जली-कटी भी सुनाते थे पर हममें से एक भी हमसे बिछुड़ता तो लगता था, स्वयं हमारा एक अंग विलग हो गया। आज कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं जो समृद्ध हैं जो समृद्ध होने पर भी, पैतृक सम्पत्ति के बँटवारे के लिए, साँप-नेवले से एक-दूसरे के खून के प्यासे बन उठते हैं।
'जयन्ती, मैं जा रही हूँ,' मैंने रुंधे गले से कहा-मैं जान गई थी कि यह हमारी अन्तिम भेंट है। उसकी स्थिर दृष्टि, शून्य ही में निबद्ध रही-तब क्या - वह निर्मोह वैराग्य का सूत्र पकड़ चुकी थी?
सुना मृत्यु से तीन-चार दिन पहले, वह फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आई थी। मैं दिन भर उसके पास बैठी रही-एकान्त का सुअवसर पा, वह मुझे अपने हृदय में गोपनीय कक्ष में खींच ले गई थी। मेरी छोटी बहन मंजुला, अपने पति के साथ रात-दिन उसकी सेवा में खड़ी रहती। पर उस दिन हम दोनों ही अकेली थीं। जयंती के छोटे पुत्र पुष्पेश ने उसकी अन्त तक ममतामयी सेवा की। पर उसकी नौकरी भी थी। वह काम पर जाता तो वह प्रायः अकेली पड़ी रहती-असहाय-विवश। जननी के हृदय में यत्न से छिपाए गए नासूरों पर सन्तान की दृष्टि पड़ती भी कम है। तिस पर रोग ने उसे चिड़चिड़ी बना दिया था, नवीन पीढ़ी की उदासीनता, अबाध्यता, अशिष्टता झेलती वह अवश हो गई थी।
'तूने अपनी किसी कहानी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है पुत्र की नाल दो बार कटती है, एक बार जब वह माँ के गर्भ से विलग होता है, दूसरी बार तब, जब उसका विवाह होता है।' फिर हँसकर उसने मेरा हाथ धीरे से दबा दिया।
एक वयस के बाद, वाणी लाख समर्थ होने पर भी जो नहीं कह पाती, स्पर्श अपने सामान्य दबाव से ही बहुत कुछ कह जाता है।
उस दिन उसका वह स्पर्श मुझसे बहुत कुछ कह गया था। दिन भर अकेली पड़ी-पड़ी, पुरानी बातें याद करती रहती हूँ। कॉलेज की, शिलांग की, बेंगलूर की, ओरछा की, राजकोट की, याद है तुझे, अम्मा कितनी मीठी आवाज में गरबा गाती थी-
'आज तो सपना मा मने
डोलता डुंगर दीव्याजो'
(अरी आज सपने में मुझे डोलते पहाड़ दिखे)
शायद, उसके सिरहाने खड़ी मौत उसे कुमाऊँ की वे ही विस्मृत गिरि श्रेणियाँ दिखा रही थी जो कभी हम अपने आँगन की ऊँची दीवार पर बैठ कर देखती थीं-कामेत, नन्दा देवी, त्रिशूल, बानड़ी...।
मुझे उसके हृदय में गड़े एक-एक गोखरू कंटक की अभिज्ञता थी किन्तु फाँस को, आज तक कौन निकालकर दूर फेंक सका है? वह तो जितना निकालने की चेष्टा करो, उतनी ही गहराई में धंसती जाती है। शायद यही कसक, उसको विपरीत दिशा में खींच ले गई थी। परनिन्दा में उसे परम आनन्द आने लगा था। सगे-सम्बन्धियों ने उसकी इस दुर्बलता को जमकर भुनाया। पहले उसे खूब बकाते, फिर उसकी अविवेकी बतकही में नमक-मिर्च लगा, इधर-उधर फैलाते-
'वह ऐसा कह रही थी'-
'तुम्हारी निन्दा करते नहीं अघा रही थी।'
'सठिया गई है, हर वक्त खाँऊ-खाँऊ...'
'अरे हमेशा से ही लोगों को असली मुर्गों-सा लड़ाती थी, आज कौन नई बात है', आदि-आदि।
किन्तु कैसा है उसका वैदुष्य। उसका अकपट हृदय कैसा दर्पण-सा स्वच्छ है। वह कितनी परम् करुणामयी भी तो हैं, सर्वस्व त्यागकर अपना खजाना लुटानेवाली औघड़ दानी। यह सब किसी ने नहीं देखा-अन्त में उसका खज़ाना एकदम खाली हो चुका था। घरवाले जानबूझकर हाथ में रुपया नहीं देते थे कि लाख रुपया भी देंगे तो लुटा देगी। पूरी पेंशन तक वह पहले ही दान कर चुकी थी। एक चमत्कारी कछुआ अवश्य उसके साथ अन्तिम साँस तक रहा। सत्तर वर्ष पूर्व, महासिद्ध नारद बाबा का उसे दिया किसी धातु का बना कछुआ।
'एक ताँबे का पैसा भी इसे छुआएगी तो चाँदी का रुपया बनकर, तेरे बटुए में स्वयं आ जाएगा।' उन्होंने कहा था-हम भाई-बहन भले ही उस चमत्कारी कछुए की पीठ-पीछे हँसी उड़ाते हों, लुकछिपकर, अपना-अपना बटुआ उसके कलेवर से हम एक न एक बार छुआ ही आते थे। स्वयं मैंने कई बार ऐसा किया और फिर मेरा बटुआ कभी खाली नहीं हुआ। प्रातः छुआया तो सन्ध्या होते-होते या रॉयल्टी या कोई साहित्यिक पुरस्कार या किसी कहानी का अप्रत्याशित पारिश्रमिक मिला अवश्य।
उसकी मृत्यु से सात-आठ दिन पहले उससे कहा-'जयन्ती, भुवाली में तेरा अपना बँगला है, चली क्यों नहीं जाती, थोड़ा बदलाव हो जाएगा, यहाँ दिन भर पड़ी-पड़ी सोचती रहती है। तुझसे बहुत छोटी हूँ पर इतना बता दूँ आदमी को बीमारी नहीं मारती, मारती हैं यादें।'
वह हँसी, सूखे पपड़ी पड़े ओठों पर क्षण भर को तिरती वह करुण हँसी, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी-मेरा हाथ पकड़ उसने अपने ज्वरतप्त हाथों में दबाकर, क्षीण स्वर में कहा-
सर सूखे पच्छी उडै और सरन समाय।
दीन मीन बिन पच्छ के कह रहीम कहँ जाय?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






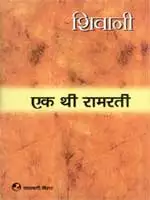


_s.jpg)
