|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
हमारी माँ कहतीं- 'साक्षात् देवी का स्पर्श है इनकी अँगुलियों में।'
एक बार मुझे तेज बुखार हो आया, आँय-बाँय बकती विस्तर से भागने लगी थी। खाला आईं और जैसे ही उन्होंने नरम हथेली मेरे माथे पर धरी, सुना में शान्त होकर सो गई। उनके शरीर से आती वह मदमस्त खुशबू, रेशमी बुर्के की सरसराहट, बुर्के की जालीदार चिलमन से स्नेह विगलित दृष्टि से मुझे देखतीं वे सुरमाभरी आँखें, आज तक न जाने मेरी कितनी कहानियों की नायिकाओं को सँवार चुकी हैं।
हम तब उस बिरादरी में ऐसे घुलमिल गए थे कि कभी-कभी भूल जाते कि हम हिन्दू हैं। एक बार हम अपने पुराने ड्राइवर, शफीकुल बारी को अम्माँ की बधाई देने उनके घर आए। उनका बेटा मुईन हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटा था। साथ में मेरा छोटा भाई राजा भी था, उस दिन जन्म था इसी से टोपी लगाए था। उसे देखते ही बारी की अम्माँ ने टोक दिया- 'हाय अल्ला, आज हिन्दुओं की-सी टोपी लगाकर आए हो भैया।' मुझे हँसी आ गई थी'क्यों अम्माँ भूल गईं, हम तो हिन्दू ही हैं।' खिसियाकर उन्होंने अपना माथा ठोककर कहा, 'हाय अल्ला, मैं तो भूल ही गई थी विन्नो!'
होली के दिन एक और चेहरा बरबस याद हो आता है, 'दाना मियाँ'नैनीताल की एक खास शख्सियत, सफेद दाढ़ी, पान से रँगी बत्तीसी, सिर पर दुपलिया टोपी, पीछे-पीछे पहाड़ी कुली के सिर पर धरी किताबों की गठरी। नित्य फेरी लगाते, कभी शेर का डाँडा, कभी अंयार पाटा और कभी तल्लीताल बस स्टैंड के पास ही अपनी फटी चादर पर, किताबें सजाकर बैठ जाते, एक किताब पढ़ाने का रेट एक चवन्नी, पुरानी किताबें पढ़कर वापस करनी होतीं।
एक दिन, हमने टोक दिया- “वाह दाना मियाँ, आपका बिजनेस अच्छा है, चित भी मेरी, पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का' किताब भी मिल गई, पैसे भी।"
चट से बोले, “माफ कीजिए हुजूर, आप पढ़े-लिखों से तो हम अनपढ़ अच्छा-इत्ती-सी बात आपकी समझ में न आई। आप लोग सलीमे जाती हैं, देखा और चली आईं, क्या सलीमे को यह कहकर घर लाती हैं कि हमने तो पैसे दिए हैं? देखा और दिमाग के कोठे में भर लिया, ऐसा ही किताबों का इल्म है, पढ़ा और दिमाग के कोठे में भर लिया।"
उनकी गठरी में फ्लौबेयर, मॉम, गॉल्सवर्दी से लेकर किस्सा हातिमताई और चहारदरवेश सबकुछ रहता, सचमुच ही उन्हीं की सीख और असंख्य चवन्नियों ने, न केवल हमारे दिमाग का कोठा ठसाठस भर दिया, हमारे बच्चों का भी कोठा भर दिया।
होली की सुबह दूर से ही अपने पठानी हाथ हिलाते, वे हाँक लगाते'होली की गुझिया मुबारक, अबीर-गुलाल मुबारक!' उनकी मेहँदी से रँगी दाढ़ी पर अबीर-गुलाल के छींटे रहते। गुझिया खा हम पर दुआएँ बरसाते वे चले जाते- 'आपको तेज बुखार है, फिर भी आप इस चढ़ाई को पार कर आ ही गए', हमने कहा तो वे हँसे–'हुजूर, प्यासा मीठे चश्मे के पास ही जाता है।' आज सोचती हूँ, क्या उन मीठे चश्मों का उत्स ही सूख गया है?
एक और घटना याद हो आती है, वह भी होली की ही। साहिबजादा हामिद अली साहिब ने हमें गोद में खिलाया था, इसी से परिचय बहुत पुराना था, अन्त तक उन्होंने वह रिश्ता निभाया, भाईदूज, रक्षाबन्धन हो या होली, दीवाली, वे हमारे प्रथम अतिथि रहते-कोई दस-बारह साल पहले की बात है, प्रातः होली का हुड़दंग आरम्भ भी नहीं हुआ था कि उन्होंने घंटी बजाई-बेहद गुस्से में थे, ‘पता नहीं तुम हिन्दुओं का यह कैसा कमबख्त त्योहार है, देखो हमारी बुर्राक तमनियों की क्या गत बना दी है। इत्ती सुबह घर से निकले कि तुम्हें होली की मुबारकबाद दे आएँ पर न जाने किस सिरफिरे को यह मजाक सूझा, लंगूर बनाकर रख दिया-लाहौल विला कूवत!'
एक तो विराट भीमकाय शरीर, उस पर लाल बैंजनी रंग की अजब बहार, मुझे हँसी आ गई तो वे फिर बिफर उठे-'हँसती है! शर्म नहीं आती?'
‘पर मैंने रंग नहीं डाला हामिद भाई।' ‘पर समझा नहीं सकतीं अपनी बिरादरी को?'
बड़ी मुश्किल से उन्हें मीठी गुझिया खिला, उनका गुस्सा शान्त किया- 'मैं लखनऊ की पूरी हिन्दू बिरादरी की ओर से आपसे माफी माँगती हूँ हामिद भाई-माफ कर दीजिए।'
'ठीक है, ठीक है, जाओ माफ किया।'
आज बेरहम जमाने ने एक फाँस हमारे कलेजे में छोड़ दी है जो रह-रह कर सालती है। त्योहार वही हैं, हम वही हैं, वे ही मन्दिर हैं, वे ही मसजिद किन्तु हमारे दिल बदल गए हैं।
क्या ईद और होली के वे सहज सुखद दिन फिर कभी लौटेंगे? क्या हममें वह औदार्य वह सहिष्णुता रह गई है जो हम कह सकें कि 'ठीक है, ठीक है, जाओ माफ किया।' आज, दूध का जला हर हिन्दू, हर मुसलमान ठंडी छाछ भी फूंक-फूंककर पी रहा है।
ईद की सेवइयों की वह मिठास, मेवे भरी गुझियों का वह अमृत तुल्य स्वाद फिर हमें पुलकित कर पाएगा? हो सकता है, स्थिति धीरे-धीरे सुधरे, इनसान एक बार फिर इनसान बनने की चेष्टा करे, किन्तु रहीम की सीख भयभीत आशंकित चित्त को विचलित अवश्य करती है।
'रहिमन तागा प्रेम का
मत तोड़ो चटकाय
टूटे तो फिर ना जुड़े
जुड़े गाँठ लग जाए।'
एक बार मुझे तेज बुखार हो आया, आँय-बाँय बकती विस्तर से भागने लगी थी। खाला आईं और जैसे ही उन्होंने नरम हथेली मेरे माथे पर धरी, सुना में शान्त होकर सो गई। उनके शरीर से आती वह मदमस्त खुशबू, रेशमी बुर्के की सरसराहट, बुर्के की जालीदार चिलमन से स्नेह विगलित दृष्टि से मुझे देखतीं वे सुरमाभरी आँखें, आज तक न जाने मेरी कितनी कहानियों की नायिकाओं को सँवार चुकी हैं।
हम तब उस बिरादरी में ऐसे घुलमिल गए थे कि कभी-कभी भूल जाते कि हम हिन्दू हैं। एक बार हम अपने पुराने ड्राइवर, शफीकुल बारी को अम्माँ की बधाई देने उनके घर आए। उनका बेटा मुईन हॉकी में स्वर्ण पदक लेकर लौटा था। साथ में मेरा छोटा भाई राजा भी था, उस दिन जन्म था इसी से टोपी लगाए था। उसे देखते ही बारी की अम्माँ ने टोक दिया- 'हाय अल्ला, आज हिन्दुओं की-सी टोपी लगाकर आए हो भैया।' मुझे हँसी आ गई थी'क्यों अम्माँ भूल गईं, हम तो हिन्दू ही हैं।' खिसियाकर उन्होंने अपना माथा ठोककर कहा, 'हाय अल्ला, मैं तो भूल ही गई थी विन्नो!'
होली के दिन एक और चेहरा बरबस याद हो आता है, 'दाना मियाँ'नैनीताल की एक खास शख्सियत, सफेद दाढ़ी, पान से रँगी बत्तीसी, सिर पर दुपलिया टोपी, पीछे-पीछे पहाड़ी कुली के सिर पर धरी किताबों की गठरी। नित्य फेरी लगाते, कभी शेर का डाँडा, कभी अंयार पाटा और कभी तल्लीताल बस स्टैंड के पास ही अपनी फटी चादर पर, किताबें सजाकर बैठ जाते, एक किताब पढ़ाने का रेट एक चवन्नी, पुरानी किताबें पढ़कर वापस करनी होतीं।
एक दिन, हमने टोक दिया- “वाह दाना मियाँ, आपका बिजनेस अच्छा है, चित भी मेरी, पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का' किताब भी मिल गई, पैसे भी।"
चट से बोले, “माफ कीजिए हुजूर, आप पढ़े-लिखों से तो हम अनपढ़ अच्छा-इत्ती-सी बात आपकी समझ में न आई। आप लोग सलीमे जाती हैं, देखा और चली आईं, क्या सलीमे को यह कहकर घर लाती हैं कि हमने तो पैसे दिए हैं? देखा और दिमाग के कोठे में भर लिया, ऐसा ही किताबों का इल्म है, पढ़ा और दिमाग के कोठे में भर लिया।"
उनकी गठरी में फ्लौबेयर, मॉम, गॉल्सवर्दी से लेकर किस्सा हातिमताई और चहारदरवेश सबकुछ रहता, सचमुच ही उन्हीं की सीख और असंख्य चवन्नियों ने, न केवल हमारे दिमाग का कोठा ठसाठस भर दिया, हमारे बच्चों का भी कोठा भर दिया।
होली की सुबह दूर से ही अपने पठानी हाथ हिलाते, वे हाँक लगाते'होली की गुझिया मुबारक, अबीर-गुलाल मुबारक!' उनकी मेहँदी से रँगी दाढ़ी पर अबीर-गुलाल के छींटे रहते। गुझिया खा हम पर दुआएँ बरसाते वे चले जाते- 'आपको तेज बुखार है, फिर भी आप इस चढ़ाई को पार कर आ ही गए', हमने कहा तो वे हँसे–'हुजूर, प्यासा मीठे चश्मे के पास ही जाता है।' आज सोचती हूँ, क्या उन मीठे चश्मों का उत्स ही सूख गया है?
एक और घटना याद हो आती है, वह भी होली की ही। साहिबजादा हामिद अली साहिब ने हमें गोद में खिलाया था, इसी से परिचय बहुत पुराना था, अन्त तक उन्होंने वह रिश्ता निभाया, भाईदूज, रक्षाबन्धन हो या होली, दीवाली, वे हमारे प्रथम अतिथि रहते-कोई दस-बारह साल पहले की बात है, प्रातः होली का हुड़दंग आरम्भ भी नहीं हुआ था कि उन्होंने घंटी बजाई-बेहद गुस्से में थे, ‘पता नहीं तुम हिन्दुओं का यह कैसा कमबख्त त्योहार है, देखो हमारी बुर्राक तमनियों की क्या गत बना दी है। इत्ती सुबह घर से निकले कि तुम्हें होली की मुबारकबाद दे आएँ पर न जाने किस सिरफिरे को यह मजाक सूझा, लंगूर बनाकर रख दिया-लाहौल विला कूवत!'
एक तो विराट भीमकाय शरीर, उस पर लाल बैंजनी रंग की अजब बहार, मुझे हँसी आ गई तो वे फिर बिफर उठे-'हँसती है! शर्म नहीं आती?'
‘पर मैंने रंग नहीं डाला हामिद भाई।' ‘पर समझा नहीं सकतीं अपनी बिरादरी को?'
बड़ी मुश्किल से उन्हें मीठी गुझिया खिला, उनका गुस्सा शान्त किया- 'मैं लखनऊ की पूरी हिन्दू बिरादरी की ओर से आपसे माफी माँगती हूँ हामिद भाई-माफ कर दीजिए।'
'ठीक है, ठीक है, जाओ माफ किया।'
आज बेरहम जमाने ने एक फाँस हमारे कलेजे में छोड़ दी है जो रह-रह कर सालती है। त्योहार वही हैं, हम वही हैं, वे ही मन्दिर हैं, वे ही मसजिद किन्तु हमारे दिल बदल गए हैं।
क्या ईद और होली के वे सहज सुखद दिन फिर कभी लौटेंगे? क्या हममें वह औदार्य वह सहिष्णुता रह गई है जो हम कह सकें कि 'ठीक है, ठीक है, जाओ माफ किया।' आज, दूध का जला हर हिन्दू, हर मुसलमान ठंडी छाछ भी फूंक-फूंककर पी रहा है।
ईद की सेवइयों की वह मिठास, मेवे भरी गुझियों का वह अमृत तुल्य स्वाद फिर हमें पुलकित कर पाएगा? हो सकता है, स्थिति धीरे-धीरे सुधरे, इनसान एक बार फिर इनसान बनने की चेष्टा करे, किन्तु रहीम की सीख भयभीत आशंकित चित्त को विचलित अवश्य करती है।
'रहिमन तागा प्रेम का
मत तोड़ो चटकाय
टूटे तो फिर ना जुड़े
जुड़े गाँठ लग जाए।'
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






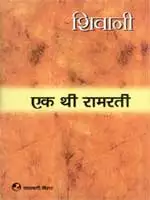


_s.jpg)
