|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
हाथ जोइँ गोरा जी
मैं तो बीबी बामणी
मैं तो बीबी बामणी
उन दिनों के उद्धत मर्कटमुखी गोरे फौजी से वह सरल निवेदन, वैसा ही कामात शत्रु
से संघर्ष का ऐसा मौलिक अभिनय कि आज की बलात्कार अभिनय पटीयसी चलचित्र तारिकाएँ
भी पानी भरें।
लोहनीजी केवल भूत-प्रेतों की ही कहानियाँ सुनाया करते थे। उनके शब्दों में वे कहानियाँ उनके भोगे हुए यथार्थ की कहानियाँ थीं।
“साली-हरामजादी चुडैलों को हम जाने क्यों पसन्द हैं! हमें देखते ही पीपल के पेड़ से टपटप टपकने लगती हैं, पर मजाल है जो आज तक हमें एक भी छू पाई हो!"
उनकी एक अत्यन्त प्रिय कहानी थी 'जागो हो, मैं लै उणयूँ' (रुक जाओ जी, मैं भी आ रहा हूँ)। कैसे वे घर से छुट्टियों के बाद अपने गाँव सतराली से, अँधेरे में उल्टी घड़ी देख, आधी रात ही को चल पड़े थे और पीछे-पीछे लग गया था मसान का खबीस। चलते-चलते घंटों बीत गये, पर रात नहीं बीती। अँधेरे घने जंगल से गुजर रहे थे तब वह नक्की स्वर गूंजा, “जागो हो...मैं लै उणयूँ।"
लोहनीजी समझ गए, वह कौन है। पर प्रेतबाधा का एक-एक कीलक अर्गला तो वे साथ लिए चलते थे, न हुंकारा दिया, न पीछे मुड़कर देखा, पर वह हरामी क्यों चूकता? मुस्टंडा, कभी बैल बनकर सींग घुमाता, कभी अग्निपुंज बनकर 'फ्वाँ फ्वाँ' करता! कभी नक्की स्वर में कहता। 'जागो हो!'
लोहनीजी स्वयं उसकी नक्की स्वर में वह हाँक दुहराते तो हम डरकर उनके पास सरक आते, “बस लोहनीजी, बस! अब कल सुनेंगे!"
वे हँसकर हमें पास खींच लेते, “अरे पगली, जब तक वह पुरुषोत्तम है ना, इस घर में मजाल है जो कोई दुष्टात्मा कदम तो धर ले!"
लेकिन उनके जाते ही, न जाने कितनी अशरीरी आत्माओं ने हमसे हृदयहीन प्रतिशोध ले लिए। रोग-शोक, दुख-परिताप, विछोह ये सब दुष्टात्माएँ ही तो थीं! किन्तु, जाने से पहले वे मुझे एक गुरुमन्त्र अवश्य थमा गए। मैं विवाह के बाद, पहली बार मायके आई। मेरी उन्हें बड़ी चिन्ता थी। कहते थे, “तूने तो बस घुड़सवारी ही सीखी है...क्या करेगी ससुराल में?"
विवाह से पूर्व मैं सचमुच ही गृहकार्य में शून्य थी। शायद ही कभी पानी का गिलास भी स्वयं उठाकर पिया हो! विवाह हुआ ऐसे कट्टर सनातनी परिवार में, जिन्हें नौकरी की छाया से भी परहेज था। उस पर मेरा सबसे बड़ा अपराध था कि मैं उच्चशिक्षा प्राप्त अपने ससुराल की पहली पढ़ी-लिखी बहू थी। कभी छाता भी लगाकर कहीं चली जाती तो अन्तःपुर से छूटे विषबुझे बाण मुझे बींध डालते। अपने प्रगतिशील मायके से वहाँ आने पर मुझे उस गहरे सांस्कृतिक आघात ने गहन नैराश्य में डुबो दिया था।
पहली बार मायके आई तो माँ से सबकुछ छिपा ले गई, पर लोहनीजी ने एकान्त में पूछा, “क्यों, कैसी बीत रही है?"
मैं उत्तर नहीं दे पाई। अब तक यत्न से छिपाई गई वेदना, शतसहस्र धाराओं में फूट पड़ी। तीसरे ही दिन मुझसे चक्की में उड़द की दाल दलवाई गई। बीसियों सीढ़ियों में लक्ष्मीजी के पैर बनवाए गए। परात भर आटा गुंधवाया, उस पर गजब की छुआछूत। एकवस्त्रा बनकर खाना बनाओ। उस पर भी बड़े घर की बेटी होने का दिन-रात ताना सुनो!
मैं बुरी तरह सिसकने लगी थी। जानती थी, अब चाबुक पड़ेगा :
“कहता था ना घर का काम सीख, तब तो बड़ी माख लगती थी। भोगो।"
पर वे एक शब्द नहीं बोले। चुपचाप सुनते रहे। फिर मेरे सिर पर उन्होंने बड़े स्नेह से हाथ फेरा, “रो मत। तुझे पति तो देवता मिला है ना? धीरे-धीरे ये छोटे-मोटे बादल खुद उँट जायेंगे। पहाड़ी डोट्यालों को देखा है ना? (पहाड़ी कुली जो अपनी ईमानदारी एवं दुर्वह बोझा ढोने के लिए कभी प्रख्यात थे) उनसे सीख! जब उनकी पीठ पर तीन-तीन मन का बोझ लाद दिया जाता है, तो जानलेवा चढ़ाई, बिना यूँ-चपड़ किए कैसे झेल लेते हैं, जानती है? उस बोझ पर स्वयं मन-भर का पत्थर लाद लेते हैं। आधी चढ़ाई चढ़ फिर खुद लादे गये उस पत्थर को दूर भनका देते हैं-पीठ का बोझा अचानक फूल-सा हलका लगने लगता है। और फिर देखते-ही-देखते रही-सही चढ़ाई वे पल भर में पार कर लेते हैं। वे कभी एक सीध में नहीं चलते, कभी दाएँ और कभी बाएँ यानी उबाऊ दिनचर्या में पल-पल खुद बदलाव ले आते हैं, वही सीख समझी। बोझ कभी भारी बोझ नहीं लगेगा।" जीवन के दुर्वह बोझ पर स्वयं लादा गया भारी पत्थर तो अब कब का भनकाकर दूर फेंक चुकी हूँ। पीठ का बोझ स्वयं ही फूल-सा हलका लगने लगा है। जीवन की एकरसता की तीखी चढ़ाई में, दायें-बायें चलने का प्रयास भी व्यर्थ नहीं गया। आधी से अधिक चढ़ाई तो पार कर ही ली है। लोहनीजी का दिया गया गुरुमन्त्र रही-सही चढ़ाई भी पार करा ही देगा। किन्तु, कभी-कभी अतीत पीछे खींचता अवश्य है :
लोहनीजी केवल भूत-प्रेतों की ही कहानियाँ सुनाया करते थे। उनके शब्दों में वे कहानियाँ उनके भोगे हुए यथार्थ की कहानियाँ थीं।
“साली-हरामजादी चुडैलों को हम जाने क्यों पसन्द हैं! हमें देखते ही पीपल के पेड़ से टपटप टपकने लगती हैं, पर मजाल है जो आज तक हमें एक भी छू पाई हो!"
उनकी एक अत्यन्त प्रिय कहानी थी 'जागो हो, मैं लै उणयूँ' (रुक जाओ जी, मैं भी आ रहा हूँ)। कैसे वे घर से छुट्टियों के बाद अपने गाँव सतराली से, अँधेरे में उल्टी घड़ी देख, आधी रात ही को चल पड़े थे और पीछे-पीछे लग गया था मसान का खबीस। चलते-चलते घंटों बीत गये, पर रात नहीं बीती। अँधेरे घने जंगल से गुजर रहे थे तब वह नक्की स्वर गूंजा, “जागो हो...मैं लै उणयूँ।"
लोहनीजी समझ गए, वह कौन है। पर प्रेतबाधा का एक-एक कीलक अर्गला तो वे साथ लिए चलते थे, न हुंकारा दिया, न पीछे मुड़कर देखा, पर वह हरामी क्यों चूकता? मुस्टंडा, कभी बैल बनकर सींग घुमाता, कभी अग्निपुंज बनकर 'फ्वाँ फ्वाँ' करता! कभी नक्की स्वर में कहता। 'जागो हो!'
लोहनीजी स्वयं उसकी नक्की स्वर में वह हाँक दुहराते तो हम डरकर उनके पास सरक आते, “बस लोहनीजी, बस! अब कल सुनेंगे!"
वे हँसकर हमें पास खींच लेते, “अरे पगली, जब तक वह पुरुषोत्तम है ना, इस घर में मजाल है जो कोई दुष्टात्मा कदम तो धर ले!"
लेकिन उनके जाते ही, न जाने कितनी अशरीरी आत्माओं ने हमसे हृदयहीन प्रतिशोध ले लिए। रोग-शोक, दुख-परिताप, विछोह ये सब दुष्टात्माएँ ही तो थीं! किन्तु, जाने से पहले वे मुझे एक गुरुमन्त्र अवश्य थमा गए। मैं विवाह के बाद, पहली बार मायके आई। मेरी उन्हें बड़ी चिन्ता थी। कहते थे, “तूने तो बस घुड़सवारी ही सीखी है...क्या करेगी ससुराल में?"
विवाह से पूर्व मैं सचमुच ही गृहकार्य में शून्य थी। शायद ही कभी पानी का गिलास भी स्वयं उठाकर पिया हो! विवाह हुआ ऐसे कट्टर सनातनी परिवार में, जिन्हें नौकरी की छाया से भी परहेज था। उस पर मेरा सबसे बड़ा अपराध था कि मैं उच्चशिक्षा प्राप्त अपने ससुराल की पहली पढ़ी-लिखी बहू थी। कभी छाता भी लगाकर कहीं चली जाती तो अन्तःपुर से छूटे विषबुझे बाण मुझे बींध डालते। अपने प्रगतिशील मायके से वहाँ आने पर मुझे उस गहरे सांस्कृतिक आघात ने गहन नैराश्य में डुबो दिया था।
पहली बार मायके आई तो माँ से सबकुछ छिपा ले गई, पर लोहनीजी ने एकान्त में पूछा, “क्यों, कैसी बीत रही है?"
मैं उत्तर नहीं दे पाई। अब तक यत्न से छिपाई गई वेदना, शतसहस्र धाराओं में फूट पड़ी। तीसरे ही दिन मुझसे चक्की में उड़द की दाल दलवाई गई। बीसियों सीढ़ियों में लक्ष्मीजी के पैर बनवाए गए। परात भर आटा गुंधवाया, उस पर गजब की छुआछूत। एकवस्त्रा बनकर खाना बनाओ। उस पर भी बड़े घर की बेटी होने का दिन-रात ताना सुनो!
मैं बुरी तरह सिसकने लगी थी। जानती थी, अब चाबुक पड़ेगा :
“कहता था ना घर का काम सीख, तब तो बड़ी माख लगती थी। भोगो।"
पर वे एक शब्द नहीं बोले। चुपचाप सुनते रहे। फिर मेरे सिर पर उन्होंने बड़े स्नेह से हाथ फेरा, “रो मत। तुझे पति तो देवता मिला है ना? धीरे-धीरे ये छोटे-मोटे बादल खुद उँट जायेंगे। पहाड़ी डोट्यालों को देखा है ना? (पहाड़ी कुली जो अपनी ईमानदारी एवं दुर्वह बोझा ढोने के लिए कभी प्रख्यात थे) उनसे सीख! जब उनकी पीठ पर तीन-तीन मन का बोझ लाद दिया जाता है, तो जानलेवा चढ़ाई, बिना यूँ-चपड़ किए कैसे झेल लेते हैं, जानती है? उस बोझ पर स्वयं मन-भर का पत्थर लाद लेते हैं। आधी चढ़ाई चढ़ फिर खुद लादे गये उस पत्थर को दूर भनका देते हैं-पीठ का बोझा अचानक फूल-सा हलका लगने लगता है। और फिर देखते-ही-देखते रही-सही चढ़ाई वे पल भर में पार कर लेते हैं। वे कभी एक सीध में नहीं चलते, कभी दाएँ और कभी बाएँ यानी उबाऊ दिनचर्या में पल-पल खुद बदलाव ले आते हैं, वही सीख समझी। बोझ कभी भारी बोझ नहीं लगेगा।" जीवन के दुर्वह बोझ पर स्वयं लादा गया भारी पत्थर तो अब कब का भनकाकर दूर फेंक चुकी हूँ। पीठ का बोझ स्वयं ही फूल-सा हलका लगने लगा है। जीवन की एकरसता की तीखी चढ़ाई में, दायें-बायें चलने का प्रयास भी व्यर्थ नहीं गया। आधी से अधिक चढ़ाई तो पार कर ही ली है। लोहनीजी का दिया गया गुरुमन्त्र रही-सही चढ़ाई भी पार करा ही देगा। किन्तु, कभी-कभी अतीत पीछे खींचता अवश्य है :
बहुदिन परे आपनार घरे
फिरिनू सारिया तीर्थ
आज साथे नाँई
चिरसाथी मोर शेई पुरातन भृत्य
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






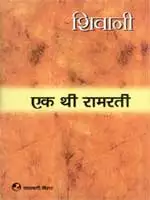


_s.jpg)
