|
नारी विमर्श >> एक थी रामरती एक थी रामरतीशिवानी
|
426 पाठक हैं |
|||||||
शिवानी के मन को छूते हुए संस्मरण
चिरसाथी मोर
प्रकृति की यह एक सुखद देन है कि मनुष्यों को उसने विस्मरणशील बनाया है। भूल
जाना भी एक शक्ति है, किन्तु जैसे-जैसे जीवन की अवनतमुखी सन्ध्या घनीभूत होती
है, वैसे-वैसे अचेतन मन में छिपे अनेक विस्मृत चेहरे प्रकाशपुंज बनकर हमारा
पथ-प्रदर्शन करने लगते हैं। जब आधुनिक युग की आधुनिकतम औषधियाँ, तन एवं मन की
व्याधियों को दूर करने में असमर्थ हो उठती हैं, तब ही दादी-नानी के अचूक
नुस्खों की भाँति उन विस्मृत व्यक्तियों के प्रेरणाप्रद वाक्य हममें नई
स्फूर्ति एवं नई ऊर्जा का संचार सहसा कर उठते हैं। जब कभी जीवन में कोई संकट
आया है, ऐसा संकट, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, जब दैवी वज्रपात ने मेरुदंड
हिलाकर रख दिया, लोहनीजी की बचपन में बार-बार श्रुतिलेख में लिखाई गई वे
पंक्तियाँ स्वयं हाथ थाम लेती थीं :
तुलसी असमय के सखा धीरज धरम विवेक
साहित, साहस, सत्यव्रत रामभरोसे एक
हमें वे नित्य ये ही पंक्तियाँ लिखने को देते और हम कभी झुंझलाकर कहते “आपको
कोई और दोहा-चौपाई नहीं आती क्या?"
आज सोचती हूँ, शायद वे जानबूझकर ही ये पंक्तियाँ बार-बार हमसे लिखवाते थे-कि उस कच्ची वयस में भले ही उन पंक्तियों का गूढार्थ समझने की शक्ति हममें नहीं थी, किन्तु रसरी के 'सिल पर पड़त पिसान' की भाँति वे गाढ़े वक़्त हमारे काम आएँगी। उनका नाम था पुरुषोत्तम और उनका व्यक्तित्व भी उनके नाम को सार्थक करता था। ऊँचा डीलडौल, गोरा रंग, घनी मूंछे, बड़ी-बड़ी लाल डोरीदार आँखें और तीखी नाक के नीचे, पुष्ट मूंछों से ढके पृथुल अधरों पर सामान्य स्मित का भी आभास नहीं। उनका कहना था कि हमारी माँ के विवाह के एक वर्ष पूर्व, हमारे गृह में उनकी नियुक्ति हुई थी, इसी से अम्मा के दादी-नानी बन जाने पर भी वे उनके लिए ‘धुलैंणी ज्यू' (दुलहनजी) ही बनी रहीं। आए थे हमारे अटाले का भार सँभालने, पर कुछ ही वर्षों में, हमारे गृह के सब ही महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनकी मुट्ठी में स्वयं सरक गए। खाना बनाने का भार उन्होंने अपने छोटे भाई देवीदत्त को सौंप दिया था। वे स्वयं अनायास ही हमारे उस गृह के सचिव, वित्त सचिव एवं सूचना प्रसारण सचिव के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे-जहाँ आए दिन महिमामय अतिथिगण, छप्पर फाड़कर टपकते रहते थे-मदनमोहन मालवीय, स्वामी नित्यानन्द, सर गिरजाशंकर, सर सुल्तान अहमद, डॉ. अंसारी, पहलवान राममूर्ति, विभिन्न रियासतों के राजकुमार, जिनमें दतिया के महाराजकुमार 'बुलबुल' तो पूरे एक वर्ष तक हमारे गृह के सदस्य बनकर रहे। आतिथ्य निर्वाह का पूरा भार लोहनीजी पर ही छोड़ दिया जाता। उस पर पूजा-पाठ, रुद्र पार्थिव पूजन, जन्मदिन, अशौच निवारण यानी हमारे गह के जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक अनुष्ठान का पौरोहित्य पूरे पचास वर्षों तक उसी विलक्षण व्यक्ति ने सँभाला। उनका स्वयं अपना भरा-पूरा परिवार था-दो पुत्र, एक पुत्री, जामाता और स्वयं उन्हीं के शब्दों में उनकी प्राणप्रिया उनकी 'बामणी', जिनसे मिलने वे वर्ष में एक ही बार जा पाते थे। ऐसे निःस्वार्थ, स्वामिभक्त सेवक की क्या इस युग में हम कल्पना कर सकते हैं!
हम भाई-बहनों में हम चार ही उनके अधिक सान्निध्य में रहे। मेरी सबसे बड़ी बहन चन्दा, जो लोहनीजी के शब्दों में 'शापभ्रष्ट गन्धर्व कन्या थी', उनकी सबसे प्रिय गृहसदस्या थी-“भगवान् की माया देखो, जन्मी तो मैंने ही पहले गोद में लिया, गई तो मेरी ही गोद में सिर रखकर।"
मेरे भाई त्रिभुवन, कुछ अपने भव्य व्यक्तित्व के कारण और कुछ दो पुत्रियों के बाद जन्मे पुत्र होने के नाते, घर-भर की आँखों के तारे थे। लोहनीजी को ‘परखिया' कहकर भी पुकारते, तो वे उसकी अक्खड़ अशिष्टता को हँसकर झेल लेते।
असल में 'लाल्सैप' (लाल साहब)-वे मेरे पिता को इसी नाम से पुकारते थे– “एक ही भूल की, बाद में समझेंगे, जिस लंगूरी कौम के पास इसे पढ़ने भेजा है, वह ऐसी ही तो शिक्षा देगी! अरे, जो दिशा-जंगल भी लोटा लेकर नहीं, कागज लेकर जाते हैं, वह तामसी कौम इसे क्या सिखाएगी? नाम जाते ही बदल दिया है, अब देखो, पूरा संस्कार भ्रष्ट कब करते हैं।"
त्रिभुवन तब नैनीताल में एक स्वतन्त्र बंगले में रह, दो विदेशी गवर्नेस मिस एवं मिसेज ममफर्ड से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्हीं ने उनका नया नाम धरा था 'टिकर' ! छुट्टियों में घर आते तो लोहनीजी का पारा गरम हो जाता, "हद है, अब रोटी भी छुरी-काँटे से खाने लगा है! मेरी मानो धुलैणी ज्यू तो जितनी जल्दी हो सके, इसके गले में जनेऊ डाल दो! वो साली दुर्मुखी मेमों की मूठ फिर इस पर नहीं चल पाएगी।"
और फिर उन्हीं की जिद से बड़ी धूमधाम से त्रिभुवन का यज्ञोपवीत संस्कार ओरछा में सम्पन्न किया गया। वह धूम-गरज क्या किसी शादी-ब्याह से कम थी? टीकाराम पंडितजी काशी से अपने साथ वेदपाठी ब्राह्मणों की पूरी टीम लेकर पधारे थे। सोने-चाँदी की अंबारी से सजा, महाराज बीरसिंह देव जू का हाथी, बिजली की रंगीन जगमगाहट से नई-नवेली दुल्हन-सी सजी हमारी कुंडेश्वर की कोठी! बालबटुक के कान में गायत्री फूंककर लोहनीजी ने कहा था, “आज से तू फिर त्रिभुवन बन गया है, समझा? टिकर नहीं...”
शायद उनकी ही प्रबल इच्छाशक्ति का चमत्कार था कि सहसा हम तीनों भाई-बहनों की शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया गया। हमें पितामह की छत्रछाया में भेज दिया गया। गार्जियन बने लोहनीजी। संस्कृत पढ़ाने आते गंगादत्त शास्त्री। गणित पढ़ाते रघुवरदत्त जोशी, जो तब कुमाऊँ के रामानुजम थे। अंग्रेज़ी पढ़ाते स्वयं पितामह। सुबह पाँच बजे उठना अनिवार्य था। फिर हाथ-मुँह धोकर, लोहनीजी त्रिफला से आँखें धुलवाते और फिर अपने साथ लम्बी सफारी पर पैदल घुमाने ले जाते। लौटते ही लोहे ही कड़ाही में औट रहे दूध से छलकते गिलास थमाकर वे अपनी सुदीर्घ पूजा में जुट जाते। उस अमृतस्वरूपी दूध की बूंट अभी भी जीभ पर धरी है। अल्मोड़े का ‘फालसिमा' ग्राम तब अपनी दूधो नहाई बिरादरी के लिए प्रसिद्ध था। वहीं का ग्वाला नागमल लोहनीजी से थरथर काँपता था। मजाल, जो कभी एक बूंद पानी मिलाने की धृष्टता कर सके!
“देख रे नागमलिया, कभी बूंद-भर पानी मिलाया साले, तो हम ब्रह्मतेज से तुझे भस्म कर देंगे..."
“कैसी बातें करते हो गुरु, पानी और इस घर के दूध में? ऐसा जिस दिन करूँ, गोहत्या का पाप लगे मुझे-राम-राम!"
एक नागमल ही नहीं, घर-भर के नौकर, नौकरानियाँ, बाजार के दुकानदार, फेरीवाले उनके ब्रह्मतेज से थरथर काँपते थे। सब जानते थे कि वे प्रसिद्ध संत नारद बाबा के साथ रहे हैं और दिवंगत बाबा का अदृश्य साया उनके साथ निरन्तर चलता रहता है। उनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता।
तब अल्मोड़ा में बहू-बेटियों के बाजार जाने पर कठोर प्रतिबन्ध था। वर्ष में केवल दो बार हमें जाने की अनमति मिलती-एक नन्दादेवी के डोले पर और दूसरी दीवाली पर। वह भी हमें पितामह के उतने ही कट्टर मित्र बद्रीलाल साहजी की नक्काशीदार अटारी से ही झाँकने-भर की। किन्तु मैं वयस में छोटी थी, इसी से लोहनीजी प्रायः ही मुझे अपने साथ ले जाते, किन्तु उनके हाट-पर्व का आरम्भ एवं अन्त होता उनके परम प्रिय मित्र सुन्दरलाल साह की दुकान पर। गत वर्ष लगभग चालीस वर्ष पश्चात् उस चिरपरिचित दुकान को देखा, तो दंग रह गई। इतने दीर्घ अन्तराल में भी न दुकान बदली है, न दुकानदार! सुन्दरलाल साह का वही चिकना-चुपड़ा गोरा चेहरा और ललाट पर वैसी ही चन्दन की बिन्दी! तब लोहनीजी को देखते ही उनका चेहरा खिल उठता था, “आओ, आओ गुरु! कहो, क्या खबर है ताजा?"
वयस में पर्याप्त अन्तर होने पर भी उनकी बातों का जैसे अन्त ही नहीं होता। मैं बुरी तरह ऊब उठती। एक तो परचून की दुकान, जम्बू, गन्फ्रेणी जैसे तीव्र पहाड़ी मसालों की सिर चकरानेवाली खुशबू, उस पर दोनों मित्रों की अशेष बतकही--मुझे चुप कराने साहजी कभी दाडिमाष्टक की पुड़िया थमा देते, कभी स्वादिष्ट काली, सफ़ेद धारीदार 'वुल्स आई', जिसे खाना और बनाना शायद अब लोग एकदम ही भूल गए हैं। पर फिर भी मैं कुनमुनाने लगती-“चलो ना, लोहनीजी बाजार..."
आज सोचती हूँ, शायद वे जानबूझकर ही ये पंक्तियाँ बार-बार हमसे लिखवाते थे-कि उस कच्ची वयस में भले ही उन पंक्तियों का गूढार्थ समझने की शक्ति हममें नहीं थी, किन्तु रसरी के 'सिल पर पड़त पिसान' की भाँति वे गाढ़े वक़्त हमारे काम आएँगी। उनका नाम था पुरुषोत्तम और उनका व्यक्तित्व भी उनके नाम को सार्थक करता था। ऊँचा डीलडौल, गोरा रंग, घनी मूंछे, बड़ी-बड़ी लाल डोरीदार आँखें और तीखी नाक के नीचे, पुष्ट मूंछों से ढके पृथुल अधरों पर सामान्य स्मित का भी आभास नहीं। उनका कहना था कि हमारी माँ के विवाह के एक वर्ष पूर्व, हमारे गृह में उनकी नियुक्ति हुई थी, इसी से अम्मा के दादी-नानी बन जाने पर भी वे उनके लिए ‘धुलैंणी ज्यू' (दुलहनजी) ही बनी रहीं। आए थे हमारे अटाले का भार सँभालने, पर कुछ ही वर्षों में, हमारे गृह के सब ही महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनकी मुट्ठी में स्वयं सरक गए। खाना बनाने का भार उन्होंने अपने छोटे भाई देवीदत्त को सौंप दिया था। वे स्वयं अनायास ही हमारे उस गृह के सचिव, वित्त सचिव एवं सूचना प्रसारण सचिव के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे-जहाँ आए दिन महिमामय अतिथिगण, छप्पर फाड़कर टपकते रहते थे-मदनमोहन मालवीय, स्वामी नित्यानन्द, सर गिरजाशंकर, सर सुल्तान अहमद, डॉ. अंसारी, पहलवान राममूर्ति, विभिन्न रियासतों के राजकुमार, जिनमें दतिया के महाराजकुमार 'बुलबुल' तो पूरे एक वर्ष तक हमारे गृह के सदस्य बनकर रहे। आतिथ्य निर्वाह का पूरा भार लोहनीजी पर ही छोड़ दिया जाता। उस पर पूजा-पाठ, रुद्र पार्थिव पूजन, जन्मदिन, अशौच निवारण यानी हमारे गह के जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक अनुष्ठान का पौरोहित्य पूरे पचास वर्षों तक उसी विलक्षण व्यक्ति ने सँभाला। उनका स्वयं अपना भरा-पूरा परिवार था-दो पुत्र, एक पुत्री, जामाता और स्वयं उन्हीं के शब्दों में उनकी प्राणप्रिया उनकी 'बामणी', जिनसे मिलने वे वर्ष में एक ही बार जा पाते थे। ऐसे निःस्वार्थ, स्वामिभक्त सेवक की क्या इस युग में हम कल्पना कर सकते हैं!
हम भाई-बहनों में हम चार ही उनके अधिक सान्निध्य में रहे। मेरी सबसे बड़ी बहन चन्दा, जो लोहनीजी के शब्दों में 'शापभ्रष्ट गन्धर्व कन्या थी', उनकी सबसे प्रिय गृहसदस्या थी-“भगवान् की माया देखो, जन्मी तो मैंने ही पहले गोद में लिया, गई तो मेरी ही गोद में सिर रखकर।"
मेरे भाई त्रिभुवन, कुछ अपने भव्य व्यक्तित्व के कारण और कुछ दो पुत्रियों के बाद जन्मे पुत्र होने के नाते, घर-भर की आँखों के तारे थे। लोहनीजी को ‘परखिया' कहकर भी पुकारते, तो वे उसकी अक्खड़ अशिष्टता को हँसकर झेल लेते।
असल में 'लाल्सैप' (लाल साहब)-वे मेरे पिता को इसी नाम से पुकारते थे– “एक ही भूल की, बाद में समझेंगे, जिस लंगूरी कौम के पास इसे पढ़ने भेजा है, वह ऐसी ही तो शिक्षा देगी! अरे, जो दिशा-जंगल भी लोटा लेकर नहीं, कागज लेकर जाते हैं, वह तामसी कौम इसे क्या सिखाएगी? नाम जाते ही बदल दिया है, अब देखो, पूरा संस्कार भ्रष्ट कब करते हैं।"
त्रिभुवन तब नैनीताल में एक स्वतन्त्र बंगले में रह, दो विदेशी गवर्नेस मिस एवं मिसेज ममफर्ड से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्हीं ने उनका नया नाम धरा था 'टिकर' ! छुट्टियों में घर आते तो लोहनीजी का पारा गरम हो जाता, "हद है, अब रोटी भी छुरी-काँटे से खाने लगा है! मेरी मानो धुलैणी ज्यू तो जितनी जल्दी हो सके, इसके गले में जनेऊ डाल दो! वो साली दुर्मुखी मेमों की मूठ फिर इस पर नहीं चल पाएगी।"
और फिर उन्हीं की जिद से बड़ी धूमधाम से त्रिभुवन का यज्ञोपवीत संस्कार ओरछा में सम्पन्न किया गया। वह धूम-गरज क्या किसी शादी-ब्याह से कम थी? टीकाराम पंडितजी काशी से अपने साथ वेदपाठी ब्राह्मणों की पूरी टीम लेकर पधारे थे। सोने-चाँदी की अंबारी से सजा, महाराज बीरसिंह देव जू का हाथी, बिजली की रंगीन जगमगाहट से नई-नवेली दुल्हन-सी सजी हमारी कुंडेश्वर की कोठी! बालबटुक के कान में गायत्री फूंककर लोहनीजी ने कहा था, “आज से तू फिर त्रिभुवन बन गया है, समझा? टिकर नहीं...”
शायद उनकी ही प्रबल इच्छाशक्ति का चमत्कार था कि सहसा हम तीनों भाई-बहनों की शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया गया। हमें पितामह की छत्रछाया में भेज दिया गया। गार्जियन बने लोहनीजी। संस्कृत पढ़ाने आते गंगादत्त शास्त्री। गणित पढ़ाते रघुवरदत्त जोशी, जो तब कुमाऊँ के रामानुजम थे। अंग्रेज़ी पढ़ाते स्वयं पितामह। सुबह पाँच बजे उठना अनिवार्य था। फिर हाथ-मुँह धोकर, लोहनीजी त्रिफला से आँखें धुलवाते और फिर अपने साथ लम्बी सफारी पर पैदल घुमाने ले जाते। लौटते ही लोहे ही कड़ाही में औट रहे दूध से छलकते गिलास थमाकर वे अपनी सुदीर्घ पूजा में जुट जाते। उस अमृतस्वरूपी दूध की बूंट अभी भी जीभ पर धरी है। अल्मोड़े का ‘फालसिमा' ग्राम तब अपनी दूधो नहाई बिरादरी के लिए प्रसिद्ध था। वहीं का ग्वाला नागमल लोहनीजी से थरथर काँपता था। मजाल, जो कभी एक बूंद पानी मिलाने की धृष्टता कर सके!
“देख रे नागमलिया, कभी बूंद-भर पानी मिलाया साले, तो हम ब्रह्मतेज से तुझे भस्म कर देंगे..."
“कैसी बातें करते हो गुरु, पानी और इस घर के दूध में? ऐसा जिस दिन करूँ, गोहत्या का पाप लगे मुझे-राम-राम!"
एक नागमल ही नहीं, घर-भर के नौकर, नौकरानियाँ, बाजार के दुकानदार, फेरीवाले उनके ब्रह्मतेज से थरथर काँपते थे। सब जानते थे कि वे प्रसिद्ध संत नारद बाबा के साथ रहे हैं और दिवंगत बाबा का अदृश्य साया उनके साथ निरन्तर चलता रहता है। उनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता।
तब अल्मोड़ा में बहू-बेटियों के बाजार जाने पर कठोर प्रतिबन्ध था। वर्ष में केवल दो बार हमें जाने की अनमति मिलती-एक नन्दादेवी के डोले पर और दूसरी दीवाली पर। वह भी हमें पितामह के उतने ही कट्टर मित्र बद्रीलाल साहजी की नक्काशीदार अटारी से ही झाँकने-भर की। किन्तु मैं वयस में छोटी थी, इसी से लोहनीजी प्रायः ही मुझे अपने साथ ले जाते, किन्तु उनके हाट-पर्व का आरम्भ एवं अन्त होता उनके परम प्रिय मित्र सुन्दरलाल साह की दुकान पर। गत वर्ष लगभग चालीस वर्ष पश्चात् उस चिरपरिचित दुकान को देखा, तो दंग रह गई। इतने दीर्घ अन्तराल में भी न दुकान बदली है, न दुकानदार! सुन्दरलाल साह का वही चिकना-चुपड़ा गोरा चेहरा और ललाट पर वैसी ही चन्दन की बिन्दी! तब लोहनीजी को देखते ही उनका चेहरा खिल उठता था, “आओ, आओ गुरु! कहो, क्या खबर है ताजा?"
वयस में पर्याप्त अन्तर होने पर भी उनकी बातों का जैसे अन्त ही नहीं होता। मैं बुरी तरह ऊब उठती। एक तो परचून की दुकान, जम्बू, गन्फ्रेणी जैसे तीव्र पहाड़ी मसालों की सिर चकरानेवाली खुशबू, उस पर दोनों मित्रों की अशेष बतकही--मुझे चुप कराने साहजी कभी दाडिमाष्टक की पुड़िया थमा देते, कभी स्वादिष्ट काली, सफ़ेद धारीदार 'वुल्स आई', जिसे खाना और बनाना शायद अब लोग एकदम ही भूल गए हैं। पर फिर भी मैं कुनमुनाने लगती-“चलो ना, लोहनीजी बाजार..."
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






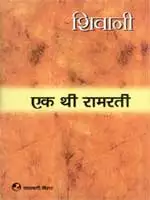


_s.jpg)
