|
नारी विमर्श >> भैरवी (अजिल्द) भैरवी (अजिल्द)शिवानी
|
358 पाठक हैं |
|||||||
पति-व्रता स्त्री के जीवन पर आधारित उपन्यास
"मन ना रांगाए
कापड़ रांगाले
की भूल कोरीले जोगी!"
(हाय रे जोगी, मन नहीं रँगा, पर कपड़े रँगाकर तू कैसी भूल कर बैठा!) किसी
अधेड़ बाईजी का-सा ही मांसल रूप से भरभराता कंठ था माया दी का! उस पर हाव-भाव
कटाक्ष से सँवारकर प्रस्तुत किए जा रहे गीत का अर्थ न समझने पर भी चन्दन उसके
बुभुक्षित प्राणों के कुत्सित आह्वान को खूब समझ गई। कौन कहेगा, यह
अरण्यवासिनी तापसी है! किस नशे ने झुका दिया है इन्हें ऐसे?
यह क्या चिलम का धुआँ है, या स्वयं प्रकृति की सुँघाई गई चिलम का नशा?
किन-किन अतृप्त वासनाओं के दग्ध अंगारे इस मत्त मयूरी को उछल-उछलकर बेढंगा
नाच करते रहने पर मजबूर किए दे रहे थे?
थाक माया दी, और नैकामी करते हौबे ना!' (रहने दो माया दी, अब और नखरे मत
दिखाओ)-चरन की यह डपट सुनकर माया दी सहम गईं। चरन ने उन्हें उठाकर खटिया पर
डाल दिया और मुँह तक चादर खींच दी।
"नहीं, नहीं, चरन! मेरी दुलारी प्यारी चरन! बस एक दम और दिला दे!" माया दी
गिड़गिड़ाने लगीं और हँसती चरन चिलम को कभी ऊँचा उठाती, कभी नीचे झुकाती माया
दी को ऐसे चिढ़ाने लगी, जैसे कोई क्रीड़ा-प्रेमी स्वामी पालतू कुत्ते को
हड्डी से लुभा रहा हो।
"अच्छा लो, बस एक ही कश खींचना, समझीं? अभी मैं हूँ, नई भैरवी है!" सन्त
सौम्य बालिका-सी ‘हाँ-हाँ,' कहती माया दी एक लम्बा लोभी कश खींचकर जैसे अचेत
हो गईं।
फिर उसी चिलम की सदय धूम्ररेखा चन्दन को सचमुच ही चेतना-जगत से बहुत ऊँचा
उड़ाती महीनों से बिछुड़े आत्मीय स्वजनों के बीच उठा ले गई। स्मृतियों के
सागर का ज्वार-भाटा, कभी उसे उठाकर पटक देता धारचूला, कभी दिल्ली और कभी
शाहजहाँपुर। पहले-पहले हँसकर खिल्ली उड़ाने लगा, चाची का स्याह चेहरा...।
“वाह, ठीक ही कहा था मैंने, अपनी माँ की काठी पर मत जाना, लड़की! पर वही किया
तूने।"
इस चाची ने विवाह के ठीक तीन दिन पहले उसको कितना रुलाया था। रात-रात भर रजाई
में मुँह छिपाकर रोई थी वह। हाय, अम्माँ ने इस कलमुँही चाची को क्यों न्यौता
होगा! पर अम्माँ भी भला क्या करतीं? लाख हो, थी तो सगी चाची, उसे भला कैसे
नहीं न्यौततीं, वैसे चतुरा अम्माँ ने चिट्ठी ऐसे कौशल से लिखी थी कि हवाई
जहाज से उड़कर आतीं तब भी शायद चाची नहीं पहुँच पातीं, पर उन्हें जाने कहाँ
से खबर लग गई!
“अरी, तूने नहीं बुलाया तो क्या हुआ!" उन्होंने अम्माँ को खूब खरी-खरी
सुनाकर, काल्पनिक अश्रुजल पोंछ, अपनी भौंडी मोटी नाक आँचल से निचोड़कर रख दी
थी, “आखिर अपना खून ही तो जोर मारता है-जैसे ही मैंने सुना, इधर-उधर से
धेला-टका कर्ज लिया और बगटुट भागी।"
तीसरे दिन अम्माँ बाजार करने गईं तो झट चाची उसे छत पर खींच ले गईं, “और क्या
मैं झूठ कहती हूँ!" वह अपनी बिल्ली की-सी कंजी आँखों को काँच की गोलियों-सा
चमकाती उससे कहती जाती थीं, "मैं तो तुझसे कहती भी नहीं, पर सोचा, पराए घर जा
रही है, वह भी ऐसे घर, जहाँ की जूतियों की धूल की भी बराबरी न तू कर सकती है,
न तेरी अम्माँ। अब उस घर की इज्जत रखियो, बिट्टी! कहीं अपनी माँ की काठी पर
मत जइयो!"
और फिर आरम्भ हुआ माँ की कलंक-गाथा का गुटका संस्करण। बीच-बीच में अपनी जबान
के सलोने छौंक लगाती, चाची आवश्यकतानुसार अश्रुजलविसर्जन भी करती चली जा रहीं
थीं-कभी उसके मृत पिता के लिए, कभी नाना के दारुण दुःख के लिए।
"वह तो हमारे जेठजी की दरियादिली थी, जो ब्राह्मण के घर की बिटिया को उबार
लिया, नहीं तो क्या कोई जान-बूझकर मक्खी निगलता है। तेरे नाना बेचारे! कहते
हैं, उन्होंने काली में कूदकर ही जान दे दी। वही हाल तेरी नानी का हुआ।
बदनामी ने क्या उन्हें अपने समाज में कहीं मुँह दिखाने लायक रखा था!"
रात-भर चन्दन रोती रही थी। उसकी शान्त सरल अम्माँ का निरीह चेहरा, उसके
सम्मुख मुस्कुराने लगता। नहीं, उसकी माँ ऐसी कभी नहीं हो सकती। यह निश्चय ही
उसकी ईर्ष्यालु चाची के मन की भड़ास रही होगी। काल्पनिक बतकही का अनावश्यक
जाल फैलाकर वह उसे फाँसने आई थी, जिससे सुख की पेंगों में झूलती भाग्यवती
भतीजी को जमीन पर घसीटकर रुला सके। चाची सधवा होकर भी जेठ-जेठानी पर आश्रिता
थी। उसके अकर्मण्य चाचा, जीवन-भर ताऊ के गृहद्वार के चौकीदार ही बने रहे। कभी
उनके बच्चों को स्कूल पहुँचाते, कभी बाजार से सौदा लाते, कभी भाई के परिवार
को पहाड़ पहुँचाते, और कभी उनकी अनुपस्थिति में उनके घर की रखवाली करते। उधर
उसकी अम्माँ, विधवा होने पर भी, अपने ही साहस से अपने पैरों पर खड़ी थीं।
वैधव्यरिपु को उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर धकेला था। सम्पूर्ण रूप से पराजित
और धराशायी कर दिया। एम. ए., एल. टी. कर अब वह प्रधानाध्यापिका थीं। रहने को
सरकारी बँगला था। एक दर्जन अध्यापिकाएँ उनके रोब से दिन-रात थर-थर काँपती
रहती थीं। नौकर-चपरासी थे। सुन्दर सौम्य पुत्री थी और ईश्वर की कृपा से अब
उसी को इतने बड़े समृद्ध गृह का राजपुत्र, स्वयं माँगकर अपनी हथेली पर बिठाने
के लिए ले जा रहा था।
|
|||||


 i
i 






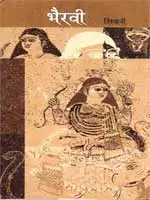


_s.jpg)
