|
लेख-निबंध >> न्याय का संघर्ष न्याय का संघर्षयशपाल
|
198 पाठक हैं |
|||||||
यशपाल के अठारह लेखों का संकलन
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
न्याय की धारणा और समाज की व्यवस्था के समान रुखे विषय की विवेचना को भी
रंजक बना देना इन लेखों की सार्थकता है। भाषा प्रवाह के रूप तैरते हुए
विद्रूप का अभिप्राय रुखे और गम्भीर विषय को रोचक बना देना ही है। इन
लेखों को पढ़-कर आपके होठों पर जो मुस्कराहट आयेगी वह आत्म-विस्मृति और
आनन्दोल्लास की न होकर क्षोभ, परिताप और करुणा की होगी।
इन लेखों में लेखक ने आत्म-विस्मृत समाज को कलम की नोक से गुदगुदा कर जाने जगाने की चेष्टा की है और समाज को करवट बदलते न देखकर कई जगह उसने कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है।
इन लेखों में लेखक ने आत्म-विस्मृत समाज को कलम की नोक से गुदगुदा कर जाने जगाने की चेष्टा की है और समाज को करवट बदलते न देखकर कई जगह उसने कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है।
भूमिका
मनुष्य-समाज की आयु और ज्ञान बढ़े और उसकी आवश्यकतायें बढ़ने लगीं। इन
आवश्यकताओं के बढ़ने और बदलने के साथ ही समाज के क्रम में भी परिवर्तन आता
रहा है। मनुष्य-समाज के जीवन को किसी क्रम-विशेष या व्यवस्था के अनुसार
संचालित करने के लिये जो परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं उनमें समाज का अपना
अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण है। समाज के संचित अनुभवों के आधार पर खड़ा
किया गया तर्क और कल्पना ही हमारा समाज-शास्त्र है। समाज शास्त्र का
उद्दे्श्य समाज की रक्षा और विकास है।
जब समाज के विकास का मार्ग आगे बन्द होने लगता है तब समाज का शास्त्र गूढ़ चिन्तन और मनन द्वारा अपनी रक्षा के लिये नया कार्यक्रम बनाने के लिये बाधित होता है। बाधिक होकर समाज द्वारा नये कार्यक्रम का तैयार किया जाना ही समाज में विचारों की क्रान्ति है।
समाज की जीर्ण अवस्था में परिवर्तन होने से पूर्व विचारों में क्रान्ति आवश्यक और प्राकृतिक क्रम है। सामाजिक क्रान्ति के मध्याह्न के लिये विचारों की क्रान्ति उषा के समान है। हमारा समाज अपनी पुरानी व्यवस्था के शिकंजे में छटपटा रहा है और नवीन व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। यह विचारों की क्रान्ति का लक्षण है। दूसरे शब्दों में कहना होगा कि हम विचारों की क्रान्ति के युग से गुजर रहे हैं।
‘न्याय’ की धारणा मनुष्य-समाज को क्रम और नियंत्रण में रखने वाली आन्तरिक श्रृंखला है। समाज समाज की प्रत्येक व्यवस्था और क्रम अपनी एक न्याय की धारणा रखता है। यह धारणा उस सामाजिक व्यवस्था को पूर्णता के लक्ष्य और आदर्श की ओर संकेत करती रहती है। विचारों की क्रान्ति का काम हमारी न्याय की धारणा को मार्ग पर लाना है।
इस पुस्तक में हमारी नवीन परिस्थितियों के लये अनुपयुक्त और जर्जर न्याय की धारणा का विश्लेषण (Vivisection) किया गया है। इस विश्लेषण में हमारी वर्तमान न्याय की धारणा में कदम-कदम पर मौजूद विरोधाभास प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था और क्रम की ओर हमारा ध्यान जाता है।
न्याय की धारणा और समाज की व्यवस्था के समान रूखे विषय की विवेचना को भी रोचक और मनोरंजक बना देना इन लेखों की सार्थकता है। भाषा प्रवाह के ऊपर तैरते हुए विद्रूप की तह में सिद्धान्तों की शिलायें मौजूद हैं। मनोरंजन और विद्रूप का अभियप्राय रूखे और गम्भीर विषय को रोचक बना देना ही है। इन लेखों को पढ़कर आपके होंठों पर जो मुस्कराहट आयेगी वह आत्म-विस्मृत और आनन्दोल्लास की न होकर क्षोभ परिताप और करुणा की होगी।
इन लेखों में लेखक ने आत्म-विस्मृत समाज को कलम की नोक से गुदगुदाकर जगाने की चेष्टा की है और समाज को करवट बदलते न देखकर कई जगह कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है।
जब समाज के विकास का मार्ग आगे बन्द होने लगता है तब समाज का शास्त्र गूढ़ चिन्तन और मनन द्वारा अपनी रक्षा के लिये नया कार्यक्रम बनाने के लिये बाधित होता है। बाधिक होकर समाज द्वारा नये कार्यक्रम का तैयार किया जाना ही समाज में विचारों की क्रान्ति है।
समाज की जीर्ण अवस्था में परिवर्तन होने से पूर्व विचारों में क्रान्ति आवश्यक और प्राकृतिक क्रम है। सामाजिक क्रान्ति के मध्याह्न के लिये विचारों की क्रान्ति उषा के समान है। हमारा समाज अपनी पुरानी व्यवस्था के शिकंजे में छटपटा रहा है और नवीन व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। यह विचारों की क्रान्ति का लक्षण है। दूसरे शब्दों में कहना होगा कि हम विचारों की क्रान्ति के युग से गुजर रहे हैं।
‘न्याय’ की धारणा मनुष्य-समाज को क्रम और नियंत्रण में रखने वाली आन्तरिक श्रृंखला है। समाज समाज की प्रत्येक व्यवस्था और क्रम अपनी एक न्याय की धारणा रखता है। यह धारणा उस सामाजिक व्यवस्था को पूर्णता के लक्ष्य और आदर्श की ओर संकेत करती रहती है। विचारों की क्रान्ति का काम हमारी न्याय की धारणा को मार्ग पर लाना है।
इस पुस्तक में हमारी नवीन परिस्थितियों के लये अनुपयुक्त और जर्जर न्याय की धारणा का विश्लेषण (Vivisection) किया गया है। इस विश्लेषण में हमारी वर्तमान न्याय की धारणा में कदम-कदम पर मौजूद विरोधाभास प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था और क्रम की ओर हमारा ध्यान जाता है।
न्याय की धारणा और समाज की व्यवस्था के समान रूखे विषय की विवेचना को भी रोचक और मनोरंजक बना देना इन लेखों की सार्थकता है। भाषा प्रवाह के ऊपर तैरते हुए विद्रूप की तह में सिद्धान्तों की शिलायें मौजूद हैं। मनोरंजन और विद्रूप का अभियप्राय रूखे और गम्भीर विषय को रोचक बना देना ही है। इन लेखों को पढ़कर आपके होंठों पर जो मुस्कराहट आयेगी वह आत्म-विस्मृत और आनन्दोल्लास की न होकर क्षोभ परिताप और करुणा की होगी।
इन लेखों में लेखक ने आत्म-विस्मृत समाज को कलम की नोक से गुदगुदाकर जगाने की चेष्टा की है और समाज को करवट बदलते न देखकर कई जगह कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है।
नरेन्द्र देव
न्याय का संघर्ष
हम सभी लोग न्याय की दुहाई देते हैं। न्याय के लिये दूसरों का सिर फोड़ने
के लिये तत्पर रहते हैं। हमारे अपने विचार में जो बात न्याय है, उसी के
अनुसार हम दूसरों को चलते देखना चाहते हैं। यदि दूसरे लोग हमारे निर्णय की
अवहेलना करें या हमारा विरोध करें तो न्याय की रक्षा के लिये उनका सिर
फोड़ना जरूरी हो जाता है।
न्याय की धारणा जिस प्रकार हमारे अपने दिमाग़ में, उसी प्रकार दूसरे के दिमाग़ में, हमारे विरोधियों के दिमाग़ में भी होती है। जैसे हम अपने दृष्टिकोण से जो न्याय है उसे लागू करना चाहते हैं, वैसे ही हमारे विरोधी भी अत्यन्त सद्भाव और सदाशय से अपनी समझ के अनुसार न्याय को लागू करना चाहते हैं। जिस समाज की दृष्टि में जो न्याय है, उस समाज को ईश्वर या उसका ईश्वर वैसी ही व्यवस्था स्थापित करने की आज्ञा देता है।
शेरों और भेड़ियों के न्याय के अनुसार यह आवश्यक है कि हिरन और बकरियां सुबह-शाम स्वयं उनके समीप आ जायं और या भेड़िये को देखकर भागें नहीं। हिरन और बकरियों के न्याय के अनुसार शेरों और भेड़ियों को घास के मैदान या पानी पीने की जगह पर नहीं आना चाहिये बल्कि एक ऐसी बिजली गिरनी चाहिये कि शेरों और भेड़ियों का नामोनिशान मिट जाय।
ज़मींदारों की बात कितनी न्यायोचित है। जो लोग उनकी मिल्कियत की ज़मीन को जोते-बायें, उनकी ज़मीन से अन्न-धन पैदा करें, उनको क्या अधिकार है कि सब कुछ स्वयं ले जायं ? जिसकी ज़मीन है उसका अधिकार पैदावार पर होना चाहिये। जिसके पेट से पैदा हुआ, उसी का बच्चा।
किसानों का न्याय कहता है, जिसके हाथ-गोड़ घिसने से ज़मीन से फल पैदा होता है, फल उसी का है। ज़मीन से स्वयं तो कुछ हो नहीं सकता ! फल ज़मीन का नहीं मेहनत का है।
ज़मीन तो किसी की नहीं। ज़मीन को किसने बनाया है ? ज़मीन को घेर कर अधिकार कर लेने से ही मिल्कियत अगर हो जाय तो कोई भी दस आदमियों को मिलाकर, लाठी बांध कर ज़मीन घेर सकता है। इसमें झूठ क्या है ? बाबर ने क्या किया था ? पंजाब के शेर रणजीतसिंह ने क्या किया था ? छत्रपतिशिवाजी ने क्या किया था ? हैदरअली ने क्या किया था ?
ज़माना बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ कोई चाहे तो बहुत सा रुपया लगाकर ज़मीन खरीद सकता है। फौज-फाटे का जोर एक साधन था। रुपया भी एक साधन है, लाठी का जोर भी एक साधन है। फर्ज़ कीजिये सरकार का दिमाग़ फिर जाय, वह ज़मीदारों के हक को जैसे आज स्वीकार करती है, स्वीकार करना छोड़ दे तो ऐसी अवस्था में न्याय बदल जायेगा। किसानों की ही राय न्याय हो जायेगी।1
किसी की सम्पत्ति या मिल्कियत किसी से छीन लेने का दूसरे को क्या अधिकार है ? मालिक उसे चाहे जिस मोल बेच सकता है, यह बिलकुल न्याय अनुमोदित है। इस तरह धनी बन जाने से न ईश्वर ही नाराज़ हो सकता है न यह न्याय के विरुद्ध है, न कचहरी-अदालत को इसमें दखल है।2 कहते हैं-हमारे गाँव के ज़मींदार के दस गाँव थे। फसल में उन्होंने अनाज के कोठे भरे। ईश्वर की इच्छा हुई, आये साल फसलें खराब हो गयीं, अनाज महंगा बिका। मुनाफा हुआ। सेठजी ने दो गाँव और खरीद लिये।
ज़रा आँख खोलकर देखने से मालूम होता है कि मेरा या मेरी श्रेणी का जिस तरह से हित हो, मेरे लिये वही न्याय है। यदि मैं अपनी शक्ति से, चाहे वह शारीरिक हो या दिमाग़ी, अपने हित के लिये काम करने के लिये दूसरों को बाधित कर सकता हूँ तो वही दूसरों के लिये भी न्याय है।
आजकल ज़माना अच्छा है। मनुष्य की शक्ति का अर्क जमा किया जा सकता है। आंख चाहिये देखने के लिये। सेठजी की तिजोरी की तरफ देखिये, उसमें एक लाख रुपये के नोट नहीं; ज्ञानशलाका लगाकर देखिये, तिजोरी में चार लाख आदमी बंद हैं। इन आदमियों की पीठ पर बोझ ढोने की तैयारी है। हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़े और मेहनत के औज़ार हैं। यदि सेठजी की इच्छा हो तो अभी यह स्थूल प्रत्यक्ष रूप धारण कर काम करने लग सकते हैं। सेठजी जो चाहें कर डालें, पृथ्वी के एक भाग को पलट डालें। सेठजी की तिजोरी में शारीरिक बल का अर्क ज़मा है। यह अर्क सेठजी के अपने शरीर का नहीं। जहाँ-तहाँ से बटोरकर दूसरों का बल खरीदकर अर्क जमा किया गया है।
गरमी की रात है, नींद नहीं आती। मेरी जेब में एक अठन्नी है। यदि मैं लोभ न करूं तो आराम से सो सकता हूँ। चवन्नी में एक आदमी का श्रम-बल (आदमी) छिपा है। उसके हाथ में एक पंखा है। वह रात भर मुझे पंखा कर सकता है।
मैं पूछता हूँ, किसके मुँह में हाथ भरकी जुबान है जो कहे कि यह अन्याय है कि मैं सोऊँ और दूसरा मुझ सा ही आदमी रात भर खड़ा-खड़ा पंखा करे क्या उसके जान नहीं ?
मैं पूछता हूँ, क्या मेरे हाथ में चवन्नी नहीं, मैं चवन्नी की मेहनत नहीं लूंगा ? जिसे अठन्नी लेना हो अपना श्रम मेरे लिये खर्च करे।
---------------------------------------------------
1. उपरोक्त लेख 1935 में लिखा गया था। आज की सरकार ज़मींदारी उन्मूलन का कानून बना रही है। परन्तु ज़मींदार को मुआविजा में दण्ड देना न्याय समझती है। सम्भव है कोई ऐसी सरकार होती जो ज़मींदार को उसकी पिछले लूट के मुआविजा में दण्ड देना ही न्याय समझती। (मार्च 1939)
2. यह धारणा भी बदल गई है क्योंकि सरकार व्यापारियों की अन्धेरगर्दी से परेशान होकर चोर-बाजार विरोधी कानून बना चुकी है।
न्याय है शक्ति में। शक्ति के अनेक रूप हैं। सबसे अच्छा रूप शक्ति का है पैसा। यह सम्भाल कर वक्त के लिये रखा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है। इस पैसे में ज़मीन के जोतने-बोने वाले किसान, सुबह से शाम तक आँखें गड़ाकर दिमाग लड़ाने वाला मुंशी, वर्दी पहन कर हुक्म मनवाने वाले सिपाही और तोप-तलवार लेकर आतंक छा देने वाले सैनिक सब निकल सकते हैं। पैसा मनुष्य का, उसकी श्रम-शक्ति का संचित अर्क है। यह है न्याय का आधार !
जिसके पास यह शक्ति है उसी की इच्छा न्याय है। मनुष्य की शक्ति का यह सार कोई अपने ही शरीर से खींचना चाहे तो नहीं खींच सकता, मर जायेगा कमबख्त। हाँ, दूसरों के शरीर से थोड़ा-थोड़ा कर, उनके श्रम को पैसे के रूप में बदल कर अर्क एकत्र किया जा सकता है। जिस अनुपात में किसी व्यक्ति के पास मनुष्य के संचित श्रम का भण्डार है, उसी अनुपात में वह शक्तिशाली है, न्याय का निर्णायक है।
एक ज़माना था जब एक मनुष्य की इच्छा ही न्याय थी। वह राजा कहलाकर जो हुक्म दे देता, वही न्याय था। वह चाहता तो उसका मंत्री हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता, शहर-ग्राम फूंक दिये जाते।
वक्त आया, राजा की स्वेच्छाचारिता अन्याय समझी जाने लगी। सरदारों सामन्तों के हाथ में भी शक्ति आ गई। न्याय में उनकी इच्छा और रात का दखल हो गया। राजा उनकी सम्मिलित शक्ति के आगे दब गया। वे जो चाहते थे, वही कानून होने लगा।
ज़माना पलटा, व्यापार ने ज़ोर पकड़ा। धन का ठेका एकमात्र सरदारों-सामन्तों के हाथों से निकल व्यापारियों, कल-कारखानों के मालिकों के हाथ में पहुँचा। शक्ति आने के साथ उन्हें ही लोग वोट देने लगे। अपने प्रतिनिधियों के जरिये न्याय में उनका भी कुछ-कुछ दखल होने लगा।
ज्यों-ज्यों शासक-समाज की शक्ति क्षीण होने लगती है या उन्हें अपने हाथों से शक्ति निकलने का भय होने लगता है वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये प्रजा के कुछ अंश को अपना साझी बना, उन्हें न्याय में दखल देने का अधिकार बाँटते हैं या प्रजा के किसी अंश के संतोष के लिये न्याय का रूप उन्हें बदलना पड़ता है।
आज भी हमारे देश में न्याय क्या है ? अपने प्रतिनिधियों की मार्फत इसमें दखल देने का अधिकार एक हद तक उन्हीं को है जो लगान या टैक्स देते हैं, जिनके पास कुछ सम्पत्ति है। इन लोगों की राय में न्याय वही है, जिससे इनकी सम्पत्ति की बढ़ती हो, वह अक्षुण्य बनी रहे। सबसे बड़े पूँजीपति ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी शक्ति की रक्षा के लिये छोटे-छोटे पूँजीपतियों को अपने चक्कर में सम्मिलित कर लिया है, परन्तु इन दस प्रतिशत1 के अलावा जो नब्बे प्रतिशत हैं उनके हक में क्या न्याय है, इसकी चिंता किसे है ?’2
-----------------------------------
1. सन् 1935 के शासन के अनुसार वैधानिक सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार कुल दस प्रतिशत भारतवासियों को था।
2. यद्यपि राष्ट्रीय सरकार के हाथ शासन आते ही जनमत के दबाव से विधान परिषद से निर्वाचन में मत देने का अधिकार बालिग उम्र के सभी लोगों को दे दिया है परन्तु यह बात अमल में नहीं जा रही। निर्वाचनों के दिन पर दिन टाला जा रहा है। 1947 से 1950 या 51 में जब तक निर्वाचन न हो जाये, शासन केवल सम्पत्ति-शालियों के प्रतिनिधियों का ही रहेगा।
------------------------------------
स्वर्ग अपने ही मरने से मिलता है। नब्बे प्रतिशत के लिये यदि न्याय की चिन्ता किसी को हो सकती है तो इन नब्बे प्रतिशत को ही होनी चाहिये। जब तक न्याय का निर्णय दस प्रतिशत के हाथ में रहेगा तब तक न्याय की कसौटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिशत के श्रम से दस प्रतिशत का काम चलता रहे। दस प्रतिशत का कल्याण इसी में है कि नब्बे प्रतिशत उन्हें ‘पिता’1 के स्थान पर मानकर ‘पुत्र’ की तरह उनकी आज्ञा-पालन करते रहें। समाज के शरीर के हाथ-पाँव बन समाज के पेट-दस प्रतिशत को भरते रहें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे न्याय, विधान और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, ‘रामराज्य’ में विघ्न डालते हैं। मुश्किल है तो यह कि नब्बे प्रतिशत यह कैसे मान लें कि ईश्वर की आज्ञा नब्बे प्रतिशत को भूखा ही रखने की है।
मनुष्य की संचित शक्ति का एक रूप पूँजी है तो दूसरा रूप ‘संघ शक्ति’ है। नब्बे प्रतिशत के पास यह दूसरी शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में है। अभी तक उन्होंने अपनी इस शक्ति को नहीं पहचाना क्योंकि अब तक ज्यों-त्यों प्राण बच रहे थे। परन्तु अब पूँजी की शक्ति का पंजा इतना कड़ा हो गया कि सांस लेना मुश्किल है। यदि नब्बे प्रतिशत अब भी अपनी इसी शक्ति के आधार पर न्याय न माँगे तभी ताज्जुब है।
न्याय की धारणा में समय-समय पर संघर्ष होता आया है और उसका रूप बदलता रहा है। यदि नब्बे प्रतिशत अपने भाग्य के निर्णय का बोझ स्वयं संभाल कर न्याय के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा। यदि हम पूँजी और संघ की शक्ति की टक्कर देखना नहीं चाहते तो हमारे लिये नब्बे प्रतिशत की शक्ति को स्वीकार कर लेने के सिवा और मार्ग नहीं।
---------------------
1. गाँधीजी कहते हैं-‘ज़मींदार-किसान का सम्बन्ध पिता-पुत्र का है।’
न्याय की धारणा जिस प्रकार हमारे अपने दिमाग़ में, उसी प्रकार दूसरे के दिमाग़ में, हमारे विरोधियों के दिमाग़ में भी होती है। जैसे हम अपने दृष्टिकोण से जो न्याय है उसे लागू करना चाहते हैं, वैसे ही हमारे विरोधी भी अत्यन्त सद्भाव और सदाशय से अपनी समझ के अनुसार न्याय को लागू करना चाहते हैं। जिस समाज की दृष्टि में जो न्याय है, उस समाज को ईश्वर या उसका ईश्वर वैसी ही व्यवस्था स्थापित करने की आज्ञा देता है।
शेरों और भेड़ियों के न्याय के अनुसार यह आवश्यक है कि हिरन और बकरियां सुबह-शाम स्वयं उनके समीप आ जायं और या भेड़िये को देखकर भागें नहीं। हिरन और बकरियों के न्याय के अनुसार शेरों और भेड़ियों को घास के मैदान या पानी पीने की जगह पर नहीं आना चाहिये बल्कि एक ऐसी बिजली गिरनी चाहिये कि शेरों और भेड़ियों का नामोनिशान मिट जाय।
ज़मींदारों की बात कितनी न्यायोचित है। जो लोग उनकी मिल्कियत की ज़मीन को जोते-बायें, उनकी ज़मीन से अन्न-धन पैदा करें, उनको क्या अधिकार है कि सब कुछ स्वयं ले जायं ? जिसकी ज़मीन है उसका अधिकार पैदावार पर होना चाहिये। जिसके पेट से पैदा हुआ, उसी का बच्चा।
किसानों का न्याय कहता है, जिसके हाथ-गोड़ घिसने से ज़मीन से फल पैदा होता है, फल उसी का है। ज़मीन से स्वयं तो कुछ हो नहीं सकता ! फल ज़मीन का नहीं मेहनत का है।
ज़मीन तो किसी की नहीं। ज़मीन को किसने बनाया है ? ज़मीन को घेर कर अधिकार कर लेने से ही मिल्कियत अगर हो जाय तो कोई भी दस आदमियों को मिलाकर, लाठी बांध कर ज़मीन घेर सकता है। इसमें झूठ क्या है ? बाबर ने क्या किया था ? पंजाब के शेर रणजीतसिंह ने क्या किया था ? छत्रपतिशिवाजी ने क्या किया था ? हैदरअली ने क्या किया था ?
ज़माना बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ कोई चाहे तो बहुत सा रुपया लगाकर ज़मीन खरीद सकता है। फौज-फाटे का जोर एक साधन था। रुपया भी एक साधन है, लाठी का जोर भी एक साधन है। फर्ज़ कीजिये सरकार का दिमाग़ फिर जाय, वह ज़मीदारों के हक को जैसे आज स्वीकार करती है, स्वीकार करना छोड़ दे तो ऐसी अवस्था में न्याय बदल जायेगा। किसानों की ही राय न्याय हो जायेगी।1
किसी की सम्पत्ति या मिल्कियत किसी से छीन लेने का दूसरे को क्या अधिकार है ? मालिक उसे चाहे जिस मोल बेच सकता है, यह बिलकुल न्याय अनुमोदित है। इस तरह धनी बन जाने से न ईश्वर ही नाराज़ हो सकता है न यह न्याय के विरुद्ध है, न कचहरी-अदालत को इसमें दखल है।2 कहते हैं-हमारे गाँव के ज़मींदार के दस गाँव थे। फसल में उन्होंने अनाज के कोठे भरे। ईश्वर की इच्छा हुई, आये साल फसलें खराब हो गयीं, अनाज महंगा बिका। मुनाफा हुआ। सेठजी ने दो गाँव और खरीद लिये।
ज़रा आँख खोलकर देखने से मालूम होता है कि मेरा या मेरी श्रेणी का जिस तरह से हित हो, मेरे लिये वही न्याय है। यदि मैं अपनी शक्ति से, चाहे वह शारीरिक हो या दिमाग़ी, अपने हित के लिये काम करने के लिये दूसरों को बाधित कर सकता हूँ तो वही दूसरों के लिये भी न्याय है।
आजकल ज़माना अच्छा है। मनुष्य की शक्ति का अर्क जमा किया जा सकता है। आंख चाहिये देखने के लिये। सेठजी की तिजोरी की तरफ देखिये, उसमें एक लाख रुपये के नोट नहीं; ज्ञानशलाका लगाकर देखिये, तिजोरी में चार लाख आदमी बंद हैं। इन आदमियों की पीठ पर बोझ ढोने की तैयारी है। हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़े और मेहनत के औज़ार हैं। यदि सेठजी की इच्छा हो तो अभी यह स्थूल प्रत्यक्ष रूप धारण कर काम करने लग सकते हैं। सेठजी जो चाहें कर डालें, पृथ्वी के एक भाग को पलट डालें। सेठजी की तिजोरी में शारीरिक बल का अर्क ज़मा है। यह अर्क सेठजी के अपने शरीर का नहीं। जहाँ-तहाँ से बटोरकर दूसरों का बल खरीदकर अर्क जमा किया गया है।
गरमी की रात है, नींद नहीं आती। मेरी जेब में एक अठन्नी है। यदि मैं लोभ न करूं तो आराम से सो सकता हूँ। चवन्नी में एक आदमी का श्रम-बल (आदमी) छिपा है। उसके हाथ में एक पंखा है। वह रात भर मुझे पंखा कर सकता है।
मैं पूछता हूँ, किसके मुँह में हाथ भरकी जुबान है जो कहे कि यह अन्याय है कि मैं सोऊँ और दूसरा मुझ सा ही आदमी रात भर खड़ा-खड़ा पंखा करे क्या उसके जान नहीं ?
मैं पूछता हूँ, क्या मेरे हाथ में चवन्नी नहीं, मैं चवन्नी की मेहनत नहीं लूंगा ? जिसे अठन्नी लेना हो अपना श्रम मेरे लिये खर्च करे।
---------------------------------------------------
1. उपरोक्त लेख 1935 में लिखा गया था। आज की सरकार ज़मींदारी उन्मूलन का कानून बना रही है। परन्तु ज़मींदार को मुआविजा में दण्ड देना न्याय समझती है। सम्भव है कोई ऐसी सरकार होती जो ज़मींदार को उसकी पिछले लूट के मुआविजा में दण्ड देना ही न्याय समझती। (मार्च 1939)
2. यह धारणा भी बदल गई है क्योंकि सरकार व्यापारियों की अन्धेरगर्दी से परेशान होकर चोर-बाजार विरोधी कानून बना चुकी है।
न्याय है शक्ति में। शक्ति के अनेक रूप हैं। सबसे अच्छा रूप शक्ति का है पैसा। यह सम्भाल कर वक्त के लिये रखा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है। इस पैसे में ज़मीन के जोतने-बोने वाले किसान, सुबह से शाम तक आँखें गड़ाकर दिमाग लड़ाने वाला मुंशी, वर्दी पहन कर हुक्म मनवाने वाले सिपाही और तोप-तलवार लेकर आतंक छा देने वाले सैनिक सब निकल सकते हैं। पैसा मनुष्य का, उसकी श्रम-शक्ति का संचित अर्क है। यह है न्याय का आधार !
जिसके पास यह शक्ति है उसी की इच्छा न्याय है। मनुष्य की शक्ति का यह सार कोई अपने ही शरीर से खींचना चाहे तो नहीं खींच सकता, मर जायेगा कमबख्त। हाँ, दूसरों के शरीर से थोड़ा-थोड़ा कर, उनके श्रम को पैसे के रूप में बदल कर अर्क एकत्र किया जा सकता है। जिस अनुपात में किसी व्यक्ति के पास मनुष्य के संचित श्रम का भण्डार है, उसी अनुपात में वह शक्तिशाली है, न्याय का निर्णायक है।
एक ज़माना था जब एक मनुष्य की इच्छा ही न्याय थी। वह राजा कहलाकर जो हुक्म दे देता, वही न्याय था। वह चाहता तो उसका मंत्री हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता, शहर-ग्राम फूंक दिये जाते।
वक्त आया, राजा की स्वेच्छाचारिता अन्याय समझी जाने लगी। सरदारों सामन्तों के हाथ में भी शक्ति आ गई। न्याय में उनकी इच्छा और रात का दखल हो गया। राजा उनकी सम्मिलित शक्ति के आगे दब गया। वे जो चाहते थे, वही कानून होने लगा।
ज़माना पलटा, व्यापार ने ज़ोर पकड़ा। धन का ठेका एकमात्र सरदारों-सामन्तों के हाथों से निकल व्यापारियों, कल-कारखानों के मालिकों के हाथ में पहुँचा। शक्ति आने के साथ उन्हें ही लोग वोट देने लगे। अपने प्रतिनिधियों के जरिये न्याय में उनका भी कुछ-कुछ दखल होने लगा।
ज्यों-ज्यों शासक-समाज की शक्ति क्षीण होने लगती है या उन्हें अपने हाथों से शक्ति निकलने का भय होने लगता है वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये प्रजा के कुछ अंश को अपना साझी बना, उन्हें न्याय में दखल देने का अधिकार बाँटते हैं या प्रजा के किसी अंश के संतोष के लिये न्याय का रूप उन्हें बदलना पड़ता है।
आज भी हमारे देश में न्याय क्या है ? अपने प्रतिनिधियों की मार्फत इसमें दखल देने का अधिकार एक हद तक उन्हीं को है जो लगान या टैक्स देते हैं, जिनके पास कुछ सम्पत्ति है। इन लोगों की राय में न्याय वही है, जिससे इनकी सम्पत्ति की बढ़ती हो, वह अक्षुण्य बनी रहे। सबसे बड़े पूँजीपति ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी शक्ति की रक्षा के लिये छोटे-छोटे पूँजीपतियों को अपने चक्कर में सम्मिलित कर लिया है, परन्तु इन दस प्रतिशत1 के अलावा जो नब्बे प्रतिशत हैं उनके हक में क्या न्याय है, इसकी चिंता किसे है ?’2
-----------------------------------
1. सन् 1935 के शासन के अनुसार वैधानिक सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार कुल दस प्रतिशत भारतवासियों को था।
2. यद्यपि राष्ट्रीय सरकार के हाथ शासन आते ही जनमत के दबाव से विधान परिषद से निर्वाचन में मत देने का अधिकार बालिग उम्र के सभी लोगों को दे दिया है परन्तु यह बात अमल में नहीं जा रही। निर्वाचनों के दिन पर दिन टाला जा रहा है। 1947 से 1950 या 51 में जब तक निर्वाचन न हो जाये, शासन केवल सम्पत्ति-शालियों के प्रतिनिधियों का ही रहेगा।
------------------------------------
स्वर्ग अपने ही मरने से मिलता है। नब्बे प्रतिशत के लिये यदि न्याय की चिन्ता किसी को हो सकती है तो इन नब्बे प्रतिशत को ही होनी चाहिये। जब तक न्याय का निर्णय दस प्रतिशत के हाथ में रहेगा तब तक न्याय की कसौटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिशत के श्रम से दस प्रतिशत का काम चलता रहे। दस प्रतिशत का कल्याण इसी में है कि नब्बे प्रतिशत उन्हें ‘पिता’1 के स्थान पर मानकर ‘पुत्र’ की तरह उनकी आज्ञा-पालन करते रहें। समाज के शरीर के हाथ-पाँव बन समाज के पेट-दस प्रतिशत को भरते रहें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे न्याय, विधान और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, ‘रामराज्य’ में विघ्न डालते हैं। मुश्किल है तो यह कि नब्बे प्रतिशत यह कैसे मान लें कि ईश्वर की आज्ञा नब्बे प्रतिशत को भूखा ही रखने की है।
मनुष्य की संचित शक्ति का एक रूप पूँजी है तो दूसरा रूप ‘संघ शक्ति’ है। नब्बे प्रतिशत के पास यह दूसरी शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में है। अभी तक उन्होंने अपनी इस शक्ति को नहीं पहचाना क्योंकि अब तक ज्यों-त्यों प्राण बच रहे थे। परन्तु अब पूँजी की शक्ति का पंजा इतना कड़ा हो गया कि सांस लेना मुश्किल है। यदि नब्बे प्रतिशत अब भी अपनी इसी शक्ति के आधार पर न्याय न माँगे तभी ताज्जुब है।
न्याय की धारणा में समय-समय पर संघर्ष होता आया है और उसका रूप बदलता रहा है। यदि नब्बे प्रतिशत अपने भाग्य के निर्णय का बोझ स्वयं संभाल कर न्याय के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा। यदि हम पूँजी और संघ की शक्ति की टक्कर देखना नहीं चाहते तो हमारे लिये नब्बे प्रतिशत की शक्ति को स्वीकार कर लेने के सिवा और मार्ग नहीं।
---------------------
1. गाँधीजी कहते हैं-‘ज़मींदार-किसान का सम्बन्ध पिता-पुत्र का है।’
गाँधीवाद
नवयुग का प्रतीक या युगान्त का ?
जीवन का उद्देश्य क्या है ? मनुष्यता के बाल्यकाल से ही यह प्रश्न मनुष्य
को परेशान किये है। मनुष्य ने मानवता के उषाकाल से ही समय के सागर के
किनारे बैठ इस समस्या के समाधान में कितने ही घरौंदे बनाये और फिर सूझ
बढ़ने के साथ इन समाधानों की विरूपता से खिन्न हो उसने इन्हें मिटा भी
दिया और सुदूर अज्ञेय, अनन्त की ओर देख-देख वह फिर चिन्ता में मग्न हो
गया।
हमारे पूर्व-पुरुषों ने, जिनके अगाध ज्ञान को संसार में फैलाने के लिये हम आज भी व्याकुल हैं, अपनी सम्पूर्ण मानसिक और शारीरिक शक्ति केवल मृत्यु की समस्या को सुलझाने में व्यय कर दी। जीवन के उद्देश्य को मृत्यु की दृष्टि से ही उन्होंने देखा। चिरसत्य मनुष्य के उद्भव से पूर्व ही मुँह फैलाकर उसके मार्ग में आ खड़ी हुई और मनुष्य अपनी असंख्या कल्पना-विकल्पना से भी उसे परास्त नहीं कर पाया।
एक तरफ से परास्त कर भी पाया। मृत्यु के भय के कारण ही मृत्यु का सब महत्व मनुष्य की दृष्टि में है। हमारे ऋषियों ने कहा-मृत्यु कुछ नहीं, एक भ्रम है, आत्मा शाश्वत है। दूसरे आप्त पुरुषों ने निर्धारित किया-संसार ही भ्रम है, बन्धन है, इससे मुक्ति ही मृत्यु है। तब मृत्यु से डरना क्यों ? मृत्यु तो सुख है।
मनुष्य का जीवन व्यक्तिगत रूप से ही पूर्ण है या वह केवल समाज के वृहत् का अंग मात्र है ? यह दूसरा प्रश्न है जिसे मनुष्य बोध और संस्कृति के विकास के साथ सोचने लगा है। जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा सहस्रों जीवन-कोष्ट मरते रहते हैं और उनके स्थान में उनसे अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, इसी समाज के जीवन की व्यवस्था करने की बात सोचें तो शायद मृत्यु से परेशान होने की कोई ज़रूरत न मालूम होगी।
भारतीय दार्शनिक विचारधारा का आधार सदा व्यक्तिगत रहा है। हमारी आध्यात्मिकता जीवन को व्यक्तिगत दृष्टि से देखकर ही सदा पनपी और विकसित हुई है। जीवन को जीतने का उपाय हमने समझा है जीवन से उपराम हो जाना। जीवन को पूर्ण करने का उपाय हमने समझा है, जीवन को संक्षिप्त करते चले जाना और जीवन में संतोष और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय हमने निश्चित किया है-इच्छा न करना, आवश्यकताओं को कम करते चले जाना। आवश्यकताओं को कम करते चले जाइये, ऊँची-ऊँची कल्पना कीजिये। (Plain Living and High Thinking,), जीवन पूर्ण संतुष्ट और सुखमय हो जायेगा।
हमारे देश की वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक तनातनी की परिस्थिति में गाँधीवाद उपर्युक्त प्रवृत्ति को ही सब समस्याओं का हल बताता है। हमारे देश और समाज को सदा परलोकाभिमुख ऋषियों की नीति पर चलने का अभिमान रहा है। आज भी हमारा यह अभिमान अक्षुण्य है। आज दिन भी हमारे राजनैतिक संग्राम के सेनानी हैं हमारे राजनैतिक ऋषि महात्मा गाँधी।1 आज तक का इतिहास हमें बताता है कि धर्म और राजनीति मिलकर अपना-अपना आधिपत्य चलाते रहे हैं बल्कि धर्म को राजनीति के अधीन होना पड़ा। हमारे देश में, हमारे आज दिन के राजनैतिक संघर्ष में, महात्माजी के नेतृत्व में राजनीति को धर्म की शरण लेना आवश्यक हो रहा है।
धर्म शब्द का व्यवहार हम साधारणतः बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। यहाँ हम ‘मज़हब’ या ‘रिलिजन’ के ही अर्थों में इस शब्द को ले रहे हैं। धर्म और राजनीति की तुलना करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों विचारधाराओं का आधार क्या है ?
साम्प्रदायिक धर्म का आधार है पारलौकिक विश्वास और उसका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से वैयक्तिक है। व्यक्ति वैराग्य की चरम सीमा तक पहुँचकर भी संसार और समाज की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता परन्तु मृत्यु के द्वार से हम जिस काल्पनिक लोक में पहुँचते हैं, यहाँ समाज का दखल नहीं। वहाँ व्यक्ति अकेला ही जाता है-‘धर्म्मोहि गच्छति केवलम्’। उस लोक की कामना और कल्पना से प्रेरित होकर मनुष्य जिस धर्म का संचय करता है, उसमें वह नितान्त रूप से आत्महित की ही बात सोचता है। उसके इस आत्महित में किसी दूसरे का साझा नहीं रहता। यदि वह ‘आत्मवत्सर्वभूतेषु’ व्यवहार करने के लिये मजबूर होता है तो वह समाज के कल्याण के प्रति व्याकुल हो कर नहीं; अपितु अपने निस्सर्ग जीवन को समाज में पग-पग पर ठोकर खाने से बचाने के लिये ही ऐसा करता है।
इसके विपरीत राजनीति का उद्देश्य समाज की इहलौकिक सफलता और समृद्धि है। राजनीति का आधार है, सामाजिक संगठन और मानव समूहों का परस्पर संघर्ष। उसका दृष्टिकोण सामाजिक है। धर्म का आधिपत्य राजनीति पर होने से एक विचित्र दोगली नीति का उत्पन्न होना अनिवार्य है, जिसमें राजनीति अवश्यम्भावी रूप से पंगु और निःशक्त हो जायेगी क्योंकि पारलौकिक धर्म केवल विश्वास की वस्तु है और राजनीति यथार्थ जीवन का संघर्ष।
गाँधीवाद मुख्यतः संकेत करता है अहिंसाव्रत की ओर। मनुष्य-समाज में शायद ही कोई ऐसा विचारक हुआ होगा जिसने हिंसा का समर्थन उसके हेय अर्थों में किया हो। यदि हम भावुकता को किनारे रख यह देखने का यत्न करें कि हिंसा का अर्थ समाज में,
----------------------------------
1. यह लेख 1938 में लिखा गया था। गाँधीजी की मृत्यु के पश्चात् आज भी हमारे शासक-संगठन का दावा है कि देश कि शासन गाँधीवाद के ही अनुसार चल रहा है।
राजनीति में और प्रकृति में क्या है तो हम इसे पाप का समानार्थक नहीं पायेंगे। हिंसा का अर्थ कोष में जो हो-व्यवहार में तटस्थ होकर देखने पर हम इसे ‘अप्रिय’ का ही द्योतक पायेंगे। स्थिरता और स्थापना के लिये किसी भी वस्तु का अपनी परिस्थिति से समद्ध होना ज़रूरी है। परिवर्तन के समय इन सम्बन्ध-स्थापक तन्तुओं का टूटना आवश्यक है। यदि यह तन्तु न होते तो स्थिरता नहीं हो सकती थी और यदि यह तन्तु न टूटें तो परिवर्तन असंभव हो जाएगा। परिवर्तन के अभाव में प्रगति रुक जाने पर समाज का जीवन क्यों कर सम्भव हो सकता है ? हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि गति और शक्ति समानार्थक हैं। जब इस गति और शक्ति का प्रयोग हमारे हितों और रुचि के विरुद्ध होता है, अप्रिय होता है; तभी हम हिंसा अनुभव करते हैं। वैयक्तिक दृष्टिकोण से हिंसा की यही कसौटी हमें दिखाई देती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसमें अपवाद की गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देती। हम यह भी कह सकते हैं। कि हिंसा के भेद की नींव हमारी न्याय और अन्याय की धारणा पर है। जो प्रयत्न या शक्ति का प्रयोग हमारी समझ के अनुसार न्याय के समर्थन के लिए किया जाता है, वह अंहिसा है और इसके विपरीत हिंसा। गाँधीवाद की दृष्टि में हिंसा या अहिंसा की उपयुक्त व्याख्या ठीक नहीं। बल्कि यही कहना होगा कि गाँधीवाद में हिंसा और अहिंसा की निर्णायक कसौटी समाज हित नहीं, व्यक्ति की धर्म अनुभूति या धर्म-बुद्धि है। धर्म-बुद्धि से अभिप्राय कर्तव्य का विवेक नहीं अपितु परलोकाभिमुख वैराग्य बुद्धि है।
हमारे पूर्व-पुरुषों ने, जिनके अगाध ज्ञान को संसार में फैलाने के लिये हम आज भी व्याकुल हैं, अपनी सम्पूर्ण मानसिक और शारीरिक शक्ति केवल मृत्यु की समस्या को सुलझाने में व्यय कर दी। जीवन के उद्देश्य को मृत्यु की दृष्टि से ही उन्होंने देखा। चिरसत्य मनुष्य के उद्भव से पूर्व ही मुँह फैलाकर उसके मार्ग में आ खड़ी हुई और मनुष्य अपनी असंख्या कल्पना-विकल्पना से भी उसे परास्त नहीं कर पाया।
एक तरफ से परास्त कर भी पाया। मृत्यु के भय के कारण ही मृत्यु का सब महत्व मनुष्य की दृष्टि में है। हमारे ऋषियों ने कहा-मृत्यु कुछ नहीं, एक भ्रम है, आत्मा शाश्वत है। दूसरे आप्त पुरुषों ने निर्धारित किया-संसार ही भ्रम है, बन्धन है, इससे मुक्ति ही मृत्यु है। तब मृत्यु से डरना क्यों ? मृत्यु तो सुख है।
मनुष्य का जीवन व्यक्तिगत रूप से ही पूर्ण है या वह केवल समाज के वृहत् का अंग मात्र है ? यह दूसरा प्रश्न है जिसे मनुष्य बोध और संस्कृति के विकास के साथ सोचने लगा है। जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षा सहस्रों जीवन-कोष्ट मरते रहते हैं और उनके स्थान में उनसे अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, इसी समाज के जीवन की व्यवस्था करने की बात सोचें तो शायद मृत्यु से परेशान होने की कोई ज़रूरत न मालूम होगी।
भारतीय दार्शनिक विचारधारा का आधार सदा व्यक्तिगत रहा है। हमारी आध्यात्मिकता जीवन को व्यक्तिगत दृष्टि से देखकर ही सदा पनपी और विकसित हुई है। जीवन को जीतने का उपाय हमने समझा है जीवन से उपराम हो जाना। जीवन को पूर्ण करने का उपाय हमने समझा है, जीवन को संक्षिप्त करते चले जाना और जीवन में संतोष और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय हमने निश्चित किया है-इच्छा न करना, आवश्यकताओं को कम करते चले जाना। आवश्यकताओं को कम करते चले जाइये, ऊँची-ऊँची कल्पना कीजिये। (Plain Living and High Thinking,), जीवन पूर्ण संतुष्ट और सुखमय हो जायेगा।
हमारे देश की वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक तनातनी की परिस्थिति में गाँधीवाद उपर्युक्त प्रवृत्ति को ही सब समस्याओं का हल बताता है। हमारे देश और समाज को सदा परलोकाभिमुख ऋषियों की नीति पर चलने का अभिमान रहा है। आज भी हमारा यह अभिमान अक्षुण्य है। आज दिन भी हमारे राजनैतिक संग्राम के सेनानी हैं हमारे राजनैतिक ऋषि महात्मा गाँधी।1 आज तक का इतिहास हमें बताता है कि धर्म और राजनीति मिलकर अपना-अपना आधिपत्य चलाते रहे हैं बल्कि धर्म को राजनीति के अधीन होना पड़ा। हमारे देश में, हमारे आज दिन के राजनैतिक संघर्ष में, महात्माजी के नेतृत्व में राजनीति को धर्म की शरण लेना आवश्यक हो रहा है।
धर्म शब्द का व्यवहार हम साधारणतः बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। यहाँ हम ‘मज़हब’ या ‘रिलिजन’ के ही अर्थों में इस शब्द को ले रहे हैं। धर्म और राजनीति की तुलना करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों विचारधाराओं का आधार क्या है ?
साम्प्रदायिक धर्म का आधार है पारलौकिक विश्वास और उसका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से वैयक्तिक है। व्यक्ति वैराग्य की चरम सीमा तक पहुँचकर भी संसार और समाज की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता परन्तु मृत्यु के द्वार से हम जिस काल्पनिक लोक में पहुँचते हैं, यहाँ समाज का दखल नहीं। वहाँ व्यक्ति अकेला ही जाता है-‘धर्म्मोहि गच्छति केवलम्’। उस लोक की कामना और कल्पना से प्रेरित होकर मनुष्य जिस धर्म का संचय करता है, उसमें वह नितान्त रूप से आत्महित की ही बात सोचता है। उसके इस आत्महित में किसी दूसरे का साझा नहीं रहता। यदि वह ‘आत्मवत्सर्वभूतेषु’ व्यवहार करने के लिये मजबूर होता है तो वह समाज के कल्याण के प्रति व्याकुल हो कर नहीं; अपितु अपने निस्सर्ग जीवन को समाज में पग-पग पर ठोकर खाने से बचाने के लिये ही ऐसा करता है।
इसके विपरीत राजनीति का उद्देश्य समाज की इहलौकिक सफलता और समृद्धि है। राजनीति का आधार है, सामाजिक संगठन और मानव समूहों का परस्पर संघर्ष। उसका दृष्टिकोण सामाजिक है। धर्म का आधिपत्य राजनीति पर होने से एक विचित्र दोगली नीति का उत्पन्न होना अनिवार्य है, जिसमें राजनीति अवश्यम्भावी रूप से पंगु और निःशक्त हो जायेगी क्योंकि पारलौकिक धर्म केवल विश्वास की वस्तु है और राजनीति यथार्थ जीवन का संघर्ष।
गाँधीवाद मुख्यतः संकेत करता है अहिंसाव्रत की ओर। मनुष्य-समाज में शायद ही कोई ऐसा विचारक हुआ होगा जिसने हिंसा का समर्थन उसके हेय अर्थों में किया हो। यदि हम भावुकता को किनारे रख यह देखने का यत्न करें कि हिंसा का अर्थ समाज में,
----------------------------------
1. यह लेख 1938 में लिखा गया था। गाँधीजी की मृत्यु के पश्चात् आज भी हमारे शासक-संगठन का दावा है कि देश कि शासन गाँधीवाद के ही अनुसार चल रहा है।
राजनीति में और प्रकृति में क्या है तो हम इसे पाप का समानार्थक नहीं पायेंगे। हिंसा का अर्थ कोष में जो हो-व्यवहार में तटस्थ होकर देखने पर हम इसे ‘अप्रिय’ का ही द्योतक पायेंगे। स्थिरता और स्थापना के लिये किसी भी वस्तु का अपनी परिस्थिति से समद्ध होना ज़रूरी है। परिवर्तन के समय इन सम्बन्ध-स्थापक तन्तुओं का टूटना आवश्यक है। यदि यह तन्तु न होते तो स्थिरता नहीं हो सकती थी और यदि यह तन्तु न टूटें तो परिवर्तन असंभव हो जाएगा। परिवर्तन के अभाव में प्रगति रुक जाने पर समाज का जीवन क्यों कर सम्भव हो सकता है ? हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं कि गति और शक्ति समानार्थक हैं। जब इस गति और शक्ति का प्रयोग हमारे हितों और रुचि के विरुद्ध होता है, अप्रिय होता है; तभी हम हिंसा अनुभव करते हैं। वैयक्तिक दृष्टिकोण से हिंसा की यही कसौटी हमें दिखाई देती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसमें अपवाद की गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देती। हम यह भी कह सकते हैं। कि हिंसा के भेद की नींव हमारी न्याय और अन्याय की धारणा पर है। जो प्रयत्न या शक्ति का प्रयोग हमारी समझ के अनुसार न्याय के समर्थन के लिए किया जाता है, वह अंहिसा है और इसके विपरीत हिंसा। गाँधीवाद की दृष्टि में हिंसा या अहिंसा की उपयुक्त व्याख्या ठीक नहीं। बल्कि यही कहना होगा कि गाँधीवाद में हिंसा और अहिंसा की निर्णायक कसौटी समाज हित नहीं, व्यक्ति की धर्म अनुभूति या धर्म-बुद्धि है। धर्म-बुद्धि से अभिप्राय कर्तव्य का विवेक नहीं अपितु परलोकाभिमुख वैराग्य बुद्धि है।
(2)
हम यह नहीं कहते कि विशुद्ध राजनीति में केवल मार-काट और रक्त-पात के
अतिरिक्त कुछ नहीं। हम यह भी नहीं कहते कि संसार के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ
नादिरशाह थे। मार-काट की पाशविक हिंस्र प्रवृत्ति बर्बरता का शेष चिन्ह
है। मनुष्य न पशु है और न मशीन जो केवल ‘हार्स-पावर’
से काम
लेगा। उसमें जो मनुष्य नाम का पदार्थ है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।
युक्ति और प्रेरणा हमारी मौजूदा संस्कृति के सबसे अनुरूप साधन हैं। आधुनिक
राजनैतिक व्यवस्था का आदर्श प्रजातन्त्र शासन प्रणाली और प्राचीन
शासन-नीति के आदर्श शक्तिप्रयोग में आधारभूत भेद है उसे हम बर्बरता या
समाज की मूढ़ता का चिन्ह समझते हैं। युक्ति और प्रेरणा की ओर मनुष्य-समाज
की उत्तरोत्तर प्रवृत्ति उसके इसी आदर्श की ओर संकेत करती है और उसके
विकास का प्रमाण है।
शस्त्र-शक्ति की जो हम बिलकुल उपेक्षा नहीं कर पाते, वह कुछ अभ्यास दोष से और कुछ पारस्परिक आशंका और अविश्वास के कारण। हम यह दावा नहीं कर सकते कि आज दिन हम संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच गये हैं। हम विकास की एक मंज़िल तक पहुंचे हैं, जिसमें हमारा साधन और नीति पूंजीवाद की प्रणाली रही है। पूंजीवाद की प्रणाली पर चलकर इस मंज़िल तक पहुंचने के लिये यह आवश्यक था कि समाज भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त रहे। पूंजीवाद की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी समाज उसे एक तरफ नहीं फेंक दे सका।
श्रेणियों का वह भेद जो एक दिन के विकास के लिये ज़रूरी था, जो उसकी आन्तरिक प्रेरक शक्ति थी, वही उसके मार्ग का अवरोधक हो रहा है। इस भेद के परिणामस्वरूप समाज में एक तनातनी और संघर्ष की जलन फैल रही है इसलिये हिंसा और बल-प्रयोग भी दिखायी पड़ रहा है। आज जो हम फ़ासिज्म और नाज़िज्म का रूप देख रहे हैं, यह समाज में आते परिवर्तन की भयंकर तड़प को दबाने का पूँजीवादी प्रयत्न है।
शस्त्र-शक्ति की जो हम बिलकुल उपेक्षा नहीं कर पाते, वह कुछ अभ्यास दोष से और कुछ पारस्परिक आशंका और अविश्वास के कारण। हम यह दावा नहीं कर सकते कि आज दिन हम संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच गये हैं। हम विकास की एक मंज़िल तक पहुंचे हैं, जिसमें हमारा साधन और नीति पूंजीवाद की प्रणाली रही है। पूंजीवाद की प्रणाली पर चलकर इस मंज़िल तक पहुंचने के लिये यह आवश्यक था कि समाज भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त रहे। पूंजीवाद की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी समाज उसे एक तरफ नहीं फेंक दे सका।
श्रेणियों का वह भेद जो एक दिन के विकास के लिये ज़रूरी था, जो उसकी आन्तरिक प्रेरक शक्ति थी, वही उसके मार्ग का अवरोधक हो रहा है। इस भेद के परिणामस्वरूप समाज में एक तनातनी और संघर्ष की जलन फैल रही है इसलिये हिंसा और बल-प्रयोग भी दिखायी पड़ रहा है। आज जो हम फ़ासिज्म और नाज़िज्म का रूप देख रहे हैं, यह समाज में आते परिवर्तन की भयंकर तड़प को दबाने का पूँजीवादी प्रयत्न है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i 






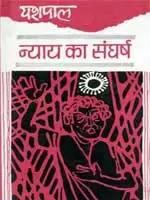


_s.jpg)
