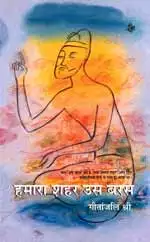|
उपन्यास >> हमारा शहर उस बरस हमारा शहर उस बरसगीतांजलि श्री
|
440 पाठक हैं |
|||||||
इसमें बहुआयामी उलझन पैदा करनेवाले आए दिन सांप्रदायिक दंगों से ग्रस्त जीवन पर प्रकाश डाला गया है...
Hamara Shahar Us Baras
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आसान दिखने वाली मुश्किल कृति 'हमारा शहर उस बरस' में साक्षात्कार होता है एक कठिन समय की बहुआयामी और उलझन पैदा करने वाली सच्चाइयों से। बात ‘उस बरस’ की है, जब हमारा शहर’ आये दिन साम्प्रदायिक दंगो से ग्रस्त हो जाता था। आगजनी, मारकाट और तदजनित दहशत रोजमर्रा का जीवन बनकर एक भयावह सहजता पाते जा रहे थे। कृत्रिम जीवन शैली का यों सहज शहरवासियों की मानसिकता, व्यक्तित्व, बल्कि पूरे वजूद पर चोट कर रहा था।
बात दरअसल उस बरस की नहीं है। उस बरस को हम आज में घसीट लाए हैं। न ही बात है सिर्फ हमारे शहर की। ‘और शहरों जैसा ही है हमारा शहर’-सुलगता, खदकता-‘स्त्रोत और प्रतिबिम्ब दोनों ही’ मौजूद स्थिति का। एक आततायी आपातस्थिति, जिसका हाल फौरन ढूँढ़ना है, पर स्थिति समझ में आये, तब न निकले हल। पुरानी धारणाएँ फिट बैठती नहीं, नई सूझती नहीं, वक्त है नहीं कि जब सूझे, तब उन्हें लागू करके जूझें स्थिति से। न जाने क्या से क्या हो जाए तब तक। वे संगीने जो दूर हैं उधर, उन पर मुड़ीं, वे हम पर भी न मुड़ जाएँ, वह धूल-धुआँ जो उधर भरा है, इधर भी न मुड़ आए।
अभी भी जो समझ रहे हैं कि दंगे उधर हैं-दूर, उस पार, उन लोगों में-पाते हैं कि-‘उधर’ ‘इधर’ बढ़ा आया है, ‘वे’ लोग ‘हम’ लोग भी हैं, और इधर-उधर वे-हम करके खुद को झूठी तसल्ली नहीं दी सकती। दंगे जहाँ हो रहे हैं, वहाँ खून बह रहा है। सो, यहाँ भी बह रहा है, हमारी खाल के नीचे !
अपनी ही खाल के नीचे छिड़े दंगे से दरपेश होने की कोशिश है इस गाथा का मूल। खुद को चीरफाड़ के लिए वैज्ञानिक की मेज पर धर देने जैसा। अपने को नंगा करने का प्रयास ही अपने शहर को समझने, उसके प्रवाहों को मोड़ देने की एकमात्र शुरुआत हो सकती है। यही शुरुआत एक जबरदस्त प्रयोग द्वारा गीतांजलिश्री ने हमारा शहर उस बरस में की है। जान न पाने की बढ़ती बेबसी के बीच जानने की तरफ ले जाते हुए।
बात दरअसल उस बरस की नहीं है। उस बरस को हम आज में घसीट लाए हैं। न ही बात है सिर्फ हमारे शहर की। ‘और शहरों जैसा ही है हमारा शहर’-सुलगता, खदकता-‘स्त्रोत और प्रतिबिम्ब दोनों ही’ मौजूद स्थिति का। एक आततायी आपातस्थिति, जिसका हाल फौरन ढूँढ़ना है, पर स्थिति समझ में आये, तब न निकले हल। पुरानी धारणाएँ फिट बैठती नहीं, नई सूझती नहीं, वक्त है नहीं कि जब सूझे, तब उन्हें लागू करके जूझें स्थिति से। न जाने क्या से क्या हो जाए तब तक। वे संगीने जो दूर हैं उधर, उन पर मुड़ीं, वे हम पर भी न मुड़ जाएँ, वह धूल-धुआँ जो उधर भरा है, इधर भी न मुड़ आए।
अभी भी जो समझ रहे हैं कि दंगे उधर हैं-दूर, उस पार, उन लोगों में-पाते हैं कि-‘उधर’ ‘इधर’ बढ़ा आया है, ‘वे’ लोग ‘हम’ लोग भी हैं, और इधर-उधर वे-हम करके खुद को झूठी तसल्ली नहीं दी सकती। दंगे जहाँ हो रहे हैं, वहाँ खून बह रहा है। सो, यहाँ भी बह रहा है, हमारी खाल के नीचे !
अपनी ही खाल के नीचे छिड़े दंगे से दरपेश होने की कोशिश है इस गाथा का मूल। खुद को चीरफाड़ के लिए वैज्ञानिक की मेज पर धर देने जैसा। अपने को नंगा करने का प्रयास ही अपने शहर को समझने, उसके प्रवाहों को मोड़ देने की एकमात्र शुरुआत हो सकती है। यही शुरुआत एक जबरदस्त प्रयोग द्वारा गीतांजलिश्री ने हमारा शहर उस बरस में की है। जान न पाने की बढ़ती बेबसी के बीच जानने की तरफ ले जाते हुए।
हमारा शहर उस बरस
यही जगह है। हमारा शहर ।
घबराकर जिस शहर में निकल गए थे वे तीन कि अपराध और अपराधी घायल और मुर्दें, सबको निकाल लाएँगे। साफ-साफ देख लेंगे और जैसा साफ देख लेंगे वैसा ही साफ दिखा देंगे। शरद, श्रुति और हनीफ जिन्होंने ठान लिया था कि लिखेंगे। कि इस वक्त चुप नहीं रहा जा सकता। सब कुछ खोलकर रख देना है। कि जो हवा चल रही है, वह हवा नहीं, बवंडर है; जो हमें कहीं उखाड़ न दे।
बारिश हो रही है। ट्रेन से उतरकर श्रुति प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी है। एक थरथराहट भरी बेचैनी उसके पैरों के नीचे से गुजरकर ट्रेन के साथ-साथ निकल जाती है। लोग गिरते, पड़ते, भीगते बाहर को सवारियाँ ढूँढ़ने दौड़ गये हैं। शहर के गाय और कुत्ते पानी टपकाते प्लेटफार्म पर सुस्ताने चले आए हैं। पानी पटरियों की तरफ रुख करके बह रहा है। वीराना है।
उस बरस एक बार सड़कों पर ऐसी ही नदियाँ बहने लगी थीं, पर वह बारिश नहीं थी, टंकियों का पानी था, जो मुहल्लों के मुहल्लों ने ज़हर के डर से खोलकर बहा दिया था।
शरद दूर से उसे पहचानकर बढ़ा। वह खड़ी रही, अकेली इंतज़ार करती। दोनों आमने-सामने आ गए हैं। उनके चेहरे उनके शब्दों में उलझकर अजीब बँधी जकड़ी चुप्पी पैदा कर रहे हैं। वे सँभले कदमों से बाहर आ गए।
तीनों समझते कि सब कुछ वहीं बाहर था, जो हमें इतना भयभीत और व्याकुल कर रहा था। उन्हीं का डर था, मुझमें भी भर गया था। मैं घबराने लगी। वे लिखने की कोशिश करते और बीच में छोड़ देते। अपने लिखे को खोखला पाते और कहते, सब रटी रटाई बातें हैं। जिनको लिखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वे हर तरफ नकारी जा रही है। सरकारी नारों की तरह बेमतलब हो चुकी हैं। तब मुझे लगा था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे भी हो, लिखना तो पड़ेगा। चाहे समझें या न समझें। और वे न सही, जिनमें से एक पेशेवर लेखिका थी और दो बुद्धिजीवी, तो मैं ही सही, जो बस नकलकर्ता हो सकती थी।
उस वक़्त में कुछ ऐसा नहीं था कि साफ़ दो टूक बात कही जाए। तभी मैं लिख सकी, जिसने दो टूक कहने का तजुर्बा था, न हठ। नकल उतारने को अगर लिखना कहें तो मैं बस वही कर रही थी। वही कर सकती थी। इनके पीछे-पीछे रहकर जो टुकड़े उठ आए, उठा लूँ। जो जहाँ मेरी नज़र में पड़ जाए।
मेरी नज़र के आगे वही घर है, वही फाटक, वही लेटरबॉक्स। उसका पल्ला खुल गया है और बारिश की सतत बूँदें उसे हिला रही हैं। श्रुति फाटक पर ठिठक गई है। उसकी चप्पलें ही नहीं पैर भी, टखनों तक भीग गए हैं। शरद ने फाटक खोला। घर के सामने की खुली जगह में जंगली घास भर गई है।
वहाँ एक मधुमालती की लतर हुआ करती थी, जिसके नीचे गुलाबी मसूढ़ों पर सफ़ेद दाँतों की कतार देखकर अजीब मतली सी आई थी और मेरा कलम मेरे हाथ से छूटकर उसी के पास जा छिटका था। बाद में मैंने सोचा भी कि क्यों नहीं उन्हें देखकर वह सुंदर सेहत पूर्ण हँसी याद आई, जो पूरे चेहरे को खिला देती थी। वह धूल में पड़े, हँसी की सारी सुंदरता को बेआबरू करते एक घिनौना आकार भर हो गए, चेहरे की सारी शख्यित को भुलाते, उस इनसान के सारे अस्तित्व को गायब करते। दद्दू कहते थे कि पहचान को गाढ़ी लकीरों से आकार बनाकर किसी टुकड़े में घुसेड़ोगे तो पहचान नहीं, बेकार बेजान कट-आउट रह जाएगा, कि पहचान तो बाहर फूटती और फैलती और खुले में विचरती, हर चीज से लिपटती घुलती, रोशनी है, जिसे किसी टुकड़े में बंद करोगे कि विशुद्ध अस्तित्व बनेगा तो बस बुझ जाएगी और मरा हुआ आकार रह जाएगा। मांस का घिनौना लोथ। मगर मैं तो टुकड़े ही उठाती रही। वक्त नहीं था, सलाहियत की छोड़िए, कि बीच के हिस्से भरूँ, जोड़ती कड़ियाँ तलाशूँ किसी भी चीज को इत्मीनान से करने का वक्त नहीं था बस, डरते-डरते जल्दी-जल्दी, इनकी कॉपी करती गई थी चाहे इधर का उधर लिखा जाए, गैर जरूरी कलम में खिंच आए, यहाँ का टुकड़ा वहाँ चस्पाँ कर जाऊँ। जब जमीन ही ‘कोलाज’ बन गया था, जिसमें बम के विस्फोट से जैसे, कतरे उछलते हैं और इस जगह के उस जगह जा चिपकते हैं, निहायत बेतुकी आकृतियाँ गढ़ते तो अधूरे बिखरे टूटे से आखिर बचाव था ही कहाँ ?
अब लाशों के खेत में गोभी की फ़सल सुने हो कभी ?
तो सुन लो।
थी हमारे शहर में उस बरस।
और सुने हो कभी कि ऐसी सफ़ेद तरोताज़ा, गठे जिस्मवाली गोभी कौड़ियों के दाम भी न बिके ?
सो भी हमारे ही शहर की बात, उसी बरस की बात।
ऐसी ही बातें थीं, जिनका न सिर, न पैर और मेरे बस का नहीं था कि टुकड़ों को जोड़-जाड़कर असल सूरत दिखाईं। बस टुकड़े ही थे, जिनकी वक़त न मैं आँक सकती थी, न मुझे आँकना ही था। वह मेरा ठेका नहीं था, बस कॉपी करना था।
शुरू से ही मैं नकलकर्ता रही हूँ।
शुरू से, कि नहीं, पता नहीं; क्योंकि यह किसी को नहीं पता था कि शुरू कहाँ है। पर वहां से जहाँ से उनकी घबराहट से डरकर मैंने झपटकर कागज खींचा कलम खोला और धूल धुएँ के मौसम में जुट गई कि तुम नहीं तो मैं ही लिखती हूँ, यानी तुम्हारी ही कॉपी करती हूँ, जो बोलो, देखो, कहो, यानी जो-जो मैं पकड़ लूं, और समझ के नहीं तो बिना समझे ही लिखती हूँ।
क्योंकि लिखना तो था ही उस बरस और शहर के बारे में।
किसी न किसी को तो गवाह बनना था।
और क्या मालूम ना समझ की अनर्गल वाणी में सार हो...और क्या पता उस बरस के बाद बरस और भी हों...
जैसे शायद यह, जिसमें श्रुति खड़ी है और शरद उसे अंदर खींचकर दरवाजे की साँकल और जंजीर लगा देता है।
वह कहता है, ‘‘आओ देख लो।’’
श्रुति ने मना किया, नहीं रहने दो।’’
‘‘देख लो।’’
‘‘छोड़ो।’’
पर शरद ने बढ़कर एक और दरवाजा़ खोल दिया है। अंदर पलंग पर जो गठरी पड़ी है, उसकी पीठ इधर है। चादर के बाहर दो पतली डंडियाँ-सी निकली हुई हैं।
श्रुति दरवाज़े के पास नहीं जाती। दूर से पलँग के पास पड़ी छोटी-छोटी मेज़ पर रखी चीज़ों को देखती है और घूमकर सीधे हॉल में आ जाती है। जो उस रोशनी में थे, जो उनके जिस्म से बाहर फैलती थी, वे जिस्म में सिमट कर जरा-सा एक गट्ठर बन गए हैं। सारी टिम-टिम मिट चुकी है। बस गाढ़ी लकीरों से बना एक कटआउट है, ‘सिकुड़न’ का कटआउट।
शरद हनीफ़ का नाम लेना चाहता है। ‘‘हनीफ ?’’ वह शुरू होकर चुप हो गया है।
‘‘लिख रहा है।’’ श्रुति बताकर पूछती है, ‘‘और तुम ?’’
शरद कंधे उचकता है।
मैं अपना पुलिंदा खोलती हूँ। जल्दी-जल्दी पन्ने फड़फड़ाती हूँ। फिर धीरे-धीरे। रमी के पत्तों की तरह लगाती हूँ, पर यहां कौन से पेयर बनेंगे, कौन सेसीक्वेन्स ? पन्ने बस बिखरे हैं और कलम खुला है।
कोई सुन नहीं रहा।
दोनों चुपचाप बैठे हैं। उनके सामने पड़ा है उस बरस का वह शीशम का दीवान।
उस बरस हमारे शहर में हिंदुओं ने शांतिप्रियता छोड़ दी थी। अबके ऐलान करके छोड़ी कि एक गाल पर तमाचा पड़ा तो दूसरा बढ़ा दिया, पर अब तीसरा गाल कहाँ से लावें ? हम मजबूर हैं, वे चीखे। पर सवार होकर त्रिशूल की नोंक पर देवी की पताका फहराने लगे कि जो हमारे संग हुआ है, वही हमें उनके संग करना है। पाप का बदला पाप से चुकेगा। साधु-संतों ने समाधि छोड़ दी और उपासना की एवज में ललकार गूँज उठी कि हमारी संतानें जाती रहीं, हमारी बेटियाँ लुटती रहीं, बेटो, हिजड़े हो क्या ? ए वीर शिवाजी की संतान, भगतसिंह राणाप्रताप के वंशज अर्जुन और भीम के पुत्रों, उट्ठो। उन दुष्टों की बस्तियों को श्मशान बना डालो। बहुत हो गई तुम्हारी भलमनसी। दैत्यों-पिशाचों के जुल्म बढ़े तो देवताओं को भी क्रोध आ गया। उट्ठो।
जागो।
बचाओ।
और निकल पड़े जत्थे के जत्थे हमारे शहर में मस्जिदों की नींव उखाड़ के अपने देवियों-देवताओं की लाशें खड़ी करने।
हमारे शहर की हवा सनसनाने लगी। उनकी मजबूरी से बूम-बूम गूजने लगी। जत्थे जोर-शोर से निकले, भभूत के बादल उड़ाते जो कभी भी धूल बनके हमारी आँखों में किचकिचा जाती, गंगाजल की नहरें बहाते, जो कभी भी खून बनके हम पर छींटे उछाल देतीं।
ज़ोरदार शोरदार मेला लगा। रंग इतने कि अबीर की आँधी हो, होली की मस्ती हो। यज्ञ हुए, जिनमें वीतराग की आड़ में पलती कायरता को तिलांजलि दे, भस्म का तिलक लगा और हाथों में धारदार धातु उछालकर सूरज की चिन्दियाँ कर डाली गईं और उन्हीं चमकते टुकड़ों को नोक पर लहराते हुए लोग गलियों में घुस गए। झूमते हुए सूरज को यों कब्जे में पाकर।
हम सहम गए सूरज की यह गत देखकर।
एक बच्चे की नज़र से लिखूँ ?’’ श्रुति पूछ रही है। उसके हाथ चुकंदर छीलने से लाल टपका रहे हैं। हमारा अनबॉन बच्चा ? जो यह सबदेखे, सुने, बताए ?’’
‘‘न।’’ हनीफ ने सिरे से ‘वीटो’ कर दिया। ‘‘एक तो’’ उसने कहा, ‘‘यह ढंग बहुत पुराना है, महाभारत काल से चला आ रहा है। दूसरे...’’ उसकी आवाज में शिद्दत है, ‘‘ख्वाब में भी हमें बच्चा नहीं चाहिए, जिसे यह वक्त विरासत में मिले ?’’
जो पैदा न हुआ हो, उस बच्चे की गवाही का खयाल आ सकता है, चाहे पलभर को ही तो मैं इतना क्यों डर रही हूँ ? परछाई की तरह लग जाऊँ और नकल बनाती जाऊँ। नकल से क्या डरना ?
‘‘हम क्यों डरें ? हम इधर रहते हैं। तुम्हारा दोस्त नाहक फ़ियर-साइकोसिस फैलाता है। उसे मजा आता है।’’ श्रुति शिकायत करती है।
वे ऊपर फ्लैट में बैठे हैं। जूठी प्लेटों का अंबार सामने है। अभी-अभी शरद नीचे अपने घर चला गया। उसके पहले तीनों साथ खा-पी रहे थे, गप्पिया रहे थे और मैं खड़ी थी कि सुनूँ उतारू, अनसुना करूँ ? प्लेटों में तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची खानेवालों ने एक तरफ़ सरका दिए हैं। शरद का आखि़री जुमला अभी तक हवा में तिर रहा है कि ‘‘शहर में आग लगी है, तुम हँस रहे हो ?’’
वहीं से मैं ठान लेती हूँ उतारूँ।
‘‘तुम ह्यूमेलेस हो, हनीफ श्रुति को चिढ़ाता है। शरद छेड रहा था, वह जानता है कि तुम बमक उठोगी।’’
‘‘कहीं नहीं छेड़-बेड़। तुम्हारा दोस्त है एकदम ह्यूमरलेस बेटा, वह भी एकदम टू मच ह्यूमरफ़ुल बाप का।’’ श्रुति शुरू गुस्से से करती है, मगर ख़त्म मुस्कराकर, जब दद्दू का ज़िक्र आ जाता है।
‘‘आग तो लगी ही है।’’
‘‘पर यहाँ नहीं। वहाँ।’’ श्रुति टोकती है।
घबराकर जिस शहर में निकल गए थे वे तीन कि अपराध और अपराधी घायल और मुर्दें, सबको निकाल लाएँगे। साफ-साफ देख लेंगे और जैसा साफ देख लेंगे वैसा ही साफ दिखा देंगे। शरद, श्रुति और हनीफ जिन्होंने ठान लिया था कि लिखेंगे। कि इस वक्त चुप नहीं रहा जा सकता। सब कुछ खोलकर रख देना है। कि जो हवा चल रही है, वह हवा नहीं, बवंडर है; जो हमें कहीं उखाड़ न दे।
बारिश हो रही है। ट्रेन से उतरकर श्रुति प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी है। एक थरथराहट भरी बेचैनी उसके पैरों के नीचे से गुजरकर ट्रेन के साथ-साथ निकल जाती है। लोग गिरते, पड़ते, भीगते बाहर को सवारियाँ ढूँढ़ने दौड़ गये हैं। शहर के गाय और कुत्ते पानी टपकाते प्लेटफार्म पर सुस्ताने चले आए हैं। पानी पटरियों की तरफ रुख करके बह रहा है। वीराना है।
उस बरस एक बार सड़कों पर ऐसी ही नदियाँ बहने लगी थीं, पर वह बारिश नहीं थी, टंकियों का पानी था, जो मुहल्लों के मुहल्लों ने ज़हर के डर से खोलकर बहा दिया था।
शरद दूर से उसे पहचानकर बढ़ा। वह खड़ी रही, अकेली इंतज़ार करती। दोनों आमने-सामने आ गए हैं। उनके चेहरे उनके शब्दों में उलझकर अजीब बँधी जकड़ी चुप्पी पैदा कर रहे हैं। वे सँभले कदमों से बाहर आ गए।
तीनों समझते कि सब कुछ वहीं बाहर था, जो हमें इतना भयभीत और व्याकुल कर रहा था। उन्हीं का डर था, मुझमें भी भर गया था। मैं घबराने लगी। वे लिखने की कोशिश करते और बीच में छोड़ देते। अपने लिखे को खोखला पाते और कहते, सब रटी रटाई बातें हैं। जिनको लिखने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वे हर तरफ नकारी जा रही है। सरकारी नारों की तरह बेमतलब हो चुकी हैं। तब मुझे लगा था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे भी हो, लिखना तो पड़ेगा। चाहे समझें या न समझें। और वे न सही, जिनमें से एक पेशेवर लेखिका थी और दो बुद्धिजीवी, तो मैं ही सही, जो बस नकलकर्ता हो सकती थी।
उस वक़्त में कुछ ऐसा नहीं था कि साफ़ दो टूक बात कही जाए। तभी मैं लिख सकी, जिसने दो टूक कहने का तजुर्बा था, न हठ। नकल उतारने को अगर लिखना कहें तो मैं बस वही कर रही थी। वही कर सकती थी। इनके पीछे-पीछे रहकर जो टुकड़े उठ आए, उठा लूँ। जो जहाँ मेरी नज़र में पड़ जाए।
मेरी नज़र के आगे वही घर है, वही फाटक, वही लेटरबॉक्स। उसका पल्ला खुल गया है और बारिश की सतत बूँदें उसे हिला रही हैं। श्रुति फाटक पर ठिठक गई है। उसकी चप्पलें ही नहीं पैर भी, टखनों तक भीग गए हैं। शरद ने फाटक खोला। घर के सामने की खुली जगह में जंगली घास भर गई है।
वहाँ एक मधुमालती की लतर हुआ करती थी, जिसके नीचे गुलाबी मसूढ़ों पर सफ़ेद दाँतों की कतार देखकर अजीब मतली सी आई थी और मेरा कलम मेरे हाथ से छूटकर उसी के पास जा छिटका था। बाद में मैंने सोचा भी कि क्यों नहीं उन्हें देखकर वह सुंदर सेहत पूर्ण हँसी याद आई, जो पूरे चेहरे को खिला देती थी। वह धूल में पड़े, हँसी की सारी सुंदरता को बेआबरू करते एक घिनौना आकार भर हो गए, चेहरे की सारी शख्यित को भुलाते, उस इनसान के सारे अस्तित्व को गायब करते। दद्दू कहते थे कि पहचान को गाढ़ी लकीरों से आकार बनाकर किसी टुकड़े में घुसेड़ोगे तो पहचान नहीं, बेकार बेजान कट-आउट रह जाएगा, कि पहचान तो बाहर फूटती और फैलती और खुले में विचरती, हर चीज से लिपटती घुलती, रोशनी है, जिसे किसी टुकड़े में बंद करोगे कि विशुद्ध अस्तित्व बनेगा तो बस बुझ जाएगी और मरा हुआ आकार रह जाएगा। मांस का घिनौना लोथ। मगर मैं तो टुकड़े ही उठाती रही। वक्त नहीं था, सलाहियत की छोड़िए, कि बीच के हिस्से भरूँ, जोड़ती कड़ियाँ तलाशूँ किसी भी चीज को इत्मीनान से करने का वक्त नहीं था बस, डरते-डरते जल्दी-जल्दी, इनकी कॉपी करती गई थी चाहे इधर का उधर लिखा जाए, गैर जरूरी कलम में खिंच आए, यहाँ का टुकड़ा वहाँ चस्पाँ कर जाऊँ। जब जमीन ही ‘कोलाज’ बन गया था, जिसमें बम के विस्फोट से जैसे, कतरे उछलते हैं और इस जगह के उस जगह जा चिपकते हैं, निहायत बेतुकी आकृतियाँ गढ़ते तो अधूरे बिखरे टूटे से आखिर बचाव था ही कहाँ ?
अब लाशों के खेत में गोभी की फ़सल सुने हो कभी ?
तो सुन लो।
थी हमारे शहर में उस बरस।
और सुने हो कभी कि ऐसी सफ़ेद तरोताज़ा, गठे जिस्मवाली गोभी कौड़ियों के दाम भी न बिके ?
सो भी हमारे ही शहर की बात, उसी बरस की बात।
ऐसी ही बातें थीं, जिनका न सिर, न पैर और मेरे बस का नहीं था कि टुकड़ों को जोड़-जाड़कर असल सूरत दिखाईं। बस टुकड़े ही थे, जिनकी वक़त न मैं आँक सकती थी, न मुझे आँकना ही था। वह मेरा ठेका नहीं था, बस कॉपी करना था।
शुरू से ही मैं नकलकर्ता रही हूँ।
शुरू से, कि नहीं, पता नहीं; क्योंकि यह किसी को नहीं पता था कि शुरू कहाँ है। पर वहां से जहाँ से उनकी घबराहट से डरकर मैंने झपटकर कागज खींचा कलम खोला और धूल धुएँ के मौसम में जुट गई कि तुम नहीं तो मैं ही लिखती हूँ, यानी तुम्हारी ही कॉपी करती हूँ, जो बोलो, देखो, कहो, यानी जो-जो मैं पकड़ लूं, और समझ के नहीं तो बिना समझे ही लिखती हूँ।
क्योंकि लिखना तो था ही उस बरस और शहर के बारे में।
किसी न किसी को तो गवाह बनना था।
और क्या मालूम ना समझ की अनर्गल वाणी में सार हो...और क्या पता उस बरस के बाद बरस और भी हों...
जैसे शायद यह, जिसमें श्रुति खड़ी है और शरद उसे अंदर खींचकर दरवाजे की साँकल और जंजीर लगा देता है।
वह कहता है, ‘‘आओ देख लो।’’
श्रुति ने मना किया, नहीं रहने दो।’’
‘‘देख लो।’’
‘‘छोड़ो।’’
पर शरद ने बढ़कर एक और दरवाजा़ खोल दिया है। अंदर पलंग पर जो गठरी पड़ी है, उसकी पीठ इधर है। चादर के बाहर दो पतली डंडियाँ-सी निकली हुई हैं।
श्रुति दरवाज़े के पास नहीं जाती। दूर से पलँग के पास पड़ी छोटी-छोटी मेज़ पर रखी चीज़ों को देखती है और घूमकर सीधे हॉल में आ जाती है। जो उस रोशनी में थे, जो उनके जिस्म से बाहर फैलती थी, वे जिस्म में सिमट कर जरा-सा एक गट्ठर बन गए हैं। सारी टिम-टिम मिट चुकी है। बस गाढ़ी लकीरों से बना एक कटआउट है, ‘सिकुड़न’ का कटआउट।
शरद हनीफ़ का नाम लेना चाहता है। ‘‘हनीफ ?’’ वह शुरू होकर चुप हो गया है।
‘‘लिख रहा है।’’ श्रुति बताकर पूछती है, ‘‘और तुम ?’’
शरद कंधे उचकता है।
मैं अपना पुलिंदा खोलती हूँ। जल्दी-जल्दी पन्ने फड़फड़ाती हूँ। फिर धीरे-धीरे। रमी के पत्तों की तरह लगाती हूँ, पर यहां कौन से पेयर बनेंगे, कौन सेसीक्वेन्स ? पन्ने बस बिखरे हैं और कलम खुला है।
कोई सुन नहीं रहा।
दोनों चुपचाप बैठे हैं। उनके सामने पड़ा है उस बरस का वह शीशम का दीवान।
उस बरस हमारे शहर में हिंदुओं ने शांतिप्रियता छोड़ दी थी। अबके ऐलान करके छोड़ी कि एक गाल पर तमाचा पड़ा तो दूसरा बढ़ा दिया, पर अब तीसरा गाल कहाँ से लावें ? हम मजबूर हैं, वे चीखे। पर सवार होकर त्रिशूल की नोंक पर देवी की पताका फहराने लगे कि जो हमारे संग हुआ है, वही हमें उनके संग करना है। पाप का बदला पाप से चुकेगा। साधु-संतों ने समाधि छोड़ दी और उपासना की एवज में ललकार गूँज उठी कि हमारी संतानें जाती रहीं, हमारी बेटियाँ लुटती रहीं, बेटो, हिजड़े हो क्या ? ए वीर शिवाजी की संतान, भगतसिंह राणाप्रताप के वंशज अर्जुन और भीम के पुत्रों, उट्ठो। उन दुष्टों की बस्तियों को श्मशान बना डालो। बहुत हो गई तुम्हारी भलमनसी। दैत्यों-पिशाचों के जुल्म बढ़े तो देवताओं को भी क्रोध आ गया। उट्ठो।
जागो।
बचाओ।
और निकल पड़े जत्थे के जत्थे हमारे शहर में मस्जिदों की नींव उखाड़ के अपने देवियों-देवताओं की लाशें खड़ी करने।
हमारे शहर की हवा सनसनाने लगी। उनकी मजबूरी से बूम-बूम गूजने लगी। जत्थे जोर-शोर से निकले, भभूत के बादल उड़ाते जो कभी भी धूल बनके हमारी आँखों में किचकिचा जाती, गंगाजल की नहरें बहाते, जो कभी भी खून बनके हम पर छींटे उछाल देतीं।
ज़ोरदार शोरदार मेला लगा। रंग इतने कि अबीर की आँधी हो, होली की मस्ती हो। यज्ञ हुए, जिनमें वीतराग की आड़ में पलती कायरता को तिलांजलि दे, भस्म का तिलक लगा और हाथों में धारदार धातु उछालकर सूरज की चिन्दियाँ कर डाली गईं और उन्हीं चमकते टुकड़ों को नोक पर लहराते हुए लोग गलियों में घुस गए। झूमते हुए सूरज को यों कब्जे में पाकर।
हम सहम गए सूरज की यह गत देखकर।
एक बच्चे की नज़र से लिखूँ ?’’ श्रुति पूछ रही है। उसके हाथ चुकंदर छीलने से लाल टपका रहे हैं। हमारा अनबॉन बच्चा ? जो यह सबदेखे, सुने, बताए ?’’
‘‘न।’’ हनीफ ने सिरे से ‘वीटो’ कर दिया। ‘‘एक तो’’ उसने कहा, ‘‘यह ढंग बहुत पुराना है, महाभारत काल से चला आ रहा है। दूसरे...’’ उसकी आवाज में शिद्दत है, ‘‘ख्वाब में भी हमें बच्चा नहीं चाहिए, जिसे यह वक्त विरासत में मिले ?’’
जो पैदा न हुआ हो, उस बच्चे की गवाही का खयाल आ सकता है, चाहे पलभर को ही तो मैं इतना क्यों डर रही हूँ ? परछाई की तरह लग जाऊँ और नकल बनाती जाऊँ। नकल से क्या डरना ?
‘‘हम क्यों डरें ? हम इधर रहते हैं। तुम्हारा दोस्त नाहक फ़ियर-साइकोसिस फैलाता है। उसे मजा आता है।’’ श्रुति शिकायत करती है।
वे ऊपर फ्लैट में बैठे हैं। जूठी प्लेटों का अंबार सामने है। अभी-अभी शरद नीचे अपने घर चला गया। उसके पहले तीनों साथ खा-पी रहे थे, गप्पिया रहे थे और मैं खड़ी थी कि सुनूँ उतारू, अनसुना करूँ ? प्लेटों में तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची खानेवालों ने एक तरफ़ सरका दिए हैं। शरद का आखि़री जुमला अभी तक हवा में तिर रहा है कि ‘‘शहर में आग लगी है, तुम हँस रहे हो ?’’
वहीं से मैं ठान लेती हूँ उतारूँ।
‘‘तुम ह्यूमेलेस हो, हनीफ श्रुति को चिढ़ाता है। शरद छेड रहा था, वह जानता है कि तुम बमक उठोगी।’’
‘‘कहीं नहीं छेड़-बेड़। तुम्हारा दोस्त है एकदम ह्यूमरलेस बेटा, वह भी एकदम टू मच ह्यूमरफ़ुल बाप का।’’ श्रुति शुरू गुस्से से करती है, मगर ख़त्म मुस्कराकर, जब दद्दू का ज़िक्र आ जाता है।
‘‘आग तो लगी ही है।’’
‘‘पर यहाँ नहीं। वहाँ।’’ श्रुति टोकती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i