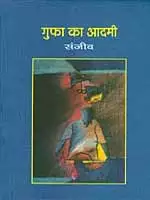|
कहानी संग्रह >> गुफा का आदमी गुफा का आदमीसंजीव
|
239 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है श्रेष्ठ कहानी संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
रूप, अन्तर्वस्तु, गुण और मात्रा-सभी स्तरों पर आठवें और नवें दशक की हिन्दी
कहानी को जिन कथाकारों ने एक सम्मानजनक मुकाम तक पहुँचाया है, संजीव उनमें प्रथम पंक्ति में आते हैं।
अन्तर्वस्तु और उपजीव्य स्तर पर संजीव ने अब तक कई अनछुए और वर्जित बीहड़ों की यात्रा की हैं,नये प्रतिमान गढ़े हैं और रूप के स्तर पर भाषा और शिल्प, व्यंजना और विन्यास के नये-नये सम्भार-सौष्ठव सिरजे हैं। बावजूद इसके आज भी वे अपनी इसी मान्यता पर कायम हैं कि कहानी प्रथमतः कहानी होती है, बाद में कुछ और।
संजीव की कहानियों के इस जाने-पहचाने चेहरे के बावजूद, उनके इस संग्रह की कहानियाँ थोड़ी भिन्न हैं। ये मात्र शोषक-शोषित, लाभ-लोभ के हड़बोंग और किन्ही लिंग, सम्प्रदाय या जातीय अन्तर्विरोधी तक जाकर ही नहीं ठहर जातीं, बल्कि इसके आगे जाकर करवट लेते काल के बीच नीयत और नियति के द्वन्द्व में मनुष्य की तकदीर का विश्लेषण करती हैं। संग्रह की ज्वार, योद्धा, बुद्धपथ राख आदि हों या गुफा का आदमी इससे पहले नहीं लिखी जा सकती थीं। निश्चित तौर पर यह संजीव की देश-काल सापेक्ष कथा-यात्रा का प्रस्थान बिन्दु है। ये कहानियाँ आज भी पाठक को यथार्थ और संवेदना के उस तलस्पर्शी लोक तक ले जाकर सभ्यता की इस आदिम पहेली के रूपरू खड़ा कर देती हैं-सच-सच बताओ, तुम गुफा के अन्दर हो या बाहर ?
संजीव का यह कहानी-संग्रह प्रकाशित करते हुए भारतीय ज्ञानपीठ को प्रसन्नता है।
अन्तर्वस्तु और उपजीव्य स्तर पर संजीव ने अब तक कई अनछुए और वर्जित बीहड़ों की यात्रा की हैं,नये प्रतिमान गढ़े हैं और रूप के स्तर पर भाषा और शिल्प, व्यंजना और विन्यास के नये-नये सम्भार-सौष्ठव सिरजे हैं। बावजूद इसके आज भी वे अपनी इसी मान्यता पर कायम हैं कि कहानी प्रथमतः कहानी होती है, बाद में कुछ और।
संजीव की कहानियों के इस जाने-पहचाने चेहरे के बावजूद, उनके इस संग्रह की कहानियाँ थोड़ी भिन्न हैं। ये मात्र शोषक-शोषित, लाभ-लोभ के हड़बोंग और किन्ही लिंग, सम्प्रदाय या जातीय अन्तर्विरोधी तक जाकर ही नहीं ठहर जातीं, बल्कि इसके आगे जाकर करवट लेते काल के बीच नीयत और नियति के द्वन्द्व में मनुष्य की तकदीर का विश्लेषण करती हैं। संग्रह की ज्वार, योद्धा, बुद्धपथ राख आदि हों या गुफा का आदमी इससे पहले नहीं लिखी जा सकती थीं। निश्चित तौर पर यह संजीव की देश-काल सापेक्ष कथा-यात्रा का प्रस्थान बिन्दु है। ये कहानियाँ आज भी पाठक को यथार्थ और संवेदना के उस तलस्पर्शी लोक तक ले जाकर सभ्यता की इस आदिम पहेली के रूपरू खड़ा कर देती हैं-सच-सच बताओ, तुम गुफा के अन्दर हो या बाहर ?
संजीव का यह कहानी-संग्रह प्रकाशित करते हुए भारतीय ज्ञानपीठ को प्रसन्नता है।
ज्वार
माँ बताती थीं कि हम फरीदपुर के ‘सोनारदीघी’ गाँव से आये हैं, जो अब पाकिस्तान है। सन् 71 में ‘बांग्लादेश’ बन जाने के बाद भी वे इसे
‘पाकिस्तान’ ही कहती रहीं। उस पार से आये कई बंगाली
‘ओ पार बांग्ला, ए पार बांग्ला’ (उस पार का बंगाल, इस
पार का बंगाल) कहकर दोनों को जोड़े रहते, माँ ही ऐसा न कर सकीं। जाने
कौन-सी ग्रन्थि थी ! ऐसा भी नहीं कि ‘उस पार’ के लिए
उन्होंने अपने खिड़की-दरवाजे पूरी तरह से बन्द कर लिये थे। ‘इस
पार’ आ जाने के बाद भी काफी दिनों तक उनकी जड़े तड़पती रहीं
वहाँ के खाद-पानी के लिए—वे लहलहाते धान के खेत, नारियल के
लम्बे-ऊँचे पेड़, आम-जामुन के स्वाद, चौड़ी-चौड़ी हिलकोरें लेतीं नदियाँ,
नदियों के पालने में झूलती नावें, रात में नावों की लालटेनों से लहरों पर
दूर तक फैली ललाई, सँवलाई-सँवलाईं रातों में नावों से उड़-उड़कर आते
भाटियाली गीत-
मॅन माझी तोर बइठाले रे,
आमी आर बाइते पारलॉम ना;
बाइते-बाइते जीवॅन गेलो,
कूलेर देखा पाइलॉम ना।
आमी आर बाइते पारलॉम ना;
बाइते-बाइते जीवॅन गेलो,
कूलेर देखा पाइलॉम ना।
(हे मन के माझी, अपनी डाँड़ सम्भालो, मुझसे अब और नहीं खेया जाता।
खेते-खेते जीवन बीता, लेकिन कहीं किनारा नहीं दिखा...।)
छुलक-छुलक पानी की आवाज मानो ताल देती और गीत की टेर दिगन्त तक फैलती जाती।
माँ अक्सर उन ‘टोंगा’ (मचानों) का जिक्र करतीं, जिन पर पानी से बचने के लिए पूरा परिवार बैठा होता। आम-जामुन के साथ-साथ कभी-कभी ‘सिलेट करवे’ के कमला नींबू की याद करतीं जिनके सामने दार्जिलिंग और नागपुर के सन्तरे उन्हें फीके लगते। मछलियाँ तो मछलियाँ, कच्चू डाँटा (अरबी की डण्ठल) मोचाई (केले के फूल), ओल (सूरन) की उम्दा सब्जी बनातीं कि हमें पूछना पड़ता, ‘‘माँ तुमने इतनी बढ़िया तरकारी बनाना कहाँ से सीखा ?’’
‘‘वहीं से, वहाँ की औरतों के बारे में कहावत है कि जूते का तलवा भी राँध दें तो खानेवाले उंगलियाँ चाटते रह जाएँ।’’
‘‘सारा कुछ अच्छा ही अच्छा था तो आपलोग चले क्यों वहाँ से ?’’ हम पूछते। माँ हर बार इस प्रश्न पर मौन साध लेतीं।
मैं कभी इसके पहले ‘सोनारदीघी’ आयी नहीं लेकिन माँ ने इतनी बार इन चीज़ों का जिक्र किया था कि मन के किसी अन्तःपुर में एक सोनारदीघी बस गया है जहाँ सुविधानुसार मैं कभी नारियल, सुपारी के पेड़ों को एक ओर कर देती, कभी दूसरी ओर। कभी नदी को बगल में ले आती, कभी दूर कर देती। कभी सारा परिवेश ही कच्चू के बड़े-बड़े पत्तों से भर जाता, और कभी आम-जामुन के पेड़ों से...। आज सोनारदीघी आते हुए मेरे कल्पना-लोक में बार-बार खलल पड़ रहा है। नदी भी है, पेड़-पल्लव भी हैं, मगर कुछ अलग-से। लुंगियाँ पहने पुरुष, धोती एक भी नहीं। अलबत्ता औरतें साड़ी में ही हैं ! वह स्कूल जो अभी भी है, मगर पक्का बन गया है—माँ ने यहीं ककहरा सीखा होगा। दूसरा स्कूल भी तो हो सकता है ? ज्यादा टोक-टाक ठीक नहीं।
सन् 47 में पार्टीशन के समय सिर्फ माँ, नानी और नाना ही बॉर्डर पार कर पाये थे। दंगाइयों ने मझली मौसी का अपहरण कर लिया था, एक मामा मार डाले गये थे। बाकी छोटी मौसी और बड़के मामा वगैरह जैसे-तैसे जान बचाकर लौट गये थे सोनारदीघी। स्थिति सामान्य होने पर वे मिलने आये। तब तक हम बर्द्धमान में बस गये थे। मेरा जन्म बांग्लादेश बन जाने के बाद हुआ था। पाँच साल की हुई तभी अणिमा दी को देखा था। छोटकी मौसी अपनी इस सात साल की बेटी को लेकर अपने इस परिवार से मिलने आयी थीं। आज अणिमा दी को छोड़कर उस परिवार में कोई नहीं बचा। वे अपनी ससुराल से वापस सोनारदीघी आ गयी थीं। पत्रों से इतना भर ही मालूम हुआ था। ये भी दस साल पहले की बातें हैं। अब तो सालों से पत्रों का सिलसिला भी टूटा हुआ है।
क्या पता, कितने हिन्दू बचे हैं यहाँ। सुना था, बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद बहुत से मन्दिर तोड़ डाले गये थे। अभी तक इस रास्ते में एक भी मन्दिर नहीं मिला। खालिदा जिया के शासनकाल में मौलवाद फिर से लौट आया है। कैसे रहती होंगी अणिमा दी ?
क्या खूब विडम्बना है ? हमें भी यहाँ पश्चिम बंगाल में ‘ईस्ट बंगाल’ का माना जाता है-‘बांगाल !’ मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की फुटबाल प्रतियोगिता में ‘घोटी-बाटी’ (कलश-कटोरे) या ‘ईस्ट-वेस्ट’ का फर्क पूरी तरह से प्रेसीपिटेड कर जाता है। लोग हमारी जाति तक पर शक करते हैं। बेचारी अणिमा दी अपनी ही जन्म-भूमि, अपने ही वतन में विजातियों, विधर्मियों, के बीच निर्वासन भोगने को अभिशप्त हैं। हम इत्ता-सा बर्दाश्त नहीं कर पाते, ‘बांगाल’ कहते ही तिलमिला उठते हैं। कैसे सहती होंगी दीदी इसे आठों पहर ? मैं एक मुहाज़िर ज़ैनुल को जानती हूँ, उसका बाप बिहार से बांग्लादेश गया था, जो तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। मुक्ति संग्राम के बाद फिर उसे भागकर पश्चिमी पाकिस्तान जाना पड़ा। उनकी वफ़ादारी पर भारत में भी शक किया गया, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी...! उसने धर्म को एक मुकम्मिल और भरोसेमन्द आइडेण्टिटी एवं सुरक्षा कवच समझा, पर ऐसा हो नहीं पाया। इन्सानी मसले सियासत और मज़हब वाले तय करते हैं, वही तय करते हैं हमारी तक़दीरें...हमसे पूछा तक नहीं जाता। इथियोपिया, सोमालिया, तुर्की मध्य एशिया कैरेबियन कण्ट्रीज—कहाँ नहीं ! यहाँ भी तो वही...! समाजशास्त्री कहेंगे, सभ्यताओं और संस्कृतियों का यह एक सामान्य-सा अन्तःप्रवाह है। मगर आबादियों के इस विस्थापन में हुई बर्बादियों की दास्तान कौन सुनना चाहेगा ? एक तार जब टूटता है तो कितना कुछ टूट और छूट जाता है !
जुड़ता क्या है...गाँठ पर पनपा जीवन का नया अध्याय ! ओह ! इस मनहूस जैनुल की याद भी अभी ही आनी थी ! मेरे साथ का पुलिस का जवान सुहेल साइकिल पर चल रहा था और मैं रिक्शे पर थी। गाँव में प्रवेश करते ही एक चाले (झोंपड़ी) में चाय की दुकान पर कुछ लोग अड्डा जमाये हुए थे। मैंने पूछा, ‘‘दादा, एई ग्रामे नीहार सिंघॅ थाहेन कुथाय ?’’ (भाई, इस गाँव में नीहार सिंह कहाँ रहते हैं ?)।
जवाब में कई सवालिया आँखें मुझ पर उठ गयीं। मुझसे क्या भूल हुई ? अपने तईं तो मैंने पूरी सावधानी बरत रखी थी। जीन्स छोड़कर साड़ी पहन रखी थी मैंने, भाषा भी...न-न, भूल हुई ‘एई’ की जगह ‘हेई’ कहना चाहिए था। मैं कट कर रह गयी। पर अब तो जो होना था, हो चुका। अड्डेवालों में आपस में कानाफूसी हुई फिर एक साँवला-सा प्रौढ़ बोला, ‘‘की नाम कोइलेन, नीहार सींघॅ ?’’
(क्या नाम बोलीं, नीहार सिंह ?)
‘‘आज्ञें हें।’’
(जी हाँ।)
‘‘नीहार सिंघा बोइल्ला काऊ रे तो जानी ना..।’’
(नीहार नाम के किसी आदमी को तो जानता नहीं।)
‘‘सिंघॉ सोब पलाई गेछे।’’ (सारे सिंह भाग गये हैं।) एक सम्मिलित ठहाके का श्लेष मुझे तेजाब-सा भिगो गया।
‘‘आपनार बासा कुथाय ?’’ (आपका घर कहाँ है ?)
चुगली खाती मेरी भाषा विश्वसनीय नहीं थी, सो अब मुझे आंचलिक भाषा का दमन छोड़कर सीधे मानक बांग्ला पर उतरना पड़ा। मैंने बांग्ला में बताया, ‘‘मैं बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल से आयी हूँ। बँटवारे के समय यहीं से गये थे हमारे पूर्वज। कभी इस गाँव में एक उज्ज्वल सिंह हुआ करते थे। मैं उन्हीं की नातिन हूँ। नीहार सिंह मेरे मौसेरे बहनोई हुए और अणिमा दी मौसेरी बहन। इधर आयी थी तो सोचा अपना पुश्तैनी घर देख लूँ और परिवार के लोगों से मिलती चलूँ।’’
अब गाँव के कुछ और लोग भी जुटने लगे थे। वे आपस में बतियाकर मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में मैं सन्दिग्ध थी या निषिद्ध।
उस प्रौढ़ ने एक किशोर को पुकारा, ‘‘ताहिर ! जरा इन्हें सलाहुद्दीन शेख के घर पहुँचा आओ तो !’’
सलाहुद्दीन शेख ! यह क्या बात हुई। मुझे अपनी पसलियों में एक मनहूस किस्म के ख़ौफ की चुभन महसूस हुई।
कच्ची सड़क पर एक मध्ययुगीन बैलगाडी चली आ रही थी। बारिश से बचने के लिए उस पर बाँस, की चटाई का चन्दोवा तना था। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। दूर-दूर पर वही पुआल के छप्परवाले घर, कहीं-कहीं दो मंजिलें भी और टीन की छत भी। जहाँ-तहाँ केले के स्तम्भ थे, कहीं-कहीं बँसवारियाँ भी। सड़क के दोनों ओर नारियल के पेड़ थे, कुछ साबूत कुछ टूटे हुए या ठूँठ। शायद बार-बार की आने वाली झड़-झंझा (आँधी-तूफान) का प्रकोप था। खेतों में इस मौसम में उपजने वाली अन्न की बालियाँ लहरा रही थीं, कहीं-कहीं झींगा (तरोई) और दूसरी सब्जियाँ भी। थाने का सिपाही अपनी साइकिल घसीटते हुए ताहिर से बात कर रहा था। भाषा कहीं कहीं अबूझ हो जाती। इतना भर पता चला कि वह यहाँ मजूरी करने आया है। आज काम नहीं मिला, सो बेकार है। पता नहीं, कब तक काम मिलेगा। माँ-बाप कौन थे, कहाँ का मूल निवासी है, उसे कुछ पता नहीं।
मुझे ढाका के दूसरे शहरों के हजारों लावारिश बच्चों के बारे में बताया गया था कि उनमें से अधिसंख्य वे बच्चे थे जो बांग्लादेश युद्ध के दौरान बाहरी फौजियों के बलात्कार से जन्मे थे। उन अभागों को किसी ने नहीं अपनाया, अपने ही ढंग से वे जैसे-तैसे पले-बढ़े, जवान हुए। फिर उनके बच्चे हुए। लावारिशों की दूसरी खेप। भयंकर गरीबी, ऊपर से मँहगाई की मार। दिल्ली, मुम्बई, दुबई और लन्दन तक फैल गयी यह अमर बेलि।
सिपाही ने मेरी ओर इशारा कर ताहिर से कुछ कहा। ताहिर झेंपते हुए मेरे साथ-साथ चलने लगा, ‘‘मुझको भी साथ ले चलिए न दीदी, सभी तरह के काम कर सकता हूँ।’’
‘‘लेकिन मैं भला कैसे लिवा ले जा सकती हूँ तुम्हें ?’’
‘‘क्यों सलाहुद्दीन के लड़कों को ले जाने आयी हैं। मैं तो उनसे भी गरीब हूँ। उनके तो माँ-बाप भी हैं, जमीन भी है...नाव भी; मेरा तो कुछ भी नहीं।’’
मैं अवाक् रह गयी, ‘‘तुम्हें किसने बताया कि मैं सलाहुद्दीन के या किसी और के बच्चों को ले जाने आयी हूँ ? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैं तो नीहार सिंह का पता करने जा रही हूँ, जो मेरे मौसेरे बहनोई हैं।’’
‘‘ओह !’’ ताहिर निराश हो गया, फिर बोला, ‘‘लेकिन मैं यहाँ छह महीने से हूँ, नीहार सिंह या किसी हिन्दू परिवार का नाम नहीं सुना। खैर, देखिए, पूछिए शायद पता लग ही जाए। बस्ती तो यही है।’’
मैं एक-एक घर को देखती हूँ, ये घर होगा, नहीं वो, नहीं, ताहिर तो आगे बढ़ गया, शायद आगे...। माँ किसी नदी का जिक्र करती थीं, जिसका पानी ज्वार के समय मचान के नीचे तक फैल जाता। न अभी तक कोई मचान मिला, न नदी की झलक। एक घर के पास ताहिर आकर रुक गया, सिपाही ने साइकिल खड़ी कर दी, ‘‘यही है।’’
फूस की छाजन। एक कोने में एक बकरा बँधा था, दूसरे कोने में एक गाय, सामने मुर्गियाँ और उनके छोटे-छोटे चूजे चिक-चिक करते टहल रहे थे। बच्चे सिर पर टोपी लगाये मदरसे में पढ़ने जा रहे थे। टिपिकल मुसलमानी घर।
‘‘शेख मोशाय कहाँ हैं, देखिए आपसे मिलने आयी हैं।’’ सिपाही ने आवाज दी। उस घर से एक औरत निकली, फिर देखते-देखते दूसरे घरों से अन्य औरतें। कुछ मर्द भी। सभी आँखें फाड़-फाड़कर मुझे देखने लगे।
‘‘सलाहुद्दीन तो ढाका गये हैं, उनकी बहू है।’’ एक औरत ने बताया।
‘‘उन्हें ही बता दीजिए।’’ सिपाही सुहेल ने कहा।
‘‘नया आदमी देख रही हूँ।’’ आँखों पर हाथ की ओट बनाकर एक बूढ़ी ने मेरे चेहरे में झाँका। मैं झेंप गयी।
‘‘हिन्दू प्रेस रिपोर्टर हैं। बर्द्धमान से आयी हैं।’’
‘‘यहाँ...?’’
‘‘यहाँ अपने बहनोई किसी नीहार सिंह को ढूँढ़ने आयी हैं। कहती हैं, इनके पूर्वज इसी गाँव से गये थे।’’
बूढ़ी थोड़ी गम्भीर हुई, ‘‘थाने का परमिशन है ?’’
‘‘हाँ, तभी तो मैं साथ-साथ आया हूँ।’’
‘‘बूड़ी, ओ अंजुमन बूड़ी, देखो तो भारत से कौन आया है तुमसे मिलने।’’
‘‘अंजुमन बूड़ी !’’ शब्दों को मैंने चुभलाया। याद आया बर्द्धमान आयी थी। तब भी अणिमा दी का पुकारने का नाम ‘बूड़ी’ ही था। तो क्या अणिमा सचमुच ही ‘अंजुमन’ बन गयी और नीहार सलाहुद्दीन ?
अन्दर से तेज-तेज चलकर कोई स्त्री आयी और चौखट के फ्रेम में फ्रीज हो गयी, जैसे हुलास के वेग पर असमंजस की लगाम लग गयी हो। हाँ, वही गन्दुमी गोल चेहरा, चेहरे में जड़ी वही बड़ी-बड़ी बिल्लौरी आँखें !
मैं अपने को और रोक न सकी। मैंने दौड़कर अणिमा दी को बाँहों में भरकर भींच लिया। ‘‘दीदी ! दीदी ! मेरी दीदी। कितने दिन बाद देख रही हूँ अपनी अणिमा दी को। पहचाना मुझे, मैं तुम्हारी शिखा हूँ—गुड्डी।’’
‘‘छोड़ो मुझे, मैं किसी शिखा, किसी गुड्डी को नहीं जानती।’’
मुझे गहरा धक्का लगा। तो क्या मैं किसी मुर्दे को पकड़े हुए थी ? हाथों के बन्द ढीले पड़े। काफी औरतें जमा हो गयी थीं। मेरी स्थिति हास्यास्पद होती जा रही थी। मैं सफाई पर उतर आयी, ‘‘याद है दीदी, जब आप बर्द्धमान आयी थीं, मैं इत्ती-सी थी।’’ मैंने हाथ से पाँच साल के बच्चे का कद बताया, ‘‘मैं पाँच साल की थी, आप सात साल की। मुझे गोद में लेकर घूमा करती थीं। उठा नहीं पाती थीं पूरी तरह। एक बार लेकर गिर पड़ी थीं, इसके चलते आपको मार भी खानी पड़ी थी। यह रहा वह दाग भौंहों पर।’’
अणिमा दी फटी-फटी आँखों से मुझे घूरे जा रही थीं।
‘‘आपने मुझे कई बार बुलाया था, मरने से पहले मिल लो...याद है ? खेल-खेल में आपने मेरी शादी में मुझे झुमका देने की बात कही थी।’’
अणिमा दी काठ की पुतली-सी निर्विकार खड़ी थीं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूँ ? तमाशा तो बन ही गयी थी मैं। शर्म और अपमान की एक ठण्डी लहर शिराओं में रेंग रही थी। इतनी बाधाएँ पारकर, इतनी दूर चलकर तो आज उन्हें पाना नसीब हुआ, और आज भी वे न बोलीं तो कब बोलेंगी ?
सिपाही ने ऊबते हुए पूछा, ‘‘और कितनी देर लगेगी ?’’
‘‘छोड़ो ! उसे जब कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो आगे क्या पूछोगी।’’ पहले वाली प्रौढ़ा ने कहा, ‘‘जो बीत गयी सो बीत गयी। हाँ ! ननिहाल आयी हो तो दो कौर भात और मछली तो पेट में डालनी ही होगी।’’
‘‘लेकिन मौसी मैं तो...।’’
‘‘कोई लेकिन-वेकिन नहीं। हाँ, अगर मुसलमान के हाथ से खाने से तुम्हारा धरम भ्रष्ट हो जाए तो और बात है !’’
‘‘नहीं मौसी ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस जरा नहाना चाहती थी। सारी देह चिपचिपा रही है।’’
‘‘ये लो, बगल में ही तो नदी है। सभी लड़कियाँ जा रही हैं। दो डुबकी मार आओ न ! अंजुमन बूड़ी लिवा जाओ इसे भी..लेकिन ज्वार का कोई भरोसा नहीं, होशियार रहना।’’
उस दल में कोई दस-एक युवतियाँ और बच्चियाँ थीं, बूढ़ी एक भी नहीं, सो वे खुलकर बोल-बतिया रही थीं।
‘‘अच्छा दीदी, आपके बर्द्धमान से कलकत्ता कितनी दूर है ?’’ एक ने पूछा।
‘‘ट्रेन से डेढ़ घण्टा लगता है।’’
‘‘बहोत बड़ा शहर है न, जमीन के अन्दर रेल चलती है ?’’
‘‘हाँ।’’
‘‘आप कभी बैठी हैं ?’’
‘‘हाँ। कई बार।’’
छुलक-छुलक पानी की आवाज मानो ताल देती और गीत की टेर दिगन्त तक फैलती जाती।
माँ अक्सर उन ‘टोंगा’ (मचानों) का जिक्र करतीं, जिन पर पानी से बचने के लिए पूरा परिवार बैठा होता। आम-जामुन के साथ-साथ कभी-कभी ‘सिलेट करवे’ के कमला नींबू की याद करतीं जिनके सामने दार्जिलिंग और नागपुर के सन्तरे उन्हें फीके लगते। मछलियाँ तो मछलियाँ, कच्चू डाँटा (अरबी की डण्ठल) मोचाई (केले के फूल), ओल (सूरन) की उम्दा सब्जी बनातीं कि हमें पूछना पड़ता, ‘‘माँ तुमने इतनी बढ़िया तरकारी बनाना कहाँ से सीखा ?’’
‘‘वहीं से, वहाँ की औरतों के बारे में कहावत है कि जूते का तलवा भी राँध दें तो खानेवाले उंगलियाँ चाटते रह जाएँ।’’
‘‘सारा कुछ अच्छा ही अच्छा था तो आपलोग चले क्यों वहाँ से ?’’ हम पूछते। माँ हर बार इस प्रश्न पर मौन साध लेतीं।
मैं कभी इसके पहले ‘सोनारदीघी’ आयी नहीं लेकिन माँ ने इतनी बार इन चीज़ों का जिक्र किया था कि मन के किसी अन्तःपुर में एक सोनारदीघी बस गया है जहाँ सुविधानुसार मैं कभी नारियल, सुपारी के पेड़ों को एक ओर कर देती, कभी दूसरी ओर। कभी नदी को बगल में ले आती, कभी दूर कर देती। कभी सारा परिवेश ही कच्चू के बड़े-बड़े पत्तों से भर जाता, और कभी आम-जामुन के पेड़ों से...। आज सोनारदीघी आते हुए मेरे कल्पना-लोक में बार-बार खलल पड़ रहा है। नदी भी है, पेड़-पल्लव भी हैं, मगर कुछ अलग-से। लुंगियाँ पहने पुरुष, धोती एक भी नहीं। अलबत्ता औरतें साड़ी में ही हैं ! वह स्कूल जो अभी भी है, मगर पक्का बन गया है—माँ ने यहीं ककहरा सीखा होगा। दूसरा स्कूल भी तो हो सकता है ? ज्यादा टोक-टाक ठीक नहीं।
सन् 47 में पार्टीशन के समय सिर्फ माँ, नानी और नाना ही बॉर्डर पार कर पाये थे। दंगाइयों ने मझली मौसी का अपहरण कर लिया था, एक मामा मार डाले गये थे। बाकी छोटी मौसी और बड़के मामा वगैरह जैसे-तैसे जान बचाकर लौट गये थे सोनारदीघी। स्थिति सामान्य होने पर वे मिलने आये। तब तक हम बर्द्धमान में बस गये थे। मेरा जन्म बांग्लादेश बन जाने के बाद हुआ था। पाँच साल की हुई तभी अणिमा दी को देखा था। छोटकी मौसी अपनी इस सात साल की बेटी को लेकर अपने इस परिवार से मिलने आयी थीं। आज अणिमा दी को छोड़कर उस परिवार में कोई नहीं बचा। वे अपनी ससुराल से वापस सोनारदीघी आ गयी थीं। पत्रों से इतना भर ही मालूम हुआ था। ये भी दस साल पहले की बातें हैं। अब तो सालों से पत्रों का सिलसिला भी टूटा हुआ है।
क्या पता, कितने हिन्दू बचे हैं यहाँ। सुना था, बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद बहुत से मन्दिर तोड़ डाले गये थे। अभी तक इस रास्ते में एक भी मन्दिर नहीं मिला। खालिदा जिया के शासनकाल में मौलवाद फिर से लौट आया है। कैसे रहती होंगी अणिमा दी ?
क्या खूब विडम्बना है ? हमें भी यहाँ पश्चिम बंगाल में ‘ईस्ट बंगाल’ का माना जाता है-‘बांगाल !’ मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की फुटबाल प्रतियोगिता में ‘घोटी-बाटी’ (कलश-कटोरे) या ‘ईस्ट-वेस्ट’ का फर्क पूरी तरह से प्रेसीपिटेड कर जाता है। लोग हमारी जाति तक पर शक करते हैं। बेचारी अणिमा दी अपनी ही जन्म-भूमि, अपने ही वतन में विजातियों, विधर्मियों, के बीच निर्वासन भोगने को अभिशप्त हैं। हम इत्ता-सा बर्दाश्त नहीं कर पाते, ‘बांगाल’ कहते ही तिलमिला उठते हैं। कैसे सहती होंगी दीदी इसे आठों पहर ? मैं एक मुहाज़िर ज़ैनुल को जानती हूँ, उसका बाप बिहार से बांग्लादेश गया था, जो तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। मुक्ति संग्राम के बाद फिर उसे भागकर पश्चिमी पाकिस्तान जाना पड़ा। उनकी वफ़ादारी पर भारत में भी शक किया गया, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी...! उसने धर्म को एक मुकम्मिल और भरोसेमन्द आइडेण्टिटी एवं सुरक्षा कवच समझा, पर ऐसा हो नहीं पाया। इन्सानी मसले सियासत और मज़हब वाले तय करते हैं, वही तय करते हैं हमारी तक़दीरें...हमसे पूछा तक नहीं जाता। इथियोपिया, सोमालिया, तुर्की मध्य एशिया कैरेबियन कण्ट्रीज—कहाँ नहीं ! यहाँ भी तो वही...! समाजशास्त्री कहेंगे, सभ्यताओं और संस्कृतियों का यह एक सामान्य-सा अन्तःप्रवाह है। मगर आबादियों के इस विस्थापन में हुई बर्बादियों की दास्तान कौन सुनना चाहेगा ? एक तार जब टूटता है तो कितना कुछ टूट और छूट जाता है !
जुड़ता क्या है...गाँठ पर पनपा जीवन का नया अध्याय ! ओह ! इस मनहूस जैनुल की याद भी अभी ही आनी थी ! मेरे साथ का पुलिस का जवान सुहेल साइकिल पर चल रहा था और मैं रिक्शे पर थी। गाँव में प्रवेश करते ही एक चाले (झोंपड़ी) में चाय की दुकान पर कुछ लोग अड्डा जमाये हुए थे। मैंने पूछा, ‘‘दादा, एई ग्रामे नीहार सिंघॅ थाहेन कुथाय ?’’ (भाई, इस गाँव में नीहार सिंह कहाँ रहते हैं ?)।
जवाब में कई सवालिया आँखें मुझ पर उठ गयीं। मुझसे क्या भूल हुई ? अपने तईं तो मैंने पूरी सावधानी बरत रखी थी। जीन्स छोड़कर साड़ी पहन रखी थी मैंने, भाषा भी...न-न, भूल हुई ‘एई’ की जगह ‘हेई’ कहना चाहिए था। मैं कट कर रह गयी। पर अब तो जो होना था, हो चुका। अड्डेवालों में आपस में कानाफूसी हुई फिर एक साँवला-सा प्रौढ़ बोला, ‘‘की नाम कोइलेन, नीहार सींघॅ ?’’
(क्या नाम बोलीं, नीहार सिंह ?)
‘‘आज्ञें हें।’’
(जी हाँ।)
‘‘नीहार सिंघा बोइल्ला काऊ रे तो जानी ना..।’’
(नीहार नाम के किसी आदमी को तो जानता नहीं।)
‘‘सिंघॉ सोब पलाई गेछे।’’ (सारे सिंह भाग गये हैं।) एक सम्मिलित ठहाके का श्लेष मुझे तेजाब-सा भिगो गया।
‘‘आपनार बासा कुथाय ?’’ (आपका घर कहाँ है ?)
चुगली खाती मेरी भाषा विश्वसनीय नहीं थी, सो अब मुझे आंचलिक भाषा का दमन छोड़कर सीधे मानक बांग्ला पर उतरना पड़ा। मैंने बांग्ला में बताया, ‘‘मैं बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल से आयी हूँ। बँटवारे के समय यहीं से गये थे हमारे पूर्वज। कभी इस गाँव में एक उज्ज्वल सिंह हुआ करते थे। मैं उन्हीं की नातिन हूँ। नीहार सिंह मेरे मौसेरे बहनोई हुए और अणिमा दी मौसेरी बहन। इधर आयी थी तो सोचा अपना पुश्तैनी घर देख लूँ और परिवार के लोगों से मिलती चलूँ।’’
अब गाँव के कुछ और लोग भी जुटने लगे थे। वे आपस में बतियाकर मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में मैं सन्दिग्ध थी या निषिद्ध।
उस प्रौढ़ ने एक किशोर को पुकारा, ‘‘ताहिर ! जरा इन्हें सलाहुद्दीन शेख के घर पहुँचा आओ तो !’’
सलाहुद्दीन शेख ! यह क्या बात हुई। मुझे अपनी पसलियों में एक मनहूस किस्म के ख़ौफ की चुभन महसूस हुई।
कच्ची सड़क पर एक मध्ययुगीन बैलगाडी चली आ रही थी। बारिश से बचने के लिए उस पर बाँस, की चटाई का चन्दोवा तना था। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। दूर-दूर पर वही पुआल के छप्परवाले घर, कहीं-कहीं दो मंजिलें भी और टीन की छत भी। जहाँ-तहाँ केले के स्तम्भ थे, कहीं-कहीं बँसवारियाँ भी। सड़क के दोनों ओर नारियल के पेड़ थे, कुछ साबूत कुछ टूटे हुए या ठूँठ। शायद बार-बार की आने वाली झड़-झंझा (आँधी-तूफान) का प्रकोप था। खेतों में इस मौसम में उपजने वाली अन्न की बालियाँ लहरा रही थीं, कहीं-कहीं झींगा (तरोई) और दूसरी सब्जियाँ भी। थाने का सिपाही अपनी साइकिल घसीटते हुए ताहिर से बात कर रहा था। भाषा कहीं कहीं अबूझ हो जाती। इतना भर पता चला कि वह यहाँ मजूरी करने आया है। आज काम नहीं मिला, सो बेकार है। पता नहीं, कब तक काम मिलेगा। माँ-बाप कौन थे, कहाँ का मूल निवासी है, उसे कुछ पता नहीं।
मुझे ढाका के दूसरे शहरों के हजारों लावारिश बच्चों के बारे में बताया गया था कि उनमें से अधिसंख्य वे बच्चे थे जो बांग्लादेश युद्ध के दौरान बाहरी फौजियों के बलात्कार से जन्मे थे। उन अभागों को किसी ने नहीं अपनाया, अपने ही ढंग से वे जैसे-तैसे पले-बढ़े, जवान हुए। फिर उनके बच्चे हुए। लावारिशों की दूसरी खेप। भयंकर गरीबी, ऊपर से मँहगाई की मार। दिल्ली, मुम्बई, दुबई और लन्दन तक फैल गयी यह अमर बेलि।
सिपाही ने मेरी ओर इशारा कर ताहिर से कुछ कहा। ताहिर झेंपते हुए मेरे साथ-साथ चलने लगा, ‘‘मुझको भी साथ ले चलिए न दीदी, सभी तरह के काम कर सकता हूँ।’’
‘‘लेकिन मैं भला कैसे लिवा ले जा सकती हूँ तुम्हें ?’’
‘‘क्यों सलाहुद्दीन के लड़कों को ले जाने आयी हैं। मैं तो उनसे भी गरीब हूँ। उनके तो माँ-बाप भी हैं, जमीन भी है...नाव भी; मेरा तो कुछ भी नहीं।’’
मैं अवाक् रह गयी, ‘‘तुम्हें किसने बताया कि मैं सलाहुद्दीन के या किसी और के बच्चों को ले जाने आयी हूँ ? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैं तो नीहार सिंह का पता करने जा रही हूँ, जो मेरे मौसेरे बहनोई हैं।’’
‘‘ओह !’’ ताहिर निराश हो गया, फिर बोला, ‘‘लेकिन मैं यहाँ छह महीने से हूँ, नीहार सिंह या किसी हिन्दू परिवार का नाम नहीं सुना। खैर, देखिए, पूछिए शायद पता लग ही जाए। बस्ती तो यही है।’’
मैं एक-एक घर को देखती हूँ, ये घर होगा, नहीं वो, नहीं, ताहिर तो आगे बढ़ गया, शायद आगे...। माँ किसी नदी का जिक्र करती थीं, जिसका पानी ज्वार के समय मचान के नीचे तक फैल जाता। न अभी तक कोई मचान मिला, न नदी की झलक। एक घर के पास ताहिर आकर रुक गया, सिपाही ने साइकिल खड़ी कर दी, ‘‘यही है।’’
फूस की छाजन। एक कोने में एक बकरा बँधा था, दूसरे कोने में एक गाय, सामने मुर्गियाँ और उनके छोटे-छोटे चूजे चिक-चिक करते टहल रहे थे। बच्चे सिर पर टोपी लगाये मदरसे में पढ़ने जा रहे थे। टिपिकल मुसलमानी घर।
‘‘शेख मोशाय कहाँ हैं, देखिए आपसे मिलने आयी हैं।’’ सिपाही ने आवाज दी। उस घर से एक औरत निकली, फिर देखते-देखते दूसरे घरों से अन्य औरतें। कुछ मर्द भी। सभी आँखें फाड़-फाड़कर मुझे देखने लगे।
‘‘सलाहुद्दीन तो ढाका गये हैं, उनकी बहू है।’’ एक औरत ने बताया।
‘‘उन्हें ही बता दीजिए।’’ सिपाही सुहेल ने कहा।
‘‘नया आदमी देख रही हूँ।’’ आँखों पर हाथ की ओट बनाकर एक बूढ़ी ने मेरे चेहरे में झाँका। मैं झेंप गयी।
‘‘हिन्दू प्रेस रिपोर्टर हैं। बर्द्धमान से आयी हैं।’’
‘‘यहाँ...?’’
‘‘यहाँ अपने बहनोई किसी नीहार सिंह को ढूँढ़ने आयी हैं। कहती हैं, इनके पूर्वज इसी गाँव से गये थे।’’
बूढ़ी थोड़ी गम्भीर हुई, ‘‘थाने का परमिशन है ?’’
‘‘हाँ, तभी तो मैं साथ-साथ आया हूँ।’’
‘‘बूड़ी, ओ अंजुमन बूड़ी, देखो तो भारत से कौन आया है तुमसे मिलने।’’
‘‘अंजुमन बूड़ी !’’ शब्दों को मैंने चुभलाया। याद आया बर्द्धमान आयी थी। तब भी अणिमा दी का पुकारने का नाम ‘बूड़ी’ ही था। तो क्या अणिमा सचमुच ही ‘अंजुमन’ बन गयी और नीहार सलाहुद्दीन ?
अन्दर से तेज-तेज चलकर कोई स्त्री आयी और चौखट के फ्रेम में फ्रीज हो गयी, जैसे हुलास के वेग पर असमंजस की लगाम लग गयी हो। हाँ, वही गन्दुमी गोल चेहरा, चेहरे में जड़ी वही बड़ी-बड़ी बिल्लौरी आँखें !
मैं अपने को और रोक न सकी। मैंने दौड़कर अणिमा दी को बाँहों में भरकर भींच लिया। ‘‘दीदी ! दीदी ! मेरी दीदी। कितने दिन बाद देख रही हूँ अपनी अणिमा दी को। पहचाना मुझे, मैं तुम्हारी शिखा हूँ—गुड्डी।’’
‘‘छोड़ो मुझे, मैं किसी शिखा, किसी गुड्डी को नहीं जानती।’’
मुझे गहरा धक्का लगा। तो क्या मैं किसी मुर्दे को पकड़े हुए थी ? हाथों के बन्द ढीले पड़े। काफी औरतें जमा हो गयी थीं। मेरी स्थिति हास्यास्पद होती जा रही थी। मैं सफाई पर उतर आयी, ‘‘याद है दीदी, जब आप बर्द्धमान आयी थीं, मैं इत्ती-सी थी।’’ मैंने हाथ से पाँच साल के बच्चे का कद बताया, ‘‘मैं पाँच साल की थी, आप सात साल की। मुझे गोद में लेकर घूमा करती थीं। उठा नहीं पाती थीं पूरी तरह। एक बार लेकर गिर पड़ी थीं, इसके चलते आपको मार भी खानी पड़ी थी। यह रहा वह दाग भौंहों पर।’’
अणिमा दी फटी-फटी आँखों से मुझे घूरे जा रही थीं।
‘‘आपने मुझे कई बार बुलाया था, मरने से पहले मिल लो...याद है ? खेल-खेल में आपने मेरी शादी में मुझे झुमका देने की बात कही थी।’’
अणिमा दी काठ की पुतली-सी निर्विकार खड़ी थीं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूँ ? तमाशा तो बन ही गयी थी मैं। शर्म और अपमान की एक ठण्डी लहर शिराओं में रेंग रही थी। इतनी बाधाएँ पारकर, इतनी दूर चलकर तो आज उन्हें पाना नसीब हुआ, और आज भी वे न बोलीं तो कब बोलेंगी ?
सिपाही ने ऊबते हुए पूछा, ‘‘और कितनी देर लगेगी ?’’
‘‘छोड़ो ! उसे जब कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो आगे क्या पूछोगी।’’ पहले वाली प्रौढ़ा ने कहा, ‘‘जो बीत गयी सो बीत गयी। हाँ ! ननिहाल आयी हो तो दो कौर भात और मछली तो पेट में डालनी ही होगी।’’
‘‘लेकिन मौसी मैं तो...।’’
‘‘कोई लेकिन-वेकिन नहीं। हाँ, अगर मुसलमान के हाथ से खाने से तुम्हारा धरम भ्रष्ट हो जाए तो और बात है !’’
‘‘नहीं मौसी ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस जरा नहाना चाहती थी। सारी देह चिपचिपा रही है।’’
‘‘ये लो, बगल में ही तो नदी है। सभी लड़कियाँ जा रही हैं। दो डुबकी मार आओ न ! अंजुमन बूड़ी लिवा जाओ इसे भी..लेकिन ज्वार का कोई भरोसा नहीं, होशियार रहना।’’
उस दल में कोई दस-एक युवतियाँ और बच्चियाँ थीं, बूढ़ी एक भी नहीं, सो वे खुलकर बोल-बतिया रही थीं।
‘‘अच्छा दीदी, आपके बर्द्धमान से कलकत्ता कितनी दूर है ?’’ एक ने पूछा।
‘‘ट्रेन से डेढ़ घण्टा लगता है।’’
‘‘बहोत बड़ा शहर है न, जमीन के अन्दर रेल चलती है ?’’
‘‘हाँ।’’
‘‘आप कभी बैठी हैं ?’’
‘‘हाँ। कई बार।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i