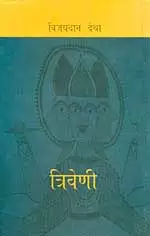|
कहानी संग्रह >> त्रिवेणी त्रिवेणीविजयदान देथा
|
109 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है तीडा राव इस्टूखाँ और भगवान की मौत, तीन उपन्यासिकाओँ के नायकों का अपूर्व संगम....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
राजस्थानी और हिन्दी के शीर्षस्थ कथाकार विजयदान देथा (बिज्जी) की तीन
उपन्यासिकाओं ‘तीडाराव’
‘इस्टूखाँ’ और भगवान की
मौत, के नायकों का अपूर्व संगम है-त्रिवेणी।
बिज्जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लोककथा की आत्मा को जीवित रखते हुए कहानी या उपन्यास के माध्यम से कथानक का सृजन इस तरह करते हैं कि बुद्धिजीवी ही नहीं, आम पाठक भी उसका आनन्द उठा सकता हैं।
लोक कथाओं को आधुनिकता देने की विलक्षण प्रतिभा बिज्जी के पास है। इन तीन कथाओं का विन्यास उन्होंने अत्यन्त कुशलता से किया है कि वे तीन कथानक भी है और व्यक्तित्व के तीन रूप भी। ये अत्यन्त रोचक और मार्मिक कहानियाँ हैं जो बिज्जी की कलात्मक तूलिका से विविध रंग-रूप लेती हैं। इतना ही नहीं, ये ऐसी कहानियाँ हैं जो बिना बोझिल हुए जीवन के लिए रोचक ढंग से अनुपम शिक्षा देती हैं।
आशा है, विजयदान देथा की यह मार्मिक, सुन्दर लोककथा-त्रयी ‘त्रिवेणी’ हिन्दी के सह्रदय पाठकों को आकर्षित करेगी।
बिज्जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लोककथा की आत्मा को जीवित रखते हुए कहानी या उपन्यास के माध्यम से कथानक का सृजन इस तरह करते हैं कि बुद्धिजीवी ही नहीं, आम पाठक भी उसका आनन्द उठा सकता हैं।
लोक कथाओं को आधुनिकता देने की विलक्षण प्रतिभा बिज्जी के पास है। इन तीन कथाओं का विन्यास उन्होंने अत्यन्त कुशलता से किया है कि वे तीन कथानक भी है और व्यक्तित्व के तीन रूप भी। ये अत्यन्त रोचक और मार्मिक कहानियाँ हैं जो बिज्जी की कलात्मक तूलिका से विविध रंग-रूप लेती हैं। इतना ही नहीं, ये ऐसी कहानियाँ हैं जो बिना बोझिल हुए जीवन के लिए रोचक ढंग से अनुपम शिक्षा देती हैं।
आशा है, विजयदान देथा की यह मार्मिक, सुन्दर लोककथा-त्रयी ‘त्रिवेणी’ हिन्दी के सह्रदय पाठकों को आकर्षित करेगी।
प्रस्तुति
सरस्वती सबसे पहले वाक् या वाणी है। इसलिए लोक-सर्जना उसकी औरस बेटी है।
सरलता, चंचलता, उछाह इसका स्वभाव है, पलभर को सकनी (शांत) नही बैठ सकती।
इसके बरक्स सरस्वती की एक और परम्परा है-पाडित्य की। वह भी हजारों वर्षों
तक मौखिक यात्रा करती रही, पर इस तरह हँसते-खेलते-बढ़ते हुए नहीं, वहाँ
रत्न-भंडार को सुरक्षित ले जाने की जद्दोजहद थी-शायद इसलिए तमाम घन, जटा
(पाठ) जैसे जटिल पहरेदारी आठों पहर होती रही। दोनों हाथ खोलकर
बस्ती
के बीचोंबीच नाचते-गाते जाने में और पेटीबंद खजाने को जंगल की राह ले जाने
में जो अंतर है, वही अंतर लोक और वेद में
है।
लोक साहित्य गामीण जनता और दादी-नानियों की पीठ पर सवारी गाँठकर बढता है।
यही कारण है कि पहले वह कान, आँख आदि इंद्रियों और काया की भाषा में
मस्तिष्क में प्रवेश करता फिर सांसो में नसों में बस जाता है और प्राण
रहते साथ नहीं छोड़ता। लोक का यही जन्मजात
है।
वक्ता और श्रोता की सृजन-प्रतिभा लोकसाहित्य में हमेशा कुछ घटाती-बढ़ाती
रहती है और कई रंगों में रंगती है। वह सुनने में सहज लेकिन गुनने में गूढ़
हैं। आप लोककथाओं, कविताओं, सूक्तियों, कहावतों को जितना खोलना चाहें, या
आपमें खोलने का जितना माद्दा हो, वे खुलती चली जाती है। एक कथा को उठा
लीजिए लगता है आख्यानों का पुलिंदा मिल गया हो। पाश्चात्य कहानी के
शास्त्र में बंधे लोग शायद ही समझ पाएँ कि हमारे पास लोक में एक पूरा
कथा-विधान और विवैंयों जैसी रेशेदारी और लोच है। इसे या तो देवेन्द्र
सत्यार्थी, कोमल कोठारी श्याम परमार जैले लोक-साधक समझते थे, या विजयदान
देथा समझते हैं कि लोक का कितना बड़ा रंग-संसार है और उसके पास किस
सलाहियत से जाना चाहिए।
लोक को ‘ड्कोड’ करना क्या होता है यह आप देथा जी की ‘बातां’ री फुलवाड़ी’ ‘घाव करे गंभीर’ जैसी ग्रंथमालाओं में, उनकी कथा कहानियों में और यहाँ इस ‘त्रिवेणी में नहा कर देख सकते हैं। देथा जी ने सरलता में छिपी गहनता को अनावृत करने में जीवन खपा दिया है। अब आज के संगणक-बिज्जुओं को यह समझने से तो रहे कि इस ‘डिकोडिग’ की क्या उलटबासी है क्योंकि उनकी निगाह में जटिल या सूत्र कोल भाषाई सम्प्रेषण या दूसरे विस्तारों में खोलना ही डिकोडिंग है।
बिज्जी हिन्दी के शार्षस्थानीय कथाकारों में हैं, परन्तु बहुत कम हिन्दी पाठकों को पता होगा कि वे उनकी जो रचना पढ़ रहे हैं वह प्रायः राजस्थानी में लिखी रचनाओं का पुनर्पाठ है। पहले देथा जी अपनी रचना राजस्थानी में लिखते है, फिर हिन्दी में उसका पुनर्सृजन करते हैं। मूल कथा वे हिन्दी में नहीं लिख सकते यह कौन कहेगा, परन्तु वे लोकभाषा में सोचने और अनुभव करने को उसी भाषा में व्यक्त करने का अपना अभ्यास बनाए और बचाए रखना चाहते हैं। संभवतः ‘त्रिवेणी’ के साथ भी यही हुआ हो और देथा जी के तीडाराव, इस्टूखाँ राजस्थानी पाठक के माथे में पहले से ही चक्कर काट रहे हों।
लोकसाहित्य का दिल बहुत बड़ा होता है। लोकगायक से लगातार कथावाचक, साधारण किस्सागो और साहित्यकार सभी उसका अपनी तरह से उल्था या सृजनान्तरण करते रहते हैं। परन्तु लोकसाहित्य सबसे पहले लोकहृदय की माँग करता है, यानी वह हदृय जो उसे बाजारू इस्तेमाल की चीज न समझे और उसकी मूल भावना, या आत्मा को संरक्षित कर सके। लोकसाहित्य को पूरी तरह आत्मसात कर लेने के बाद कोई भले ही आसमान नाप ले उसे ऐतराज नहीं होता; पर अश्रद्ध कृत्रिम और स्वर्थसाधक, न लोक की आत्मा छू पाता है न लोक-साहित्य की। उसका हाथ सिर्फ एक मरा हुआ ढाँचा ही लगता है। बहरहाल।
विजयदान देथा की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वे लोककथा की आत्मा को जीवित रखते हुए उसका पुनः सृजन इस तरह करते हैं कि नागरिक या बौद्धिक भी उसका आस्वाद ले सके। यह लेखक की ऐसी शक्ति है जिसे विरुद्धों के नहीं तो, विभिन्नों के सामंजस्य की शक्ति कह सकते हैं, जो ब्राह्मवरण बेधकर अंतःकरण की एकता दिखाती है। हम चोहे तो इसे स्वीकार न करें लेकिन हर एक के हृदय की किसी तह में ‘लोक’ की सहज निश्छलता के लिए एक जगह ज़रूरी होती है। अगर देथा जी इस रहस्य को और अपनी शक्ति को स्वयं नहीं पहचानते तो शायद ठेठ लोक कथाओं, जन श्रुतियों और कई अविश्वनीय संयोगों की अत्याधुनिकता भाषा के प्रबुद्ध पाठकों के बीच इतनी फक्कड़ तबीयत से नहीं रखते। स्वयं ‘त्रिवेणी’ में ही ऐसे चरित नायक, ऐसे संयोग और ऐसी फेंटेसियां हैं जिनपर आधुनिक प्रबुद्ध पाठक रास्ता चलते भरोसा नहीं करेगा भरोसे के इस तत्त्व को लोक-विश्वास के हवाले कर देथा को इस तरह रचते हैं मानों तमाम असंभव संयोग चरित नायक की मिथकीय उपलब्धियों या विडम्बनाएं हों। अथवा यह इस कास्मिक तंत्र को कोई अदृश्य अनपहचाना चक्र हो, जहाँ असम्भव को भी उस नाम से पुकारने की गुंजायश न हो। अक्सर देथा जी की कथा के यहाँ तो चरित्र, प्रतीक के किसी महीन अर्थ गुँथाकर अपना स्थूल रूप खो देते हैं और कथाएं शरीर त्याग कर कोई जीवननार्थ उदघाटित करती हैं। शायद इसलिए उनका लोकलेखन, आधुनिक चारितार्थता हो पाता है। यानी लोक भी रहता है और आधुनिक भी।
देथा जी ने यह चीज़ यों हो नहीं पायीं, उन्होंने स्थाई रूप से राजस्थान के बोरुन्दा गाँव को अपनी सृजन- भूमि बनाया है। ऐसे कम बड़े लेखक होंगे जो दुनिया भर से जुड़े हों और जिनका आशियाँ सुदूर ग्राम में हो। जेथा जी के दिल्ली और मास्कों तक उड़े अन्नतः बोरुन्दा में ही लैंड करते हैं। लोक से यह अनवरत अविच्छिन्न ,सम्बन्ध उन नारों पर बहुत भारी पड़ता हैं जो जड़ो से जुड़ने का हल्ला मचाते हैं। देथा जी का सृजन और जीवन यह बताता है कि आधुनिक होने के लिए सहज ग्रामीणता छोडना ज़रूरी नहीं है। जो लेखक रचना में विरुद्धो या विभिन्नों का सामांजस्य करने पर तुला हो, वह अगर अपने जीवन में ही यह न कर सके तो फटे बाँस की बाँसुरी जैसा होगा।
बिज्जी की ‘त्रिव्रेणी’ तीन उपन्यासिकाओं ‘तीडाराव’ ‘इस्टूखाँ और ‘भगवान की मौत’ का संकलन है। हालाँकि शीर्षक की व्याख्या से आलोचना प्रारम्भ करना एक ऐसी घटिया सी शुरूआत है। परन्तु यो तीन कथाएं जो परस्पर जुड़ी भी है और अलग भी- मानो उदगम से निकली तीन धाराएँ पर्वत श्रृंखला के तीन ग या किसी कुँआरी लड़की के घने बालों की तीन चोटियाँ हैं ये कथाएँ दोस्तों की तरह साथ भी है और अलग भी। तीनों चरित नायक संयोगों के हिचकोले खाते हैं। ‘तीडाराव और भगवान की मोत’ के चरित्र नायक के तो नाम भी एक ही है और अनेक संयोग समान हैं। मिस्टूखाँ का बेटा ‘इस्टूखाँ’ तो खुद जिन्दगी घड़ता है। पर बापड़े पर हरसिंहार के फूल जैसे टपकते संयोग एक तरह की आफत ही हैं। संयोगों पर इन कविताओं को विभिन्न रंग-रूप और व्यक्तित्व कर देता है। इससे एक संकेत तो हम अभी ले ले कि संसार में देश काल-घर –समाज-घटनाएँ और सम्बन्धों की समानता होने पर भी व्यक्तित्व की विशिष्टता या अद्वितीयता जिस खाने में ढलती हैं उसका नाम है ‘प्रतिक्रिया’ ‘चीजों के प्रति हमारा बर्ताव’ और इनसे उत्पन्न हमारी ‘अवधारणा’ या ‘स्टेण्ड’।
उदाहरण के लिए सड़क के एक कोने में नोटों की भारी गड्डी पड़ी है। एक यात्री चारों ओर देखता है और एकान्त पा उसे उठा लेता है। दूसरा उसे ठोकरमार कर उछाल देता है। तीसरा भगवान की कृपा मानकर उसे जेब के हवाले करता है। चौथा उसे सुरक्षित करने के लिए उठाता है और एक तरह बैठ जाता है और एक तरफ बैठ जाता है ताकि जो उसे खोजने आये उसे सौप दे। पाँचवा नोट उठाकर थाने में दजमा कर देता है। छठा उसकी ओर उड़ती निगाह से देखता है और चला जाता है एक ही चीज अपने स्तर पर कितने इंसानों को पता दे रही है ! इसे कहते हैं- ‘एक में से, निकले छह।’ संसार भर की अनेक कथा सृष्टियाँ लोक के ऐसे व्यवहार भेद से जन्म लेकर विविभ रूप लेती हैं और न जाने कितने वक्त तक चलती रहती हैं ! इनमें लोक विविध रूप लेती हैं और न जाने कितने वक्त तक चलली रहती है ! इनमें लोक के खालिस अनुभव भाँति-भाँति के तिलिस्म की तरह खुलते हैं।
कहा –जा चुका है कि ‘तीडाराव’ और ‘भगवान की मौत’ दोनों उपन्यासिकाओं के चरित नायक ‘तीडा रावे’ है। राजस्थान की लोक परम्परा में न जाने कितने तोड़ा राव होंगे और न जाने कितनों के साथ एक जैसे संयोग घटित हुए होंगे, फिर भी वे अलग-अलग होंगे, जैसे आँख नाक आदि अवयवों के बावजूद कोई ऐसा अंतर जरूर होता है जो एक आदमी को दूसरे से अलग करता है।
लोक कथाओं, लोक कविताओं, लोकोक्तियों आदि कि आवृत्तियाँ और उनके भीतर की आवृत्तियाँ प्रकृतिया ईश्वर के इसी विधान का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं। आखिर ‘लोक’ प्रकृति और परमत्मा का पड़ोस ही तो है। उतना ही सहज ही गहन और उतना ही करिश्माई। उक्त दोंनों कथाओं के ‘तीडाराव’ के साथ पर ‘तीडाराव’ उपन्यासिका का तीडा लगभग एक जैसे संयोग घटित होते हैं। परिहारल है और भगवान का मौत का तीड़ा ‘बामन’ है। एक तो यही नाम भेद है। जो जाति भेद से हुआ है। सम्भव है इनमें जातीय स्वभाव के संकेत मौजूद हो। खैर तीडा परिहार गरीब है। पिता ठाकुर की घुड़सवाली में लीद उठाता है। पर तीड़ा गाँव के भजनियों में अव्वल है और गाँव की भजन मंडली में अलग बानक में रहता है- ‘बगुलें के पाँख के उनमान सामने के दो बुर्राक दाँतों में सोने की चमकती चूँपें। दोनों हाथों में चाँदी के कड़े। रेजे (खद्दर) की सफेद अँगरखी। लम्बे स्याह बालों में पीछे की तरफ खोंसा हुआ चन्दन का कंघा और आँखों में तीखा सुरमा डाले, जिस मंडली में जुड़ जाता। उसकी सोभा दुगुनी बढ़ जाती कैसे कंचों के बीच असली मोती चमक रहा हो। ये थे तीड़ा के ठाठ, धज और लोक-रंग। शायद वह वेशभूषा उसे भजन मण्डली से मिली हो, अन्यथा वह गरीब कहां से लाता ! खैर इस उद्धरण में जेथा जी की भाषा, शैली की विशेष बानक और मस्त अन्दाज पर ग़ौर करें।
गरीब घर हुआ तो क्या माँ उसे बाबा रामदेव का अवतार मानती थी। तीड़ा भी अपना खानदानी धान्धा सुहाता नहीं था और वह गाँव-गाँव में भजनमण्डली बना कर अलख जगाना चाहता था। उसे लगता था कि इससे उसे धन-माल-सम्पत्ति के साथ अलौकिक वैभव की विशालता भी, प्राप्त होगी। जाहिर है कि इस भजन-कीर्तन में सिर्फ सावधान नहीं था। उसके भीतर एक पेशेवर चेतना भी थी, जगह-जगह दिखाई देती हैं। यहीं यह ‘तीड़ा’ ‘भगवान की मौत वाले ‘तीड़ा’ से अलग हो जाता है और सान-संयोग अपना अर्थ बदल देते हैं।
लेखक भी उनका भी उस ‘कलयुगी अवतार’ को सम्बन्धित करता है। और कथान्त में उसका विवाह किसी तिकड़मी अय्यार की तरह राजकुँमारी से हो जाता है। भजनिया तीड़ा की इस उपलब्धि में संयोग के साथ उसकी चेष्टाएँ बनावटी तौर तरीके सभी कुछ न कुछ जोड़ते है जो आज के बाबाओं की याद दिलाते हैं। जैसे राजा के आने की खबर पा कर वह पद्मासन में बैठ आँखें मूंद लेता है या राजकुमारी को सुनाने के लिए भीड़ को संबोधित करता है, जैसे प्रसंग तीड़ा के चरित्र की ओर संकेत करते है। इसी कथा में कालिदास और विद्योत्तमा जैसा प्रसंग भी आ गया है ! लोककथाएँ कहाँ से लेकर कहाँ, क्या जो़ड़ दें इसका कोई ठिकाना नही। मौन का बहाना बना चेष्टाओँ द्वारा दिए उत्तरों के मनचाहे अर्थ लगाए गए है, पर आत्मगत व्याख्या अधूरी और अपर्याप्त होती हैं।
लोक को ‘ड्कोड’ करना क्या होता है यह आप देथा जी की ‘बातां’ री फुलवाड़ी’ ‘घाव करे गंभीर’ जैसी ग्रंथमालाओं में, उनकी कथा कहानियों में और यहाँ इस ‘त्रिवेणी में नहा कर देख सकते हैं। देथा जी ने सरलता में छिपी गहनता को अनावृत करने में जीवन खपा दिया है। अब आज के संगणक-बिज्जुओं को यह समझने से तो रहे कि इस ‘डिकोडिग’ की क्या उलटबासी है क्योंकि उनकी निगाह में जटिल या सूत्र कोल भाषाई सम्प्रेषण या दूसरे विस्तारों में खोलना ही डिकोडिंग है।
बिज्जी हिन्दी के शार्षस्थानीय कथाकारों में हैं, परन्तु बहुत कम हिन्दी पाठकों को पता होगा कि वे उनकी जो रचना पढ़ रहे हैं वह प्रायः राजस्थानी में लिखी रचनाओं का पुनर्पाठ है। पहले देथा जी अपनी रचना राजस्थानी में लिखते है, फिर हिन्दी में उसका पुनर्सृजन करते हैं। मूल कथा वे हिन्दी में नहीं लिख सकते यह कौन कहेगा, परन्तु वे लोकभाषा में सोचने और अनुभव करने को उसी भाषा में व्यक्त करने का अपना अभ्यास बनाए और बचाए रखना चाहते हैं। संभवतः ‘त्रिवेणी’ के साथ भी यही हुआ हो और देथा जी के तीडाराव, इस्टूखाँ राजस्थानी पाठक के माथे में पहले से ही चक्कर काट रहे हों।
लोकसाहित्य का दिल बहुत बड़ा होता है। लोकगायक से लगातार कथावाचक, साधारण किस्सागो और साहित्यकार सभी उसका अपनी तरह से उल्था या सृजनान्तरण करते रहते हैं। परन्तु लोकसाहित्य सबसे पहले लोकहृदय की माँग करता है, यानी वह हदृय जो उसे बाजारू इस्तेमाल की चीज न समझे और उसकी मूल भावना, या आत्मा को संरक्षित कर सके। लोकसाहित्य को पूरी तरह आत्मसात कर लेने के बाद कोई भले ही आसमान नाप ले उसे ऐतराज नहीं होता; पर अश्रद्ध कृत्रिम और स्वर्थसाधक, न लोक की आत्मा छू पाता है न लोक-साहित्य की। उसका हाथ सिर्फ एक मरा हुआ ढाँचा ही लगता है। बहरहाल।
विजयदान देथा की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वे लोककथा की आत्मा को जीवित रखते हुए उसका पुनः सृजन इस तरह करते हैं कि नागरिक या बौद्धिक भी उसका आस्वाद ले सके। यह लेखक की ऐसी शक्ति है जिसे विरुद्धों के नहीं तो, विभिन्नों के सामंजस्य की शक्ति कह सकते हैं, जो ब्राह्मवरण बेधकर अंतःकरण की एकता दिखाती है। हम चोहे तो इसे स्वीकार न करें लेकिन हर एक के हृदय की किसी तह में ‘लोक’ की सहज निश्छलता के लिए एक जगह ज़रूरी होती है। अगर देथा जी इस रहस्य को और अपनी शक्ति को स्वयं नहीं पहचानते तो शायद ठेठ लोक कथाओं, जन श्रुतियों और कई अविश्वनीय संयोगों की अत्याधुनिकता भाषा के प्रबुद्ध पाठकों के बीच इतनी फक्कड़ तबीयत से नहीं रखते। स्वयं ‘त्रिवेणी’ में ही ऐसे चरित नायक, ऐसे संयोग और ऐसी फेंटेसियां हैं जिनपर आधुनिक प्रबुद्ध पाठक रास्ता चलते भरोसा नहीं करेगा भरोसे के इस तत्त्व को लोक-विश्वास के हवाले कर देथा को इस तरह रचते हैं मानों तमाम असंभव संयोग चरित नायक की मिथकीय उपलब्धियों या विडम्बनाएं हों। अथवा यह इस कास्मिक तंत्र को कोई अदृश्य अनपहचाना चक्र हो, जहाँ असम्भव को भी उस नाम से पुकारने की गुंजायश न हो। अक्सर देथा जी की कथा के यहाँ तो चरित्र, प्रतीक के किसी महीन अर्थ गुँथाकर अपना स्थूल रूप खो देते हैं और कथाएं शरीर त्याग कर कोई जीवननार्थ उदघाटित करती हैं। शायद इसलिए उनका लोकलेखन, आधुनिक चारितार्थता हो पाता है। यानी लोक भी रहता है और आधुनिक भी।
देथा जी ने यह चीज़ यों हो नहीं पायीं, उन्होंने स्थाई रूप से राजस्थान के बोरुन्दा गाँव को अपनी सृजन- भूमि बनाया है। ऐसे कम बड़े लेखक होंगे जो दुनिया भर से जुड़े हों और जिनका आशियाँ सुदूर ग्राम में हो। जेथा जी के दिल्ली और मास्कों तक उड़े अन्नतः बोरुन्दा में ही लैंड करते हैं। लोक से यह अनवरत अविच्छिन्न ,सम्बन्ध उन नारों पर बहुत भारी पड़ता हैं जो जड़ो से जुड़ने का हल्ला मचाते हैं। देथा जी का सृजन और जीवन यह बताता है कि आधुनिक होने के लिए सहज ग्रामीणता छोडना ज़रूरी नहीं है। जो लेखक रचना में विरुद्धो या विभिन्नों का सामांजस्य करने पर तुला हो, वह अगर अपने जीवन में ही यह न कर सके तो फटे बाँस की बाँसुरी जैसा होगा।
बिज्जी की ‘त्रिव्रेणी’ तीन उपन्यासिकाओं ‘तीडाराव’ ‘इस्टूखाँ और ‘भगवान की मौत’ का संकलन है। हालाँकि शीर्षक की व्याख्या से आलोचना प्रारम्भ करना एक ऐसी घटिया सी शुरूआत है। परन्तु यो तीन कथाएं जो परस्पर जुड़ी भी है और अलग भी- मानो उदगम से निकली तीन धाराएँ पर्वत श्रृंखला के तीन ग या किसी कुँआरी लड़की के घने बालों की तीन चोटियाँ हैं ये कथाएँ दोस्तों की तरह साथ भी है और अलग भी। तीनों चरित नायक संयोगों के हिचकोले खाते हैं। ‘तीडाराव और भगवान की मोत’ के चरित्र नायक के तो नाम भी एक ही है और अनेक संयोग समान हैं। मिस्टूखाँ का बेटा ‘इस्टूखाँ’ तो खुद जिन्दगी घड़ता है। पर बापड़े पर हरसिंहार के फूल जैसे टपकते संयोग एक तरह की आफत ही हैं। संयोगों पर इन कविताओं को विभिन्न रंग-रूप और व्यक्तित्व कर देता है। इससे एक संकेत तो हम अभी ले ले कि संसार में देश काल-घर –समाज-घटनाएँ और सम्बन्धों की समानता होने पर भी व्यक्तित्व की विशिष्टता या अद्वितीयता जिस खाने में ढलती हैं उसका नाम है ‘प्रतिक्रिया’ ‘चीजों के प्रति हमारा बर्ताव’ और इनसे उत्पन्न हमारी ‘अवधारणा’ या ‘स्टेण्ड’।
उदाहरण के लिए सड़क के एक कोने में नोटों की भारी गड्डी पड़ी है। एक यात्री चारों ओर देखता है और एकान्त पा उसे उठा लेता है। दूसरा उसे ठोकरमार कर उछाल देता है। तीसरा भगवान की कृपा मानकर उसे जेब के हवाले करता है। चौथा उसे सुरक्षित करने के लिए उठाता है और एक तरह बैठ जाता है और एक तरफ बैठ जाता है ताकि जो उसे खोजने आये उसे सौप दे। पाँचवा नोट उठाकर थाने में दजमा कर देता है। छठा उसकी ओर उड़ती निगाह से देखता है और चला जाता है एक ही चीज अपने स्तर पर कितने इंसानों को पता दे रही है ! इसे कहते हैं- ‘एक में से, निकले छह।’ संसार भर की अनेक कथा सृष्टियाँ लोक के ऐसे व्यवहार भेद से जन्म लेकर विविभ रूप लेती हैं और न जाने कितने वक्त तक चलती रहती हैं ! इनमें लोक विविध रूप लेती हैं और न जाने कितने वक्त तक चलली रहती है ! इनमें लोक के खालिस अनुभव भाँति-भाँति के तिलिस्म की तरह खुलते हैं।
कहा –जा चुका है कि ‘तीडाराव’ और ‘भगवान की मौत’ दोनों उपन्यासिकाओं के चरित नायक ‘तीडा रावे’ है। राजस्थान की लोक परम्परा में न जाने कितने तोड़ा राव होंगे और न जाने कितनों के साथ एक जैसे संयोग घटित हुए होंगे, फिर भी वे अलग-अलग होंगे, जैसे आँख नाक आदि अवयवों के बावजूद कोई ऐसा अंतर जरूर होता है जो एक आदमी को दूसरे से अलग करता है।
लोक कथाओं, लोक कविताओं, लोकोक्तियों आदि कि आवृत्तियाँ और उनके भीतर की आवृत्तियाँ प्रकृतिया ईश्वर के इसी विधान का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं। आखिर ‘लोक’ प्रकृति और परमत्मा का पड़ोस ही तो है। उतना ही सहज ही गहन और उतना ही करिश्माई। उक्त दोंनों कथाओं के ‘तीडाराव’ के साथ पर ‘तीडाराव’ उपन्यासिका का तीडा लगभग एक जैसे संयोग घटित होते हैं। परिहारल है और भगवान का मौत का तीड़ा ‘बामन’ है। एक तो यही नाम भेद है। जो जाति भेद से हुआ है। सम्भव है इनमें जातीय स्वभाव के संकेत मौजूद हो। खैर तीडा परिहार गरीब है। पिता ठाकुर की घुड़सवाली में लीद उठाता है। पर तीड़ा गाँव के भजनियों में अव्वल है और गाँव की भजन मंडली में अलग बानक में रहता है- ‘बगुलें के पाँख के उनमान सामने के दो बुर्राक दाँतों में सोने की चमकती चूँपें। दोनों हाथों में चाँदी के कड़े। रेजे (खद्दर) की सफेद अँगरखी। लम्बे स्याह बालों में पीछे की तरफ खोंसा हुआ चन्दन का कंघा और आँखों में तीखा सुरमा डाले, जिस मंडली में जुड़ जाता। उसकी सोभा दुगुनी बढ़ जाती कैसे कंचों के बीच असली मोती चमक रहा हो। ये थे तीड़ा के ठाठ, धज और लोक-रंग। शायद वह वेशभूषा उसे भजन मण्डली से मिली हो, अन्यथा वह गरीब कहां से लाता ! खैर इस उद्धरण में जेथा जी की भाषा, शैली की विशेष बानक और मस्त अन्दाज पर ग़ौर करें।
गरीब घर हुआ तो क्या माँ उसे बाबा रामदेव का अवतार मानती थी। तीड़ा भी अपना खानदानी धान्धा सुहाता नहीं था और वह गाँव-गाँव में भजनमण्डली बना कर अलख जगाना चाहता था। उसे लगता था कि इससे उसे धन-माल-सम्पत्ति के साथ अलौकिक वैभव की विशालता भी, प्राप्त होगी। जाहिर है कि इस भजन-कीर्तन में सिर्फ सावधान नहीं था। उसके भीतर एक पेशेवर चेतना भी थी, जगह-जगह दिखाई देती हैं। यहीं यह ‘तीड़ा’ ‘भगवान की मौत वाले ‘तीड़ा’ से अलग हो जाता है और सान-संयोग अपना अर्थ बदल देते हैं।
लेखक भी उनका भी उस ‘कलयुगी अवतार’ को सम्बन्धित करता है। और कथान्त में उसका विवाह किसी तिकड़मी अय्यार की तरह राजकुँमारी से हो जाता है। भजनिया तीड़ा की इस उपलब्धि में संयोग के साथ उसकी चेष्टाएँ बनावटी तौर तरीके सभी कुछ न कुछ जोड़ते है जो आज के बाबाओं की याद दिलाते हैं। जैसे राजा के आने की खबर पा कर वह पद्मासन में बैठ आँखें मूंद लेता है या राजकुमारी को सुनाने के लिए भीड़ को संबोधित करता है, जैसे प्रसंग तीड़ा के चरित्र की ओर संकेत करते है। इसी कथा में कालिदास और विद्योत्तमा जैसा प्रसंग भी आ गया है ! लोककथाएँ कहाँ से लेकर कहाँ, क्या जो़ड़ दें इसका कोई ठिकाना नही। मौन का बहाना बना चेष्टाओँ द्वारा दिए उत्तरों के मनचाहे अर्थ लगाए गए है, पर आत्मगत व्याख्या अधूरी और अपर्याप्त होती हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i