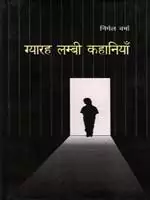|
लेख-निबंध >> दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों मेंनिर्मल वर्मा
|
392 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है विचार चिन्तन निबन्ध......
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
अपने इस नये निबन्ध संग्रह में निर्मल वर्मा ने उन समस्त दबावों और तकाजों
को अपनी चिर-परिचित प्रश्नाकुलता से रेखांकित किया है,जिनके कारण आज
शताब्दी के अंतिम वर्षों में हमें पुनःअपनी भाषा,परंपरा और जातीय अस्मिता
की पड़ताल उतनी ही जरूरी जान पड़ती है,जितनी इस शताब्दी के आरम्भ में
मनीषियों को लगी थी।
प्राक्कथन
यह पुस्तक मेरे उन लेखों का संकलन है, जो
मैंने पिछले तीन
वर्षों के दौरान लिखे थे। इनमें कुछ ऐसे आलेख, वक्तव्य और टिप्पणियाँ भी
शामिल हैं, जिन्हें समय के तात्कालिक दबावों और तकाजों के तहत लिखा गया
था। इनमें कुछ ऐसे साक्षात्कारों को भी चुनकर सम्मिलित किया गया है,
जिनमें दूसरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों-तले मुझे दुबारा से अपनी मान्यताओं
को पुनःपरिभाषित करने का मौका मिला था। विषय लगभग वहीं हैं, जो मेरी पिछली
पुस्तकों की चिंताओं के केन्द्र में रहे हैं, लेकिन नई परिस्थितियों और
संदर्भों में उनके कुछ ऐसे अप्रत्याशित पक्ष खुलते हैं, जिन पर
‘दूसरे शब्दों में पुनर्विचार करना जरूरी लगता है।
वैसे भी निबन्ध लिखना-मेरे लिए-चिंताओं को सुलझाना उतना नहीं, जितना बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में उनका नए सिरे से सामना करना है। जहाँ पहले पके हुए विश्वास थे, वहाँ अब संशय के काँटे दिखाई देने लगते हैं। हमारे युग में जिस तरह ईश्वर के सच्चे नामलेवा सिर्फ नास्तिक बचे रहे हैं, उसी तरह अपने भीतर उगनेवाले पीड़ित संदेहों से सही मुठभेड़ वही लोग कर पाते हैं, जिनमें आस्था पाने की प्यास सबसे अधिक झुलसा देनेवाली होती है। निबंध विधा एक तरह का चक्रव्यूह है जहाँ संदेह और आस्था हर अँधेरे कोने, हर अप्रत्याशित मोड़ पर एक-दूसरे के सामने क्षत-विक्षत, लहूलुहान खड़े दिखाई देते हैं। वहाँ यदि ‘सिनिसिज़्म के लिए जगह नहीं है तो परम विश्वासों की गुंजाइश भी नहीं है।
पुस्तक में संकलित करने से पूर्व जब इन लेखों को दुबारा से देखने का अवसर मिला, तो कुछ अजीब-सा अनुभव हुआ जैसे मैं किसी जानी-पहचानी पगडंडी पर चल रहा हूँ, जहाँ से इस शताब्दी के आरंभ में मेरे पूर्वज-पितामह गुजरे थे। मुझे लगता है जैसे किसी जादू के खेल से बींसवीं शती के अंत तक पहुँचते-पहुँचते हमारा देश वहीं पहुँच गया है, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी; अंतर इतना ही है-और वह बड़ा अंतर है-कि जहाँ पहले अपने को पाने का स्वप्न था, वहाँ आज सब-कुछ खो जाने की पीड़ा है।
इतिहास की धूल से पाँच हजार वर्ष पुरानी यात्रा के पद-चिह्न जहाँ-जहाँ खो गए थे, मिट गये थे, आँखों से ओझल हो गए थे, विवेकानन्द, गाँधी, श्री अरविंद आदि मनीषियों ने बीच के समस्त झाड़-झंखाड़ हटाकर उसे दुबारा से एक पवित्र और प्रशस्त मार्ग में परिणत किया था। वह हमारी सभ्यता का खोया हुआ रास्ता था, जिसने पहली बार पूरे आत्म-विश्वास के साथ पश्चिम की आधुनिक सभ्यता के सम्मुख एक नितांत अनूठा मानवदर्शी (मानव-केंद्रित नहीं) विकल्प उपस्थित किया था। इस रास्ते पर चलकर हमने अपनी भूली हुई पहचान, अपने चेहरे, अपने ‘निज’ को पहचाना था।
स्वतंत्रता पाने के पचास वर्ष पूर्व जिस सांस्कृतिक जागरण की शुरूआत हुई थी, क्या आज-पचास वर्ष बाद-हम उस नवोन्मेष की कोई छाप अपने में देख पाते हैं ? हमारे पूर्वजों ने ‘आत्म-बोध’ का जो अनमोल रत्न हमारे हाथ में सौंपा था, क्या हमने उसे कंकर समझकर दुबारा तो मिट्टी में नहीं मिला दिया ? हमने अपने को कैसा बना दिया ? क्या यह वह ‘छवि’ है जिसे हमने बीसवीं शती के आरंभ में पुन:स्मृत किया था और अब-उसकी ढलती घड़ियों में-भुला दिया है ? उस सभ्यता का क्या होता है जो जीवित रहते हुए भी आत्म-विस्मृत हो जाती है ?
ये प्रश्न जब भावात्मक पीड़ा और कुहासे से फूटकर बाहर तर्क के आलोक में आते हैं तब भाषा, परंपरा, धर्म जैसी अवधारणाएँ सिर्फ बौद्धिक विलास के खेल न रहकर एक सभ्यता के जिंदा रहने की शर्त, मूल प्रतिज्ञा बन जाते हैं। हम दुबारा उन प्रत्ययों की खोजबीन करते हैं जो एक समय में हमारी जातीय अस्मिता के चिह्न, संस्कृति के प्रतीक और सभ्यता के स्मृति संकेत थे। यदि इन लेखों और निबंधों में मैं पुन: उन प्रत्ययों और प्रश्नों की ओर लौटने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, तो इसलिए कि वे भारतीय सभ्यता के केंद्रीय-भाव थे, जिनसे आज हम छिटककर इतनी दूर चले गए हैं। रास्ता खोजने की शुरूआत ठीक उस जगह से शुरू होनी चाहिए, जहाँ हम अपनी राह से भटक गए थे।
अंत में मैं भारतीय ज्ञानपीठ के प्रति अपना आभार प्रगट करना चाहूँगा, जिसने इतने कम समय में इतनी सुरुचि संपन्नता से पुस्तक को प्रकाशित किया है।
वैसे भी निबन्ध लिखना-मेरे लिए-चिंताओं को सुलझाना उतना नहीं, जितना बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में उनका नए सिरे से सामना करना है। जहाँ पहले पके हुए विश्वास थे, वहाँ अब संशय के काँटे दिखाई देने लगते हैं। हमारे युग में जिस तरह ईश्वर के सच्चे नामलेवा सिर्फ नास्तिक बचे रहे हैं, उसी तरह अपने भीतर उगनेवाले पीड़ित संदेहों से सही मुठभेड़ वही लोग कर पाते हैं, जिनमें आस्था पाने की प्यास सबसे अधिक झुलसा देनेवाली होती है। निबंध विधा एक तरह का चक्रव्यूह है जहाँ संदेह और आस्था हर अँधेरे कोने, हर अप्रत्याशित मोड़ पर एक-दूसरे के सामने क्षत-विक्षत, लहूलुहान खड़े दिखाई देते हैं। वहाँ यदि ‘सिनिसिज़्म के लिए जगह नहीं है तो परम विश्वासों की गुंजाइश भी नहीं है।
पुस्तक में संकलित करने से पूर्व जब इन लेखों को दुबारा से देखने का अवसर मिला, तो कुछ अजीब-सा अनुभव हुआ जैसे मैं किसी जानी-पहचानी पगडंडी पर चल रहा हूँ, जहाँ से इस शताब्दी के आरंभ में मेरे पूर्वज-पितामह गुजरे थे। मुझे लगता है जैसे किसी जादू के खेल से बींसवीं शती के अंत तक पहुँचते-पहुँचते हमारा देश वहीं पहुँच गया है, जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी; अंतर इतना ही है-और वह बड़ा अंतर है-कि जहाँ पहले अपने को पाने का स्वप्न था, वहाँ आज सब-कुछ खो जाने की पीड़ा है।
इतिहास की धूल से पाँच हजार वर्ष पुरानी यात्रा के पद-चिह्न जहाँ-जहाँ खो गए थे, मिट गये थे, आँखों से ओझल हो गए थे, विवेकानन्द, गाँधी, श्री अरविंद आदि मनीषियों ने बीच के समस्त झाड़-झंखाड़ हटाकर उसे दुबारा से एक पवित्र और प्रशस्त मार्ग में परिणत किया था। वह हमारी सभ्यता का खोया हुआ रास्ता था, जिसने पहली बार पूरे आत्म-विश्वास के साथ पश्चिम की आधुनिक सभ्यता के सम्मुख एक नितांत अनूठा मानवदर्शी (मानव-केंद्रित नहीं) विकल्प उपस्थित किया था। इस रास्ते पर चलकर हमने अपनी भूली हुई पहचान, अपने चेहरे, अपने ‘निज’ को पहचाना था।
स्वतंत्रता पाने के पचास वर्ष पूर्व जिस सांस्कृतिक जागरण की शुरूआत हुई थी, क्या आज-पचास वर्ष बाद-हम उस नवोन्मेष की कोई छाप अपने में देख पाते हैं ? हमारे पूर्वजों ने ‘आत्म-बोध’ का जो अनमोल रत्न हमारे हाथ में सौंपा था, क्या हमने उसे कंकर समझकर दुबारा तो मिट्टी में नहीं मिला दिया ? हमने अपने को कैसा बना दिया ? क्या यह वह ‘छवि’ है जिसे हमने बीसवीं शती के आरंभ में पुन:स्मृत किया था और अब-उसकी ढलती घड़ियों में-भुला दिया है ? उस सभ्यता का क्या होता है जो जीवित रहते हुए भी आत्म-विस्मृत हो जाती है ?
ये प्रश्न जब भावात्मक पीड़ा और कुहासे से फूटकर बाहर तर्क के आलोक में आते हैं तब भाषा, परंपरा, धर्म जैसी अवधारणाएँ सिर्फ बौद्धिक विलास के खेल न रहकर एक सभ्यता के जिंदा रहने की शर्त, मूल प्रतिज्ञा बन जाते हैं। हम दुबारा उन प्रत्ययों की खोजबीन करते हैं जो एक समय में हमारी जातीय अस्मिता के चिह्न, संस्कृति के प्रतीक और सभ्यता के स्मृति संकेत थे। यदि इन लेखों और निबंधों में मैं पुन: उन प्रत्ययों और प्रश्नों की ओर लौटने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, तो इसलिए कि वे भारतीय सभ्यता के केंद्रीय-भाव थे, जिनसे आज हम छिटककर इतनी दूर चले गए हैं। रास्ता खोजने की शुरूआत ठीक उस जगह से शुरू होनी चाहिए, जहाँ हम अपनी राह से भटक गए थे।
अंत में मैं भारतीय ज्ञानपीठ के प्रति अपना आभार प्रगट करना चाहूँगा, जिसने इतने कम समय में इतनी सुरुचि संपन्नता से पुस्तक को प्रकाशित किया है।
-निर्मल वर्मा
सृजन का परिवेश
मनुष्यत्व से साक्षात्कार
सत्ता का सत्य उतना ही चिरंतन है, जितना सत्य
की सत्ता का
अनुभव। हर सत्ता के पीछे एक तरह की शक्ति क्रियाशील रहती है; वह परिवार
हो, धर्म प्रतिष्ठान हो या राज्य-सत्ता हो, वे समस्त संस्थाएँ जो मनुष्य
और मनुष्य, या मनुष्य और मनुष्येतर सत्ताओं के बीच संबंध निर्धारित करती
हैं, इसी कोटि में आती हैं। मानव संसार में जहाँ भी मनुष्य अपनी भौतिक और
आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पू्र्ति के लिए अपने से बाहर किसी अन्य सत्ता पर
निर्भर करता है, उसे अनिवार्यत: उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। वह अब
पूर्णत: अपना स्वामी नहीं रहता, स्वाधीनता का अंश उन सत्ताओं को अर्पित
करना पड़ता है, जो धरती पर उसका जीवन संभव बनाती हैं। बदले में ये सत्ताएँ
उसके लिए पूरा एक नीति-विधान और नियम संहिता बनाती हैं, जो उसके जीवन के
समस्त पक्षों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य वह अब भी रहता है, किंतु अब
उसका मनुष्यत्व सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक इकाइयों में विभाजित होने लगता
है। यह कहना भी कठिन लगता है कि उसकी अपनी एक अखंडित अस्मिता है-उसके भीतर
उसकी ‘अस्मिताएँ’ कभी एक-दूसरे से अनजान, कभी आपस में
टकराती
हुई कायम रहती हैं।
इन सबके बीच ‘साहित्य’ का स्थान कहाँ है-यह एक प्रश्न है; शायद इससे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह क्यों है, क्या प्रयोजन है उसके होने का ? साहित्य के बारे में यह जिज्ञासा इसलिए जगती है, क्योंकि अन्य सामाजिक सत्ताओं की तरह वह कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता। मनुष्य का कोई ऐसा पक्ष नहीं, जो उसके बिना सूखा या अतृप्त बचा रहे। उसकी समस्त भौतिक, सांसारिक इच्छाओं को दूसरी सत्ताएँ न्यूनाधिक मात्रा में तुष्ट कर देती हैं। और जहाँ तक उसकी आध्यात्मिक तृष्णा का प्रश्न है, शताब्दियों से विभिन्न धर्म-प्रतिष्ठान, ईश्वर की अवधारणाएँ, देवी-देवताओं का अस्तित्व किसी-न-किसी रूप में उसके जीवन और मृत्यु को अर्थ देते रहे हैं। इन सबके बावजूद अवश्य ही मनुष्य के भीतर कोई ऐसा रिक्त स्थान, कोई सूखापन, कोई तड़प बची रहती होगी जिसे कोई सत्ता अपने हिसाब-खाते में दर्ज नहीं करती, लेकिन जिसकी छाया में हर अनलिखे पन्ने पर मँडराती है। क्या है वह छाया, जिसका ‘सत्ता’ केवल साहित्य में मूर्तिमान होती है ?
इसका एक सीधा-सा उत्तर होगा-मनुष्य के भीतर ‘मनुष्यत्व’ पाने की आकांक्षा। यह ऊपर से थोड़ा विरोधाभास जान पड़ेगा। वह जो पहले से ही ‘मनुष्य’ है, भला उसे मनुष्यत्व पाने का स्वप्न क्यों देखना चाहिए ? यह इसलिए कि जिन सामाजिक-राजनीतिक सत्ताओं के बीच मनुष्य रहता है, वहाँ उसका केवल एक अंश उद्घाटित होता है, केवल उतना अंश जो इतिहास द्वारा परिचालित होता है। किन्तु मनुष्य सिर्फ ऐतिहासिक प्राणी नहीं है। इतिहास में वह जीता जरूर है (उसका कोई विकल्प नहीं है), लेकिन वह उसका ‘घर’ नहीं है। वह उसमें एक निर्वासित व्यक्ति की तरह जीता है। वह उसमें होकर भी कहीं और है, जिसकी कल्पना तो वह कर सकता है, किंतु जिसे वह परिभाषित नहीं कर सकता। इतिहास और समाज की सत्ताएँ उसे बाँधती हैं-कल्पना में वह हर दिए हुए बंधन, कानून, नियम संहिताओं से मुक्त हो जाता है। दो शब्दों में कहें, तो वह पहली बार सामाजिक, ऐतिहासिक प्राणी होने के बजाय सिर्फ एक ‘मनुष्य’ होने की परिकल्पना करता है।
साहित्य वह ‘घर’ है-बिना दीवारों का घर- जहाँ वह पहली बार अपने ‘मनुष्यत्व’ से साक्षात्कार करता है।
यह सत्य का अनुभव है, सुख का नहीं। यदि हमें सुख की सुरक्षा चाहिए, तो हमें साहित्य के पास नहीं जाना चाहिए, घर शब्द से जो सुरक्षा की सुगंध आती है, वह साहित्य में नहीं है। घर वह सिर्फ इस अर्थ में है कि वहाँ हम समस्त बाहरी सत्ताओं से छुटकारा पाकर अपने सत्य के पास लौटते हैं। अपना सत्य यानी समूची मनुष्यता का अखंडित, अविभाजित सत्य। सत्ता हमेशा मनुष्य सापेक्ष होती है-साहित्य की विशेषता इसमें है कि वह मनुष्य द्वारा सृजित होने पर भी मनुष्येतर शक्तियों से नाता जोड़ता है, अपने को केवल मानव समाज तक सीमित नहीं रखता। साहित्य का संबंध प्रकृति और ब्रह्मांड की उन समस्त अंधकारपूर्ण, रहस्यमय शक्तियों से है, जो मनुष्य के बाहर होते हुए भी उसकी नियति में दखल देती हैं। सत्ता का क्षेत्र मनुष्य जगत् है, किंतु शक्ति का साम्राज्य समूचे प्राकृतिक परिवेश को घेरता है। मनुष्य जब अपने में लौटता है तो यहीं, इसी ‘घर’ में जिसकी विराटता, असीमता और अज्ञेयता आदिम मनुष्य को इतना आतंकित और सम्मोहित करती थी। साहित्य की ‘सत्ता’- यदि उसे सत्ता कहा जा सके-उस वैदिक वृक्ष की याद दिलाती है, जिसकी जड़ें अंतरिक्ष की ओर उठी हैं और शाखाएँ नीचे धरती की ओर झुकी हैं।
साहित्य का यह एक दूसरा विरोधाभास है कि उसमें मनुष्य अपनी औसत औकात से हटकर अपने अतिरेक में जीता है-और इस अतिरेक के माध्यम से हम उसके मनुष्यत्व के असली मर्म की तह में जा पाते हैं। महाकाव्यों के चरित्र ‘अतिरेक’ के कारण ही नायक या हीरो बनने का गौरव प्राप्त करते हैं-क्योंकि वे जीवन की औसत सीमाओं का उल्लंघन करने का जोखिम उठाते हैं-अर्जुन अपनी वीरता में, दुर्योधन अपनी लिप्सा में, कर्ण अपनी दानशीलता में, युधिष्ठिर अपनी धर्म मर्यादा में, द्रौपदी अपने प्रतिशोध में लगी-बँधी लीकों को तोड़कर हमारे सामने मानव-प्रकृति के चरम रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। साहित्य की उत्कृष्ट कृतियाँ वे नहीं हैं जहाँ मनुष्य समाज के आईने में अपने प्रतिबिंब को देखता है, बल्कि वे हैं जिनमें वह आईने को तोड़कर अपने से परे जाता है, अपनी संभावना के अंतिम छोर पर, जो उसके चरित्र की परिणित है-वह छोर है, जहाँ समसा नाम का एक ट्रैवलिंग सेल्समैन एक सुबह अपनी औसत जिंदगी में अपने को एक कीड़े की तरह रेंगता पाता है और अन्ना कैरेनिना जैसी नायिका का प्रेम रेल की पटरी पर अपनी लहूलुहान लोथ में संपूर्ति पाता है। व्यास, टॉल्स्टॉय, काफ़्का के ये पात्र हमसे क्या कहते हैं ? वे मानव जीवन के एक मूल सत्य को उद्घाटित करते हैं-वह यह कि मनुष्य का मनुष्यत्व उसकी यथास्थिति में नहीं, उसके अतिक्रमण में; उसकी औसत अवस्था में नहीं, उसके उल्लंघन में प्रगट होता है। ‘अतिरेक’ का क्षेत्र ‘प्रकृति’ का क्षेत्र है, सामाजिक नियमों का क्षेत्र नहीं। इन पात्रों में मनुष्य अपनी छद्म मर्यादाओं की ओढ़-बिछावन फेंफकर प्रकृति के नग्न बीहड़ क्षेत्र में प्रवेश करता है।
इसी अर्थ में साहित्य के पात्र और स्थितियाँ मिथकीय आकार प्राप्त करती हैं। मिथक का प्रकृति से वही संबंध है, जो मनुष्य का अपने आभ्यंतरिक जगत् से। दोनों में एक ऐसी विराट अतिमानवीय शक्ति प्रवाहित होती है, जो झंझावत की तरह समाज के किसी नियम-कानून की परवाह किए बिना अपनी रौ में चलती है। कृष्ण जिस ‘धर्म-मर्यादा’ की बात दुर्योधन से करते हैं, वह दुर्योधन के क्रोध, आवेश, विजय-लालसा के सामने क्या कुछ भी अर्थ रखते हैं, क्या कुंती के आँसू कर्ण की आक्रोश-अग्नि को थोड़ा भी बुझा पाते हैं ? इलेक्ट्रा अपने भाई का दाह-संस्कार करने की आकांक्षा में क्या राजनियमों की जरा भी चिंता करती है ? नहीं, क्योंक वे इन क्षणों में सामाजिक सत्ताओं के ऊपर किसी और शक्ति के नियंत्रण में हैं। सत्ता हमेशा मनुष्य सापेक्ष होती है, जबकि शक्ति एक मनुष्येतर दुनिया में प्रवाहित होती है। वह अपने ‘होने’ के लिए समाज की स्वीकृति और ‘सैक्शन’ पर निर्भर नहीं होती। सत्ता का क्षेत्र मनुष्य जगत् है। वहीं से वह अपनी वैधता प्राप्त करती है। शक्ति का क्षेत्र समूचा ब्रह्मांड और मनुष्य की आंतरिक प्रकृति है-दोनों जिस विस्फोटनीय स्थल पर मिलते हैं, वहाँ मिथकीय चरित्रों का जन्म होता है। साहित्य का स्रोत और कविता का उद्गम स्थल भी वही है।
यही कारण है कि साहित्य और सामाजिक सत्ताओं के बीच का संबंध इतना पेचीदा, दुविधाजनक और पीड़ायुक्त होता है। साहित्यकार भले ही जीने के लिए सत्ताओं के आगे घुटने टेकता रहे-साहित्य या वह साहित्य, जिसका उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं, हमेशा सत्ताओं की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। समाज, विशेषकर राज्य सत्ता अपने सदस्यों को एक खास लीक पर चलने के लिए बाध्य कर सकती है, विरोध करनेवालों को दंडित कर सकती है। बहुत समय नहीं गुजरा जब राज्यों के नरेश अपनी सत्ता को ‘दैवी अधिकार’ (डिवाइन राइट) मानते आए थे। बीसवीं शताब्दी ऐसी निरंकुश शासक-सत्ताओं से अटी पड़ी है जिनकी तानाशाही का आतंक हर नीति-नियम, हर संविधान की सीमाओं के बाहर था। सत्ता की यह लिप्सा केवल सेक्यूलर राज्य-संस्थाओं तक सीमित नहीं थी। उनके ‘धर्म-प्रतिष्ठान’ आज भी इतने शक्तिशाली हैं कि उनके आदेश का उल्लंघन ही एक अक्षम्य अपराध हो जाता है-और यह केवल मध्ययुग में ही नहीं था, जब लूथर और यान हुस को कैथलिक चर्च के हाथों अपनी ‘हैरेसी’ के लिए दंड भोगना पड़ा था, हमारे समय में सलमान रुश्दी और तसलीमा नसरीन को स्वयं अपनी अंतश्चेतना की आवाज सुनने की सजा भुगतनी पड़ी है।
इसके विपरीत साहित्य के पीछे न राज्य सत्ता का बल है, न किसी धार्मिक संस्थान का आतंक। लेखकों को कारागृह में डाला जा सकता है, पुस्तकों को गली-चौराहों पर जलाया जा सकता है। ये हादसे कोई ‘प्रिमिटिव’ समाज की बर्बर सत्ताओं तले नहीं, ऐसे ‘सभ्य’ समाजों में होते थे जहाँ एक तरफ गोएटे और टॉल्स्टॉय की पूजा होती थी, दूसरी तरफ टॉमस मान और मेंडलश्टाम की पुस्तकों को पढ़ना निषिद्ध था। लिखा हुआ शब्द हमारे आधुनिक समाजों में जितना निरीह और निष्कवच रहा है, उतना शायद कभी नहीं। फिर क्या कारण है कि आततायी सत्ताओं को हमेशा वह एक खतरे भरा अंदेशा जान पड़ता है ? कहाँ छिपा है उसकी शक्ति का स्रोत ? यह स्रोत किसी बाहरी सत्ता में न होकर स्वयं शब्द के भीतर विद्यमान है। जो शब्द राजनीतिक सत्ताओं के समक्ष इतना निरीह और अवश दिखाई देता है, वही साहित्य में प्रवेश करते ही एक तरह की अज्ञात, असीमित ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। बिना शब्द के साहित्य की परिकल्पना असंभव है-इस दृष्टि से वह अन्य कलाओं से इतना भिन्न है। एक साहित्यिक कृति अपनी ऊर्जा उस भाषा से प्राप्त करती है, जिसमें वह अपने को रूपायित करती है। भाषा का सामाजिक पहलू उसके संप्रेषण में है, वहाँ वह एक ‘माध्यम’ के रूप में प्रयुक्त होती है। किंतु साहित्य के सृजन क्षेत्र में वह महज माध्यम बनकर नहीं रह पाती, बल्कि एक स्वायत्त शक्ति के रूप में प्रकट होती है। वह अपने प्रयोजन में समाजोन्मुख भले ही हो, अपने ‘होने’ के लिए समाज पर आश्रित नहीं है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन एक कविता, नाटक, उपन्यास में आते ही वे अपनी स्मृतियों, संस्कारों, संदर्भों को उजागर करते हैं, वे सामाजिक संप्रेषण की व्यावहारिक शब्दावली से कहीं अधिक ‘अस्तित्ववान’ होते हैं-‘अस्तित्ववान’ इस अर्थ में कि वे सामाजिक उपादेयता से ऊपर उठकर स्वयं मनुष्य को अपने अस्तित्व की मूलगामी स्थिति की ओर आकृष्ट करते हैं। साहित्य में प्रवेश करते ही ‘शब्द’ एक अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर लेता है।
यहाँ प्रश्न तथाकथित साहित्यिक भाषा का नहीं है, जो बोलचाल की भाषा की तुलना में कहीं अधिक बोझिल, कृत्रिम और पंडिताऊ होती है। मैं जिस अंतर की ओर संकेत कर रहा हूँ, वह भाषा के चरित्र से नहीं, उसके उपयोग से संबंध रखता है। सामाजिक और राजनीतिक सत्ताओं के लिए भाषा सिर्फ एक उपयोग का साधन है-जिसे समाचारपत्रों, राजनैतिक घोषणाओं और प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी उपादेयता का मापदंड इसमें है कि वह किस वर्ग और संप्रदाय का कितना हित साधने में सफल होती है। इसके विपरीत जो शब्द कविता और उपन्यास में प्रयुक्त होता है, उसकी शक्ति किसी सत्ता के स्वार्थ के लिए नहीं, स्वयं अपना ‘अर्थ’ उद्घाटित करने में प्रकट होती है। साहित्य के ‘मैग्नेटिक फील्ड’ में प्रवेश करते ही वह एक अद्भुत उज्जवलता, पवित्रता और ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। क्रिश्चियन धार्मिक अर्थ में वह ‘ग्रेस’ के आलोकमंडल में आ जाता है। हम चाहें तो कह सकते हैं कि जिस तरह मिथक औसत का अतिरेक है, उसी तरह कविता का शब्द स्वयं भाषा का अतिरेक है, उसकी शक्ति दूसरों तक पहुँचने में नहीं, अपनी ओर लौटने में है। अपनी ओर लौटकर ही वह साहित्य के सत्य को दूसरों तक पहुँचा सकता है।
हमने ऊपर ‘साहित्यिक शब्द’ को अस्तित्ववान कहा था-उसे थोड़ा और स्पष्ट करने की जरूरत है। हर सामाजिक सत्ता एक ऐतिहासिक क्षण की उपज है, इस अर्थ में वह समय-सापेक्ष है। वह चाहे कितनी मानववादी, कितनी लोकतांत्रिक क्यों न हो, मनुष्य के समूचे अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में हमेशा अधूरी, असंतोषजनक, अपनी ऐतिहासिक बाध्यताओं द्वारा सीमित होती है। समय उनके भीतर बहता है, इसलिए भ्रष्ट होने के कीटाणु उनमें हमेशा मौजूद रहते हैं। यथार्थ और आदर्श के बीच की अँधेरी खाई हमेशा खुली रहती है। साहित्य पर इस तरह का कोई अंकुश नहीं है। वह अपनी शक्ति भाषा के जिस स्रोत से प्राप्त करता है, वह मानव स्वभाव की चिरंतनता, समग्रता, उसके आदि स्वरूप से संबंध रखती है। इतिहास की छायाएँ उस पर जरूर हैं, उसके स्वरूप को तिरोहित नहीं करतीं, उलटे उसकी आत्यंतिक छवि, उसके ‘अस्तित्ववान’ सत्य को और अधिक सघनता और उज्जवलता में उद्घाटित करती हैं। साहि्त्य वह लीला स्थल है, जिसमें इतिहास की छाया और मनुष्य के सत्य की द्वंद्व-क्रीड़ा चलती है विश्व साहित्य के शायद सबसे शक्तिशाली प्रसंग वहाँ आते हैं, जहाँ इस द्वंद्व के कुहासे में पहली बार मनुष्य को अपने ‘अस्तित्व’ का स्वर एक मर्मांतक चीख की तरह सुनाई देता है-एक ऐसी चीख जो समस्त ऐतिहासिक और सत्य सत्ताओं को भेदती हुई समय के आर-पार चली जाती है। एक ऐसा ही दृश्य टॉल्स्टॉय अपने उपन्यास ‘युद्ध और शांति’ में प्रस्तुत करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अन्यत्र किया है और जिसे मैं दोबारा उद्धृत करना चाहूँगा।
प्रसंग युद्ध का है, जब समूचा मॉस्को शहर धू-धू जल रहा है। उपन्यास का एक मुख्य पात्र पियेर बदहवास-सा होकर जलते हुए मकानों और रोते-चीखते लोगों के हाहाकार के बीच भाग रहा है। अचानक नेपोलियन के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है।
और तब उसे लगा, जैसे वह किसी दीर्घ निद्रा से जागा है। वह सोचता है, उन्होंने मुझे बंदी बना लिया है, मैं पकड़ लिया गया हूँ। लेकिन मैं कौन ? उन्होंने किसे बंदी बनाया है, वह जो मेरी अमर आत्मा है ? वह हँसने लगा और फिर अचानक उसकी आँखें आकाश की ओर उठ गईं जहाँ मॉस्को के आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। ‘यह सब मेरा है और यह सब मैं हूँ।’ और यह विचार आते ही व्यथा का सारा बोझ उसकी आत्मा से उतर गया मानो सहसा उसने अपने और सृष्टि के बीच एक गहरा एकात्म पा लिया हो।
ऊपर के उद्धरण में, जैसा आपने नोट किया होगा, एक अजीब वाक्य आता है, ‘जैसे वह किसी दीर्घ निद्रा से जागा है।’ यह वह ‘नींद’ है जिसमें हम मरते हैं, मारते हैं, जीत और हार का खेल खेलते हैं, जहाँ मनुष्य के सब काम जैसे उसकी चेतना के बाहर अँधेरे में होते हैं। किंतु कोई ऐसा दुर्लभ क्षण आता है, जब इतिहास की कुहेलिका में नीचे सहसा हमारी आँखें खुल जाती हैं और हम अपने समूचे ‘अस्तित्व’ के प्रति सचेत हो जाते हैं, हमारे अहं और सृष्टि के बीच की दीवारें ढह जाती हैं। यह वह क्षण होता है, जब मनुष्य की ‘विभाजित अस्मिताएँ’ जिसका उल्लेख हमने आलेख के आरंभ में किया था, एक-दूसरे में घुल-मिल जाती हैं। मनुष्य अपने भूले हुए ‘मनुष्यत्व’ को पा लेता है, जहाँ वह इस धरती पर एक अनाथ व्यक्ति नहीं, एक ‘अमर आत्मा’ को जाने का चमत्कारिक अनुभव करता है। वह अपनी निर्वासित अवस्था से मुक्ति पाकर अपने खोए हुए ‘घर’ में लौट आता है।
अपने ‘संपूर्ण’ होने का जो बोध मनुष्य को साहित्य में होता है, वह एक समग्र अनुभव है। मनुष्य उसे एक स्मृति की तरह अपने भीतर सँजोकर जीता है। जिस विराट का अनुभव टॉल्स्टॉय के पात्र को युद्ध की विभीषिका तले हुआ था, हमें अपने जीवन के खंडित, जर्जरित, दिग्भ्रांत क्षणों में होता है, जब हम किसी महान् कलाकृति के संपर्क में आते हैं। जरूरी नहीं, यह अनुभव स्थायी हो। यह एक तरह का अपूर्व, अद्वितीय आनंद है- एक एक्स्टेसी का स्पंदन-जो होता भाषा में है लेकिन अपने में शब्दातीत है। क्षणिक होता हुआ भी वह एक अमिट स्मृति की छाप हम पर छोड़ जाता है। कालांतर में इन्हीं स्मृतियों की श्रृंखला एक जाति का संस्कार बन जाती है, उसकी जीवन गति को एक विशिष्ट लय प्रदान करती है। यूरोपीय मानसिकता को जहाँ बाइबिल की धार्मिक-आध्यात्मिक परंपरा ने प्रभावित किया है, वहाँ उतनी ही तेजस्विता से ग्रीक महाकाव्यों की कथाओं ने एक विशिष्ट जीवन-दृष्टि में ढाला है। पश्चिमी सभ्यता की परिकल्पना उनके बिना करना उतना ही असंभव होगा, जितना महाभारत और रामायण के बिना भारतीय संस्कृति के मूल चरित्र के संबंध में कुछ भी कहना सारहीन होगा। किसी जाति की एपिक-गाथाएँ और महाकाव्य अपनी प्रभाव शक्ति में उसके ‘धर्मग्रंथों’ से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। भारतीय परंपरा में तो एक को दूसरे से अलग करना ही असंभव होगा। रामायण और महाभारत की काव्यात्मकता उतनी ही प्रखर और ओजपूर्ण है, जितनी उनकी आध्यात्मिक गहनता (यह आकस्मिक नहीं है, कि गीता का प्रवचन युद्ध की छाया तले दिया गया था, किसी तपोवन के मनोरम परिवेश में नहीं)। भारतीय संस्कृति की ये महान् काव्य रचनाएँ न तो ओल्ड टेस्टामेंट और कुरान की तरह निरी धर्म-पुस्तकें और आचार-संहिताएँ हैं, न ग्रीक महाकाव्यों-ईलियड और ओडिसी- की तरह ‘सेक्यूलर’ साहित्यिक कृतियाँ हैं। वे दोनों हैं और दोनों में से एक भी नहीं हैं। वे मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसके उदात्त और पाशविक, गौरवपूर्ण और घृणास्पद, उजले और गँदले- उसके समस्त पक्षों को अपने प्रवाह में समेटकर बहती हैं। कला में सौंदर्य का आस्वादन और सत्य की बीहड़ खोज कोई अलग-अलग अनुभूतियाँ न होकर एक अखंडित और विराट अनुभव का साक्ष्य बन जाती है।
काव्य का यह अनुभव हमें ऐसे स्तर पर ले जाता है, जहाँ साहित्य न तो सत्ता के विरोध में है, न उसके समर्थन में। पक्ष-प्रतिपक्ष का प्रश्न वहीं उठता है, जहाँ दोनों को अलग इकाइयों में बाँटकर देखा जाता है जबकि यथार्थ में इस तरह का अलगाव असंभव है। हर सामाजिक सत्ता, वह शासन की हो अथवा किसी चर्च या धर्म-प्रतिष्ठान की, एक तरह से मनुष्य का ही बृहत्तर स्वरूप है, उसकी आंतरिक आकांक्षाओं, कामनाओं का प्रत्यक्षीकरण। इस अर्थ में हर सत्ता आधा स्वप्न, आधा यथार्थ होती है। यथार्थ में हिंसा, लोलुपता, अहम्मन्यता के तामसिक तत्त्व क्रियाशील रहते हैं, स्वप्न में उनका अतिक्रमण करके एक ‘ईश्वरीय’ व्यवस्था (संत आगस्टाइन के शब्दों में, ‘किंग्डम ऑफ गॉड’) रचने का आदर्श निहित रहता है। दार्शनिकों ने जिस ‘यूटोपिया’ की परिकल्पना की थी वह चाहे रूसो की प्राकृतिक जीवन व्यवस्था हो, मार्क्स का वर्गहीन समाज या गाँधी का रामराज्य, उनके मूल में भविष्य के आदर्श समाज का यही स्वप्न मौजूद रहता है। बाइबिल की कथा में जिस आदि मानव को ‘गार्डन ऑफ ईडन’ से बहिष्कृत करके पाप के कीचड़ में फेंक दिया था- जो यह संसार है-यह उससे उबरकर पुन: उस खोई हुई पवित्रावस्था में लौटने की लालसा है। क्या यह ‘लालसा’ हमें उस अनुभव की याद नहीं दिलाती, जो हमें संसार की महान् साहित्यिक कृतियों के संपर्क में होती है-अपनी निर्वासित अवस्था से मुक्ति पाकर अपने ‘घर’ लौटने की लालसा, ताकि मनुष्य इस धरती पर एक अजनबी बनकर न रहे ? सामाजिक क्रांतियों की परिणति कितनी ही भयावह हो, उनके उत्स में इसी आदर्शमय, काल्पनिक, स्वर्णिम समाज को धरती पर बसाने की आकांक्षा होती है। यह बात अलग है कि सफल होने पर हर क्रांति कल्पना के ‘घर’ को कारागृह के यथार्थ में बदल देती है।
सच पूछा जाए तो इस धरती पर यह कारागृह ही मनुष्य का असली घर है- बाकी सब उसकी कामनाओं का कल्पनालोक है। किंतु कल्पनालोक का सत्य भी कारागृह की दीवारों से कम यथार्थपूर्ण, कम जीवनदायी, कम शक्तिवान् नहीं होता। साहित्य हमें मुक्ति नहीं दिलाता, वह हमें बंदी होने का एहसास कराता है। वह हमारे भीतर के रिक्त स्थानों को नहीं भरता, उनमें खालीपन को दर्शाता है। यह खालीपन हर जगह है, जहाँ पहले ईश्वर वास करता था। साहित्य का शब्द ईश्वर के विरह शोक को नहीं भरता, उसे एक घाव की तरह खोलता है। इस अर्थ में हर साहित्यिक कृति सेक्यूलर सत्ताओं के मरुस्थल में एक असीम तृष्णा का अनुभव कराती है।
आधुनिक समय में हमने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया है, जहाँ से ईश्वर को ‘देश-निकाला’ दे दिया गया है। किसी दूसरे ग्रह का प्राणी अगर हमारी दुनिया के प्रवेशद्वार पर आएगा, तो वह वहाँ पर यह तख्ती देखेगा-‘ईश्वर अब यहाँ नहीं रहता !’ यदि ईश्वर कहीं है, तो उसी निर्वासित अवस्था में, जिसमें मनुष्य अपने को बिना ईश्वर के पाता है। एक दुनिया के बाहर, बहिष्कृत। दूसरा, दुनिया के भीतर निर्वासित...किंतु ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ दोनों एक-दूसरे को खोजते हुए पा लेते हैं, फिर खो देते हैं, फिर पा लेते हैं। खोने और पाने की यह आँख-मिचौली जब तक चलती रहेगी, कविता और उपन्यास लिखे जाते रहेंगे। ईश्वर एक भिखारी है, जो हर घर का दरवाजा खटखटाता है। कवि उसे अपनी आत्मा के निविड़ अंधकार और सन्नाटे में सुनता है। हमने यदि साहित्य के शब्द को ‘ग्रेस’ की महिमा दी थी, तो कुछ सोच-समझकर ही। वह शब्द के भीतर ईश्वर की खटखटाहट है, जिसे इतिहास की सत्ताएँ, अनसुना कर देती हैं। और लेखक अपनी रचना में ‘दर्ज’ कर लेता है। जिस रचना में वह खटखटाहट नहीं सुनाई देती, वह कितनी ही ‘सत्तावान’ क्यों न हो, साहित्य नहीं होती।
हमने शब्द को भाषा का अतिरेक माना था। हम चाहें तो कह सकते हैं कि ‘ईश्वर’ की अदृश्य सत्ता समस्त सत्ताओं का अतिरेक है। किसी लगे-बंधे ‘धार्मिक’ अर्थ में नहीं, बल्कि एक मनुष्येतर शक्ति के अर्थ में, जो मनुष्य के भीतर अंतनिर्हित है, उसके बाहर नहीं। साहित्य का संबंध लौकिक सत्ताओं से क्या होगा, कैसा होना चाहिए, यह अंतत: इस पर निर्भर करता है कि वह मनुष्य की इस ‘अतिरेक सत्ता’ से कैसा संबंध जोड़ता है। आज के ‘सेक्यूलर’ युग में जब मनुष्य की स्थिति को बदलने का दावा करने वाली सब क्रांतियाँ धूल में ध्वस्त हो गई हैं- लौकिक सत्ता और ‘अलौकिक’ के बीच संबंध की पड़ताल क्या नए सिरे से आरंभ नहीं होनी चाहिए ?
इन सबके बीच ‘साहित्य’ का स्थान कहाँ है-यह एक प्रश्न है; शायद इससे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह क्यों है, क्या प्रयोजन है उसके होने का ? साहित्य के बारे में यह जिज्ञासा इसलिए जगती है, क्योंकि अन्य सामाजिक सत्ताओं की तरह वह कोई प्रयोजन पूरा नहीं करता। मनुष्य का कोई ऐसा पक्ष नहीं, जो उसके बिना सूखा या अतृप्त बचा रहे। उसकी समस्त भौतिक, सांसारिक इच्छाओं को दूसरी सत्ताएँ न्यूनाधिक मात्रा में तुष्ट कर देती हैं। और जहाँ तक उसकी आध्यात्मिक तृष्णा का प्रश्न है, शताब्दियों से विभिन्न धर्म-प्रतिष्ठान, ईश्वर की अवधारणाएँ, देवी-देवताओं का अस्तित्व किसी-न-किसी रूप में उसके जीवन और मृत्यु को अर्थ देते रहे हैं। इन सबके बावजूद अवश्य ही मनुष्य के भीतर कोई ऐसा रिक्त स्थान, कोई सूखापन, कोई तड़प बची रहती होगी जिसे कोई सत्ता अपने हिसाब-खाते में दर्ज नहीं करती, लेकिन जिसकी छाया में हर अनलिखे पन्ने पर मँडराती है। क्या है वह छाया, जिसका ‘सत्ता’ केवल साहित्य में मूर्तिमान होती है ?
इसका एक सीधा-सा उत्तर होगा-मनुष्य के भीतर ‘मनुष्यत्व’ पाने की आकांक्षा। यह ऊपर से थोड़ा विरोधाभास जान पड़ेगा। वह जो पहले से ही ‘मनुष्य’ है, भला उसे मनुष्यत्व पाने का स्वप्न क्यों देखना चाहिए ? यह इसलिए कि जिन सामाजिक-राजनीतिक सत्ताओं के बीच मनुष्य रहता है, वहाँ उसका केवल एक अंश उद्घाटित होता है, केवल उतना अंश जो इतिहास द्वारा परिचालित होता है। किन्तु मनुष्य सिर्फ ऐतिहासिक प्राणी नहीं है। इतिहास में वह जीता जरूर है (उसका कोई विकल्प नहीं है), लेकिन वह उसका ‘घर’ नहीं है। वह उसमें एक निर्वासित व्यक्ति की तरह जीता है। वह उसमें होकर भी कहीं और है, जिसकी कल्पना तो वह कर सकता है, किंतु जिसे वह परिभाषित नहीं कर सकता। इतिहास और समाज की सत्ताएँ उसे बाँधती हैं-कल्पना में वह हर दिए हुए बंधन, कानून, नियम संहिताओं से मुक्त हो जाता है। दो शब्दों में कहें, तो वह पहली बार सामाजिक, ऐतिहासिक प्राणी होने के बजाय सिर्फ एक ‘मनुष्य’ होने की परिकल्पना करता है।
साहित्य वह ‘घर’ है-बिना दीवारों का घर- जहाँ वह पहली बार अपने ‘मनुष्यत्व’ से साक्षात्कार करता है।
यह सत्य का अनुभव है, सुख का नहीं। यदि हमें सुख की सुरक्षा चाहिए, तो हमें साहित्य के पास नहीं जाना चाहिए, घर शब्द से जो सुरक्षा की सुगंध आती है, वह साहित्य में नहीं है। घर वह सिर्फ इस अर्थ में है कि वहाँ हम समस्त बाहरी सत्ताओं से छुटकारा पाकर अपने सत्य के पास लौटते हैं। अपना सत्य यानी समूची मनुष्यता का अखंडित, अविभाजित सत्य। सत्ता हमेशा मनुष्य सापेक्ष होती है-साहित्य की विशेषता इसमें है कि वह मनुष्य द्वारा सृजित होने पर भी मनुष्येतर शक्तियों से नाता जोड़ता है, अपने को केवल मानव समाज तक सीमित नहीं रखता। साहित्य का संबंध प्रकृति और ब्रह्मांड की उन समस्त अंधकारपूर्ण, रहस्यमय शक्तियों से है, जो मनुष्य के बाहर होते हुए भी उसकी नियति में दखल देती हैं। सत्ता का क्षेत्र मनुष्य जगत् है, किंतु शक्ति का साम्राज्य समूचे प्राकृतिक परिवेश को घेरता है। मनुष्य जब अपने में लौटता है तो यहीं, इसी ‘घर’ में जिसकी विराटता, असीमता और अज्ञेयता आदिम मनुष्य को इतना आतंकित और सम्मोहित करती थी। साहित्य की ‘सत्ता’- यदि उसे सत्ता कहा जा सके-उस वैदिक वृक्ष की याद दिलाती है, जिसकी जड़ें अंतरिक्ष की ओर उठी हैं और शाखाएँ नीचे धरती की ओर झुकी हैं।
साहित्य का यह एक दूसरा विरोधाभास है कि उसमें मनुष्य अपनी औसत औकात से हटकर अपने अतिरेक में जीता है-और इस अतिरेक के माध्यम से हम उसके मनुष्यत्व के असली मर्म की तह में जा पाते हैं। महाकाव्यों के चरित्र ‘अतिरेक’ के कारण ही नायक या हीरो बनने का गौरव प्राप्त करते हैं-क्योंकि वे जीवन की औसत सीमाओं का उल्लंघन करने का जोखिम उठाते हैं-अर्जुन अपनी वीरता में, दुर्योधन अपनी लिप्सा में, कर्ण अपनी दानशीलता में, युधिष्ठिर अपनी धर्म मर्यादा में, द्रौपदी अपने प्रतिशोध में लगी-बँधी लीकों को तोड़कर हमारे सामने मानव-प्रकृति के चरम रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। साहित्य की उत्कृष्ट कृतियाँ वे नहीं हैं जहाँ मनुष्य समाज के आईने में अपने प्रतिबिंब को देखता है, बल्कि वे हैं जिनमें वह आईने को तोड़कर अपने से परे जाता है, अपनी संभावना के अंतिम छोर पर, जो उसके चरित्र की परिणित है-वह छोर है, जहाँ समसा नाम का एक ट्रैवलिंग सेल्समैन एक सुबह अपनी औसत जिंदगी में अपने को एक कीड़े की तरह रेंगता पाता है और अन्ना कैरेनिना जैसी नायिका का प्रेम रेल की पटरी पर अपनी लहूलुहान लोथ में संपूर्ति पाता है। व्यास, टॉल्स्टॉय, काफ़्का के ये पात्र हमसे क्या कहते हैं ? वे मानव जीवन के एक मूल सत्य को उद्घाटित करते हैं-वह यह कि मनुष्य का मनुष्यत्व उसकी यथास्थिति में नहीं, उसके अतिक्रमण में; उसकी औसत अवस्था में नहीं, उसके उल्लंघन में प्रगट होता है। ‘अतिरेक’ का क्षेत्र ‘प्रकृति’ का क्षेत्र है, सामाजिक नियमों का क्षेत्र नहीं। इन पात्रों में मनुष्य अपनी छद्म मर्यादाओं की ओढ़-बिछावन फेंफकर प्रकृति के नग्न बीहड़ क्षेत्र में प्रवेश करता है।
इसी अर्थ में साहित्य के पात्र और स्थितियाँ मिथकीय आकार प्राप्त करती हैं। मिथक का प्रकृति से वही संबंध है, जो मनुष्य का अपने आभ्यंतरिक जगत् से। दोनों में एक ऐसी विराट अतिमानवीय शक्ति प्रवाहित होती है, जो झंझावत की तरह समाज के किसी नियम-कानून की परवाह किए बिना अपनी रौ में चलती है। कृष्ण जिस ‘धर्म-मर्यादा’ की बात दुर्योधन से करते हैं, वह दुर्योधन के क्रोध, आवेश, विजय-लालसा के सामने क्या कुछ भी अर्थ रखते हैं, क्या कुंती के आँसू कर्ण की आक्रोश-अग्नि को थोड़ा भी बुझा पाते हैं ? इलेक्ट्रा अपने भाई का दाह-संस्कार करने की आकांक्षा में क्या राजनियमों की जरा भी चिंता करती है ? नहीं, क्योंक वे इन क्षणों में सामाजिक सत्ताओं के ऊपर किसी और शक्ति के नियंत्रण में हैं। सत्ता हमेशा मनुष्य सापेक्ष होती है, जबकि शक्ति एक मनुष्येतर दुनिया में प्रवाहित होती है। वह अपने ‘होने’ के लिए समाज की स्वीकृति और ‘सैक्शन’ पर निर्भर नहीं होती। सत्ता का क्षेत्र मनुष्य जगत् है। वहीं से वह अपनी वैधता प्राप्त करती है। शक्ति का क्षेत्र समूचा ब्रह्मांड और मनुष्य की आंतरिक प्रकृति है-दोनों जिस विस्फोटनीय स्थल पर मिलते हैं, वहाँ मिथकीय चरित्रों का जन्म होता है। साहित्य का स्रोत और कविता का उद्गम स्थल भी वही है।
यही कारण है कि साहित्य और सामाजिक सत्ताओं के बीच का संबंध इतना पेचीदा, दुविधाजनक और पीड़ायुक्त होता है। साहित्यकार भले ही जीने के लिए सत्ताओं के आगे घुटने टेकता रहे-साहित्य या वह साहित्य, जिसका उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं, हमेशा सत्ताओं की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। समाज, विशेषकर राज्य सत्ता अपने सदस्यों को एक खास लीक पर चलने के लिए बाध्य कर सकती है, विरोध करनेवालों को दंडित कर सकती है। बहुत समय नहीं गुजरा जब राज्यों के नरेश अपनी सत्ता को ‘दैवी अधिकार’ (डिवाइन राइट) मानते आए थे। बीसवीं शताब्दी ऐसी निरंकुश शासक-सत्ताओं से अटी पड़ी है जिनकी तानाशाही का आतंक हर नीति-नियम, हर संविधान की सीमाओं के बाहर था। सत्ता की यह लिप्सा केवल सेक्यूलर राज्य-संस्थाओं तक सीमित नहीं थी। उनके ‘धर्म-प्रतिष्ठान’ आज भी इतने शक्तिशाली हैं कि उनके आदेश का उल्लंघन ही एक अक्षम्य अपराध हो जाता है-और यह केवल मध्ययुग में ही नहीं था, जब लूथर और यान हुस को कैथलिक चर्च के हाथों अपनी ‘हैरेसी’ के लिए दंड भोगना पड़ा था, हमारे समय में सलमान रुश्दी और तसलीमा नसरीन को स्वयं अपनी अंतश्चेतना की आवाज सुनने की सजा भुगतनी पड़ी है।
इसके विपरीत साहित्य के पीछे न राज्य सत्ता का बल है, न किसी धार्मिक संस्थान का आतंक। लेखकों को कारागृह में डाला जा सकता है, पुस्तकों को गली-चौराहों पर जलाया जा सकता है। ये हादसे कोई ‘प्रिमिटिव’ समाज की बर्बर सत्ताओं तले नहीं, ऐसे ‘सभ्य’ समाजों में होते थे जहाँ एक तरफ गोएटे और टॉल्स्टॉय की पूजा होती थी, दूसरी तरफ टॉमस मान और मेंडलश्टाम की पुस्तकों को पढ़ना निषिद्ध था। लिखा हुआ शब्द हमारे आधुनिक समाजों में जितना निरीह और निष्कवच रहा है, उतना शायद कभी नहीं। फिर क्या कारण है कि आततायी सत्ताओं को हमेशा वह एक खतरे भरा अंदेशा जान पड़ता है ? कहाँ छिपा है उसकी शक्ति का स्रोत ? यह स्रोत किसी बाहरी सत्ता में न होकर स्वयं शब्द के भीतर विद्यमान है। जो शब्द राजनीतिक सत्ताओं के समक्ष इतना निरीह और अवश दिखाई देता है, वही साहित्य में प्रवेश करते ही एक तरह की अज्ञात, असीमित ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। बिना शब्द के साहित्य की परिकल्पना असंभव है-इस दृष्टि से वह अन्य कलाओं से इतना भिन्न है। एक साहित्यिक कृति अपनी ऊर्जा उस भाषा से प्राप्त करती है, जिसमें वह अपने को रूपायित करती है। भाषा का सामाजिक पहलू उसके संप्रेषण में है, वहाँ वह एक ‘माध्यम’ के रूप में प्रयुक्त होती है। किंतु साहित्य के सृजन क्षेत्र में वह महज माध्यम बनकर नहीं रह पाती, बल्कि एक स्वायत्त शक्ति के रूप में प्रकट होती है। वह अपने प्रयोजन में समाजोन्मुख भले ही हो, अपने ‘होने’ के लिए समाज पर आश्रित नहीं है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन एक कविता, नाटक, उपन्यास में आते ही वे अपनी स्मृतियों, संस्कारों, संदर्भों को उजागर करते हैं, वे सामाजिक संप्रेषण की व्यावहारिक शब्दावली से कहीं अधिक ‘अस्तित्ववान’ होते हैं-‘अस्तित्ववान’ इस अर्थ में कि वे सामाजिक उपादेयता से ऊपर उठकर स्वयं मनुष्य को अपने अस्तित्व की मूलगामी स्थिति की ओर आकृष्ट करते हैं। साहित्य में प्रवेश करते ही ‘शब्द’ एक अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर लेता है।
यहाँ प्रश्न तथाकथित साहित्यिक भाषा का नहीं है, जो बोलचाल की भाषा की तुलना में कहीं अधिक बोझिल, कृत्रिम और पंडिताऊ होती है। मैं जिस अंतर की ओर संकेत कर रहा हूँ, वह भाषा के चरित्र से नहीं, उसके उपयोग से संबंध रखता है। सामाजिक और राजनीतिक सत्ताओं के लिए भाषा सिर्फ एक उपयोग का साधन है-जिसे समाचारपत्रों, राजनैतिक घोषणाओं और प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी उपादेयता का मापदंड इसमें है कि वह किस वर्ग और संप्रदाय का कितना हित साधने में सफल होती है। इसके विपरीत जो शब्द कविता और उपन्यास में प्रयुक्त होता है, उसकी शक्ति किसी सत्ता के स्वार्थ के लिए नहीं, स्वयं अपना ‘अर्थ’ उद्घाटित करने में प्रकट होती है। साहित्य के ‘मैग्नेटिक फील्ड’ में प्रवेश करते ही वह एक अद्भुत उज्जवलता, पवित्रता और ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। क्रिश्चियन धार्मिक अर्थ में वह ‘ग्रेस’ के आलोकमंडल में आ जाता है। हम चाहें तो कह सकते हैं कि जिस तरह मिथक औसत का अतिरेक है, उसी तरह कविता का शब्द स्वयं भाषा का अतिरेक है, उसकी शक्ति दूसरों तक पहुँचने में नहीं, अपनी ओर लौटने में है। अपनी ओर लौटकर ही वह साहित्य के सत्य को दूसरों तक पहुँचा सकता है।
हमने ऊपर ‘साहित्यिक शब्द’ को अस्तित्ववान कहा था-उसे थोड़ा और स्पष्ट करने की जरूरत है। हर सामाजिक सत्ता एक ऐतिहासिक क्षण की उपज है, इस अर्थ में वह समय-सापेक्ष है। वह चाहे कितनी मानववादी, कितनी लोकतांत्रिक क्यों न हो, मनुष्य के समूचे अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में हमेशा अधूरी, असंतोषजनक, अपनी ऐतिहासिक बाध्यताओं द्वारा सीमित होती है। समय उनके भीतर बहता है, इसलिए भ्रष्ट होने के कीटाणु उनमें हमेशा मौजूद रहते हैं। यथार्थ और आदर्श के बीच की अँधेरी खाई हमेशा खुली रहती है। साहित्य पर इस तरह का कोई अंकुश नहीं है। वह अपनी शक्ति भाषा के जिस स्रोत से प्राप्त करता है, वह मानव स्वभाव की चिरंतनता, समग्रता, उसके आदि स्वरूप से संबंध रखती है। इतिहास की छायाएँ उस पर जरूर हैं, उसके स्वरूप को तिरोहित नहीं करतीं, उलटे उसकी आत्यंतिक छवि, उसके ‘अस्तित्ववान’ सत्य को और अधिक सघनता और उज्जवलता में उद्घाटित करती हैं। साहि्त्य वह लीला स्थल है, जिसमें इतिहास की छाया और मनुष्य के सत्य की द्वंद्व-क्रीड़ा चलती है विश्व साहित्य के शायद सबसे शक्तिशाली प्रसंग वहाँ आते हैं, जहाँ इस द्वंद्व के कुहासे में पहली बार मनुष्य को अपने ‘अस्तित्व’ का स्वर एक मर्मांतक चीख की तरह सुनाई देता है-एक ऐसी चीख जो समस्त ऐतिहासिक और सत्य सत्ताओं को भेदती हुई समय के आर-पार चली जाती है। एक ऐसा ही दृश्य टॉल्स्टॉय अपने उपन्यास ‘युद्ध और शांति’ में प्रस्तुत करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अन्यत्र किया है और जिसे मैं दोबारा उद्धृत करना चाहूँगा।
प्रसंग युद्ध का है, जब समूचा मॉस्को शहर धू-धू जल रहा है। उपन्यास का एक मुख्य पात्र पियेर बदहवास-सा होकर जलते हुए मकानों और रोते-चीखते लोगों के हाहाकार के बीच भाग रहा है। अचानक नेपोलियन के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है।
और तब उसे लगा, जैसे वह किसी दीर्घ निद्रा से जागा है। वह सोचता है, उन्होंने मुझे बंदी बना लिया है, मैं पकड़ लिया गया हूँ। लेकिन मैं कौन ? उन्होंने किसे बंदी बनाया है, वह जो मेरी अमर आत्मा है ? वह हँसने लगा और फिर अचानक उसकी आँखें आकाश की ओर उठ गईं जहाँ मॉस्को के आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। ‘यह सब मेरा है और यह सब मैं हूँ।’ और यह विचार आते ही व्यथा का सारा बोझ उसकी आत्मा से उतर गया मानो सहसा उसने अपने और सृष्टि के बीच एक गहरा एकात्म पा लिया हो।
ऊपर के उद्धरण में, जैसा आपने नोट किया होगा, एक अजीब वाक्य आता है, ‘जैसे वह किसी दीर्घ निद्रा से जागा है।’ यह वह ‘नींद’ है जिसमें हम मरते हैं, मारते हैं, जीत और हार का खेल खेलते हैं, जहाँ मनुष्य के सब काम जैसे उसकी चेतना के बाहर अँधेरे में होते हैं। किंतु कोई ऐसा दुर्लभ क्षण आता है, जब इतिहास की कुहेलिका में नीचे सहसा हमारी आँखें खुल जाती हैं और हम अपने समूचे ‘अस्तित्व’ के प्रति सचेत हो जाते हैं, हमारे अहं और सृष्टि के बीच की दीवारें ढह जाती हैं। यह वह क्षण होता है, जब मनुष्य की ‘विभाजित अस्मिताएँ’ जिसका उल्लेख हमने आलेख के आरंभ में किया था, एक-दूसरे में घुल-मिल जाती हैं। मनुष्य अपने भूले हुए ‘मनुष्यत्व’ को पा लेता है, जहाँ वह इस धरती पर एक अनाथ व्यक्ति नहीं, एक ‘अमर आत्मा’ को जाने का चमत्कारिक अनुभव करता है। वह अपनी निर्वासित अवस्था से मुक्ति पाकर अपने खोए हुए ‘घर’ में लौट आता है।
अपने ‘संपूर्ण’ होने का जो बोध मनुष्य को साहित्य में होता है, वह एक समग्र अनुभव है। मनुष्य उसे एक स्मृति की तरह अपने भीतर सँजोकर जीता है। जिस विराट का अनुभव टॉल्स्टॉय के पात्र को युद्ध की विभीषिका तले हुआ था, हमें अपने जीवन के खंडित, जर्जरित, दिग्भ्रांत क्षणों में होता है, जब हम किसी महान् कलाकृति के संपर्क में आते हैं। जरूरी नहीं, यह अनुभव स्थायी हो। यह एक तरह का अपूर्व, अद्वितीय आनंद है- एक एक्स्टेसी का स्पंदन-जो होता भाषा में है लेकिन अपने में शब्दातीत है। क्षणिक होता हुआ भी वह एक अमिट स्मृति की छाप हम पर छोड़ जाता है। कालांतर में इन्हीं स्मृतियों की श्रृंखला एक जाति का संस्कार बन जाती है, उसकी जीवन गति को एक विशिष्ट लय प्रदान करती है। यूरोपीय मानसिकता को जहाँ बाइबिल की धार्मिक-आध्यात्मिक परंपरा ने प्रभावित किया है, वहाँ उतनी ही तेजस्विता से ग्रीक महाकाव्यों की कथाओं ने एक विशिष्ट जीवन-दृष्टि में ढाला है। पश्चिमी सभ्यता की परिकल्पना उनके बिना करना उतना ही असंभव होगा, जितना महाभारत और रामायण के बिना भारतीय संस्कृति के मूल चरित्र के संबंध में कुछ भी कहना सारहीन होगा। किसी जाति की एपिक-गाथाएँ और महाकाव्य अपनी प्रभाव शक्ति में उसके ‘धर्मग्रंथों’ से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। भारतीय परंपरा में तो एक को दूसरे से अलग करना ही असंभव होगा। रामायण और महाभारत की काव्यात्मकता उतनी ही प्रखर और ओजपूर्ण है, जितनी उनकी आध्यात्मिक गहनता (यह आकस्मिक नहीं है, कि गीता का प्रवचन युद्ध की छाया तले दिया गया था, किसी तपोवन के मनोरम परिवेश में नहीं)। भारतीय संस्कृति की ये महान् काव्य रचनाएँ न तो ओल्ड टेस्टामेंट और कुरान की तरह निरी धर्म-पुस्तकें और आचार-संहिताएँ हैं, न ग्रीक महाकाव्यों-ईलियड और ओडिसी- की तरह ‘सेक्यूलर’ साहित्यिक कृतियाँ हैं। वे दोनों हैं और दोनों में से एक भी नहीं हैं। वे मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसके उदात्त और पाशविक, गौरवपूर्ण और घृणास्पद, उजले और गँदले- उसके समस्त पक्षों को अपने प्रवाह में समेटकर बहती हैं। कला में सौंदर्य का आस्वादन और सत्य की बीहड़ खोज कोई अलग-अलग अनुभूतियाँ न होकर एक अखंडित और विराट अनुभव का साक्ष्य बन जाती है।
काव्य का यह अनुभव हमें ऐसे स्तर पर ले जाता है, जहाँ साहित्य न तो सत्ता के विरोध में है, न उसके समर्थन में। पक्ष-प्रतिपक्ष का प्रश्न वहीं उठता है, जहाँ दोनों को अलग इकाइयों में बाँटकर देखा जाता है जबकि यथार्थ में इस तरह का अलगाव असंभव है। हर सामाजिक सत्ता, वह शासन की हो अथवा किसी चर्च या धर्म-प्रतिष्ठान की, एक तरह से मनुष्य का ही बृहत्तर स्वरूप है, उसकी आंतरिक आकांक्षाओं, कामनाओं का प्रत्यक्षीकरण। इस अर्थ में हर सत्ता आधा स्वप्न, आधा यथार्थ होती है। यथार्थ में हिंसा, लोलुपता, अहम्मन्यता के तामसिक तत्त्व क्रियाशील रहते हैं, स्वप्न में उनका अतिक्रमण करके एक ‘ईश्वरीय’ व्यवस्था (संत आगस्टाइन के शब्दों में, ‘किंग्डम ऑफ गॉड’) रचने का आदर्श निहित रहता है। दार्शनिकों ने जिस ‘यूटोपिया’ की परिकल्पना की थी वह चाहे रूसो की प्राकृतिक जीवन व्यवस्था हो, मार्क्स का वर्गहीन समाज या गाँधी का रामराज्य, उनके मूल में भविष्य के आदर्श समाज का यही स्वप्न मौजूद रहता है। बाइबिल की कथा में जिस आदि मानव को ‘गार्डन ऑफ ईडन’ से बहिष्कृत करके पाप के कीचड़ में फेंक दिया था- जो यह संसार है-यह उससे उबरकर पुन: उस खोई हुई पवित्रावस्था में लौटने की लालसा है। क्या यह ‘लालसा’ हमें उस अनुभव की याद नहीं दिलाती, जो हमें संसार की महान् साहित्यिक कृतियों के संपर्क में होती है-अपनी निर्वासित अवस्था से मुक्ति पाकर अपने ‘घर’ लौटने की लालसा, ताकि मनुष्य इस धरती पर एक अजनबी बनकर न रहे ? सामाजिक क्रांतियों की परिणति कितनी ही भयावह हो, उनके उत्स में इसी आदर्शमय, काल्पनिक, स्वर्णिम समाज को धरती पर बसाने की आकांक्षा होती है। यह बात अलग है कि सफल होने पर हर क्रांति कल्पना के ‘घर’ को कारागृह के यथार्थ में बदल देती है।
सच पूछा जाए तो इस धरती पर यह कारागृह ही मनुष्य का असली घर है- बाकी सब उसकी कामनाओं का कल्पनालोक है। किंतु कल्पनालोक का सत्य भी कारागृह की दीवारों से कम यथार्थपूर्ण, कम जीवनदायी, कम शक्तिवान् नहीं होता। साहित्य हमें मुक्ति नहीं दिलाता, वह हमें बंदी होने का एहसास कराता है। वह हमारे भीतर के रिक्त स्थानों को नहीं भरता, उनमें खालीपन को दर्शाता है। यह खालीपन हर जगह है, जहाँ पहले ईश्वर वास करता था। साहित्य का शब्द ईश्वर के विरह शोक को नहीं भरता, उसे एक घाव की तरह खोलता है। इस अर्थ में हर साहित्यिक कृति सेक्यूलर सत्ताओं के मरुस्थल में एक असीम तृष्णा का अनुभव कराती है।
आधुनिक समय में हमने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया है, जहाँ से ईश्वर को ‘देश-निकाला’ दे दिया गया है। किसी दूसरे ग्रह का प्राणी अगर हमारी दुनिया के प्रवेशद्वार पर आएगा, तो वह वहाँ पर यह तख्ती देखेगा-‘ईश्वर अब यहाँ नहीं रहता !’ यदि ईश्वर कहीं है, तो उसी निर्वासित अवस्था में, जिसमें मनुष्य अपने को बिना ईश्वर के पाता है। एक दुनिया के बाहर, बहिष्कृत। दूसरा, दुनिया के भीतर निर्वासित...किंतु ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ दोनों एक-दूसरे को खोजते हुए पा लेते हैं, फिर खो देते हैं, फिर पा लेते हैं। खोने और पाने की यह आँख-मिचौली जब तक चलती रहेगी, कविता और उपन्यास लिखे जाते रहेंगे। ईश्वर एक भिखारी है, जो हर घर का दरवाजा खटखटाता है। कवि उसे अपनी आत्मा के निविड़ अंधकार और सन्नाटे में सुनता है। हमने यदि साहित्य के शब्द को ‘ग्रेस’ की महिमा दी थी, तो कुछ सोच-समझकर ही। वह शब्द के भीतर ईश्वर की खटखटाहट है, जिसे इतिहास की सत्ताएँ, अनसुना कर देती हैं। और लेखक अपनी रचना में ‘दर्ज’ कर लेता है। जिस रचना में वह खटखटाहट नहीं सुनाई देती, वह कितनी ही ‘सत्तावान’ क्यों न हो, साहित्य नहीं होती।
हमने शब्द को भाषा का अतिरेक माना था। हम चाहें तो कह सकते हैं कि ‘ईश्वर’ की अदृश्य सत्ता समस्त सत्ताओं का अतिरेक है। किसी लगे-बंधे ‘धार्मिक’ अर्थ में नहीं, बल्कि एक मनुष्येतर शक्ति के अर्थ में, जो मनुष्य के भीतर अंतनिर्हित है, उसके बाहर नहीं। साहित्य का संबंध लौकिक सत्ताओं से क्या होगा, कैसा होना चाहिए, यह अंतत: इस पर निर्भर करता है कि वह मनुष्य की इस ‘अतिरेक सत्ता’ से कैसा संबंध जोड़ता है। आज के ‘सेक्यूलर’ युग में जब मनुष्य की स्थिति को बदलने का दावा करने वाली सब क्रांतियाँ धूल में ध्वस्त हो गई हैं- लौकिक सत्ता और ‘अलौकिक’ के बीच संबंध की पड़ताल क्या नए सिरे से आरंभ नहीं होनी चाहिए ?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i