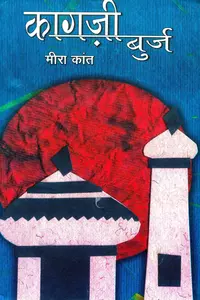|
कहानी संग्रह >> गली दुल्हनवाली गली दुल्हनवालीमीरा कांत
|
419 पाठक हैं |
|||||||
स्त्री के जीवन से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर रचनात्मक बहस को आमंत्रित करने का माद्दा इन कहानियों में भरपूर है...
कथाकार मीरा कांत की कहानियों का यह तीसरा
संग्रह है। पहले से और अधिक रची-पगी भाषा में वह इन ग्यारह कहानियों में अपने साथ बहा ले जाने की सामर्थ्य लेकर उपस्थित हुई हैं। यहां ‘धामपुर’ की
नित्या है, जो अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम नजर आती है तो ‘कागजी
बुर्ज’ की गोपा भी जो खुद के बारे में सोचते-सोचते शर्ली के
डिप्रेशन तक सोचने लगती है और अंततः भीतरी गहराई में उतरकर कागजी बुर्ज का
सही अर्थ पा जाती है। कथा यहां जीवन-सत्य की खोज भी करती है और परीक्षण
भी। तभी वह ‘स्मृति-पिंड’ के माध्यम से स्मृतियों को बचाए
रखने की कोशिश में सन्नद्ध हो जाती है। विषय की खोज एक नए कथ्य के रूप में
करती मीराजी ‘हाइफन’ जैसी कहानी लिखती हैं तो परिवार और
पारिवारिकता के बीच ‘बाबूजी की थाली’ के बहाने इस अदा में
बहुत कुछ कह जाती हैं कि पाठक स्वयं भी उस शीत गृह-युद्ध में शरीक हो जाए।
उनका कथाकार यह बखूबी जानता है कि कैसे कहानी को एक सार्वजनिक संवाद में बदल दिया जाता है। ‘नीम’ के जरिये उठाए गए सवाल ही नहीं, ‘डर के पौधे’ से आती आवाज़ें भी इसका प्रमाण हैं। संग्रह की मुख्य कहानी की नायिका दुल्हन यानी नगीना का जीवन संघर्ष इस संग्रह की प्रतिनिधि अंतरध्वनि बनकर उभरा है।
जीवन-अनुभव कथाकार के यहां अनंत हैं। उनका प्रयोग वह कथा में पूरी सावधानी और कुशलता से इस तरह करती हैं कि उपलब्ध यथार्थ के बीच से अपेक्षित यथार्थ का मार्ग बनने की संभावना भी बनी रहे और पात्र हिम्मत भी न हारें।
स्त्री के जीवन से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर रचनात्मक बहस को आमंत्रित करने का माद्दा इन कहानियों में भरपूर है।
उनका कथाकार यह बखूबी जानता है कि कैसे कहानी को एक सार्वजनिक संवाद में बदल दिया जाता है। ‘नीम’ के जरिये उठाए गए सवाल ही नहीं, ‘डर के पौधे’ से आती आवाज़ें भी इसका प्रमाण हैं। संग्रह की मुख्य कहानी की नायिका दुल्हन यानी नगीना का जीवन संघर्ष इस संग्रह की प्रतिनिधि अंतरध्वनि बनकर उभरा है।
जीवन-अनुभव कथाकार के यहां अनंत हैं। उनका प्रयोग वह कथा में पूरी सावधानी और कुशलता से इस तरह करती हैं कि उपलब्ध यथार्थ के बीच से अपेक्षित यथार्थ का मार्ग बनने की संभावना भी बनी रहे और पात्र हिम्मत भी न हारें।
स्त्री के जीवन से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों पर रचनात्मक बहस को आमंत्रित करने का माद्दा इन कहानियों में भरपूर है।
अनुक्रम
धामपुर
जाने क्यों रात और दिन पौराणिक कथाओं की तरह
जीवन में बस
गए हैं। एक के बाद एक, लगातार-लगातार। खत्म होने में ही नहीं आते। यूं ही
जीवन बिता रहे हैं एक-दूसरे का पीछा करते। जाने रात दिन का पीछा कर रही है
या दिन रात को खोजता फिर रहा है। उजाले से मुंह मोड़ती एक उदास शाम के बाद
फिर वही रात अंधेरा बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। घर के खिड़की-दरवाज़ों
को बिना चबाए निगलता हुआ। भूखा भिखारी! अपने बिस्तर पर एक और करवट बदलते
हुए सोचा नित्य ने। मन की जड़े भी बहुत अंधेरी होती हैं। आपस में उलझी
हुईं। ऐसे अंधेरे में उन्हें किन आंखों से देखा जाए! कहते हैं पृथ्वी के
नीचे सात लोग हैं यानी सात पाताल। इस मनोलोक के न जाने कितने पाताल हों!
अपने मन के इस उफान का क्या करे नित्या? बीच-बीच में करवटें बदल लेती है बस! ज्यों उबलते दूध में करछी चलाई जाती है। लगता है अब भोर के साथ ही यह आंच ठंडी होगी और उफान थमेगा। भोर के उजास का इंतजार हरेक को होता है चाहे वह भोर पाले की मारी ही क्यों न हो। उसकी भोर भी होगी कल। इस शब्द ‘कल’ के साथ ही अंधकार की काली बरौनियों में कुछ हरकत हुई। उसने पलकें खोलकर देखा तो पाया कि नित्या के चेहरे पर एक विद्रूप भरी मुस्कान थी। कुछ ही घंटों दूर खड़ा समय भी कल कहलाता है। कल जो है वही तो कहलाएगा यानी कल–जैसे उसका घर क्योंकि घर है इसलिए घर कहलाता है। तो कल सुबह उसे घर लौटना है। अपने घर!
उसे याद आया ये एक शब्द ‘घर’ कभी भीतर किसी सलोने स्वप्न-सा पींगें भरता रहता था रह-रहकर। घर एक सपना है और उसका अपना होना उससे भी बड़ा अहसास। यही तो लिखा था उसने अपनी लिपिस्टिक से अलमारी के एक पल्ले पर जड़े-बड़े आईने पर उस दिन जब पहली बार उसने चंद्रमोहन के गाजियाबाद वाले कमरे को सजाकर घर बनाया था। अब यह शब्द ‘घर’ क्यों उबलते हुए भात की तरह सीने में खदबदाता रहता है। वह झट से उठ बैठी और खुद से कहा उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। कल सुबह उसे घर लौटना है। अपने घर!
इस घुप्प अंधेरे में उसने इन शब्दों को स्वर नहीं दिया था। भला अंधेरे में कानों को शब्द दिखाई कैसे देते? इसलिए कान बेखबर रहे और मन भी। उसने तकिया उठाया और बाहर आ गई खुले में। शायद मन कुछ लंबी सांसें खींच सके यहां। आंगन में एक ओर दीवार के सहारे खड़ी चटाई को बिछाया और तकिया उस पर रख वहीं लेटना चाहा। कृष्णपक्ष की त्रयोदशी जितना प्रकाश लिए चांद शायद उसे ही देख रहा था। उस मद्धम प्रकाश में तकिये पर निगाह गई तो एक ही क्षण में उसे लगा कि वह पत्थर की मूर्ति है या कोई खंडहर क्योंकि खंडहर इतिहास और वर्तमान दोनों को जीते हैं।
मन में एक पुराना पीला-सा दृश्य थरथरा उठा। इसी मकान की छत पर बिछी खाट पर प्रभा बुआ बैठी तारकशी से तकिये के गिलाफ पर कढ़ाई कर रही थीं और पाताने बैठी नन्हीं नित्या खुली किताब हाथ में लिए गिलाफ पर कढ़े ‘स्वागतम्’ और गुलाब के फूल को देख रही थी। प्रभा बुआ उस फूल के हरे कांटे बना रही थी।
‘‘बुआ इतनी सुंदर कढ़ाई कैसे होती है?’’
‘‘मैं क्या जानूं, सूई से पूछ!’’
नाक चिढ़ाकर नित्या ने चेहरा खुली किताब में छिपा लिया था। प्रभा बुआ मुस्करा रही थीं। सूई से धागे को ऊपर की ओर खींचते हुए उन्होंने पूछा था–‘‘कहानी पढ़ रही है? कैसी है?’’
‘‘मैं क्या जानूं…किताब से पूछो!’’ कहकर नित्या अपनी हाजिरजवाबी पर खुश होकर ऐसे हँसी कि कुछ पल प्रभा बुआ अपना हाथ ऊपर का ऊपर रोककर उसे देखती रह गई थीं। फिर वह हँसी अकेली न रही थी।
नित्या के बचपन ने दूर तक प्रभा बुआ का साथ पाया था। बुआ होने के अतिरिक्त प्रभा बुआ उसकी क्या थीं? शायद बड़ी बहन, शायद छोटी मां, शायद बूढ़ी सहेली, शायद सब कुछ या शायद कुछ भी नहीं क्योंकि औरों की तरह नित्या भी नहीं जानती थी कि प्रभा बुआ आखिर कहां…! अचानक नित्या के खयाल ठिठककर कांप-से गए। कई साल पहले प्रभा बुआ का वह धामपुर से भेजा गया खत याद आया जिसमें उन्होंने खुद अपने हाथ से छोटे-छोटे सुंदर अक्षरों से सिर्फ एक कोटेशन लिखकर भेजी थी–
‘हमारे भीतर ऐसी बेइंतहा जमीन पड़ी है जिस पर कोई नक्शा नहीं खिंचा। यदि हमें अपने भीतर उठने वाली तेज हवाओं और तूफानों को समझना है तो इस जमीन का भी ध्यान रखना होगा।’
अंत में लिखा था–‘लिखने वाले का नाम नहीं लिख रही हूं क्योंकि न तुझे ये इम्तिहान के लिए याद करना है और न उससे कोई फर्क पड़ता है।’ खत में नीचे उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा था। शायद उससे भी कोई फर्क न पड़ता हो!
मन के आकाश में आकृतियों, घटनाओं और शब्दों का शोर-सा रहता है। ये आपस में कतराते-बचते हुए भी प्रायः टकरा जाते हैं। कभी शब्द ढूंढ़ता है किसी आकृति को जो बैठी होती है किसी घटना के कंधे पर सिर टिकाए तो कभी कोई आकृति पीछा करती है किसी घटना का जो अवसन्न खड़ी होती है कुछ शब्दों की ओट में।
आज इस धुंधली चांदनी में प्रभा बुआ के हाथों की कढ़ाई वाले तकिये के गिलाफ पर सिर रखकर नित्या देखना चाहती है उन क्षणों को क्रम से जिनमें उसने प्रभा बुआ को पाया था। पर कहां से लाए जाएं वे गुजरे लम्हे? सामने खड़े कुछ क्षण एक माफी मांगती-सी हँसी हँस देते हैं क्योंकि न जाने कितने क्षणों का तो रक्तपात हो चुका है। ‘‘नीतू इतिहास भूलने की नहीं, बार-बार याद करने की चीज हैं।’’ कहती थीं वह। सर्दियों की धूप का पीछा करना पड़ता है जैसे, वैसे ही नित्या गुजरे समय के पीछे हो ली। पर हाथ कितनी आ पाती है वह धूप!
प्रभा बुआ के पिता यानी नित्या के दादा कालीचरण का परिवार हापुड़ से आकर दिल्ली में तभी बस गया था जब कालीचरण की बड़ी बहन प्राणो देवी अंबिका दत्त से दिल्ली में ब्याही गई थीं। बिन मां-बाप के इन दोनों बच्चों को ताऊ ने पाला था। कालीचरण दो साल छोटे थे पर उनकी शादी पहले करवा दी गई थी क्योंकि ताई को वह अपनी सगी भतीजी के लिए भा गए थे। प्राणो के लिए लड़का मिलने में वक्त लग रहा था। फिर दिल्ली के अंबिका दत्त का रिश्ता आया जिनकी दो पत्नियों का स्वर्गवास हो चुका था। शुभ लाभ की करनी यह थी कि दहेज तो दोनों ओर से अच्छा मिला था पर परिवार का बहीखाता खाली था। सो इस बार उन्हें दहेज का अधिक लालच न था। इसलिए बिन मां-बाप की बेटी प्राणो अंबिका दत्त के इस अच्छे खाते-पीते परिवार में प्रवेश पा सकी।
इकलौता छोटा भाई कालीचरण यानी काली वह तोता था जिसमें प्राणो देवी के प्राण बसते थे। सो कुछ ही सप्ताह में अंबिका दत्त को राजी कर प्राणो देवी ने अपने काली को सदा के लिए सपरिवार अपने यहां बुला लिया था। परिवार के नाम पर कालीचरण के पास अब तक एक धर्मपत्नी और एक बेटा द्वारिका प्रसाद ही थे। अंबिका दत्त की आटे की मिल थी। काम लगातार बढ़ रहा था जिसे संभालने के लिए एक मैनेजरनुमा व्यक्ति की सख्त जरूरत थी वर्ना उनकी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आटे की गर्द से बशक्ल हो जाती। ऐसे में खास अपने साले से अधिक सगा और विश्वासपात्र मैनेजर कहां मिलता! फिर रिश्ता ऐसा कि जो दे देते ले लेता। मुंह खोलकर मांगने की हिम्मत न करता। पत्नी प्राणो पर जीवन भर का अहसान रहा सो अलग।
कालीचरण के बाकी तीन बच्चों यानी सरोज बाला, प्रह्लाद प्रसाद और प्रभा बाला ने उसी आटे की मिल के परिसर में जन्म लिया जो दिल्ली में थी। ताजिंदगी घर पर प्राणो बीबी का वर्चस्व रहा तो जिंदगियों पर अंबिका दत्त का। किस बच्चे को किस स्कूल या कॉलेज में जाना है, कितना पढ़ना है या नहीं पढ़ना है–ये फैसले मूलतः अंबिका दत्त के होते थे। खुद उनका सिर्फ एक बेटा हुआ जिसने उन्हें इस तरह के फैसलों की जिम्मेदारी से मुक्त ही रखा। आठवीं के बाद उसने विद्यालय को सदा के लिए प्रणाम किया और मोहल्ले की दादागिरी का बीड़ा उठाया। उसके रंग-ढंग देख प्राणो देवी के कहने पर अंबिका दत्त ने उसे जल्दी ही मिल के कामों में लगा दिया था। उसे उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार पैसों की उगाही का जो काम सौंपा गया था वह उसने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। इस तरह धीरे-धीरे मिल का आर्थिक पक्ष उसकी जेबों में भरने लगा। बेचारे मामा कालीचरण बहीखातों के आधे-अधूरे पन्नों को देख खून सुखाते रहते। उन्हें बरसों पहले तय किया गया वेतन मिलता जो लगातार बढ़ते परिवार पर एक फटी छोटी चादर-सा तना रहता। किसी महीने द्वारिका प्रसाद के पांव उघड़े रहते तो किसी महीने प्रह्लाद प्रसाद के, पर जिंदगी प्राणो बीबी के स्नेह की छाया में आत्मिक संतोष के साथ कट रही थी।
घर में पहला विद्रोह का स्वर प्रह्लाद की ओर से उठा जब उन्होंने आटे की मिल में जुटने से मना कर दिया। उन्होंने फिजिक्स में बी.एससी. करने की ठान ली थी। वे द्वारिका प्रसाद की तरह एकाउंट्स में बी.ए. कर सपनों में आटे की मिल देखना बर्दाश्त न कर पाते थे। बी.एससी. तक बात जैसे-तैसे निभ गई पर उसके बाद जब उन्होंने एम.एससी. की रणभेरी बजाई तो अंबिका दत्त को सख्त फैसला लेना पड़ा। प्रह्लाद प्रसाद को घर से मिलने वाली हर प्रकार की आर्थिक मदद बंद कर दी गई। अब प्रह्लाद प्रसाद ट्यूशन कर अपनी एम.एससी. करने लगे थे। उन्हें कोई मलाल न था बल्कि खुशी थी। उन्होंने सोचा भी न था कि उन्हें आटे की मिल से इस तरह इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। उनका घर मिल के परिसर में था पर दुनिया उस परिसर से बाहर थी।
उनकी इस दुनिया में घर से सिर्फ एक ही शख्स का आना-जाना था और वह थीं प्रभा बाला यानी नित्या की प्रभा बुआ। प्रभा अपने भाई प्रह्लाद से सिर्फ तीन साल छोटी थीं। पढ़ने में अच्छी थीं पर अंबिका दत्त के विचारों के अनुसार उन्हें ग्यारहवीं करवाकर सिलाई के कोर्स में डाला गया था। सिलाई-कढ़ाई वह चाव से सीखी थीं पर अधिक मन उनका लगता था प्रह्लाद भाई साहब की दी गई पुस्तकों में। प्रह्लाद भाई साहब जो किस्से-कहानियां और उपन्यास लाते थे उन्हें जब तक प्रभा न पढ़ ले वे वापस नहीं जाते थे। प्रह्लाद भाई साहब के साथ वह एक-दो बार दिल्ली विश्वविद्यालय भी हो आई थीं और उसकी वह आटे की मिल जितनी बड़ी लाइब्रेरी भी। भाई साहब के साथ रेलवे स्टेशन पर बनी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाना भी उसे बहुत भला लगता था।
अपने मन के इस उफान का क्या करे नित्या? बीच-बीच में करवटें बदल लेती है बस! ज्यों उबलते दूध में करछी चलाई जाती है। लगता है अब भोर के साथ ही यह आंच ठंडी होगी और उफान थमेगा। भोर के उजास का इंतजार हरेक को होता है चाहे वह भोर पाले की मारी ही क्यों न हो। उसकी भोर भी होगी कल। इस शब्द ‘कल’ के साथ ही अंधकार की काली बरौनियों में कुछ हरकत हुई। उसने पलकें खोलकर देखा तो पाया कि नित्या के चेहरे पर एक विद्रूप भरी मुस्कान थी। कुछ ही घंटों दूर खड़ा समय भी कल कहलाता है। कल जो है वही तो कहलाएगा यानी कल–जैसे उसका घर क्योंकि घर है इसलिए घर कहलाता है। तो कल सुबह उसे घर लौटना है। अपने घर!
उसे याद आया ये एक शब्द ‘घर’ कभी भीतर किसी सलोने स्वप्न-सा पींगें भरता रहता था रह-रहकर। घर एक सपना है और उसका अपना होना उससे भी बड़ा अहसास। यही तो लिखा था उसने अपनी लिपिस्टिक से अलमारी के एक पल्ले पर जड़े-बड़े आईने पर उस दिन जब पहली बार उसने चंद्रमोहन के गाजियाबाद वाले कमरे को सजाकर घर बनाया था। अब यह शब्द ‘घर’ क्यों उबलते हुए भात की तरह सीने में खदबदाता रहता है। वह झट से उठ बैठी और खुद से कहा उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। कल सुबह उसे घर लौटना है। अपने घर!
इस घुप्प अंधेरे में उसने इन शब्दों को स्वर नहीं दिया था। भला अंधेरे में कानों को शब्द दिखाई कैसे देते? इसलिए कान बेखबर रहे और मन भी। उसने तकिया उठाया और बाहर आ गई खुले में। शायद मन कुछ लंबी सांसें खींच सके यहां। आंगन में एक ओर दीवार के सहारे खड़ी चटाई को बिछाया और तकिया उस पर रख वहीं लेटना चाहा। कृष्णपक्ष की त्रयोदशी जितना प्रकाश लिए चांद शायद उसे ही देख रहा था। उस मद्धम प्रकाश में तकिये पर निगाह गई तो एक ही क्षण में उसे लगा कि वह पत्थर की मूर्ति है या कोई खंडहर क्योंकि खंडहर इतिहास और वर्तमान दोनों को जीते हैं।
मन में एक पुराना पीला-सा दृश्य थरथरा उठा। इसी मकान की छत पर बिछी खाट पर प्रभा बुआ बैठी तारकशी से तकिये के गिलाफ पर कढ़ाई कर रही थीं और पाताने बैठी नन्हीं नित्या खुली किताब हाथ में लिए गिलाफ पर कढ़े ‘स्वागतम्’ और गुलाब के फूल को देख रही थी। प्रभा बुआ उस फूल के हरे कांटे बना रही थी।
‘‘बुआ इतनी सुंदर कढ़ाई कैसे होती है?’’
‘‘मैं क्या जानूं, सूई से पूछ!’’
नाक चिढ़ाकर नित्या ने चेहरा खुली किताब में छिपा लिया था। प्रभा बुआ मुस्करा रही थीं। सूई से धागे को ऊपर की ओर खींचते हुए उन्होंने पूछा था–‘‘कहानी पढ़ रही है? कैसी है?’’
‘‘मैं क्या जानूं…किताब से पूछो!’’ कहकर नित्या अपनी हाजिरजवाबी पर खुश होकर ऐसे हँसी कि कुछ पल प्रभा बुआ अपना हाथ ऊपर का ऊपर रोककर उसे देखती रह गई थीं। फिर वह हँसी अकेली न रही थी।
नित्या के बचपन ने दूर तक प्रभा बुआ का साथ पाया था। बुआ होने के अतिरिक्त प्रभा बुआ उसकी क्या थीं? शायद बड़ी बहन, शायद छोटी मां, शायद बूढ़ी सहेली, शायद सब कुछ या शायद कुछ भी नहीं क्योंकि औरों की तरह नित्या भी नहीं जानती थी कि प्रभा बुआ आखिर कहां…! अचानक नित्या के खयाल ठिठककर कांप-से गए। कई साल पहले प्रभा बुआ का वह धामपुर से भेजा गया खत याद आया जिसमें उन्होंने खुद अपने हाथ से छोटे-छोटे सुंदर अक्षरों से सिर्फ एक कोटेशन लिखकर भेजी थी–
‘हमारे भीतर ऐसी बेइंतहा जमीन पड़ी है जिस पर कोई नक्शा नहीं खिंचा। यदि हमें अपने भीतर उठने वाली तेज हवाओं और तूफानों को समझना है तो इस जमीन का भी ध्यान रखना होगा।’
अंत में लिखा था–‘लिखने वाले का नाम नहीं लिख रही हूं क्योंकि न तुझे ये इम्तिहान के लिए याद करना है और न उससे कोई फर्क पड़ता है।’ खत में नीचे उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा था। शायद उससे भी कोई फर्क न पड़ता हो!
मन के आकाश में आकृतियों, घटनाओं और शब्दों का शोर-सा रहता है। ये आपस में कतराते-बचते हुए भी प्रायः टकरा जाते हैं। कभी शब्द ढूंढ़ता है किसी आकृति को जो बैठी होती है किसी घटना के कंधे पर सिर टिकाए तो कभी कोई आकृति पीछा करती है किसी घटना का जो अवसन्न खड़ी होती है कुछ शब्दों की ओट में।
आज इस धुंधली चांदनी में प्रभा बुआ के हाथों की कढ़ाई वाले तकिये के गिलाफ पर सिर रखकर नित्या देखना चाहती है उन क्षणों को क्रम से जिनमें उसने प्रभा बुआ को पाया था। पर कहां से लाए जाएं वे गुजरे लम्हे? सामने खड़े कुछ क्षण एक माफी मांगती-सी हँसी हँस देते हैं क्योंकि न जाने कितने क्षणों का तो रक्तपात हो चुका है। ‘‘नीतू इतिहास भूलने की नहीं, बार-बार याद करने की चीज हैं।’’ कहती थीं वह। सर्दियों की धूप का पीछा करना पड़ता है जैसे, वैसे ही नित्या गुजरे समय के पीछे हो ली। पर हाथ कितनी आ पाती है वह धूप!
प्रभा बुआ के पिता यानी नित्या के दादा कालीचरण का परिवार हापुड़ से आकर दिल्ली में तभी बस गया था जब कालीचरण की बड़ी बहन प्राणो देवी अंबिका दत्त से दिल्ली में ब्याही गई थीं। बिन मां-बाप के इन दोनों बच्चों को ताऊ ने पाला था। कालीचरण दो साल छोटे थे पर उनकी शादी पहले करवा दी गई थी क्योंकि ताई को वह अपनी सगी भतीजी के लिए भा गए थे। प्राणो के लिए लड़का मिलने में वक्त लग रहा था। फिर दिल्ली के अंबिका दत्त का रिश्ता आया जिनकी दो पत्नियों का स्वर्गवास हो चुका था। शुभ लाभ की करनी यह थी कि दहेज तो दोनों ओर से अच्छा मिला था पर परिवार का बहीखाता खाली था। सो इस बार उन्हें दहेज का अधिक लालच न था। इसलिए बिन मां-बाप की बेटी प्राणो अंबिका दत्त के इस अच्छे खाते-पीते परिवार में प्रवेश पा सकी।
इकलौता छोटा भाई कालीचरण यानी काली वह तोता था जिसमें प्राणो देवी के प्राण बसते थे। सो कुछ ही सप्ताह में अंबिका दत्त को राजी कर प्राणो देवी ने अपने काली को सदा के लिए सपरिवार अपने यहां बुला लिया था। परिवार के नाम पर कालीचरण के पास अब तक एक धर्मपत्नी और एक बेटा द्वारिका प्रसाद ही थे। अंबिका दत्त की आटे की मिल थी। काम लगातार बढ़ रहा था जिसे संभालने के लिए एक मैनेजरनुमा व्यक्ति की सख्त जरूरत थी वर्ना उनकी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आटे की गर्द से बशक्ल हो जाती। ऐसे में खास अपने साले से अधिक सगा और विश्वासपात्र मैनेजर कहां मिलता! फिर रिश्ता ऐसा कि जो दे देते ले लेता। मुंह खोलकर मांगने की हिम्मत न करता। पत्नी प्राणो पर जीवन भर का अहसान रहा सो अलग।
कालीचरण के बाकी तीन बच्चों यानी सरोज बाला, प्रह्लाद प्रसाद और प्रभा बाला ने उसी आटे की मिल के परिसर में जन्म लिया जो दिल्ली में थी। ताजिंदगी घर पर प्राणो बीबी का वर्चस्व रहा तो जिंदगियों पर अंबिका दत्त का। किस बच्चे को किस स्कूल या कॉलेज में जाना है, कितना पढ़ना है या नहीं पढ़ना है–ये फैसले मूलतः अंबिका दत्त के होते थे। खुद उनका सिर्फ एक बेटा हुआ जिसने उन्हें इस तरह के फैसलों की जिम्मेदारी से मुक्त ही रखा। आठवीं के बाद उसने विद्यालय को सदा के लिए प्रणाम किया और मोहल्ले की दादागिरी का बीड़ा उठाया। उसके रंग-ढंग देख प्राणो देवी के कहने पर अंबिका दत्त ने उसे जल्दी ही मिल के कामों में लगा दिया था। उसे उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार पैसों की उगाही का जो काम सौंपा गया था वह उसने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। इस तरह धीरे-धीरे मिल का आर्थिक पक्ष उसकी जेबों में भरने लगा। बेचारे मामा कालीचरण बहीखातों के आधे-अधूरे पन्नों को देख खून सुखाते रहते। उन्हें बरसों पहले तय किया गया वेतन मिलता जो लगातार बढ़ते परिवार पर एक फटी छोटी चादर-सा तना रहता। किसी महीने द्वारिका प्रसाद के पांव उघड़े रहते तो किसी महीने प्रह्लाद प्रसाद के, पर जिंदगी प्राणो बीबी के स्नेह की छाया में आत्मिक संतोष के साथ कट रही थी।
घर में पहला विद्रोह का स्वर प्रह्लाद की ओर से उठा जब उन्होंने आटे की मिल में जुटने से मना कर दिया। उन्होंने फिजिक्स में बी.एससी. करने की ठान ली थी। वे द्वारिका प्रसाद की तरह एकाउंट्स में बी.ए. कर सपनों में आटे की मिल देखना बर्दाश्त न कर पाते थे। बी.एससी. तक बात जैसे-तैसे निभ गई पर उसके बाद जब उन्होंने एम.एससी. की रणभेरी बजाई तो अंबिका दत्त को सख्त फैसला लेना पड़ा। प्रह्लाद प्रसाद को घर से मिलने वाली हर प्रकार की आर्थिक मदद बंद कर दी गई। अब प्रह्लाद प्रसाद ट्यूशन कर अपनी एम.एससी. करने लगे थे। उन्हें कोई मलाल न था बल्कि खुशी थी। उन्होंने सोचा भी न था कि उन्हें आटे की मिल से इस तरह इतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। उनका घर मिल के परिसर में था पर दुनिया उस परिसर से बाहर थी।
उनकी इस दुनिया में घर से सिर्फ एक ही शख्स का आना-जाना था और वह थीं प्रभा बाला यानी नित्या की प्रभा बुआ। प्रभा अपने भाई प्रह्लाद से सिर्फ तीन साल छोटी थीं। पढ़ने में अच्छी थीं पर अंबिका दत्त के विचारों के अनुसार उन्हें ग्यारहवीं करवाकर सिलाई के कोर्स में डाला गया था। सिलाई-कढ़ाई वह चाव से सीखी थीं पर अधिक मन उनका लगता था प्रह्लाद भाई साहब की दी गई पुस्तकों में। प्रह्लाद भाई साहब जो किस्से-कहानियां और उपन्यास लाते थे उन्हें जब तक प्रभा न पढ़ ले वे वापस नहीं जाते थे। प्रह्लाद भाई साहब के साथ वह एक-दो बार दिल्ली विश्वविद्यालय भी हो आई थीं और उसकी वह आटे की मिल जितनी बड़ी लाइब्रेरी भी। भाई साहब के साथ रेलवे स्टेशन पर बनी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाना भी उसे बहुत भला लगता था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i