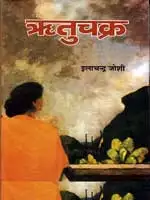|
उपन्यास >> ऋतुचक्र ऋतुचक्रइलाचन्द्र जोशी
|
253 पाठक हैं |
|||||||
श्री इलाचन्द्र जोशी का एक अत्यन्त रोचक रोमांचक उपन्यास...
श्री इलाचन्द्र जोशी हिंदी के अत्यंत
अतिष्ठित उपन्यासकार थे। उनके प्रायः सभी उपन्यासों का गठन हमारे समाज के
जिन पात्रों के आधार पर हुआ है वे मनोवैज्ञानिक सार्थकता के लिए सर्वथा
अद्वितीय हैं।
प्रस्तुत उपन्यास ऋतुचक्र एक अत्यन्त रोचक रोमांचक उपन्यास है जिसमें सुरम्य पहाड़ी प्रकृति के अन्तर्प्राणों में छिपे आनंद-कोष के मूलतत्वों का उद्घाटन, आज के रेगिस्तानी जीवन की विश्वव्यापी धूल और धुएँ के भीतर से हरियाली के बिखरे हुए बीजों की खोज, सामूहिक पागलपन के विरुद्ध वैयक्तिक आत्मा के विद्रोह का परिचित्रण, रोमांस की एकदम नई और मौलिक परिकल्पना, रोमांचक रोमांसों के रहस्यों की मार्मिक अन्तरकथा, युग-जीवन की विसंगतियों की कहानी इत्यादि तथ्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
आशा है पुस्तक पाठकों का मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगी।
प्रस्तुत उपन्यास ऋतुचक्र एक अत्यन्त रोचक रोमांचक उपन्यास है जिसमें सुरम्य पहाड़ी प्रकृति के अन्तर्प्राणों में छिपे आनंद-कोष के मूलतत्वों का उद्घाटन, आज के रेगिस्तानी जीवन की विश्वव्यापी धूल और धुएँ के भीतर से हरियाली के बिखरे हुए बीजों की खोज, सामूहिक पागलपन के विरुद्ध वैयक्तिक आत्मा के विद्रोह का परिचित्रण, रोमांस की एकदम नई और मौलिक परिकल्पना, रोमांचक रोमांसों के रहस्यों की मार्मिक अन्तरकथा, युग-जीवन की विसंगतियों की कहानी इत्यादि तथ्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
आशा है पुस्तक पाठकों का मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगी।
ऋतुचक्र
‘‘क-कु-कु-क्रू-कुर-कुर-कुर !’’
यह चिड़िया बोल रही थी।
‘‘हे-हे-हे-ए-ए ! हँ-हँ-हँ-हँ ! हा-हा-हा-हा-हा-,!’’ यह आदमी बोल रहा था चारों ओर ऊँचे पहाड़ी पर क़तारों में खड़े देवदारु के लम्बे-लम्बे और नुकीले पेड़ों की छाया सघन से सघनतर होती चली आ रही थी। उन पेड़ों की चोटियाँ पहाड़ों के उस पार डूबते हुए सूरज की अंतिम पीली धूप से, जो हरीतिमा में घुली हुई थी, एक नये ही रंग से झिलमिला रही थीं।
पिछले दो दिन काफी अच्छा पानी बरस गया था। भरपूर जेठ के महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी-कभी भाग्य से ही हो जाती है। पानी बरसने के कारण उत्तर क्षितिज में जमी हुई धूल गलकर धुल गयी थी। उस क्षितिज के ऊपर पहाड़ों की दो नीली क़तारों के पीछे तीन-चार ऊँचे और बड़े-बड़े चाँदी के-से गुंबद उठे हुए थे, जिनकी चोटियों पर सुनहरा रंग गाढ़ा होता चला जा रहा था। वे चिर-परिचित से हिम-शिखर आज काफ़ी दिनों बाद अचानक दिखायी दिये थे। दादा को लगा, जैसे आज पहली बार उन्हें देख रहे हों। वह उस टीले पर खड़े होकर, छड़ी की नोक एक उभरते हुए पत्थर से टिकाये, एकटक, निःस्पंद आँखों से काफ़ी देर से उसी ओर दृष्टि गड़ाये हुए थे। लगता था, जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में स्थित सोने के तीन विशाल मंदिर, युग-युग से कर्मक्लांत मानव को किसी जादू की-सी माया से भुलावा देकर, निरंतर अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं।
दूर सामने, बहुत नीचे, एक छोटी-सी नदी बही चली जा रही थी। वह इतनी दूरी पर थी कि लगता था, जैसे वह सचमुच की नहीं, वरन किसी चित्र में उतारी गयी नदी हो। उसकी केवल एक टुकड़ी ही देखने में आती थी–तलवार की तरह बाँकी। उस तलवार पर भी डूबते हुए सूरज के सोने का पानी चढ़ता, हिलता-डुलता और उछलता चला जा रहा था।
दादा टीले पर एकमात्र देवदारू की छत्र-छाया में खड़े थे। वह स्थान एक ऐसे कोण पर स्थित था कि सुदूर सामने की उस बाँकी तलवार पर चढ़ा वह सुनहला पानी–उतनी दूरी के बावजूद–उनकी आँखों से टकराकर उन्हें चौंधिया रहा था। जैसे कोई नटखट बच्चा, उन्हें खिझाने के लिये, एक शीशे पर पड़ी परछाँई उनकी आँखों में फेंक रहा हो।
दादा छड़ी को पत्थर पर टिकाये ही रहे। अपने चारों ओर के दृश्यों को वह आँखों और कानों से पीते हुए, एकांत ध्यान में मग्न, मन्त्रमुग्ध से खड़े थे। जैसे समाधि लग गयी हो। वह ऊपर बन्द गले का लम्बा-सा, अचकननुमाँ गरम काला कोट पहने थे। और नीचे झलझलाती हुई धोती, जो चुस्त पाजामें की तरह दिखाई देती थी। काले रंग के पंप शू के ऊपर हलके आसमानी रंग के मोजे कुछ अजब ही रंग दे रहे थे। गोरे रंग पर उभरी हुई नुकीली नाक, काली और धनुषाकार तीखी भवें उनकी बुद्धि और अनुभूति की प्रखरता का परिचय दे रही थीं। सुन्दर, लम्बी और खिची-सी, बादाम के आकारवाली आँखों पर एक मुग्ध, मोहक विस्मय का-सा भाव चश्मे की तरह चमक रहा था।
नीचे दाँए और बाँए दोनों ओर फैली हुई, बाँज और देवदारू के सधन पुंजों से हरी-भरी दो घाटियाँ, जैसे एक नीरव निराली और कटीली पुलक से सिहरती हुई-सी, अलग-अलग दिशाओं से आकर, एक-दूसरे से प्रायः मिलती हुई, एक चौड़ा त्रिकोण बना रही थीं। बीच में, ऊपर से आता हुआ एक नाला, ज्यामिति के लम्ब की तरह उस त्रिकोण को बीचों-बीच विभक्त कर रहा था। नाले की दोनों ओर दो छोटे-छोटे पटों पर अंकित वनों में देवदारू के ऊँचे, घने, नुकीले और कटीले पेड़ों की कतारें फौजी सिपाहियों की तरह कायदे से खड़ी थीं।
दोनों तस्वीरनुमाँ घाटियाँ न जाने कितने युगों से एक-दूसरे से मिलने, एक-दूसरे का स्पर्श करने के लिये विकल पड़ी हुई थीं ! पर हाय रे एक नाले का व्यवधान ! छोटा किन्तु क्रूर और दुर्लंघ्य ! उस एकांत सन्नाटे में, जाने कैसे, दादा के मन में यह विचित्र कल्पना घर कर गयी और घर करते ही ऐसी सजीव बन गयी कि उनके अन्तर को कचोटने लगी। जैसे वे दो हरी घाटियाँ सचमुच में रक्त-मांस की बनी हों। दोनों जैसे सप्राण रूप से एक-दूसरे से मिलने–एक-दूसरे को छूने के लिये तड़प रही हों; और निकट की वह दूरी दोनों को जैसे और अधिक प्रेम-विह्वल करके, युग-युग से दोनों में कभी पुलक और कभी उच्छ्वास भरती चली आती हों। दोनों के पुलकित रोएँ जैसे देवदारु की ऊर्ध्वमुखी कटीली चोटियों के रूप में सीधे खड़े हो गये हों।
तभी सहसा कोई अकेली चिड़िया सामने बुरूँस के बड़े-से पेड़ पर लगे अंगारे से फूलों के भीतर छिपकर ‘कु-क्रू-कुर-कुर-कुर’ की आवाज में बोल उठी। दादा चौंक पड़े और उनका ध्यान उचटा।
किसी विचित्र काकताली से, सामने उस पारवाले पहाड़ की पगडंडी से ‘हे-हे-हे-!-हँ-हँ-हँ–गुलि-गुलि-गुलि ! हा-हा-हा-हा-हा’ की-सो एक अनोखी बोली किसी मानव-कंठ से निकलती हुई सुनायी दी। दादा ने फिर एक बार चौंकते हुए उस ओर नजर डाली। किसी चरवाहे का एक नौजवान छोकरा, मटमैले रंग का कालरदार कोट और उसी रंग का चुस्त पाजामा पहने, एक पलती-सी बेंतनुमाँ छड़ी हाथ में लिये, गायों और भैसों को दिन-भर चराने के बाद धीमी चाल से वारस चला जा रहा था। सबसे आगेवाली जो गाय रास्ते से भटककर, पगडंडी के नीचे, घाटीवाले खड्ड की ओर पाँव बढ़ाने लगी थी, उसे वापस बुलाने के लिये वह छोकरा उस निराली और अमावीय भाषा में उससे कुछ कह रहा था। आश्चर्य से दादा ने देखा कि उस विचित्र बोली को सुनते ही भटकी हुई गाय जैसे उसका अर्थ समझ गयी। वह सहसा ऊपर की ओर इस तरह लौट पड़ी जैसे अपराध करती हुई पकड़ ली गयी हो।
और तभी छोकरे ने छड़ीनुमाँ लकड़ी को बगल में दबाकर अपने मैले-कुचैले कोट की बाई पाकिट से एक बाँसुरी निकाली। उसे ओठों से लगाकर, उसके छेदों पर दोनों हाथों की उँगलियाँ बड़ी तेजी से फेरते हुए, उसने अचानक एक अपूर्व मोहक धुन निकाली और फिर एक लम्बा, विलंबित पहाड़ी राग बजाया। वह धुन अगल-बगल की पहाड़ियों को पुलकित करती और नीचे की घाटियों को गुँजाती हुई, लौटकर ऊपर को आयी और देवदारु और बाँज की चोटियों से टकराकर, उत्तरी क्षितिज पर खड़े होने और चाँदी के पिरामिडों की ओर बढ़ती हुई, उनमें सिहरन पैदा करने लगी।
दादा के कान जैसे उसी धुन की तरंग का ग्राफ बना रहे थे। उसी ग्राफ का अनुसरण करते हुए उन्होंने आँखें घुमायीं। वे उन्हीं नुकीले और बड़े-बड़े प्रिज्यों पर जा टिकीं। जिन पर डूबते सूरज की किरनें उसी राग से सिहरती हुई झिलमिला रही थीं। किरनों के काँपते हुए सुनहरे तार उसी धुन के ताल और लय के साथ झंकृत होने लगे थे।
और तभी दादा ने देखा, बड़ी तेजी से पच्छिमी क्षितिज को भेदकर ढलता हुआ सुनहला सूरज, एक बड़े से पहाड़ी पिरामिड नुकीली चोटी के नीचे, तीन-चौथाई से अधिक डूब चुका था। अब केवल उसके ऊपर चमकते हुए ताज वाला अंश ही शेष रह गया था। पर कैसा मनोरम मुकुट था वह ! नीली झाँइयों वाली चोटियों के क्षितिज पर, हल्के मटमैले से मोटे बादल की सपाट रेखा पर, चिर-प्रसन्न, चिर-आनन्दमय, चिर-मुक्त और चिर-निष्कलंक माया से दीप्त, चिर-परिचित सूर्यराज का चिर-मंगलमय मुकुट ! लम्बे से बादल की मोटी-गाढ़ी परतों को पूरे अधिकार से चीरती हुई उसकी किरनें दलदल में फँसने लगी थीं। फँसने पर भी अपने हजारों गुना अधिक लम्बें आकार और बड़े-बड़े समान कोणवाले पंखों को नाचनेवाले मोर की तरह, उस मुकुट के नीचे, ऊपर, दाँए, बाँए–चारों ओर फैलाये हुए थीं।
इस तरह की अनेक साँझें दादा उसी टीले पर से देख चुके थे। पर इस तरह का मुकुट रोज-रोज नहीं दिखाई देता।
झिलमिलाती हुई और बारीक बुने हुए सुनहले झालर के भीतर से बिखरती हुई, किरनें उनकी चमकती हुई आँखों पर बुरी तरह हमला कर रही थीं। पर दादा तन से, मन से और आत्मा से उस हमले का स्वागत कर रहे थे। उनकी आँखें एक अभौतिक अनुभूति की मोहक माया से चमकने लगी थीं। वह तब तक उस ओर एकटक देखते रहे जब तक वह अभिनव मुकुट, अपनी विपुल महिमा के साथ, देखते-देखते आँखों से ओझल न हो गया।
एक पतली सुनहरी रेखा अब भी पश्चिम क्षितिज के नुकीले पेड़ों की कतार के ऊपर से गुजरती हुई, अंतिम उजले सन्नाटे का आलिम्पन लिख रही थी। उत्तरी क्षितिज पर, आकाश की ओर भागने का प्रयास करनेवाली चाँदी के बड़े-बड़े गुंबदों के कलशों के नीचे तक सुनहला पानी चढ़ा हुआ था, जो कुछ नीचे से धीरे-धीरे तमैला होने के लक्षण प्रकट कर रहा था।
पलक मारते-मारते पश्चिमी क्षितिज की स्वर्णिम रेखा ताँबें में पिघलकर नीचे गिर गयी। उत्तर के सफेद पिरामिड पर अब सोने के बदले ताँबा जमने लगा था। दादा उस ओर एकटक देख रहे थे–चारों ओर एक एकांत और आश्चर्यजनक सन्नाटे के बीच उनका देखना और अनुभव करना एक हो गया था। वह सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ अनुभव कर रहे थे, पर कुछ भी देख नहीं रहे थे और कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे थे–केवल एक अनुभूति को छोड़कर। कमर तक आधा पिरामिड ताँबे का, कमर के नीचे सफेद पिरामिड जैसे महानारी बन गया था। ऊपर की अथाह नीलाई में उड़कर मग्न हो जाने का प्रयास करती हुई महांगना। उस महा-सौन्दर्य का अस्तित्व पृथ्वी की मिट्टी में सम्भव नहीं था।
जब तक सारा ताँबा फुँककर एकदम सफेद राख न बन गया तब तक दादा उसी समाधि की-सी अवस्था में खड़े रहे। जब समाधि भंग हुई तब सोचने लगे कि किस विचित्र रहस्यानुभूति में खोये रहे इतनी देर तक ! आधे क्षण के लिये भूल गये कि वह अनुभूति क्या थी, जो अभी तक मन और प्राण को गुदगुदा रही थी। तुरन्त ही याद आ गया। एक अपूर्व सुन्दरी महानील को गोद पकड़-कर उड़ने और उसी में विलीन होने को आतुर है। मन-ही-मन कहने लगे : ‘‘कैसा अद्भूत, अपूर्व दृश्य था वह ! और कितना प्यारा, कितना सुखकर, घरेलू–’’ और ‘घरेलू’ कहते-कहते रुक गये–हैं ! यह सब क्या ! ‘घरेलू !’ और यह सारा रूपक ! कैसा अद्भुत और अर्थहीन था वह ! पिरामिड एक महारानी ! ऐसे विराट का परिकल्प पुरुष न होकर नारी के रूप में उनके सामने आया ! और वह मूक अट्टाहास कर उठे। फिर गम्भीर वैज्ञानिक विवेक से सोचने लगे : ‘‘पर वह प्यारी, परिपूर्ण रूप से मग्न कर देनेवाली, सहज-सुखद अनुभूति आयी क्यों, कैसे और कहाँ से ? और फिरा ऐसा विराट दृश्य ‘घरेलू’ क्यों, लगा ? ठीक है, आ रही है बात कुछ पकड़ में–पिरामिड की वह अपूर्व रंगमयी विराट नारी पृथ्वी के मध्याकर्षण के बन्धन से मुक्त होकर, प्रतिपल फिसलते हुए अनंत को पकड़कर, उसे सांत और अनंत की संध्या-रेखा में चिरकाल के लिये बाँधने के लिये विकल है। सम्पूर्ण सांत एक विराट नारी है और महानील निवासी अनंत एकमात्र विश्व-पुरुष। छायी हुई यह नारी समय विश्व-जीवन की परिधि के चारों ओर–और केन्द्र के भी केन्द्र में। प्रतिक्षण और प्रतिरण को बाँधती हुईष वह महानील और महानारी की गोद में लेटी हुई है–अनादि युग से लेकर अनंत के अछोर तक वह कैसी ही थी और वैसी ही रहेगी। जो युग-युग में परिवर्तनशील चक्र नये-नये रूपों में चलता चला आ रहा है वह है उस महापरिधि के भीतर स्थित उन अनंत क्षणों और असंख्य कणों का खेल।
‘‘पर इस सारे चक्कर का अर्थ क्या हो सकता है ?’’ दादा के भीतर फिर प्रश्न उठा। और फिर बिजली की तरह उत्तर भी दिमाग में कौंध गया; ‘‘अर्थ कुछ नहीं, केवल खेल और केवल नयी-नयी रहस्यात्मक अनुभूतियाँ। खेल का क्या अर्थ हो सकता था ? केवल रस-मग्नता ! केवल नित नयी रागानुभूति ! सुख-दुःख, संघर्ष-विघर्ष, राग-रंग, स्वार्थ की छीना-झपटी, शक्ति-मद का नंगापन–सब इसी खेल के अंग हैं।’’
दादा ने फिर एक बार हिम-शिखरो की ओर दृष्टि गड़ायी। विराटा नारी की वेश-भूषा का रंग धीरे-धीरे उड़ता जा रहा था। पर क्षितिज के ऊपर सारा आकाश एक निराली गुलाबी ज्वाली में बदल गया था। बीच में, छिटपुट रूप से तैरनेवाले बादलों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ गुलेनारी आग से दहकने लगी थीं। दृश्य की इन्द्रियातीत मोहकता गहरी से और गहरी होती जा रही थी।
दादा को लगा कि उनकी आँखें और पाँव अपने बस के नहीं रहे। ये दोनों जैसे पंख बनकर उन्हें सामने वाले ऊर्ध्व-क्षितिज के मायालोक की ओर बरबस उड़ाये लिये जा रहे हों। सारे जग की चंचल व्याकुलता, सारे जीवन की कुटिल काँटेदार अशांति, समस्त युग का सब कुछ लील लेने वाला अंधकार एक अस्पष्ट, धुँधले, काले स्वप्न की तरह पल में काफूर हो गया। सब कुछ ऐसी मोहक रंगीनी में बदल गया, जिसे छाती से चिपकाने के लिये दादा जैसे युग-युग से, जन्म-जन्म से व्याकुल थे।
‘‘हे-हे-हे-ए-ए ! हँ-हँ-हँ-हँ ! हा-हा-हा-हा-हा-,!’’ यह आदमी बोल रहा था चारों ओर ऊँचे पहाड़ी पर क़तारों में खड़े देवदारु के लम्बे-लम्बे और नुकीले पेड़ों की छाया सघन से सघनतर होती चली आ रही थी। उन पेड़ों की चोटियाँ पहाड़ों के उस पार डूबते हुए सूरज की अंतिम पीली धूप से, जो हरीतिमा में घुली हुई थी, एक नये ही रंग से झिलमिला रही थीं।
पिछले दो दिन काफी अच्छा पानी बरस गया था। भरपूर जेठ के महीने में इस प्रकार की वर्षा कभी-कभी भाग्य से ही हो जाती है। पानी बरसने के कारण उत्तर क्षितिज में जमी हुई धूल गलकर धुल गयी थी। उस क्षितिज के ऊपर पहाड़ों की दो नीली क़तारों के पीछे तीन-चार ऊँचे और बड़े-बड़े चाँदी के-से गुंबद उठे हुए थे, जिनकी चोटियों पर सुनहरा रंग गाढ़ा होता चला जा रहा था। वे चिर-परिचित से हिम-शिखर आज काफ़ी दिनों बाद अचानक दिखायी दिये थे। दादा को लगा, जैसे आज पहली बार उन्हें देख रहे हों। वह उस टीले पर खड़े होकर, छड़ी की नोक एक उभरते हुए पत्थर से टिकाये, एकटक, निःस्पंद आँखों से काफ़ी देर से उसी ओर दृष्टि गड़ाये हुए थे। लगता था, जैसे पृथ्वी और आकाश के बीच में स्थित सोने के तीन विशाल मंदिर, युग-युग से कर्मक्लांत मानव को किसी जादू की-सी माया से भुलावा देकर, निरंतर अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं।
दूर सामने, बहुत नीचे, एक छोटी-सी नदी बही चली जा रही थी। वह इतनी दूरी पर थी कि लगता था, जैसे वह सचमुच की नहीं, वरन किसी चित्र में उतारी गयी नदी हो। उसकी केवल एक टुकड़ी ही देखने में आती थी–तलवार की तरह बाँकी। उस तलवार पर भी डूबते हुए सूरज के सोने का पानी चढ़ता, हिलता-डुलता और उछलता चला जा रहा था।
दादा टीले पर एकमात्र देवदारू की छत्र-छाया में खड़े थे। वह स्थान एक ऐसे कोण पर स्थित था कि सुदूर सामने की उस बाँकी तलवार पर चढ़ा वह सुनहला पानी–उतनी दूरी के बावजूद–उनकी आँखों से टकराकर उन्हें चौंधिया रहा था। जैसे कोई नटखट बच्चा, उन्हें खिझाने के लिये, एक शीशे पर पड़ी परछाँई उनकी आँखों में फेंक रहा हो।
दादा छड़ी को पत्थर पर टिकाये ही रहे। अपने चारों ओर के दृश्यों को वह आँखों और कानों से पीते हुए, एकांत ध्यान में मग्न, मन्त्रमुग्ध से खड़े थे। जैसे समाधि लग गयी हो। वह ऊपर बन्द गले का लम्बा-सा, अचकननुमाँ गरम काला कोट पहने थे। और नीचे झलझलाती हुई धोती, जो चुस्त पाजामें की तरह दिखाई देती थी। काले रंग के पंप शू के ऊपर हलके आसमानी रंग के मोजे कुछ अजब ही रंग दे रहे थे। गोरे रंग पर उभरी हुई नुकीली नाक, काली और धनुषाकार तीखी भवें उनकी बुद्धि और अनुभूति की प्रखरता का परिचय दे रही थीं। सुन्दर, लम्बी और खिची-सी, बादाम के आकारवाली आँखों पर एक मुग्ध, मोहक विस्मय का-सा भाव चश्मे की तरह चमक रहा था।
नीचे दाँए और बाँए दोनों ओर फैली हुई, बाँज और देवदारू के सधन पुंजों से हरी-भरी दो घाटियाँ, जैसे एक नीरव निराली और कटीली पुलक से सिहरती हुई-सी, अलग-अलग दिशाओं से आकर, एक-दूसरे से प्रायः मिलती हुई, एक चौड़ा त्रिकोण बना रही थीं। बीच में, ऊपर से आता हुआ एक नाला, ज्यामिति के लम्ब की तरह उस त्रिकोण को बीचों-बीच विभक्त कर रहा था। नाले की दोनों ओर दो छोटे-छोटे पटों पर अंकित वनों में देवदारू के ऊँचे, घने, नुकीले और कटीले पेड़ों की कतारें फौजी सिपाहियों की तरह कायदे से खड़ी थीं।
दोनों तस्वीरनुमाँ घाटियाँ न जाने कितने युगों से एक-दूसरे से मिलने, एक-दूसरे का स्पर्श करने के लिये विकल पड़ी हुई थीं ! पर हाय रे एक नाले का व्यवधान ! छोटा किन्तु क्रूर और दुर्लंघ्य ! उस एकांत सन्नाटे में, जाने कैसे, दादा के मन में यह विचित्र कल्पना घर कर गयी और घर करते ही ऐसी सजीव बन गयी कि उनके अन्तर को कचोटने लगी। जैसे वे दो हरी घाटियाँ सचमुच में रक्त-मांस की बनी हों। दोनों जैसे सप्राण रूप से एक-दूसरे से मिलने–एक-दूसरे को छूने के लिये तड़प रही हों; और निकट की वह दूरी दोनों को जैसे और अधिक प्रेम-विह्वल करके, युग-युग से दोनों में कभी पुलक और कभी उच्छ्वास भरती चली आती हों। दोनों के पुलकित रोएँ जैसे देवदारु की ऊर्ध्वमुखी कटीली चोटियों के रूप में सीधे खड़े हो गये हों।
तभी सहसा कोई अकेली चिड़िया सामने बुरूँस के बड़े-से पेड़ पर लगे अंगारे से फूलों के भीतर छिपकर ‘कु-क्रू-कुर-कुर-कुर’ की आवाज में बोल उठी। दादा चौंक पड़े और उनका ध्यान उचटा।
किसी विचित्र काकताली से, सामने उस पारवाले पहाड़ की पगडंडी से ‘हे-हे-हे-!-हँ-हँ-हँ–गुलि-गुलि-गुलि ! हा-हा-हा-हा-हा’ की-सो एक अनोखी बोली किसी मानव-कंठ से निकलती हुई सुनायी दी। दादा ने फिर एक बार चौंकते हुए उस ओर नजर डाली। किसी चरवाहे का एक नौजवान छोकरा, मटमैले रंग का कालरदार कोट और उसी रंग का चुस्त पाजामा पहने, एक पलती-सी बेंतनुमाँ छड़ी हाथ में लिये, गायों और भैसों को दिन-भर चराने के बाद धीमी चाल से वारस चला जा रहा था। सबसे आगेवाली जो गाय रास्ते से भटककर, पगडंडी के नीचे, घाटीवाले खड्ड की ओर पाँव बढ़ाने लगी थी, उसे वापस बुलाने के लिये वह छोकरा उस निराली और अमावीय भाषा में उससे कुछ कह रहा था। आश्चर्य से दादा ने देखा कि उस विचित्र बोली को सुनते ही भटकी हुई गाय जैसे उसका अर्थ समझ गयी। वह सहसा ऊपर की ओर इस तरह लौट पड़ी जैसे अपराध करती हुई पकड़ ली गयी हो।
और तभी छोकरे ने छड़ीनुमाँ लकड़ी को बगल में दबाकर अपने मैले-कुचैले कोट की बाई पाकिट से एक बाँसुरी निकाली। उसे ओठों से लगाकर, उसके छेदों पर दोनों हाथों की उँगलियाँ बड़ी तेजी से फेरते हुए, उसने अचानक एक अपूर्व मोहक धुन निकाली और फिर एक लम्बा, विलंबित पहाड़ी राग बजाया। वह धुन अगल-बगल की पहाड़ियों को पुलकित करती और नीचे की घाटियों को गुँजाती हुई, लौटकर ऊपर को आयी और देवदारु और बाँज की चोटियों से टकराकर, उत्तरी क्षितिज पर खड़े होने और चाँदी के पिरामिडों की ओर बढ़ती हुई, उनमें सिहरन पैदा करने लगी।
दादा के कान जैसे उसी धुन की तरंग का ग्राफ बना रहे थे। उसी ग्राफ का अनुसरण करते हुए उन्होंने आँखें घुमायीं। वे उन्हीं नुकीले और बड़े-बड़े प्रिज्यों पर जा टिकीं। जिन पर डूबते सूरज की किरनें उसी राग से सिहरती हुई झिलमिला रही थीं। किरनों के काँपते हुए सुनहरे तार उसी धुन के ताल और लय के साथ झंकृत होने लगे थे।
और तभी दादा ने देखा, बड़ी तेजी से पच्छिमी क्षितिज को भेदकर ढलता हुआ सुनहला सूरज, एक बड़े से पहाड़ी पिरामिड नुकीली चोटी के नीचे, तीन-चौथाई से अधिक डूब चुका था। अब केवल उसके ऊपर चमकते हुए ताज वाला अंश ही शेष रह गया था। पर कैसा मनोरम मुकुट था वह ! नीली झाँइयों वाली चोटियों के क्षितिज पर, हल्के मटमैले से मोटे बादल की सपाट रेखा पर, चिर-प्रसन्न, चिर-आनन्दमय, चिर-मुक्त और चिर-निष्कलंक माया से दीप्त, चिर-परिचित सूर्यराज का चिर-मंगलमय मुकुट ! लम्बे से बादल की मोटी-गाढ़ी परतों को पूरे अधिकार से चीरती हुई उसकी किरनें दलदल में फँसने लगी थीं। फँसने पर भी अपने हजारों गुना अधिक लम्बें आकार और बड़े-बड़े समान कोणवाले पंखों को नाचनेवाले मोर की तरह, उस मुकुट के नीचे, ऊपर, दाँए, बाँए–चारों ओर फैलाये हुए थीं।
इस तरह की अनेक साँझें दादा उसी टीले पर से देख चुके थे। पर इस तरह का मुकुट रोज-रोज नहीं दिखाई देता।
झिलमिलाती हुई और बारीक बुने हुए सुनहले झालर के भीतर से बिखरती हुई, किरनें उनकी चमकती हुई आँखों पर बुरी तरह हमला कर रही थीं। पर दादा तन से, मन से और आत्मा से उस हमले का स्वागत कर रहे थे। उनकी आँखें एक अभौतिक अनुभूति की मोहक माया से चमकने लगी थीं। वह तब तक उस ओर एकटक देखते रहे जब तक वह अभिनव मुकुट, अपनी विपुल महिमा के साथ, देखते-देखते आँखों से ओझल न हो गया।
एक पतली सुनहरी रेखा अब भी पश्चिम क्षितिज के नुकीले पेड़ों की कतार के ऊपर से गुजरती हुई, अंतिम उजले सन्नाटे का आलिम्पन लिख रही थी। उत्तरी क्षितिज पर, आकाश की ओर भागने का प्रयास करनेवाली चाँदी के बड़े-बड़े गुंबदों के कलशों के नीचे तक सुनहला पानी चढ़ा हुआ था, जो कुछ नीचे से धीरे-धीरे तमैला होने के लक्षण प्रकट कर रहा था।
पलक मारते-मारते पश्चिमी क्षितिज की स्वर्णिम रेखा ताँबें में पिघलकर नीचे गिर गयी। उत्तर के सफेद पिरामिड पर अब सोने के बदले ताँबा जमने लगा था। दादा उस ओर एकटक देख रहे थे–चारों ओर एक एकांत और आश्चर्यजनक सन्नाटे के बीच उनका देखना और अनुभव करना एक हो गया था। वह सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ अनुभव कर रहे थे, पर कुछ भी देख नहीं रहे थे और कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे थे–केवल एक अनुभूति को छोड़कर। कमर तक आधा पिरामिड ताँबे का, कमर के नीचे सफेद पिरामिड जैसे महानारी बन गया था। ऊपर की अथाह नीलाई में उड़कर मग्न हो जाने का प्रयास करती हुई महांगना। उस महा-सौन्दर्य का अस्तित्व पृथ्वी की मिट्टी में सम्भव नहीं था।
जब तक सारा ताँबा फुँककर एकदम सफेद राख न बन गया तब तक दादा उसी समाधि की-सी अवस्था में खड़े रहे। जब समाधि भंग हुई तब सोचने लगे कि किस विचित्र रहस्यानुभूति में खोये रहे इतनी देर तक ! आधे क्षण के लिये भूल गये कि वह अनुभूति क्या थी, जो अभी तक मन और प्राण को गुदगुदा रही थी। तुरन्त ही याद आ गया। एक अपूर्व सुन्दरी महानील को गोद पकड़-कर उड़ने और उसी में विलीन होने को आतुर है। मन-ही-मन कहने लगे : ‘‘कैसा अद्भूत, अपूर्व दृश्य था वह ! और कितना प्यारा, कितना सुखकर, घरेलू–’’ और ‘घरेलू’ कहते-कहते रुक गये–हैं ! यह सब क्या ! ‘घरेलू !’ और यह सारा रूपक ! कैसा अद्भुत और अर्थहीन था वह ! पिरामिड एक महारानी ! ऐसे विराट का परिकल्प पुरुष न होकर नारी के रूप में उनके सामने आया ! और वह मूक अट्टाहास कर उठे। फिर गम्भीर वैज्ञानिक विवेक से सोचने लगे : ‘‘पर वह प्यारी, परिपूर्ण रूप से मग्न कर देनेवाली, सहज-सुखद अनुभूति आयी क्यों, कैसे और कहाँ से ? और फिरा ऐसा विराट दृश्य ‘घरेलू’ क्यों, लगा ? ठीक है, आ रही है बात कुछ पकड़ में–पिरामिड की वह अपूर्व रंगमयी विराट नारी पृथ्वी के मध्याकर्षण के बन्धन से मुक्त होकर, प्रतिपल फिसलते हुए अनंत को पकड़कर, उसे सांत और अनंत की संध्या-रेखा में चिरकाल के लिये बाँधने के लिये विकल है। सम्पूर्ण सांत एक विराट नारी है और महानील निवासी अनंत एकमात्र विश्व-पुरुष। छायी हुई यह नारी समय विश्व-जीवन की परिधि के चारों ओर–और केन्द्र के भी केन्द्र में। प्रतिक्षण और प्रतिरण को बाँधती हुईष वह महानील और महानारी की गोद में लेटी हुई है–अनादि युग से लेकर अनंत के अछोर तक वह कैसी ही थी और वैसी ही रहेगी। जो युग-युग में परिवर्तनशील चक्र नये-नये रूपों में चलता चला आ रहा है वह है उस महापरिधि के भीतर स्थित उन अनंत क्षणों और असंख्य कणों का खेल।
‘‘पर इस सारे चक्कर का अर्थ क्या हो सकता है ?’’ दादा के भीतर फिर प्रश्न उठा। और फिर बिजली की तरह उत्तर भी दिमाग में कौंध गया; ‘‘अर्थ कुछ नहीं, केवल खेल और केवल नयी-नयी रहस्यात्मक अनुभूतियाँ। खेल का क्या अर्थ हो सकता था ? केवल रस-मग्नता ! केवल नित नयी रागानुभूति ! सुख-दुःख, संघर्ष-विघर्ष, राग-रंग, स्वार्थ की छीना-झपटी, शक्ति-मद का नंगापन–सब इसी खेल के अंग हैं।’’
दादा ने फिर एक बार हिम-शिखरो की ओर दृष्टि गड़ायी। विराटा नारी की वेश-भूषा का रंग धीरे-धीरे उड़ता जा रहा था। पर क्षितिज के ऊपर सारा आकाश एक निराली गुलाबी ज्वाली में बदल गया था। बीच में, छिटपुट रूप से तैरनेवाले बादलों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ गुलेनारी आग से दहकने लगी थीं। दृश्य की इन्द्रियातीत मोहकता गहरी से और गहरी होती जा रही थी।
दादा को लगा कि उनकी आँखें और पाँव अपने बस के नहीं रहे। ये दोनों जैसे पंख बनकर उन्हें सामने वाले ऊर्ध्व-क्षितिज के मायालोक की ओर बरबस उड़ाये लिये जा रहे हों। सारे जग की चंचल व्याकुलता, सारे जीवन की कुटिल काँटेदार अशांति, समस्त युग का सब कुछ लील लेने वाला अंधकार एक अस्पष्ट, धुँधले, काले स्वप्न की तरह पल में काफूर हो गया। सब कुछ ऐसी मोहक रंगीनी में बदल गया, जिसे छाती से चिपकाने के लिये दादा जैसे युग-युग से, जन्म-जन्म से व्याकुल थे।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i