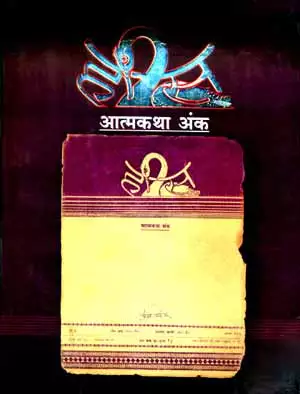|
जीवनी/आत्मकथा >> आत्मकथा अंक आत्मकथा अंकप्रेमचंद
|
435 पाठक हैं |
|||||||
हिन्दी के अनेकानेक मूर्धन्य विद्वानों के आत्मकथानकों से पूर्ण 1932 ई. में प्रकाशित हंस का यह विशेषांक ‘आत्मकथा अंक’...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘‘मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं है। इस समय तो
सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजयी हों। धन या
यश की लालसा मुझे नहीं रही। खाने भर को मिल जाता है। मोटर और बंगले की
मुझे हविस नहीं। हाँ, यह जरूर चाहता हूँ कि दो चार ऊँची कोटि की पुस्तकें
लिखूं, पर उनका उद्देश्य भी स्वराज्य विजय ही है। मुझे अपने दोनों लड़कों
के विषय में कोई बड़ी लालसा नहीं है। यही चाहता हूँ कि वह ईमानदार, सच्चे
और पक्के इरादे के हों। विलासी, धनी, खुशामदी सन्तान से मुझे घृणा है। मैं
शान्ति से बैठना भी नहीं चाहता। साहित्य और स्वदेश के लिये कुछ न कुछ करते
रहना चाहता हूँ। हाँ, रोटी-दाल और तोला भर घी और मामूली कपड़े मयस्सर होते
रहें ।’’
प्रेमचंद (संस्मरण–पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी )
पचहत्तर वर्ष उपरान्त ‘हंस’ का ‘आत्मकथा अंक’
उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के सम्पादन में हंस का
प्रकाशन मार्च, 1930 में वसंत पंचमी के दिन प्रारम्भ हुआ था। देशप्रेम,
साहित्यिक अभिरुचि एवं साहित्य सेवा की अदम्य लालसा ने उन्हें काशी से एक
साहित्यिक पत्रिका निकालने के लिए प्रेरित किया। प्रकाशन के पूर्व
उन्होंने अपने मित्र सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसादजी को पत्र लिखा–‘‘काशी से कोई साहित्यिक पत्रिका न निकलती थी। मैं धनी नहीं हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैंने हंस निकालने का निश्चय कर लिया है।’’ हंस का नामकरण जयशंकर प्रसादजी ने ही किया था।
हंस के प्रकाशन से एक नये युग का सूत्रपात हुआ। राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा हंस के प्रत्येक अंक से परिलक्षित होती है। गांधीजी के विचारों से प्रभावित प्रेमचंदजी ने अपनी बीस वर्षों की नौकरी छोड़कर देश की स्वतन्त्रता हेतु ‘कलम के सिपाही’ के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जैसा कि स्वयं उन्होंने इस ‘आत्मकथा अंक’ के पृष्ठ 166 पर अपने आलेख में लिखा है, ‘‘यह 1920 की बात है। असहयोग आन्दोलन ज़ोरों पर था। जलियावाला बाग़ का हत्याकांड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया। गाज़ी मियाँ के मैदान में ऊँचा प्लेटफार्म तैयार किया गया। दो लाख से कम का जमाव न था। क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था। महात्माजी के दर्शनों का यह प्रताप था, कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा। उसके दो-ही-चार दिन बाद मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया।’’
हंस गांधीयुग की प्रमुख साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। अनेकानेक प्रतिभाशाली लेखकों, कवियों, नाटककारों, कहानीकारों को जन्म देने, तराशने, निखारने में इसने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं इस पत्रिका ने प्रगतिवादी आन्दोलन को जन्म दिया। इसके द्वारा प्रेमचंदजी ने हिन्दी भाषा ही नहीं स्वतन्त्रता की भी लड़ाई लड़ी।
हंस अपनी उग्रतर नीतियों के कारण ब्रिटिश सरकार की आँखों की किरकिरी बना हुआ था। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जब हंस पत्रिका को जब्त करने का आदेश दिया तो सम्पादक मुंशी प्रेमचंद झुके नहीं। इण्डियन प्रेस आर्डिनेन्स 1930 के अन्तर्गत हंस को कई बार जमानत देने का सरकार ने आदेश दिया पर प्रेमचंद ने बीच-बीच में कई बार उसका प्रकाशन स्थगित करना ही उचित समझा।
1932 ई. में प्रकाशित हंस का यह विशेषांक ‘आत्मकथा अंक’ दशकों से अप्राप्य था, पाठक ऐसे ही स्तरीय, विलुप्त हो चले, पठनीय साहित्य की तलाश में हैं। वर्तमान समय में इस ग्रन्थ की उपादेयता कहीं अधिक बढ़ जाती है। आज पाठकों, अध्येताओं की बहुप्रतीक्षित उत्कट अभिलाषा पूर्ण हो रही है।
आज हम यत्र-तत्र आत्मकथा और संस्मरणों का जो दौर देखते हैं उसका जनक था हंस का यह ‘आत्मकथा अंक’। जयशंकर प्रसाद, रायसाहब लाला सीतारामजी, पं. रामचन्द्र शुक्ल, पं. रामनायणजी मिश्र, पं. विनोदशंकर व्यास, श्री शिवपूजन सहायजी, श्री रायकृष्णदासजी, श्री धीरेन्द्र वर्मा, गोपाल राम गहमरी (सम्पादक : जासूस), बद्रीनाथ भट्ट, सद्गुरुशरणजी अवस्थी, डॉ० धनीरामजी ‘प्रेम’ (सम्पादक : चाँद), ठाकुर श्रीनाथ सिंहजी (सम्पादक : बालसखा), श्री गंगाप्रसादजी उपाध्याय (सम्पादत : वेदोदय), प्रेमचंद बी० ए० आदि अनेकानेक हिन्दी के मूर्धन्य विद्वानों के आत्मकथानक (जीवन-वृत्त) आज के पाठकों के लिए संजीवनी का कार्य करेंगे।
हंस के प्रकाशन से एक नये युग का सूत्रपात हुआ। राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनकी निष्ठा हंस के प्रत्येक अंक से परिलक्षित होती है। गांधीजी के विचारों से प्रभावित प्रेमचंदजी ने अपनी बीस वर्षों की नौकरी छोड़कर देश की स्वतन्त्रता हेतु ‘कलम के सिपाही’ के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जैसा कि स्वयं उन्होंने इस ‘आत्मकथा अंक’ के पृष्ठ 166 पर अपने आलेख में लिखा है, ‘‘यह 1920 की बात है। असहयोग आन्दोलन ज़ोरों पर था। जलियावाला बाग़ का हत्याकांड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया। गाज़ी मियाँ के मैदान में ऊँचा प्लेटफार्म तैयार किया गया। दो लाख से कम का जमाव न था। क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था। महात्माजी के दर्शनों का यह प्रताप था, कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा। उसके दो-ही-चार दिन बाद मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया।’’
हंस गांधीयुग की प्रमुख साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। अनेकानेक प्रतिभाशाली लेखकों, कवियों, नाटककारों, कहानीकारों को जन्म देने, तराशने, निखारने में इसने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं इस पत्रिका ने प्रगतिवादी आन्दोलन को जन्म दिया। इसके द्वारा प्रेमचंदजी ने हिन्दी भाषा ही नहीं स्वतन्त्रता की भी लड़ाई लड़ी।
हंस अपनी उग्रतर नीतियों के कारण ब्रिटिश सरकार की आँखों की किरकिरी बना हुआ था। परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जब हंस पत्रिका को जब्त करने का आदेश दिया तो सम्पादक मुंशी प्रेमचंद झुके नहीं। इण्डियन प्रेस आर्डिनेन्स 1930 के अन्तर्गत हंस को कई बार जमानत देने का सरकार ने आदेश दिया पर प्रेमचंद ने बीच-बीच में कई बार उसका प्रकाशन स्थगित करना ही उचित समझा।
1932 ई. में प्रकाशित हंस का यह विशेषांक ‘आत्मकथा अंक’ दशकों से अप्राप्य था, पाठक ऐसे ही स्तरीय, विलुप्त हो चले, पठनीय साहित्य की तलाश में हैं। वर्तमान समय में इस ग्रन्थ की उपादेयता कहीं अधिक बढ़ जाती है। आज पाठकों, अध्येताओं की बहुप्रतीक्षित उत्कट अभिलाषा पूर्ण हो रही है।
आज हम यत्र-तत्र आत्मकथा और संस्मरणों का जो दौर देखते हैं उसका जनक था हंस का यह ‘आत्मकथा अंक’। जयशंकर प्रसाद, रायसाहब लाला सीतारामजी, पं. रामचन्द्र शुक्ल, पं. रामनायणजी मिश्र, पं. विनोदशंकर व्यास, श्री शिवपूजन सहायजी, श्री रायकृष्णदासजी, श्री धीरेन्द्र वर्मा, गोपाल राम गहमरी (सम्पादक : जासूस), बद्रीनाथ भट्ट, सद्गुरुशरणजी अवस्थी, डॉ० धनीरामजी ‘प्रेम’ (सम्पादक : चाँद), ठाकुर श्रीनाथ सिंहजी (सम्पादक : बालसखा), श्री गंगाप्रसादजी उपाध्याय (सम्पादत : वेदोदय), प्रेमचंद बी० ए० आदि अनेकानेक हिन्दी के मूर्धन्य विद्वानों के आत्मकथानक (जीवन-वृत्त) आज के पाठकों के लिए संजीवनी का कार्य करेंगे।
पुरुषोत्तमदास मोदी
अपनी कहानी
लेखक-श्रीयुत रायसाहब लाला सीतारामजी,
बी.ए.
यों तो किसी सभा या परिषदु से बुलावा आया, और
वहाँ जाने में विशेष कष्ट न उठाना पड़ा, तो मैं चला जाता हूँ ; परन्तु जहाँ विशेष
रूप से गुल-गपाड़ा हो, वहाँ कभी नहीं गया। कांग्रेस का एक ही जलसा सन्
1888 ई० में देखा, सो भी एक मित्र के आग्रह से। कायस्थ-कान्फ्रेन्स के दो
जलसों में उपस्थित हुआ, सो दोनों बार यहीं प्रयागराज में। जिस साल कलकत्ते
के पंडित गोविन्द नारायण चौधरी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हुए थे,
उस समय, एक महाशय के कहने से–जिन्हें अब मेरा नाम सुनने से
शिरःशूल होता है ; परन्तु जिनको अपनी उद्दंड़ता का दण्ड मिल ही जाता
है–सभासदों को पाटीं दी गई। उसमें मेरा कुछ खर्च हुआ। इसपर एक
कर्मचारी ने मेरे एक मित्र से कहा–‘क्या यह हिन्दुस्तान को एक
करना चाहते है।’’ यह बीस-बाईस वर्ष पहले की बात है। उसके पीछे
जब पेंशन मिल गई, तो समझा कि अब सुचित्त हुए। परन्तु सुचितई कहाँ। आज एक
हिसाब से 75 वाँ वर्ष लगा। अब भी कुछ पत्रिकाओं के सम्पादक पीछे पड़े हुए
हैं। ‘हंस ’ के प्रधान और सहायक सम्पादकों ने भी आग्रह किया
कि अपनी कहानी लिख दो। इसलिये कुछ लिखने के लिये मजबूर हो गया हूँ।
सुनिए–
मार्च 1911 में मैंने पेन्शन ले ली। डिप्टी कलक्टर होने से पहले मैं 16 वर्ष तक शिक्षा-विभाग में रहा। सीतापूर-हाईस्कूल, मेरठ-हाईस्कूल, कानपूर-हाईस्कूल, फैजाबाद-इण्टरमीडियट कॉलेज का हेडमास्टर और इलाहाबाद-डिवीज़न, लखनऊ-डिवीज़न और बुन्देलखण्ड-एण्यू नेशनल डिवीज़न का असिस्टेंट इस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहा। क्वीन्स कॉलेज बनारस में साढ़े चार वर्ष सेकेण्ड मास्टरी की। अफसर मेरे काम से सदा प्रसन्न रहे। वरन यों कहिये कि इसी प्रसन्नता के कारण डिप्टी कलेक्टरी मिली; परन्तु सार्वजनिक शिक्षा में मेरा प्रेम कम न हुआ और पढ़ना-लिखना भी न छूटा। पेन्शन लेते ही इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के सुयोग्य डाइरेक्टर श्रीमान डीलाफ़ास की (जो अब सर क्ला़ड डीलफ़ास है) चिट्ठी आई कि तुम टेक्सबुक कमेटी के मेम्बर बनाये गये। उसी साल गवर्मेण्ट ने आज्ञा दी कि हिन्दी-उर्दू की कॉमन लैग्वेज रीडरें बने; जिनकी भाषा एक हो और लिपि भिन्न। इनके पाठ अनेक विद्वानों ने बनाये और सब की जाँच करने के लिए सरकार की ओर से एक कमेटी बनी। इसमें नौ सदस्य थे। चार हिन्दू, चार मुसलिम। और पं० रमाशंकरजी मिश्र भूतपूर्व कलेक्टर–सभापति। हिन्दू सदस्यों में एक थे पण्डित सुन्दरलाल, जो पीछे सर सुन्दर-लाल हुए। शिक्षा-विभाग के दो हिन्दू हेडमास्टर, और एक इस आत्म-कहानी का लेखक। मुसलिमों में एक हादी साहब डिप्टी कमिश्नर, शिक्षा-विभाग के दो अधिकारी और एक अलीगढ़ के शेख अबदुल्लाह। इस कमेटी की बैठक साल भर रही। हिन्दी के पक्षपाती जानते थे कि कामन लैग्वेज का ढकोसला हिन्दी को नष्ट करने के लिये बनाया गया है। परदेसी हाकिम–जो हम लोगों के भेदभाव से अपरिचित है–नहीं समझती कि एक देश के रहनेवाले भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं। उर्दू के पक्षपातियों ने उर्दू में फारसी और अरबी की भरमार करदी। मुसलिम राज्य के दफ़्तर फ़ारसी भाषा और फारसी अक्षरों में था। ईरानी सम्यता का पूरा प्रभाव उत्तर में खीवा बुखारा तक और पूर्व में अफ़गानिस्तान तक पड़ा हुआ था। अफ़गान बादशाहों के दरबार में फ़रदीसी आदि फ़ारसी के कवि थे। ईस्ट इण्डिया कंपनी के कर्मचारी भी मुसलिम बादशाहों और नवाबों से फ़ारसी में पत्र-व्यवहार करते थे। जब अँगरेजी सरकार ने देश भाषा में दफ्तरों की कारवाई करने की आज्ञा दी, तो कर्मचारी तो वही थे, उन्होंने नाम मात्र के लिये देश-माषा को स्थान दिया। इससे दफ़्तरों में उर्दू की उत्पत्ति हुई। सर चार्ल्स लायक का यह अनुमान है कि उर्दू के जन्मदाता कायस्थ ही थे। इसका एक उदाहरण लीजिये। तहसील के अहलकार से ‘कैफ़ियत’ माँगी गई। जब दफ़तर में आई, तो उस पर लिखा था–
मार्च 1911 में मैंने पेन्शन ले ली। डिप्टी कलक्टर होने से पहले मैं 16 वर्ष तक शिक्षा-विभाग में रहा। सीतापूर-हाईस्कूल, मेरठ-हाईस्कूल, कानपूर-हाईस्कूल, फैजाबाद-इण्टरमीडियट कॉलेज का हेडमास्टर और इलाहाबाद-डिवीज़न, लखनऊ-डिवीज़न और बुन्देलखण्ड-एण्यू नेशनल डिवीज़न का असिस्टेंट इस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहा। क्वीन्स कॉलेज बनारस में साढ़े चार वर्ष सेकेण्ड मास्टरी की। अफसर मेरे काम से सदा प्रसन्न रहे। वरन यों कहिये कि इसी प्रसन्नता के कारण डिप्टी कलेक्टरी मिली; परन्तु सार्वजनिक शिक्षा में मेरा प्रेम कम न हुआ और पढ़ना-लिखना भी न छूटा। पेन्शन लेते ही इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के सुयोग्य डाइरेक्टर श्रीमान डीलाफ़ास की (जो अब सर क्ला़ड डीलफ़ास है) चिट्ठी आई कि तुम टेक्सबुक कमेटी के मेम्बर बनाये गये। उसी साल गवर्मेण्ट ने आज्ञा दी कि हिन्दी-उर्दू की कॉमन लैग्वेज रीडरें बने; जिनकी भाषा एक हो और लिपि भिन्न। इनके पाठ अनेक विद्वानों ने बनाये और सब की जाँच करने के लिए सरकार की ओर से एक कमेटी बनी। इसमें नौ सदस्य थे। चार हिन्दू, चार मुसलिम। और पं० रमाशंकरजी मिश्र भूतपूर्व कलेक्टर–सभापति। हिन्दू सदस्यों में एक थे पण्डित सुन्दरलाल, जो पीछे सर सुन्दर-लाल हुए। शिक्षा-विभाग के दो हिन्दू हेडमास्टर, और एक इस आत्म-कहानी का लेखक। मुसलिमों में एक हादी साहब डिप्टी कमिश्नर, शिक्षा-विभाग के दो अधिकारी और एक अलीगढ़ के शेख अबदुल्लाह। इस कमेटी की बैठक साल भर रही। हिन्दी के पक्षपाती जानते थे कि कामन लैग्वेज का ढकोसला हिन्दी को नष्ट करने के लिये बनाया गया है। परदेसी हाकिम–जो हम लोगों के भेदभाव से अपरिचित है–नहीं समझती कि एक देश के रहनेवाले भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं। उर्दू के पक्षपातियों ने उर्दू में फारसी और अरबी की भरमार करदी। मुसलिम राज्य के दफ़्तर फ़ारसी भाषा और फारसी अक्षरों में था। ईरानी सम्यता का पूरा प्रभाव उत्तर में खीवा बुखारा तक और पूर्व में अफ़गानिस्तान तक पड़ा हुआ था। अफ़गान बादशाहों के दरबार में फ़रदीसी आदि फ़ारसी के कवि थे। ईस्ट इण्डिया कंपनी के कर्मचारी भी मुसलिम बादशाहों और नवाबों से फ़ारसी में पत्र-व्यवहार करते थे। जब अँगरेजी सरकार ने देश भाषा में दफ्तरों की कारवाई करने की आज्ञा दी, तो कर्मचारी तो वही थे, उन्होंने नाम मात्र के लिये देश-माषा को स्थान दिया। इससे दफ़्तरों में उर्दू की उत्पत्ति हुई। सर चार्ल्स लायक का यह अनुमान है कि उर्दू के जन्मदाता कायस्थ ही थे। इसका एक उदाहरण लीजिये। तहसील के अहलकार से ‘कैफ़ियत’ माँगी गई। जब दफ़तर में आई, तो उस पर लिखा था–
‘कैफ़ियत बाला वास्ते सुदूर हुक्म हरसाल हुजूर है।’
इसमें एक शब्द ‘है’ देश की बोली का है और सब
अरबी हैं, या फ़ारसी। दूसरी ओर से लात मारने के बदले पाद-प्रहार करना
इत्यादि लिखे जाने लगे। दोनों में मेल कौन करा सकता था ? बढ़ते-बढ़ते अब
यह भाषा और इसका उर्दू नाम इस्लाम के अंश हो गये हैं। मैं अपनी कहानी
लिखने बैठा था और यह लिख मारा; परन्तु इसका कारण यह है कि इस झगड़े में
मुझे भी सरकार ने डाल दिया। मेरे मित्र और कर्मचारी, जो मेरे स्वभाव से
परिचित थे, मुझसे बार-बार कहते थे कि हम लोग आप ही ता मुँह देख रहे हैं।
मैंने भी उत्तर दिया, कि जो कुछ मुझसे हो सकेगा, उसमें कसर न की जायगी।
कमेटी में एक-एक शब्द पर झगड़ा हुआ। एक बार एक साहब ने फरमाया, यह
गवर्नमेण्ट की ‘पालिसी’ है। मैंने उत्तर दिया कि जिस
गवर्नमेंट ने आपको मेम्बर बनाया, उसी ने मुझको बनाया, आपको पालिसी बता दी,
मुझे न बताई। सर सुन्दरलालजी शान्तिप्रिय थे, कहा करते थे–लड़िये
मत। राधास्वामी मत के थे, उन्होंने खुदा और ईश्वर दोनों का बहिष्कार करके
कहा कि ‘मालिक’ लिखा जाय। मैंने थोड़ी फ़ारसी भी पढ़ी है,
परन्तु उत्तर दिया कि मालिक अरबी भाषा का शब्द है, और इसके तीन अर्थ
हैं–
1–स्वामी। 2–नरक के द्वार का रखवाला। 3–वह मनुष्य जिसके हाथ यूसुफ़ मिस्त्र में बिके थे। अन्त में श्रीमान् डाइरेक्टर साहब ने यह निर्णय किया कि हिन्दी में ईश्वर रहे और उर्दू में खुदा।
‘खुदा-खुदा’ करके कमेटी का कारवाई समाप्त हुई। उर्दूके पक्षपातियों से कहा कि आपको उचित था कि आप इस बात पर अड़ जाते, कि हमें शुद्ध उर्दू चाहिये और हम भी हठ करते कि हमें शुद्ध हिन्दी अपेक्षित है। अब परिणाम यह हुआ कि रीडरों में न हिन्दी शुद्ध है, न उर्दू।
इन्हीं रीडरों की समीक्षा के लिये श्रीमान् किचलू साहब के सभापतित्व में एक और कमेटी बनी, जिसमें सभापति को छोड़ कर दो ही सदस्य थे। एक हिन्दू और एक मुसलिम, मुसलिम साहब प्रयाग के सुप्रसिद्घ बैरिस्टर थे और देवनागरी अक्षरों के कट्टरविरोधी। उनका संकल्प यह था कि स्कूलों में देवनागरी अक्षर पढ़ाये ही न जाय। कमेटी तो बन गई ; परन्तु सभापतिजी मेरे घर पर दौड़े आते थे और कहते थे कि आप लोग लड़ेंगे, तो बड़ी बदनामी होगी। उनसे कहा कि आप निश्चिन्त रहें। काम बड़ी सावधानी से किया जायगा। डाइरेक्टर साहब को भी आश्चर्य हुआ और बोले how could they both agree ? (दोनों कैसे एक मत हो गये ?) मैंने कमेटी में इतना ही कहा कि कोई बात ऐसी न होनी चाहिये, जिससे हिन्दू-मुसलिम बच्चों की शिक्षा में बाधा पढ़े। कमेटी की कार्रवाई से बैरिस्टर साहब इतने सन्तुष्ट हुए कि युनीवर्सिटी-कनवोकेशन के दिन फेलोज़ रूम में सारे मुसलिम फेलोज़ (सदस्यगण) के सामने मुझे ले जाकर कहने लगे कि शिक्षा का प्रबंध इनके हाथ में दिया जाय, तो सारे झगड़े निपट जाय। यहाँ इतना लिखना आवश्यक है कि मैंने साहित्य-सम्मेलन के एक प्रवर्त्तक से कहा था कि हम दोनों का उद्देश्य हिन्दी की उन्नति करना है। हम मिलकर काम करें, तो बड़ी सफलता हो ; परन्तु बात ही खाली गई।
उसके पीछे शिक्षा-विभाग में हिन्दी का काम धूम-धाम से होने लगा। इतिहास के कई ग्रन्थ लिखे गये। हिन्दी में जितनी पुस्तकें आई, सबका मेरी ही सम्मति से निर्णय हुआ। एक महाशय ने–जो अब तक अनायास द्वेष मानते है–कुछ दोष भी निकाले; परन्तु उन्होंने मुँह की खाई और उन्हीं का अनुवाद अशुद्ध निकला।
दूसरा काम लिखने-योग्य यह है कि आज से बारह-तेरह वर्ष पूर्व कलकत्ता-विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध वाइस चान्सलर सर आशुतोष मुकर्जी प्रयागराज आये थे। उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। उनसे मैं अनेक बार मिला और प्रसंगवश एम० ए० की परीक्षा में हिन्दी को भी स्थान देने की बात छिड़ी। सर आशुतोष ने कहा कि बंगला में प्रचुर साहित्य है और रायबहादुर दिनेशचन्द्र सेन ने एक संग्रह भी बनाया है, हिन्दी में भी कुछ है ? मैंने उत्तर दिया कि हिन्दी आधे से अधिक भारतवर्ष की बोली है और इसमें हजार वर्ष का पुराना साहित्य है। इसके पीछे सर आशुतोष कलकत्ते चले गये। कलकत्ता-युनिवर्सिटी-कमीशन के सदस्य होकर भारतवर्ष का दौरा करते हुए वे यहाँ फिर आये। मैं फिर उनसे मिला। उस समय तो वे कुछ न बोले; परन्तु कमीशन का कार्य समाप्त होने पर गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा–यह पत्र सर आशुतोष की आज्ञा से मेरे रचे कलकत्ता-युनिवर्सिटी हिन्दी-सिलेकशन्स की पहली जिल्द Bardie poetry में छपा है और इसकी नकल मैंने इलाहाबाद-युनिवर्सिटी, हिन्दू-युनिवर्सिटी आदि में भेजकर हिन्दी में एक परीक्षा का प्रस्ताव किया।–जिसमें भारत की भाषाओं में एम० ए० की परीक्षा होने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी और हिन्दी का एक संग्रह बनाने की आज्ञा दी। मैं भी तुरन्त उनकी आज्ञा के प्रतिपालन में लग गया और कई वर्ष के कठिन परिश्रम से सात जिल्दों में संग्रह तैयार हुआ, जिसका विवरण यह है–
भाग 1 Bardie poetry अर्थात् बन्दीजन या चारण काव्य। भाग 2. Krishna cult कृष्ण की उपासना, अष्ट छाप। भाग 3, तुलसीदास। भाग 4, सन्त कबीर इत्यादि। भाग 5, साहित्य शास्त्र, रस, नायिका-भेद। भाग 6, दो जिल्दों में अन्य कवि।
यह ग्रन्थ कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किये और मेरे ही कहने से इण्डियन-प्रेस के स्वामी ने भाग 5,छापकर कलकत्ता-विश्वविद्यालय को भेंट किया और लाला रामनाराणलालजी ने भाग 6 की एक जिल्द की छपाई नहीं ली।
मैंने सुना है, कि एक महाशय ने कहा था, कि ‘बाबू सीताराम ने संग्रह बनाया; परन्तु अच्छा नहीं बना।’ मैंने पगडंडी बनाई है, अब रेल की सड़क बनाना औरों का काम है। मैं कायस्थ कुल-भास्कर मु० कालीप्रसाद का पुत्र-तुल्य शिप्य हूँ। उनकी शिक्षाओं में से एक यह भी थी, कि भारतवर्ष की बिगड़ी दशा में जितनी देश-सेवा हो सके, उसे करना और किसी से सहायता की आशा न रखना। इसी कर्त्तव्य के पालन में उमर बीत गई और व्यर्थ या ईर्ष्या-वश द्वेष करनेवालों की कभी परवाह न की।
1–स्वामी। 2–नरक के द्वार का रखवाला। 3–वह मनुष्य जिसके हाथ यूसुफ़ मिस्त्र में बिके थे। अन्त में श्रीमान् डाइरेक्टर साहब ने यह निर्णय किया कि हिन्दी में ईश्वर रहे और उर्दू में खुदा।
‘खुदा-खुदा’ करके कमेटी का कारवाई समाप्त हुई। उर्दूके पक्षपातियों से कहा कि आपको उचित था कि आप इस बात पर अड़ जाते, कि हमें शुद्ध उर्दू चाहिये और हम भी हठ करते कि हमें शुद्ध हिन्दी अपेक्षित है। अब परिणाम यह हुआ कि रीडरों में न हिन्दी शुद्ध है, न उर्दू।
इन्हीं रीडरों की समीक्षा के लिये श्रीमान् किचलू साहब के सभापतित्व में एक और कमेटी बनी, जिसमें सभापति को छोड़ कर दो ही सदस्य थे। एक हिन्दू और एक मुसलिम, मुसलिम साहब प्रयाग के सुप्रसिद्घ बैरिस्टर थे और देवनागरी अक्षरों के कट्टरविरोधी। उनका संकल्प यह था कि स्कूलों में देवनागरी अक्षर पढ़ाये ही न जाय। कमेटी तो बन गई ; परन्तु सभापतिजी मेरे घर पर दौड़े आते थे और कहते थे कि आप लोग लड़ेंगे, तो बड़ी बदनामी होगी। उनसे कहा कि आप निश्चिन्त रहें। काम बड़ी सावधानी से किया जायगा। डाइरेक्टर साहब को भी आश्चर्य हुआ और बोले how could they both agree ? (दोनों कैसे एक मत हो गये ?) मैंने कमेटी में इतना ही कहा कि कोई बात ऐसी न होनी चाहिये, जिससे हिन्दू-मुसलिम बच्चों की शिक्षा में बाधा पढ़े। कमेटी की कार्रवाई से बैरिस्टर साहब इतने सन्तुष्ट हुए कि युनीवर्सिटी-कनवोकेशन के दिन फेलोज़ रूम में सारे मुसलिम फेलोज़ (सदस्यगण) के सामने मुझे ले जाकर कहने लगे कि शिक्षा का प्रबंध इनके हाथ में दिया जाय, तो सारे झगड़े निपट जाय। यहाँ इतना लिखना आवश्यक है कि मैंने साहित्य-सम्मेलन के एक प्रवर्त्तक से कहा था कि हम दोनों का उद्देश्य हिन्दी की उन्नति करना है। हम मिलकर काम करें, तो बड़ी सफलता हो ; परन्तु बात ही खाली गई।
उसके पीछे शिक्षा-विभाग में हिन्दी का काम धूम-धाम से होने लगा। इतिहास के कई ग्रन्थ लिखे गये। हिन्दी में जितनी पुस्तकें आई, सबका मेरी ही सम्मति से निर्णय हुआ। एक महाशय ने–जो अब तक अनायास द्वेष मानते है–कुछ दोष भी निकाले; परन्तु उन्होंने मुँह की खाई और उन्हीं का अनुवाद अशुद्ध निकला।
दूसरा काम लिखने-योग्य यह है कि आज से बारह-तेरह वर्ष पूर्व कलकत्ता-विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध वाइस चान्सलर सर आशुतोष मुकर्जी प्रयागराज आये थे। उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। उनसे मैं अनेक बार मिला और प्रसंगवश एम० ए० की परीक्षा में हिन्दी को भी स्थान देने की बात छिड़ी। सर आशुतोष ने कहा कि बंगला में प्रचुर साहित्य है और रायबहादुर दिनेशचन्द्र सेन ने एक संग्रह भी बनाया है, हिन्दी में भी कुछ है ? मैंने उत्तर दिया कि हिन्दी आधे से अधिक भारतवर्ष की बोली है और इसमें हजार वर्ष का पुराना साहित्य है। इसके पीछे सर आशुतोष कलकत्ते चले गये। कलकत्ता-युनिवर्सिटी-कमीशन के सदस्य होकर भारतवर्ष का दौरा करते हुए वे यहाँ फिर आये। मैं फिर उनसे मिला। उस समय तो वे कुछ न बोले; परन्तु कमीशन का कार्य समाप्त होने पर गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा–यह पत्र सर आशुतोष की आज्ञा से मेरे रचे कलकत्ता-युनिवर्सिटी हिन्दी-सिलेकशन्स की पहली जिल्द Bardie poetry में छपा है और इसकी नकल मैंने इलाहाबाद-युनिवर्सिटी, हिन्दू-युनिवर्सिटी आदि में भेजकर हिन्दी में एक परीक्षा का प्रस्ताव किया।–जिसमें भारत की भाषाओं में एम० ए० की परीक्षा होने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी और हिन्दी का एक संग्रह बनाने की आज्ञा दी। मैं भी तुरन्त उनकी आज्ञा के प्रतिपालन में लग गया और कई वर्ष के कठिन परिश्रम से सात जिल्दों में संग्रह तैयार हुआ, जिसका विवरण यह है–
भाग 1 Bardie poetry अर्थात् बन्दीजन या चारण काव्य। भाग 2. Krishna cult कृष्ण की उपासना, अष्ट छाप। भाग 3, तुलसीदास। भाग 4, सन्त कबीर इत्यादि। भाग 5, साहित्य शास्त्र, रस, नायिका-भेद। भाग 6, दो जिल्दों में अन्य कवि।
यह ग्रन्थ कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किये और मेरे ही कहने से इण्डियन-प्रेस के स्वामी ने भाग 5,छापकर कलकत्ता-विश्वविद्यालय को भेंट किया और लाला रामनाराणलालजी ने भाग 6 की एक जिल्द की छपाई नहीं ली।
मैंने सुना है, कि एक महाशय ने कहा था, कि ‘बाबू सीताराम ने संग्रह बनाया; परन्तु अच्छा नहीं बना।’ मैंने पगडंडी बनाई है, अब रेल की सड़क बनाना औरों का काम है। मैं कायस्थ कुल-भास्कर मु० कालीप्रसाद का पुत्र-तुल्य शिप्य हूँ। उनकी शिक्षाओं में से एक यह भी थी, कि भारतवर्ष की बिगड़ी दशा में जितनी देश-सेवा हो सके, उसे करना और किसी से सहायता की आशा न रखना। इसी कर्त्तव्य के पालन में उमर बीत गई और व्यर्थ या ईर्ष्या-वश द्वेष करनेवालों की कभी परवाह न की।
धर्म करैं गारी सहैं, लावैं नहिं मन रोष।
अहै हमारे धर्म में, बुरो मानिषी दोष।
अहै हमारे धर्म में, बुरो मानिषी दोष।
----------------------------------------------------------------
(4 थे पृष्ठ का शेषांश)
छत पर बैठे चौधरी साहब से बात-चीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैम्प जल रहा था। लैम्प की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूँ; पर पण्डित लक्ष्मीनारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे हैं ‘अरे, जब फूट जाई तबै चलत जाबह।’ अन्त में चिमनी ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई; पर चौधरी साहब का हाथ लैम्प की तरफ़ न बढ़ा।
उपाध्यायजी नागरी को भाषा का नाम मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से, जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई, वही नागरी कहलाई। इसी प्रकार वे मिर्जापुर न लिखकर मीरजापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर मीर–समुद्र ;+ जा =पुत्री + पुर।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i