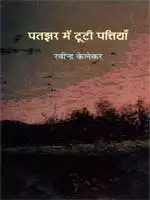|
विविध >> पतझर में टूटी पत्तियाँ पतझर में टूटी पत्तियाँरवीन्द्र केलेकर
|
145 पाठक हैं |
|||||||
गाँधीवादी विचारक, कोकणी एवं मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रवीन्द्र केलेकर के प्रेरक प्रसंगों का अद्भुत संकलन...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गाँधीवादी विचारक, कोकणी एवं मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रवीन्द्र
केलेकर के प्रेरक प्रसंगों का अद्भुत संकलन है ‘पतझर में टूटी
पत्तियाँ’। केलेकर का सम्पूर्ण साहित्य संघर्षशील चेतना से
ओतप्रोत है। ‘पतझर में टूटी पत्तियाँ’ में लेखक ने
निजी जीवन की कथा-व्यथा न लिखकर जन-जीवन के विविध, पक्षों,मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है।
अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिन्तन की मौलिकता के साथ ही, इनमें विविध
प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से मानवीय सत्य तक पहुँचने की सहज चेष्टा है।
इस दृष्टि से देखा जाय तो यह कृति अपने पाठकों के लिए मात्र पढ़ने-सुनने
की नहीं, एक जागरूक एवं सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। ये आलेख
कोंकणी में प्रकाशित केलेकर की कृति ‘ओथांबे’ से चुनकर अनूदित किये गये हैं। अनुवाद किया है माधवी सरदेसाई ने,जो गोवा विश्वविद्यालय के कोंकणी विभाग में भाषा-विज्ञान की वरिष्ठ अध्यापिका हैं। यह महत्वपूर्ण कृति हिन्दी पाठकों को समर्पित करते हुए भारतीय ज्ञानपीठ को प्रसन्नता है।
प्राक्कथन
जिस बात को कहने के लिए दूसरों को एक पूरी
पुस्तक लिखनी
पड़ती है-फिर भी वे कभी-कभी वह नहीं कह पाते जो वे कहना चाहते हैं, उसी
बात को दस पंक्तियों में लिखने की महत्त्वाकांक्षा सामने रखकर जर्मन
दार्शनिक फ्रेडेरिक नित्शे ने ‘Twilight of Idols और
‘Anti-Christ’ जैसी पुस्तकें लिखीं। मैंने ये
पुस्तकें पढ़ीं
तब लगा-जिसे कहने के लिए मैं पूरा एक निबन्ध लिखकर पाठकों के सामने रखता
आया हूँ, वह भले ही दस पंक्तियों में न हो, पर डायरी के एक दो पृष्ठों में
तो लिखने की कोशिश करके देखनी ही चाहिए। प्रसार माध्यमों की वृद्धि की वजह
से आजकल शब्दों का काफी अवमूल्यन हुआ है। शब्दों का कम-से-कम उपयोग करके
ज्यादा से ज्यादा कहने की कोशिश में शब्दों का मूल्य बढ़ता है या नहीं यह
देखना चाहिए। और मैं इस तरह के चिन्तन लिखता रहा।
इन चिन्तनों में से कुछ चुनकर कोंकणी में ‘ओथांबे’ नाम की एक पुस्तक पाँच साल पहले लिखी थी। उसी पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद मेरी बेटी चि. माधवी रसदेसाई ने किया है। मैंने यह अनुवाद देखा है और मुझे उससे सन्तोष है।
सावन में जब कभी बारिश जाने के बाद पेड़ों के पत्तों से टपक-टपक कर जो बूँदें गिरती हैं उन्हें कोंकणी में ‘ओथांबे’ कहते हैं। ‘ओथांबे’ के लिए हिन्दी में क्या शब्द है यह न तो चि. माधवी को सूझा, न मुझे। इसलिए पुस्तक का नाम ‘पतझर में टूटी पत्तियाँ’ रख दिया, अच्छा लगा।
जो कुछ कहना था, पुस्तक में कह दिया है। हिन्दी-जगत् इसका किस तरह स्वागत करता है यह देखने की अब उत्सुकता है।
इन चिन्तनों में से कुछ चुनकर कोंकणी में ‘ओथांबे’ नाम की एक पुस्तक पाँच साल पहले लिखी थी। उसी पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद मेरी बेटी चि. माधवी रसदेसाई ने किया है। मैंने यह अनुवाद देखा है और मुझे उससे सन्तोष है।
सावन में जब कभी बारिश जाने के बाद पेड़ों के पत्तों से टपक-टपक कर जो बूँदें गिरती हैं उन्हें कोंकणी में ‘ओथांबे’ कहते हैं। ‘ओथांबे’ के लिए हिन्दी में क्या शब्द है यह न तो चि. माधवी को सूझा, न मुझे। इसलिए पुस्तक का नाम ‘पतझर में टूटी पत्तियाँ’ रख दिया, अच्छा लगा।
जो कुछ कहना था, पुस्तक में कह दिया है। हिन्दी-जगत् इसका किस तरह स्वागत करता है यह देखने की अब उत्सुकता है।
रवीन्द्र केलकर
1
शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग।
गिन्नी के सोने
में थोड़ा-सा ताँबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और
शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अकसर इसी सोने के गहने बनवा लेती
हैं।
फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना।
शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चन्द लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा-सा ताँबा मिला देतें हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब वह लोग उन्हें ‘प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट’ कहकर उनका बखान करते हैं।
पर बात न भूलें की बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब ‘प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों’ के जीवन से आदर्श धीरे-धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है।
सोना पीछे रहकर ताँबा ही आगे आता है।
चन्द लोग कहते हैं, गाँधी जी ‘प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट’ थे। व्यावहारिकता को पहचानते थे। उसकी कीमत जानते थे। इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। वरना हवा में ही उड़ते रहते। देश उनके पीछे न जाता।
हाँ, पर गाँधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में ताँबा नहीं बल्कि ताँबे सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे।
इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था।
व्यावहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। लाभ-हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं ? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्त्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ ही तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यावहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है।
फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना।
शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चन्द लोग उनमें व्यावहारिकता का थोड़ा-सा ताँबा मिला देतें हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब वह लोग उन्हें ‘प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट’ कहकर उनका बखान करते हैं।
पर बात न भूलें की बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब ‘प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों’ के जीवन से आदर्श धीरे-धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है।
सोना पीछे रहकर ताँबा ही आगे आता है।
चन्द लोग कहते हैं, गाँधी जी ‘प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट’ थे। व्यावहारिकता को पहचानते थे। उसकी कीमत जानते थे। इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। वरना हवा में ही उड़ते रहते। देश उनके पीछे न जाता।
हाँ, पर गाँधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में ताँबा नहीं बल्कि ताँबे सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे।
इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था।
व्यावहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। लाभ-हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं ? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्त्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ ही तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यावहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है।
2
सुकरात लोगों से पूछता,
‘‘तुम्हारा जूता टूट जाए तो
उसे जोड़ने के लिए तुम किसके पास जाओगे ?’’
‘‘मोची के पास।’’ लोग जवाब देते।
‘‘मोची के पास ही क्यों ? बढ़ई के पास क्यों नहीं ?’’
‘‘क्योंकि जूते बनाने-जोड़ने का काम मोची का है, बढ़ई का नहीं।’’ लोग जवाब देते।
‘‘अच्छा, मान लो, तुम्हारी माँ बीमार है। तो दवाई के बारे में तुम किसकी सलाह लोगे ?’’
‘‘डॉक्टर की।’’ लोग जवाब देते।
‘‘डॉक्टर की ही क्यों ? वकील की क्यों नहीं ?’’
‘‘क्योंकि दवाई की जानकारी डॉक्टरों को ही होती है, वकीलों को नहीं।’’
सुकरात इस प्रकार, लोगों से एक के बाद एक प्रश्न पूछता था और उनसे जवाब पाने की कोशिश करता था। फिर हँसता हुआ कहता था, ‘‘सज्जनों, जूता सिलवाना हो तो तुम मोची के पास जाते हो, मकान बनवाना हो तो मिस्त्री की मदद लेते हो। फर्नीचर बनवाना हो तो बढ़ई को काम सौंपते हो। बीमार पड़ने पर डॉक्टरों की सलाह लेते हो। किसी झमेले में फँस जाते हो तब वकीलों के पास दौड़ते हो। क्यों ? ये सब लोग अपने-अपने क्षेत्र के जानकार हैं इसीलिए न ? फिर बताओ, राजकाज तुम ‘किसी के भी’ हाथ में कैसे सौंप देते हो ? क्या राजकाज चलाने के लिए जानकारों की जरूरत नहीं होती ? ऐरे-गैरों से काम चल सकता है ?’’
स्वराज्य में हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में ‘किसी को भी’ भेज दिया, ‘किसी को भी’ मन्त्री बना दिया। हमने उनका अनुभव वगैरह कुछ नहीं देखा। देखी सिर्फ उनकी जाति या उनका धर्म। नतीजा-मौजूदा सरकार से पहले की सरकार अच्छी थी, उससे अच्छी उससे पहले की थी, यह कहते-कहते अन्त में सबसे अच्छी अँग्रेजों की थी, इस नतीजे पर आ पहुँचते हैं।
लोकतन्त्र को बचाना हो तो किसी-न-किसी को समाज में सुकरात की भूमिका निभानी ही होगी। लोगों से प्रश्न पूछ-पूछकर उन्हें सजग करने का काम करना होगा। हो सकता है, लोगों को वह असहनीय मालूम हो और लोग उसे जहर पिलाने के लिए उद्यत हो जाएँ।
लेकिन यह कीमत हमें स्वराज्य और लोकतन्त्र को बचाने के लिए चुकानी ही होगी।
‘‘मोची के पास।’’ लोग जवाब देते।
‘‘मोची के पास ही क्यों ? बढ़ई के पास क्यों नहीं ?’’
‘‘क्योंकि जूते बनाने-जोड़ने का काम मोची का है, बढ़ई का नहीं।’’ लोग जवाब देते।
‘‘अच्छा, मान लो, तुम्हारी माँ बीमार है। तो दवाई के बारे में तुम किसकी सलाह लोगे ?’’
‘‘डॉक्टर की।’’ लोग जवाब देते।
‘‘डॉक्टर की ही क्यों ? वकील की क्यों नहीं ?’’
‘‘क्योंकि दवाई की जानकारी डॉक्टरों को ही होती है, वकीलों को नहीं।’’
सुकरात इस प्रकार, लोगों से एक के बाद एक प्रश्न पूछता था और उनसे जवाब पाने की कोशिश करता था। फिर हँसता हुआ कहता था, ‘‘सज्जनों, जूता सिलवाना हो तो तुम मोची के पास जाते हो, मकान बनवाना हो तो मिस्त्री की मदद लेते हो। फर्नीचर बनवाना हो तो बढ़ई को काम सौंपते हो। बीमार पड़ने पर डॉक्टरों की सलाह लेते हो। किसी झमेले में फँस जाते हो तब वकीलों के पास दौड़ते हो। क्यों ? ये सब लोग अपने-अपने क्षेत्र के जानकार हैं इसीलिए न ? फिर बताओ, राजकाज तुम ‘किसी के भी’ हाथ में कैसे सौंप देते हो ? क्या राजकाज चलाने के लिए जानकारों की जरूरत नहीं होती ? ऐरे-गैरों से काम चल सकता है ?’’
स्वराज्य में हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में ‘किसी को भी’ भेज दिया, ‘किसी को भी’ मन्त्री बना दिया। हमने उनका अनुभव वगैरह कुछ नहीं देखा। देखी सिर्फ उनकी जाति या उनका धर्म। नतीजा-मौजूदा सरकार से पहले की सरकार अच्छी थी, उससे अच्छी उससे पहले की थी, यह कहते-कहते अन्त में सबसे अच्छी अँग्रेजों की थी, इस नतीजे पर आ पहुँचते हैं।
लोकतन्त्र को बचाना हो तो किसी-न-किसी को समाज में सुकरात की भूमिका निभानी ही होगी। लोगों से प्रश्न पूछ-पूछकर उन्हें सजग करने का काम करना होगा। हो सकता है, लोगों को वह असहनीय मालूम हो और लोग उसे जहर पिलाने के लिए उद्यत हो जाएँ।
लेकिन यह कीमत हमें स्वराज्य और लोकतन्त्र को बचाने के लिए चुकानी ही होगी।
3
मेरे और उनके विचारों में जमीन-आसमान का
अन्तर है। मैं मानता हूँ, ठीक
उससे उल्टा वे मानते हैं। और वे मेरे पड़ोस में रहने आये हैं !
मुझे क्या करना चाहिए ? इनके पड़ोस में मुझे रहना नहीं है, कहकर यहाँ से और कहीं चले जाना चाहिए ? नहीं, मैं बेबस आदमी नहीं हूँ। मुझे यहाँ से खिसकना नहीं चाहिए। तो क्या, उन्हें मेरे विचारों के अनुरूप ढालने के प्रयासों में लग जाना चाहिए ? नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या उनसे बोलना बन्द कर देना चाहिए ? उनसे कोई सम्बन्ध ही न रखना चाहिए ? नहीं, मैं बुजदिल नहीं हूँ। मेरे सामने एक ही रास्ता है। उनसे दूर भागने, सम्बन्ध तोड़ने या उन्हें अपने विचारों का बनाने के प्रयास करने के बजाय उनके पड़ोस में ही रहकर मुझे अपने विचारों को लेकर चलना चाहिए और उन्हें अपने विचारों से चलने देना चाहिए। हो सके तो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सौ फीसदी मतभेद तोअपने कट्टर दुश्मनों से भी नहीं होते। दस फीसदी मदभेद हों तो नब्बे फीसदी ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ हम साथ-साथ काम कर सकते हैं।
मतभेद तो विचारों की दुनिया की शान है।
जैनों का एक सिद्धान्त है, जिसे वे स्याद्वाद कहते हैं। वे कहते हैं कि सम्पूर्ण सत्य तो किसी को भी पूर्णरूप से दिखाई नहीं देता। किस जगह पर खड़े रहकर उसकी ओर हम देखते हैं, इसी पर हमारे सत्य का दर्शन निर्भर होता है। और ऐसी जगहें तो अनगिनत हैं। मान लीजिए किसी सैलानी ने हमसे पूछा, गोवा किस ओर है ? वह दिल्ली का हो तो हमारा जवाब होगा, गोवा दिल्ली के दक्षिण की ओर है और वह बैंगलोर का हो तो हम कहेंगे गोवा बैंगलोर के उत्तर की ओर है। गोवा से अगर पूछें तो वह कहेगा, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वही हूँ। हाँ, दिल्ली मेरे उत्तर दिशा में है, और बैंगलोर दक्षिण की ओर है। इनमें से एक भी जवाब झूठा नहीं है। सभी सत्य हैं। लेकिन अलग-अलग जगहों पर खड़े रहकर उत्तर दिये हुए हैं। इस सत्य की अगर प्रतीति हो जाए तो अनेक परस्पर विरोधी विचारों के लोग एक-दूसरे के पड़ोस में जरूर रह सकेंगे।
मुझे क्या करना चाहिए ? इनके पड़ोस में मुझे रहना नहीं है, कहकर यहाँ से और कहीं चले जाना चाहिए ? नहीं, मैं बेबस आदमी नहीं हूँ। मुझे यहाँ से खिसकना नहीं चाहिए। तो क्या, उन्हें मेरे विचारों के अनुरूप ढालने के प्रयासों में लग जाना चाहिए ? नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। क्या उनसे बोलना बन्द कर देना चाहिए ? उनसे कोई सम्बन्ध ही न रखना चाहिए ? नहीं, मैं बुजदिल नहीं हूँ। मेरे सामने एक ही रास्ता है। उनसे दूर भागने, सम्बन्ध तोड़ने या उन्हें अपने विचारों का बनाने के प्रयास करने के बजाय उनके पड़ोस में ही रहकर मुझे अपने विचारों को लेकर चलना चाहिए और उन्हें अपने विचारों से चलने देना चाहिए। हो सके तो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। सौ फीसदी मतभेद तोअपने कट्टर दुश्मनों से भी नहीं होते। दस फीसदी मदभेद हों तो नब्बे फीसदी ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ हम साथ-साथ काम कर सकते हैं।
मतभेद तो विचारों की दुनिया की शान है।
जैनों का एक सिद्धान्त है, जिसे वे स्याद्वाद कहते हैं। वे कहते हैं कि सम्पूर्ण सत्य तो किसी को भी पूर्णरूप से दिखाई नहीं देता। किस जगह पर खड़े रहकर उसकी ओर हम देखते हैं, इसी पर हमारे सत्य का दर्शन निर्भर होता है। और ऐसी जगहें तो अनगिनत हैं। मान लीजिए किसी सैलानी ने हमसे पूछा, गोवा किस ओर है ? वह दिल्ली का हो तो हमारा जवाब होगा, गोवा दिल्ली के दक्षिण की ओर है और वह बैंगलोर का हो तो हम कहेंगे गोवा बैंगलोर के उत्तर की ओर है। गोवा से अगर पूछें तो वह कहेगा, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वही हूँ। हाँ, दिल्ली मेरे उत्तर दिशा में है, और बैंगलोर दक्षिण की ओर है। इनमें से एक भी जवाब झूठा नहीं है। सभी सत्य हैं। लेकिन अलग-अलग जगहों पर खड़े रहकर उत्तर दिये हुए हैं। इस सत्य की अगर प्रतीति हो जाए तो अनेक परस्पर विरोधी विचारों के लोग एक-दूसरे के पड़ोस में जरूर रह सकेंगे।
4
जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा,
‘‘यहाँ के
लोगों को कौन-सी बीमारियाँ अधिक होती हैं ?’’
‘‘मानसिक’’, उन्होंने जवाब दिया, ‘‘यहाँ के अस्सी फीसदी लोग मनोरुग्ण हैं।’’
‘‘इसकी क्या वजह है ?’’
कहने लगे, ‘‘हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गयी है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पड़ते हैं, तब अपने आपसे लगातार बड़बड़ाते रहते हैं।...अमरीका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एकमहीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे ‘स्पीड’ का इंजन लगाने पर वह हजार गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है, जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है।...यही कारण है, जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गये हैं।...’’
शाम को वह मुझे एक ‘टी सेरेमनी’ में ले गये। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा-नो-यू कहते हैं।
वह एक छ: मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारोंवाली और तातामी (चटाई) की जमीनवाली एक सुन्दर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब-सा एक मिट्टी का बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ-पाँव इस पानी से धोये। तौलिए से पोंछे और अन्दर गये। अन्दर ‘चाजीन’ बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो...झो (आइए, तशरीफ लाइए) कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखायी। अँगीठी सुलगायी। उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिये से बर्तन साफ किये। सभी क्रियाएँ इतनी गरिमापूर्ण ढंग से कीं कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जयजयवन्ती के सुर गूँज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शान्त था कि चायदानी के पानी का बदबदाना भी सुनाई दे रहा था।
चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिये गये। वहाँ हम तीन मित्र ही थे। इस विधि में शान्ति मुख्य बात होती है। इसलिए वहाँ तीन से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में दो घूँट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक-एक बूँद चाय पीते रहे। करीब डेढ़ घण्टे तक चुसकियों का यह सिलसिला चलता रहा।
पहले दस-पन्द्रह मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। फिर देखा, दिमाग की रफ्तार धीरे-धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिलकुल बन्द भी हो गयी। मुझे लगा, मानों अनन्तकाल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा।
अकसर हम या तो गुजरे दिनों की खट्टी-मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भवि्ष्यकाल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते-पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गये थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था। और वह अनन्तकाल जितना विस्तृत था।
जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ।
झेन परम्परा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को !
‘‘मानसिक’’, उन्होंने जवाब दिया, ‘‘यहाँ के अस्सी फीसदी लोग मनोरुग्ण हैं।’’
‘‘इसकी क्या वजह है ?’’
कहने लगे, ‘‘हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गयी है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। कोई बोलता नहीं, बकता है। हम जब अकेले पड़ते हैं, तब अपने आपसे लगातार बड़बड़ाते रहते हैं।...अमरीका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एकमहीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे ‘स्पीड’ का इंजन लगाने पर वह हजार गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है, जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है।...यही कारण है, जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गये हैं।...’’
शाम को वह मुझे एक ‘टी सेरेमनी’ में ले गये। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में उसे चा-नो-यू कहते हैं।
वह एक छ: मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारोंवाली और तातामी (चटाई) की जमीनवाली एक सुन्दर पर्णकुटी थी। बाहर बेढब-सा एक मिट्टी का बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ-पाँव इस पानी से धोये। तौलिए से पोंछे और अन्दर गये। अन्दर ‘चाजीन’ बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो...झो (आइए, तशरीफ लाइए) कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखायी। अँगीठी सुलगायी। उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिये से बर्तन साफ किये। सभी क्रियाएँ इतनी गरिमापूर्ण ढंग से कीं कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जयजयवन्ती के सुर गूँज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शान्त था कि चायदानी के पानी का बदबदाना भी सुनाई दे रहा था।
चाय तैयार हुई। उसने वह प्यालों में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिये गये। वहाँ हम तीन मित्र ही थे। इस विधि में शान्ति मुख्य बात होती है। इसलिए वहाँ तीन से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में दो घूँट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक-एक बूँद चाय पीते रहे। करीब डेढ़ घण्टे तक चुसकियों का यह सिलसिला चलता रहा।
पहले दस-पन्द्रह मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। फिर देखा, दिमाग की रफ्तार धीरे-धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिलकुल बन्द भी हो गयी। मुझे लगा, मानों अनन्तकाल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा।
अकसर हम या तो गुजरे दिनों की खट्टी-मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भवि्ष्यकाल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए। चाय पीते-पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गये थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था। और वह अनन्तकाल जितना विस्तृत था।
जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ।
झेन परम्परा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को !
5
बस स्टॉप पर मैं अपनी बस की प्रतीक्षा कर रहा
था। वहीं
‘भैया, बच्चे को कुछ दे दो’ कहकर एक भिखारिन ने मेरे
सामने
हाथ फैलाया। मैंने अपनी जेब टटोली। एक रुपये का सिक्का मिला। मैंने उसे दे
दिया।
मेरे साथ एक मित्र कतार में खड़े थे। कहने लगे, ‘‘भिखारियों को पैसे देने की यह आदत अच्छी नहीं है। भीख माँगना आजकल अच्छा-खासा धंधा बन गया है। ऐसे लोगों से काम करने को कहना चाहिए।’’
मेरे पास जवाब था, लेकिन देने की इच्छा नहीं हुई। खामखाँ रास्ते पर ही बहस छिड़ जाती।
मन बरसों पीछे चला गया।
मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा था। दोपहर के समय ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। बीस मिनट का पड़ाव था। वहीं मेरी थाली आयी। खाना शुरू करने ही जा रहा था कि ‘भैया, बच्चे को कुछ दे दो’ कहकर एक भिखारिन हाथ फैलाये खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गयी। ‘कम्बख्त, ठीक इसी वक्त आयी है’ कहकर मैंने उसे मन ही मन कोसा। दिल कठोर करके उसे आगे जाने को कहा और खिड़की बन्द कर दी।
लेकिन गले के नीचे कौर उतरे तब न ! थोड़ी देर उधेड़बुन में पड़ा रहा। मन ही मन मैंने अपने को कोसते हुए कहा-बेचारी लाचार है, इसीलिए भीख माँग रही है। उसका यह धन्धा थोड़ी ही है ! समाज उसे काम नहीं दे सका इसलिए उसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा...काम मिलता तो भीख कौन माँगता ? उसे ‘आगे जाओ’ कहकर मैंने खिड़की बन्द कर दी थी, इस बात पर मुझे अब शर्म महसूस होने लगी। दूसरे ही क्षण मैंने निर्णय ले लिया। एक रोटी पर थोड़ी सब्जी अपने लिए अलग रख ली और बाकी की सारी थाली भिखारिन को देने की सोची। खिड़की खोल दी। बाहर वह भिखारिन नहीं दिखी। मैं उसे ढूँढ़ने प्लेटफॉर्म पर उतरा। वह कहीं नजर नहीं आयी। मैं अपना-सा मुँह लेकर डिब्बे में लौट आया। अपने लिए अलग रखी हुई रोटी और सब्जी फिर से थाली में रख दी और थाली सीट के नीचे सरका दी।
गाड़ी छूटने के समय वेटर आया। वह पैसे और थाली दोनों ले गया।
मेरी बगल में एक नवजवान बैठा था। इण्टरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा था। बड़ा बातूनी था। ऐन रैण्ड की पुस्तक पढ़ रहा था। उसके साथ देर शाम तक बातें करता रहा।
ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रात को एक बड़ा स्टेशन आया, जहाँ वह रुक गयी। वहाँ मेरी थाली आयी। मैं खाने जा ही रहा था कि मुझे उस भिखारिन की वही आवाज फिर से सुनाई दी-‘भैया, बच्चे को कुछ दे दो।’ ‘अच्छा ! तो यह हमारे साथ ट्रेन में ही है !’ मैंने आश्चर्यचकित होकर अपने आपसे कहा और अपनी थाली उसे देने को हुआ। अचानक मेरी नजर भिखारिन के चेहरे पर पड़ी। हक्का-बक्का होकर उसे देखने लगा। मैं बुदबुदाया, ‘‘तुम ? भीख माँग रही हो ? नहीं...मैं जब तक जिन्दा हूँ तुम्हें इस हालत में कभी नहीं पड़ने दूँगा....कभी नहीं...।’’ यह कहकर मैं सिसकियाँ लेने लगा।
मैंने स्वप्न में अपनी माँ को भीख माँगते देखा था।
ट्रेन छुक-छुक-छुक-छुक करके दौड़ रही थी।
तब से किसी भी भिखारिन को ‘आगे जाओ’ कहने की हिम्मत मुझे नहीं होती। जेब में जो कुछ हाथ आता है, निकालकर दे देता हूँ।
मेरे साथ एक मित्र कतार में खड़े थे। कहने लगे, ‘‘भिखारियों को पैसे देने की यह आदत अच्छी नहीं है। भीख माँगना आजकल अच्छा-खासा धंधा बन गया है। ऐसे लोगों से काम करने को कहना चाहिए।’’
मेरे पास जवाब था, लेकिन देने की इच्छा नहीं हुई। खामखाँ रास्ते पर ही बहस छिड़ जाती।
मन बरसों पीछे चला गया।
मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा था। दोपहर के समय ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। बीस मिनट का पड़ाव था। वहीं मेरी थाली आयी। खाना शुरू करने ही जा रहा था कि ‘भैया, बच्चे को कुछ दे दो’ कहकर एक भिखारिन हाथ फैलाये खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गयी। ‘कम्बख्त, ठीक इसी वक्त आयी है’ कहकर मैंने उसे मन ही मन कोसा। दिल कठोर करके उसे आगे जाने को कहा और खिड़की बन्द कर दी।
लेकिन गले के नीचे कौर उतरे तब न ! थोड़ी देर उधेड़बुन में पड़ा रहा। मन ही मन मैंने अपने को कोसते हुए कहा-बेचारी लाचार है, इसीलिए भीख माँग रही है। उसका यह धन्धा थोड़ी ही है ! समाज उसे काम नहीं दे सका इसलिए उसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा...काम मिलता तो भीख कौन माँगता ? उसे ‘आगे जाओ’ कहकर मैंने खिड़की बन्द कर दी थी, इस बात पर मुझे अब शर्म महसूस होने लगी। दूसरे ही क्षण मैंने निर्णय ले लिया। एक रोटी पर थोड़ी सब्जी अपने लिए अलग रख ली और बाकी की सारी थाली भिखारिन को देने की सोची। खिड़की खोल दी। बाहर वह भिखारिन नहीं दिखी। मैं उसे ढूँढ़ने प्लेटफॉर्म पर उतरा। वह कहीं नजर नहीं आयी। मैं अपना-सा मुँह लेकर डिब्बे में लौट आया। अपने लिए अलग रखी हुई रोटी और सब्जी फिर से थाली में रख दी और थाली सीट के नीचे सरका दी।
गाड़ी छूटने के समय वेटर आया। वह पैसे और थाली दोनों ले गया।
मेरी बगल में एक नवजवान बैठा था। इण्टरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा था। बड़ा बातूनी था। ऐन रैण्ड की पुस्तक पढ़ रहा था। उसके साथ देर शाम तक बातें करता रहा।
ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रात को एक बड़ा स्टेशन आया, जहाँ वह रुक गयी। वहाँ मेरी थाली आयी। मैं खाने जा ही रहा था कि मुझे उस भिखारिन की वही आवाज फिर से सुनाई दी-‘भैया, बच्चे को कुछ दे दो।’ ‘अच्छा ! तो यह हमारे साथ ट्रेन में ही है !’ मैंने आश्चर्यचकित होकर अपने आपसे कहा और अपनी थाली उसे देने को हुआ। अचानक मेरी नजर भिखारिन के चेहरे पर पड़ी। हक्का-बक्का होकर उसे देखने लगा। मैं बुदबुदाया, ‘‘तुम ? भीख माँग रही हो ? नहीं...मैं जब तक जिन्दा हूँ तुम्हें इस हालत में कभी नहीं पड़ने दूँगा....कभी नहीं...।’’ यह कहकर मैं सिसकियाँ लेने लगा।
मैंने स्वप्न में अपनी माँ को भीख माँगते देखा था।
ट्रेन छुक-छुक-छुक-छुक करके दौड़ रही थी।
तब से किसी भी भिखारिन को ‘आगे जाओ’ कहने की हिम्मत मुझे नहीं होती। जेब में जो कुछ हाथ आता है, निकालकर दे देता हूँ।
6
बरसों से हम इसी रास्ते को, जिस पर हम चल रहे
हैं, सही
मानते आये। अब मालूम हुआ कि यह सही रास्ता नहीं, बल्कि गलत है। जिस मंजिल
पर पहुँचना चाहते हैं वहाँ ले जाने वाला नहीं है। मगर, यकायक उसे छोड़
कैसे दें, इस उलझन में उसी रास्ते पर हम अब भी चल रहे हैं।
गाँधीजी के रास्ते चलते, तो गरीबों को कम से कम दो रोटियाँ तो हम मुहैया करा ही देते। गरीबी कुछ हद तक कम हो जाती। पर हमने इस रास्ते को पुराना, सोलहवीं सदी का माना और उसे छोड़ दिया। बदले में जवाहरलाल नेहरू का चार रोटियाँ देने की इच्छा रखने वाला ‘आधुनिक’ रास्ता अपनाया। इस रास्ते पर चलते अब हमें पचास साल से ज्यादा हो गये। गरीबों को आधी रोटी भी हम मुहैया नहीं करा सके। इस प्रतीति के बाद भी हम यह रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। इसी रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं।
हमने गलत रास्ता अपनाया है, यह कबूल करने की नैतिक हिम्मत देश के कर्णधारों में नहीं है।
हम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं। अपने आपको कैसे देंगे ?
जहाँ नींद खुल जाती है, वहीं से हमारी सुबह शुरू होती है। इस अर्थ का एक मुहावरा गुजराती भाषा में है-‘जाग्या त्यॉथी सवार।’ गोवा से मुम्बई जाने के लिए निकला हुआ आदमी मंगलूर पहुँच जाए तो कहना चाहिए, वह गलत रास्ते जा रहा है। और इसी रास्ते आगे जाने की वह जिद ठान ले तो उसे बताना चाहिए, ‘भाई, तुम इसी रास्ते आगे बढ़ोगे तो कोचीन पहुँच जाओगे, कन्याकुमारी पहुँचोगे।’ यहाँ तक कि दक्षिण ध्रुव तक भी जा सकते हो मगर मुम्बई नहीं पहुँचोगे। गलत रास्ते से चलनेवाले के कदम सही रास्ते पर कभी नहीं पड़ते। अपनी तय की हुई मंजिल पर वह कभी नहीं पहुँच सकता। इसने साल हम इसी रास्ते चलते आये, अब उसे कैसे छोड़ सकते हैं, यह कहना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। गलत रास्ता छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। एक बार निर्णय लेना पड़ेगा-‘हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे...नहीं यानी नहीं, कभी नहीं। बस, सारी उधेड़-बुन दूर हो जाएगी और जिस रास्ते चलना चाहिए, उसी रास्ते पर कदम पड़ते रहेंगे।
अपना रास्ता गलत था यह जवाहरलाल को आखिर में महसूस हो गया था। पर रास्ता बदलने का निश्चय करने के पहले ही वे चल बसे। दुर्भाग्य से उनके उत्तराधिकारी भी उसी गलत रास्ते चलते रहे। नतीजा-समाजवाद के स्वर्ग में जाने के लिए निकले हुए हम लोग विश्व बैंक के मुक्त बाजार की दलदल में फँस गये।
गाँधीजी के रास्ते चलते, तो गरीबों को कम से कम दो रोटियाँ तो हम मुहैया करा ही देते। गरीबी कुछ हद तक कम हो जाती। पर हमने इस रास्ते को पुराना, सोलहवीं सदी का माना और उसे छोड़ दिया। बदले में जवाहरलाल नेहरू का चार रोटियाँ देने की इच्छा रखने वाला ‘आधुनिक’ रास्ता अपनाया। इस रास्ते पर चलते अब हमें पचास साल से ज्यादा हो गये। गरीबों को आधी रोटी भी हम मुहैया नहीं करा सके। इस प्रतीति के बाद भी हम यह रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। इसी रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं।
हमने गलत रास्ता अपनाया है, यह कबूल करने की नैतिक हिम्मत देश के कर्णधारों में नहीं है।
हम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं। अपने आपको कैसे देंगे ?
जहाँ नींद खुल जाती है, वहीं से हमारी सुबह शुरू होती है। इस अर्थ का एक मुहावरा गुजराती भाषा में है-‘जाग्या त्यॉथी सवार।’ गोवा से मुम्बई जाने के लिए निकला हुआ आदमी मंगलूर पहुँच जाए तो कहना चाहिए, वह गलत रास्ते जा रहा है। और इसी रास्ते आगे जाने की वह जिद ठान ले तो उसे बताना चाहिए, ‘भाई, तुम इसी रास्ते आगे बढ़ोगे तो कोचीन पहुँच जाओगे, कन्याकुमारी पहुँचोगे।’ यहाँ तक कि दक्षिण ध्रुव तक भी जा सकते हो मगर मुम्बई नहीं पहुँचोगे। गलत रास्ते से चलनेवाले के कदम सही रास्ते पर कभी नहीं पड़ते। अपनी तय की हुई मंजिल पर वह कभी नहीं पहुँच सकता। इसने साल हम इसी रास्ते चलते आये, अब उसे कैसे छोड़ सकते हैं, यह कहना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। गलत रास्ता छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। एक बार निर्णय लेना पड़ेगा-‘हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे...नहीं यानी नहीं, कभी नहीं। बस, सारी उधेड़-बुन दूर हो जाएगी और जिस रास्ते चलना चाहिए, उसी रास्ते पर कदम पड़ते रहेंगे।
अपना रास्ता गलत था यह जवाहरलाल को आखिर में महसूस हो गया था। पर रास्ता बदलने का निश्चय करने के पहले ही वे चल बसे। दुर्भाग्य से उनके उत्तराधिकारी भी उसी गलत रास्ते चलते रहे। नतीजा-समाजवाद के स्वर्ग में जाने के लिए निकले हुए हम लोग विश्व बैंक के मुक्त बाजार की दलदल में फँस गये।
7
यूँ तो हम सब समान हैं। लेकिन मैं जिस तरह से
सोचता हूँ उस
तरह से दूसरा नहीं सोचता। हर एक के सोचने का ढंग अलग होता है। हर एक की
रुचि अलग होती है। हर एक की कार्यपद्धति अलग होती है। क्योंकि हर एक के
संस्कार अलग होते हैं। इसलिए दो अन्तरंग मित्रों के बीच भी मतभेद होते
हैं। यही नहीं, दोनों के बीच कभी-कभी गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं।
आज की सभ्य दुनिया में औचित्य के बारे में कुछ गलत धारणाएँ प्रचलित हैं। अपने अन्तरंग मित्र के बारे में मन में कोई शंका पैदा हो जाए तो मैं निखालिसता के साथ उसे बताता नहीं। उसे बुरा न लगे इस डर से मैं बताने से हिचकिचाता हूँ। लेकिन तीसरे किसी को बिना दुविधा के बता देता हूँ। कभी-कभी किसी दूसरे नाम से लिख भी डालता हूँ और अखबारों में भी भेज देता हूँ।
अनुभव यह है कि मैं जो तीसरे से कहता हूँ, वह उसे मालूम हो ही जाता है। अखबारों में देता हूँ तो वह किसने लिखा है, यह भी उसे पता चल ही जाता है।
और उसका मन दूषित होता है।
एक नीतिवचन सुना था-
आज का तुम्हारा मित्र कल शत्रु बन सकता है। इसी तरह आज का शत्रु कल मित्र बन सकता है। आज का मित्र कल शत्रु बनने पर तुम्हारे मर्म दुनिया के सामने खोल सकता है। इसलिए आज भी तुम उससे इस तरह की सर्तकता से पेश आओ जिससे तुम्हारे मर्म उसके ध्यान में ही न आ पाएँ। इसी तरह आज का शत्रु कल मित्र बनने पर शर्म के मारे तुम्हें उसके सामने अपना सिर झुकाना न पड़े, यह ध्यान में रखकर ऐसा कोई काम न करो जिससे उसे चोट पहुँचे।
ऊपर से देखने पर यह नीति व्यवहार कुशल लोगों की सी लगती है पर गहराई में उतरने पर इस नीति में आर्यत्व का भी अंश दिखाई देगा।
किसी के भी मर्मस्थान पर हमारे हाथों कोई आघात नहीं पहुँचना चाहिए।
कवि बोरकजी के साथ मेरे अकसर मतभेद हुआ करते थे। लेकिन हम दोनों ने एक नियम बना लिया था। मन में थोड़ी-सी भी शंका-कुशंका पैदा होते ही हम एक-दूसरे से मिलते और मन की बात एक-दूसरे को बता देते। हमारे बीच मतभेद हमेशा रहे, पर गलतफहमी कभी भी पैदा न हो पायी।
दोष हम सबमें हैं। अच्छे से अच्छे माने जाने वाले लोगों में भी हैं। गुण भी हम सबमें हैं। बुरे से बुरे माने जाने वाले लोगों में भी। गुणों और दोषों के तानों-बानों से हम सबका जीवनपट बुना हुआ है।
अपने दोष दुनिया के सामने न आएँ इसकी दक्षता हर आदमी प्राप्त करता आया है। इस इच्छा की हमें कद्र करनी चाहिए और दूसरे के दोष दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न किसी भी संस्कारी आदमी को नहीं करना चाहिए। नियम ही बना लेना चाहिए कि मन में शंका पैदा हो तो उसे हम उसी को बता देंगे, तीसरे को कभी नहीं। छद्म नाम से अखबारों में तो कभी नहीं लिखेंगे। पीठ पीछे बुराई करने वालों को हम चुगलखोर कहते हैं। और चुगलखोर को हमेशा घटिया आदमी मानते आये हैं।
आज की सभ्य दुनिया में औचित्य के बारे में कुछ गलत धारणाएँ प्रचलित हैं। अपने अन्तरंग मित्र के बारे में मन में कोई शंका पैदा हो जाए तो मैं निखालिसता के साथ उसे बताता नहीं। उसे बुरा न लगे इस डर से मैं बताने से हिचकिचाता हूँ। लेकिन तीसरे किसी को बिना दुविधा के बता देता हूँ। कभी-कभी किसी दूसरे नाम से लिख भी डालता हूँ और अखबारों में भी भेज देता हूँ।
अनुभव यह है कि मैं जो तीसरे से कहता हूँ, वह उसे मालूम हो ही जाता है। अखबारों में देता हूँ तो वह किसने लिखा है, यह भी उसे पता चल ही जाता है।
और उसका मन दूषित होता है।
एक नीतिवचन सुना था-
आज का तुम्हारा मित्र कल शत्रु बन सकता है। इसी तरह आज का शत्रु कल मित्र बन सकता है। आज का मित्र कल शत्रु बनने पर तुम्हारे मर्म दुनिया के सामने खोल सकता है। इसलिए आज भी तुम उससे इस तरह की सर्तकता से पेश आओ जिससे तुम्हारे मर्म उसके ध्यान में ही न आ पाएँ। इसी तरह आज का शत्रु कल मित्र बनने पर शर्म के मारे तुम्हें उसके सामने अपना सिर झुकाना न पड़े, यह ध्यान में रखकर ऐसा कोई काम न करो जिससे उसे चोट पहुँचे।
ऊपर से देखने पर यह नीति व्यवहार कुशल लोगों की सी लगती है पर गहराई में उतरने पर इस नीति में आर्यत्व का भी अंश दिखाई देगा।
किसी के भी मर्मस्थान पर हमारे हाथों कोई आघात नहीं पहुँचना चाहिए।
कवि बोरकजी के साथ मेरे अकसर मतभेद हुआ करते थे। लेकिन हम दोनों ने एक नियम बना लिया था। मन में थोड़ी-सी भी शंका-कुशंका पैदा होते ही हम एक-दूसरे से मिलते और मन की बात एक-दूसरे को बता देते। हमारे बीच मतभेद हमेशा रहे, पर गलतफहमी कभी भी पैदा न हो पायी।
दोष हम सबमें हैं। अच्छे से अच्छे माने जाने वाले लोगों में भी हैं। गुण भी हम सबमें हैं। बुरे से बुरे माने जाने वाले लोगों में भी। गुणों और दोषों के तानों-बानों से हम सबका जीवनपट बुना हुआ है।
अपने दोष दुनिया के सामने न आएँ इसकी दक्षता हर आदमी प्राप्त करता आया है। इस इच्छा की हमें कद्र करनी चाहिए और दूसरे के दोष दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न किसी भी संस्कारी आदमी को नहीं करना चाहिए। नियम ही बना लेना चाहिए कि मन में शंका पैदा हो तो उसे हम उसी को बता देंगे, तीसरे को कभी नहीं। छद्म नाम से अखबारों में तो कभी नहीं लिखेंगे। पीठ पीछे बुराई करने वालों को हम चुगलखोर कहते हैं। और चुगलखोर को हमेशा घटिया आदमी मानते आये हैं।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i