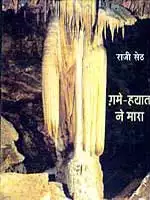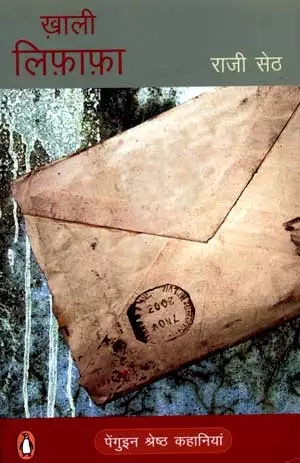|
कहानी संग्रह >> गमे हयात ने मारा गमे हयात ने माराराजी सेठ
|
54 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है राजी सेठ द्वारा चुनी हुई कहानियों का संग्रह...
Gamey
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी की चर्चित कथाकार राजी सेठ का नवीनतम कहानी-संग्रह। राजी ने अपनी कहानियों में वर्तमान की भूमि पर जमकर संघर्ष करने के लिए गत और आगत मूल्यों के विध्यात्मक अर्थों की खोज की है। वास्तव में विध्यात्मकता स्वयं नकारात्मक मूल्यों का निषेध है। यह प्रहार की एक शैली भी हो सकती है,जिसे राजी ने भली-भाँति जाना समझा है। व्यक्ति और परिवार की सीमा में वे बहुत कुछ असीम कहती हैं। वे सपाट माँडल रचकर एक रूढ़ि को तोड़ते हुए दूसरी रूढ़ि बनातीं। पुरुष की निष्करुणता और करुणा को एक साथ प्रचलित उपादानों के विभिन्न संयोजनों में रखकर अनुभव की पूर्णता और सृजनात्मक सामर्थ्य का परिचय देती हैं।
माँ, तुम गयीं तो अपने कंगन
मेरे लिए छोड़ गयीं
ये मुझे बेहद प्रिय हैं, पर
मैं इन्हें बेहिचक
किसी को भी दे सकती हूँ
पर
अपना वह अविचल अकूल साहस
कब्र के अँधेरे में
अपने साथ लेती गयीं
जिनकी तुम्हें तो जरूरत नहीं थी
पर मुझे ? ?....
मेरे लिए छोड़ गयीं
ये मुझे बेहद प्रिय हैं, पर
मैं इन्हें बेहिचक
किसी को भी दे सकती हूँ
पर
अपना वह अविचल अकूल साहस
कब्र के अँधेरे में
अपने साथ लेती गयीं
जिनकी तुम्हें तो जरूरत नहीं थी
पर मुझे ? ?....
एडना सेंट विंसेंट मिले की कविता
माइन द हारवेस्ट’ का भावानुवाद
मुलाकात
घण्टी बजी। चपरासी ने कहा उन्हें अन्दर बुलाया गया है। वे घण्टों से काठ की दुखदायी बेंच पर सिर झुकाये बैठे थे। शायद बीच-बीच में ऊँघ भी जाते रहे हों। खाली बैठे होने पर थकान भी अपनी याद कराने के लिए धमनियों में लपलपाने लगती है, नहीं तो मेहनत-मशक्कत, भागदौड़ में थकान का क्या जिक्र। सुबह गये थे...चाय के थोक व्यापारी की दुकान से खपच्चियाँ बीनकर लाये थे। अखबार में लिपटा वह बेडौल-सा बण्डल उनके साथ था। बण्डल उन्होंने बेंच के नीचे खिसका दिया था, बल्कि पैरों की टेक ऐसे उसे रोक रखा था। दूसरे देख लेंगे तो वे संकुचित होंगे।
चपरासी ने अन्दर बुलाये जाने की सूचना दी तो विश्वास नहीं हुआ। घण्टों बैठे रहने के कारण तत्परता रीत चुकी थी। इन्तजारियों की भीड़ धीरे-धीरे छँट चुकी थी। उठे, चपरासी ने स्प्रिंगवाला जालीदार दरवाजा खोला। अन्दर दाखिल हुए। लगा नहीं कि दाखिल हुए। अन्दर का दृश्य अपने अब तक के होने के विपरीत था-ठण्डा, आरामदेह, गुदगुदा।
सामने कुर्सी पर कलेक्टर साहब बैठे थे। नाम राम दयाल त्रिपाठी सुना था। आला अफसर होना सुना था। दयालु-कृपालु होना सुना था। उखड़े-पुखड़े जो भी लोग उनके जिले के जुगराफिए में आये, जल्द से जल्द उनकी बसाहट के बारे में उनका कमर कसना सुना था, फिर भी...
अन्दर घुसते वे जानते थे, अफसर भी उन्हें हिकारत से ही देखेंगे। हर मौके, हर जगह वे हिकारत के इस आमने-सामने से बच नहीं सकते थे। ऐसी निगाह अब उनके भाग्य में लिखी थी।
उन्होंने त्रिपाठीजी को घूरा। वहाँ हिकारत नहीं थी। दयार्द्र नरमी थी। चेहरा कोमल था पर अनुभवों से पका हुआ।
‘‘बैठिए’’ उन्होंने त्रिपाठी जी को कहते सुना।
पहले सकपकाये, फिर बैठ गये। वैसे भी अपनी इतनी लम्बाई, कुर्सी पर बैठे ठिगने अफसर के सामने अजीब लग रही थी।
‘‘कैसे आना हुआ ?’’
वह आँखें झुकाये रहे। कलेक्टर साहब ने अपनी गलती महसूस की। पटरी बदली, ‘‘उधर, कौन से शहर में बसे हुए थे ?’’
‘‘लाहौर में...’’
‘‘अभी कैम्प में ही रिहायश है या...’’ त्रिपाठीजी ने वाक्य लटकता छोड़ दिया।
‘‘नहीं, दो कमरों का एक घर किराये पर ले लिया है...हाजी जी की बिल्डिंग में....’’
‘‘आराम में हो ?’’
एक लड़खड़ाती हुई ‘‘जीऽऽऽऽ’’
अब ? आगे ? एक बेढब-सी चुप्पी। कलेक्टर साहब को शायद लग रहा होगा कि वे आये हैं तो वही बोलें...जुबान खोलें...वही जरूरतमन्द हैं। जो प्यासा होगा वही तो कुएँ के पास जाएगा।
चुप्पी नहीं टूटी तो उकसाया ‘‘क्या चाहिए ?’’
‘‘यही कोई छोटा-मोटा काम...जिससे गुजारा हो जाए। आजकल इतनी चीजों पर राशन है..वैसी कोई दुकान।’’
‘‘कितना परिवार है ?’’
‘‘हैं, छह-सात लोग...सब साथ रहते हैं।’’
‘‘लड़के ?’’
‘‘हाँ, हैं दो...एक तो नाबालिग है...देर की औलाद।’’
तभी एक चपरासीनुमा आदमी कमरे के दायें से दाखिल हुआ। उसके हाथ में गत्ते का एक बड़ा डिब्बा था। डिब्बा आदमी ने आगत के नजदीक रख दिया। जैसे कि पहले से पता हो उसे कहाँ रखना है।
‘‘इसे ले जाइए।’’ कलेक्टर ने अपना मुँह परे घुमाकर कहा।
‘‘इसमें क्या है ?’’
‘‘ऐसे ही थोड़ा-सा कुछ गुजारे लायक।’’
‘‘गुजारा नहीं चाहिए...काम चाहिए।’’ उनकी आवाज बुरी तरह काँप रही थी।
‘‘ऐसा कुछ खास नहीं है...थोड़ा आटा, थोड़े चावल, चाय, साबुन चीनी वगैरह वगैरह...यही जरूरत की छोटी-मोटी चीजें। फिलहाल तो इसे ले जाइए। खोलकर दिखा दो बलबीर।’’
उन्होंने हाथ के इशारे से बलवीर को मना किया खोलने से। खोलकर दिखाने से। खुद कुर्सी की पीठ से अपनी पीठ लगाकर बैठ गये। इस बार सीधे। अब तक पीठ और आँखें झुकाकर बैठने की आदत बन चुकी थी। हाथ-सिर के पीछे बाँध लिये। कद-काठी की उठान सीधे बैठ जाने से पूरमपूर दिखाने लगी। आमना-सामना एकाएक उजागर हो गया इतने बड़े अफसर के सामने।
बोलने की सुगबुगाहट सामने से दिखाई नहीं दी तो अफसर अफसरी में आ गये, ‘‘कुछ बोलिए तो सही श्रीमान....क्या सोच रहे हैं ?’’
‘‘सोच रहा हूँ....लगातार सोच ही रहा हूँ। उन फसादों में सबके बच्चे मर गये...मेरे क्यों नहीं मरे...क्यों जिन्दा रह गये सब के...।’’
बात के पिछले सिरे तक पहुँचते तक तो शब्द लड़खड़ा गये। जुबान धोखा दे गयी। हाँफती जैसी एक सिसकी उन्होंने भरसक अपने होठों के कोटर में भींचनी चाही पर सफल नहीं हुए। फूट पड़े। फिर तो हाथ सिर से पीछे बँधे रहे। गाल गीले होते रहे। आँखें बन्द रहीं। सुबकियाँ गले में ठेली जाती रहीं। छाती धौकनी सी बजती रही। शरीर हिलता रहा। शर्म छिपा सकने का भी इस समय होश नहीं था।
होश यह भी नहीं था कि इस समय वह अपनी ही कही हुई बातों से मुकर रहे हैं। पलट रहे हैं कैसे भूल गये कि इन्हीं बातों को उन्होंने ही कहा था कुछ दूसरी तरह। कुछेक महीने पहले। पूरे दमखम, पूरी दयानतदारी के साथ। इसी जीवन में। इसी आकाश के नीचे। इसी दिलोदिमाग के रहते। अभी इतने दिन तो नहीं बीते थे कि याद न रख सकें। भूल जाएँ कि क्या कहा था उन्होंने अपनी आँसू-आँसू होती पत्नी से। अपना पुश्तैनी घर छोड़ते समय। लाहौर में। अब के पाकिस्तान में।
पत्नी बारम्बार अपने छूटते घर को मुड़-मुड़कर देखती और आँसुओं के उलार में डूबती। ससुर के साथ होने के कारण उसकी सिसकियाँ छोटी-छोटी, दबी-दबी सी थीं पर उनकी छाती पर जोरदार ढंग से बज रही थीं। ताउम्र साथ रहे पति को इस तरह पहुँच रही थी पत्नी की भाषा।
कोई और कारगार तरीका उनकी समझ में नहीं आया तो चलते-चलते रुके। कुछ आगे चलते पिता की उपस्थित को अनदेखा किया। पत्नी की कलाई पकड़ी। जकड़ी। दायें हाथ के पोरों से उसकी ठोढ़ी ऊपर उठायी। ठकठोरा, ‘‘किसलिए यह रोना धोना ?...जानती हो तुम कोई घर-वर नहीं छोड़ रही हो। अपने देश जा रही हो, अपने देश...पण्डित नेहरू को आज़ादी की बधाई देने। तुम किस्मतवाली हो। भगवान का शुक्र करो, लोगों के सारे मर गये...तुम्हारा एक भी नहीं मरा...।’’
यह सब कहा था उन्होंने। उन्हीं ने। घर छोड़ते समय, पत्नी की कलाई पकड़कर। पूरे विश्वास और दयानतदारी के साथ। गुज़र रहे इस साल के केवल छः-सात महीने पहले। इसी जीवन में। इसी आकाश के नीचे। इसी दिलोदिमाग के रहते। इतने से समय में क्या आदमी की तासीर बदल जाती है...? इतिहास कूटपीट कर क्या किसी आदमी को दूसरा आदमी बना देता है ?
यह सब त्रिपाठी जी को पता होगा। अनुग्रही उदार होने का बाद भी काफिलों और कैम्पों में पकता-टीसता दर्द कुर्सी की समझ से बाहर छूट गया होगा। अपनी समझ से वह दयालु-कृपालु ही थे। देख-सुन भी रहे थे। उपचार भी कर रहे थे। गुज़ारे की पोटलियाँ दर्दी के साथ बाँध देने जैसी मौलिक किस्म की कृपालुता से अपने दरवाजे पर रोज-दर-रोज टूटती को सँभाल भी रहे थे। कई दिनों से। कई महीनों से। दयालु-कृपालु त्रिपाठी जी।
इस समय....इस तरह...सामने फोड़े से फूटते इस अजीब आदमी को देखकर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। इतना लहीम-शहीम; इतना खुद्दार आदमी....उनके सामने बैठा...इस तरह फफक-फफककर...उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं था....दुत्कारा फटकारा भी नहीं था...फिर क्यों...फिर क्यों ?
त्रिपाठीजी को ज्यादा सोचने का समय उन्होंने नहीं दिया। उबाल थमा तो उठ खड़े हुए। ‘गुस्ताखी माफ़ हो साब’ कहकर कमरे से बाहर निकल गये। भूल गये खपच्चियों का बण्डल बेंच के नीचे रखा था घर ले जाने को। अब पता नहीं आग कैसे जलेगी..बुरादा तो कब का खत्म हो चुका अँगीठी का।
चपरासी ने अन्दर बुलाये जाने की सूचना दी तो विश्वास नहीं हुआ। घण्टों बैठे रहने के कारण तत्परता रीत चुकी थी। इन्तजारियों की भीड़ धीरे-धीरे छँट चुकी थी। उठे, चपरासी ने स्प्रिंगवाला जालीदार दरवाजा खोला। अन्दर दाखिल हुए। लगा नहीं कि दाखिल हुए। अन्दर का दृश्य अपने अब तक के होने के विपरीत था-ठण्डा, आरामदेह, गुदगुदा।
सामने कुर्सी पर कलेक्टर साहब बैठे थे। नाम राम दयाल त्रिपाठी सुना था। आला अफसर होना सुना था। दयालु-कृपालु होना सुना था। उखड़े-पुखड़े जो भी लोग उनके जिले के जुगराफिए में आये, जल्द से जल्द उनकी बसाहट के बारे में उनका कमर कसना सुना था, फिर भी...
अन्दर घुसते वे जानते थे, अफसर भी उन्हें हिकारत से ही देखेंगे। हर मौके, हर जगह वे हिकारत के इस आमने-सामने से बच नहीं सकते थे। ऐसी निगाह अब उनके भाग्य में लिखी थी।
उन्होंने त्रिपाठीजी को घूरा। वहाँ हिकारत नहीं थी। दयार्द्र नरमी थी। चेहरा कोमल था पर अनुभवों से पका हुआ।
‘‘बैठिए’’ उन्होंने त्रिपाठी जी को कहते सुना।
पहले सकपकाये, फिर बैठ गये। वैसे भी अपनी इतनी लम्बाई, कुर्सी पर बैठे ठिगने अफसर के सामने अजीब लग रही थी।
‘‘कैसे आना हुआ ?’’
वह आँखें झुकाये रहे। कलेक्टर साहब ने अपनी गलती महसूस की। पटरी बदली, ‘‘उधर, कौन से शहर में बसे हुए थे ?’’
‘‘लाहौर में...’’
‘‘अभी कैम्प में ही रिहायश है या...’’ त्रिपाठीजी ने वाक्य लटकता छोड़ दिया।
‘‘नहीं, दो कमरों का एक घर किराये पर ले लिया है...हाजी जी की बिल्डिंग में....’’
‘‘आराम में हो ?’’
एक लड़खड़ाती हुई ‘‘जीऽऽऽऽ’’
अब ? आगे ? एक बेढब-सी चुप्पी। कलेक्टर साहब को शायद लग रहा होगा कि वे आये हैं तो वही बोलें...जुबान खोलें...वही जरूरतमन्द हैं। जो प्यासा होगा वही तो कुएँ के पास जाएगा।
चुप्पी नहीं टूटी तो उकसाया ‘‘क्या चाहिए ?’’
‘‘यही कोई छोटा-मोटा काम...जिससे गुजारा हो जाए। आजकल इतनी चीजों पर राशन है..वैसी कोई दुकान।’’
‘‘कितना परिवार है ?’’
‘‘हैं, छह-सात लोग...सब साथ रहते हैं।’’
‘‘लड़के ?’’
‘‘हाँ, हैं दो...एक तो नाबालिग है...देर की औलाद।’’
तभी एक चपरासीनुमा आदमी कमरे के दायें से दाखिल हुआ। उसके हाथ में गत्ते का एक बड़ा डिब्बा था। डिब्बा आदमी ने आगत के नजदीक रख दिया। जैसे कि पहले से पता हो उसे कहाँ रखना है।
‘‘इसे ले जाइए।’’ कलेक्टर ने अपना मुँह परे घुमाकर कहा।
‘‘इसमें क्या है ?’’
‘‘ऐसे ही थोड़ा-सा कुछ गुजारे लायक।’’
‘‘गुजारा नहीं चाहिए...काम चाहिए।’’ उनकी आवाज बुरी तरह काँप रही थी।
‘‘ऐसा कुछ खास नहीं है...थोड़ा आटा, थोड़े चावल, चाय, साबुन चीनी वगैरह वगैरह...यही जरूरत की छोटी-मोटी चीजें। फिलहाल तो इसे ले जाइए। खोलकर दिखा दो बलबीर।’’
उन्होंने हाथ के इशारे से बलवीर को मना किया खोलने से। खोलकर दिखाने से। खुद कुर्सी की पीठ से अपनी पीठ लगाकर बैठ गये। इस बार सीधे। अब तक पीठ और आँखें झुकाकर बैठने की आदत बन चुकी थी। हाथ-सिर के पीछे बाँध लिये। कद-काठी की उठान सीधे बैठ जाने से पूरमपूर दिखाने लगी। आमना-सामना एकाएक उजागर हो गया इतने बड़े अफसर के सामने।
बोलने की सुगबुगाहट सामने से दिखाई नहीं दी तो अफसर अफसरी में आ गये, ‘‘कुछ बोलिए तो सही श्रीमान....क्या सोच रहे हैं ?’’
‘‘सोच रहा हूँ....लगातार सोच ही रहा हूँ। उन फसादों में सबके बच्चे मर गये...मेरे क्यों नहीं मरे...क्यों जिन्दा रह गये सब के...।’’
बात के पिछले सिरे तक पहुँचते तक तो शब्द लड़खड़ा गये। जुबान धोखा दे गयी। हाँफती जैसी एक सिसकी उन्होंने भरसक अपने होठों के कोटर में भींचनी चाही पर सफल नहीं हुए। फूट पड़े। फिर तो हाथ सिर से पीछे बँधे रहे। गाल गीले होते रहे। आँखें बन्द रहीं। सुबकियाँ गले में ठेली जाती रहीं। छाती धौकनी सी बजती रही। शरीर हिलता रहा। शर्म छिपा सकने का भी इस समय होश नहीं था।
होश यह भी नहीं था कि इस समय वह अपनी ही कही हुई बातों से मुकर रहे हैं। पलट रहे हैं कैसे भूल गये कि इन्हीं बातों को उन्होंने ही कहा था कुछ दूसरी तरह। कुछेक महीने पहले। पूरे दमखम, पूरी दयानतदारी के साथ। इसी जीवन में। इसी आकाश के नीचे। इसी दिलोदिमाग के रहते। अभी इतने दिन तो नहीं बीते थे कि याद न रख सकें। भूल जाएँ कि क्या कहा था उन्होंने अपनी आँसू-आँसू होती पत्नी से। अपना पुश्तैनी घर छोड़ते समय। लाहौर में। अब के पाकिस्तान में।
पत्नी बारम्बार अपने छूटते घर को मुड़-मुड़कर देखती और आँसुओं के उलार में डूबती। ससुर के साथ होने के कारण उसकी सिसकियाँ छोटी-छोटी, दबी-दबी सी थीं पर उनकी छाती पर जोरदार ढंग से बज रही थीं। ताउम्र साथ रहे पति को इस तरह पहुँच रही थी पत्नी की भाषा।
कोई और कारगार तरीका उनकी समझ में नहीं आया तो चलते-चलते रुके। कुछ आगे चलते पिता की उपस्थित को अनदेखा किया। पत्नी की कलाई पकड़ी। जकड़ी। दायें हाथ के पोरों से उसकी ठोढ़ी ऊपर उठायी। ठकठोरा, ‘‘किसलिए यह रोना धोना ?...जानती हो तुम कोई घर-वर नहीं छोड़ रही हो। अपने देश जा रही हो, अपने देश...पण्डित नेहरू को आज़ादी की बधाई देने। तुम किस्मतवाली हो। भगवान का शुक्र करो, लोगों के सारे मर गये...तुम्हारा एक भी नहीं मरा...।’’
यह सब कहा था उन्होंने। उन्हीं ने। घर छोड़ते समय, पत्नी की कलाई पकड़कर। पूरे विश्वास और दयानतदारी के साथ। गुज़र रहे इस साल के केवल छः-सात महीने पहले। इसी जीवन में। इसी आकाश के नीचे। इसी दिलोदिमाग के रहते। इतने से समय में क्या आदमी की तासीर बदल जाती है...? इतिहास कूटपीट कर क्या किसी आदमी को दूसरा आदमी बना देता है ?
यह सब त्रिपाठी जी को पता होगा। अनुग्रही उदार होने का बाद भी काफिलों और कैम्पों में पकता-टीसता दर्द कुर्सी की समझ से बाहर छूट गया होगा। अपनी समझ से वह दयालु-कृपालु ही थे। देख-सुन भी रहे थे। उपचार भी कर रहे थे। गुज़ारे की पोटलियाँ दर्दी के साथ बाँध देने जैसी मौलिक किस्म की कृपालुता से अपने दरवाजे पर रोज-दर-रोज टूटती को सँभाल भी रहे थे। कई दिनों से। कई महीनों से। दयालु-कृपालु त्रिपाठी जी।
इस समय....इस तरह...सामने फोड़े से फूटते इस अजीब आदमी को देखकर पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। इतना लहीम-शहीम; इतना खुद्दार आदमी....उनके सामने बैठा...इस तरह फफक-फफककर...उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं था....दुत्कारा फटकारा भी नहीं था...फिर क्यों...फिर क्यों ?
त्रिपाठीजी को ज्यादा सोचने का समय उन्होंने नहीं दिया। उबाल थमा तो उठ खड़े हुए। ‘गुस्ताखी माफ़ हो साब’ कहकर कमरे से बाहर निकल गये। भूल गये खपच्चियों का बण्डल बेंच के नीचे रखा था घर ले जाने को। अब पता नहीं आग कैसे जलेगी..बुरादा तो कब का खत्म हो चुका अँगीठी का।
ग़मे-हयात ने मारा
मैंने उसे तुरन्त ही पहचान लिया था। विशाल सहन के बीचोंबीच रखे, बड़े हवनकुण्ड के उस पार वाले हिस्से में वह अपने घुटनों को बाँहों में घेरे दत्तचित्त बैठी थी। लपटों से बनती भाप की थरथराहट के पास उसका चेहरा अचानक मेरी पकड़ में आया था।
वह थी-चन्नी। माथे की ढलुवाँ गोलाई को काटती सुघड़ नाक, भरे-भरे होठ। दन्तपंक्ति में दायें को अलग से उठा हुआ एक दाँत, जो दोनों होठों के मिलाप को बाधित करता था। चेहरा पहले से ज्यादा भरपूर, माथे पर बड़ी-सी बिन्दी, जिसके चलते सारा मुख-मण्डल नया-सा लग रहा था। उससे लगकर जो व्यक्ति बैठा था शायद उसका पति होगा।
मैंने उमगकर अपनी बाँह उठायी। सिर के ऊपर ले जाकर हिलायी, उसे सत्कारते हुए। आँख मिली थी। पहचान चटक हुई थी। पर वह साझा क्षण उसी निमिष टूट गया था। मुझे लगा उसी ने टूट जाने दिया है। मुँह फेर लिया है।
अविश्वास को भ्रम का सहारा दे देना सहज लगा। हवन के समाप्त होने की प्रतीक्षा की।
‘ओउम अग्नये नय सपथा’ पण्डितजी उपासना मन्त्रों के निकट पहुँच रहे थे। अपनी दोनों फैली हथेलियाँ ऊपर को उछाल रहे थे। लोगों को उपासना मन्त्रों के उच्चारण में सम्मिलित होने को उकसा रहे थे।
अनुष्ठान के अन्त तक आते तो वातावरण काफी सामूहिक और समावेशी हो चला था। मृत्यु के प्रसंग की प्रगाढ़ता पिघल रही थी।
अब, जेठे को पगड़ी पहनाने की रस्म, फिर दान-दक्षिणा, फिर सामूहिक रूप से उच्चारा जाता शान्ति पाठ। बन्द आँखें। अपने-अपने आसनों पर खड़े हो चुके लोग।
‘‘ओउम् शान्तिः....शान्ति:....शान्ति:....ओउम्।’’ ओंकार की पिछड़ती लय अभी डूबी भी नहीं थी कि मैं भीड़ काटकर सहन के उसी हिस्से में पहुँच गयी थी। वह वहाँ नहीं थी। वह कहीं भी नहीं थी। मेरी अधीरता ने उसे लगभग हर सम्भव जगह ढूँढ़ा।
भीड़ छितरने लगी थी। मैंने गेट के पास ऊँचाई पर के एक कोने में अपने को स्थित किया। वहाँ जल्दी ही मृतक के सगे-सम्बन्धी कतार बाँधे, हाथ जोड़े, आगतों को विदा करने के लिए खड़े हो जाने को थे।
मेरे देखते-देखते परिजनों की आमने-सामने खड़ी कतारों के बीच एक गलियारा जैसा बन गया था, जिसमें से होकर गुजरता हर व्यक्ति मुझे साफ दीख रहा था। भीड़ छँट गयी थी। वह कहीं नहीं थी। जाने कब तिरोहित हो गयी थी।
मैं जैसे ठगी-सी गयी। समझ नहीं पायी कि यह मेरी अवहेलना है या उसके घाव अभी भी हरे हैं।
यह चन्नी का वर्तमान है, जिसमें वह अचानक, इस तरह प्रकट हुई है। चन्नी का एक अतीत भी है, जिसमें एक दुर्घटना है। दुर्घटना ने चन्नी के जीवन की निरन्तरता को काट दिया है। क्या वह अभी भी बीच में बिछी उसी सुरंग में से गुजर रही है ?
चन्नी के अतीत में मैं भी हूँ। उसमें शामिल नहीं हूँ, पर उसके साथ चलते-चलते उसे देख-सुन रही हूँ। अतीत के लड़ते-भिड़ते, लाँघते-फलाँगते दृश्य इस समय मेरे सामने हैं।
मैं और चन्नी स्कूल जा रहे हैं, इकट्ठे। खेतों, खलिहानों पगडण्डियों को लाँघते-फलाँगते। निमौलियाँ बीनते, कच्ची इमली, आम और जामुन बटोरते, हरे छोलिए की झाड़ियाँ उखाड़ते, रहट वाले कुओं पर रुकते, दृश्य को जी-भर निहारते, छल-छल पानी में पैर छपछपाते।
यह सब दृश्य मेरे नये हैं, खूब रोचक और उत्तेजक। चन्नी इन सब चीजों से एकरस है...भीतर तक घुली हुई, आनन्दित।
मेरे पिता चन्नी के कस्बे में जिला विकास अधिकारी के पद पर स्थानान्तरित होकर आये हैं। पिता की उस कस्बे में पोस्टिंग मेरी नागरी समझ को खूब रोमांचित करने वाली है। मैंने यहाँ आकर दसवीं में दाखिला लिया है चन्नी उस कक्षा में एक साल पहले से पढ़ रही हैं। शायद पिछले साल फेल हो चुकी है। वैसे भी वह मुझसे उम्र में बड़ी है।
चन्नी का असली नाम चन्द्रकुमारी गुप्ता है। यह नाम उसकी बुआ ने रखा है। ऐसा चाँद का सा नाम उसकी माँ तो रख ही नहीं सकती थी। ऐसा चन्नी कहती रहती है। अपनी माँ से उसकी बिल्कुल नहीं पटती फिर भी वह हर समय अपनी माँ के राग अलापती रहती है।
हमारा घर अनाज मण्डी में है। चन्नी भी वहीं रहती है। हम दोनों मण्डी के ऊपर बने चौबारों जैसे घरों में आस-पड़ोस में रहते हैं, इसीलिए साथ-साथ स्कूल जाते हैं। मण्डी से स्कूल का फासला डेढ़ मील का है पर इस फासले को छात्रों द्वारा पैदल ही पटाने का वहाँ चलन है।
मण्डी का इतिहास-भूगोल मेरे लिए उतना ही नया है जितना यहाँ की और सब चीजें। दो सदर दरवाजों वाली चौखूँटे आकार वाली विशाल चारदीवारी जिसमें चौबीस घण्टे गहमागहमी मची रहती है। यह गल्ले की आढ़त और अनाज के थोक व्यापार की मण्डी है।
मण्डी का दृश्य कुछ-कुछ ऐसा है। जगह-जगह अनाज की ढेरियाँ, बोरियाँ, मवेशी, खुली और जुती हुई बैलगाड़ियाँ, दुकानों के सामने लटके भीमकाय तराजू, ढेरों व्यापारी मजदूर पट्टेदार गुड़ की भेलियाँ भिनभिन मक्खियाँ तेल-घी के पीपे। चौबीस घण्टे जलेबियाँ छानते एक हलवाई की दुकान मण्डी के बीचोंबीच। एक हैण्डपम्प, एक परोपकारी कुआँ जिससे पानी की गागरें भर-भरकर झीवर ऊपर बने घरों में पहुँचाते हैं। दुकानों की गद्दियों पर स्थापित लाला चौबारों पर चढ़ती उतरती स्त्रियों को कनखियों से ताकते तौलते रहते हैं।
नीले गल्ले की दुकानें हैं, ऊपर घर। नीचे पुरुष हैं, ऊपर स्त्रियाँ, बच्चे। नीचे सब कुछ दृश्य है, ऊपर का सबकुछ अदृश्य। नीचे खड़े होकर देखने पर दीखती हैं लम्बाई में नीचे तक फहरती चुन्नियाँ, साड़ियाँ। या फिर दुकानों के साथ-साथ लगी सीढ़ियों में से अचानक प्रकट होती स्त्रियाँ। स्त्री प्रायः एक सीढ़ी से उतरकर दूसरी सीढ़ी में चढ़ जाती है। वह चादर से इतनी ढकी हुई होती है कि चलता-फिरता लबादा जैसी लगती है। घरों से बाहर जाने-आने का यही एक रास्ता है। जो कोई भी कहीं आता-जाता है, नीचे बैठे लोगों को दिखाई देता है।
चन्नी खूब स्वस्थ है, खूब सुन्दर। नख-शिखवाली सुन्दरता उतनी नहीं जितनी गोलाई-चिकनाई वाली सुन्दरता। खूब कसे गोल गुलाबी गाल, चंचल आँखें, दायीं ओर दन्तपंक्ति के बीच एक उठा दाँत, जो दोनों होठों को अधखुला रहने देता है। इस मुद्रा में चेहरा और ज्यादा सुन्दर लगता है। उसे लगता नहीं कि वह रोज माँ से पिटकर आती है। सिर को ढाँके रखने के लिए पल-पल दुपट्टे तक पहुँचते उसके हाथ, सदा दिखाई देते रहते हैं। उसके नाखूनों पर झाँकते चिकनाई के निशान उसके घर की कहानी कहते हैं। हर समय सिर ढँकने और गले के पास दुपट्टे को दोनों छोरों से पकड़े रहने की मजबूरी उसकी नहीं, उस क़स्बे में रहने की है जहाँ ऐसा ही लड़कीपन चाहा और सराहा जाता है।
खेतों, पगडण्डियों, फसलों, कुओं से बतियाने और दोस्ती करने का ढंग मुझे चन्नी ने ही सिखाया था। मण्डी का सदर दरवाजा छोड़कर सड़क पर आते ही वह कहीं से एक सण्टी तोड़ लेती और ईख की खड़ी उठान को छेड़ती, झकझोरती, गाती जाती। उसके इस जीवन्त खिलन्दड़ेपन को मैं मुँह-बाये देखती। वातावरण से इतना एकरस, इतना तन्मय देखकर यह अन्दाजा लगाना कठिन होता कि वह आज भी माँ से पिटकर आयी हैं। वह लगभग रोज ही अपनी माँ से पिटती है, यह सूचना भी चन्नी की ही दी हुई होती। बकौल उसके उसकी माँ को उससे वैर है, क्योंकि चन्नी के पैदा होते ही उसके ऊपर वाला भाई हैजे से मर गया था। माँ के हिसाब से यह घर में चन्नी के अशुभ पदार्पण की छाया है।
स्कूल से वापसी पर ईख का खेत पार करते ही सरदारी का कुआँ दिखाई देने लगता। कुएँ को देखते ही चन्नी का तेवर बदल जाता। कन्धे से बस्ता उतारकर वह एक कोने में पटक देती। सिर से दुपट्टा उतारकर कमर में बाँध लेती। सैण्डिल खोलती, जूतों की उस जोड़ी को अपने नीचे रखकर पानी की निकासी के लिए बनी मेंड़, के किनारे धसककर बैठ जाती। उन छोटी-छोटी नालियों में ठण्डा पारदर्शी पानी बहता होता, वह अद्भुत मनोहारी दृश्य होता। बैलों की जोड़ी गोल-गोल घूमती रहट से पानी खिंचता, टीन के डिब्बे गुडुप-गुडुप पानी उलटते और नालियों की राह पानी खेतों को चल निकलता। चन्नी अपना आपा भूलकर बहते पानी में पैर डाले बैठी रहती। स्कूल के टिफिन का आधा बचाया गया खाना निकालकर वह बगल में रख लेती। ऐसा लगभग रोज-रोज होता।
मेरा बेचैन होना चन्नी के चैन में होने के साथ-साथ चलता। चन्नी के कुरते पर फैलते कीचड़ के निशान मुझे बेतरह परेशान करते, तिस पर घर पहुँचने में देरी का डर।
‘‘चन्नी, उठ न, जल्दी चल, नहीं तो तेरी माँ मारेगी।’’
‘‘चुप बैठ’’ पेड़ों पर बैठे तोतों को देखते चन्नी मुझे झिड़क देती-‘‘बताया नहीं था, मेरी माँ तो पूरी पागल है। जब मुझे पीटने लगती है तो उसका झोंटा खुल जाता है और फिर तो वह एकदम पागल लगती है। मैं तो चुड़ैलों जैसा उसका चेहरा देखती रहती हूँ। पिट रही हूँ इस बात की तो मुझे याद ही नहीं रहती।’’
ऐसी बातें मैंने कभी सुनी नहीं थीं, ऐसी माँ भी मैंने कभी देखी नहीं थी। उसकी माँ की मू्र्ति का खाका मैंने घर जाकर अपनी माँ के सामने खींचा था। सोचा था खुश हो जाएगी। तुलना में अपने को अच्छा मानेगी पर माँ थी कि चिन्ता में पड़ गयी थी। पिताजी से खुसफुस में लग गयी।
नतीजा यह कि दशहरे की छुट्टी के बाद मेरे स्कूल जाने-लौटने के लिए मैकू का साइकिल रिक्शा बाँध दिया गया। मैकू, घर वालों का मुँह लगा रिक्शा वाला तो क्या पूरा गार्जियन था। पल-पल की खोज-खबर रखता। चन्नी का और मेरा साथ इस तरह छूट गया। मुझे खूब बुरा लगा। चन्नी के चलते मैं कोई दूसरी दुनिया देख रही थी। मुझे लगा। शायद चन्नी को भी इतना ही बुरा लगा होगा, पर तब मुझे मालूम नहीं था कि चन्नी के मन में दूसरों के दर्दों के लिए जगह नहीं है।
हो सकता है मेरा साथ छूट जाने से चन्नी को सुविधा ही मिली हो। नहीं तो क्यों सरदारी का ही कुआँ ? क्यों देर ? क्यों बचाया हुआ खाना ? क्यों वैसी तन्मयता और अतिरेक कि देह को पड़ती मार, मार ही न लगे। पहुँचे हुए लोगों की तरह अपने से अलग होकर वह अपनी माँ की त्वरा देखती रहे। कस्बे के इतिहास-भूगोल के चलते हो सकता है, यह दयालु-कृपालु कुआँ ही चन्नी नरेन्द्र के लिए असली ‘लोकेल’ रहा हो।
फरवरी और अन्त का दिन। लीप ईयर की पूँछ लगी होने के कारण वह दिन सदा याद रह जाने जैसा है। वैसे भी उस दिन मेरे छोटे भाई का जन्मदिन मनाया जाना था।
मण्डी की ऊँची दीवारों में उगते सवेरे को एक उन्मादी आर्तनाद ने जगाया था। हवा को लपेटती दारुण जैसी चीखें। चीखों का पीछे करते चारदीवारी में धीरे-धीरे हो हल्ला गाढ़ा हुआ था। पता लगा अनाज के सबसे बड़े व्यापारी चौधरी चतुरसिंह चन्देल के लड़के नरेन्द्र और घी-तेल के सबसे बड़े आढ़ती गोकुलचन्द्र गुप्ता की लड़की चन्नी ने विष पीकर आत्महत्या कर ली है।
रेशम का कुर्ता पहनकर मरे नरेन्द्र की ऐंठी हुई मुट्ठी में एक मुड़ा-तुड़ा पत्र पाया गया था। उसमें जो तफसील दर्ज थी वह कुछ-कुछ इस अर्थ की थी-प्रेम की राह में रोड़े अटकाने वाले पिता को दण्ड और अपने दोनों की एक साथ मुक्ति। आगे फिर मुक्ति की योजना का खुलासा किया गया था कि कैसे रात को गुलाबी चुन्नी ओढ़कर चन्नी भी, अपने घर में ठीक उसी समय, जहर खाएगी पर आखिरी आरजू यह है कि अर्थियाँ उठायीं जाएँ एक साथ। मण्डी के सदर दरवाजे से दोनों अर्थियाँ साथ-साथ निकलें, इकलौते की इच्छा मानकर।
चौधरी चतुर सिंह चन्देल की संस्कारी अहंकारी उठान पर ऐसा हिंसक वार। वह भी अपने बेटे द्वारा। बेटा सभी इकलौता जिसे इकलौता ही रहना था क्योंकि चौधराइन की जनाना क्षमताओं में चिकित्सा की गलत दखलअन्दाजी से खोट पैदा हो गया था। पन्तनगर विश्वविद्यालय से कृषिविज्ञान में ऊँची डिग्री को लेकर आते बेटे के चर्चे अभी तक लोगों की जुबान पर ताजा थे। सुना था इस मौके पर चौधरी ने सोने की मूठ वाली एक छड़ी नरेन्द्र को दी थी और रिश्तेदारों में गिन्नियाँ बाँटी थीं।
वह थी-चन्नी। माथे की ढलुवाँ गोलाई को काटती सुघड़ नाक, भरे-भरे होठ। दन्तपंक्ति में दायें को अलग से उठा हुआ एक दाँत, जो दोनों होठों के मिलाप को बाधित करता था। चेहरा पहले से ज्यादा भरपूर, माथे पर बड़ी-सी बिन्दी, जिसके चलते सारा मुख-मण्डल नया-सा लग रहा था। उससे लगकर जो व्यक्ति बैठा था शायद उसका पति होगा।
मैंने उमगकर अपनी बाँह उठायी। सिर के ऊपर ले जाकर हिलायी, उसे सत्कारते हुए। आँख मिली थी। पहचान चटक हुई थी। पर वह साझा क्षण उसी निमिष टूट गया था। मुझे लगा उसी ने टूट जाने दिया है। मुँह फेर लिया है।
अविश्वास को भ्रम का सहारा दे देना सहज लगा। हवन के समाप्त होने की प्रतीक्षा की।
‘ओउम अग्नये नय सपथा’ पण्डितजी उपासना मन्त्रों के निकट पहुँच रहे थे। अपनी दोनों फैली हथेलियाँ ऊपर को उछाल रहे थे। लोगों को उपासना मन्त्रों के उच्चारण में सम्मिलित होने को उकसा रहे थे।
अनुष्ठान के अन्त तक आते तो वातावरण काफी सामूहिक और समावेशी हो चला था। मृत्यु के प्रसंग की प्रगाढ़ता पिघल रही थी।
अब, जेठे को पगड़ी पहनाने की रस्म, फिर दान-दक्षिणा, फिर सामूहिक रूप से उच्चारा जाता शान्ति पाठ। बन्द आँखें। अपने-अपने आसनों पर खड़े हो चुके लोग।
‘‘ओउम् शान्तिः....शान्ति:....शान्ति:....ओउम्।’’ ओंकार की पिछड़ती लय अभी डूबी भी नहीं थी कि मैं भीड़ काटकर सहन के उसी हिस्से में पहुँच गयी थी। वह वहाँ नहीं थी। वह कहीं भी नहीं थी। मेरी अधीरता ने उसे लगभग हर सम्भव जगह ढूँढ़ा।
भीड़ छितरने लगी थी। मैंने गेट के पास ऊँचाई पर के एक कोने में अपने को स्थित किया। वहाँ जल्दी ही मृतक के सगे-सम्बन्धी कतार बाँधे, हाथ जोड़े, आगतों को विदा करने के लिए खड़े हो जाने को थे।
मेरे देखते-देखते परिजनों की आमने-सामने खड़ी कतारों के बीच एक गलियारा जैसा बन गया था, जिसमें से होकर गुजरता हर व्यक्ति मुझे साफ दीख रहा था। भीड़ छँट गयी थी। वह कहीं नहीं थी। जाने कब तिरोहित हो गयी थी।
मैं जैसे ठगी-सी गयी। समझ नहीं पायी कि यह मेरी अवहेलना है या उसके घाव अभी भी हरे हैं।
यह चन्नी का वर्तमान है, जिसमें वह अचानक, इस तरह प्रकट हुई है। चन्नी का एक अतीत भी है, जिसमें एक दुर्घटना है। दुर्घटना ने चन्नी के जीवन की निरन्तरता को काट दिया है। क्या वह अभी भी बीच में बिछी उसी सुरंग में से गुजर रही है ?
चन्नी के अतीत में मैं भी हूँ। उसमें शामिल नहीं हूँ, पर उसके साथ चलते-चलते उसे देख-सुन रही हूँ। अतीत के लड़ते-भिड़ते, लाँघते-फलाँगते दृश्य इस समय मेरे सामने हैं।
मैं और चन्नी स्कूल जा रहे हैं, इकट्ठे। खेतों, खलिहानों पगडण्डियों को लाँघते-फलाँगते। निमौलियाँ बीनते, कच्ची इमली, आम और जामुन बटोरते, हरे छोलिए की झाड़ियाँ उखाड़ते, रहट वाले कुओं पर रुकते, दृश्य को जी-भर निहारते, छल-छल पानी में पैर छपछपाते।
यह सब दृश्य मेरे नये हैं, खूब रोचक और उत्तेजक। चन्नी इन सब चीजों से एकरस है...भीतर तक घुली हुई, आनन्दित।
मेरे पिता चन्नी के कस्बे में जिला विकास अधिकारी के पद पर स्थानान्तरित होकर आये हैं। पिता की उस कस्बे में पोस्टिंग मेरी नागरी समझ को खूब रोमांचित करने वाली है। मैंने यहाँ आकर दसवीं में दाखिला लिया है चन्नी उस कक्षा में एक साल पहले से पढ़ रही हैं। शायद पिछले साल फेल हो चुकी है। वैसे भी वह मुझसे उम्र में बड़ी है।
चन्नी का असली नाम चन्द्रकुमारी गुप्ता है। यह नाम उसकी बुआ ने रखा है। ऐसा चाँद का सा नाम उसकी माँ तो रख ही नहीं सकती थी। ऐसा चन्नी कहती रहती है। अपनी माँ से उसकी बिल्कुल नहीं पटती फिर भी वह हर समय अपनी माँ के राग अलापती रहती है।
हमारा घर अनाज मण्डी में है। चन्नी भी वहीं रहती है। हम दोनों मण्डी के ऊपर बने चौबारों जैसे घरों में आस-पड़ोस में रहते हैं, इसीलिए साथ-साथ स्कूल जाते हैं। मण्डी से स्कूल का फासला डेढ़ मील का है पर इस फासले को छात्रों द्वारा पैदल ही पटाने का वहाँ चलन है।
मण्डी का इतिहास-भूगोल मेरे लिए उतना ही नया है जितना यहाँ की और सब चीजें। दो सदर दरवाजों वाली चौखूँटे आकार वाली विशाल चारदीवारी जिसमें चौबीस घण्टे गहमागहमी मची रहती है। यह गल्ले की आढ़त और अनाज के थोक व्यापार की मण्डी है।
मण्डी का दृश्य कुछ-कुछ ऐसा है। जगह-जगह अनाज की ढेरियाँ, बोरियाँ, मवेशी, खुली और जुती हुई बैलगाड़ियाँ, दुकानों के सामने लटके भीमकाय तराजू, ढेरों व्यापारी मजदूर पट्टेदार गुड़ की भेलियाँ भिनभिन मक्खियाँ तेल-घी के पीपे। चौबीस घण्टे जलेबियाँ छानते एक हलवाई की दुकान मण्डी के बीचोंबीच। एक हैण्डपम्प, एक परोपकारी कुआँ जिससे पानी की गागरें भर-भरकर झीवर ऊपर बने घरों में पहुँचाते हैं। दुकानों की गद्दियों पर स्थापित लाला चौबारों पर चढ़ती उतरती स्त्रियों को कनखियों से ताकते तौलते रहते हैं।
नीले गल्ले की दुकानें हैं, ऊपर घर। नीचे पुरुष हैं, ऊपर स्त्रियाँ, बच्चे। नीचे सब कुछ दृश्य है, ऊपर का सबकुछ अदृश्य। नीचे खड़े होकर देखने पर दीखती हैं लम्बाई में नीचे तक फहरती चुन्नियाँ, साड़ियाँ। या फिर दुकानों के साथ-साथ लगी सीढ़ियों में से अचानक प्रकट होती स्त्रियाँ। स्त्री प्रायः एक सीढ़ी से उतरकर दूसरी सीढ़ी में चढ़ जाती है। वह चादर से इतनी ढकी हुई होती है कि चलता-फिरता लबादा जैसी लगती है। घरों से बाहर जाने-आने का यही एक रास्ता है। जो कोई भी कहीं आता-जाता है, नीचे बैठे लोगों को दिखाई देता है।
चन्नी खूब स्वस्थ है, खूब सुन्दर। नख-शिखवाली सुन्दरता उतनी नहीं जितनी गोलाई-चिकनाई वाली सुन्दरता। खूब कसे गोल गुलाबी गाल, चंचल आँखें, दायीं ओर दन्तपंक्ति के बीच एक उठा दाँत, जो दोनों होठों को अधखुला रहने देता है। इस मुद्रा में चेहरा और ज्यादा सुन्दर लगता है। उसे लगता नहीं कि वह रोज माँ से पिटकर आती है। सिर को ढाँके रखने के लिए पल-पल दुपट्टे तक पहुँचते उसके हाथ, सदा दिखाई देते रहते हैं। उसके नाखूनों पर झाँकते चिकनाई के निशान उसके घर की कहानी कहते हैं। हर समय सिर ढँकने और गले के पास दुपट्टे को दोनों छोरों से पकड़े रहने की मजबूरी उसकी नहीं, उस क़स्बे में रहने की है जहाँ ऐसा ही लड़कीपन चाहा और सराहा जाता है।
खेतों, पगडण्डियों, फसलों, कुओं से बतियाने और दोस्ती करने का ढंग मुझे चन्नी ने ही सिखाया था। मण्डी का सदर दरवाजा छोड़कर सड़क पर आते ही वह कहीं से एक सण्टी तोड़ लेती और ईख की खड़ी उठान को छेड़ती, झकझोरती, गाती जाती। उसके इस जीवन्त खिलन्दड़ेपन को मैं मुँह-बाये देखती। वातावरण से इतना एकरस, इतना तन्मय देखकर यह अन्दाजा लगाना कठिन होता कि वह आज भी माँ से पिटकर आयी हैं। वह लगभग रोज ही अपनी माँ से पिटती है, यह सूचना भी चन्नी की ही दी हुई होती। बकौल उसके उसकी माँ को उससे वैर है, क्योंकि चन्नी के पैदा होते ही उसके ऊपर वाला भाई हैजे से मर गया था। माँ के हिसाब से यह घर में चन्नी के अशुभ पदार्पण की छाया है।
स्कूल से वापसी पर ईख का खेत पार करते ही सरदारी का कुआँ दिखाई देने लगता। कुएँ को देखते ही चन्नी का तेवर बदल जाता। कन्धे से बस्ता उतारकर वह एक कोने में पटक देती। सिर से दुपट्टा उतारकर कमर में बाँध लेती। सैण्डिल खोलती, जूतों की उस जोड़ी को अपने नीचे रखकर पानी की निकासी के लिए बनी मेंड़, के किनारे धसककर बैठ जाती। उन छोटी-छोटी नालियों में ठण्डा पारदर्शी पानी बहता होता, वह अद्भुत मनोहारी दृश्य होता। बैलों की जोड़ी गोल-गोल घूमती रहट से पानी खिंचता, टीन के डिब्बे गुडुप-गुडुप पानी उलटते और नालियों की राह पानी खेतों को चल निकलता। चन्नी अपना आपा भूलकर बहते पानी में पैर डाले बैठी रहती। स्कूल के टिफिन का आधा बचाया गया खाना निकालकर वह बगल में रख लेती। ऐसा लगभग रोज-रोज होता।
मेरा बेचैन होना चन्नी के चैन में होने के साथ-साथ चलता। चन्नी के कुरते पर फैलते कीचड़ के निशान मुझे बेतरह परेशान करते, तिस पर घर पहुँचने में देरी का डर।
‘‘चन्नी, उठ न, जल्दी चल, नहीं तो तेरी माँ मारेगी।’’
‘‘चुप बैठ’’ पेड़ों पर बैठे तोतों को देखते चन्नी मुझे झिड़क देती-‘‘बताया नहीं था, मेरी माँ तो पूरी पागल है। जब मुझे पीटने लगती है तो उसका झोंटा खुल जाता है और फिर तो वह एकदम पागल लगती है। मैं तो चुड़ैलों जैसा उसका चेहरा देखती रहती हूँ। पिट रही हूँ इस बात की तो मुझे याद ही नहीं रहती।’’
ऐसी बातें मैंने कभी सुनी नहीं थीं, ऐसी माँ भी मैंने कभी देखी नहीं थी। उसकी माँ की मू्र्ति का खाका मैंने घर जाकर अपनी माँ के सामने खींचा था। सोचा था खुश हो जाएगी। तुलना में अपने को अच्छा मानेगी पर माँ थी कि चिन्ता में पड़ गयी थी। पिताजी से खुसफुस में लग गयी।
नतीजा यह कि दशहरे की छुट्टी के बाद मेरे स्कूल जाने-लौटने के लिए मैकू का साइकिल रिक्शा बाँध दिया गया। मैकू, घर वालों का मुँह लगा रिक्शा वाला तो क्या पूरा गार्जियन था। पल-पल की खोज-खबर रखता। चन्नी का और मेरा साथ इस तरह छूट गया। मुझे खूब बुरा लगा। चन्नी के चलते मैं कोई दूसरी दुनिया देख रही थी। मुझे लगा। शायद चन्नी को भी इतना ही बुरा लगा होगा, पर तब मुझे मालूम नहीं था कि चन्नी के मन में दूसरों के दर्दों के लिए जगह नहीं है।
हो सकता है मेरा साथ छूट जाने से चन्नी को सुविधा ही मिली हो। नहीं तो क्यों सरदारी का ही कुआँ ? क्यों देर ? क्यों बचाया हुआ खाना ? क्यों वैसी तन्मयता और अतिरेक कि देह को पड़ती मार, मार ही न लगे। पहुँचे हुए लोगों की तरह अपने से अलग होकर वह अपनी माँ की त्वरा देखती रहे। कस्बे के इतिहास-भूगोल के चलते हो सकता है, यह दयालु-कृपालु कुआँ ही चन्नी नरेन्द्र के लिए असली ‘लोकेल’ रहा हो।
फरवरी और अन्त का दिन। लीप ईयर की पूँछ लगी होने के कारण वह दिन सदा याद रह जाने जैसा है। वैसे भी उस दिन मेरे छोटे भाई का जन्मदिन मनाया जाना था।
मण्डी की ऊँची दीवारों में उगते सवेरे को एक उन्मादी आर्तनाद ने जगाया था। हवा को लपेटती दारुण जैसी चीखें। चीखों का पीछे करते चारदीवारी में धीरे-धीरे हो हल्ला गाढ़ा हुआ था। पता लगा अनाज के सबसे बड़े व्यापारी चौधरी चतुरसिंह चन्देल के लड़के नरेन्द्र और घी-तेल के सबसे बड़े आढ़ती गोकुलचन्द्र गुप्ता की लड़की चन्नी ने विष पीकर आत्महत्या कर ली है।
रेशम का कुर्ता पहनकर मरे नरेन्द्र की ऐंठी हुई मुट्ठी में एक मुड़ा-तुड़ा पत्र पाया गया था। उसमें जो तफसील दर्ज थी वह कुछ-कुछ इस अर्थ की थी-प्रेम की राह में रोड़े अटकाने वाले पिता को दण्ड और अपने दोनों की एक साथ मुक्ति। आगे फिर मुक्ति की योजना का खुलासा किया गया था कि कैसे रात को गुलाबी चुन्नी ओढ़कर चन्नी भी, अपने घर में ठीक उसी समय, जहर खाएगी पर आखिरी आरजू यह है कि अर्थियाँ उठायीं जाएँ एक साथ। मण्डी के सदर दरवाजे से दोनों अर्थियाँ साथ-साथ निकलें, इकलौते की इच्छा मानकर।
चौधरी चतुर सिंह चन्देल की संस्कारी अहंकारी उठान पर ऐसा हिंसक वार। वह भी अपने बेटे द्वारा। बेटा सभी इकलौता जिसे इकलौता ही रहना था क्योंकि चौधराइन की जनाना क्षमताओं में चिकित्सा की गलत दखलअन्दाजी से खोट पैदा हो गया था। पन्तनगर विश्वविद्यालय से कृषिविज्ञान में ऊँची डिग्री को लेकर आते बेटे के चर्चे अभी तक लोगों की जुबान पर ताजा थे। सुना था इस मौके पर चौधरी ने सोने की मूठ वाली एक छड़ी नरेन्द्र को दी थी और रिश्तेदारों में गिन्नियाँ बाँटी थीं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i