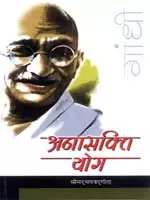|
विविध >> अनासक्ति योग अनासक्ति योगमहात्मा गाँधी
|
198 पाठक हैं |
|||||||
अनासक्ति योग
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में कई वर्ष तक अनासक्ति योग का
पालन किया। उन्होंने गीता के श्लोकों का सरल अनुवाद करके
‘अनासक्ति
योग’ का नाम दिया। अपने अनुभवों को लोगों में बाँटा और इसके
महत्व
को समझाया था। इसमें उन्होंने आश्रम वासियों के जीवन दर्शन का भी उल्लेख
किया है। गांधी जी ने अनासक्ति योग की उपनिषदों का सार बताया है।
भारत की धरती ने एक ऐसा महान मानव पैदा किया जिसने न केवल भारत की राजनीति का नक्शा बदल दिया अपितु विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम की उस अजेय शक्ति के दर्शन कराए जिसके लिए ऐसा या गौतम बुद्घ का स्मरण किया जाता है। गांधी जी का धर्म समूची मानव-जाति के लिए कल्याणकारी था। उन्होंने स्वयं को दरिद्र नारायण का प्रतिनिधि माना। गांधी जी का विश्वास था कि भारत का उत्थान गाँवों की उन्नति से ही होगा। उनके लिए सत्य से बढ़कर कोई कर्त्तव्य नहीं था। गांधी जी संसार की अमर विभूति हैं।
भारत की धरती ने एक ऐसा महान मानव पैदा किया जिसने न केवल भारत की राजनीति का नक्शा बदल दिया अपितु विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम की उस अजेय शक्ति के दर्शन कराए जिसके लिए ऐसा या गौतम बुद्घ का स्मरण किया जाता है। गांधी जी का धर्म समूची मानव-जाति के लिए कल्याणकारी था। उन्होंने स्वयं को दरिद्र नारायण का प्रतिनिधि माना। गांधी जी का विश्वास था कि भारत का उत्थान गाँवों की उन्नति से ही होगा। उनके लिए सत्य से बढ़कर कोई कर्त्तव्य नहीं था। गांधी जी संसार की अमर विभूति हैं।
प्रस्तावना
1
जैसे स्वामी आनंद आदि मित्रों के प्रेम के वश होकर मैंने सत्य के प्रयोगों
के लिए आत्मकथा का लिखना आरंभ किया था, वैसे गीता का अनुवाद भी। स्वामी
आनंद ने असहयोग के जमाने में मुझसे कहा था-‘आप गीता का अर्थ
करते
हैं, वह अर्थ तभी समझ में आ सकता है, जब आप एक बार समूची गीता का अनुवाद
कर जाएँ और उसके ऊपर जो टीका करने हो, वह करें और वह संपूर्ण एक बार पढ़
जाएँ। फुटकर श्लोकों में से अहिसादि का प्रतिपादन मुझे तो ठीक नहीं लगता
है।’ फिर मैं जेल गया। वहाँ तो गीता का अध्ययन कुछ अधिक गहराई
से
करने का मौक़ा मिला। लोकमान्य का ज्ञान का भंडार पढ़ा। उन्होंने ही पहले
मुझे मराठी, हिंदी और गुजराती अनुवाद प्रेमपूर्वक भेजे थे और सिफ़ारिश की
थी कि मराठी न पढ़ सकूं तो गुजराती अवश्य पढूँ। जेल के बाहर तो उसे न पढ़
पाया, पर जेल में गुजराती अनुवाद पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद गीता के संबंध
में अधिक पढ़ने की इच्छा हुई गीता-संबंधी अनेक ग्रंथ उलटे-पलटे।
मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नाल्ड के पद्य-अनुवाद से सन् 1888-89 में प्राप्त हुआ। उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे, उन्हें पढ़ गया; परंतु ऐसी पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद जनता के सामने ऱखने का बिल्कुल अधिकार नहीं देती। इसके सिवा मेरा संस्कृत-ज्ञान अल्प है, गुजराती का ज्ञान विद्वता के विचार से कुछ नहीं है। तब मैंने अनुवाद करने की धृष्टता क्यों की ?
गीता को मैंने जिस प्रकार समझा है, उस प्रकार का आचरण करने का मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियों का बराबर प्रयास है। गीता हमारे लिए आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसके अनुवाद आचरण में निष्फलता रोज आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है इस निष्फलता में सफलता की फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है। यह नन्हा-सा जन-समुदाय जिस अर्थ को आचार में परिणत करने का प्रयत्न करता है, वह इस अनुवाद में है।
इसके सिवा स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र-सरीखे, जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कृत में गीता समझने का समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परंतु जिन्हे गीता रूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्हीं के लिए इस अनुवाद की कल्पना है।1 गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियों को, मेरे पास जो कुछ पूँजी हो वह, दे जाने की मुझे सदा भारी अभिलाषा रही है। मैं यह चाहता हूँ अवश्य कि आज गंदे साहित्य का जो प्रवाह जोरों से जारी है, उस समय में हिन्दू-धर्म में अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रंथ का सरल अनुवाद गुजराती जनता को मिले और उसमें से वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे।
इस अभिलाषा में दूसरे गुजराती अनुवादों की अवहेलना नहीं है। उन सबका स्थान भले ही हो; पर उनके पीछे उनके अनुवादों का आचार-रूपी अनुभव का दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। इस अनुवाद के पीछे अड़तीस वर्ष के आचार के प्रयत्न का दावा है। इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि प्रत्येक गुजराती भाई और बहन, जिन्हें धर्म को आचरण में लाने की इच्छा है, इसे पढ़े, विचारें और इसमें से शक्ति प्राप्त करें।
इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है। मेरा संस्कृत-ज्ञान बहुत अधूरा होने के कारण शब्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नही हो सकता था, अतः इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोरीलाल मशरूवाला ने देख लिया है।
मुझे गीता का प्रथम परिचय एडविन आर्नाल्ड के पद्य-अनुवाद से सन् 1888-89 में प्राप्त हुआ। उससे गीता का गुजराती अनुवाद पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई और जितने अनुवाद हाथ लगे, उन्हें पढ़ गया; परंतु ऐसी पढ़ाई मुझे अपना अनुवाद जनता के सामने ऱखने का बिल्कुल अधिकार नहीं देती। इसके सिवा मेरा संस्कृत-ज्ञान अल्प है, गुजराती का ज्ञान विद्वता के विचार से कुछ नहीं है। तब मैंने अनुवाद करने की धृष्टता क्यों की ?
गीता को मैंने जिस प्रकार समझा है, उस प्रकार का आचरण करने का मेरा और मेरे साथ रहनेवाले कई साथियों का बराबर प्रयास है। गीता हमारे लिए आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसके अनुवाद आचरण में निष्फलता रोज आती है, पर वह निष्फलता हमारा प्रयत्न रहते हुए है इस निष्फलता में सफलता की फूटती हुई किरणों की झलक दिखाई देती है। यह नन्हा-सा जन-समुदाय जिस अर्थ को आचार में परिणत करने का प्रयत्न करता है, वह इस अनुवाद में है।
इसके सिवा स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र-सरीखे, जिन्हें अक्षरज्ञान थोड़ा ही है, जिन्हें मूल संस्कृत में गीता समझने का समय नहीं है, इच्छा नहीं है, परंतु जिन्हे गीता रूपी सहारे की आवश्यकता है, उन्हीं के लिए इस अनुवाद की कल्पना है।1 गुजराती भाषा का मेरा ज्ञान कम होने पर भी उसके द्वारा गुजरातियों को, मेरे पास जो कुछ पूँजी हो वह, दे जाने की मुझे सदा भारी अभिलाषा रही है। मैं यह चाहता हूँ अवश्य कि आज गंदे साहित्य का जो प्रवाह जोरों से जारी है, उस समय में हिन्दू-धर्म में अद्वितीय माने जानेवाले इस ग्रंथ का सरल अनुवाद गुजराती जनता को मिले और उसमें से वह उस प्रवाह का सामना करने की शक्ति प्राप्त करे।
इस अभिलाषा में दूसरे गुजराती अनुवादों की अवहेलना नहीं है। उन सबका स्थान भले ही हो; पर उनके पीछे उनके अनुवादों का आचार-रूपी अनुभव का दावा हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। इस अनुवाद के पीछे अड़तीस वर्ष के आचार के प्रयत्न का दावा है। इसलिए मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि प्रत्येक गुजराती भाई और बहन, जिन्हें धर्म को आचरण में लाने की इच्छा है, इसे पढ़े, विचारें और इसमें से शक्ति प्राप्त करें।
इस अनुवाद में मेरे साथियों की मेहनत मौजूद है। मेरा संस्कृत-ज्ञान बहुत अधूरा होने के कारण शब्दार्थ पर मुझे पूरा विश्वास नही हो सकता था, अतः इतने भर के लिए इस अनुवाद को विनोबा, काका कालेलकर, महादेव देसाई और किशोरीलाल मशरूवाला ने देख लिया है।
2
अब गीता के अर्थ पर आता हूँ।
सन् 1888-89 में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरंतर होते रहनेवाले द्वंद्व-युद्ध का ही वर्णन है। मानुषी योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरण धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गई। महाभारत पढ़ने के बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत-ग्रंथ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इसके प्रबल प्रमाण आदिपर्व में ही है। पात्रों की अमानुषी और अतिमानुषी उत्पति का वर्णन करके व्यास भगवान् ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हों, परंतु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान् ने केवल धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है।
महाभारतकार ने भौतिक युद्घ की आवश्यकता नहीं, उसकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेता ने रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुख के सिवा और कुछ नहीं करने दिया।
1. गांधी जी का अनुवाद गुजराती में है। यह उसी का हिंदी-रूपांतर है।
इस महाग्रंथ में गीता शिरोमणि रूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण सिखाता है। स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई संबंध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणों में ही मुझे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक झगड़ों के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना संभव नहीं है।
गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्ध संपूर्ण ज्ञान हैं। पंरतु काल्पनिक हैं। यहाँ कृष्ण नाम के अवतारी पुरुष का निषेध नहीं है। केवल संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, संपूर्णावतार का आरोपण पीछे से हुआ है।
अवतार से तात्पर्य है शरीरघारी पुरुष विशेष। जीवमात्र ईश्वर के अवतार है, परंतु लौकिक भाषा में सबकों हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान् है, उसे भावी प्रजा अवताररूप से पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न ईश्वर के बड़प्पन में कमी आती है, न उसमें सत्य को आघात पहुँचता है। ‘आदम खुदा नहीं; लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।’ जिसमें धर्म-जागृति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावतार है। इस विचार-श्रेणी से कृष्णरूपी संपूर्णावतार आज हिंदू-धर्म में साम्राज्य भोग रहा है।
यह दृश्य मनु्ष्य की अंतिम सद्भिलाषा का सूचक है। मनुष्य को ईश्वर-रूप हुए बिना चैन नहीं, पड़ता, शांति नहीं मिलती। ईश्वररूप होने के प्रयत्न का नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन सब धर्म-ग्रंथों का विषय है वैसे ही गीता का भी है। पर गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची, वरन् आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का आशय है। जो चीज हिंदू धर्म-ग्रंथों में छिट-पुट दिखाई देती हैं, उसे गीता ने अनेक रुपों में, अनेक शब्दों में, पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है।
वह अद्वितीय उपाय है ‘कर्मफलत्याग।’
इस मध्यबिंदु के चारों ओर गीता की सारी सजावट है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि इसके आसपास तारा-मंडल-रूप में सज गए है। जहाँ देह है, वहाँ कर्म तो है ही। उससे कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभु का मंदिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मों ने प्रतिपादित किया है; परंतु कर्ममात्र में कुछ दोष तो हैं ही, मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब कर्मबंधन में से अर्थात् दोष-स्पर्श में से कैसे छुटकारा हो ? इसका जवाब गीताजी ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है-‘निष्काम कर्म से, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफल त्याग करके, सब कर्मों को कृष्णार्पण करके, अर्थात् मन, वचन और काया को ईश्वर में होम करके।’
पर निष्कामता, कर्मफल-त्याग कहने-भर से नहीं हो जाता। यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदय-मंथन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान तो बहुतेरे पंडित पाते हैं।
वेदादि उन्हें कंठस्थल होते हैं, उनमें से अधिकांश भोगादि में लगे-लिपटे रहते हैं। ज्ञान का अतिरेक शुष्क पांडित्य के रूप में न हो जाए, इस ख्याल से गीताकार ने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भक्ति का ज्ञान हानिकार है। इसलिए कहा गया-‘भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जाएगा।’ पर भक्ति तो ‘सिर का सौदा’ है, इसलिए गीताकार ने भक्ति के लक्षण स्थितप्रज्ञ के-से बतलाए हैं।
तात्पर्य, गीता की भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। गीता में बताए उपचार का बाह्य चेष्टा या क्रिया के साथ कम-से-कम संबंध हैं, माला-तिलक, अर्ध्यादि साधन भले भी भक्त बरते, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं। जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो करूणा का भंडार है और ममता-रहित हैं, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दुःख शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिए हैं, जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं रखता, जो शुभाशुभ का प्याग करनेवाला है, जो शत्रु-मित्र पर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान-अपमान समान है, जिस स्तुति से खुशी नहीं होती और निदा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है। यह भक्ति आसक्त स्त्री-पुरुषों में संभव नहीं है।
इससे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे रुपए के बदले में ज़हर ख़रीदा जा सकता है और भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्ति के बदले बंधन भी लाया जा सके और मोक्ष भी, यह संभव नहीं हैं। यहाँ तो साधन और साध्य, बिल्कुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की पराकाष्ठा जो है, वही मोक्ष है और गीता के मोक्ष का अर्थ परम शांति हैं।
किंतु ऐसे ज्ञान और भक्ति को कर्म-फल-त्याग की कसौटी पर चढ़ना ठहरा। लौकिक कल्पना में शुष्क पंडित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम करने को नहीं रहता। हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्म-बंधन है। यज्ञशून्य जहाँ ज्ञानी गिना जाए वहाँ लोटा उठाने जैसी तुच्छ लौकिक क्रिया को स्थान ही कैसे मिल सकता है ?
लौकिक कल्पना में भक्त से मतलब है बाह्याचारी2, माला लेकर जप करनेवाला। सेवा-कर्म करते भी उसकी माला में विक्षेप पड़ता है। इसलिए वह खाने-पीने आदि भोग-भोगने के समय ही माला को हाथ से छोड़ता हैं, चक्की चलाने या रोगी की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए कभी नहीं छोड़ता।
इन दोनों वर्गों को गीता ने साफ़ तौर से कह दिया-‘कर्म बिना किसी ने सिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कर्म द्वारा ज्ञानी हुए। यदि मैं भी आलस्य रहित
2. जो बाह्याचार मे लीन रहता है और शुद्ध भाव से मानता है कि यही भक्ति हैं।
होकर कर्म न करता रहूँ तो इन श्लोकों का नाश हो जाए।’ तो फिर लोगों के लिए पूछना ही क्या रह जाता है ?
परंतु एक ओर से कर्ममात्र बंधनरूप हैं, यह निर्विवाद है। दूसरी ओर से देही इच्छा-अनिच्छा से भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएँ कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधनमुक्त कैसे रहे ? जहाँ तक मुझे मालूम है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है, वैसे दूसरे किसी भी धर्म-ग्रंथ ने नहीं किया है। गीता का कहना है-‘फलासक्ति छोड़ों और कर्म करो,’ ‘आशरहित होकर कर्म करो’, निष्काम होकर कर्म करो।’ यह गीता की वह ध्वनि है, जो भलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छो़ड़ता है, वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है, वह चढ़ता है। फल-त्याग का यह अर्थ नहीं है कि परिणाम के संबंध में लापरवाही रहे।
परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान आत्मावश्यक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में तन्मय रहता है, वह फलत्यागी है।
पर यहाँ फलत्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता नहीं। गीता में ऐसे अर्थ का कहीं स्थान नहीं हैं। फलत्याग से मतलब है फल के संबंध में आसक्ति का अभाव। वास्तव में देखा जाए तो फलत्यागी को तो हज़ारगुना फल मिलता है। गीता के फलत्याग में तो अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य परिणाम का ध्यान करता रहता है, वह बहुत बार कर्म-कर्त्तव्यभ्रष्ट हो जाता है। उसे अधीरता घेरती हैं, इससे वह क्रोध के वश हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता है, एक कर्म में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में पड़ता जाता है। परिणाम की चिंता करनेवाले की स्थिति विषयांध की-सी हो जाती है। और अंत में यह विषयी की भाँति सारासार का, नीति-अनीति का विवेक छोड़ देता हैं, और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी साधन से काम लेता है और उसे धर्म मानता है।
फलासक्ति के ऐसे कटु परिणामों में से गीतकार ने अनासक्ति का अर्थात् कर्मफलत्याग का सिद्धांत निकाला और संसार के सामने अत्यंत आकर्षक भाषा में रखा। साधारणतः तो यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी वस्तु हैं, ‘व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहार में धर्म नहीं बचाया जा सकता, धर्म को जगह नहीं हो सकती, धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और अर्थ की जगह अर्थ।’ बहुतों को ऐसा कहते हम सुनते हैं। गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष और व्यवहार के बीच ऐसा भेद नहीं रखा है, वरन् व्यवहार में धर्म को उतारा है। जो धर्म व्यवहार में न लाया जा सके, वह धर्म नहीं है, मेरी समझ से यह बात गीता में हैं। मतलब, गीता के मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्ति के बिना हो ही न सकें, वे भी त्याज्य हैं।
सन् 1888-89 में जब गीता का प्रथम दर्शन हुआ तभी मुझे ऐसा लगा कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वरन् इसमें भौतिक युद्ध के वर्णन के बहाने प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर निरंतर होते रहनेवाले द्वंद्व-युद्ध का ही वर्णन है। मानुषी योद्धाओं की रचना हृदयगत युद्ध को रोचक बनाने के लिए गढ़ी हुई कल्पना है। यह प्राथमिक स्फुरण धर्म का और गीता का विशेष विचार करने के बाद पक्की हो गई। महाभारत पढ़ने के बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया। महाभारत-ग्रंथ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता। इसके प्रबल प्रमाण आदिपर्व में ही है। पात्रों की अमानुषी और अतिमानुषी उत्पति का वर्णन करके व्यास भगवान् ने राजा-प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हों, परंतु महाभारत में तो उनका उपयोग व्यास भगवान् ने केवल धर्म का दर्शन कराने के लिए ही किया है।
महाभारतकार ने भौतिक युद्घ की आवश्यकता नहीं, उसकी निरर्थकता सिद्ध की है। विजेता ने रुदन कराया है, पश्चात्ताप कराया है और दुख के सिवा और कुछ नहीं करने दिया।
1. गांधी जी का अनुवाद गुजराती में है। यह उसी का हिंदी-रूपांतर है।
इस महाग्रंथ में गीता शिरोमणि रूप से विराजती है। उसका दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध-व्यवहार सिखाने के बदले स्थितप्रज्ञ के लक्षण सिखाता है। स्थितप्रज्ञ का ऐहिक युद्ध के साथ कोई संबंध नहीं होता, यह बात उसके लक्षणों में ही मुझे प्रतीत हुई है। साधारण पारिवारिक झगड़ों के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय करने के लिए गीता-जैसी पुस्तक की रचना संभव नहीं है।
गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्ध संपूर्ण ज्ञान हैं। पंरतु काल्पनिक हैं। यहाँ कृष्ण नाम के अवतारी पुरुष का निषेध नहीं है। केवल संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक हैं, संपूर्णावतार का आरोपण पीछे से हुआ है।
अवतार से तात्पर्य है शरीरघारी पुरुष विशेष। जीवमात्र ईश्वर के अवतार है, परंतु लौकिक भाषा में सबकों हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान् है, उसे भावी प्रजा अवताररूप से पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न ईश्वर के बड़प्पन में कमी आती है, न उसमें सत्य को आघात पहुँचता है। ‘आदम खुदा नहीं; लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं।’ जिसमें धर्म-जागृति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावतार है। इस विचार-श्रेणी से कृष्णरूपी संपूर्णावतार आज हिंदू-धर्म में साम्राज्य भोग रहा है।
यह दृश्य मनु्ष्य की अंतिम सद्भिलाषा का सूचक है। मनुष्य को ईश्वर-रूप हुए बिना चैन नहीं, पड़ता, शांति नहीं मिलती। ईश्वररूप होने के प्रयत्न का नाम सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है और यही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन सब धर्म-ग्रंथों का विषय है वैसे ही गीता का भी है। पर गीताकार ने इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रची, वरन् आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का आशय है। जो चीज हिंदू धर्म-ग्रंथों में छिट-पुट दिखाई देती हैं, उसे गीता ने अनेक रुपों में, अनेक शब्दों में, पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित किया है।
वह अद्वितीय उपाय है ‘कर्मफलत्याग।’
इस मध्यबिंदु के चारों ओर गीता की सारी सजावट है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि इसके आसपास तारा-मंडल-रूप में सज गए है। जहाँ देह है, वहाँ कर्म तो है ही। उससे कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को प्रभु का मंदिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, यह सब धर्मों ने प्रतिपादित किया है; परंतु कर्ममात्र में कुछ दोष तो हैं ही, मुक्ति तो निर्दोष की ही होती है। तब कर्मबंधन में से अर्थात् दोष-स्पर्श में से कैसे छुटकारा हो ? इसका जवाब गीताजी ने निश्चयात्मक शब्दों में दिया है-‘निष्काम कर्म से, यज्ञार्थ कर्म करके, कर्मफल त्याग करके, सब कर्मों को कृष्णार्पण करके, अर्थात् मन, वचन और काया को ईश्वर में होम करके।’
पर निष्कामता, कर्मफल-त्याग कहने-भर से नहीं हो जाता। यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदय-मंथन से ही उत्पन्न होता है। यह त्याग-शक्ति पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान तो बहुतेरे पंडित पाते हैं।
वेदादि उन्हें कंठस्थल होते हैं, उनमें से अधिकांश भोगादि में लगे-लिपटे रहते हैं। ज्ञान का अतिरेक शुष्क पांडित्य के रूप में न हो जाए, इस ख्याल से गीताकार ने ज्ञान के साथ भक्ति को मिलाया और उसे प्रथम स्थान दिया। बिना भक्ति का ज्ञान हानिकार है। इसलिए कहा गया-‘भक्ति करो तो ज्ञान मिल ही जाएगा।’ पर भक्ति तो ‘सिर का सौदा’ है, इसलिए गीताकार ने भक्ति के लक्षण स्थितप्रज्ञ के-से बतलाए हैं।
तात्पर्य, गीता की भक्ति बाह्याचारिता नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। गीता में बताए उपचार का बाह्य चेष्टा या क्रिया के साथ कम-से-कम संबंध हैं, माला-तिलक, अर्ध्यादि साधन भले भी भक्त बरते, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं। जो किसी का द्वेष नहीं करता, जो करूणा का भंडार है और ममता-रहित हैं, जो निरहंकार है, जिसे सुख-दुःख शीत-उष्ण समान हैं, जो क्षमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, जिसने मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिए हैं, जिससे लोग उद्वेग नहीं पाते, जो लोगों का भय नहीं रखता, जो शुभाशुभ का प्याग करनेवाला है, जो शत्रु-मित्र पर समभाव रखनेवाला है, जिसे मान-अपमान समान है, जिस स्तुति से खुशी नहीं होती और निदा से ग्लानि नहीं होती, जो मौनधारी है, जिसे एकांत प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है, वह भक्त है। यह भक्ति आसक्त स्त्री-पुरुषों में संभव नहीं है।
इससे हम देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना ही आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जैसे रुपए के बदले में ज़हर ख़रीदा जा सकता है और भी लाया जा सकता है, वैसे ज्ञान या भक्ति के बदले बंधन भी लाया जा सके और मोक्ष भी, यह संभव नहीं हैं। यहाँ तो साधन और साध्य, बिल्कुल एक नहीं तो लगभग एक ही वस्तु हैं, साधन की पराकाष्ठा जो है, वही मोक्ष है और गीता के मोक्ष का अर्थ परम शांति हैं।
किंतु ऐसे ज्ञान और भक्ति को कर्म-फल-त्याग की कसौटी पर चढ़ना ठहरा। लौकिक कल्पना में शुष्क पंडित भी ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम करने को नहीं रहता। हाथ से लोटा तक उठाना भी उसके लिए कर्म-बंधन है। यज्ञशून्य जहाँ ज्ञानी गिना जाए वहाँ लोटा उठाने जैसी तुच्छ लौकिक क्रिया को स्थान ही कैसे मिल सकता है ?
लौकिक कल्पना में भक्त से मतलब है बाह्याचारी2, माला लेकर जप करनेवाला। सेवा-कर्म करते भी उसकी माला में विक्षेप पड़ता है। इसलिए वह खाने-पीने आदि भोग-भोगने के समय ही माला को हाथ से छोड़ता हैं, चक्की चलाने या रोगी की सेवा-शुश्रूषा करने के लिए कभी नहीं छोड़ता।
इन दोनों वर्गों को गीता ने साफ़ तौर से कह दिया-‘कर्म बिना किसी ने सिद्धि नहीं पाई। जनकादि भी कर्म द्वारा ज्ञानी हुए। यदि मैं भी आलस्य रहित
2. जो बाह्याचार मे लीन रहता है और शुद्ध भाव से मानता है कि यही भक्ति हैं।
होकर कर्म न करता रहूँ तो इन श्लोकों का नाश हो जाए।’ तो फिर लोगों के लिए पूछना ही क्या रह जाता है ?
परंतु एक ओर से कर्ममात्र बंधनरूप हैं, यह निर्विवाद है। दूसरी ओर से देही इच्छा-अनिच्छा से भी कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएँ कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधनमुक्त कैसे रहे ? जहाँ तक मुझे मालूम है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है, वैसे दूसरे किसी भी धर्म-ग्रंथ ने नहीं किया है। गीता का कहना है-‘फलासक्ति छोड़ों और कर्म करो,’ ‘आशरहित होकर कर्म करो’, निष्काम होकर कर्म करो।’ यह गीता की वह ध्वनि है, जो भलाई नहीं जा सकती। जो कर्म छो़ड़ता है, वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है, वह चढ़ता है। फल-त्याग का यह अर्थ नहीं है कि परिणाम के संबंध में लापरवाही रहे।
परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान आत्मावश्यक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में तन्मय रहता है, वह फलत्यागी है।
पर यहाँ फलत्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता नहीं। गीता में ऐसे अर्थ का कहीं स्थान नहीं हैं। फलत्याग से मतलब है फल के संबंध में आसक्ति का अभाव। वास्तव में देखा जाए तो फलत्यागी को तो हज़ारगुना फल मिलता है। गीता के फलत्याग में तो अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य परिणाम का ध्यान करता रहता है, वह बहुत बार कर्म-कर्त्तव्यभ्रष्ट हो जाता है। उसे अधीरता घेरती हैं, इससे वह क्रोध के वश हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता है, एक कर्म में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में पड़ता जाता है। परिणाम की चिंता करनेवाले की स्थिति विषयांध की-सी हो जाती है। और अंत में यह विषयी की भाँति सारासार का, नीति-अनीति का विवेक छोड़ देता हैं, और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी साधन से काम लेता है और उसे धर्म मानता है।
फलासक्ति के ऐसे कटु परिणामों में से गीतकार ने अनासक्ति का अर्थात् कर्मफलत्याग का सिद्धांत निकाला और संसार के सामने अत्यंत आकर्षक भाषा में रखा। साधारणतः तो यह माना जाता है कि धर्म और अर्थ विरोधी वस्तु हैं, ‘व्यापार इत्यादि लौकिक व्यवहार में धर्म नहीं बचाया जा सकता, धर्म को जगह नहीं हो सकती, धर्म का उपयोग केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है। धर्म की जगह धर्म शोभा देता है और अर्थ की जगह अर्थ।’ बहुतों को ऐसा कहते हम सुनते हैं। गीताकार ने इस भ्रम को दूर किया है। उसने मोक्ष और व्यवहार के बीच ऐसा भेद नहीं रखा है, वरन् व्यवहार में धर्म को उतारा है। जो धर्म व्यवहार में न लाया जा सके, वह धर्म नहीं है, मेरी समझ से यह बात गीता में हैं। मतलब, गीता के मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्ति के बिना हो ही न सकें, वे भी त्याज्य हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i