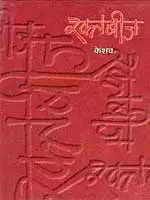|
कहानी संग्रह >> रक्तबीज रक्तबीजकेशव
|
55 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है केशव की श्रेष्ठतम कहानियों का संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
केशव सिर्फ कथाकार नहीं कवि-कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ अत्यन्त मार्मिक और
गहरी होती हैं। अपने हर शब्द और अभिव्यक्ति की हर भंगिमा के लिए लगातार
संघर्ष करता उनका कथाकार कथ्य को इस तरह रचता है, मानों वह उसका निजी
सरोकार हो। केशव के रचाव में एक ऐसा आयासहीन मोजेइक है,जो कहीं से भी
आरोपित नहीं लगता, क्योंकि सृजन के प्रति केशव पल भर के लिए भी संसार या
स्मृति की रक्षा करते हुए भी वे उसमें गहनता और विस्तार रचते हैं। कई
कहानियाँ युवकों, बच्चों, वृद्धों-असहायों गरीबों के पक्ष में लिखी गई बड़े
केनवास की कहानियाँ हैं। केशव की भाषा का सौन्दर्य विशिष्ट है। बिम्ब और
प्रतीक इसे मार्मिक बनाते हैं,परन्तु कथातत्व को कहीं चोट नहीं पहुँचाते।
केशव अपनी कहानियों के लिए एक नया कथा-शिल्प रचते हैं जिसमें
किस्सागोई, कविता और संवेदना के सूक्ष्म तन्तु हैं, जिनके सहारे पाठक कता के
भीतर उतरता चलता है। केशव की कहानियों में चित्रित पहाड़ी अंचल अपनी सीमा
में भी व्यापक संवेदनशील है। ये कहानियाँ जगह-जगह रोककर अपने कुछ अंशों को
दुबारा-तिबारा पढ़ने पर विवश करती हैं, लेकिन उबाती नहीं।
उत्सव
कहीं टिकना नहीं हो पाता था। कुछ पिता की
नौकरी का मौसम।
कुछ उसका तापमान। कुछ उनका दबंग अन्दाज। अपने ऊपर से किसी को न लाँघने
देने की जिद। सिद्धान्तों के तार पर तनिक भी डगमगाये बिना, बेखौफ चलते
जाने का उनका तप। हद से हद साल भर में ही पूरा परिवार तम्बू उखाड़कर दूसरी
जगह की ओर रवाना हो लेता था। कभी-कभी तो छः-सात माह बाद ही पिता आगे बढ़
जाते। और हम अपनी परिक्षाओं या नये स्थान से पटरी न बैठ सकने की वजह से
पीछे छूट जाते। परीक्षाएँ समाप्त होते ही अपना माल-असबाब किसी मोटर की छत
पर या रेलगाड़ी के डिब्बे में ठूसकर पिता के पास पहुँच जाते। एकदम पराये
और एक-दूसरे से असम्बद्ध माहौल में छलाँग लगा देते।
कई-कई दिन पूरा परिवार सकते की हालत में रहता। अजनबी, चेहरों उनकी भाषा, उनके रहन-सहन में उतरने से पहले एक झिझकभरी विवशता में छटपटाता। उन तक पहुँचने की कोशिश में घिसती अपनी पहचान को थामे रखने के आतंक से घिरा।
कई कस्बों, शहरों से होता इस कस्बे तक घिसटते-घिसटते ग्यारहवीं कक्षा तक पहुँच चुका था मैं। भाई-बहन अभी काफी छोटे से मुझसे। छोटे थे इसलिए छोटी कक्षाओं में थे।
यह कस्बा हमारे रहन-सहन, बोल-चाल, पैतृक घर-बार से कोसों दूर था। अभी कुल मिला कर महीना भर ही हुआ था यहाँ आये।
कस्बे में हायर सेकेण्डरी स्कूल था, थाना था, एक सरकारी डिस्पेंसरी थी। और बाजार भी था जहाँ दिन में भी अँधेरा-सा रहता था। बाज़ार से गुजरते हुए ऐसा लगता जैसे आप किन्हीं खँडहरों से गुज़र रहे हों। बाज़ार में किसी भी वक्त जाओ दुकानों के थड़े अक्सर ग्राहकों के इन्तजार में ऊँघते दिखाई देते। जैसे कस्बे के लोगों की घरेलू जरूरतें घरों में ही पूरी हो जाती थीं। या फिर उस बाज़ार में लोगों की दिलचस्पी लायक कुछ था ही नहीं।
अपनी उम्र से कई गज़ ऊपर दिखता थुलथुल देह वाला थानेदार का लड़का अपनी सहपाठिन प्रेमा से प्रेम करता था। बाँस की खपच्चियों जैसी गोरी-चिट्टी प्रेमा से। धंसे हुए गाल और कमान की तरह मुड़ी हुई कमर वाला डॉक्टर का लड़का अक्सर भाँग, गाँजे और दारू के नशे में टुन रहता था। उसके पेट और पीठ में भेद करना एकदम दुश्वार था। वह ऐसे बोलता था जैसे उसके मुँह में दाँत ही न हों। और कई-कई दिन स्कूल से गायब रहता था। स्कूल से ही क्यों, घर और कस्बे से भी।
सड़क के अन्दर की ओर फूटती, धूल के अम्बार उगलती गली के आर-पार दस-बारह कच्चे-पक्के, समय की मार से थोड़ा-बहुत सुरक्षित मकानों को पार करके था एक दोमंज़िला मकान, जिसकी ऊपर की मंज़िल में अपनी गृहस्थी को जमाने में जुटा हुआ था सारा परिवार। लगातार भोथरी होती इच्छा के बावजूद।
नीचे की मंज़िल में मकान मालकिन रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। दस बरस से कम उम्र के। कुछ दिन बाद ही हमें पता चल पाया कि उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ रहने लग गया था। वह बहुत अच्छे स्वभाव वाली ममतालु किस्म की औरत थी। और संकोची भी। बात अटक-अटककर करती। और बात करते हुए अधिकतर उसकी नज़रें अपने पैरों पर टिकी रहतीं। उतनी देर उसकी समूची देह थरथराती रहती। जैसे तेज बुखार में। आँखें हर पल मिचमिचातीं। जैसे किसी भाव-भंगिमा को भीतर ही पकड़े रखने की एक सायास चेष्टा के साथ। चलते-फिरते उसके दोनों कन्धे आगे की ओर झुके रहते थे जिन पर उसकी बाँहें बेजान-सी झूलतीं।
वह किसी भी सूरत में अपने में से उगती हुई स्त्री नहीं थी। अपने में धँसती हुई। लगातार धँसती स्त्री थी। अपने हँसने में भी मुरझायी हुई। उसके व्यक्तित्व के दो छोंरो के बीच हमेशा गहरी धुन्ध छायी रहती थी। उसके पति की रेडीमेड कपड़ों की दूकान थी, जिसमें उसके हाथ से बुने स्वेटर, मौजे, स्कार्फ और टोपियाँ भी बिकती थीं। लेकिन अब क्योंकि पति नहीं था इसलिए दूकान घर में आ गयी थी। लोग कपड़े दे जाते और वह सिल देती। इस काम को वह बोझ न समझकर पूरे श्रम और लगन से करती थी। देर रात तक।
वह सिलाई करते हुए अधिकतर रात के समय, एक टप्पा गुनगुनाया करती थी, ‘‘साडा चोला लीराँ दा, इक बारी पा फेरा तक हाल फकीराँ दा’’।
वह स्वर कोकिला तो नहीं थी, पर उसके स्वर में एक भीनी-भीनी कसक थी। जैसे गाढ़ी सर्दियों में आग को और-और करीब से तापने का मन होता है। ताप जब किरच की तरह देह में घुसता है तो हम बिदकते हैं। लेकिन फिर भी आग के उतने ही निकट होने को व्यग्र।
इधर-उधर दूर-दूर तक इसके सिवा कोई दोमंज़िला मकान नहीं था। इसलिए ऊपर की मंज़िल में रहने का मजा ही कुछ और था। मकानों के साथ सटे मकान। बीच में बाँहों की तरह फैली धूसर पतली-पतली गलियाँ।
शुरू-शुरू में हर रोज सुबह एक स्त्री-स्वर मुझे चौंकाता, ‘सरवण दी माँ लस्सी घिण बंज।’
कई दिन बाद मुझे पता चला कि सामने की ओर वाले मकान से एक औरत हमारी मकान मालकिन को लस्सी ले जाने के लिए आवाज़ देती है। जिसकी मैं सिर्फ आवाज़ ही सुनता था। सूरत बहुत कोशिश के बावजूद नहीं देख पाया था।
हमारे मकान से सटा हुआ था एक दूसरा मकान। बीच में थी मुश्किल से तीन फुट चौड़ी गली, जो और-और मकानों की ओर जाती गली से छिटककर हमारे मकान के प्रवेश-द्वार पर रूक जाती थी। उसी प्रवेश-द्वार के बगल में हाथ भर की दूरी पर था दूसरे मकान का गली में खुलने वाला द्वार। द्वार के अन्दर बेहड़ा (आँगन) और एक सीध में दो कमरे। उन दो कमरों में आबाद थी एक नर्स। उसी की डिस्पेंसरी में चपरासी के पद पर कार्यरत उसका पति। और हाँ, उनकी एकमात्र जीवित औलाद इन्दिरा भी।
वह कहने भर को पति-पत्नी थे। एक-दूसरे के ऊपर चढ़-दौड़ने की फुर्सत का उनके पास कोई अभाव नहीं था। गली में, बेहड़े में, कमरों में उनके चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर मँडराती रहती थीं। उनके बीच न तो कोई मौसम था, न किसी मौसम का इन्तजार। बस अपना रास्ता बदल चुकी नदी का पाट था। सूखा और उजाड़। उनके अपनी-अपनी ओर खुलने वाले दरवाजे न जाने कब से बन्द थे। उनके बीच दौड़ती रहती थी उनकी बेटी। हाँफती। कभी इस दरवाजे को भड़भड़ाती, कभी उस दरवाजे को। तसल्ली पर लगातार कमजोर पड़ती अपनी पकड़ के बावजूद कि कभी-न-कभी कोई द्वार जरूर खुलेगा। एक खुलेगा तो दूसरा....
स्कूल में भर्ती का पहला दिन था। पिता मुझे साथ लिये सीधे प्रिंसिपल के कमरे में चले गये थे। कुछ पल की औपचारिकताओं के बाद प्रिंसिपल ने घण्टी बजाकर चपरासी को बुलाया। चपरासी हमारे साथ हो लिया।
पिता भी क्लास तक आये थे। मास्टर जी ने कहा, ‘क्लास स्टैण्ड’। कोई भी आये क्लास को जरूर खड़ा होना पड़ता होगा। क्लास से थोड़ा हटकर पिता कुछ पल उनसे बतियाये और फिर चले गये।
कक्षाओं में अध्यापक पढ़ा रहे थे।
एल आकार की स्कूल की इमारत के सामने बिछा था अच्छा-ख़ासा मैदान, घास से कम, धूल से ज्यादा अटा। मैदान में कबूतरों के दाना तलाशते अलग-अलग झुण्डों की तरह तीन-चार कक्षाएँ चल रही थीं। एक-दूसरे से ज्यादा दूर न होते हुए भी एक दूसरे से असम्पृक्त। कक्षाओं में अध्यापक थे। और उनकी पढ़ाने की मुद्राओं में कुछ तलाशने की कोशिश में अपना सर खुजलाते, जमुहाइयां लेते विद्यार्थी। गर्मियों की शुरूआत थी। पसीना बेशक न आता हो, पर सूरज को तापना भी जरूरी नहीं था। तीसरा पीरियड शुरू होते ही विद्यार्थी कन्धों पर बस्ते लटकाये कमरों में भरने लगे, तभी यह रहस्य खुला।
मास्टर रामसहाय की कक्षा के छात्र तीन कतारों में विराजमान थे। दो में लड़के और एक में लड़कियाँ।
‘‘ज़रा उधर सरको।’’
मास्टर रामसहाय ने पहली कतार में पहले नम्बर पर बैठे थानेदार के लड़के से कहा। थानेदार का लड़का अपनी जगह बैठे-बैठे ही कसमसाया। सामने रखे बस्ते पर उसके हाथ पत्थर की सिल की तरह जम गये थे।
एकदम दुबले-पतले निरीह से दिखने वाले रामसहाय लगभग चीख पड़े, ‘‘सुना नहीं।’’
कुछ पल तक उनके चेहरे की झुर्रियाँ पानी पर कांपती छायाओं की तरह हिलती रहीं। असमय बुढ़ापे ने वक्त से पहले ही उनकी देह को निचोड़ना शुरू कर दिया था।
थानेदार का लड़का बस्ता उठाकर थोड़ा सरक गया। सिर्फ इतना ही कि मैं टाट पर उकड़ूँ बैठ सकूँ।
‘‘आज से तुम यहीं बैठोगे।’’ रामसहाय की आवाज़ कमजोर होते हुए भी दृढ़ थी।
पूरी क्लास के लड़के नेकर पहने हुए थे। सिर्फ तीन को छोड़। डॉक्टर के लड़के और मैंने खाकी पैण्ट पहन रखी थी। थानेदार का लड़का सफेद पायजामे में था। पता नहीं रामसहाय मुझे पहले नम्बर पर क्यों बिठाना चाहते थे। इस बात का बाद में ही पता चला कि स्कूल में दो ही विद्यार्थियों के बाप गजेटिड थे। एक डॉक्टर और दूसरे मेरे पिता। पर डॉक्टर का लड़का तो हमारी कतार के सबसे अन्त में बैठता था।
दरअसल मुझे कुछ अरसे से एक अजीब किस्म का चर्म रोग हो गया था। सारी देह पर फफोले पड़ जाते। फिर उनमें से पानी रिसता रहता। माँ उन पर दवाई लगाते हुए अक्सर बुदबुदाती, यह नामुराद रोग पता नहीं कहाँ से आकर चिपट गया है मेरे बच्चे को।
स्कूल जाने से पहले लगभग हर रोज दवाई का गाढ़ा-गाढ़ा लेप लगाने की प्रक्रिया माँ द्वारा सम्पन्न होती थी। छोटे भाई-बहन इर्द-गिर्द मँडराते कुछ-कुछ कौतुक से उस क्रिया को देखते थे। माँ अक्सर उन्हें डाँट दिया करती, ‘‘इधर क्या बिसूर रहे हो। अपना बस्ता और किताबें सँभालो। स्कूल को देरी हो रही है।’’
पिछले चार-पाँच रोज से माँ बुखार में तप रही थी। स्कूल का समय हो रहा था। भाई-बहन स्कूल जा चुके थे। ‘‘देर हो रही है माँ। जल्दी लगा दो।’’ जाँघिया पहने नंग-धड़ंग मैं माँ की चारपाई के पास नीचे फर्श पर बैठा था। माँ बार-बार उठने की कोशिश करती और फिर निढाल-सी चारपाई पर ढह जाती।
‘‘आज तू ऐसे ही चला जा। छुट्टी होने के बाद लेप लगा दूँगी।’’ कहते-कहते माँ बेदम-सी हो आयी थी।
इससे पहले कि मैं उठकर कपड़े पहनता, दरवाजे पर से आवाज़ आयी, ‘‘आज स्कूल नहीं जाना है ?’’
देखा, दरवाजे पर इन्दिरा खड़ी थी।
मुझे उस हालत में देख कर कुछ सकपकायी।
उसके कपोल आरक्त हो गये।
मैं भी कुछ पल जड़वत्-सा उसी हालात में बैठा उसे ताकता रहा।
इन्दिरा धीरे से आकर मेरे पास बैठ गयी। वह किंचित विस्मय से मेरी उघड़ी हुई फफोलों से पटी पीठ को ताक रही थी।
‘‘तू कपड़े क्यों नहीं पहनता। बेशर्म कहीं का।’’ माँ ने मुझे करारी हिदायत दी।
‘‘मुए हाथ ही नहीं चल रहे आज। दवा कैसे लगाऊँ।’’
माँ ने इन्दिरा की ओर देखते हुए कहा।
मैं उठने को ही था कि इन्दिरा ने बाजू पकड़कर मुझे उसी हालात में बिठा दिया।
‘‘मैं लगा देती हूँ माँ जी।’’
‘‘न-न बेटी। यह काम तेरा नहीं है। कहीं छूत लग गयी तो ?’’ माँ की आवाज़ एकदम अशक्त-सी हो गयी थी। वह सिरहाने पर सर रखे गहरी-गहरी साँसें लेने लगी थी। फिर इन्दिरा ने झपटकर माँ के सिरहाने से दवा की शीशी उठायी और दवाई का लेप करने लगी थी। माँ कातर निगाहों ने उसे बस ताकती रही। मुझे भी कुछ अटपटा जरूर लगा था।
एक में लोरी जैसा कुछ और दूसरे में उपलों की-सी मीठी-मीठी आँच जैसा। पर देह में एक पुलक भी थी और थरथराहट भी। फिर भी दो स्त्रियों के स्पर्श में कामन थी स्निग्धता।
फिर तो कभी सुबह, कभी शाम, लेप लगाने की क्रिया इन्दिरा द्वारा ही सम्पन्न होने लगी थी। माँ का विरोध भी शिथिल पड़ते-पड़ते अन्ततः स्वीकार में बदल गया था।
एक दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में कहा था मैंने, ‘‘अगर तुम्हें छूत लग गयी तो ?’’
‘‘आज तक माँ जी को लगी क्या ? और लग भी गयी तो तुम लेप लगा दिया करना मुझे।’’
कहकर इन्दिरा खिलखिलाकर हँस दी थी। वह जब भी हँसती उसकी यह खिलखिलाहट बहुत देर तक उसकी छोटी-छोटी पर गहरी आँखों में रंग-बिरंगे पतंगों की तरह डोलती रहती।
अपने कैशोर्य से वह बाहर निकल आयी थी। कल-कल करती। पर उस कल-कल के नाद से अनभिज्ञ। जंगल को अपने उत्सव से सराबोर करने के लिए आतुर। नींद से जागे वसन्त की तरह।
कई-कई दिन पूरा परिवार सकते की हालत में रहता। अजनबी, चेहरों उनकी भाषा, उनके रहन-सहन में उतरने से पहले एक झिझकभरी विवशता में छटपटाता। उन तक पहुँचने की कोशिश में घिसती अपनी पहचान को थामे रखने के आतंक से घिरा।
कई कस्बों, शहरों से होता इस कस्बे तक घिसटते-घिसटते ग्यारहवीं कक्षा तक पहुँच चुका था मैं। भाई-बहन अभी काफी छोटे से मुझसे। छोटे थे इसलिए छोटी कक्षाओं में थे।
यह कस्बा हमारे रहन-सहन, बोल-चाल, पैतृक घर-बार से कोसों दूर था। अभी कुल मिला कर महीना भर ही हुआ था यहाँ आये।
कस्बे में हायर सेकेण्डरी स्कूल था, थाना था, एक सरकारी डिस्पेंसरी थी। और बाजार भी था जहाँ दिन में भी अँधेरा-सा रहता था। बाज़ार से गुजरते हुए ऐसा लगता जैसे आप किन्हीं खँडहरों से गुज़र रहे हों। बाज़ार में किसी भी वक्त जाओ दुकानों के थड़े अक्सर ग्राहकों के इन्तजार में ऊँघते दिखाई देते। जैसे कस्बे के लोगों की घरेलू जरूरतें घरों में ही पूरी हो जाती थीं। या फिर उस बाज़ार में लोगों की दिलचस्पी लायक कुछ था ही नहीं।
अपनी उम्र से कई गज़ ऊपर दिखता थुलथुल देह वाला थानेदार का लड़का अपनी सहपाठिन प्रेमा से प्रेम करता था। बाँस की खपच्चियों जैसी गोरी-चिट्टी प्रेमा से। धंसे हुए गाल और कमान की तरह मुड़ी हुई कमर वाला डॉक्टर का लड़का अक्सर भाँग, गाँजे और दारू के नशे में टुन रहता था। उसके पेट और पीठ में भेद करना एकदम दुश्वार था। वह ऐसे बोलता था जैसे उसके मुँह में दाँत ही न हों। और कई-कई दिन स्कूल से गायब रहता था। स्कूल से ही क्यों, घर और कस्बे से भी।
सड़क के अन्दर की ओर फूटती, धूल के अम्बार उगलती गली के आर-पार दस-बारह कच्चे-पक्के, समय की मार से थोड़ा-बहुत सुरक्षित मकानों को पार करके था एक दोमंज़िला मकान, जिसकी ऊपर की मंज़िल में अपनी गृहस्थी को जमाने में जुटा हुआ था सारा परिवार। लगातार भोथरी होती इच्छा के बावजूद।
नीचे की मंज़िल में मकान मालकिन रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। दस बरस से कम उम्र के। कुछ दिन बाद ही हमें पता चल पाया कि उसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ रहने लग गया था। वह बहुत अच्छे स्वभाव वाली ममतालु किस्म की औरत थी। और संकोची भी। बात अटक-अटककर करती। और बात करते हुए अधिकतर उसकी नज़रें अपने पैरों पर टिकी रहतीं। उतनी देर उसकी समूची देह थरथराती रहती। जैसे तेज बुखार में। आँखें हर पल मिचमिचातीं। जैसे किसी भाव-भंगिमा को भीतर ही पकड़े रखने की एक सायास चेष्टा के साथ। चलते-फिरते उसके दोनों कन्धे आगे की ओर झुके रहते थे जिन पर उसकी बाँहें बेजान-सी झूलतीं।
वह किसी भी सूरत में अपने में से उगती हुई स्त्री नहीं थी। अपने में धँसती हुई। लगातार धँसती स्त्री थी। अपने हँसने में भी मुरझायी हुई। उसके व्यक्तित्व के दो छोंरो के बीच हमेशा गहरी धुन्ध छायी रहती थी। उसके पति की रेडीमेड कपड़ों की दूकान थी, जिसमें उसके हाथ से बुने स्वेटर, मौजे, स्कार्फ और टोपियाँ भी बिकती थीं। लेकिन अब क्योंकि पति नहीं था इसलिए दूकान घर में आ गयी थी। लोग कपड़े दे जाते और वह सिल देती। इस काम को वह बोझ न समझकर पूरे श्रम और लगन से करती थी। देर रात तक।
वह सिलाई करते हुए अधिकतर रात के समय, एक टप्पा गुनगुनाया करती थी, ‘‘साडा चोला लीराँ दा, इक बारी पा फेरा तक हाल फकीराँ दा’’।
वह स्वर कोकिला तो नहीं थी, पर उसके स्वर में एक भीनी-भीनी कसक थी। जैसे गाढ़ी सर्दियों में आग को और-और करीब से तापने का मन होता है। ताप जब किरच की तरह देह में घुसता है तो हम बिदकते हैं। लेकिन फिर भी आग के उतने ही निकट होने को व्यग्र।
इधर-उधर दूर-दूर तक इसके सिवा कोई दोमंज़िला मकान नहीं था। इसलिए ऊपर की मंज़िल में रहने का मजा ही कुछ और था। मकानों के साथ सटे मकान। बीच में बाँहों की तरह फैली धूसर पतली-पतली गलियाँ।
शुरू-शुरू में हर रोज सुबह एक स्त्री-स्वर मुझे चौंकाता, ‘सरवण दी माँ लस्सी घिण बंज।’
कई दिन बाद मुझे पता चला कि सामने की ओर वाले मकान से एक औरत हमारी मकान मालकिन को लस्सी ले जाने के लिए आवाज़ देती है। जिसकी मैं सिर्फ आवाज़ ही सुनता था। सूरत बहुत कोशिश के बावजूद नहीं देख पाया था।
हमारे मकान से सटा हुआ था एक दूसरा मकान। बीच में थी मुश्किल से तीन फुट चौड़ी गली, जो और-और मकानों की ओर जाती गली से छिटककर हमारे मकान के प्रवेश-द्वार पर रूक जाती थी। उसी प्रवेश-द्वार के बगल में हाथ भर की दूरी पर था दूसरे मकान का गली में खुलने वाला द्वार। द्वार के अन्दर बेहड़ा (आँगन) और एक सीध में दो कमरे। उन दो कमरों में आबाद थी एक नर्स। उसी की डिस्पेंसरी में चपरासी के पद पर कार्यरत उसका पति। और हाँ, उनकी एकमात्र जीवित औलाद इन्दिरा भी।
वह कहने भर को पति-पत्नी थे। एक-दूसरे के ऊपर चढ़-दौड़ने की फुर्सत का उनके पास कोई अभाव नहीं था। गली में, बेहड़े में, कमरों में उनके चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर मँडराती रहती थीं। उनके बीच न तो कोई मौसम था, न किसी मौसम का इन्तजार। बस अपना रास्ता बदल चुकी नदी का पाट था। सूखा और उजाड़। उनके अपनी-अपनी ओर खुलने वाले दरवाजे न जाने कब से बन्द थे। उनके बीच दौड़ती रहती थी उनकी बेटी। हाँफती। कभी इस दरवाजे को भड़भड़ाती, कभी उस दरवाजे को। तसल्ली पर लगातार कमजोर पड़ती अपनी पकड़ के बावजूद कि कभी-न-कभी कोई द्वार जरूर खुलेगा। एक खुलेगा तो दूसरा....
स्कूल में भर्ती का पहला दिन था। पिता मुझे साथ लिये सीधे प्रिंसिपल के कमरे में चले गये थे। कुछ पल की औपचारिकताओं के बाद प्रिंसिपल ने घण्टी बजाकर चपरासी को बुलाया। चपरासी हमारे साथ हो लिया।
पिता भी क्लास तक आये थे। मास्टर जी ने कहा, ‘क्लास स्टैण्ड’। कोई भी आये क्लास को जरूर खड़ा होना पड़ता होगा। क्लास से थोड़ा हटकर पिता कुछ पल उनसे बतियाये और फिर चले गये।
कक्षाओं में अध्यापक पढ़ा रहे थे।
एल आकार की स्कूल की इमारत के सामने बिछा था अच्छा-ख़ासा मैदान, घास से कम, धूल से ज्यादा अटा। मैदान में कबूतरों के दाना तलाशते अलग-अलग झुण्डों की तरह तीन-चार कक्षाएँ चल रही थीं। एक-दूसरे से ज्यादा दूर न होते हुए भी एक दूसरे से असम्पृक्त। कक्षाओं में अध्यापक थे। और उनकी पढ़ाने की मुद्राओं में कुछ तलाशने की कोशिश में अपना सर खुजलाते, जमुहाइयां लेते विद्यार्थी। गर्मियों की शुरूआत थी। पसीना बेशक न आता हो, पर सूरज को तापना भी जरूरी नहीं था। तीसरा पीरियड शुरू होते ही विद्यार्थी कन्धों पर बस्ते लटकाये कमरों में भरने लगे, तभी यह रहस्य खुला।
मास्टर रामसहाय की कक्षा के छात्र तीन कतारों में विराजमान थे। दो में लड़के और एक में लड़कियाँ।
‘‘ज़रा उधर सरको।’’
मास्टर रामसहाय ने पहली कतार में पहले नम्बर पर बैठे थानेदार के लड़के से कहा। थानेदार का लड़का अपनी जगह बैठे-बैठे ही कसमसाया। सामने रखे बस्ते पर उसके हाथ पत्थर की सिल की तरह जम गये थे।
एकदम दुबले-पतले निरीह से दिखने वाले रामसहाय लगभग चीख पड़े, ‘‘सुना नहीं।’’
कुछ पल तक उनके चेहरे की झुर्रियाँ पानी पर कांपती छायाओं की तरह हिलती रहीं। असमय बुढ़ापे ने वक्त से पहले ही उनकी देह को निचोड़ना शुरू कर दिया था।
थानेदार का लड़का बस्ता उठाकर थोड़ा सरक गया। सिर्फ इतना ही कि मैं टाट पर उकड़ूँ बैठ सकूँ।
‘‘आज से तुम यहीं बैठोगे।’’ रामसहाय की आवाज़ कमजोर होते हुए भी दृढ़ थी।
पूरी क्लास के लड़के नेकर पहने हुए थे। सिर्फ तीन को छोड़। डॉक्टर के लड़के और मैंने खाकी पैण्ट पहन रखी थी। थानेदार का लड़का सफेद पायजामे में था। पता नहीं रामसहाय मुझे पहले नम्बर पर क्यों बिठाना चाहते थे। इस बात का बाद में ही पता चला कि स्कूल में दो ही विद्यार्थियों के बाप गजेटिड थे। एक डॉक्टर और दूसरे मेरे पिता। पर डॉक्टर का लड़का तो हमारी कतार के सबसे अन्त में बैठता था।
दरअसल मुझे कुछ अरसे से एक अजीब किस्म का चर्म रोग हो गया था। सारी देह पर फफोले पड़ जाते। फिर उनमें से पानी रिसता रहता। माँ उन पर दवाई लगाते हुए अक्सर बुदबुदाती, यह नामुराद रोग पता नहीं कहाँ से आकर चिपट गया है मेरे बच्चे को।
स्कूल जाने से पहले लगभग हर रोज दवाई का गाढ़ा-गाढ़ा लेप लगाने की प्रक्रिया माँ द्वारा सम्पन्न होती थी। छोटे भाई-बहन इर्द-गिर्द मँडराते कुछ-कुछ कौतुक से उस क्रिया को देखते थे। माँ अक्सर उन्हें डाँट दिया करती, ‘‘इधर क्या बिसूर रहे हो। अपना बस्ता और किताबें सँभालो। स्कूल को देरी हो रही है।’’
पिछले चार-पाँच रोज से माँ बुखार में तप रही थी। स्कूल का समय हो रहा था। भाई-बहन स्कूल जा चुके थे। ‘‘देर हो रही है माँ। जल्दी लगा दो।’’ जाँघिया पहने नंग-धड़ंग मैं माँ की चारपाई के पास नीचे फर्श पर बैठा था। माँ बार-बार उठने की कोशिश करती और फिर निढाल-सी चारपाई पर ढह जाती।
‘‘आज तू ऐसे ही चला जा। छुट्टी होने के बाद लेप लगा दूँगी।’’ कहते-कहते माँ बेदम-सी हो आयी थी।
इससे पहले कि मैं उठकर कपड़े पहनता, दरवाजे पर से आवाज़ आयी, ‘‘आज स्कूल नहीं जाना है ?’’
देखा, दरवाजे पर इन्दिरा खड़ी थी।
मुझे उस हालत में देख कर कुछ सकपकायी।
उसके कपोल आरक्त हो गये।
मैं भी कुछ पल जड़वत्-सा उसी हालात में बैठा उसे ताकता रहा।
इन्दिरा धीरे से आकर मेरे पास बैठ गयी। वह किंचित विस्मय से मेरी उघड़ी हुई फफोलों से पटी पीठ को ताक रही थी।
‘‘तू कपड़े क्यों नहीं पहनता। बेशर्म कहीं का।’’ माँ ने मुझे करारी हिदायत दी।
‘‘मुए हाथ ही नहीं चल रहे आज। दवा कैसे लगाऊँ।’’
माँ ने इन्दिरा की ओर देखते हुए कहा।
मैं उठने को ही था कि इन्दिरा ने बाजू पकड़कर मुझे उसी हालात में बिठा दिया।
‘‘मैं लगा देती हूँ माँ जी।’’
‘‘न-न बेटी। यह काम तेरा नहीं है। कहीं छूत लग गयी तो ?’’ माँ की आवाज़ एकदम अशक्त-सी हो गयी थी। वह सिरहाने पर सर रखे गहरी-गहरी साँसें लेने लगी थी। फिर इन्दिरा ने झपटकर माँ के सिरहाने से दवा की शीशी उठायी और दवाई का लेप करने लगी थी। माँ कातर निगाहों ने उसे बस ताकती रही। मुझे भी कुछ अटपटा जरूर लगा था।
एक में लोरी जैसा कुछ और दूसरे में उपलों की-सी मीठी-मीठी आँच जैसा। पर देह में एक पुलक भी थी और थरथराहट भी। फिर भी दो स्त्रियों के स्पर्श में कामन थी स्निग्धता।
फिर तो कभी सुबह, कभी शाम, लेप लगाने की क्रिया इन्दिरा द्वारा ही सम्पन्न होने लगी थी। माँ का विरोध भी शिथिल पड़ते-पड़ते अन्ततः स्वीकार में बदल गया था।
एक दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में कहा था मैंने, ‘‘अगर तुम्हें छूत लग गयी तो ?’’
‘‘आज तक माँ जी को लगी क्या ? और लग भी गयी तो तुम लेप लगा दिया करना मुझे।’’
कहकर इन्दिरा खिलखिलाकर हँस दी थी। वह जब भी हँसती उसकी यह खिलखिलाहट बहुत देर तक उसकी छोटी-छोटी पर गहरी आँखों में रंग-बिरंगे पतंगों की तरह डोलती रहती।
अपने कैशोर्य से वह बाहर निकल आयी थी। कल-कल करती। पर उस कल-कल के नाद से अनभिज्ञ। जंगल को अपने उत्सव से सराबोर करने के लिए आतुर। नींद से जागे वसन्त की तरह।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i