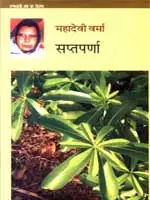|
कविता संग्रह >> सप्तपर्णा सप्तपर्णामहादेवी वर्मा
|
357 पाठक हैं |
|||||||
महादेवी वर्मा का छठा कविता-संग्रह...
Saptparna - A Hindi Book - by Mahadevi Verma
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मनुष्य की स्थूल पार्थिव सत्ता उसकी रंग-रूपमयी आकृति में व्यक्त होती है। उसके बैद्धिक संगठन से जीवन और जगत सम्बन्धी अनेक जिज्ञासाओं, उनके तत्व के शोध और समाधान के प्रयास, चिन्तन की दिशा आदि संचालित और संयमित होते हैं। उसकी रागात्मक वृत्तियों का संघात उसके सौन्दर्य-संवेदन, जीवन और जगत के प्रति आकर्षण-विकर्षण, उन्हें अनुकूल और मधुर बनाने की इच्छा, उसे अन्य मानवों की इच्छा से सम्पृक्त कर अधिक विस्तार देने की कामना और उसकी कर्म-परिणति आदि का सर्जक है।
कृती कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त को
जिनकी षष्ठिपूर्ति के वर्षों ने, नूतन
किशलय-सुमनों में नव नव अवतार
लेने वाले पल्लवों के समान झर
कर सार्थकता पाई है
कृती कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त को
जिनकी षष्ठिपूर्ति के वर्षों ने, नूतन
किशलय-सुमनों में नव नव अवतार
लेने वाले पल्लवों के समान झर
कर सार्थकता पाई है
अपनी बात
एक विशेष भू-खण्ड में जन्म और विकास पाने वाले मानव को अपनी धरती से पार्थिव अस्तित्व ही नहीं प्राप्त होता, उसे अपने परिवेश से विशेष बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता का दाय भी अनायास उपलब्ध हो जाता है। वह स्थूल-सूक्ष्म, बाह्य-आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष-अगोचर ऐसी विशेषताओं का सहज ही उत्तराधिकारी बन जाता है जिनके कारण मानव-समष्टि में सामान्य रहते हुए भी सबसे भिन्न पहचाना जा सकता है। यह सामान्यता में विशेषता न उसे मानव-समष्टि के निकट इतना अपरिचित होने देती है कि उसे आश्चर्य समझा जा सके और न इतना परिचित बना देती है कि उसके सम्बन्ध में जिज्ञासा ही समाप्त हो जाये।
इस प्रकार प्रत्येक भू-खण्ड का मानव दूसरों की जानता भी है और अधिक जानना भी चाहता है।
मनुष्य को स्थूल पार्थिव सत्ता उसकी रंग-रूपमयी आकृति में व्यक्त होती है। उनके बौद्धिक संगठन से, जीवन और जगत सम्बन्धी अनेक जिज्ञासायें, उनके तत्व की शोध और समाधान के प्रयास, चिन्तन की दिशा आदि संचालित और संयमित होते हैं। उसकी रागात्मक वृत्तियों का संघात उसके सौन्दर्य-संवदेन, जीवन और जगत के प्रति आकर्षण-विकर्षण उन्हें अनुकूल और मधुर बनाने की इच्छा, उसे अन्य मानवों की इच्छा से सम्पृक्त कर अधिक विस्तार देने की कामना और उसकी कर्म-परिणति आदि का सर्जक है।
मानव-जाति की इन मूल प्रवृत्तियों के लिए वही सत्य है जो भवभूति ने करुण रस के सम्बन्ध में कहा है-
इस प्रकार प्रत्येक भू-खण्ड का मानव दूसरों की जानता भी है और अधिक जानना भी चाहता है।
मनुष्य को स्थूल पार्थिव सत्ता उसकी रंग-रूपमयी आकृति में व्यक्त होती है। उनके बौद्धिक संगठन से, जीवन और जगत सम्बन्धी अनेक जिज्ञासायें, उनके तत्व की शोध और समाधान के प्रयास, चिन्तन की दिशा आदि संचालित और संयमित होते हैं। उसकी रागात्मक वृत्तियों का संघात उसके सौन्दर्य-संवदेन, जीवन और जगत के प्रति आकर्षण-विकर्षण उन्हें अनुकूल और मधुर बनाने की इच्छा, उसे अन्य मानवों की इच्छा से सम्पृक्त कर अधिक विस्तार देने की कामना और उसकी कर्म-परिणति आदि का सर्जक है।
मानव-जाति की इन मूल प्रवृत्तियों के लिए वही सत्य है जो भवभूति ने करुण रस के सम्बन्ध में कहा है-
एको रसः करुण एव निमित्त भेदा-
दभित्रः पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्त्तान्।
आवर्तबुदबुद् तरंगमयान् विकारा-
नम्भों यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्।।
दभित्रः पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्त्तान्।
आवर्तबुदबुद् तरंगमयान् विकारा-
नम्भों यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्।।
एक करुण रस ही निमित्त भेद से भिन्न-भिन्न मनोविकारों में परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रकार आवर्त, बुदबुद्, तरंग आदि में परिवर्तित जल, जल ही रहता है।
यह निमित्त भेद अर्थात् देश, काल, परिवेश आदि से उत्पन्न विभिन्नातायें, एक मानव या मानव-समूह को दूसरों से सर्वथा भिन्न नहीं कर देतीं, प्रत्युत् वे उसे पार्थिव, बौद्धिक और रागात्मक दृष्टि से विशेष व्यक्तित्व देकर ही मानव सामान्य सत्य के लिए प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।
किसी मानव-समूह को, उसके समस्त परिवेश के साथ तत्वतः जानने के लिए जितने माध्यम उपलब्ध हैं, उनमें सबसे पूर्ण और मधुर उसका साहित्य ही कहा जायगा। साहित्य में मनुष्य का असीम, अतः अपरिचित और दुर्बोध जान पड़ने वाला अन्तर्जगत बाह्य जगत में अवतरित होकर निश्चित परिधि तथा सरल स्पष्टता में बँध जाता है तथा सीमित, अतः चिर-परिचय के कारण पुराना लगने वाला बाह्य जगत अन्तर्जगत के विस्तार में मुक्त होकर चिर नवीन रहस्यमयता पा लेता है। इस प्रकार हमें सीमा में असीम की और असीम में संभावित सीमा की अनुभूति युगपद् होने लगती है। दूसरे शब्दों में, हम कुछ क्षणों में असंख्य अनुभूतियों पर विराट ज्ञान के साथ जीवित रहते हैं, जो स्थिति हमारे सान्त जीवन को अनन्त जीवन से एकाकार कर उसे विशेष सार्थकता और सामान्य गन्तव्य देने की क्षमता रखती है। प्रवाह में बनने मिटने वाली लहर नव-नव रूप पाती हुई लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, परन्तु प्रवाह से भटक कर अकेले तट से टकराने और बिखर जाने वाली तरंग की यात्रा वहीं बालू-मिट्टी में समाप्त हो जाती है। साहित्य हमारे जीवन को, ऐसे एकाकी अन्त से बचा कर उसे जीवन के निरन्तर गतिशील प्रवाह में मिलने का सम्बल देता है।
जहाँ तक परिवर्तन का प्रश्न है, मनुष्य के पार्थिव परिवेश में भी निरन्तर परिवर्तन हो रहा है और उसके जीवन में भी। जहाँ किसी युग में ऊँचे पर्वत थे, वहाँ आज गहरा समुद्र है और जहाँ आज अथाह सागर लहरा रहा है, वहाँ किसी भावी युग में दुर्लध्य पर्वत शिर उठा कर खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन ने भी सफल-असफल संघर्षों के बीच जाग कर, सोकर, चलकर, बैठकर, यात्रा के असंख्य आयाम पार किए हैं। पर न किसी भौगोलिक परिवर्तन से धरती की पार्थिव एकसूत्रता खण्डित हुई है, न परिवेश और जीवन की चिर नवीन स्थितियों में मनुष्य अतीत बसेरों को स्मृति भूला है।
अपने विराट और निरन्तर परिवर्तनशील परिवेश तथा अनदेखे अतीत और केवल कल्पना में स्थिति रखने वाले भविष्य के प्रति मनुष्य की आस्था इतनी विशाल और गुरु है कि उसे सँभालने के लिए उसके एक विराट, अखण्ड और सर्वज्ञ सत्ता को खोज लिया है जो हर अप्रत्यावर्तित अतीत की साक्षी और हर अनागत भविष्य से प्रतिश्रुत है।
हमारा विशाल देश, असंख्य परिवर्तन सँभालने वाली अखण्ड भौगोलिक पीठिका की दृष्टि से विशेष व्यक्तित्व रखता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जाति के बौद्धिक और रागात्मक विकास ने उस पर जो अमिट चरणचिन्ह छोड़े हैं, उन्होंने इसके सब ओर महिमा की विशेष परिधि खींच दी है। यह उसका दाय भी है और न्यास भी।
जिस प्रकार ऊँचे-शिखर पर जल, हिम बन कर शिला-खण्डों के साथ पाषाण रूप में अनन्त काल तक स्थिर भी रह सकता है और अपनी तरलता के साथ प्रपात और प्रपात से नदी बनकर निरन्तर प्रवाहित भी होता रह सकता है, इसी प्रकार मानव-संस्कृति को विकास के एक बिन्दु पर चिर निस्पन्दता भी प्राप्त हो सकती है और अनवरत प्रवाहशीलता भी। एक में एकरस ऊँचाई है और दूसरी स्थिति में समतल पाने के लिए भी पहले उसका निम्नगा होना अनिवार्य ही रहेगा।
धरती के प्रत्येक कोने और काल के प्रत्येक प्रहर में मनुष्य का हृदय किसी उन्नत स्थिति के भी पाषाणीकरण को अभिशाप मानता रहा है। इस स्थिति से बचने के उसने जितने प्रयत्न किये हैं, उनमें साहित्य उसका निरन्तर साक्षी रहा है।
दर्शन पूर्ण होने का दावा कर सकता है, धर्म अपने निर्भ्रान्त होने की घोषणा कर सकता है, परन्तु साहित्य मनुष्य को शक्ति-दुर्बलता जय-पराजय, हास-अश्रु और जीवन-मृत्यु की कथा है। वह मनुष्य रूप में अवतरित होने पर स्वयं ईश्वर को भी पूर्ण मानना अस्वीकार कर देता है।
पर इस स्वेच्छा स्वीकृत अपूर्णता या परिवर्तनशीलता से जीवन और उसके विकास की एकता का सूत्र भंग नहीं होता।
नदी के एक होने का कारण उसका पुरातन जल नहीं, नवीन तरंगभंगिमा है। देश-विशेष के साहित्य के लिए भी यही सत्य है। प्रत्येक युग के साहित्य में नवीन तरंगाकुलता उसे मूल प्रवाहिनी से विच्छिन्न नहीं करती, वरन् उन्हीं नवीन तरंगभंगिमाओं की अनन्त आवृत्तियों के कारणमूल प्रवाहिनी अपने लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति पाती है।
इस दृष्टि से यदि हम भारतीय साहित्य की परीक्षा करें तो काल, स्थिति जीवन, समाज, भाषा धर्म आदि से सम्बन्ध रखने वाले अनन्त परिवर्तनों की भीड़ में भी उसमें एक ऐसी तारतम्यता प्राप्त होगी जिसके अभाव में किसी परिवर्तन की स्थिति सम्भव नहीं रहती। समुद्र की बेला में जो धरती व्यक्त है, उसी की अव्यक्त सत्ता तल बन कर समुद्र की अथाह जलराशि को संभालती है। हमें समुद्र के जल का व्यवधान बने रहने के लिए तल को धरती चाहिए। साहित्य के पुरातन और नूतन के अविच्छिन्न सम्बन्ध के मूल में भी जीवन की ऐसी ही धरती है।
संस्कृति मनुष्य के, बुद्धि और हृदय के जिस परिष्कार और जीवन में उसके व्यक्तीकरण का पर्याय है, उसका दाय विभिन्न भू-खण्डों में बसे हुए मानव-मात्र को प्राप्त है, परन्तु संस्कृति की साहित्य में प्राचीनतम अभिव्यक्ति वेद-साहित्य के अतिरिक्त अन्य नहीं है।
वस्तुतः देश काल की सीमा के परे उक्त साहित्य मानव-जाति के विकास की आदिम गाथा है।
सहस्त्रों वर्षों के व्यवधान के उपरान्त भी भारतीय चिन्तन, अनुभूति, सौंदर्यबोध, आस्था आदि में उसके चिन्ह अमिट हैं। यह तथ्य तब और भी अधिक विस्मयकारक बन जाता है जब हम समय के कुहरे के अनन्त स्तर और अपनी दृष्टि की व्यर्थता का अनुभव करते हैं। पर प्रकृति के जिस नियम से मनुष्य के शरीर को पैतृक दाय के रूप में शक्ति, दुर्बलता, व्याधि विशेष के कीटाणु, रोग विशेष के प्रतिरोध के क्षमता आदि अनजाने ही प्राप्त हो जाते हैं, उसी नियम से उसके मानसिक गठन का प्रभावित होना भी स्वाभाविक कहा जायगा।
जीवन की दृष्टि के वेद-साहित्य इतना अधिक विविध है कि उसके लिए, महाभारत की विशालता व्यक्त करने वाली उक्ति ‘यन्नभारते तन्नभारते’ ही चरितार्थ होती है।
दाशराज्ञ युद्ध जैसे सर्वसंहारी संघर्ष में महाभारत का पूर्वरंग है। अनेक नाटकीय संवादों में नाट्यशास्त्र की भूमिका है। विभिन्न-विचारों के प्रतिपादन में दर्शन की अनेक आस्तिक नास्तिक सरणियों की उदार स्वीकृति है। जल, स्थल, अन्तरिक्ष आकाश आदि के व्याप्त शक्तियों की रूपात्मक अनुभूति और उनके रागात्मक अभिनन्दन में काव्य और कलाओं के विकास के इंगित हैं। व्यक्ति और समष्टि की कल्याण कामनाओं में जीवन के नैतिक मूल्यों के निर्देश हैं। कर्म के विस्तृत विवेचन में कर्तव्य की रेखायें आँकी गई हैं। व्यापक कोमल कल्पना के छायालोक में, जीवन के कठोर सीमित यथार्थ चित्रों ने धरती के निकट रहने का संकेत दिया है।
भारतीय जीवन में स्थूल कर्म से लेकर सूक्ष्म बौद्धिक प्रक्रिया और गम्भीर रागात्मकता तक जो विशेषतायें हैं, उनका तत्वतः अनुसन्धान हमें किसी न किसी पथ में इस वृहत जीवन-कोष के समीप पहुँचाए बिना नहीं रहता।
इसका तात्पर्य यह नहीं कि वर्तमान अतीत की अनुकृति मात्र है। पर हम यदि मानव जीवन की निरन्तर और किसी सामान्य लक्ष्योन्मुख गतिशीलता को स्वीकृति देते हैं तो उसकी यात्रा के आरम्भ का कोई बिन्दु स्वीकार करना ही होगा, जो गन्तव्य के चरम और अन्तिम बिन्दु से अदृष्ट रहकर भी उससे विच्छिन्न नहीं हो सकता। विकास पथ का एक होना, यात्रियों की विभिन्नता, उनकी शक्तियों की विषमता, पाथेय की विविधता और गति की अनेकता को अस्वीकार नहीं करता। इतना ही नहीं वह चलने वालों की बौद्धिक और रागात्मक वृत्तियों की मुक्तावस्था को भी किसी संकीर्ण क्षितिज से नहीं घेरता।
धर्मग्रन्थों के लिए मनुष्य की एकांगी दृष्टि ऐसा अंधेरा बन्दीगृह बन जाती है, जिसमें उनकी उज्ज्वल रेखाएँ भी धूमिल हो जाती हैं। एक ओर धर्मविशेष के प्रति आस्थावान तत्सम्बन्धी ग्रन्थों के चतुर्दिक, अपने अन्धविश्वास और रूढ़िवादिता को अग्निरेखा खींच देते हैं और दूसरी ओर भिन्न धर्मपद्धति के अनुयायी अपने चारों ओर उपेक्षा की इतनी ऊँची दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जिन्हें अन्य दिशा से आने वाली वायु के पंख भी नहीं छू पाते। ऐसी स्थिति में धर्मग्रन्थ, अनजान कृपण की रत्नमंजूषा बन जाते हैं, जिसके यथार्थ मूल्याकन में एक ओऱ मोहान्धता बाधक है और दूसरी ओर अपरिचयजनित उपेक्षा।
वह स्वाभाविक ही है कि धर्मग्रन्थों की सीमा के भीतर रहकर अपना परिचय देने वाले साहित्य को भी इस भ्रान्त परिचय और अपरिचय का अभिशाप झेलना पड़ा। ऐसे धर्मग्रन्थों की संख्या अधिक है जो अपने कथ्य की मर्मस्पर्शी सामान्यता, शैली की मधुर स्पष्टता और भाषा के सहज सात्विक प्रवाह के कारण साहित्य की कोटि में स्थिति रखते हैं, परन्तु उनके लिए साहित्य की देश-काल-सम्प्रदायातीत मुक्ति दुर्लभ ही रहेगी।
वेद साहित्य संकीर्ण अर्थ में धर्म विशेष का परिचायक ग्रन्थ-समूह नहीं है। उसमें न किसी धर्म विशेष के संस्थापक के प्रवचनों का संग्रह है और न किसी एक धर्म की आचार-पद्धित या मतवाद का प्रतिष्ठापन या प्रतिपादन है।
यह निमित्त भेद अर्थात् देश, काल, परिवेश आदि से उत्पन्न विभिन्नातायें, एक मानव या मानव-समूह को दूसरों से सर्वथा भिन्न नहीं कर देतीं, प्रत्युत् वे उसे पार्थिव, बौद्धिक और रागात्मक दृष्टि से विशेष व्यक्तित्व देकर ही मानव सामान्य सत्य के लिए प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।
किसी मानव-समूह को, उसके समस्त परिवेश के साथ तत्वतः जानने के लिए जितने माध्यम उपलब्ध हैं, उनमें सबसे पूर्ण और मधुर उसका साहित्य ही कहा जायगा। साहित्य में मनुष्य का असीम, अतः अपरिचित और दुर्बोध जान पड़ने वाला अन्तर्जगत बाह्य जगत में अवतरित होकर निश्चित परिधि तथा सरल स्पष्टता में बँध जाता है तथा सीमित, अतः चिर-परिचय के कारण पुराना लगने वाला बाह्य जगत अन्तर्जगत के विस्तार में मुक्त होकर चिर नवीन रहस्यमयता पा लेता है। इस प्रकार हमें सीमा में असीम की और असीम में संभावित सीमा की अनुभूति युगपद् होने लगती है। दूसरे शब्दों में, हम कुछ क्षणों में असंख्य अनुभूतियों पर विराट ज्ञान के साथ जीवित रहते हैं, जो स्थिति हमारे सान्त जीवन को अनन्त जीवन से एकाकार कर उसे विशेष सार्थकता और सामान्य गन्तव्य देने की क्षमता रखती है। प्रवाह में बनने मिटने वाली लहर नव-नव रूप पाती हुई लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, परन्तु प्रवाह से भटक कर अकेले तट से टकराने और बिखर जाने वाली तरंग की यात्रा वहीं बालू-मिट्टी में समाप्त हो जाती है। साहित्य हमारे जीवन को, ऐसे एकाकी अन्त से बचा कर उसे जीवन के निरन्तर गतिशील प्रवाह में मिलने का सम्बल देता है।
जहाँ तक परिवर्तन का प्रश्न है, मनुष्य के पार्थिव परिवेश में भी निरन्तर परिवर्तन हो रहा है और उसके जीवन में भी। जहाँ किसी युग में ऊँचे पर्वत थे, वहाँ आज गहरा समुद्र है और जहाँ आज अथाह सागर लहरा रहा है, वहाँ किसी भावी युग में दुर्लध्य पर्वत शिर उठा कर खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन ने भी सफल-असफल संघर्षों के बीच जाग कर, सोकर, चलकर, बैठकर, यात्रा के असंख्य आयाम पार किए हैं। पर न किसी भौगोलिक परिवर्तन से धरती की पार्थिव एकसूत्रता खण्डित हुई है, न परिवेश और जीवन की चिर नवीन स्थितियों में मनुष्य अतीत बसेरों को स्मृति भूला है।
अपने विराट और निरन्तर परिवर्तनशील परिवेश तथा अनदेखे अतीत और केवल कल्पना में स्थिति रखने वाले भविष्य के प्रति मनुष्य की आस्था इतनी विशाल और गुरु है कि उसे सँभालने के लिए उसके एक विराट, अखण्ड और सर्वज्ञ सत्ता को खोज लिया है जो हर अप्रत्यावर्तित अतीत की साक्षी और हर अनागत भविष्य से प्रतिश्रुत है।
हमारा विशाल देश, असंख्य परिवर्तन सँभालने वाली अखण्ड भौगोलिक पीठिका की दृष्टि से विशेष व्यक्तित्व रखता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जाति के बौद्धिक और रागात्मक विकास ने उस पर जो अमिट चरणचिन्ह छोड़े हैं, उन्होंने इसके सब ओर महिमा की विशेष परिधि खींच दी है। यह उसका दाय भी है और न्यास भी।
जिस प्रकार ऊँचे-शिखर पर जल, हिम बन कर शिला-खण्डों के साथ पाषाण रूप में अनन्त काल तक स्थिर भी रह सकता है और अपनी तरलता के साथ प्रपात और प्रपात से नदी बनकर निरन्तर प्रवाहित भी होता रह सकता है, इसी प्रकार मानव-संस्कृति को विकास के एक बिन्दु पर चिर निस्पन्दता भी प्राप्त हो सकती है और अनवरत प्रवाहशीलता भी। एक में एकरस ऊँचाई है और दूसरी स्थिति में समतल पाने के लिए भी पहले उसका निम्नगा होना अनिवार्य ही रहेगा।
धरती के प्रत्येक कोने और काल के प्रत्येक प्रहर में मनुष्य का हृदय किसी उन्नत स्थिति के भी पाषाणीकरण को अभिशाप मानता रहा है। इस स्थिति से बचने के उसने जितने प्रयत्न किये हैं, उनमें साहित्य उसका निरन्तर साक्षी रहा है।
दर्शन पूर्ण होने का दावा कर सकता है, धर्म अपने निर्भ्रान्त होने की घोषणा कर सकता है, परन्तु साहित्य मनुष्य को शक्ति-दुर्बलता जय-पराजय, हास-अश्रु और जीवन-मृत्यु की कथा है। वह मनुष्य रूप में अवतरित होने पर स्वयं ईश्वर को भी पूर्ण मानना अस्वीकार कर देता है।
पर इस स्वेच्छा स्वीकृत अपूर्णता या परिवर्तनशीलता से जीवन और उसके विकास की एकता का सूत्र भंग नहीं होता।
नदी के एक होने का कारण उसका पुरातन जल नहीं, नवीन तरंगभंगिमा है। देश-विशेष के साहित्य के लिए भी यही सत्य है। प्रत्येक युग के साहित्य में नवीन तरंगाकुलता उसे मूल प्रवाहिनी से विच्छिन्न नहीं करती, वरन् उन्हीं नवीन तरंगभंगिमाओं की अनन्त आवृत्तियों के कारणमूल प्रवाहिनी अपने लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति पाती है।
इस दृष्टि से यदि हम भारतीय साहित्य की परीक्षा करें तो काल, स्थिति जीवन, समाज, भाषा धर्म आदि से सम्बन्ध रखने वाले अनन्त परिवर्तनों की भीड़ में भी उसमें एक ऐसी तारतम्यता प्राप्त होगी जिसके अभाव में किसी परिवर्तन की स्थिति सम्भव नहीं रहती। समुद्र की बेला में जो धरती व्यक्त है, उसी की अव्यक्त सत्ता तल बन कर समुद्र की अथाह जलराशि को संभालती है। हमें समुद्र के जल का व्यवधान बने रहने के लिए तल को धरती चाहिए। साहित्य के पुरातन और नूतन के अविच्छिन्न सम्बन्ध के मूल में भी जीवन की ऐसी ही धरती है।
संस्कृति मनुष्य के, बुद्धि और हृदय के जिस परिष्कार और जीवन में उसके व्यक्तीकरण का पर्याय है, उसका दाय विभिन्न भू-खण्डों में बसे हुए मानव-मात्र को प्राप्त है, परन्तु संस्कृति की साहित्य में प्राचीनतम अभिव्यक्ति वेद-साहित्य के अतिरिक्त अन्य नहीं है।
वस्तुतः देश काल की सीमा के परे उक्त साहित्य मानव-जाति के विकास की आदिम गाथा है।
सहस्त्रों वर्षों के व्यवधान के उपरान्त भी भारतीय चिन्तन, अनुभूति, सौंदर्यबोध, आस्था आदि में उसके चिन्ह अमिट हैं। यह तथ्य तब और भी अधिक विस्मयकारक बन जाता है जब हम समय के कुहरे के अनन्त स्तर और अपनी दृष्टि की व्यर्थता का अनुभव करते हैं। पर प्रकृति के जिस नियम से मनुष्य के शरीर को पैतृक दाय के रूप में शक्ति, दुर्बलता, व्याधि विशेष के कीटाणु, रोग विशेष के प्रतिरोध के क्षमता आदि अनजाने ही प्राप्त हो जाते हैं, उसी नियम से उसके मानसिक गठन का प्रभावित होना भी स्वाभाविक कहा जायगा।
जीवन की दृष्टि के वेद-साहित्य इतना अधिक विविध है कि उसके लिए, महाभारत की विशालता व्यक्त करने वाली उक्ति ‘यन्नभारते तन्नभारते’ ही चरितार्थ होती है।
दाशराज्ञ युद्ध जैसे सर्वसंहारी संघर्ष में महाभारत का पूर्वरंग है। अनेक नाटकीय संवादों में नाट्यशास्त्र की भूमिका है। विभिन्न-विचारों के प्रतिपादन में दर्शन की अनेक आस्तिक नास्तिक सरणियों की उदार स्वीकृति है। जल, स्थल, अन्तरिक्ष आकाश आदि के व्याप्त शक्तियों की रूपात्मक अनुभूति और उनके रागात्मक अभिनन्दन में काव्य और कलाओं के विकास के इंगित हैं। व्यक्ति और समष्टि की कल्याण कामनाओं में जीवन के नैतिक मूल्यों के निर्देश हैं। कर्म के विस्तृत विवेचन में कर्तव्य की रेखायें आँकी गई हैं। व्यापक कोमल कल्पना के छायालोक में, जीवन के कठोर सीमित यथार्थ चित्रों ने धरती के निकट रहने का संकेत दिया है।
भारतीय जीवन में स्थूल कर्म से लेकर सूक्ष्म बौद्धिक प्रक्रिया और गम्भीर रागात्मकता तक जो विशेषतायें हैं, उनका तत्वतः अनुसन्धान हमें किसी न किसी पथ में इस वृहत जीवन-कोष के समीप पहुँचाए बिना नहीं रहता।
इसका तात्पर्य यह नहीं कि वर्तमान अतीत की अनुकृति मात्र है। पर हम यदि मानव जीवन की निरन्तर और किसी सामान्य लक्ष्योन्मुख गतिशीलता को स्वीकृति देते हैं तो उसकी यात्रा के आरम्भ का कोई बिन्दु स्वीकार करना ही होगा, जो गन्तव्य के चरम और अन्तिम बिन्दु से अदृष्ट रहकर भी उससे विच्छिन्न नहीं हो सकता। विकास पथ का एक होना, यात्रियों की विभिन्नता, उनकी शक्तियों की विषमता, पाथेय की विविधता और गति की अनेकता को अस्वीकार नहीं करता। इतना ही नहीं वह चलने वालों की बौद्धिक और रागात्मक वृत्तियों की मुक्तावस्था को भी किसी संकीर्ण क्षितिज से नहीं घेरता।
धर्मग्रन्थों के लिए मनुष्य की एकांगी दृष्टि ऐसा अंधेरा बन्दीगृह बन जाती है, जिसमें उनकी उज्ज्वल रेखाएँ भी धूमिल हो जाती हैं। एक ओर धर्मविशेष के प्रति आस्थावान तत्सम्बन्धी ग्रन्थों के चतुर्दिक, अपने अन्धविश्वास और रूढ़िवादिता को अग्निरेखा खींच देते हैं और दूसरी ओर भिन्न धर्मपद्धति के अनुयायी अपने चारों ओर उपेक्षा की इतनी ऊँची दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जिन्हें अन्य दिशा से आने वाली वायु के पंख भी नहीं छू पाते। ऐसी स्थिति में धर्मग्रन्थ, अनजान कृपण की रत्नमंजूषा बन जाते हैं, जिसके यथार्थ मूल्याकन में एक ओऱ मोहान्धता बाधक है और दूसरी ओर अपरिचयजनित उपेक्षा।
वह स्वाभाविक ही है कि धर्मग्रन्थों की सीमा के भीतर रहकर अपना परिचय देने वाले साहित्य को भी इस भ्रान्त परिचय और अपरिचय का अभिशाप झेलना पड़ा। ऐसे धर्मग्रन्थों की संख्या अधिक है जो अपने कथ्य की मर्मस्पर्शी सामान्यता, शैली की मधुर स्पष्टता और भाषा के सहज सात्विक प्रवाह के कारण साहित्य की कोटि में स्थिति रखते हैं, परन्तु उनके लिए साहित्य की देश-काल-सम्प्रदायातीत मुक्ति दुर्लभ ही रहेगी।
वेद साहित्य संकीर्ण अर्थ में धर्म विशेष का परिचायक ग्रन्थ-समूह नहीं है। उसमें न किसी धर्म विशेष के संस्थापक के प्रवचनों का संग्रह है और न किसी एक धर्म की आचार-पद्धित या मतवाद का प्रतिष्ठापन या प्रतिपादन है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i