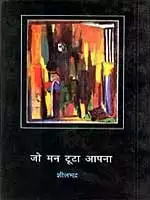|
विविध उपन्यास >> जो मन टूटा आपना जो मन टूटा आपनाशीलभद्र
|
43 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत उपन्यास का असमिया से हिन्दी रूपान्यतर...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रस्तुत है साहित्य अकादेमी सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित
असमिया के सुविख्यात कथाकार का यह उपन्यास ‘जो मन टूटा
आपना’। मन की अतल गहराइयों में पैठकर उसमें छिपे हर
गुण-अवगुण,हर शक्ति, हर कमजोरी,हर सुन्दर-असुन्दर को ऊपर निकाल रखने और इस
उपक्रम में अपने समकालीन समाज को आँखों-आगे प्रत्यक्ष रख देने की दुर्लभ
क्षमता श्री शीलभद्र ने ‘जो मन टूटा आपना’ में दिखाई
है। इस उपन्यास की कथा परिवेशगत यथार्थ की आकार-रेखाओं को उजागर करने के
साथ ही उसके भीतर के बहुरंगी अर्थों को भी खोजती और व्यक्त करती है।
‘जो मन टूटा आपना’ में शीलभद्र जी ने अपने व्यापक
अनुभवों की पृष्टभूमि में व्यक्ति की मानसिक व्यथाओं और आसपास के वातावरण
में छायी व्यर्थता का लेखाजोखा पूरी कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है।
दरअसल जीवन की विविधताओं की पड़ताल करता यह उपन्यास अपने चरित्रों और
प्रसंगों के माध्यम से जटिल मानवीय सम्बन्धों की एक विलक्षण अभिव्यक्ति है।
जो मन टूटा आपना
बाहर की ओर आँखें खोलकर तो देख ही नहीं सकते। सूरज की तीखी किरणें चारों
ओर से झपट्टामार घेरकर चौंधिया देती हैं। तनिक-सी हवा का भी पता नहीं,
पूरा वातावरण गुम्म पड़ा है। प्रखर प्रकृति ने महारुद्र रुप धारण कर लिया
है। सभी कुछ तवे-सा जल-धधक रहा है। ऊपर से इस पूरे इलाके में बड़े भोर से
ही बिजली लाइन आने का क्रम भंग हो गया है। बिजली होती तो कुछ पंखा-वंखा भी
चलता। मध्य दुपहरी तो ऐसी धधक रही है कि बिछौने पर सोये भी नहीं रहा जा
सकता, बैठे भी नहीं रहा जा सकता। ललाट और मुँह पर जो पसीना उमड़-उमड़कर
बहने लगा है उसे पोंछने से भी कोई लाभ नहीं होनेवाला। पोंछ भी दो तो भी
फिर तुरन्त ही रिस-रिसकर पसीने की बूँदें चुकचुकाकर छलकने लगेंगी। पसीने
की छोटी-छोटी उभरती बूँदें एक-दूसरे से सट-सटकर ऐसी मोटी हो जाती हैं कि
अपने भार से फिर टप्प-टप्प कर आँखों की पलकों पर आ गिरती हैं। कुछ नाक की
नोक पर पहुँच कर वहाँ से लुढ़कने लगती हैं।
इस कदर की प्रचण्ड गरमी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ थम गया है। नहीं, आदमियों के काम-काज ठप्प नहीं हो गये हैं। भृगु चौधुरी के मकान के बिलकुल पास ही गोयेनका एक महाविशाल अट्टालिका बनवा रहे हैं। इस भरी दुपहरी में भी उनके यहाँ हो रहे काम की रफ्तार में तनिक भी कमी नहीं आयी है। लगातार एक-सी ही तेजी से काम बढ़ता जा रहा है। भृगु चौधुरी के पड़ोसी जो महेन्द्र दास थे, उन्हीं की जमीन को खरीदकर गोयेनका वहाँ अब यह विशाल भवन बनवा रहे हैं। यह भवन ऊपर उठते-उठते कितनी ऊँचाई तक उठेगा, इसका अनुमान लगा पाना भी कठिन है, उठ रहा है तो उठता ही चला जा रहा है ऊपर-और ऊपर।
भृगु चौधुरी की सोचने की चिन्ताधारा आजकल इधर-उधर भटकती रहती है, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के चक्कर खाती रहती है। कोई एक दृश्य देखकर, अथवा कोई एक शब्द सुनकर, उसी का सूत्र पकड़कर वे ऐसे दृश्य दृश्यान्तरों में जा पहुँचते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता।
कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ है। अभी कोई बहुत अधिक समय थोडे़ ही बीता है, गुवाहाटी में रहनेवाला कोई भी बड़ा-बूढ़ा आदमी बड़ी स्पष्टता से बता सकता है कि साँझ-ढलने के बाद इस शहर के मुहल्ले शिलपुखरी की पोखर के पूरब की ओर के इन इलाकों की ओर आने में आदमी डर के मारे काँपने लगते थे। (आज यह सब जो जाक-जमक पूर्ण नगर है) जंगली वृक्षों, झाड़ियों, झाड़-झंखाड़ों से भरा हुआ, अथवा बीच-बीच में जहाँ-तहाँ खेतों मैदानों से भरा हुआ, यह भाग ऐसा जन-मानवहीन था, कि बस बीच-बीच में कहीं-कहीं कुछ आदिवासी जनजातियों के गाँव-घर छिटके-छितराये थे।
शिलपुखरी की पुष्करणी के आस-पास जलावन की लकड़ी, बाँस-काठ के टुकड़ों के गट्ठर के गट्ठर बिकते थे। एक प्रकार से उसे लकड़ी घास-फूस का बाजार ही कह सकते थे। (यह सारा कुछ जंगलों से काट-कूट, बीन-बानकर जो जनजातीय मनुष्य ले आते थे) वे जनजातीय मनुष्य तो अब जैसे लुप्त ही हो गये। इस शहराती चकाचौंध में वे सब जाने कहाँ खो गये। अत्यधिक चतुर-चालाक और बलवान आदमियों की बढ़ती हुई ताकत को रोक पाने में नाकामयाब हो, वे पीछे-और पीछे हटते-हटते जाने पीछे कितनी दूर चले गये हैं।
आगे जो दौर आनेवाला है, उसमें ठीक यही दशा शहर के शेष स्थानीय निवासियों की भी होगी। शहर के इस भाग में भृगु चौधुरी ने जिस समय मकान बनवाना शुरू किया था, उस समय इधर और आदमी जन नहीं रहते थे। इसी से उनके जो थोड़े से शुभचिन्तक लोग थे, उन सभी ने उन्हें मना किया था, ‘‘अरे भाई ! यह तू क्या करने जा रहा है रे। दिन-दुपहरी में ही बाघ-शेर उठा ले जाएँगे, इसका कुछ थाह-पता भी पा सकोगे ?’’
आज चारों ओर से ऊँची-ऊँची विशाल अट्टालिकाओं ने उनके घर को चारों ओर से घेरकर चाँप रखा है। ये अट्टालिकाएँ रुपये-पैसे से गुच्च महाधनाढ्य लोगों की हैं। इन महाधनाढ्यों में अधिकांश बहुत दूर से आये हुए व्यापारी हैं। कुछ समय पहले तक महेन्द्र दास मजाक-मजाक में कहा करता था, ‘‘मकान बनाने के लिए यह जो प्लाट की थोड़ी-सी जमीन मेरी पड़ी है, अगर इसे ही बेचने की बात प्रचारित कर दूँ, तो एक लाख रुपये पा जाऊँगा।’’-और सच्चाई तो यह कि उसके थोड़े समय बाद ही उसने जमीन का यह टुकड़ा तीन लाख में बेच भी दिया। गोयेनका ने खुशी-खुशी खरीद लिया। और फिर तीन लाख ही क्यों ? अगर वह इसका दाम पाँच लाख माँगता तो वह भी पा जाता। परिस्थिति अब ऐसी है जिन्हें जमीन की जरूरत है, उन्हें तो बस जमीन ही चाहिए, वह चाहे जैसे मिले, दर-दम की तो कोई परवाह ही नहीं। जान पड़ता है कि कुछ समय बाद जो जमाना आनेवाला है, उस समय तक तो नौकरी-चाकरी करनेवाले मनुष्य अथवा साधारण स्तर की कमाई करनेवाले लोग मान-सम्मान के साथ, भले ढंग से शहर में रह ही नहीं पाएँगे। शहर छोड़कर कहीं दूर भाग जाना पड़ेगा उन्हें।
महेन्द्र दास के दो बेटे हैं। दोनों ही काफी समय से अमेरिका में रहते हैं। उनकी अपनी धर्मपत्नी तो कभी की स्वर्ग सिधार चुकी हैं। सो, जमीन का यह टुकड़ा बेच देने के बाद महेन्द्र दास घूम-घूमकर जैसे स्पष्टीकरण देता फिरता था-
‘‘यहाँ (घर बनाकर) अकेले-अकेले भूत की तरह रह रहकर क्या करूँगा, भाई ! गाँव में इतना बड़ा घर-द्वार यूँ ही पड़ा हुआ है। वहाँ रहने में यह तो सुख है ही कि अगर वहाँ रहते-रहते मृत्यु हो गयी तो जो भतीजे वगैरह हैं, वे मुँह में कम-से-कम एक चुल्लू पानी तो डाल सकेंगे।’’
बड़ी अच्छी बात है। बड़ी ही सुन्दर युक्ति है।
परन्तु आदमी जैसा सोचता है, ठीक उसी प्रकार का काम तो होता नहीं। अब महेन्द्र दास को ही लो। अभी बीते कल के दिन ही महेन्द्र दास भृगु चौधुरी के घर आ पधारे थे। लेकिन कैसे ? एकदम शान्त, मौन-गम्भीर। हमेशा चुहुलबाजी करते, हँसी-ठठ्टा उड़ाते रहनेवाला बतक्कड़ आदमी इस रूप में कि मुँह से कोई बोल ही नहीं फूट रहा था। दुःख विषाद की प्रतिमूर्ति बना-सा।
‘‘खुद अपना ही गुह खुद अपने से खानेवाले आदमी जैसा महा बुरबकिया काम कर डाला था ऐ चौधुरी ! खीझ तो ऐसी कि अपने ही हाथों अपने गाल पर चाँटा लगाने का मन करता है। गाँव में जो भतीजे छोकरे सब हैं, वे बस एकमात्र इस घात में हैं कि मेरा जो कुछ भी रुपया-पैसा, धन-सम्पत्ति है, उसे कैसे हथिया लें। अब तो उनका आतंक इतना भयानक हो उठा है कि वे जैसे ही रुपया माँगते हैं, तुरन्त वैसे ही उन्हें रुपये न दे दो तो गर्दन चाँप कर कहीं मार ही न डालें, यही डर बराबर बना रहता है। ऐसी हालत में अब क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।’’
उसकी बात सुनकर भृगु चौधुरी ने सहज-सरल ढंग से ही कहा था, ‘‘इसमें सोचने-विचारने की क्या बात ? इस समय तो तुम्हारे हाथ में काफी रुपया है। अमेरिका (अपने बेटों के पास) ही क्यों नहीं चले जाते ?’’ ऐसा कहने के पीछे उन्हें चिढ़ाने का कोई मतलब भृगु चौधुरी का नहीं था। परन्तु महेन्द्र दास अचानक ही चिढ़कर खंगार हो उठा। किरमिसाता हुआ चीख पड़ा, ‘‘मेरी हँसी उड़ा रहे हो ? आप मुझे बेवकूफ समझकर हँसी-ठट्टा कर रहे हो ? अरे बेटे ऐसे नालायक हैं कि पत्र भेजते-भेजते थक गये, किसी एक का उत्तर तक नहीं देते। आज कितने युग बीत गये, उन्होंने कोई खोज-खबर तक नहीं ली। इसका भी थाह-पता नहीं किया कि मर गया कि अभी जिन्दा हूँ।’’
इतना कहकर भला आदमी फुक्का मारकर रोने लगा। भृगु चौधुरी तो अवाक् रह गये, जैसे सारी सिट्टी-पिट्टी ही गुम हो गयी हो। अब भला ये सब बातें वे कैसे जानते होंगे ? महेन्द्र दास तो हमेशा उनसे, या उनसे से ही क्यों, हर एक आदमी से यही कहता फिर रहा है कि उसके प्यारे बेटे उसे बराबर अपने पास बुलाते ही रहते हैं। कहते हैं कि वहाँ अकेले-अकेले पड़े रहने की क्या जरूरत है ? वह सब छोड़-छाड़कर हम लोगों के पास ही क्यों नहीं चले आते ?
इस कदर की प्रचण्ड गरमी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ थम गया है। नहीं, आदमियों के काम-काज ठप्प नहीं हो गये हैं। भृगु चौधुरी के मकान के बिलकुल पास ही गोयेनका एक महाविशाल अट्टालिका बनवा रहे हैं। इस भरी दुपहरी में भी उनके यहाँ हो रहे काम की रफ्तार में तनिक भी कमी नहीं आयी है। लगातार एक-सी ही तेजी से काम बढ़ता जा रहा है। भृगु चौधुरी के पड़ोसी जो महेन्द्र दास थे, उन्हीं की जमीन को खरीदकर गोयेनका वहाँ अब यह विशाल भवन बनवा रहे हैं। यह भवन ऊपर उठते-उठते कितनी ऊँचाई तक उठेगा, इसका अनुमान लगा पाना भी कठिन है, उठ रहा है तो उठता ही चला जा रहा है ऊपर-और ऊपर।
भृगु चौधुरी की सोचने की चिन्ताधारा आजकल इधर-उधर भटकती रहती है, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के चक्कर खाती रहती है। कोई एक दृश्य देखकर, अथवा कोई एक शब्द सुनकर, उसी का सूत्र पकड़कर वे ऐसे दृश्य दृश्यान्तरों में जा पहुँचते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता।
कितनी तेजी से परिवर्तन हुआ है। अभी कोई बहुत अधिक समय थोडे़ ही बीता है, गुवाहाटी में रहनेवाला कोई भी बड़ा-बूढ़ा आदमी बड़ी स्पष्टता से बता सकता है कि साँझ-ढलने के बाद इस शहर के मुहल्ले शिलपुखरी की पोखर के पूरब की ओर के इन इलाकों की ओर आने में आदमी डर के मारे काँपने लगते थे। (आज यह सब जो जाक-जमक पूर्ण नगर है) जंगली वृक्षों, झाड़ियों, झाड़-झंखाड़ों से भरा हुआ, अथवा बीच-बीच में जहाँ-तहाँ खेतों मैदानों से भरा हुआ, यह भाग ऐसा जन-मानवहीन था, कि बस बीच-बीच में कहीं-कहीं कुछ आदिवासी जनजातियों के गाँव-घर छिटके-छितराये थे।
शिलपुखरी की पुष्करणी के आस-पास जलावन की लकड़ी, बाँस-काठ के टुकड़ों के गट्ठर के गट्ठर बिकते थे। एक प्रकार से उसे लकड़ी घास-फूस का बाजार ही कह सकते थे। (यह सारा कुछ जंगलों से काट-कूट, बीन-बानकर जो जनजातीय मनुष्य ले आते थे) वे जनजातीय मनुष्य तो अब जैसे लुप्त ही हो गये। इस शहराती चकाचौंध में वे सब जाने कहाँ खो गये। अत्यधिक चतुर-चालाक और बलवान आदमियों की बढ़ती हुई ताकत को रोक पाने में नाकामयाब हो, वे पीछे-और पीछे हटते-हटते जाने पीछे कितनी दूर चले गये हैं।
आगे जो दौर आनेवाला है, उसमें ठीक यही दशा शहर के शेष स्थानीय निवासियों की भी होगी। शहर के इस भाग में भृगु चौधुरी ने जिस समय मकान बनवाना शुरू किया था, उस समय इधर और आदमी जन नहीं रहते थे। इसी से उनके जो थोड़े से शुभचिन्तक लोग थे, उन सभी ने उन्हें मना किया था, ‘‘अरे भाई ! यह तू क्या करने जा रहा है रे। दिन-दुपहरी में ही बाघ-शेर उठा ले जाएँगे, इसका कुछ थाह-पता भी पा सकोगे ?’’
आज चारों ओर से ऊँची-ऊँची विशाल अट्टालिकाओं ने उनके घर को चारों ओर से घेरकर चाँप रखा है। ये अट्टालिकाएँ रुपये-पैसे से गुच्च महाधनाढ्य लोगों की हैं। इन महाधनाढ्यों में अधिकांश बहुत दूर से आये हुए व्यापारी हैं। कुछ समय पहले तक महेन्द्र दास मजाक-मजाक में कहा करता था, ‘‘मकान बनाने के लिए यह जो प्लाट की थोड़ी-सी जमीन मेरी पड़ी है, अगर इसे ही बेचने की बात प्रचारित कर दूँ, तो एक लाख रुपये पा जाऊँगा।’’-और सच्चाई तो यह कि उसके थोड़े समय बाद ही उसने जमीन का यह टुकड़ा तीन लाख में बेच भी दिया। गोयेनका ने खुशी-खुशी खरीद लिया। और फिर तीन लाख ही क्यों ? अगर वह इसका दाम पाँच लाख माँगता तो वह भी पा जाता। परिस्थिति अब ऐसी है जिन्हें जमीन की जरूरत है, उन्हें तो बस जमीन ही चाहिए, वह चाहे जैसे मिले, दर-दम की तो कोई परवाह ही नहीं। जान पड़ता है कि कुछ समय बाद जो जमाना आनेवाला है, उस समय तक तो नौकरी-चाकरी करनेवाले मनुष्य अथवा साधारण स्तर की कमाई करनेवाले लोग मान-सम्मान के साथ, भले ढंग से शहर में रह ही नहीं पाएँगे। शहर छोड़कर कहीं दूर भाग जाना पड़ेगा उन्हें।
महेन्द्र दास के दो बेटे हैं। दोनों ही काफी समय से अमेरिका में रहते हैं। उनकी अपनी धर्मपत्नी तो कभी की स्वर्ग सिधार चुकी हैं। सो, जमीन का यह टुकड़ा बेच देने के बाद महेन्द्र दास घूम-घूमकर जैसे स्पष्टीकरण देता फिरता था-
‘‘यहाँ (घर बनाकर) अकेले-अकेले भूत की तरह रह रहकर क्या करूँगा, भाई ! गाँव में इतना बड़ा घर-द्वार यूँ ही पड़ा हुआ है। वहाँ रहने में यह तो सुख है ही कि अगर वहाँ रहते-रहते मृत्यु हो गयी तो जो भतीजे वगैरह हैं, वे मुँह में कम-से-कम एक चुल्लू पानी तो डाल सकेंगे।’’
बड़ी अच्छी बात है। बड़ी ही सुन्दर युक्ति है।
परन्तु आदमी जैसा सोचता है, ठीक उसी प्रकार का काम तो होता नहीं। अब महेन्द्र दास को ही लो। अभी बीते कल के दिन ही महेन्द्र दास भृगु चौधुरी के घर आ पधारे थे। लेकिन कैसे ? एकदम शान्त, मौन-गम्भीर। हमेशा चुहुलबाजी करते, हँसी-ठठ्टा उड़ाते रहनेवाला बतक्कड़ आदमी इस रूप में कि मुँह से कोई बोल ही नहीं फूट रहा था। दुःख विषाद की प्रतिमूर्ति बना-सा।
‘‘खुद अपना ही गुह खुद अपने से खानेवाले आदमी जैसा महा बुरबकिया काम कर डाला था ऐ चौधुरी ! खीझ तो ऐसी कि अपने ही हाथों अपने गाल पर चाँटा लगाने का मन करता है। गाँव में जो भतीजे छोकरे सब हैं, वे बस एकमात्र इस घात में हैं कि मेरा जो कुछ भी रुपया-पैसा, धन-सम्पत्ति है, उसे कैसे हथिया लें। अब तो उनका आतंक इतना भयानक हो उठा है कि वे जैसे ही रुपया माँगते हैं, तुरन्त वैसे ही उन्हें रुपये न दे दो तो गर्दन चाँप कर कहीं मार ही न डालें, यही डर बराबर बना रहता है। ऐसी हालत में अब क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।’’
उसकी बात सुनकर भृगु चौधुरी ने सहज-सरल ढंग से ही कहा था, ‘‘इसमें सोचने-विचारने की क्या बात ? इस समय तो तुम्हारे हाथ में काफी रुपया है। अमेरिका (अपने बेटों के पास) ही क्यों नहीं चले जाते ?’’ ऐसा कहने के पीछे उन्हें चिढ़ाने का कोई मतलब भृगु चौधुरी का नहीं था। परन्तु महेन्द्र दास अचानक ही चिढ़कर खंगार हो उठा। किरमिसाता हुआ चीख पड़ा, ‘‘मेरी हँसी उड़ा रहे हो ? आप मुझे बेवकूफ समझकर हँसी-ठट्टा कर रहे हो ? अरे बेटे ऐसे नालायक हैं कि पत्र भेजते-भेजते थक गये, किसी एक का उत्तर तक नहीं देते। आज कितने युग बीत गये, उन्होंने कोई खोज-खबर तक नहीं ली। इसका भी थाह-पता नहीं किया कि मर गया कि अभी जिन्दा हूँ।’’
इतना कहकर भला आदमी फुक्का मारकर रोने लगा। भृगु चौधुरी तो अवाक् रह गये, जैसे सारी सिट्टी-पिट्टी ही गुम हो गयी हो। अब भला ये सब बातें वे कैसे जानते होंगे ? महेन्द्र दास तो हमेशा उनसे, या उनसे से ही क्यों, हर एक आदमी से यही कहता फिर रहा है कि उसके प्यारे बेटे उसे बराबर अपने पास बुलाते ही रहते हैं। कहते हैं कि वहाँ अकेले-अकेले पड़े रहने की क्या जरूरत है ? वह सब छोड़-छाड़कर हम लोगों के पास ही क्यों नहीं चले आते ?
2
बहुत दिनों बाद रजत कलिता आज भृगु चौधुरी के घर पर आ पहुँचे,
‘‘अरे कलिता साहब, आप ! कहाँ से आ रहे हैं
? आइए, आइए,
पधारिए।’’
चौधरी की बात सुनकर कलिता ने उत्तर में कुछ कहा नहीं, बस तनिक-सी मुसकान जरूर बिखेरी उनकी ओर देखकर। बात दरअसल यह है कि आयु की अपेक्षा कुछ अधिक ही लज्जालु किस्म के आदमी हैं कलिताजी। स्वभाव के बड़े ही भले हैं। फिर भी एक विशेष किस्म के एक सुर्रे-से है, सनक की हद तक, फिर भी उन्हें पागल नहीं कह सकते। परन्तु कभी-कभी लगता है कि पागल भी उन्हें क्यों नहीं कहा-समझा जा सकता है ? पागल नहीं हैं तो और क्या ? साहित्य और साहित्याकारों के प्रति रजत कलिता में जो जरूरत से बहुत अधिक मात्रा की दुर्बलता है, वही क्या काफी नहीं है, उन्हें पागल समझने के लिए ? ऐसा देखा गया है कि कुछ-कुछ मनुष्यों में उनका मानसिक विकास एक खास मुकाम पर पहुँचकर रुक जाता है। इस कलिता महाशय में भी यही एक पुरानी दुर्बलता है। वे कोशिश कर-करके साहित्यकारों के करीब पहुँचते हैं, उनसे सम्पर्क स्थापित करते हैं।
यदि उनके निकट नहीं पहुँच सके तो फिर उनके नाम-पते ही इकट्ठा करते हैं, और फिर उन्हें पत्र लिखते हैं। अब उन्हें पत्र लिखकर या जैसे भी निकट सम्पर्क स्थापित कर वे उनसे साहित्य सम्बन्धी कोई आलोचना-प्रत्यालोचना करते हैं, या कोई गम्भीर विचार-विमर्श करना चाहते हैं,-ऐसी भी कोई बात नहीं। बस सम्पर्क स्थापित कर लेने भर से ही परम परितृप्त हो जाते हैं। हाँ, वे स्वयं भी कविताएँ और छोटी कहानियाँ लिखते हैं। जैसे उनके लिखे हुए साहित्य में भावावेश इतने प्रचण्ड रूप से होता है कि उसके मूल में, असली भाव या मन्तव्य क्या है उसका कुछ पता ही नहीं चलता। नये-नये उभरते, या यूँ कहिए कि उम्र के दो विशेष स्तरों के जोड़ की जगह पहुँचे हुए किशोर की काल्पनिक अनिश्चितता-सी उनमें रहती है। उनकी रचनाओं को देखकर यतीन ने एक बार विचार प्रकट किया था, ‘‘कक्षा आठ की किशोरी की रचना।’’
उसकी इस बात पर भृगु चौधुरी ने पूछा था, ‘‘क्यों, भाई ! ऐसा क्यों कहते हो ? कक्षा आठ की ही क्यों ? और सो भी किसी किशोरी की ही क्यों ?’’
‘‘बिलकुल सही कारण से ही कह रहा हूँ।’’-कहकर यतीन अलग हो गया था। बिलकुल सहज-सरल उत्तर। जैसे कि इसके आगे किसी प्रकार के आधार की या व्याख्या की कोई जरूरत ही नहीं।
रजत कलिता हमेशा किसी-न-किसी एक पत्रिका से जुड़े रहते हैं। उसमें किसी कर्मचारी के रूप में या उसके कर्ता-धर्ता के किसी रूप में नहीं। किसी प्रकार के प्रतिफल या लाभ पाने की गरज से भी नहीं। बस, इस तरह जुड़े रहना उन्हें अच्छा लगता है, इसी से उसके साथ चिपके रहते हैं। वस्तुतः बड़े भले स्वभाव के आदमी हैं वे। इसी से सभी लोग उन्हें मानते हैं। यदा-कदा कोई सम्पादक उनकी कोई कविता अथवा कोई और रचना प्रकाशित कर देता है, बस इतने से ही वे परम प्रफुल्लित हो जाते हैं। कृतज्ञता के बोझों तले दब जाते हैं। सो रजत कलिता मनुष्य के रूप में सचमुच ही बड़े भले आदमी हैं।
पहनावे-ओढ़ावे में रजत कलिता का सदा-सर्वदा बस एक-सा ही पहनावा है। खूब लम्बा-चौड़ा पायजामा और घुटनों तक तटकता बड़ा-सा ढीला-ढाला कुर्ता। यह भी एक प्रकार से अर्थपूर्ण है। माने, पहनावे में जैसे वे आज के जीन्स के फैशन तक नहीं पहुँच पाये हैं, उसी तरह उनकी साहित्यिक रुचि और विचारधारा भी बहुत पुरानी, अर्थात् आज से चालीस वर्ष पहले के जमाने के स्तर तक पहुँचकर ही थम गयी है। परन्तु इसके लिए अकेले-अकेले रजत कलिता को ही दोषी ठहराने से क्या लाभ ? साहित्य-जगत् में जिन लोगों के विचारों को, जिनके निर्णयों को विशेष महत्त्व दिया जाता है, वे सारे-के-सारे लोग बहुत लब्धप्रतिष्ठ लोग, यानी कि बहुत दिनों से जमे-जमाये पुराने लोग ही तो होते हैं ! उतने तक पहुँचते-पहुँचते उन लोगों की समझ, ध्यान-धारणा, सोच-विचार, पसन्द-नापसन्द सभी कुछ एक विशेष रूप ग्रहण कर चुका होता है। पुराने आदर्शों, परम्परा से चले आ रहे विधि-विधानों, बनी-बनायी परिपाटियों से दूर हट आने, लीक से अलग प्रकार का हो जाने पर उनकी भृकुटि तन जाती है। वे झुँझला उठते हैं। चौधुरी ने खुद ही देखा और समझा है कि जिन गानों और धुनों को उनके पिताजी बेहद पसन्द करते थे, वे स्वयं उन्हें पसन्द नहीं करते और अब उन्हें जो संगीत बहुत मनोहारी लगता है, आजकल के युवक-युवतियाँ उन्हें पसन्द नहीं करते। यह तो एक चिरन्तन सत्य है।
भृगु चौधुरी ने दो-चार अँग्रेजी उपन्यास पढ़े हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासों में नायक-नायिका के जीवन की सभी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ बिलकुल दृश्यमान थीं, जिन्हें प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से देखा-दिखाया जा सकता था। सारी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का धारावाहिक विवरण साफ-साफ शब्दों में बयान किया होता था। हाँ, यह जरूर है कि व्यक्ति विशेष रचयिता की देखने-परखने की शक्ति, देखने का नजरिया और विश्लेषण कर पाने की क्षमता के अनुरूप इस प्रकार का विवरण अच्छा हो सकता है, तो बुरा भी हो सकता है।
चित्रकला के क्षेत्र में जैसा कुछ हुआ है, उपन्यास-रचना के क्षेत्र में भी ठीक उसी प्रकार की स्थितियाँ रही हैं। रचना लेखक की व्यक्तिगत उपलब्धियों का ही प्रतिफल हो गयी है, लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियों से सराबोर। अब इन सब अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए सम्भवतः नयी शैली, नयी भंगिमा, नयी तर्ज और नये कौशल की जरूरत है। उसे देखकर मुँह-बिचकाने से, चिढ़ने से भला कैसे काम चलेगा ?
इस प्रसंग में वर्जीनिया उल्फ की कही हुई एक बात भृगु चौधुरी के मन में बार-बार कौंध उठती है-
‘‘सत्य का यथार्थ रूप क्या है ? दरअसल, यह बड़ा ही अस्थिर और अनिश्चित है। कभी-कभी तो यह रास्ते में पड़ी धूल में धूल-धूसरित हो उसी में घुला-मिला पड़ा रहता है, कभी रास्ते के किनारे फेंके-पवारे कागज के एक टुकड़े की खड़खड़ाहट में झलकता नजर आ सकता है, तो कभी यह सूरज की प्रातःकालीन किरणों से फूल उठे फूल की एक पंखुड़ी के भीतर ही झिलमिला उठ सकता है।’’
एक बहुत भारी घटना की अपेक्षा एक अत्यन्त साधारण, छोटी-सी घटना भी मनुष्य के मन में अधिक प्रभाव डाल सकती है।
डीकेन्स, थेकरे, जार्ज इलियट अथवा थामस हार्डी के लिखने की कला भिन्न प्रकार की है और वर्जीनिया उल्फ, जेम्स जॉयस, अथवा लारेंस के लिखने की शैली भिन्न ही प्रकार की है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की पद्धति और रचना-शिल्प की प्रक्रिया में परिवर्तन तो होता ही रहता है। किस जमाने में वह काफी आगे की ओर बढ़ गया है, अथवा बहुत पीछे की ओर ही लुढकता चला गया है, इस तरह का निर्णय देना तो विवाद का विषय है। अतएव सारे संक्षेप में यही कहना उचित है कि परिवर्तन होता ही रहता है, या परिवर्तन हो गया है। प्रत्येक युग-जमाने के प्रतिभाशाली रचनाकार अपनी महिमा से ही प्रकाशित हैं। अतएव एक युग अथवा जमाने कि विशिष्ट रचना-मानदण्डों से दूसरे युग के रचयिता का मूल्यांकन करने की कोशिश करने से एक भारी विपत्ति ही आ पड़ेगी।
सो, चौधुरी ने कलिता का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘बहुत दिनों से आप से भेंट-मुलाकात नहीं हो पायी थी। कहिए, क्या समाचार हैं ?’’
उनकी बात सुन कलिताजी लज्जापूर्ण हँसी-हँस पड़े, ‘‘अरे, यही पेन्शन, ग्रेच्युइटी, प्रॉविडेण्ट फण्ड वगैरह के लफड़े में पड़ा रहा था।’’
‘‘क्यों, भाई ! सेवा-निवृत्त भी हो गये क्या ? तुम तो अभी काफी नौजवान-से दीखते हो।’’
कलिता फिर और भी लजाते हुए मुसकरा दिये। जैसे-तैसे उन्होंने जो कुछ बताया, वह संक्षेप में यह कि शीघ्र ही वे एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करेंगे। वैसे यह कोई उनका आज का नया-नया शौक नहीं है, बल्कि उनके जीवन के बहुत दिनों की उनकी यह मनोभिलाषा है। इतने दिनों तक मुँह खोलकर किसी के सामने जरूर ही कभी कह नहीं सके थे। वैसे तब ऐसा कर पाना सम्भव भी नहीं था। मगर इस समय अब और कोई असुविधा नहीं है। ग्रेच्युइटी के रुपये पा ही गये हैं, सो अब हो ही जाएगा।
भृगु चौधुरी ने बड़ी तीखी-गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या मतिभ्रम पैदा हो गया क्या ? नयी-नयी जवानी की उमंग के समय में तो इस तरह का कुछ करने का कुछ अर्थ भी होता है, परन्तु अब इस उम्र में ?
‘‘जरा ठहरो भी। अरे भाई, सुनो तो, पत्रिका प्रकाशित कर चला पाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। विशेषतः जब तक अपना निजी कोई छापाखाना (प्रेस) न हो, तब तक किस तरह से क्या कुछ कर पाओगे ?’’
‘‘ग्रेट इण्डियन प्रेस के मालिक से बातचीत कर चुका हूँ। उन्होंने पत्रिका को समयानुसार प्रकाशित करते रहने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है।’’
‘‘लेकिन प्रकाशित कर देने भर से ही तो काम नहीं चल जाएगा। उसे प्रचारित करने, बेचने-बेचवाने की व्यवस्था का भी तो सवाल है।’’
‘‘आजकल इस सबकी कोई असुविधा नहीं है। देख नहीं रहे हैं कि कितनी सारी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती चली जा रही हैं।’’
‘‘हाँ, ठीक है। प्रकाशित हो रही हैं, मगर कितने दिनों तक जीवित रह पाती हैं ? जो जमे-जमाये, नामी-गरामी प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए यह सब करने में कोई विशेष असुविधा नहीं है। उन लोगों की अपनी सुनिश्चित और स्थायी प्रभावशाली विचरण-व्यवस्था है। माल भेज चुकने के बाद उसके मूल्य का पैसा वसूल होने में कोई कठिनाई उन्हें नहीं है। परन्तु ऐसी दशा में आप क्या करेंगे भला ? बहुत करेंगे दुकान-दुकान दौड़-दौड़कर बेचने के लिए प्रतियाँ रख आएँगे, तो यही तो सोचेंगे कि वे आपका पैसा आप को दे देंगे। परन्तु यदि उन्होंने बेच लेने के बाद भी पैसा नहीं दिया तब ?’’
‘‘देंगे भाई ! देंगे, आप घबराते क्यों हैं ?’’
समझ गये कि अब मना करने से भी कोई लाभ नहीं। कलिता अपनी योजना पूरी करने को दृढ़प्रतिज्ञा हैं, अब टस-से-मस नहीं होंगे। भृगु चौधुरी पास आने का उनका खास मतलब है कि अपनी पत्रिका के लिए उन्हें भृगु चौधुरी से एक धारावाहिक उपन्यास चाहिए।
‘‘सो तो देना ही पड़ेगा। और किसी के लिए न सही, परन्तु मेरे लिए तो आपको एक उपन्यास रचकर देना ही पड़ेगा।’’
‘‘मैं रचकर दूँगा उपन्यास ? मैं भला...।’’
‘‘आप तो पहले बहुत सुन्दर लिखते थे भाई ! अब उपन्यास रचना क्या बन्द कर दिया ? अरे अगर बन्द भी कर दिया हो, तो भी अब फिर से आरम्भ कीजिए।’’
‘अब रचना आरम्भ करने की बात कह भी दूँ तो क्या इतने से ही रच पा सकूँगा ? अरे अपने पास इस क्षेत्र का जो कुछ मूलधन था, वह तो जाने कभी का खत्म हो चुका। और मान लो कि मैं रच भी दूँ, लिखकर प्रकाशित भी करवा दूँ, तो आजकल के आदमी तो मेरी रचना पढ़ने से रहे।’’
‘‘क्या कहते हैं आप ? क्या मैं आजकल के लेखकों की कहानियाँ या उनके उपन्यास पढ़ता नहीं हूँ। आज के लेखक भी पहले के लेखकों जैसे ही हैं।’’
अब तो फिर बचने का कोई उपाय ही नहीं। यह एक बहुत पुराने समय से चला आ रहा अभियोग है। कहानी-उपन्यास जो पहले रच दिये गये, लिखकर प्रकाशित कर दिये गये, सो हो गये। जो वे बन गये, अपनी जगह सर्वोत्तम बन गये। आजकल कोई नयी अच्छी, सार्थक रचना बन नहीं सकी। सबसे पहली बात यह कि कालजयी श्रेणी की साहित्यिक रचना हजारों-हजारों की संख्या में कहीं भी रची नहीं जा रहीं। भृगु चौधुरी का मन हुआ कि उनसे पूछे कि पहले के जमाने में ही भला कौन-सी कालजयी साहित्यिक रचना रची गयी ? जरा कुछेक का नाम तो गिनाएँ। परन्तु पूछने से भी कोई लाभ नहीं। यह सब तो अपने-अपने मानने, अपने विश्वास करने की बात है। अच्छी तरह से सोच-विचारकर, गम्भीरतापूर्वक विचार-विश्लेषण करके कही जानेवाली बात नहीं है।
रजत कलिता ने फिर सकुचाते-सकुचाते जैसे उपसंहार किया, ‘‘इसके मतलब कि तब आप एक उपन्यास रचकर मुझे देंगे। तो फिर बतलाएँ कि उसे लेने के लिए मैं दुबारा कब आऊँ ? जो कुछ सम्मानार्थ पत्रं-पुष्पं हो सकेगा सो...’’
‘‘अरे नहीं, नहीं। वैसी कोई बात नहीं है। देखता हूँ कि क्या कुछ कर पाता हूँ।’’
‘‘देखने-देखने की बात नहीं, देनी ही पड़ेगी। मैं अपनी पत्रिका के इसी अंक में विज्ञापन देकर इस सम्बन्ध में सभी को जना दूँगा।’’
चौधरी की बात सुनकर कलिता ने उत्तर में कुछ कहा नहीं, बस तनिक-सी मुसकान जरूर बिखेरी उनकी ओर देखकर। बात दरअसल यह है कि आयु की अपेक्षा कुछ अधिक ही लज्जालु किस्म के आदमी हैं कलिताजी। स्वभाव के बड़े ही भले हैं। फिर भी एक विशेष किस्म के एक सुर्रे-से है, सनक की हद तक, फिर भी उन्हें पागल नहीं कह सकते। परन्तु कभी-कभी लगता है कि पागल भी उन्हें क्यों नहीं कहा-समझा जा सकता है ? पागल नहीं हैं तो और क्या ? साहित्य और साहित्याकारों के प्रति रजत कलिता में जो जरूरत से बहुत अधिक मात्रा की दुर्बलता है, वही क्या काफी नहीं है, उन्हें पागल समझने के लिए ? ऐसा देखा गया है कि कुछ-कुछ मनुष्यों में उनका मानसिक विकास एक खास मुकाम पर पहुँचकर रुक जाता है। इस कलिता महाशय में भी यही एक पुरानी दुर्बलता है। वे कोशिश कर-करके साहित्यकारों के करीब पहुँचते हैं, उनसे सम्पर्क स्थापित करते हैं।
यदि उनके निकट नहीं पहुँच सके तो फिर उनके नाम-पते ही इकट्ठा करते हैं, और फिर उन्हें पत्र लिखते हैं। अब उन्हें पत्र लिखकर या जैसे भी निकट सम्पर्क स्थापित कर वे उनसे साहित्य सम्बन्धी कोई आलोचना-प्रत्यालोचना करते हैं, या कोई गम्भीर विचार-विमर्श करना चाहते हैं,-ऐसी भी कोई बात नहीं। बस सम्पर्क स्थापित कर लेने भर से ही परम परितृप्त हो जाते हैं। हाँ, वे स्वयं भी कविताएँ और छोटी कहानियाँ लिखते हैं। जैसे उनके लिखे हुए साहित्य में भावावेश इतने प्रचण्ड रूप से होता है कि उसके मूल में, असली भाव या मन्तव्य क्या है उसका कुछ पता ही नहीं चलता। नये-नये उभरते, या यूँ कहिए कि उम्र के दो विशेष स्तरों के जोड़ की जगह पहुँचे हुए किशोर की काल्पनिक अनिश्चितता-सी उनमें रहती है। उनकी रचनाओं को देखकर यतीन ने एक बार विचार प्रकट किया था, ‘‘कक्षा आठ की किशोरी की रचना।’’
उसकी इस बात पर भृगु चौधुरी ने पूछा था, ‘‘क्यों, भाई ! ऐसा क्यों कहते हो ? कक्षा आठ की ही क्यों ? और सो भी किसी किशोरी की ही क्यों ?’’
‘‘बिलकुल सही कारण से ही कह रहा हूँ।’’-कहकर यतीन अलग हो गया था। बिलकुल सहज-सरल उत्तर। जैसे कि इसके आगे किसी प्रकार के आधार की या व्याख्या की कोई जरूरत ही नहीं।
रजत कलिता हमेशा किसी-न-किसी एक पत्रिका से जुड़े रहते हैं। उसमें किसी कर्मचारी के रूप में या उसके कर्ता-धर्ता के किसी रूप में नहीं। किसी प्रकार के प्रतिफल या लाभ पाने की गरज से भी नहीं। बस, इस तरह जुड़े रहना उन्हें अच्छा लगता है, इसी से उसके साथ चिपके रहते हैं। वस्तुतः बड़े भले स्वभाव के आदमी हैं वे। इसी से सभी लोग उन्हें मानते हैं। यदा-कदा कोई सम्पादक उनकी कोई कविता अथवा कोई और रचना प्रकाशित कर देता है, बस इतने से ही वे परम प्रफुल्लित हो जाते हैं। कृतज्ञता के बोझों तले दब जाते हैं। सो रजत कलिता मनुष्य के रूप में सचमुच ही बड़े भले आदमी हैं।
पहनावे-ओढ़ावे में रजत कलिता का सदा-सर्वदा बस एक-सा ही पहनावा है। खूब लम्बा-चौड़ा पायजामा और घुटनों तक तटकता बड़ा-सा ढीला-ढाला कुर्ता। यह भी एक प्रकार से अर्थपूर्ण है। माने, पहनावे में जैसे वे आज के जीन्स के फैशन तक नहीं पहुँच पाये हैं, उसी तरह उनकी साहित्यिक रुचि और विचारधारा भी बहुत पुरानी, अर्थात् आज से चालीस वर्ष पहले के जमाने के स्तर तक पहुँचकर ही थम गयी है। परन्तु इसके लिए अकेले-अकेले रजत कलिता को ही दोषी ठहराने से क्या लाभ ? साहित्य-जगत् में जिन लोगों के विचारों को, जिनके निर्णयों को विशेष महत्त्व दिया जाता है, वे सारे-के-सारे लोग बहुत लब्धप्रतिष्ठ लोग, यानी कि बहुत दिनों से जमे-जमाये पुराने लोग ही तो होते हैं ! उतने तक पहुँचते-पहुँचते उन लोगों की समझ, ध्यान-धारणा, सोच-विचार, पसन्द-नापसन्द सभी कुछ एक विशेष रूप ग्रहण कर चुका होता है। पुराने आदर्शों, परम्परा से चले आ रहे विधि-विधानों, बनी-बनायी परिपाटियों से दूर हट आने, लीक से अलग प्रकार का हो जाने पर उनकी भृकुटि तन जाती है। वे झुँझला उठते हैं। चौधुरी ने खुद ही देखा और समझा है कि जिन गानों और धुनों को उनके पिताजी बेहद पसन्द करते थे, वे स्वयं उन्हें पसन्द नहीं करते और अब उन्हें जो संगीत बहुत मनोहारी लगता है, आजकल के युवक-युवतियाँ उन्हें पसन्द नहीं करते। यह तो एक चिरन्तन सत्य है।
भृगु चौधुरी ने दो-चार अँग्रेजी उपन्यास पढ़े हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासों में नायक-नायिका के जीवन की सभी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ बिलकुल दृश्यमान थीं, जिन्हें प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से देखा-दिखाया जा सकता था। सारी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का धारावाहिक विवरण साफ-साफ शब्दों में बयान किया होता था। हाँ, यह जरूर है कि व्यक्ति विशेष रचयिता की देखने-परखने की शक्ति, देखने का नजरिया और विश्लेषण कर पाने की क्षमता के अनुरूप इस प्रकार का विवरण अच्छा हो सकता है, तो बुरा भी हो सकता है।
चित्रकला के क्षेत्र में जैसा कुछ हुआ है, उपन्यास-रचना के क्षेत्र में भी ठीक उसी प्रकार की स्थितियाँ रही हैं। रचना लेखक की व्यक्तिगत उपलब्धियों का ही प्रतिफल हो गयी है, लेखक की व्यक्तिगत अनुभूतियों से सराबोर। अब इन सब अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए सम्भवतः नयी शैली, नयी भंगिमा, नयी तर्ज और नये कौशल की जरूरत है। उसे देखकर मुँह-बिचकाने से, चिढ़ने से भला कैसे काम चलेगा ?
इस प्रसंग में वर्जीनिया उल्फ की कही हुई एक बात भृगु चौधुरी के मन में बार-बार कौंध उठती है-
‘‘सत्य का यथार्थ रूप क्या है ? दरअसल, यह बड़ा ही अस्थिर और अनिश्चित है। कभी-कभी तो यह रास्ते में पड़ी धूल में धूल-धूसरित हो उसी में घुला-मिला पड़ा रहता है, कभी रास्ते के किनारे फेंके-पवारे कागज के एक टुकड़े की खड़खड़ाहट में झलकता नजर आ सकता है, तो कभी यह सूरज की प्रातःकालीन किरणों से फूल उठे फूल की एक पंखुड़ी के भीतर ही झिलमिला उठ सकता है।’’
एक बहुत भारी घटना की अपेक्षा एक अत्यन्त साधारण, छोटी-सी घटना भी मनुष्य के मन में अधिक प्रभाव डाल सकती है।
डीकेन्स, थेकरे, जार्ज इलियट अथवा थामस हार्डी के लिखने की कला भिन्न प्रकार की है और वर्जीनिया उल्फ, जेम्स जॉयस, अथवा लारेंस के लिखने की शैली भिन्न ही प्रकार की है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की पद्धति और रचना-शिल्प की प्रक्रिया में परिवर्तन तो होता ही रहता है। किस जमाने में वह काफी आगे की ओर बढ़ गया है, अथवा बहुत पीछे की ओर ही लुढकता चला गया है, इस तरह का निर्णय देना तो विवाद का विषय है। अतएव सारे संक्षेप में यही कहना उचित है कि परिवर्तन होता ही रहता है, या परिवर्तन हो गया है। प्रत्येक युग-जमाने के प्रतिभाशाली रचनाकार अपनी महिमा से ही प्रकाशित हैं। अतएव एक युग अथवा जमाने कि विशिष्ट रचना-मानदण्डों से दूसरे युग के रचयिता का मूल्यांकन करने की कोशिश करने से एक भारी विपत्ति ही आ पड़ेगी।
सो, चौधुरी ने कलिता का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘बहुत दिनों से आप से भेंट-मुलाकात नहीं हो पायी थी। कहिए, क्या समाचार हैं ?’’
उनकी बात सुन कलिताजी लज्जापूर्ण हँसी-हँस पड़े, ‘‘अरे, यही पेन्शन, ग्रेच्युइटी, प्रॉविडेण्ट फण्ड वगैरह के लफड़े में पड़ा रहा था।’’
‘‘क्यों, भाई ! सेवा-निवृत्त भी हो गये क्या ? तुम तो अभी काफी नौजवान-से दीखते हो।’’
कलिता फिर और भी लजाते हुए मुसकरा दिये। जैसे-तैसे उन्होंने जो कुछ बताया, वह संक्षेप में यह कि शीघ्र ही वे एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करेंगे। वैसे यह कोई उनका आज का नया-नया शौक नहीं है, बल्कि उनके जीवन के बहुत दिनों की उनकी यह मनोभिलाषा है। इतने दिनों तक मुँह खोलकर किसी के सामने जरूर ही कभी कह नहीं सके थे। वैसे तब ऐसा कर पाना सम्भव भी नहीं था। मगर इस समय अब और कोई असुविधा नहीं है। ग्रेच्युइटी के रुपये पा ही गये हैं, सो अब हो ही जाएगा।
भृगु चौधुरी ने बड़ी तीखी-गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या मतिभ्रम पैदा हो गया क्या ? नयी-नयी जवानी की उमंग के समय में तो इस तरह का कुछ करने का कुछ अर्थ भी होता है, परन्तु अब इस उम्र में ?
‘‘जरा ठहरो भी। अरे भाई, सुनो तो, पत्रिका प्रकाशित कर चला पाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। विशेषतः जब तक अपना निजी कोई छापाखाना (प्रेस) न हो, तब तक किस तरह से क्या कुछ कर पाओगे ?’’
‘‘ग्रेट इण्डियन प्रेस के मालिक से बातचीत कर चुका हूँ। उन्होंने पत्रिका को समयानुसार प्रकाशित करते रहने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है।’’
‘‘लेकिन प्रकाशित कर देने भर से ही तो काम नहीं चल जाएगा। उसे प्रचारित करने, बेचने-बेचवाने की व्यवस्था का भी तो सवाल है।’’
‘‘आजकल इस सबकी कोई असुविधा नहीं है। देख नहीं रहे हैं कि कितनी सारी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती चली जा रही हैं।’’
‘‘हाँ, ठीक है। प्रकाशित हो रही हैं, मगर कितने दिनों तक जीवित रह पाती हैं ? जो जमे-जमाये, नामी-गरामी प्रतिष्ठान हैं, उनके लिए यह सब करने में कोई विशेष असुविधा नहीं है। उन लोगों की अपनी सुनिश्चित और स्थायी प्रभावशाली विचरण-व्यवस्था है। माल भेज चुकने के बाद उसके मूल्य का पैसा वसूल होने में कोई कठिनाई उन्हें नहीं है। परन्तु ऐसी दशा में आप क्या करेंगे भला ? बहुत करेंगे दुकान-दुकान दौड़-दौड़कर बेचने के लिए प्रतियाँ रख आएँगे, तो यही तो सोचेंगे कि वे आपका पैसा आप को दे देंगे। परन्तु यदि उन्होंने बेच लेने के बाद भी पैसा नहीं दिया तब ?’’
‘‘देंगे भाई ! देंगे, आप घबराते क्यों हैं ?’’
समझ गये कि अब मना करने से भी कोई लाभ नहीं। कलिता अपनी योजना पूरी करने को दृढ़प्रतिज्ञा हैं, अब टस-से-मस नहीं होंगे। भृगु चौधुरी पास आने का उनका खास मतलब है कि अपनी पत्रिका के लिए उन्हें भृगु चौधुरी से एक धारावाहिक उपन्यास चाहिए।
‘‘सो तो देना ही पड़ेगा। और किसी के लिए न सही, परन्तु मेरे लिए तो आपको एक उपन्यास रचकर देना ही पड़ेगा।’’
‘‘मैं रचकर दूँगा उपन्यास ? मैं भला...।’’
‘‘आप तो पहले बहुत सुन्दर लिखते थे भाई ! अब उपन्यास रचना क्या बन्द कर दिया ? अरे अगर बन्द भी कर दिया हो, तो भी अब फिर से आरम्भ कीजिए।’’
‘अब रचना आरम्भ करने की बात कह भी दूँ तो क्या इतने से ही रच पा सकूँगा ? अरे अपने पास इस क्षेत्र का जो कुछ मूलधन था, वह तो जाने कभी का खत्म हो चुका। और मान लो कि मैं रच भी दूँ, लिखकर प्रकाशित भी करवा दूँ, तो आजकल के आदमी तो मेरी रचना पढ़ने से रहे।’’
‘‘क्या कहते हैं आप ? क्या मैं आजकल के लेखकों की कहानियाँ या उनके उपन्यास पढ़ता नहीं हूँ। आज के लेखक भी पहले के लेखकों जैसे ही हैं।’’
अब तो फिर बचने का कोई उपाय ही नहीं। यह एक बहुत पुराने समय से चला आ रहा अभियोग है। कहानी-उपन्यास जो पहले रच दिये गये, लिखकर प्रकाशित कर दिये गये, सो हो गये। जो वे बन गये, अपनी जगह सर्वोत्तम बन गये। आजकल कोई नयी अच्छी, सार्थक रचना बन नहीं सकी। सबसे पहली बात यह कि कालजयी श्रेणी की साहित्यिक रचना हजारों-हजारों की संख्या में कहीं भी रची नहीं जा रहीं। भृगु चौधुरी का मन हुआ कि उनसे पूछे कि पहले के जमाने में ही भला कौन-सी कालजयी साहित्यिक रचना रची गयी ? जरा कुछेक का नाम तो गिनाएँ। परन्तु पूछने से भी कोई लाभ नहीं। यह सब तो अपने-अपने मानने, अपने विश्वास करने की बात है। अच्छी तरह से सोच-विचारकर, गम्भीरतापूर्वक विचार-विश्लेषण करके कही जानेवाली बात नहीं है।
रजत कलिता ने फिर सकुचाते-सकुचाते जैसे उपसंहार किया, ‘‘इसके मतलब कि तब आप एक उपन्यास रचकर मुझे देंगे। तो फिर बतलाएँ कि उसे लेने के लिए मैं दुबारा कब आऊँ ? जो कुछ सम्मानार्थ पत्रं-पुष्पं हो सकेगा सो...’’
‘‘अरे नहीं, नहीं। वैसी कोई बात नहीं है। देखता हूँ कि क्या कुछ कर पाता हूँ।’’
‘‘देखने-देखने की बात नहीं, देनी ही पड़ेगी। मैं अपनी पत्रिका के इसी अंक में विज्ञापन देकर इस सम्बन्ध में सभी को जना दूँगा।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i