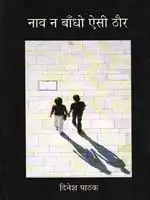|
श्रंगार - प्रेम >> नाव न बाँधो ऐसी ठौर नाव न बाँधो ऐसी ठौरदिनेश पाठक
|
222 पाठक हैं |
|||||||
दोनों की आँखों ने एक-दूसरे का स्पर्श किया। दीपांकर के भीतर एक अजीब-सी बयार बही...उस बयार में एक अनुगूँज भी उभरी...तो क्या शाल्मली के मन में आज भी, अब भी उनके लिए जगह है ?
नाव न बाँधो ऐसी ठौर
इस तरह के आयोजनों में दीपांकर आम तौर पर नहीं जाते। पता नहीं क्यों
उन्हें यह सब फिजूल-सा लगता है। कहीं कोई सार्थक बातचीत या बहस होती नहीं
दीखती। बस, आए, इकट्ठे हुए, अपने-अपने अहं का प्रदर्शन हुआ, खाया-पीया,
टी.ए.-डी. ए. बनाया और चल दिए। दीपांकर को सदा से ही इस सबसे वितृष्णा रही
है। आज भी है।
पर इस बार स्थिति कुछ दूसरी थी। हालाँकि शुरू में तो वे मना ही करते रहे थे, पर एक तो संयोजक सिर्फ प्राध्यापक ही नहीं वरन् लेखक भी थे, दूसरे उनके पुराने मित्र भी, अतः उनके बार-बार आग्रह की वे अनदेखी नहीं कर सके। अलावा इसके एक दूसरी बात भी थी, सेमिनार का मुख्य विषय ग्राम साहित्य था। ग्राम साहित्य को लेकर उनकी अपनी कुछ विशिष्ट और अलग मान्यताएँ रही हैं। अपनी मान्यताएँ समय-समय पर वे पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में भी लाते रहे हैं। सोचा, यह अच्छा अवसर है जब प्राध्यापकों और एकत्रित लेखक-समूह के मध्य वे अपनी बात सीधे-साधे रख सकते हैं। उन्होंने यह आग्रह स्वीकार कर लिया। वे तय करके आए थे, पहले ही दिन अपने व्याख्यान के तुरंत बाद, समय रहा तो निकल जाएँगे। नहीं तो दूसरे दिन सुबह की पहली बस तो पकड़ ही लेंगे। अनावश्यक भीड़भाड़ दीपांकर को पसंद नहीं है, मानो दम घुटने लगता है। जिंदगी को मस्ती मानकर जीने का अंदाज भी उन्हें नहीं आता या यूँ कहा जा सकता है कि उस तरह से कभी जीए ही नहीं। अपना अकेलापन ही आनंददायक लगता है, आकाश की अनंत ऊँचाई में उड़ते उस पक्षी की तरह जो अकेले हवा में अपने पंखों को तौलता है।
दीपांकर का व्याख्यान देर से शुरू हुआ, लंच के बाद। व्याख्यान के बाद कई प्रश्न-प्रतिप्रश्न उठे। खासा वक्त निकल गया। बहरहाल वे संतुष्ट थे कि लोगों के सम्मुख अपनी बात रख सके। कई जाने-माने साहित्यकार भी वहाँ बैठे थे। साहित्य जगत् में एक लेखक के तौर पर अब तक उनकी भी जगह बन चुकी थी। जानते थे, पूर्वाग्रह के चलते चाहे कोई उनकी बात की अपेक्षा भले ही कर दे, पर उन्हें हलके से लेने की गलती नहीं कर सकता था।
उस विशाल सभागार के मंच से जब वे नीचे उतर रहे थे तो परम संतुष्ट थे। सभागार में बहुत भीड़ थी। आयोजक महाविद्यालय का प्राध्यापक वर्ग आगंतुकों के प्रति पूरी तरह सतर्क दिखाई देता था। पुरुष हों या महिलाएँ, सभी ने अपने सीने पर रंगीन रिबन से बने खूबसूरत बिल्ले धारण किए हुए थे। दीपांकर को आयोजक मित्र के प्रबंध और महाविद्यालय के सहयोगियों द्वारा उन्हें मिल रहे सहयोग पर अतीव प्रसन्नता हुई। आज के दौर में यह परम दुर्लभ दृश्य था। ऐसी एकता, ऐसा ऐक्य भाव अब कहाँ रहा ? नीचे उतरकर सभागार की अपनी कुरसी पर वापस बैठे तो थका हुआ अनुभव कर रहे थे। प्यास का अनुभव भी हुआ। पानी के लिए आँखें उठाकर जब तक इधर-उधर देखते, ट्रे में पानी लिया हुआ एक हाथ ठीक उनके सामने आ गया। साँवला किंतु खूबसूरत हाथ, जिसकी कलाई पर एक पतली सुनहरी घड़ी बँधी हुई थी। वे चौंके, कलाई कुछ-कुछ परिचित-सी लगी, जैसे पहले भी कहीं यह कलाई देखी हो। चकित भाव से आँखें उठाकर देखा तो देखते रह गए। सामने अपनी परिचित मुस्कराहट बिखेरती हुई शाल्मती खड़ी थी–डॉ० शाल्मली कुमार, हलके चमकदार बादामी बॉर्डर वाली आसमानी रंग की साड़ी में फबती हुई।
‘मुझे पता है कि इस वक्त आपको पानी की जरूरत होगी। कॉलेज में हर लेक्चर के बाद आप पानी पिया करते थे...’ शाल्मली ने बहुत गहरी आँखों से उन्हें निहारा। बोली, ‘लीजिए, सर !’
लगा, प्यास ही गायब हो गई है। यह इतना अप्रत्याशित था कि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। शाल्मली से दोबारा फिर कभी भेंट हो सकेगी, वह भी इस तरह से, सोचा नहीं था। पर सामने शाल्मली ही थी, सचमुच की शाल्मली।
पानी की एक घूँट के साथ ही वे निमिष-भर के लिए कहीं पीछे चले गए...सप्ताह-भर बुखार में रहने के बाद वापस कॉलेज आए हुए थे। कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। शाल्मली मौका तलाशकर विभाग में आई थी और उनकी अलमारी में ग्लूकोन-डी का डब्बा रखती हुई बोली थी, ‘आप ग्लूकोज का पानी पिया कीजिए, सर ! वीकनेस हो रही होगी...’ हैरत हुई कि इस क्षण भी पानी में ग्लूकोज डला हुआ था। उन्होंने हैरत-भरी आँखें उठाई और उसे देखने लगे।
‘पानी पीजिए, सर, लोग देख रहे हैं...’ शाल्मली किंचित् शरारत से मुस्कराई। उसका यह शरारताना अंदाज वैसा ही था, पुराना। वे सजग हुए। आखिर वे सभागार में बैठे हुए थे और उनके चतुर्दिक, तमाम लोग थे। उन्होंने पानी पिया और गिलास वापस ट्रे में रख दिया।
‘थोड़ी देर में मिलते हैं, सर !...’ शाल्मली जैसे फुसफुसाई थी। वह मुड़ी, ‘धीरे-धीरे उनसे दूर निकलकर आँखों से ओझल हो गई।
एक तरह की अचकचाई-सी स्थिति में जस के तस बैठे रह गए दीपांकर...
शेष वक्त अब सभागार में उनका मन नहीं लगा। वहाँ होते हुए भी जैसे वे वहाँ नहीं रह गए थे। कौन क्या कह रहा है ? क्या कार्रवाई चल रही है ? कौन वक्ता बोल रहा है ? उनके लिए सब अर्थहीन हो गया था। कानों में सिर्फ ध्वनियाँ थीं, शब्द नहीं। लगा, शरीर भर यहाँ रह गया है, मन न जाने कहाँ-कहाँ भटकने लगा है, किस लोक में। हालाँकि वे भरपूर कोशिश कर रहे थे कि पूरे मनोयोग से यहाँ रह सकें, मन को लौटा भी रहे थे बार-बार ताकि वह यहीं बना रहे, इसी सभागार में। पर लगा, चीजें एकाएक और अभी-अभी उनके अपने नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। उनका कतई कोई वश ही नहीं रह गया है उन पर। अपने को सभागार की कार्रवाई पर केंद्रित रखना सच में मुश्किल पड़ने लगा था। दीपांकर ने आँखें मूँदीं और कुरसी के पुश्ते पर आराम से पीठ टिका ली।
आयोजन का यह अंतिम सत्र था, इसलिए जल्दी समाप्त हो गया था। उन्होंने राहत की साँस ली। राहत का यह माहौल पूरे सभागार में ही प्याप्त दिखाई दिया। लोग जैसे किसी बंधन से मुक्त हुए थे और खुलकर चहकने लगे थे। पूरे सभागार में अब में अब बोलने-बतियाने की ध्वनि थी, एक कोने से दूसरे कोने तक उठती-गिरती स्वर-लहरी...। अब सामान्य बातें होने लगी थीं–दुनियादारी की वे सब बातें जिनमें आम तौर पर उनकी कोई रुचि नहीं है। आयोजकों ने बताया था कि यहाँ से निवृत होकर सीधे शाम की चाय पर चलना है। वे लोगों का अनुसरण करते हुए धीरे-धीरे बढ़ने लगे। कुछ एक युवा प्राध्यापक व शोधार्थी उनके साथ हो लिए थे, कदाचित् उनकी रुचि दीपांकर के साहित्य में प्रतीत होती थी। लेखक को यदि उसके पाठक मिल जाएँ तो फिर उसे और क्या चाहिए ? वह इतना गदगद हो उठता है कि दुनिया-जहान की दूसरी तमाम बातें ही भूल जाता है। पर उस क्षण उनसे बतियाते हुए भी पहली बार ऐसा लग रहा था कि पाठक भी उनके अनमनेपन को नहीं तोड़ पा रहे हैं।
जहाँ चाय की व्यवस्था थी, वहाँ लोग समूहों में बँट गए थे, अपनी-अपनी बातों में खोए, हँसते-बतियाते हुए। कुछ लोग उनके आसपास भी थे। किसी ने उनके आज के व्याख्यान की चर्चा की थी, उन्हें नई स्थापनाओं के लिए साधुवाद दिया था। किसी ने जानना चाहा था कि इन दिनों वे क्या नया लिख रहे हैं ? उन्होंने यथासंभव सबकी जिज्ञासाओं का समाधान किया था, कोशिश की थी कि उन्हीं की तरह हँसते, मुस्कराते दिख सकें। पर सच्चाई तो यह थी कि वे एकदम अकेले होना चाहते थे ताकि यदि कहीं आसमान शाल्मली हो तो उनकी आँखें उसे खोज सकें। अंततः वे क्षमायाचना करते हुए खुद ही एक किनारे जाकर खड़े हो गए। चाय सिप करते हुए उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी आँखें घुमाईं। अकस्मात् देखा, शाल्मली कुछ ही दूरी पर खड़ी उन्हीं को निहार रही है। दोनों की आँखों ने एक-दूसरे का स्पर्श किया। दीपांकर के भीतर एक अजीब-सी बयार बही...उस बयार में एक अनुगूँज भी उभरी...तो क्या शाल्मली के मन में आज भी, अब भी उनके लिए जगह है ? या वह यूँ ही देख रही थी ? वह देखना महज एक संयोग भर था ? या फिर वह खुद भी कहीं यह तो नहीं जाँचना चाह रही थी कि दीपांकर के मन में उसके लिए आज भी कुछ बचा है या...
उन्होंने आँखें हटा लीं और दूसरी दिशा में देखने लगे, कुछ ड्रस तरह जैसे उनकी आँखों को उसकी तलाश नहीं है। वह महज इत्तफाक है कि आँखें मिल गईं।...तभी महसूस हुआ, शाल्मली उनके निकट चली आ रही है, धीरे-धीरे और सधे कदमों से। शाल्मली का चलना सदैव बहुत सधा हुआ होता था। निकट पहुँचकर उन्हें जैसे चौंकाते हुए पूछा, ‘कैसे हैं, सर ?’
आँखें उठाई और शाल्मली पर टिका दीं। शाल्मली आज भी वैसी ही लगी, उतनी ही युवा और उतनी ही ताजा, हालाँकि देह से थोड़ी स्थूल लग रही थी, कुछ ज्यादा ही मांसल। और उसकी वे खूबसूरत, मायाविनी आँखें...? वे भी जस की तस थीं, जादू से परिपूर्ण। उन्होंने अपने जीवन में दोबारा फिर वैसी आँखें नहीं देखीं–बोलती, गाती और नृत्य करती आँखें...।
‘ठीक हूँ। आप सुनाएँ, आप कैसी हैं ?’ दीपांकर ने अपने को संयत किया, सँभाला। हालाँकि जानते थे, शाल्मली कुछ और ही सुनना चाहती होगी, कुछ ऐसा जो उसे गुदगुदाए, खुशी से सराबोर करे, मसलन यही कि तुम्हारे बिना मैं कैसा हो सकता हूँ, जरा कल्पना करो तो शाल्मली...! पर नहीं, इस तरह के किसी संवाद का कोई मतलब नहीं था, निरर्थक था वह सब, अतीत कथा हो चुका था। उनके उत्तर से शाल्मली के चेहरे पर हलकी बेचैनी उभरी। बोली, ‘अब भी वही ‘आप’ संबोधन, सर...अब तो कम से कम लौट आइए ‘तुम’ पर...।’
‘अतीत कभी लौटकर आता है, शाल्मली जी ? नहीं आता न ! आप चाहे अतीत से कितने ही चिपके रहें, पर वहाँ वापस तो नहीं पहुँच सकते। वहाँ से आप आगे बढ़ चुके होते हैं...’ वे मुस्कराए। भीतर चाहे कितनी ही उथल-पुथल क्यों न हो रही हो, पर बाहर से वे निर्विकार बने रहना चाहते थे, एकदम तटस्थ, जैसे वह सब वे वास्तव में भूल चुके हैं, उबर चुके हैं उस सबसे। कहा, ‘जीवन का नाम ही गति है। उसमें कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। जो कल था वह आज कैसे हो सकता है और जो आज है वह कल नहीं होगा...’
चाय पीती हुई शाल्मली के होंठ हलके से हिले, काँपे, थरथराए। कदाचित् वह कुछ कहना चाहती थी कि तभी सेमिनार के संयोजक उनके लेखक मित्र डॉ० रिपुदमन निकट आए। बोले, ‘यहाँ कहाँ खड़े हो, यार ! चलो, उधर चौकड़ी जमी है। तुम्हारे मतलब की बात तो वहाँ पर है।’
उन्होंने आँख उठाकर देखा। उधर चंद-एक स्वनामधन्य आलोचक थे, बेहद भदेस ढंग से हँसते-ठठाते हुए। उनके मित्र रिपुदमन इस सब काम में सिद्धहस्त हैं। साल-दो-साल में कहानी चाहे एकाध ही लिखें या वह भी नहीं, पर जोड़-जुगाड़ कुछ इस तरह बिठाए रहते हैं कि लगता है, पहुँचे हुए लेखक हैं। बिना कुछ लिखे हुए भी अपनी चर्चा करवा लेते हैं। इन तथाकथित बड़े महंतों की परिक्रमा कर इधर के छोटे-मोटे महंत के रूप में अपनी मान्यता के लिए वे जिस तरह छटपटाते हैं, देखकर दया आती है। पर दीपांकर को तो ये तथाकथित महंत सदा से ही परोपजीवी लगते रहे हैं, दूसरों के उच्छिष्ट अन्न पर पलने वाले मंदिरों-आश्रमों के मुस्टंज महंतों की तरह। लेखक लिखेगा ही नहीं तो ये आलोचक बेचारे कहाँ से अपनी दुकान चलाएँगे ! शताब्दियाँ बीत गई हैं, सूर-तुलसी अपनी जगह अमर हैं, पर कहाँ हैं उनके टिप्पणीकार, उनके आलोचक ? कोई जानता भी है क्या उन्हें ? दीपांकर समझ नहीं पाते, क्यों एक लेखक को आलचकों के पीछे लगकर अपनी ऊर्जा नष्ट करनी चाहिए ? पर आश्चर्य है कि आजकल ऐसा ही ज्यादा हो रहा है। एक अजब उलटी रीत बह रही है। लेखक का काम लिखना है, उसे सिर्फ लिखते रहना चाहिए। हाँ, अपने पाठकों पर उसकी सजग दृष्टि अवश्य होनी चाहिए, बाकी रही आलोचकों की बात, तो लेखक को क्यों उनके आगे-पीछे घूमना चाहिए ? क्यों उनकी चिरौरी करनी चाहिए ? पर हो ऐसा ही रहा है, फलतः कोयल तो हाशिए पर आ गई हैं और दादुरों की चल पड़ी है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे कभी इस मार्ग पर नहीं चले हैं। समझ रहे हैं कि रिपुदमन उनका भला ही चाहते हैं। सोच रहे हैं कि संयोग से एकत्रित हुए इन पाँच-सात आलोचकों से वे मिल लें, उन्हें प्रसन्न कर लें ताकि वे उनकी चर्चा भी करें, उन पर भी कुछ लिखें।
‘सोच क्या रहे हो...’ दीपांकर को विचारमग्न देख रिपुदमन ने झकझोरा, ‘मिल लो, यार ! क्या पता तुम्हारे नए उपन्यास पर ही कुछ चर्चा-वर्चा कर दें...’
पर इस बार स्थिति कुछ दूसरी थी। हालाँकि शुरू में तो वे मना ही करते रहे थे, पर एक तो संयोजक सिर्फ प्राध्यापक ही नहीं वरन् लेखक भी थे, दूसरे उनके पुराने मित्र भी, अतः उनके बार-बार आग्रह की वे अनदेखी नहीं कर सके। अलावा इसके एक दूसरी बात भी थी, सेमिनार का मुख्य विषय ग्राम साहित्य था। ग्राम साहित्य को लेकर उनकी अपनी कुछ विशिष्ट और अलग मान्यताएँ रही हैं। अपनी मान्यताएँ समय-समय पर वे पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में भी लाते रहे हैं। सोचा, यह अच्छा अवसर है जब प्राध्यापकों और एकत्रित लेखक-समूह के मध्य वे अपनी बात सीधे-साधे रख सकते हैं। उन्होंने यह आग्रह स्वीकार कर लिया। वे तय करके आए थे, पहले ही दिन अपने व्याख्यान के तुरंत बाद, समय रहा तो निकल जाएँगे। नहीं तो दूसरे दिन सुबह की पहली बस तो पकड़ ही लेंगे। अनावश्यक भीड़भाड़ दीपांकर को पसंद नहीं है, मानो दम घुटने लगता है। जिंदगी को मस्ती मानकर जीने का अंदाज भी उन्हें नहीं आता या यूँ कहा जा सकता है कि उस तरह से कभी जीए ही नहीं। अपना अकेलापन ही आनंददायक लगता है, आकाश की अनंत ऊँचाई में उड़ते उस पक्षी की तरह जो अकेले हवा में अपने पंखों को तौलता है।
दीपांकर का व्याख्यान देर से शुरू हुआ, लंच के बाद। व्याख्यान के बाद कई प्रश्न-प्रतिप्रश्न उठे। खासा वक्त निकल गया। बहरहाल वे संतुष्ट थे कि लोगों के सम्मुख अपनी बात रख सके। कई जाने-माने साहित्यकार भी वहाँ बैठे थे। साहित्य जगत् में एक लेखक के तौर पर अब तक उनकी भी जगह बन चुकी थी। जानते थे, पूर्वाग्रह के चलते चाहे कोई उनकी बात की अपेक्षा भले ही कर दे, पर उन्हें हलके से लेने की गलती नहीं कर सकता था।
उस विशाल सभागार के मंच से जब वे नीचे उतर रहे थे तो परम संतुष्ट थे। सभागार में बहुत भीड़ थी। आयोजक महाविद्यालय का प्राध्यापक वर्ग आगंतुकों के प्रति पूरी तरह सतर्क दिखाई देता था। पुरुष हों या महिलाएँ, सभी ने अपने सीने पर रंगीन रिबन से बने खूबसूरत बिल्ले धारण किए हुए थे। दीपांकर को आयोजक मित्र के प्रबंध और महाविद्यालय के सहयोगियों द्वारा उन्हें मिल रहे सहयोग पर अतीव प्रसन्नता हुई। आज के दौर में यह परम दुर्लभ दृश्य था। ऐसी एकता, ऐसा ऐक्य भाव अब कहाँ रहा ? नीचे उतरकर सभागार की अपनी कुरसी पर वापस बैठे तो थका हुआ अनुभव कर रहे थे। प्यास का अनुभव भी हुआ। पानी के लिए आँखें उठाकर जब तक इधर-उधर देखते, ट्रे में पानी लिया हुआ एक हाथ ठीक उनके सामने आ गया। साँवला किंतु खूबसूरत हाथ, जिसकी कलाई पर एक पतली सुनहरी घड़ी बँधी हुई थी। वे चौंके, कलाई कुछ-कुछ परिचित-सी लगी, जैसे पहले भी कहीं यह कलाई देखी हो। चकित भाव से आँखें उठाकर देखा तो देखते रह गए। सामने अपनी परिचित मुस्कराहट बिखेरती हुई शाल्मती खड़ी थी–डॉ० शाल्मली कुमार, हलके चमकदार बादामी बॉर्डर वाली आसमानी रंग की साड़ी में फबती हुई।
‘मुझे पता है कि इस वक्त आपको पानी की जरूरत होगी। कॉलेज में हर लेक्चर के बाद आप पानी पिया करते थे...’ शाल्मली ने बहुत गहरी आँखों से उन्हें निहारा। बोली, ‘लीजिए, सर !’
लगा, प्यास ही गायब हो गई है। यह इतना अप्रत्याशित था कि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। शाल्मली से दोबारा फिर कभी भेंट हो सकेगी, वह भी इस तरह से, सोचा नहीं था। पर सामने शाल्मली ही थी, सचमुच की शाल्मली।
पानी की एक घूँट के साथ ही वे निमिष-भर के लिए कहीं पीछे चले गए...सप्ताह-भर बुखार में रहने के बाद वापस कॉलेज आए हुए थे। कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। शाल्मली मौका तलाशकर विभाग में आई थी और उनकी अलमारी में ग्लूकोन-डी का डब्बा रखती हुई बोली थी, ‘आप ग्लूकोज का पानी पिया कीजिए, सर ! वीकनेस हो रही होगी...’ हैरत हुई कि इस क्षण भी पानी में ग्लूकोज डला हुआ था। उन्होंने हैरत-भरी आँखें उठाई और उसे देखने लगे।
‘पानी पीजिए, सर, लोग देख रहे हैं...’ शाल्मली किंचित् शरारत से मुस्कराई। उसका यह शरारताना अंदाज वैसा ही था, पुराना। वे सजग हुए। आखिर वे सभागार में बैठे हुए थे और उनके चतुर्दिक, तमाम लोग थे। उन्होंने पानी पिया और गिलास वापस ट्रे में रख दिया।
‘थोड़ी देर में मिलते हैं, सर !...’ शाल्मली जैसे फुसफुसाई थी। वह मुड़ी, ‘धीरे-धीरे उनसे दूर निकलकर आँखों से ओझल हो गई।
एक तरह की अचकचाई-सी स्थिति में जस के तस बैठे रह गए दीपांकर...
शेष वक्त अब सभागार में उनका मन नहीं लगा। वहाँ होते हुए भी जैसे वे वहाँ नहीं रह गए थे। कौन क्या कह रहा है ? क्या कार्रवाई चल रही है ? कौन वक्ता बोल रहा है ? उनके लिए सब अर्थहीन हो गया था। कानों में सिर्फ ध्वनियाँ थीं, शब्द नहीं। लगा, शरीर भर यहाँ रह गया है, मन न जाने कहाँ-कहाँ भटकने लगा है, किस लोक में। हालाँकि वे भरपूर कोशिश कर रहे थे कि पूरे मनोयोग से यहाँ रह सकें, मन को लौटा भी रहे थे बार-बार ताकि वह यहीं बना रहे, इसी सभागार में। पर लगा, चीजें एकाएक और अभी-अभी उनके अपने नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। उनका कतई कोई वश ही नहीं रह गया है उन पर। अपने को सभागार की कार्रवाई पर केंद्रित रखना सच में मुश्किल पड़ने लगा था। दीपांकर ने आँखें मूँदीं और कुरसी के पुश्ते पर आराम से पीठ टिका ली।
आयोजन का यह अंतिम सत्र था, इसलिए जल्दी समाप्त हो गया था। उन्होंने राहत की साँस ली। राहत का यह माहौल पूरे सभागार में ही प्याप्त दिखाई दिया। लोग जैसे किसी बंधन से मुक्त हुए थे और खुलकर चहकने लगे थे। पूरे सभागार में अब में अब बोलने-बतियाने की ध्वनि थी, एक कोने से दूसरे कोने तक उठती-गिरती स्वर-लहरी...। अब सामान्य बातें होने लगी थीं–दुनियादारी की वे सब बातें जिनमें आम तौर पर उनकी कोई रुचि नहीं है। आयोजकों ने बताया था कि यहाँ से निवृत होकर सीधे शाम की चाय पर चलना है। वे लोगों का अनुसरण करते हुए धीरे-धीरे बढ़ने लगे। कुछ एक युवा प्राध्यापक व शोधार्थी उनके साथ हो लिए थे, कदाचित् उनकी रुचि दीपांकर के साहित्य में प्रतीत होती थी। लेखक को यदि उसके पाठक मिल जाएँ तो फिर उसे और क्या चाहिए ? वह इतना गदगद हो उठता है कि दुनिया-जहान की दूसरी तमाम बातें ही भूल जाता है। पर उस क्षण उनसे बतियाते हुए भी पहली बार ऐसा लग रहा था कि पाठक भी उनके अनमनेपन को नहीं तोड़ पा रहे हैं।
जहाँ चाय की व्यवस्था थी, वहाँ लोग समूहों में बँट गए थे, अपनी-अपनी बातों में खोए, हँसते-बतियाते हुए। कुछ लोग उनके आसपास भी थे। किसी ने उनके आज के व्याख्यान की चर्चा की थी, उन्हें नई स्थापनाओं के लिए साधुवाद दिया था। किसी ने जानना चाहा था कि इन दिनों वे क्या नया लिख रहे हैं ? उन्होंने यथासंभव सबकी जिज्ञासाओं का समाधान किया था, कोशिश की थी कि उन्हीं की तरह हँसते, मुस्कराते दिख सकें। पर सच्चाई तो यह थी कि वे एकदम अकेले होना चाहते थे ताकि यदि कहीं आसमान शाल्मली हो तो उनकी आँखें उसे खोज सकें। अंततः वे क्षमायाचना करते हुए खुद ही एक किनारे जाकर खड़े हो गए। चाय सिप करते हुए उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी आँखें घुमाईं। अकस्मात् देखा, शाल्मली कुछ ही दूरी पर खड़ी उन्हीं को निहार रही है। दोनों की आँखों ने एक-दूसरे का स्पर्श किया। दीपांकर के भीतर एक अजीब-सी बयार बही...उस बयार में एक अनुगूँज भी उभरी...तो क्या शाल्मली के मन में आज भी, अब भी उनके लिए जगह है ? या वह यूँ ही देख रही थी ? वह देखना महज एक संयोग भर था ? या फिर वह खुद भी कहीं यह तो नहीं जाँचना चाह रही थी कि दीपांकर के मन में उसके लिए आज भी कुछ बचा है या...
उन्होंने आँखें हटा लीं और दूसरी दिशा में देखने लगे, कुछ ड्रस तरह जैसे उनकी आँखों को उसकी तलाश नहीं है। वह महज इत्तफाक है कि आँखें मिल गईं।...तभी महसूस हुआ, शाल्मली उनके निकट चली आ रही है, धीरे-धीरे और सधे कदमों से। शाल्मली का चलना सदैव बहुत सधा हुआ होता था। निकट पहुँचकर उन्हें जैसे चौंकाते हुए पूछा, ‘कैसे हैं, सर ?’
आँखें उठाई और शाल्मली पर टिका दीं। शाल्मली आज भी वैसी ही लगी, उतनी ही युवा और उतनी ही ताजा, हालाँकि देह से थोड़ी स्थूल लग रही थी, कुछ ज्यादा ही मांसल। और उसकी वे खूबसूरत, मायाविनी आँखें...? वे भी जस की तस थीं, जादू से परिपूर्ण। उन्होंने अपने जीवन में दोबारा फिर वैसी आँखें नहीं देखीं–बोलती, गाती और नृत्य करती आँखें...।
‘ठीक हूँ। आप सुनाएँ, आप कैसी हैं ?’ दीपांकर ने अपने को संयत किया, सँभाला। हालाँकि जानते थे, शाल्मली कुछ और ही सुनना चाहती होगी, कुछ ऐसा जो उसे गुदगुदाए, खुशी से सराबोर करे, मसलन यही कि तुम्हारे बिना मैं कैसा हो सकता हूँ, जरा कल्पना करो तो शाल्मली...! पर नहीं, इस तरह के किसी संवाद का कोई मतलब नहीं था, निरर्थक था वह सब, अतीत कथा हो चुका था। उनके उत्तर से शाल्मली के चेहरे पर हलकी बेचैनी उभरी। बोली, ‘अब भी वही ‘आप’ संबोधन, सर...अब तो कम से कम लौट आइए ‘तुम’ पर...।’
‘अतीत कभी लौटकर आता है, शाल्मली जी ? नहीं आता न ! आप चाहे अतीत से कितने ही चिपके रहें, पर वहाँ वापस तो नहीं पहुँच सकते। वहाँ से आप आगे बढ़ चुके होते हैं...’ वे मुस्कराए। भीतर चाहे कितनी ही उथल-पुथल क्यों न हो रही हो, पर बाहर से वे निर्विकार बने रहना चाहते थे, एकदम तटस्थ, जैसे वह सब वे वास्तव में भूल चुके हैं, उबर चुके हैं उस सबसे। कहा, ‘जीवन का नाम ही गति है। उसमें कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। जो कल था वह आज कैसे हो सकता है और जो आज है वह कल नहीं होगा...’
चाय पीती हुई शाल्मली के होंठ हलके से हिले, काँपे, थरथराए। कदाचित् वह कुछ कहना चाहती थी कि तभी सेमिनार के संयोजक उनके लेखक मित्र डॉ० रिपुदमन निकट आए। बोले, ‘यहाँ कहाँ खड़े हो, यार ! चलो, उधर चौकड़ी जमी है। तुम्हारे मतलब की बात तो वहाँ पर है।’
उन्होंने आँख उठाकर देखा। उधर चंद-एक स्वनामधन्य आलोचक थे, बेहद भदेस ढंग से हँसते-ठठाते हुए। उनके मित्र रिपुदमन इस सब काम में सिद्धहस्त हैं। साल-दो-साल में कहानी चाहे एकाध ही लिखें या वह भी नहीं, पर जोड़-जुगाड़ कुछ इस तरह बिठाए रहते हैं कि लगता है, पहुँचे हुए लेखक हैं। बिना कुछ लिखे हुए भी अपनी चर्चा करवा लेते हैं। इन तथाकथित बड़े महंतों की परिक्रमा कर इधर के छोटे-मोटे महंत के रूप में अपनी मान्यता के लिए वे जिस तरह छटपटाते हैं, देखकर दया आती है। पर दीपांकर को तो ये तथाकथित महंत सदा से ही परोपजीवी लगते रहे हैं, दूसरों के उच्छिष्ट अन्न पर पलने वाले मंदिरों-आश्रमों के मुस्टंज महंतों की तरह। लेखक लिखेगा ही नहीं तो ये आलोचक बेचारे कहाँ से अपनी दुकान चलाएँगे ! शताब्दियाँ बीत गई हैं, सूर-तुलसी अपनी जगह अमर हैं, पर कहाँ हैं उनके टिप्पणीकार, उनके आलोचक ? कोई जानता भी है क्या उन्हें ? दीपांकर समझ नहीं पाते, क्यों एक लेखक को आलचकों के पीछे लगकर अपनी ऊर्जा नष्ट करनी चाहिए ? पर आश्चर्य है कि आजकल ऐसा ही ज्यादा हो रहा है। एक अजब उलटी रीत बह रही है। लेखक का काम लिखना है, उसे सिर्फ लिखते रहना चाहिए। हाँ, अपने पाठकों पर उसकी सजग दृष्टि अवश्य होनी चाहिए, बाकी रही आलोचकों की बात, तो लेखक को क्यों उनके आगे-पीछे घूमना चाहिए ? क्यों उनकी चिरौरी करनी चाहिए ? पर हो ऐसा ही रहा है, फलतः कोयल तो हाशिए पर आ गई हैं और दादुरों की चल पड़ी है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे कभी इस मार्ग पर नहीं चले हैं। समझ रहे हैं कि रिपुदमन उनका भला ही चाहते हैं। सोच रहे हैं कि संयोग से एकत्रित हुए इन पाँच-सात आलोचकों से वे मिल लें, उन्हें प्रसन्न कर लें ताकि वे उनकी चर्चा भी करें, उन पर भी कुछ लिखें।
‘सोच क्या रहे हो...’ दीपांकर को विचारमग्न देख रिपुदमन ने झकझोरा, ‘मिल लो, यार ! क्या पता तुम्हारे नए उपन्यास पर ही कुछ चर्चा-वर्चा कर दें...’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i