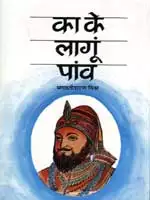|
जीवन कथाएँ >> का के लागूं पांव का के लागूं पांवभगवतीशरण मिश्र
|
209 पाठक हैं |
|||||||
गुरु गोविन्द सिंह के आरंभिक जीवन और उनके पिता गुरु तेगबहादुर के साहस, शौर्य और अन्ततः उनकी लौहर्षक शहादत की यथापरक रोचक भाव-गाथा...
Ka ke Lagun Panv - A hindi Book by - Bhagwati Sharan Mishra का के लागू पाँव - भगवतीशरण मिश्र
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
गुरु गोविन्द सिंह के आरंभिक जीवन और उनके पिता गुरु तेगबहादुर के साहस, शौर्य और अन्ततः उनकी लौहर्षक शहादत की यथापरक रोचक भाव-गाथा। भाषागत सौन्दर्य और शिल्पगत उत्कर्ष का एक अद्भुत उदाहरण। इतिहास के कटु यथार्थ को कल्पना की इन्द्रधनुषी छटा का एक सम्मोहक सम्मिश्रण जिसने प्रस्तुत की है एक ऐसी औपन्यासिक कृति जो अपने विशिष्ट प्रवहमानता और पटनीयता के कारण पाठक को आद्यन्त बाँधने में समक्ष होने के साथ साथ उसके चिन्तन को नयी क्षितिज और उसकी संवेदना को एक अनाम पुलक प्रदान करने में सक्षम है।
आरम्भ
हां, यह आरम्भ ही है एक ऐसे अन्त का जो अनन्त काल तक इतिहास-पृष्ठों को अमर करता रहेगा। यह कहानी है एक पुत्र की। एक पिता की। पिता जो हंसते-हंसते अपने आदर्शों की बलि चढ़ गया, शहादत गले लगा ली। पुत्र जिसकी तैयारी पूरी है पिता के मार्ग पर—पितृपथ—पर बढ़ने की। पिता जो शेर था, पुत्र जो अभी शेर-शावक है, सिंह-पुत्र। सिहों की जमाते नहीं होतीं पर वह वही करने वाला है—आदमियों को सिंह बनाने वाला। पिता हैं गुरु तेगबहादुर और पुत्र है गुरु गोबिन्द सिंह, अभी मात्र गोबिन्द, गोबिन्द राय।
यह गाथा है पिता के बलिदान की, शहादत की, साहस और शौर्य की, उसके अन्त की; तो यह कहानी है पुत्र के आरम्भ की, उसमें निहित सम्भावनाओं की, इन सम्भावनाओं के इजहार की। एक महापुरुष के निर्माण और उसके लिए आवश्यक आत्मविश्वास, अपार सहनशक्ति और अलौकिक आदान-अवदान की। उसके लिए प्राप्त पिता के स्नेह-प्रेम की, शिक्षण-प्रशिक्षण की। पितृ-पक्ष की।
कहना कठिन है कि यह गुरु गोबिन्द सिंह के आरम्भिक दिनों की कहानी अधिक है अथवा गुरु तेगबहादुर के त्याग-तपस्या, साधना-साहस और अन्ततः एक सार्थक शहादत, एक अर्थपूर्ण निर्वाण, एक अभूतपूर्व उत्सर्ग और एक निर्भीक बलिदान की। शायद दोनों की। पर एक का अन्त ही दूसरे का आरम्भ है। दूसरे की आरम्भ हुई गाथा भी एक दिन इसके अन्त तक गाई जा सकेगी, ‘वाहे गुरु’ से इसी आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ इस ग्रंथ को एक महान् शहादत के खून की स्याही से समाप्त किया गया है। पिता की चिता की राख झाड़कर खड़े होते उस नर-केसरी की शेष कहानी की प्रतीक्षा कीजिए जिसने इतिहास के पृष्ठों को एक नया अर्थ दिया। यह पुस्तक तो एक ग्रंथ की भूमिका मात्र है—पूर्व-पीठिका।
जी, यह उपन्यास जैसी लिखी जीवनियां हैं दो की, एक के आरम्भ और दूसरे के अन्त की। सूर्योदय और सूर्यास्त की सम्मिलित गाथा है यह। यह अकिंचन अर्घ्य दोनों को समान रूप से निवेदित है।
उगते सूर्य को नैवेद्य अर्पित करने की प्रथा यहां पुरानी है, डूबते सूर्य को उपेक्षित करने की भी। पर यह भूलना कितनी बड़ी मूर्खता है कि सूर्यास्त नहीं हो तो सूर्योदय के दर्शन किधर से हों ? सूर्यास्त के गर्भ से ही सूर्योदय को प्रकट होना है, इसे कम ही समझ पाते हैं।
गुरु गोबिन्द सिंह की गाथा के साथ इतिहास और साहित्य में भले ही पूरा न्याय हुआ हो पर पिता गुरु तेगबहादुर को भरपूर न्याय मिला कलमकारों के हाथों, इसका दावा कौन करेगा ? आने वाली पंक्तियों में इसी क्षतिपूर्ति का आयोजन है। सही है, यह पुस्तक गुरु गोबिन्द को लेकर आरम्भ हुई है पर इसमें सर्वाधिक न्याय हुआ है पुत्र के बदले पिता के साथ ही। यह कहानी अगर पुत्र के निर्माण और निर्भीकता की है तो पिता के पंथ हेतु प्रचार-प्रसार, त्याग-बलिदान और संघर्ष तथा अन्ततः समाप्ति की कुछ कम नहीं है।
हां, न्याय हुआ है पुत्र की इस गाथा में पिता के साथ भी पर्याप्त ही। इस क्रम में मेरे अपने कुछ अनुभवों का कम योगदान नहीं है। सही है कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इतिहास-पृष्ठों को ही उपजीव्य बनाकर इसे पूरा किया जा सकता था पर मुझे मात्र इतने से संतोष करने की विविशता नहीं रही।
उस असम की धरती, उसके लोगों और उसके मिज़ाज से परिचित होने का मुझे ही किसी कारण पूर्ण अवसर मिला है, जहां धर्म-प्रचार के लिए गुरु तेगबहादुर ने अपने जीवन का एक बहुमूल्य अंश लगाया। मैं पूरी तरह परिचित हूं ब्रह्मपुत्र नद की प्रकृति और उसकी सदा परिवर्तित होती भंगिमाओं से जिसके तीर कभी गुरु-चरण-धर्म-प्रचार में भटके थे। मैंने सवारी की है इस नद के पेट पर तैरती छोटी-बड़ी विचित्र नौकाओं में जिनका सहारा गुरु-तेगबहादुर ने भी अपने असम अभियान के समय लिया। मैं परिचित हूं आज से वर्षों पूर्व की असम की उस धरती से, उसके वनस्पति-संकुल ग्राम-गृहों से, वहां के भोले-भाले वासियों आदि-वासियों से जब इस धरती पर बारुदी सुरंगें नहीं बिछती थीं और जब ब्रह्मपुत्र नद का पानी मनुष्यों के रक्त से रंजित नहीं हुआ करता था। यह आज से प्रायः 25 वर्ष पूर्व संभव हुआ। समय का वह बहुमूल्य टुकड़ा, वह मोहक काल-खंड आज मेरे लिए सार्थक हो आया है जब मैंने गुरु के असम-प्रवास में प्राणवत्ता भरने का प्रयास किया।
यही कारण है कि उपन्यास होते हुए भी यह कृति काल्पनिक अतिरंजना से रहित है। जो कुछ है वह यथार्थ के इर्द-गिर्द ही बुना गया है। ठीक उसी तरह जैसे असम के हस्त-करघों पर कभी अनेकानेक कोमल-कमनीय कर रेशम के वस्त्र बुना करते थे, कुछ आज भी बुनते हैं।
ऐतिहासिक उपन्यास है। यह पर इसमें इतिहास अधिक बोलता है, उपन्यास कम। यही कारण है कि इसका एक पात्र भी काल्पनिक नहीं, चाहे इसका सम्बन्ध गुरु-पुत्र से हो या पिता से। कोई यह भ्रम नहीं पाले कि अर्द्ध विक्षिप्त पंडित शिवदत्त से लेकर पीर भीखन शाह अथवा अथवा राजा फतहचन्द मैनी और मामा किरपालचन्द में से कोई भी लेखकीय कल्पना की उपज है।
पाटलिपुत्र-वासी हूं मैं। अतः गुरु बालक गोबिन्द राय की बाल्यकाल की घटनाओं का साक्षी नहीं होकर भी उनके वर्णन के लिए काल्पनिक अतिरंजना की बैसाखी मुझे नहीं थामनी पड़ी। जो कुछ लिखा गया वह सत्य के समीप है, कल्पना से दूर। आज भी गुरुद्वारा हरिमन्दिर साहब के आंगन और पटना सिटी (पाटलिपुत्र) की बंकिम गलियों की हवाओं में गुरु बालक की बाल-क्रीड़ाओं की गंध घुली मिल जायेगी। आवश्यकता है पर्याप्त घ्राण-शक्ति की, गहरी संवेदनशीलता की।
बहुत डोला हूं मैं इस गुरुद्वारे के प्रांगण में—इसके उस प्रसिद्ध कुएं के आस-पास जिसका जल मिश्री की मिठास संजोये है, इसके उपयोगी संग्रहालय के अन्दर, इसकी उस पक्की बारहदरी के आसपास जो कभी मात्र पगडंडी थी जिस पर पैर रोप कर पहुंचा था गुरु-परिवार यहां उस समय जब गुरु-गोबिन्द गर्भस्थ ही थे। बहुत कुछ, सुना-समझा है यहां, अनुभूत किया है तब लिपि-बद्ध करने का साहस संजोया है इस गुरु-गाथा को।
नहीं, प्रायः कुछ भी काल्पनिक नहीं है इस उपन्यास में सिवा उन स्थानों के जहां मेरा कथाकार प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में रमने से अपने को रोक नहीं पाया है अथवा मेरे अन्दर का दार्शनिक जग पड़ा है अपने कुछ चिन्तत-मनन के साथ जो कुछ के लिए सम्मोहक और उपयोगी हो सकता है तो कुछ के लिए अनावश्यक भी। पर समीक्षक-पाठक मुझे क्षमा करेंगे, गंगा और सतलुज की धारा प्रतिक्षण नवीन होती रहती है तो औपन्यासिक शिल्प को भी अपने पुराने केंचुल से बाहर निकालना मेरी विवशता है। सपाट-बयानी का मैं कायल नहीं। अगर अधिकांश अध्यायों का आरम्भ, उनमें अन्तर्निहित कथा का सार चिन्तन-धाराओं के माध्यम से प्रस्तुत करता जाता है तो मैं इसके लिए अपने ‘अनर्गल’ दर्शन को आप पर थोपने का अपराधी नहीं हूं। लकीर के फकीर इसे पढ़कर सिर पीटने को स्वतंत्र हैं पर इस सबके माध्यम से मैंने कुछ देने का ही प्रयास किया है—कम-से-कम एक नये शिल्प-विधान को, कुछ नहीं तो एक नूतन-कथ्य-संयोजन को। अगर यह आपके पल्ले नहीं पड़े और आप इसे उपन्यासकार का पाठक के आमने-सामने आ खड़ा होने की घटना कहें तो मैं इतना ही कहूँगा की उपन्यासकार से भागने की आपकी यह प्रवृत्ति व्यर्थ ही है। वह सीधे सामने नहीं भी आये तो पुस्तक के पृष्ठ-पृष्ठ पर तो वह वर्तमान ही है। अधिकांश चरित्र तो उसी की भावना, उसी के मनोभावों तक को अभिव्यक्ति देते हैं। एक कथा-पाठक एक कथा- लेखक से कब तक और कहां-कहां तक भागता फिरेगा ?
फिर भी, जैसा कहा, पूरी तरह, यथार्थ के इर्द-गिर्द ही बुना गया है इस कहानी को। इतिहास के साथ विशेषकर किसी धर्म-सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्धित इतिहास के साथ बहुत खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं मिलती उपन्यासकार को। अगर कोई यह समझे कि पाटलिपुत्र से आनन्दपुर की यात्रा को मैंने कल्पना के बल पर आवश्यक रूप से लम्बा खींचा है तो जवाब उसे इतिहास पृष्ठों में ढूँढ़ना चाहिए। नानकी देवी का तीर्थ-यात्रा-प्रेम मेरी कपोल-कल्पना नहीं है, न उनका मायका-प्रेम ही। अगर गुरु गोबिन्द को आनन्दपुर पहुंचाने में उन्होंने इतना समय लिया था कुछ प्रमाद का ही जाने अनजाने प्रदर्शन किया तो इसका स्पष्टीकरण उन्हीं के पास होगा। एक ऐतिहासिक उपन्यासकार को सत्य को नकारने की स्वतन्त्रता नहीं होती।
जीवनीपरक उपन्यासों के लेखन की ओर मेरी प्रवृत्ति इधर क्यों बढ़ी है, इसको लेकर भी प्रश्न उठाये गए हैं। उत्तर सीधा है। जिनकी जीवनियां पढ़ने-योग्य हैं, प्रेरणापूर्ण हैं, उन्हें नहीं पढ़ना अपने को वंचित ही करना है। पर आप जीवनी नहीं पढ़ना चाहते—उपन्यास पढ़ सकते हैं, विशेषकर नई पीढ़ी के लोग। इसलिए ये जीवनीपरक उपन्यास परोसने जा रहा हूं मैं। ऐसे नहीं तो, ऐसे जानिए उनको जिन्हें नहीं जानकर आप अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता, अपने समृद्ध इतिहास में ही कट जाइएगा। कुनैन की गोलियों को मीठी चाशनी में डुबो-कर ही देना पड़ता है। यही विवशता है मेरी। जीवनी आप पढ़ने से भागिए पर मैं उपन्यास के रूप से ही उसे पढ़ने को विवश करूंगा आपको।
अपने पाठकों के अपार प्रेम तथा अपने मित्रों यथा समर्थ समीक्षक डॉ. पुष्पाल सिंह, उपन्यासकार डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, कथाकार भाई राजेन्द्र अवस्थी, सुधी समीक्षक डॉ.बालेन्दुशेखर तिवारी और डॉ.अमर कुमार सिंह, डॉ.भूपेन्द्र कलसी, श्रेष्ठ साहित्यकार श्री जयप्रकाश भारती, विद्वान सम्पादक डॉ.गिरिजाशंकर त्रिवेदी, श्रेष्ठ लेखक और मेरे उपन्यास ‘पहला सूरज’ के तमिल अनुवादक श्री गौरीराजन, ‘एक और अहल्या’ के बंगला सम्पादक तथा श्रेष्ठ कवि—लेखक श्री कालिपद दास, नई पीढ़ी के अपने अनुजवत् साहित्यकारों डॉ. शिवनारायण, श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी, श्री भोलाप्रसाद सिंह तोमर, डॉ.सतीश राज पुष्करणा, श्री राजेन्द्र परदेसी, स्वच्छतावादी समीक्षक प्रो.डॉ.अजब सिंह (अलीगढ़ विश्वविद्यालय), डॉ.नागेन्द्र सिंह मेहता, इस पांडुलिपी के प्रस्तुतिकरण में सहयोगी फिलोमिना टोप्पो, श्री देवेन्द्र चौधरी, मो.नसीम, श्री जगत नारायण राय, अरविन्द, अनिल, राजपाल एण्ड सन्स के श्री सतीश जी, श्री अंजनी कुमार मिश्र, मेरे ऊपर शोध-कार्य सम्पन्न करने वाले डॉ. कुणाल कुमार, सुश्री एस.रत्ना तथा अन्य शोधकर्ता-कर्त्तृ, जिनकी संख्या दर्जनों में है, के साथ-साथ अपने परिजनों प्राचार्य डॉ.सीताशरण मिश्र, श्री श्रीनिवास पांडेय, बहन गीता पांडेय की स्नेह-श्रद्धा का आभार मानता हूं।
अन्त में राजपाल एंड सन्ज़ के विद्वान् स्वत्वाधिकारी श्री विश्वनाथजी का साधुवाद करना चाहूंगा जिनके स्नेहपूर्ण आग्रह और विस्मयकारी तत्परता के फल-स्वरूप ही मेरी कृतियाँ इस रूप में प्रकाश में आती रही हैं।
आस्थावान हूं अतः, अपनी नगण्य उपलब्धियों के मूल में निश्चित रूप से निहित किसी दैवी शक्ति के प्रति भी विनम्र नमन निवेदित करना अपना धर्म ही नहीं कर्तव्य मानता हूं।
यह गाथा है पिता के बलिदान की, शहादत की, साहस और शौर्य की, उसके अन्त की; तो यह कहानी है पुत्र के आरम्भ की, उसमें निहित सम्भावनाओं की, इन सम्भावनाओं के इजहार की। एक महापुरुष के निर्माण और उसके लिए आवश्यक आत्मविश्वास, अपार सहनशक्ति और अलौकिक आदान-अवदान की। उसके लिए प्राप्त पिता के स्नेह-प्रेम की, शिक्षण-प्रशिक्षण की। पितृ-पक्ष की।
कहना कठिन है कि यह गुरु गोबिन्द सिंह के आरम्भिक दिनों की कहानी अधिक है अथवा गुरु तेगबहादुर के त्याग-तपस्या, साधना-साहस और अन्ततः एक सार्थक शहादत, एक अर्थपूर्ण निर्वाण, एक अभूतपूर्व उत्सर्ग और एक निर्भीक बलिदान की। शायद दोनों की। पर एक का अन्त ही दूसरे का आरम्भ है। दूसरे की आरम्भ हुई गाथा भी एक दिन इसके अन्त तक गाई जा सकेगी, ‘वाहे गुरु’ से इसी आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ इस ग्रंथ को एक महान् शहादत के खून की स्याही से समाप्त किया गया है। पिता की चिता की राख झाड़कर खड़े होते उस नर-केसरी की शेष कहानी की प्रतीक्षा कीजिए जिसने इतिहास के पृष्ठों को एक नया अर्थ दिया। यह पुस्तक तो एक ग्रंथ की भूमिका मात्र है—पूर्व-पीठिका।
जी, यह उपन्यास जैसी लिखी जीवनियां हैं दो की, एक के आरम्भ और दूसरे के अन्त की। सूर्योदय और सूर्यास्त की सम्मिलित गाथा है यह। यह अकिंचन अर्घ्य दोनों को समान रूप से निवेदित है।
उगते सूर्य को नैवेद्य अर्पित करने की प्रथा यहां पुरानी है, डूबते सूर्य को उपेक्षित करने की भी। पर यह भूलना कितनी बड़ी मूर्खता है कि सूर्यास्त नहीं हो तो सूर्योदय के दर्शन किधर से हों ? सूर्यास्त के गर्भ से ही सूर्योदय को प्रकट होना है, इसे कम ही समझ पाते हैं।
गुरु गोबिन्द सिंह की गाथा के साथ इतिहास और साहित्य में भले ही पूरा न्याय हुआ हो पर पिता गुरु तेगबहादुर को भरपूर न्याय मिला कलमकारों के हाथों, इसका दावा कौन करेगा ? आने वाली पंक्तियों में इसी क्षतिपूर्ति का आयोजन है। सही है, यह पुस्तक गुरु गोबिन्द को लेकर आरम्भ हुई है पर इसमें सर्वाधिक न्याय हुआ है पुत्र के बदले पिता के साथ ही। यह कहानी अगर पुत्र के निर्माण और निर्भीकता की है तो पिता के पंथ हेतु प्रचार-प्रसार, त्याग-बलिदान और संघर्ष तथा अन्ततः समाप्ति की कुछ कम नहीं है।
हां, न्याय हुआ है पुत्र की इस गाथा में पिता के साथ भी पर्याप्त ही। इस क्रम में मेरे अपने कुछ अनुभवों का कम योगदान नहीं है। सही है कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इतिहास-पृष्ठों को ही उपजीव्य बनाकर इसे पूरा किया जा सकता था पर मुझे मात्र इतने से संतोष करने की विविशता नहीं रही।
उस असम की धरती, उसके लोगों और उसके मिज़ाज से परिचित होने का मुझे ही किसी कारण पूर्ण अवसर मिला है, जहां धर्म-प्रचार के लिए गुरु तेगबहादुर ने अपने जीवन का एक बहुमूल्य अंश लगाया। मैं पूरी तरह परिचित हूं ब्रह्मपुत्र नद की प्रकृति और उसकी सदा परिवर्तित होती भंगिमाओं से जिसके तीर कभी गुरु-चरण-धर्म-प्रचार में भटके थे। मैंने सवारी की है इस नद के पेट पर तैरती छोटी-बड़ी विचित्र नौकाओं में जिनका सहारा गुरु-तेगबहादुर ने भी अपने असम अभियान के समय लिया। मैं परिचित हूं आज से वर्षों पूर्व की असम की उस धरती से, उसके वनस्पति-संकुल ग्राम-गृहों से, वहां के भोले-भाले वासियों आदि-वासियों से जब इस धरती पर बारुदी सुरंगें नहीं बिछती थीं और जब ब्रह्मपुत्र नद का पानी मनुष्यों के रक्त से रंजित नहीं हुआ करता था। यह आज से प्रायः 25 वर्ष पूर्व संभव हुआ। समय का वह बहुमूल्य टुकड़ा, वह मोहक काल-खंड आज मेरे लिए सार्थक हो आया है जब मैंने गुरु के असम-प्रवास में प्राणवत्ता भरने का प्रयास किया।
यही कारण है कि उपन्यास होते हुए भी यह कृति काल्पनिक अतिरंजना से रहित है। जो कुछ है वह यथार्थ के इर्द-गिर्द ही बुना गया है। ठीक उसी तरह जैसे असम के हस्त-करघों पर कभी अनेकानेक कोमल-कमनीय कर रेशम के वस्त्र बुना करते थे, कुछ आज भी बुनते हैं।
ऐतिहासिक उपन्यास है। यह पर इसमें इतिहास अधिक बोलता है, उपन्यास कम। यही कारण है कि इसका एक पात्र भी काल्पनिक नहीं, चाहे इसका सम्बन्ध गुरु-पुत्र से हो या पिता से। कोई यह भ्रम नहीं पाले कि अर्द्ध विक्षिप्त पंडित शिवदत्त से लेकर पीर भीखन शाह अथवा अथवा राजा फतहचन्द मैनी और मामा किरपालचन्द में से कोई भी लेखकीय कल्पना की उपज है।
पाटलिपुत्र-वासी हूं मैं। अतः गुरु बालक गोबिन्द राय की बाल्यकाल की घटनाओं का साक्षी नहीं होकर भी उनके वर्णन के लिए काल्पनिक अतिरंजना की बैसाखी मुझे नहीं थामनी पड़ी। जो कुछ लिखा गया वह सत्य के समीप है, कल्पना से दूर। आज भी गुरुद्वारा हरिमन्दिर साहब के आंगन और पटना सिटी (पाटलिपुत्र) की बंकिम गलियों की हवाओं में गुरु बालक की बाल-क्रीड़ाओं की गंध घुली मिल जायेगी। आवश्यकता है पर्याप्त घ्राण-शक्ति की, गहरी संवेदनशीलता की।
बहुत डोला हूं मैं इस गुरुद्वारे के प्रांगण में—इसके उस प्रसिद्ध कुएं के आस-पास जिसका जल मिश्री की मिठास संजोये है, इसके उपयोगी संग्रहालय के अन्दर, इसकी उस पक्की बारहदरी के आसपास जो कभी मात्र पगडंडी थी जिस पर पैर रोप कर पहुंचा था गुरु-परिवार यहां उस समय जब गुरु-गोबिन्द गर्भस्थ ही थे। बहुत कुछ, सुना-समझा है यहां, अनुभूत किया है तब लिपि-बद्ध करने का साहस संजोया है इस गुरु-गाथा को।
नहीं, प्रायः कुछ भी काल्पनिक नहीं है इस उपन्यास में सिवा उन स्थानों के जहां मेरा कथाकार प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में रमने से अपने को रोक नहीं पाया है अथवा मेरे अन्दर का दार्शनिक जग पड़ा है अपने कुछ चिन्तत-मनन के साथ जो कुछ के लिए सम्मोहक और उपयोगी हो सकता है तो कुछ के लिए अनावश्यक भी। पर समीक्षक-पाठक मुझे क्षमा करेंगे, गंगा और सतलुज की धारा प्रतिक्षण नवीन होती रहती है तो औपन्यासिक शिल्प को भी अपने पुराने केंचुल से बाहर निकालना मेरी विवशता है। सपाट-बयानी का मैं कायल नहीं। अगर अधिकांश अध्यायों का आरम्भ, उनमें अन्तर्निहित कथा का सार चिन्तन-धाराओं के माध्यम से प्रस्तुत करता जाता है तो मैं इसके लिए अपने ‘अनर्गल’ दर्शन को आप पर थोपने का अपराधी नहीं हूं। लकीर के फकीर इसे पढ़कर सिर पीटने को स्वतंत्र हैं पर इस सबके माध्यम से मैंने कुछ देने का ही प्रयास किया है—कम-से-कम एक नये शिल्प-विधान को, कुछ नहीं तो एक नूतन-कथ्य-संयोजन को। अगर यह आपके पल्ले नहीं पड़े और आप इसे उपन्यासकार का पाठक के आमने-सामने आ खड़ा होने की घटना कहें तो मैं इतना ही कहूँगा की उपन्यासकार से भागने की आपकी यह प्रवृत्ति व्यर्थ ही है। वह सीधे सामने नहीं भी आये तो पुस्तक के पृष्ठ-पृष्ठ पर तो वह वर्तमान ही है। अधिकांश चरित्र तो उसी की भावना, उसी के मनोभावों तक को अभिव्यक्ति देते हैं। एक कथा-पाठक एक कथा- लेखक से कब तक और कहां-कहां तक भागता फिरेगा ?
फिर भी, जैसा कहा, पूरी तरह, यथार्थ के इर्द-गिर्द ही बुना गया है इस कहानी को। इतिहास के साथ विशेषकर किसी धर्म-सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्धित इतिहास के साथ बहुत खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं मिलती उपन्यासकार को। अगर कोई यह समझे कि पाटलिपुत्र से आनन्दपुर की यात्रा को मैंने कल्पना के बल पर आवश्यक रूप से लम्बा खींचा है तो जवाब उसे इतिहास पृष्ठों में ढूँढ़ना चाहिए। नानकी देवी का तीर्थ-यात्रा-प्रेम मेरी कपोल-कल्पना नहीं है, न उनका मायका-प्रेम ही। अगर गुरु गोबिन्द को आनन्दपुर पहुंचाने में उन्होंने इतना समय लिया था कुछ प्रमाद का ही जाने अनजाने प्रदर्शन किया तो इसका स्पष्टीकरण उन्हीं के पास होगा। एक ऐतिहासिक उपन्यासकार को सत्य को नकारने की स्वतन्त्रता नहीं होती।
जीवनीपरक उपन्यासों के लेखन की ओर मेरी प्रवृत्ति इधर क्यों बढ़ी है, इसको लेकर भी प्रश्न उठाये गए हैं। उत्तर सीधा है। जिनकी जीवनियां पढ़ने-योग्य हैं, प्रेरणापूर्ण हैं, उन्हें नहीं पढ़ना अपने को वंचित ही करना है। पर आप जीवनी नहीं पढ़ना चाहते—उपन्यास पढ़ सकते हैं, विशेषकर नई पीढ़ी के लोग। इसलिए ये जीवनीपरक उपन्यास परोसने जा रहा हूं मैं। ऐसे नहीं तो, ऐसे जानिए उनको जिन्हें नहीं जानकर आप अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता, अपने समृद्ध इतिहास में ही कट जाइएगा। कुनैन की गोलियों को मीठी चाशनी में डुबो-कर ही देना पड़ता है। यही विवशता है मेरी। जीवनी आप पढ़ने से भागिए पर मैं उपन्यास के रूप से ही उसे पढ़ने को विवश करूंगा आपको।
अपने पाठकों के अपार प्रेम तथा अपने मित्रों यथा समर्थ समीक्षक डॉ. पुष्पाल सिंह, उपन्यासकार डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, कथाकार भाई राजेन्द्र अवस्थी, सुधी समीक्षक डॉ.बालेन्दुशेखर तिवारी और डॉ.अमर कुमार सिंह, डॉ.भूपेन्द्र कलसी, श्रेष्ठ साहित्यकार श्री जयप्रकाश भारती, विद्वान सम्पादक डॉ.गिरिजाशंकर त्रिवेदी, श्रेष्ठ लेखक और मेरे उपन्यास ‘पहला सूरज’ के तमिल अनुवादक श्री गौरीराजन, ‘एक और अहल्या’ के बंगला सम्पादक तथा श्रेष्ठ कवि—लेखक श्री कालिपद दास, नई पीढ़ी के अपने अनुजवत् साहित्यकारों डॉ. शिवनारायण, श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी, श्री भोलाप्रसाद सिंह तोमर, डॉ.सतीश राज पुष्करणा, श्री राजेन्द्र परदेसी, स्वच्छतावादी समीक्षक प्रो.डॉ.अजब सिंह (अलीगढ़ विश्वविद्यालय), डॉ.नागेन्द्र सिंह मेहता, इस पांडुलिपी के प्रस्तुतिकरण में सहयोगी फिलोमिना टोप्पो, श्री देवेन्द्र चौधरी, मो.नसीम, श्री जगत नारायण राय, अरविन्द, अनिल, राजपाल एण्ड सन्स के श्री सतीश जी, श्री अंजनी कुमार मिश्र, मेरे ऊपर शोध-कार्य सम्पन्न करने वाले डॉ. कुणाल कुमार, सुश्री एस.रत्ना तथा अन्य शोधकर्ता-कर्त्तृ, जिनकी संख्या दर्जनों में है, के साथ-साथ अपने परिजनों प्राचार्य डॉ.सीताशरण मिश्र, श्री श्रीनिवास पांडेय, बहन गीता पांडेय की स्नेह-श्रद्धा का आभार मानता हूं।
अन्त में राजपाल एंड सन्ज़ के विद्वान् स्वत्वाधिकारी श्री विश्वनाथजी का साधुवाद करना चाहूंगा जिनके स्नेहपूर्ण आग्रह और विस्मयकारी तत्परता के फल-स्वरूप ही मेरी कृतियाँ इस रूप में प्रकाश में आती रही हैं।
आस्थावान हूं अतः, अपनी नगण्य उपलब्धियों के मूल में निश्चित रूप से निहित किसी दैवी शक्ति के प्रति भी विनम्र नमन निवेदित करना अपना धर्म ही नहीं कर्तव्य मानता हूं।
भगवतीशरण मिश्र
45/60, बेली रोड, पटना
27 फरवरी, 1994
45/60, बेली रोड, पटना
27 फरवरी, 1994
1
पवित्र भागीरथी के पश्चिमी कूल पर अवस्थित पाटलिपुत्र नगर। श्रेष्ठियों की गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से सज्जित, धन-धान्य-पूर्ण एक धर्मपरायण धरती, समृद्धि जहाँ कुंडली मारकर विराजमान थी।
अनेक उथल-पुथल, उत्थान-पतन, उत्सव-महोत्सव देखे हैं इस पुरातन नगर ने। अनेक महापुरुषों, धर्म-संस्थापकों-धर्माधिकारियों, विद्वानों, चिंतकों के चरण-रज से पवित्र हुए हैं यहां के राज-पथ, यहां कि लम्बी-पतली सौ-सौ बल खाती बंकिम वीथियां।
हां, कभी अनन्त ज्ञान-सम्पन्न भगवान बुद्ध ने भी धन्य किया था इस धरती को अपने चरण-चिह्नों से और अशोक महान् ने इसी नगरी को अपनी राजस्थली बनाकर तथागत के धर्मचक्र के नवीन गति एवं नूतन ऊर्जा भर सागर-पार तक पहुँचा दिया था उसे।
और तो और ‘ननकाना साहब’, उस समय की तलवंडी और अब पाकिस्तान के एक अंश में जन्मे सिखधर्म के महान प्रवर्तक गुरु नानक साहब ने भी अपने देश-विदेश-व्यापी यात्रा-क्रम में यहां आकर विशेष मान प्रदान किया था इस नगर और नगरवासियों को।
आज इस नगर की शोभा अनुपमेय थी। राजपथों पर भिश्तियों ने सुगन्धित जल का छिड़काव किया था। प्रवेशद्वार को कदली-स्तम्भों और अशोक वृक्ष के हरित पत्रों से सजाया गया था। उसके दोनों ओर चित्र-खचित, जल-पूरति मंगल-घटों की ऊर्ध्वाकार पंक्तियां भी रच दी गई थीं। महाद्वार के ठीक सामने दो गजराज रक्त-कमल-युक्त अपने विशाल सूँड़ों को स्वागत की मुद्रा में उठाए झूम रहे थे। स्वर्ण-तारों से निर्मित परिधानों से आच्छादित उनका सर्वांग अति सुन्दर लग रहा था। कुशल महावतों ने उनके प्रशस्त मस्तक को विभिन्न रंगों की चित्र-कारी द्वारा असामान्य रूप से मनोहारी बना दिया था।
इस प्रमुख प्रवेशद्वार के अतिरिक्त नगर के अन्य राजपथों, पथों और विभिन्न पथों तक को आकर्षक प्रवेश-द्वारों तथा तोरण-बन्दनवारों से सजाया गया था।
कई दिनों से नगर के कोष्ठों-प्रकोष्ठों और सामान्य गृहों में भी संध्या होते ही दीपमालिकाएं सजाई जा रही थीं। ये अनन्त दीपशिखाएं पृथ्वी पर आकाश के सम्पूर्ण तारक मंडल के ही अवतरित होने का भ्रम पैदा करती प्रतीत होती थीं।
शोभा-सजावट का यह अभियान नगर के उस भाग में विशेष रूप से सम्पन्न हो रहा था जहां सिख समुदाय की बहुलता थी। पर प्रत्येक नागरिक उल्लसित और उत्साहपूरित हो एक अभिनव स्वागत-समारोह के आयोजन में मग्न था।
इस सबका—इस विशेष आयोजन का, जन-मन में जग आये उल्लास-उत्साह का—कोई कारण था और वह सामान्य नहीं था। विशिष्ट था यह अवसर।
नगर में आज सिखों के नौवें गुरु गेबिन्द सिंह के पिता श्री गुरु तेगबहादुर सिंह पधारने वाले थे। नागरिकों का उत्साह अगर गुरु तेगबहादुर के आगमन के उस काल चरमोत्कर्ष पर था तो वह यों ही नहीं था। प्रथम गुरु नानक के बाद अगर किसी सिख गुरु ने इस नगर की ओर मुख करने की अनुकम्पा की थी तो ये नवम् गुरु तेगबहादुर ही थे। बीच के सात गुरुओं के समीप तो शिष्यों-अनुयायियों को ही इस सुदूर प्रदेश से चलकर पंजाब के गुरुतख्त तक जाना पड़ता था। और यह सबके के लिए सम्भव ही कहां और कैसे था ? सम्पन्न, ऐश्वर्यपूर्ण और युवा जन-यात्रा की बाधाओं की उपेक्षा कर वहां पहुंच गुरु-दर्शन की अपनी आकांक्षा तो पूर्ण कर लेते थे, पर विपन्न, वृद्ध, विकलांग और कोमल-गात नारियों, को तो इस सौभाग्य से वंचित ही रहना पड़ता था। पर आज सबकी मनोकामना पूर्ति का अवसर आ पहुँचा था। आज आराधक को आराध्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, आज स्वयं वही यहां पधार रहा था।
पर मात्र यही कारण नहीं था इस नवम गुरु के प्रति लोगों के भक्तिभाव के आकस्मिक रूप से उमड़ पड़ने का। इस गुरु, गुरु तेगबहादुर की और भी कुछ विषेशताएं जो उन्हें जन-जन की अप्रतिम श्रद्धा का पात्र बना रही थीं।
त्यागी था वह गुरु। वीतराग। गुरुगद्दी का यह वैधानिक उत्तराधिकारी, गद्दी को ही ठुकराने को उद्यत हो आया था। अष्टम गुरु की इहलीला की समाप्ति के पश्चात् जब उसके सिर पर स्वर्ण किरीट सजाने का अवसर आया तो उसने स्पष्ट कर दिया कि वह सुख-साधन, श्री-समृद्धि, मान-प्रतिष्ठा, पूजा-सेवा का आकांक्षी नहीं। संतोष में ही वह परम सुख मानता था। पर प्रेम-परवश कर देता है। भक्ति विवश। शिष्यों और अनुयायियों के आग्रह पर उन्हें अपना प्रण तोड़ने को बाध्य होना पड़ा था और उनकी अछोर श्रद्धा और अथाह प्रेम के वशीभूत हो उन्हें गुरुगद्दी पर आरूढ़ होने के लिए प्रस्तुत होना ही पड़ा था।
पर मात्र इतनी ही विशेषता होती इस नवम गुरु की तो वे लोकप्रियता की इस पराकाष्ठा पर नहीं भी पहुंचते। गुरु-पद धारण करने से पूर्व उन्होंने उसके प्रति जितनी अरुचि प्रदर्शित की थी, गद्दी आसीन होते ही वे पूरी तरह पंथ के ही होकर रह गए। सर्वप्रथम उन्होंने मुगलों के आये दिन के उत्पात से सुरक्षा हेतु ‘मेघवाली’ में एक अभेद्य गढ़ का निर्माण कराया जहां उनके शिष्य और अनुयायी सुरक्षा का जीवन जी सकें।
स्थान को सुरक्षित कर गुरु तेगबहादुर धर्म-प्रचारार्थ प्रस्थित हुए। गुरु ने, विशेषकर, देश के पूर्वी भाग पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम तक की दुरूह और कष्टसाध्य यात्राएं कर उन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित पंथ का प्राणपण से प्रचार प्रारम्भ किया। यायावरी उनकी वृत्ति बन गई। वे शायद भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा—‘चरैवेति, चरैवेति’—चलते रहो, चलते रहो—से पूर्ण परिचित थे, इसीलिए अष्टम गुरु तक आते-आते जो पंथ पंचनद प्रदेश में ही सीमित होने की स्थिति में आ गया था उसमें उन्होंने अपने परिव्राजक जीवन द्वारा नये प्राण ही फूंक दिए।
उन्हें ज्ञात था—सभी महापुरुष, सभी धर्म-संस्थापक और धर्माधिकारी, सभी ज्ञान-पिपासू चलते रहे हैं। चलना सत्ययुग है, खड़े रहना त्रेता, बैठ पड़ना द्वापर और सोये रहना कलि। राम चले अयोध्या से लेकर लंका तक। श्रीकृष्ण चले वृन्दावन, मथुरा से लेकर सागरकुल द्वारिका तक। बुद्ध चले कपिलवस्तु से लेकर बोधगया, वैशाली, सारनाथ, राजगृह और कुशीनगर तक। सभी चले, चाहे वे अद्वैतवादी शंकराचार्य रहे हों या द्वैतवादी रामानुजाचार्य अथवा विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टिमत के प्रचारक प्रभु वल्लभाचार्य। चलने को तो श्री वल्लभाचार्य के इष्ट-विग्रह श्रीनाथ जी भी चले और भक्तों के कंधे पर आसीन वे महीनों की यात्रा पूरी कर गोवर्द्धन के अपने प्रसिद्ध मंदिर से उतरकर राजस्थान के नाथद्वार तक आ पहुंचे जहां उन्हीं के नाम पर एक विशाल नगर भी बस आया—नाथद्वारा। औरंगज़ेब का यह काल था जिसमें भगवान को भी भागते रहना पड़ा था, भले ही वह भक्तों में भर आए भय के कारण ही हो वर्ना भय ही जिससे भय खाता हो उस भगवान को कब किससे भय होने लगा ?
मतलब गति ही प्रगति का मूल मंत्र है, इस तथ्य को सभी चिन्तकों-मनीषियों ने स्वीकार और अपने-अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग किया। गुरु तेगबहादुर भी इसके अपवाद कैसे होते ?
पर यहीं कहां समाप्त होती है उनके त्याग की गाथा ? यातना नहीं भोगी तो त्याग क्या, तपस्या क्या ? अपने इसी यात्रा-क्रम में ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात:’ की तरह अपने भ्रमण के प्रायः आरम्भिक चरण में ही घोर अमंगल का सामना करना पड़ा उन्हें। सदा सशंकित शाहंशाह, आलमगीर औरंगज़ेब उनके इस अभियान से आशंकित और भयग्रस्त हो आया था। उनके पूर्व के गुरुओं के प्रताप से वह पूर्ण परिचित था और उसे स्पष्ट लग रहा था कि सिख मुगलिया सल्तनत के एक सशक्त शत्रु के रूप में उभर रहे हैं।
वह इस बात से अधिक चिन्तित हुआ कि यह नवां गुरु अपनी गतिविधियों को पंजाब और उसके आसापास ही केन्द्रित कर उन्हें अधिक विस्तार देने को प्रस्तुत हो आया है। और उसने गुरु की इस योजना को क्रियान्वित नहीं होने देने का मन बना लिया। पर दूरदर्शी और कुशल कूटनीतिज्ञ था यह शाहजहां-पुत्र। पंजाब की सीमाओं के अंदर गुरु से छेड़छाड़ करने का अंज़ाम का अंदाज़ वह नहीं लगा सके ऐसा हो ही नहीं सकता था। जब वे पंजाब में स्थान-स्थान पर अपना आख्यान देकर और अपने अनुयायियों को आश्वस्त कर आगे बढ़े और दिल्ली के समीप एक ग्राम से गुजरने लगे तो छद्म वेश में उनके पीछे निरन्तर लगे औरंगज़ेब के सैनिकों ने उन्हैं कैद कर लिया।
उस कैद में उन्हें कठोर यातनाएं भोगनी पड़ीं। औरंगज़ेब उनके मनोबल को पूरी तरह तोड़कर उन्हें अपने धर्म-प्रचार-अभियान से विमुख कर देने पर कटिबद्ध था। पर मनस्वी थे सिख-गुरु। औरंगज़ेब के कुकर्मी कर्मचारियों का अत्याचार उन्हें अपने संकल्प से डिगाने में समर्थ नहीं हो सका। कारागार के सींखचों के अन्दर बन्द रहकर भी वे अकाल-पुरुष की आराधना में रत रहे। गुरुवाणी के पाठ-क्रम में कोई व्यवधान नहीं आने दिया और अन्ततः एक दिन उन्होंने अपने को कारागृह से बाहर पाया।
यह चमत्कार औरंगज़ेब के विश्वस्त सिपहसालार मिर्जा़ राजा जयसिंह के सुपुत्र रामसिंह के कारण घटा।
‘‘खता मुआफ़ हो जहां पनाह, यह समय सिखों से बैर लेने का नहीं है।’’ रामसिंह ने औरंगज़ेब से एकान्त में कहा था।
‘‘क्यों ? तुम तो काफिरों के हिमायती कभी नहीं रहे तब इस पाखंडी की वकालत तुम्हें कैसे सूझी ?’’ औरंगज़ेब ने अपनी कड़कड़ाती आवाज़ में पूछा।
‘‘गुरु तेगबहादुर काफिर नहीं हैं। गुरु नानक मूर्ति पूजा के आग्रही कभी नहीं रहे। उनके शिष्यों ने भी मूर्ति-पूजन पर जोर नहीं दिया पर मेरी इस फरियाद का कारण कुछ और है।’’ रामसिंह निर्भय बोले।
‘‘क्या ?’’ औरंगज़ेब ने आंखों में प्रश्न भरकर उनकी ओर देखा।
‘‘हम एक ही साथ सभी से शत्रुता मोल नहीं ले सकते। आपको पता ही है हिन्दू आपसे खार खाए बैठे हैं। विशेषकर आपके मंदिर-ध्वंस अभियान ने उन्हें आपसे अलग-थलग कर दिया है। बलात् धर्म-परिवर्तन ने भी उनमें साम्राज्य के प्रति आक्रोश ही भरा है। ऐसी स्थिति में सिखों को भी शत्रु बना लेना बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती।’’
अनेक उथल-पुथल, उत्थान-पतन, उत्सव-महोत्सव देखे हैं इस पुरातन नगर ने। अनेक महापुरुषों, धर्म-संस्थापकों-धर्माधिकारियों, विद्वानों, चिंतकों के चरण-रज से पवित्र हुए हैं यहां के राज-पथ, यहां कि लम्बी-पतली सौ-सौ बल खाती बंकिम वीथियां।
हां, कभी अनन्त ज्ञान-सम्पन्न भगवान बुद्ध ने भी धन्य किया था इस धरती को अपने चरण-चिह्नों से और अशोक महान् ने इसी नगरी को अपनी राजस्थली बनाकर तथागत के धर्मचक्र के नवीन गति एवं नूतन ऊर्जा भर सागर-पार तक पहुँचा दिया था उसे।
और तो और ‘ननकाना साहब’, उस समय की तलवंडी और अब पाकिस्तान के एक अंश में जन्मे सिखधर्म के महान प्रवर्तक गुरु नानक साहब ने भी अपने देश-विदेश-व्यापी यात्रा-क्रम में यहां आकर विशेष मान प्रदान किया था इस नगर और नगरवासियों को।
आज इस नगर की शोभा अनुपमेय थी। राजपथों पर भिश्तियों ने सुगन्धित जल का छिड़काव किया था। प्रवेशद्वार को कदली-स्तम्भों और अशोक वृक्ष के हरित पत्रों से सजाया गया था। उसके दोनों ओर चित्र-खचित, जल-पूरति मंगल-घटों की ऊर्ध्वाकार पंक्तियां भी रच दी गई थीं। महाद्वार के ठीक सामने दो गजराज रक्त-कमल-युक्त अपने विशाल सूँड़ों को स्वागत की मुद्रा में उठाए झूम रहे थे। स्वर्ण-तारों से निर्मित परिधानों से आच्छादित उनका सर्वांग अति सुन्दर लग रहा था। कुशल महावतों ने उनके प्रशस्त मस्तक को विभिन्न रंगों की चित्र-कारी द्वारा असामान्य रूप से मनोहारी बना दिया था।
इस प्रमुख प्रवेशद्वार के अतिरिक्त नगर के अन्य राजपथों, पथों और विभिन्न पथों तक को आकर्षक प्रवेश-द्वारों तथा तोरण-बन्दनवारों से सजाया गया था।
कई दिनों से नगर के कोष्ठों-प्रकोष्ठों और सामान्य गृहों में भी संध्या होते ही दीपमालिकाएं सजाई जा रही थीं। ये अनन्त दीपशिखाएं पृथ्वी पर आकाश के सम्पूर्ण तारक मंडल के ही अवतरित होने का भ्रम पैदा करती प्रतीत होती थीं।
शोभा-सजावट का यह अभियान नगर के उस भाग में विशेष रूप से सम्पन्न हो रहा था जहां सिख समुदाय की बहुलता थी। पर प्रत्येक नागरिक उल्लसित और उत्साहपूरित हो एक अभिनव स्वागत-समारोह के आयोजन में मग्न था।
इस सबका—इस विशेष आयोजन का, जन-मन में जग आये उल्लास-उत्साह का—कोई कारण था और वह सामान्य नहीं था। विशिष्ट था यह अवसर।
नगर में आज सिखों के नौवें गुरु गेबिन्द सिंह के पिता श्री गुरु तेगबहादुर सिंह पधारने वाले थे। नागरिकों का उत्साह अगर गुरु तेगबहादुर के आगमन के उस काल चरमोत्कर्ष पर था तो वह यों ही नहीं था। प्रथम गुरु नानक के बाद अगर किसी सिख गुरु ने इस नगर की ओर मुख करने की अनुकम्पा की थी तो ये नवम् गुरु तेगबहादुर ही थे। बीच के सात गुरुओं के समीप तो शिष्यों-अनुयायियों को ही इस सुदूर प्रदेश से चलकर पंजाब के गुरुतख्त तक जाना पड़ता था। और यह सबके के लिए सम्भव ही कहां और कैसे था ? सम्पन्न, ऐश्वर्यपूर्ण और युवा जन-यात्रा की बाधाओं की उपेक्षा कर वहां पहुंच गुरु-दर्शन की अपनी आकांक्षा तो पूर्ण कर लेते थे, पर विपन्न, वृद्ध, विकलांग और कोमल-गात नारियों, को तो इस सौभाग्य से वंचित ही रहना पड़ता था। पर आज सबकी मनोकामना पूर्ति का अवसर आ पहुँचा था। आज आराधक को आराध्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, आज स्वयं वही यहां पधार रहा था।
पर मात्र यही कारण नहीं था इस नवम गुरु के प्रति लोगों के भक्तिभाव के आकस्मिक रूप से उमड़ पड़ने का। इस गुरु, गुरु तेगबहादुर की और भी कुछ विषेशताएं जो उन्हें जन-जन की अप्रतिम श्रद्धा का पात्र बना रही थीं।
त्यागी था वह गुरु। वीतराग। गुरुगद्दी का यह वैधानिक उत्तराधिकारी, गद्दी को ही ठुकराने को उद्यत हो आया था। अष्टम गुरु की इहलीला की समाप्ति के पश्चात् जब उसके सिर पर स्वर्ण किरीट सजाने का अवसर आया तो उसने स्पष्ट कर दिया कि वह सुख-साधन, श्री-समृद्धि, मान-प्रतिष्ठा, पूजा-सेवा का आकांक्षी नहीं। संतोष में ही वह परम सुख मानता था। पर प्रेम-परवश कर देता है। भक्ति विवश। शिष्यों और अनुयायियों के आग्रह पर उन्हें अपना प्रण तोड़ने को बाध्य होना पड़ा था और उनकी अछोर श्रद्धा और अथाह प्रेम के वशीभूत हो उन्हें गुरुगद्दी पर आरूढ़ होने के लिए प्रस्तुत होना ही पड़ा था।
पर मात्र इतनी ही विशेषता होती इस नवम गुरु की तो वे लोकप्रियता की इस पराकाष्ठा पर नहीं भी पहुंचते। गुरु-पद धारण करने से पूर्व उन्होंने उसके प्रति जितनी अरुचि प्रदर्शित की थी, गद्दी आसीन होते ही वे पूरी तरह पंथ के ही होकर रह गए। सर्वप्रथम उन्होंने मुगलों के आये दिन के उत्पात से सुरक्षा हेतु ‘मेघवाली’ में एक अभेद्य गढ़ का निर्माण कराया जहां उनके शिष्य और अनुयायी सुरक्षा का जीवन जी सकें।
स्थान को सुरक्षित कर गुरु तेगबहादुर धर्म-प्रचारार्थ प्रस्थित हुए। गुरु ने, विशेषकर, देश के पूर्वी भाग पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम तक की दुरूह और कष्टसाध्य यात्राएं कर उन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रतिपादित पंथ का प्राणपण से प्रचार प्रारम्भ किया। यायावरी उनकी वृत्ति बन गई। वे शायद भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा—‘चरैवेति, चरैवेति’—चलते रहो, चलते रहो—से पूर्ण परिचित थे, इसीलिए अष्टम गुरु तक आते-आते जो पंथ पंचनद प्रदेश में ही सीमित होने की स्थिति में आ गया था उसमें उन्होंने अपने परिव्राजक जीवन द्वारा नये प्राण ही फूंक दिए।
उन्हें ज्ञात था—सभी महापुरुष, सभी धर्म-संस्थापक और धर्माधिकारी, सभी ज्ञान-पिपासू चलते रहे हैं। चलना सत्ययुग है, खड़े रहना त्रेता, बैठ पड़ना द्वापर और सोये रहना कलि। राम चले अयोध्या से लेकर लंका तक। श्रीकृष्ण चले वृन्दावन, मथुरा से लेकर सागरकुल द्वारिका तक। बुद्ध चले कपिलवस्तु से लेकर बोधगया, वैशाली, सारनाथ, राजगृह और कुशीनगर तक। सभी चले, चाहे वे अद्वैतवादी शंकराचार्य रहे हों या द्वैतवादी रामानुजाचार्य अथवा विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टिमत के प्रचारक प्रभु वल्लभाचार्य। चलने को तो श्री वल्लभाचार्य के इष्ट-विग्रह श्रीनाथ जी भी चले और भक्तों के कंधे पर आसीन वे महीनों की यात्रा पूरी कर गोवर्द्धन के अपने प्रसिद्ध मंदिर से उतरकर राजस्थान के नाथद्वार तक आ पहुंचे जहां उन्हीं के नाम पर एक विशाल नगर भी बस आया—नाथद्वारा। औरंगज़ेब का यह काल था जिसमें भगवान को भी भागते रहना पड़ा था, भले ही वह भक्तों में भर आए भय के कारण ही हो वर्ना भय ही जिससे भय खाता हो उस भगवान को कब किससे भय होने लगा ?
मतलब गति ही प्रगति का मूल मंत्र है, इस तथ्य को सभी चिन्तकों-मनीषियों ने स्वीकार और अपने-अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका प्रयोग किया। गुरु तेगबहादुर भी इसके अपवाद कैसे होते ?
पर यहीं कहां समाप्त होती है उनके त्याग की गाथा ? यातना नहीं भोगी तो त्याग क्या, तपस्या क्या ? अपने इसी यात्रा-क्रम में ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात:’ की तरह अपने भ्रमण के प्रायः आरम्भिक चरण में ही घोर अमंगल का सामना करना पड़ा उन्हें। सदा सशंकित शाहंशाह, आलमगीर औरंगज़ेब उनके इस अभियान से आशंकित और भयग्रस्त हो आया था। उनके पूर्व के गुरुओं के प्रताप से वह पूर्ण परिचित था और उसे स्पष्ट लग रहा था कि सिख मुगलिया सल्तनत के एक सशक्त शत्रु के रूप में उभर रहे हैं।
वह इस बात से अधिक चिन्तित हुआ कि यह नवां गुरु अपनी गतिविधियों को पंजाब और उसके आसापास ही केन्द्रित कर उन्हें अधिक विस्तार देने को प्रस्तुत हो आया है। और उसने गुरु की इस योजना को क्रियान्वित नहीं होने देने का मन बना लिया। पर दूरदर्शी और कुशल कूटनीतिज्ञ था यह शाहजहां-पुत्र। पंजाब की सीमाओं के अंदर गुरु से छेड़छाड़ करने का अंज़ाम का अंदाज़ वह नहीं लगा सके ऐसा हो ही नहीं सकता था। जब वे पंजाब में स्थान-स्थान पर अपना आख्यान देकर और अपने अनुयायियों को आश्वस्त कर आगे बढ़े और दिल्ली के समीप एक ग्राम से गुजरने लगे तो छद्म वेश में उनके पीछे निरन्तर लगे औरंगज़ेब के सैनिकों ने उन्हैं कैद कर लिया।
उस कैद में उन्हें कठोर यातनाएं भोगनी पड़ीं। औरंगज़ेब उनके मनोबल को पूरी तरह तोड़कर उन्हें अपने धर्म-प्रचार-अभियान से विमुख कर देने पर कटिबद्ध था। पर मनस्वी थे सिख-गुरु। औरंगज़ेब के कुकर्मी कर्मचारियों का अत्याचार उन्हें अपने संकल्प से डिगाने में समर्थ नहीं हो सका। कारागार के सींखचों के अन्दर बन्द रहकर भी वे अकाल-पुरुष की आराधना में रत रहे। गुरुवाणी के पाठ-क्रम में कोई व्यवधान नहीं आने दिया और अन्ततः एक दिन उन्होंने अपने को कारागृह से बाहर पाया।
यह चमत्कार औरंगज़ेब के विश्वस्त सिपहसालार मिर्जा़ राजा जयसिंह के सुपुत्र रामसिंह के कारण घटा।
‘‘खता मुआफ़ हो जहां पनाह, यह समय सिखों से बैर लेने का नहीं है।’’ रामसिंह ने औरंगज़ेब से एकान्त में कहा था।
‘‘क्यों ? तुम तो काफिरों के हिमायती कभी नहीं रहे तब इस पाखंडी की वकालत तुम्हें कैसे सूझी ?’’ औरंगज़ेब ने अपनी कड़कड़ाती आवाज़ में पूछा।
‘‘गुरु तेगबहादुर काफिर नहीं हैं। गुरु नानक मूर्ति पूजा के आग्रही कभी नहीं रहे। उनके शिष्यों ने भी मूर्ति-पूजन पर जोर नहीं दिया पर मेरी इस फरियाद का कारण कुछ और है।’’ रामसिंह निर्भय बोले।
‘‘क्या ?’’ औरंगज़ेब ने आंखों में प्रश्न भरकर उनकी ओर देखा।
‘‘हम एक ही साथ सभी से शत्रुता मोल नहीं ले सकते। आपको पता ही है हिन्दू आपसे खार खाए बैठे हैं। विशेषकर आपके मंदिर-ध्वंस अभियान ने उन्हें आपसे अलग-थलग कर दिया है। बलात् धर्म-परिवर्तन ने भी उनमें साम्राज्य के प्रति आक्रोश ही भरा है। ऐसी स्थिति में सिखों को भी शत्रु बना लेना बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती।’’
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i