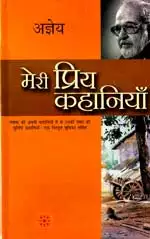|
विशेष >> मेरी प्रिय कहानियाँ अज्ञेय मेरी प्रिय कहानियाँ अज्ञेयसच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय
|
182 पाठक हैं |
||||||||
प्रस्तुत संकलन की कहानियाँ...मेरी तो वे हैं ही, (‘कहानियाँ’ भी मैं उन्हें मानता हूँ) और ‘प्रिय’ भी वे हुई हैं या होंगी, पर प्रिय मेरी नहीं मेरे पाठक समाज की
Meri priya kahaniyan
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
प्रख्यात साहित्यकार ‘अज्ञेय’ ने यद्यपि कहानियां कम ही लिखीं और एक समय के बाद कहानी लिखना बिलकुल बंद कर दिया-परन्तु हिन्दी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। इस संग्रह में इस प्रकार की सभी कहानियां, कहानी-लेखन संबंधी उनके महत्वपूर्ण विचारों के साथ प्रस्तुत हैं।
‘मेरी प्रिय कहानियाँ’ की बात सोचते समय मैंने यह बात सामने रखने की बिलकुल कोशिश नहीं कि मेरी कौन-सी कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, यही दृष्टि रखी की मेरी कहानियों में कौन-सी दूसरों को....अच्छी लगीं या अच्छी लग सकती हैं...प्रस्तुत संकलन की कहानियाँ...मेरी तो वे हैं ही, (‘कहानियाँ’ भी मैं उन्हें मानता हूँ) और ‘प्रिय’ भी वे हुई हैं या होंगी, पर प्रिय मेरी नहीं मेरे पाठक समाज की....यह बात जितनी मेरी विगत की जानकारी पर आधारित है, उतनी ही मेरी भविष्यत् की आशा पर। ये कहानियाँ पाठकों को प्रिय रही हैं, और मुझे आशा है कि आज भी वे पाठकों को प्रिय लगेंगी।
‘मेरी प्रिय कहानियाँ’ की बात सोचते समय मैंने यह बात सामने रखने की बिलकुल कोशिश नहीं कि मेरी कौन-सी कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, यही दृष्टि रखी की मेरी कहानियों में कौन-सी दूसरों को....अच्छी लगीं या अच्छी लग सकती हैं...प्रस्तुत संकलन की कहानियाँ...मेरी तो वे हैं ही, (‘कहानियाँ’ भी मैं उन्हें मानता हूँ) और ‘प्रिय’ भी वे हुई हैं या होंगी, पर प्रिय मेरी नहीं मेरे पाठक समाज की....यह बात जितनी मेरी विगत की जानकारी पर आधारित है, उतनी ही मेरी भविष्यत् की आशा पर। ये कहानियाँ पाठकों को प्रिय रही हैं, और मुझे आशा है कि आज भी वे पाठकों को प्रिय लगेंगी।
प्रतिवेदन
(कुछ मेरी कहानी के बारे में, कुछ कहानी मात्र के)
अपनी कहानियों के बारे में इस दृष्टि से सोचा नहीं कि उनमें मेरी प्रिय कहानियाँ कौन-सी हैं। एक तो (अपनी पुरानी कहानियाँ पढ़ने और उनसे अपने लगाव की पड़ताल का कभी भी संयोग हो ही जाने पर !) पाता हूँ कि कभी एक प्रिय लगती है तो कभी दूसरी-उस समय की मनोदशा की बात है-और कभी यह भी हो सकता है कि सभी के प्रति एक विराग का भाव उदित हो। दूसरे, मैं बुनियादी तौर पर इसे अप्रासंगिक मानता हूँ कि स्वयं लेखक को अपनी कौन-सी रचना प्रिय लगती है। लेखक का ‘मेरा’ ही नहीं, ‘मैं’ भी वहाँ अप्रासंगिक होता है और होना चाहिए, जहाँ रचना के ग्रहण-आस्वादन की बात है।
एक तीसरा भी कारण है। वह और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। ‘प्रिय’ गहरे में कहीं ‘सफल’ के साथ बँधा हुआ भी होता है : लेखक को वह कहानी अधिक ‘प्रिय’ होगी जो उसकी राय में अधिक ‘सफल’ है। अब यह सफलता क्या होती हैं-यानी लेखक की राय में सफलता ?
मैंने हमेशा यह संप्रेषण की कला को बुनियादी महत्त्व दिया है और सम्प्रेषणीयता का अन्तिम निर्णायक लेखक नहीं हो सकता, पाठक अथवा सामाजिक ही हो सकता है। लेखक अपनी सफलता इसमें तो देख सकता है कि ‘जो मैं पकड़ना चाहता था वह मैं पकड़ पाया या नहीं’ पर स्पष्ट है कि कहानी की सफलता यहाँ इस अर्थ में लेखक की सफलता से अलग है कि कहानी की सफलता की कसौटी के लिए हम यह पूछना चाहेंगे कि जो कुछ भी लेखक ने पाना चाहा या पाया, उसे दूसरे तक-सामाजिक तक-पहुँचाने में वह वहाँ तक सफल हुआ ? (और यह तो है ही कि पहुँचाया जाकर वह सामाजिक को कितना मूल्यवान् लगा !)
इसीलिए ‘मेरी प्रिय कहानियाँ’ की बात सोचते समय मैंने यह बात सामने रखने की बिलकुल कोशिश नहीं कि मेरी कौन-सी कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं; यह दृष्टि रखी कि मेरी कहानियों में कौन-सी दूसरों को-मेरी समझ में ‘अच्छे पाठकों को-अच्छी लगीं (जहाँ तक मुझे जानकारी मिली) या अच्छी लग सकती हैं (जहाँ तक मैं अपने सामाजिक को पहचान सकता हूँ)।
प्रस्तुत संकलन की कहानियाँ इसी दृष्टि में चुनी गई हैं। ‘मेरी’ तो वे हुई हैं या होंगी, पर प्रिय मेरी नहीं, मेरे पाठक-समाज की।
पिछले पन्द्रह-बीस वर्षों में मैंने कोई कहानी नहीं लिखी है। कह सकता हूँ कि कहानी लिखना मैंने छोड़ दिया है-या कि मुझसे छूट गया है। इस दूरी से अपनी कहानियों और उन कहानियों के लेखक के प्रति एक अपेक्षया निर्वैयक्तिक भाव भी मेरे मन में है। उसके बूते पर ऐसा भी दावा कर सकता हूँ कि उनका सही आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर सकता हूँ-पर वह न मुझे अभीष्ट है, न पाठक को उससे इस समय उससे सरोकार होगा। हाँ, यह कदाचित् वह जानना चाहे कि (खासकर अगर ये कहानियाँ पाठकों को ‘प्रिय’ हैं) मैंने कहनी लिखना क्यों छोड़ दिया ? यह भी संभव हैं कि इस प्रश्न का उत्तर उसे इन कहानियों का आस्वादन (और अन्तत: मूल्यांकन) करने में सहायक भी हो।
संक्षेप में, मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए रचना-कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से जुड़ा रहा है, और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है क्योंकि कहानी को मैंने उसके लिए नाकाफ़ी पाया: पर मैं जानता हूँ कि इतने संक्षेपन से बात नहीं भी समझी जा सकती है और यह गलत भी समझी जा सकती है, इसलिए थोड़ा और विस्तार से इस प्रश्न की चर्चा करूँगा। वह मेरी कहानियों को ही नहीं, कहानी-मात्र को और आज की कहानी-संबंधी चर्चा को एक परिप्रेक्ष्य दे सकेगी जो मेरी समझ में सही परिप्रेक्ष्य होगा और ‘यथार्थ’ का यथार्थ अर्थ करने में भी सहायक होगा।
बिना कहानी की सम्यक् परिभाषा के कहा जा सकता है कि कहानी एक क्षण का चित्र प्रस्तुत करती है। क्षण का अर्थ आप चाहे एक छोटा काल-खंड लगा लें, चाहे एक अल्पकालिक स्थिति, एक घटना, प्रभावी डायलॉग, एक मनोदशा, एक दृष्टि, एक (बाह्य या आभ्यन्तर) झाँकी, संत्रास, तनाव, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया...इसी प्रकार का चित्र अर्थ आप वर्णन, निरूपण, संकेतन, सम्पुंजन, रेखांकन अभिव्यंजन, रंजन प्रतीकन, द्योतन, आलोकन, जो चाहें लगा लें- या इनके जो भी जोड़-मेल। बल्कि और भी महीन-मुंशी तबीयत के हों तो ‘प्रस्तुत करना’ को लेकर भी काफ़ी छान-बीन कर सकते हैं। इस सबके लिए न अटक कर कहूँ कि कहानी क्षण का चित्र है और क्षण क्या है, इसी की हमारी पहचान निरन्तर गड़बड़ा रही है या संदिग्ध होती जा रही है। शेक्सपियर के चरित्र को ही लगा था कि काल की चूल उखड़ी हुई है-‘द टाइम इज आउट आफ़ जायंट’-और शेक्सपियर की क्षति तो अपेक्षया स्थिर, मूल्यों के मामले में आश्वस्त और भविष्य के प्रति आशा-भरी थी ! आज तो सचमुच टाइम ‘आउट आफ़ जॉयंट’ है: न केवल सभी कुछ संदिग्ध है, बल्कि हमारा यह भरोसा भी दिन-ब-दिन घटता जा रहा है कि कुछ भी हम असन्दिग्ध रूप से जान सकेंगे-और अनेक कारणों के अलावा एक इस कारण से भी जानकारी हासिल करने (या जानकारी को विकृत करके जबरन वह विकृति ही स्वीकार करने !) के साधन लगातार उन लोगों के दृढ़तर नियंत्रण में चले जा रहे हैं जिन पर हमारा नियंत्रण लगातार कमज़ोर होता जा रहा है।
अगर काल की चूल उखड़ी हुई है तो यथार्थ का क्या होता है ? ‘यथार्थ की पकड़’ की जो चर्चा है, उस पकड़ या पहचान के बारे में जो दावे हैं, उनका क्या होता है ? स्वयं कहानी का क्या होता है जो इस पहले से ही चूल-उखड़े काल के भी केवल एक विखंडित अंश का चित्र है ? (और चित्र फिर काल-में एक रचना है-यानी काल उसका एक आयाम है।)
अवश्य ही कहानी भी ‘आउट आफ़ जॉयंट’ होगी। आज है भी : और इसमें एक तर्क-संगीत भी है। कुछ लोग इसे स्पष्टतया, और बहुत-से लोग परिमाणत:, स्वीकार करते भी जान पड़ते हैं। लेकिन मेरे लिए जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर नहीं मिलता : उन उत्तरों की खोज भी मुझे कहानी संबंधी चर्चा में नजर नहीं आती।
यथार्थ की पकड़ की इस शब्द-बहुल चर्चा में, लोग दो चीज़ें मानकर चलते जान पड़ते हैं जो दोनों ही प्रश्नाधीन हैं-पहली यह कि ‘यथार्थ’ सब ‘बाहर’ होता है, सतह पर होता है, दूसरी यह कि इकहरा या एकस्तरीय होता है। जो दीखता नहीं है, या थोड़ा और आगे बढ़कर कह लें, कि जो गोचर नहीं है, वह यथार्थ नहीं है, यह एक नये प्रकार का अन्धापन है जिसे यथार्थ-बोध का नाम दिया जा रहा है। और अगर यथार्थ के वास्तव में अनेक स्तर होते हैं, तो केवल एक बाहरी खोल को देखने तक सीमित रहने में कौन-सी बहादुरी या विशिष्ट प्रतिभा है ?
मैं मानता ही नहीं, जानता हूँ कि यथार्थ इकहरा या सपाट या एकस्तरीय नहीं होता। मैं इससे आगे जाकर यह भी कह सकता हूँ कि कला के क्षेत्र में एक विशेष आशय में ‘यथार्थ’ अर्थहीन होता है, हमेशा अर्थहीन होता है-क्योंकि जिसे हम वस्तु यथार्थ या विषय-निरपेक्ष यथार्थ या आब्जेक्टिव रिएलिटी कहते या कह सकते हैं, उसमें फिर अर्थवत्ता का प्रश्न ही कहाँ रहता है जब कि अर्थ अनिवार्यत: अर्थ की पहचान करने वाले के, विषयी के, साथ बँधा है ? केवल सब्जेक्टिव यथार्थ में ही अर्थवत्ता का प्रश्न उठ सकता है, विषयीगत यथार्थ ही कला का यथार्थ होता है और उसी में अर्थ हो सकता है और इसलिए अर्थ की खोज हो सकती है।
मैंने जब कहा कि मेरे लिए रचना-कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से जुड़ा रहा है, और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है, तब मेरा यही अभिप्राय था। साहित्यकार के नाते मुझे अर्थहीन यथार्थ की तलाश नहीं है। आब्जेक्टिव संसार में ऐसे यथार्थ है जिनमें अर्थवत्ता की खोज बेमानी है, यह मैं जानता हूँ, उस अर्थातीत संसार से आगे बढ़कर ही मैं एक अर्थवान् जगत की खोज में जाता हूँ और उस जगत के निर्माण में स्वयं मेरा भी योग है। कोई चाहे तो यह कह सकता है कि जो सब्जेक्टिव है वह तो आत्यन्तिक रूप में अर्थहीन है; और यह कहकर बाहर और भीतर दोनों क्षेत्रों में एक अर्थहीन, एब्सर्ड संसार के निर्माण में प्रवृत्त हो सकता है। मैं वैसा नहीं मानता; वैसे निर्माण में मेरी रूचि नहीं है; मानव की मेरी परिकल्पना में वह अनिवार्यत: अर्थवत्ता का खोजी और स्रष्टा है और यही उसके मानवत्व की पहचान है। अगर वह एब्सर्ड को प्रस्तुत करता भी है तो वह भी अर्थवत्ता की खोज की ही यन्त्रणा दिखाने के लिए-अर्थवत्ता की खोज जिजीविषा का एक पहलू है और अर्थ या अर्थ की चाह को अन्तिम रूप से खो देना जीवन की चाह ही खो देना है। मैं जीवन से चिपटा नहीं हूँ पर जीना चाहता हूँ और अन्त तक जीना चाहते रहना चाहता हूँ।
अपनी कहानियों के बारे में इस दृष्टि से सोचा नहीं कि उनमें मेरी प्रिय कहानियाँ कौन-सी हैं। एक तो (अपनी पुरानी कहानियाँ पढ़ने और उनसे अपने लगाव की पड़ताल का कभी भी संयोग हो ही जाने पर !) पाता हूँ कि कभी एक प्रिय लगती है तो कभी दूसरी-उस समय की मनोदशा की बात है-और कभी यह भी हो सकता है कि सभी के प्रति एक विराग का भाव उदित हो। दूसरे, मैं बुनियादी तौर पर इसे अप्रासंगिक मानता हूँ कि स्वयं लेखक को अपनी कौन-सी रचना प्रिय लगती है। लेखक का ‘मेरा’ ही नहीं, ‘मैं’ भी वहाँ अप्रासंगिक होता है और होना चाहिए, जहाँ रचना के ग्रहण-आस्वादन की बात है।
एक तीसरा भी कारण है। वह और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। ‘प्रिय’ गहरे में कहीं ‘सफल’ के साथ बँधा हुआ भी होता है : लेखक को वह कहानी अधिक ‘प्रिय’ होगी जो उसकी राय में अधिक ‘सफल’ है। अब यह सफलता क्या होती हैं-यानी लेखक की राय में सफलता ?
मैंने हमेशा यह संप्रेषण की कला को बुनियादी महत्त्व दिया है और सम्प्रेषणीयता का अन्तिम निर्णायक लेखक नहीं हो सकता, पाठक अथवा सामाजिक ही हो सकता है। लेखक अपनी सफलता इसमें तो देख सकता है कि ‘जो मैं पकड़ना चाहता था वह मैं पकड़ पाया या नहीं’ पर स्पष्ट है कि कहानी की सफलता यहाँ इस अर्थ में लेखक की सफलता से अलग है कि कहानी की सफलता की कसौटी के लिए हम यह पूछना चाहेंगे कि जो कुछ भी लेखक ने पाना चाहा या पाया, उसे दूसरे तक-सामाजिक तक-पहुँचाने में वह वहाँ तक सफल हुआ ? (और यह तो है ही कि पहुँचाया जाकर वह सामाजिक को कितना मूल्यवान् लगा !)
इसीलिए ‘मेरी प्रिय कहानियाँ’ की बात सोचते समय मैंने यह बात सामने रखने की बिलकुल कोशिश नहीं कि मेरी कौन-सी कहानियाँ मुझे अच्छी लगती हैं; यह दृष्टि रखी कि मेरी कहानियों में कौन-सी दूसरों को-मेरी समझ में ‘अच्छे पाठकों को-अच्छी लगीं (जहाँ तक मुझे जानकारी मिली) या अच्छी लग सकती हैं (जहाँ तक मैं अपने सामाजिक को पहचान सकता हूँ)।
प्रस्तुत संकलन की कहानियाँ इसी दृष्टि में चुनी गई हैं। ‘मेरी’ तो वे हुई हैं या होंगी, पर प्रिय मेरी नहीं, मेरे पाठक-समाज की।
पिछले पन्द्रह-बीस वर्षों में मैंने कोई कहानी नहीं लिखी है। कह सकता हूँ कि कहानी लिखना मैंने छोड़ दिया है-या कि मुझसे छूट गया है। इस दूरी से अपनी कहानियों और उन कहानियों के लेखक के प्रति एक अपेक्षया निर्वैयक्तिक भाव भी मेरे मन में है। उसके बूते पर ऐसा भी दावा कर सकता हूँ कि उनका सही आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कर सकता हूँ-पर वह न मुझे अभीष्ट है, न पाठक को उससे इस समय उससे सरोकार होगा। हाँ, यह कदाचित् वह जानना चाहे कि (खासकर अगर ये कहानियाँ पाठकों को ‘प्रिय’ हैं) मैंने कहनी लिखना क्यों छोड़ दिया ? यह भी संभव हैं कि इस प्रश्न का उत्तर उसे इन कहानियों का आस्वादन (और अन्तत: मूल्यांकन) करने में सहायक भी हो।
संक्षेप में, मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए रचना-कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से जुड़ा रहा है, और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है क्योंकि कहानी को मैंने उसके लिए नाकाफ़ी पाया: पर मैं जानता हूँ कि इतने संक्षेपन से बात नहीं भी समझी जा सकती है और यह गलत भी समझी जा सकती है, इसलिए थोड़ा और विस्तार से इस प्रश्न की चर्चा करूँगा। वह मेरी कहानियों को ही नहीं, कहानी-मात्र को और आज की कहानी-संबंधी चर्चा को एक परिप्रेक्ष्य दे सकेगी जो मेरी समझ में सही परिप्रेक्ष्य होगा और ‘यथार्थ’ का यथार्थ अर्थ करने में भी सहायक होगा।
बिना कहानी की सम्यक् परिभाषा के कहा जा सकता है कि कहानी एक क्षण का चित्र प्रस्तुत करती है। क्षण का अर्थ आप चाहे एक छोटा काल-खंड लगा लें, चाहे एक अल्पकालिक स्थिति, एक घटना, प्रभावी डायलॉग, एक मनोदशा, एक दृष्टि, एक (बाह्य या आभ्यन्तर) झाँकी, संत्रास, तनाव, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया...इसी प्रकार का चित्र अर्थ आप वर्णन, निरूपण, संकेतन, सम्पुंजन, रेखांकन अभिव्यंजन, रंजन प्रतीकन, द्योतन, आलोकन, जो चाहें लगा लें- या इनके जो भी जोड़-मेल। बल्कि और भी महीन-मुंशी तबीयत के हों तो ‘प्रस्तुत करना’ को लेकर भी काफ़ी छान-बीन कर सकते हैं। इस सबके लिए न अटक कर कहूँ कि कहानी क्षण का चित्र है और क्षण क्या है, इसी की हमारी पहचान निरन्तर गड़बड़ा रही है या संदिग्ध होती जा रही है। शेक्सपियर के चरित्र को ही लगा था कि काल की चूल उखड़ी हुई है-‘द टाइम इज आउट आफ़ जायंट’-और शेक्सपियर की क्षति तो अपेक्षया स्थिर, मूल्यों के मामले में आश्वस्त और भविष्य के प्रति आशा-भरी थी ! आज तो सचमुच टाइम ‘आउट आफ़ जॉयंट’ है: न केवल सभी कुछ संदिग्ध है, बल्कि हमारा यह भरोसा भी दिन-ब-दिन घटता जा रहा है कि कुछ भी हम असन्दिग्ध रूप से जान सकेंगे-और अनेक कारणों के अलावा एक इस कारण से भी जानकारी हासिल करने (या जानकारी को विकृत करके जबरन वह विकृति ही स्वीकार करने !) के साधन लगातार उन लोगों के दृढ़तर नियंत्रण में चले जा रहे हैं जिन पर हमारा नियंत्रण लगातार कमज़ोर होता जा रहा है।
अगर काल की चूल उखड़ी हुई है तो यथार्थ का क्या होता है ? ‘यथार्थ की पकड़’ की जो चर्चा है, उस पकड़ या पहचान के बारे में जो दावे हैं, उनका क्या होता है ? स्वयं कहानी का क्या होता है जो इस पहले से ही चूल-उखड़े काल के भी केवल एक विखंडित अंश का चित्र है ? (और चित्र फिर काल-में एक रचना है-यानी काल उसका एक आयाम है।)
अवश्य ही कहानी भी ‘आउट आफ़ जॉयंट’ होगी। आज है भी : और इसमें एक तर्क-संगीत भी है। कुछ लोग इसे स्पष्टतया, और बहुत-से लोग परिमाणत:, स्वीकार करते भी जान पड़ते हैं। लेकिन मेरे लिए जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर नहीं मिलता : उन उत्तरों की खोज भी मुझे कहानी संबंधी चर्चा में नजर नहीं आती।
यथार्थ की पकड़ की इस शब्द-बहुल चर्चा में, लोग दो चीज़ें मानकर चलते जान पड़ते हैं जो दोनों ही प्रश्नाधीन हैं-पहली यह कि ‘यथार्थ’ सब ‘बाहर’ होता है, सतह पर होता है, दूसरी यह कि इकहरा या एकस्तरीय होता है। जो दीखता नहीं है, या थोड़ा और आगे बढ़कर कह लें, कि जो गोचर नहीं है, वह यथार्थ नहीं है, यह एक नये प्रकार का अन्धापन है जिसे यथार्थ-बोध का नाम दिया जा रहा है। और अगर यथार्थ के वास्तव में अनेक स्तर होते हैं, तो केवल एक बाहरी खोल को देखने तक सीमित रहने में कौन-सी बहादुरी या विशिष्ट प्रतिभा है ?
मैं मानता ही नहीं, जानता हूँ कि यथार्थ इकहरा या सपाट या एकस्तरीय नहीं होता। मैं इससे आगे जाकर यह भी कह सकता हूँ कि कला के क्षेत्र में एक विशेष आशय में ‘यथार्थ’ अर्थहीन होता है, हमेशा अर्थहीन होता है-क्योंकि जिसे हम वस्तु यथार्थ या विषय-निरपेक्ष यथार्थ या आब्जेक्टिव रिएलिटी कहते या कह सकते हैं, उसमें फिर अर्थवत्ता का प्रश्न ही कहाँ रहता है जब कि अर्थ अनिवार्यत: अर्थ की पहचान करने वाले के, विषयी के, साथ बँधा है ? केवल सब्जेक्टिव यथार्थ में ही अर्थवत्ता का प्रश्न उठ सकता है, विषयीगत यथार्थ ही कला का यथार्थ होता है और उसी में अर्थ हो सकता है और इसलिए अर्थ की खोज हो सकती है।
मैंने जब कहा कि मेरे लिए रचना-कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से जुड़ा रहा है, और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है, तब मेरा यही अभिप्राय था। साहित्यकार के नाते मुझे अर्थहीन यथार्थ की तलाश नहीं है। आब्जेक्टिव संसार में ऐसे यथार्थ है जिनमें अर्थवत्ता की खोज बेमानी है, यह मैं जानता हूँ, उस अर्थातीत संसार से आगे बढ़कर ही मैं एक अर्थवान् जगत की खोज में जाता हूँ और उस जगत के निर्माण में स्वयं मेरा भी योग है। कोई चाहे तो यह कह सकता है कि जो सब्जेक्टिव है वह तो आत्यन्तिक रूप में अर्थहीन है; और यह कहकर बाहर और भीतर दोनों क्षेत्रों में एक अर्थहीन, एब्सर्ड संसार के निर्माण में प्रवृत्त हो सकता है। मैं वैसा नहीं मानता; वैसे निर्माण में मेरी रूचि नहीं है; मानव की मेरी परिकल्पना में वह अनिवार्यत: अर्थवत्ता का खोजी और स्रष्टा है और यही उसके मानवत्व की पहचान है। अगर वह एब्सर्ड को प्रस्तुत करता भी है तो वह भी अर्थवत्ता की खोज की ही यन्त्रणा दिखाने के लिए-अर्थवत्ता की खोज जिजीविषा का एक पहलू है और अर्थ या अर्थ की चाह को अन्तिम रूप से खो देना जीवन की चाह ही खो देना है। मैं जीवन से चिपटा नहीं हूँ पर जीना चाहता हूँ और अन्त तक जीना चाहते रहना चाहता हूँ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i