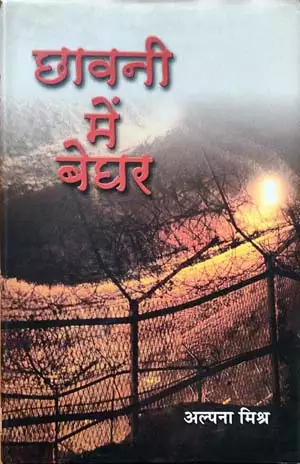|
कहानी संग्रह >> छावनी में बेघर छावनी में बेघरअल्पना मिश्र
|
163 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है पुस्तक छावनी में बेघर .......
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘छावनी में बेघर’ अल्पना मिश्र का उनके
पहले चर्चित
कथा-संकलन ‘भीतर का वक़्त’ के उपरान्त प्रशिक्षित
दूसरा संकलन
है, जो कथा-साहित्य में उनकी उपस्थिति को निस्सन्देह एक युवा रचनाकार के
तौर पर प्रतिष्ठित करता है। गहन भीतरी संवेदना की आँच में सीझी हुई उनकी
ये कहानियाँ, अपने सरोकारों में सघन व्यापकता समेटे हैं, जो राजनीतिक,
आर्थिक, नैतिक-अनैतिक मूल्यों को उनके बहुपक्षीय बिन्दुओं की विरूपताओं और
विडम्बनाओं से उपजी द्वन्द्वात्मकता के तनाव में, जिस दक्षता से महीन
बुनावट में सिरजती हैं- चकित करती हैं।
अतिरिक्त शिल्प सर्तकता से अक्रान्त इधर किसी हद तक दुरूह हुई रचनाशीलता के बरक्स, अल्पना की रचनाएँ भाषा, शिल्प और कहन के आनुपातिक शरबती रसायन-सी पाठकों के लिए अबूझ नहीं होतीं। वे सीधे संवाद करती हैं- उन्हीं स्थितियों-परिस्थितियों के सजीव परिवेश के गली-गलियारों में ले जाकर, उन्हीं की काया में प्रवेश कर, उन्हीं की विसंगतियों की त्रासदी में साँसे भरते हुए। चाहे इस संग्रह की, प्रश्नों के कटघरे में लेती ‘बेदखल’ हो या ‘मिड डे मील’ या ‘मुक्ति प्रसंग’ या हिन्दी कहानी की उपलब्धि ‘छावनी में बेघर’ !
‘छावनी में बेघर’ अल्पना की रचनाशीलता के प्रति आश्वस्ति की बुलन्द इमारत की पुख्ता उठान ही नहीं निर्मित करता है, पाठकों के मन में अपेक्षा और उम्मीद की चौतरफा खिड़कियों की भी आशा बोता है- जो अपने समय की हवा की उन्मुक्त आवाजाही की साक्ष्य भर ही नहीं बनेंगी, उन्हें खुली साँसों की मोहलत भी प्रदान करेगी।
अतिरिक्त शिल्प सर्तकता से अक्रान्त इधर किसी हद तक दुरूह हुई रचनाशीलता के बरक्स, अल्पना की रचनाएँ भाषा, शिल्प और कहन के आनुपातिक शरबती रसायन-सी पाठकों के लिए अबूझ नहीं होतीं। वे सीधे संवाद करती हैं- उन्हीं स्थितियों-परिस्थितियों के सजीव परिवेश के गली-गलियारों में ले जाकर, उन्हीं की काया में प्रवेश कर, उन्हीं की विसंगतियों की त्रासदी में साँसे भरते हुए। चाहे इस संग्रह की, प्रश्नों के कटघरे में लेती ‘बेदखल’ हो या ‘मिड डे मील’ या ‘मुक्ति प्रसंग’ या हिन्दी कहानी की उपलब्धि ‘छावनी में बेघर’ !
‘छावनी में बेघर’ अल्पना की रचनाशीलता के प्रति आश्वस्ति की बुलन्द इमारत की पुख्ता उठान ही नहीं निर्मित करता है, पाठकों के मन में अपेक्षा और उम्मीद की चौतरफा खिड़कियों की भी आशा बोता है- जो अपने समय की हवा की उन्मुक्त आवाजाही की साक्ष्य भर ही नहीं बनेंगी, उन्हें खुली साँसों की मोहलत भी प्रदान करेगी।
चित्रा मुद्गल
मुक्ति-प्रसंग
तो वे बदहवास-सी भीड़-भरे चौराहे को पार करते बस के पीछे दौड़ी जा रही
थीं। साड़ी की चुन्नटों को एक हाथ से थोड़ा-सा उठाये, दाहिने हाथ के पर्स
को पेट पर चिपकाये चिल्लाये जा रही थीं- ‘‘रोकना भाई,
रोकना
!’’
इस बस के छूटने का मतलब था पन्द्रह-बीस मिनट या आधे घंटे इन्तजार और। फिलहाल वे अपनी तमाम दुनियावी इच्छाओं के एवज में भी यह नहीं चाहेंगी कि यह बस छूट जाए। बेकार में प्रिंसिपल की कुदृष्टि और विभागाध्यक्ष के व्यंग्यबाण कौन चाहेगा ! एक बार बस में चढ़ जाएँ और भाग्यवश या चलिए कर्मवश कह लीजिए अर्थात् छीनते-झपटते हुए यदि खिड़की के पास की सीट मिल जाय और यदि भाग्यवश उनके बगल में कोई बुजुर्ग (सभ्य भाषा में वे बुजुर्ग कह देती हैं, पर इस बुजुर्ग से कमीने अधेड़ों, कुंठित बुड्ढों या फिर सेक्सियाये आदमियों से होता है) बैठ न जाये या फिर कोई दुष्ट जवान बैठते-बैठते रह जाये, तो इसे वे कर्म से इतर ही मानेंगी। कोई डरता-सा बालक या कोई शान्त-सी स्त्री बैठे तो कम से कम वे कुछ देर के लिए नैतिक संसार से इतर उस विश्वासमय भावलोक की यात्रा कर सकेंगी, जिसे वे थोड़ी देर के लिए ‘मुक्ति की साँस’ लेना कहती हैं।
कई बार तो छीना-झपटी का कर्म करते हुए वे उन्हीं के महाविद्यालय की मीना को भी भूल जाती हैं, जो स्टाप से उन्हें कभी-कभी मिल जाती है। उनकी आँख उस समय अर्जुन की आँख होती है और मछली की आँख होती है वह खाली जगह, जो कभी भी, किसी भी वक्त बस में बन सकती है। इस खाली जगह को प्राप्त करने के लिए वे वह सब कुछ कर सकती हैं, जो बस में किया जा सकता है। मसलन अपनी लाबेला की चप्पल किसी के भी पैर पर रखते हुए, किसी के भी हाथ, कोहनी, कन्धे, पुट्ठे से टकराते हुए, यहाँ तक कि कई बार तो कोई भद्दा आदमी जानबूझकर उनके उरोजों से टकरा जाता, पर वे लक्ष्य नहीं छोड़ती, परवाह नहीं करतीं। अब बस में जाना है तो यह सब तो लगा ही रहेगा।
‘अब क्या वे हवाई जहाज से जाएँगी।’ (हवाले से डॉक्टर साहब)
मीना के लिए वे जगह नहीं बनातीं। वे मानती हैं कि व्यक्ति को अपने लिए जगह खुद बनानी चाहिए, दूसरे कितने दिन किसी का हाथ पकड़कर चलना सिखाएँगे। ‘काक चेष्टा बको-ध्यानम्’ का पालन मीना को भी करना चाहिए। अब उन्हें डोसाइल (घरेलू, नाजुक) औरतें अच्छी नहीं लगतीं। इन्हें देखकर वे घबराने लगती हैं- अपने पुराने रूप की झलक, इतनी दब्बू, डरपोक वे थीं क्या ? इच्छा-अनिच्छा के अर्थपूर्ण झंझटों से अलग, भावाभाव से चिड़चिड़ाती, जय-पराजय से उद्वेलित, आदेशों के उल्लंघन से डरती-ऐसी थीं वे- बच्चों की नींदों के साथ जगती, डॉक्टर साहब के खर्राटों के साथ उँघती- इससे ज्यादा क्या ? किताबों के समन्दर में डूबती, सूर-तुलसी, मीरा के गहन आदर्श प्रेम के सपने देखती, घनानन्द के साथ रोती, बिहारी के साथ सौन्दर्य निहारती- इससे ज्यादा सचमुच क्या ? अब ये सब प्रेम, रोमांस वगैरह डॉ. साहब की परिपक्वता के आगे तुच्छ लड़कपन के खेल थे, पर वे क्या उस समय लड़कपन के बाहर थीं ?
कुल उन्नीस बरस में ही तो अपनी गरदन पर भोला-सा चेहरा लगाये दुनिया की समझ से बेखबर, अपनी किताबों का छोटा –सा संसार लिए डॉ. साहब के साथ चली तो आयीं थीं। अब क्या बताइए, उस लड़कपने की आदर्श रूमानियत। अपनी शादी के बक्सों में, कपड़ों में तहा-तहा कर तो किताबें रखीं थी उन्होंने। अब यह तो सरासर उन्हीं की गलती थी कि वे एक रात में परिपक्व नहीं हो पायीं ! तो आगे पढ़ते जाने जैसे विद्रोह की पहली चिंगारी उनमें यहीं से सुलगी थी। और रास्ता भी क्या था ? तो आगे पढ़ते जाने जैसे परिपक्व फैसले के बावजूद मायके से ससुराल तक उन्हें परिपक्व नहीं माना गया। चलिए, लोग न मानें पर वे तो मानती हैं कि सपने की दुनिया में विचरने का सुख अपना निहायत व्यक्तिगत होता है और यह सपनों की दुनिया उन्हें किताबों के रास्ते से गुजरकर मिलती थी।
अब अगर बस में उनके मन मुताबिक जगह न मिले तो वे बराबर सतर्क रहती हैं। यह सतर्कता उनकी मजबूरी है। यह मजबूरी उन्होंने अपने अनुभवों से हासिल की है। हालाँकि यदि वे डॉ. साहब को यह सब छीना-झपटी, यहाँ तक कि रगड़ा-रगड़ी की कहानी भी सुना दें तो भी वे ये यकीन नहीं कर पाएँगे। वैसे भी वे इस तरह की बातों को तूल नहीं देते। हाँ, कोई उनके सामने करके देखे।
दरअसल डॉ. साहब जिस मारुति कार में जीते हैं, उसी की सीट को वे बस की सीट की तरह देख लेते हैं। एक तरफ वे चाहते थे कि पत्नी को ऐसी नौकरी न करनी पड़ती। कहाँ तो उन्होंने सोचा था डिग्री कॉलेज की मस्ती की नौकरी होगी और कहाँ देहरादून से ऋषिकेश दौड़ने की त्रासदी। तो क्या करें ? पत्नी को मिली हुई सरकारी नौकरी छुड़वा दें ? वाह, कैसे ? जब देहरादून जैसी जगह में हैं तो बच्चों को ऋषिकेश रखने का क्या तुक ? पत्नी ने जब अपने बलबूते नौकरी शुरू की है तो दुनिया-जहान की जलालतें-मलालतें उन्हीं के हिस्से। उन्होंने कब कहा था ? वे तो चुप थे। सो अब करो नौकरी ! दूसरी तरफ डॉ. साहब यह सोचकर, कहकर अपने को समझा लेते हैं कि ‘वे डॉ. साहब को डराना चाहती हैं, जिससे नौकरी छुड़वाकर घर बैठा दे।’ पर डॉ. साहब यह नहीं जानते। शायद जानते हों, स्वीकार न करते हों कि अब वे उन्हें घर बैठने को कहें भी तो वे नहीं बैठेंगी। वह मुक्ति की साँस क्या घर बैठे मिलेगी ? अब तो वे जान की बाजी लगाकर भी नौकरी करेंगी। यह उन्होंने आज नहीं, बल्कि उसी दिन ठान लिया था, जब देहरादून से ऋषिकेश तक इसी बस में बैठकर पहले दिन गयी थीं। यह पहला दिन ही उन्हें मुक्ति का एक हल्का-सा अहसास करा गया था।
हुआ यूँ था कि जब डॉ. साहब अपनी मारुति में बैठाकर उन्हें बस स्टेशन तक लाये, तो वहाँ ऋषिकेश के लिए कोई बस नहीं थी। पूछताँछ काउंटर पर हर बार यही पता चलता कि बस आती होगी। डॉ. साहब अपनी आदत के विपरीत आधे घंटे तक इन्तजार करते रहे। आखिरकार जब बस आयी तो डॉ. साहब ड्यूटी पर लेट होने लगे थे और ‘यही ऋषिकेशवाली बस, जो आ रही है, इसी में बैठ जाना’ ऐसा निर्देश देकर चले गये। यह पहला वक्त था जब कोई भी उनके साथ नहीं था। कह लीजिए यह पहली अकेली यात्रा थी उनकी। ऋषिकेश महाविद्यालय में ज्वॉइनिंग तक तो डॉ. साहब लगातार उनके साथ बने हुए थे। पर कब तक बने रहते ? आखिर आज छोड़ना ही पड़ा। वह भी कैसे ? न तो बस में एक सुरक्षित सीट पर बैठा पाये, न ही बस ड्राइवर-कंडक्टर को सौंप पाये अपनी जिम्मेदारी। सीट आज उनके काउंसलिंग विभाग में जरूरी मीटिंग न होती तो क्या उन्हें बस स्टेशन पर अकेला छोड़कर वे जाते ? क्या डॉ. साहब के लिए अपनी नौकरी इतनी महत्त्वपूर्ण है, जिसके आगे वे नातों, रिश्तों, व्यक्ति और समाज को बौना करके देखते हैं ? तो फिर उनके लिए भी उनकी नौकरी यानी महाविद्यालय की मास्टरी महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। बस स्टेशन पर खड़े ही खड़े उन्होंने अचानक अपने जीवन को संशोधित करता एक निहायत जरूरी फैसला ले डाला।
तो वे बस के सामने अकेले दाहिने हाथ का पर्स पेट पर चिपकाये, थोड़ा-सा नर्वस, डर, घबराहट के साथ खड़ी थीं।
‘‘ऋषिकेश जाना है ?’’
उनके बायें कान के पास कोई फुसफुसाया।
वे भौंचक। इसे कैसे पता कि उन्हें ऋषिकेश जाना है ?
‘‘आइए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी।’’
जब वे यन्त्रचालित-सी उस आदमी के पीछे बस में चढ़ रही थीं तो उनके किताबी ज्ञान ने उन्हें हल्का-सा धिक्कारा था। अब इस सहारे की क्या जरूरत ? बस सामने खड़ी थी तो उन्हें खुद ही चढ़ जाना था। अब तो देर हो चुकी थी वे उस अधेड़ आदमी की बगल में बैठ भी चुकी थीं। उस आदमी ने बड़ी शालीनता से उनसे पैसे लेकर उनका भी टिकट ला दिया। वे कृतज्ञ हुईं। हालाँकि यहीं पर उनके किताबी ज्ञान ने उन्हें फिर धिक्कारा था। इस सहारे की क्या जरूरत ? वे खुद उठकर टिकट ला सकती थीं। धीरे-धीरे इस किताबी ज्ञान ने कुछ ज्यादा ही धिक्कारना शुरू कर दिया। सभ्य-शालीन-अधेड़ (जिन्हें अब वे कमीने अधेड़ कहती हैं) उन पर कृपादिष्ट फेरने लगे। निकट और निकट। अधेड़ का बायाँ अंग और उनका दायाँ अंग लगभग एक हो गये थे। वे जितना दबकर किनारे जा सकती थीं, जाती रहीं। वे कैसे इस आदमी को कुछ कहें ? कृतज्ञ भी थीं ? इस कृतज्ञता से कैसे मुक्त हों ? इस मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने अपना दायाँ पैर उठाकर बायें के ऊपर कर लिया। चेहरा खिड़की से लगभग बाहर।
‘‘ऋषिकेश में कहाँ जाओगी ?’’
बदबू की एक लहर, पसीने की इतनी तेज गन्ध, वे इसे सहन करते हुए मुँह उधर किये हुए ही बोलीं, ‘‘डिग्री कॉलेज।’’
उन्हें लगा डिग्री कॉलेज कहने से उनका कद दो फुट बढ़ गया है और अब तो यह आदमी जरूर ठीक व्यवहार करेगा।
‘‘पढ़ने या पढ़ाने ?’’
इस प्रश्न से वे बुरी तरह गिरीं। हालाँकि उन्हें खुश होना चाहिए था कि वे इतनी छोटी दीखती हैं, पर वे बड़ा दीखना चाहती हैं- अपनी उम्र से भी और सामाजिक दायरों के कसाव से भी।
‘‘पढ़ाने ?.......क्यों ?’’
अब उनका ध्यान गया कि यह बदबू पसीने की कम और उसके मुँह में भरे तम्बाकू की ज्यादा है। यह तो ऐसे गन्धा रहा है, जैसे टट्टी लपेटे बैठा हो। वितृष्णा से उन्हें उबकाई आयी।
‘‘मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ाती है।’’
कहकर उस अधेड़ ने अपना बायाँ हाथ, जोकि अब तक उनके दायें हाथ से सटा था, उठाकर उनके कन्धे के पीछे कर लिया। अब उनके दायें हाथ का कन्धा उसके सीने से सट रहा था। अगर बस जरा-सा हिचकोले खाये तो वे उसकी गोद में गिरते हुए बाहुपाश में बँध जाएँगी। ‘अभद्र’ उन्होंने सोचा। ये किस नौकरी में फँस गयीं वे ? यह रोज देहरादून से ऋषिकेश आना-जाना। क्या करें ? ऋषिकेश जाकर रहें, लेकिन डॉ. साहब बच्चों को देहरादून पढ़ाना चाहते हैं। ये किस मुसीबत में डाल दिया डॉ. साहब ने उन्हें ? उन्होंने अनजाने ही डॉ. साहब को कोसा।
‘‘कितने बजे लौटती हो ?’’
अब सचमुच उनके लिए इस बोझ को सहना कठिन हो रहा है। इनकी बेटी कैसे स्कूल में पढ़ाने जाती होगी ? पता नहीं जाती भी है या नहीं ? ऐसे ही भाव मारने के लिए कह रहा हो। अगर जाती ही है तो कैसे ? बस, टैम्पो किसी से तो जाती होगी। या हो सकता है कि अपनी बाइक हो। स्कूल में लोग नहीं हैं ? स्कूल का अपना प्रबन्धतन्त्र, फिर भी दूसरी औरतों को तकलीफ देते हैं। ‘सड़े हुए बेचारे लोग’, ऐसे तो वे अनुभवों के खजाने पर खड़ी होकर सोचती हैं। पर तब बहुत विद्रोह था मन में।
‘‘पती नहीं’’ उन्होंने थोड़ा सख्त मुद्रा में कहा।
‘‘फिर भी कोई तो टाइम तो होगा। मुझे भी लौटना है, साथ ही लौटते.....’’
यह कहते हुए वह थोड़ा-सा घबराया।
प्रेम और रोमांस। एक अतृप्त आकांक्षा- वे हतप्रभ थीं। भारतीय समाज के बेचारे ये बूढ़े बुजुर्ग !
इस बस के छूटने का मतलब था पन्द्रह-बीस मिनट या आधे घंटे इन्तजार और। फिलहाल वे अपनी तमाम दुनियावी इच्छाओं के एवज में भी यह नहीं चाहेंगी कि यह बस छूट जाए। बेकार में प्रिंसिपल की कुदृष्टि और विभागाध्यक्ष के व्यंग्यबाण कौन चाहेगा ! एक बार बस में चढ़ जाएँ और भाग्यवश या चलिए कर्मवश कह लीजिए अर्थात् छीनते-झपटते हुए यदि खिड़की के पास की सीट मिल जाय और यदि भाग्यवश उनके बगल में कोई बुजुर्ग (सभ्य भाषा में वे बुजुर्ग कह देती हैं, पर इस बुजुर्ग से कमीने अधेड़ों, कुंठित बुड्ढों या फिर सेक्सियाये आदमियों से होता है) बैठ न जाये या फिर कोई दुष्ट जवान बैठते-बैठते रह जाये, तो इसे वे कर्म से इतर ही मानेंगी। कोई डरता-सा बालक या कोई शान्त-सी स्त्री बैठे तो कम से कम वे कुछ देर के लिए नैतिक संसार से इतर उस विश्वासमय भावलोक की यात्रा कर सकेंगी, जिसे वे थोड़ी देर के लिए ‘मुक्ति की साँस’ लेना कहती हैं।
कई बार तो छीना-झपटी का कर्म करते हुए वे उन्हीं के महाविद्यालय की मीना को भी भूल जाती हैं, जो स्टाप से उन्हें कभी-कभी मिल जाती है। उनकी आँख उस समय अर्जुन की आँख होती है और मछली की आँख होती है वह खाली जगह, जो कभी भी, किसी भी वक्त बस में बन सकती है। इस खाली जगह को प्राप्त करने के लिए वे वह सब कुछ कर सकती हैं, जो बस में किया जा सकता है। मसलन अपनी लाबेला की चप्पल किसी के भी पैर पर रखते हुए, किसी के भी हाथ, कोहनी, कन्धे, पुट्ठे से टकराते हुए, यहाँ तक कि कई बार तो कोई भद्दा आदमी जानबूझकर उनके उरोजों से टकरा जाता, पर वे लक्ष्य नहीं छोड़ती, परवाह नहीं करतीं। अब बस में जाना है तो यह सब तो लगा ही रहेगा।
‘अब क्या वे हवाई जहाज से जाएँगी।’ (हवाले से डॉक्टर साहब)
मीना के लिए वे जगह नहीं बनातीं। वे मानती हैं कि व्यक्ति को अपने लिए जगह खुद बनानी चाहिए, दूसरे कितने दिन किसी का हाथ पकड़कर चलना सिखाएँगे। ‘काक चेष्टा बको-ध्यानम्’ का पालन मीना को भी करना चाहिए। अब उन्हें डोसाइल (घरेलू, नाजुक) औरतें अच्छी नहीं लगतीं। इन्हें देखकर वे घबराने लगती हैं- अपने पुराने रूप की झलक, इतनी दब्बू, डरपोक वे थीं क्या ? इच्छा-अनिच्छा के अर्थपूर्ण झंझटों से अलग, भावाभाव से चिड़चिड़ाती, जय-पराजय से उद्वेलित, आदेशों के उल्लंघन से डरती-ऐसी थीं वे- बच्चों की नींदों के साथ जगती, डॉक्टर साहब के खर्राटों के साथ उँघती- इससे ज्यादा क्या ? किताबों के समन्दर में डूबती, सूर-तुलसी, मीरा के गहन आदर्श प्रेम के सपने देखती, घनानन्द के साथ रोती, बिहारी के साथ सौन्दर्य निहारती- इससे ज्यादा सचमुच क्या ? अब ये सब प्रेम, रोमांस वगैरह डॉ. साहब की परिपक्वता के आगे तुच्छ लड़कपन के खेल थे, पर वे क्या उस समय लड़कपन के बाहर थीं ?
कुल उन्नीस बरस में ही तो अपनी गरदन पर भोला-सा चेहरा लगाये दुनिया की समझ से बेखबर, अपनी किताबों का छोटा –सा संसार लिए डॉ. साहब के साथ चली तो आयीं थीं। अब क्या बताइए, उस लड़कपने की आदर्श रूमानियत। अपनी शादी के बक्सों में, कपड़ों में तहा-तहा कर तो किताबें रखीं थी उन्होंने। अब यह तो सरासर उन्हीं की गलती थी कि वे एक रात में परिपक्व नहीं हो पायीं ! तो आगे पढ़ते जाने जैसे विद्रोह की पहली चिंगारी उनमें यहीं से सुलगी थी। और रास्ता भी क्या था ? तो आगे पढ़ते जाने जैसे परिपक्व फैसले के बावजूद मायके से ससुराल तक उन्हें परिपक्व नहीं माना गया। चलिए, लोग न मानें पर वे तो मानती हैं कि सपने की दुनिया में विचरने का सुख अपना निहायत व्यक्तिगत होता है और यह सपनों की दुनिया उन्हें किताबों के रास्ते से गुजरकर मिलती थी।
अब अगर बस में उनके मन मुताबिक जगह न मिले तो वे बराबर सतर्क रहती हैं। यह सतर्कता उनकी मजबूरी है। यह मजबूरी उन्होंने अपने अनुभवों से हासिल की है। हालाँकि यदि वे डॉ. साहब को यह सब छीना-झपटी, यहाँ तक कि रगड़ा-रगड़ी की कहानी भी सुना दें तो भी वे ये यकीन नहीं कर पाएँगे। वैसे भी वे इस तरह की बातों को तूल नहीं देते। हाँ, कोई उनके सामने करके देखे।
दरअसल डॉ. साहब जिस मारुति कार में जीते हैं, उसी की सीट को वे बस की सीट की तरह देख लेते हैं। एक तरफ वे चाहते थे कि पत्नी को ऐसी नौकरी न करनी पड़ती। कहाँ तो उन्होंने सोचा था डिग्री कॉलेज की मस्ती की नौकरी होगी और कहाँ देहरादून से ऋषिकेश दौड़ने की त्रासदी। तो क्या करें ? पत्नी को मिली हुई सरकारी नौकरी छुड़वा दें ? वाह, कैसे ? जब देहरादून जैसी जगह में हैं तो बच्चों को ऋषिकेश रखने का क्या तुक ? पत्नी ने जब अपने बलबूते नौकरी शुरू की है तो दुनिया-जहान की जलालतें-मलालतें उन्हीं के हिस्से। उन्होंने कब कहा था ? वे तो चुप थे। सो अब करो नौकरी ! दूसरी तरफ डॉ. साहब यह सोचकर, कहकर अपने को समझा लेते हैं कि ‘वे डॉ. साहब को डराना चाहती हैं, जिससे नौकरी छुड़वाकर घर बैठा दे।’ पर डॉ. साहब यह नहीं जानते। शायद जानते हों, स्वीकार न करते हों कि अब वे उन्हें घर बैठने को कहें भी तो वे नहीं बैठेंगी। वह मुक्ति की साँस क्या घर बैठे मिलेगी ? अब तो वे जान की बाजी लगाकर भी नौकरी करेंगी। यह उन्होंने आज नहीं, बल्कि उसी दिन ठान लिया था, जब देहरादून से ऋषिकेश तक इसी बस में बैठकर पहले दिन गयी थीं। यह पहला दिन ही उन्हें मुक्ति का एक हल्का-सा अहसास करा गया था।
हुआ यूँ था कि जब डॉ. साहब अपनी मारुति में बैठाकर उन्हें बस स्टेशन तक लाये, तो वहाँ ऋषिकेश के लिए कोई बस नहीं थी। पूछताँछ काउंटर पर हर बार यही पता चलता कि बस आती होगी। डॉ. साहब अपनी आदत के विपरीत आधे घंटे तक इन्तजार करते रहे। आखिरकार जब बस आयी तो डॉ. साहब ड्यूटी पर लेट होने लगे थे और ‘यही ऋषिकेशवाली बस, जो आ रही है, इसी में बैठ जाना’ ऐसा निर्देश देकर चले गये। यह पहला वक्त था जब कोई भी उनके साथ नहीं था। कह लीजिए यह पहली अकेली यात्रा थी उनकी। ऋषिकेश महाविद्यालय में ज्वॉइनिंग तक तो डॉ. साहब लगातार उनके साथ बने हुए थे। पर कब तक बने रहते ? आखिर आज छोड़ना ही पड़ा। वह भी कैसे ? न तो बस में एक सुरक्षित सीट पर बैठा पाये, न ही बस ड्राइवर-कंडक्टर को सौंप पाये अपनी जिम्मेदारी। सीट आज उनके काउंसलिंग विभाग में जरूरी मीटिंग न होती तो क्या उन्हें बस स्टेशन पर अकेला छोड़कर वे जाते ? क्या डॉ. साहब के लिए अपनी नौकरी इतनी महत्त्वपूर्ण है, जिसके आगे वे नातों, रिश्तों, व्यक्ति और समाज को बौना करके देखते हैं ? तो फिर उनके लिए भी उनकी नौकरी यानी महाविद्यालय की मास्टरी महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। बस स्टेशन पर खड़े ही खड़े उन्होंने अचानक अपने जीवन को संशोधित करता एक निहायत जरूरी फैसला ले डाला।
तो वे बस के सामने अकेले दाहिने हाथ का पर्स पेट पर चिपकाये, थोड़ा-सा नर्वस, डर, घबराहट के साथ खड़ी थीं।
‘‘ऋषिकेश जाना है ?’’
उनके बायें कान के पास कोई फुसफुसाया।
वे भौंचक। इसे कैसे पता कि उन्हें ऋषिकेश जाना है ?
‘‘आइए, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी।’’
जब वे यन्त्रचालित-सी उस आदमी के पीछे बस में चढ़ रही थीं तो उनके किताबी ज्ञान ने उन्हें हल्का-सा धिक्कारा था। अब इस सहारे की क्या जरूरत ? बस सामने खड़ी थी तो उन्हें खुद ही चढ़ जाना था। अब तो देर हो चुकी थी वे उस अधेड़ आदमी की बगल में बैठ भी चुकी थीं। उस आदमी ने बड़ी शालीनता से उनसे पैसे लेकर उनका भी टिकट ला दिया। वे कृतज्ञ हुईं। हालाँकि यहीं पर उनके किताबी ज्ञान ने उन्हें फिर धिक्कारा था। इस सहारे की क्या जरूरत ? वे खुद उठकर टिकट ला सकती थीं। धीरे-धीरे इस किताबी ज्ञान ने कुछ ज्यादा ही धिक्कारना शुरू कर दिया। सभ्य-शालीन-अधेड़ (जिन्हें अब वे कमीने अधेड़ कहती हैं) उन पर कृपादिष्ट फेरने लगे। निकट और निकट। अधेड़ का बायाँ अंग और उनका दायाँ अंग लगभग एक हो गये थे। वे जितना दबकर किनारे जा सकती थीं, जाती रहीं। वे कैसे इस आदमी को कुछ कहें ? कृतज्ञ भी थीं ? इस कृतज्ञता से कैसे मुक्त हों ? इस मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने अपना दायाँ पैर उठाकर बायें के ऊपर कर लिया। चेहरा खिड़की से लगभग बाहर।
‘‘ऋषिकेश में कहाँ जाओगी ?’’
बदबू की एक लहर, पसीने की इतनी तेज गन्ध, वे इसे सहन करते हुए मुँह उधर किये हुए ही बोलीं, ‘‘डिग्री कॉलेज।’’
उन्हें लगा डिग्री कॉलेज कहने से उनका कद दो फुट बढ़ गया है और अब तो यह आदमी जरूर ठीक व्यवहार करेगा।
‘‘पढ़ने या पढ़ाने ?’’
इस प्रश्न से वे बुरी तरह गिरीं। हालाँकि उन्हें खुश होना चाहिए था कि वे इतनी छोटी दीखती हैं, पर वे बड़ा दीखना चाहती हैं- अपनी उम्र से भी और सामाजिक दायरों के कसाव से भी।
‘‘पढ़ाने ?.......क्यों ?’’
अब उनका ध्यान गया कि यह बदबू पसीने की कम और उसके मुँह में भरे तम्बाकू की ज्यादा है। यह तो ऐसे गन्धा रहा है, जैसे टट्टी लपेटे बैठा हो। वितृष्णा से उन्हें उबकाई आयी।
‘‘मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ाती है।’’
कहकर उस अधेड़ ने अपना बायाँ हाथ, जोकि अब तक उनके दायें हाथ से सटा था, उठाकर उनके कन्धे के पीछे कर लिया। अब उनके दायें हाथ का कन्धा उसके सीने से सट रहा था। अगर बस जरा-सा हिचकोले खाये तो वे उसकी गोद में गिरते हुए बाहुपाश में बँध जाएँगी। ‘अभद्र’ उन्होंने सोचा। ये किस नौकरी में फँस गयीं वे ? यह रोज देहरादून से ऋषिकेश आना-जाना। क्या करें ? ऋषिकेश जाकर रहें, लेकिन डॉ. साहब बच्चों को देहरादून पढ़ाना चाहते हैं। ये किस मुसीबत में डाल दिया डॉ. साहब ने उन्हें ? उन्होंने अनजाने ही डॉ. साहब को कोसा।
‘‘कितने बजे लौटती हो ?’’
अब सचमुच उनके लिए इस बोझ को सहना कठिन हो रहा है। इनकी बेटी कैसे स्कूल में पढ़ाने जाती होगी ? पता नहीं जाती भी है या नहीं ? ऐसे ही भाव मारने के लिए कह रहा हो। अगर जाती ही है तो कैसे ? बस, टैम्पो किसी से तो जाती होगी। या हो सकता है कि अपनी बाइक हो। स्कूल में लोग नहीं हैं ? स्कूल का अपना प्रबन्धतन्त्र, फिर भी दूसरी औरतों को तकलीफ देते हैं। ‘सड़े हुए बेचारे लोग’, ऐसे तो वे अनुभवों के खजाने पर खड़ी होकर सोचती हैं। पर तब बहुत विद्रोह था मन में।
‘‘पती नहीं’’ उन्होंने थोड़ा सख्त मुद्रा में कहा।
‘‘फिर भी कोई तो टाइम तो होगा। मुझे भी लौटना है, साथ ही लौटते.....’’
यह कहते हुए वह थोड़ा-सा घबराया।
प्रेम और रोमांस। एक अतृप्त आकांक्षा- वे हतप्रभ थीं। भारतीय समाज के बेचारे ये बूढ़े बुजुर्ग !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i