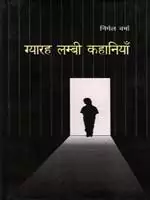|
कहानी संग्रह >> मेरी प्रिय कहानियाँ (अजिल्द) मेरी प्रिय कहानियाँ (अजिल्द)निर्मल वर्मा
|
204 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत हैं निर्मल वर्मा की प्रिय कहानियों का संग्रह...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
पिछले पन्द्रह वर्षों में समय-समय पर जो कहानियाँ लिखी थीं,
उनमें
से कुछ भी चुनकर एक जगह संकलित करने का यह पहला अवसर है। इससे पहले मैंने
कल्पना नहीं की थी कि चुनने के काम में इतना घना ख़ालीपन महसूस हो सकता
है। खुद भी अपनी कहानियों के बारे में यों भी कुछ कहना एक निर्थक प्रयास
है। सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनने-छांटने का काम कुछ अर्से बाद समय खुद कर
लेता है, बल्कि इसलिए भी जिस मोह में कहानियाँ जन्म लेती हैं, वह बराबर
कायम नहीं रहता।
कभी वह कम हो जाता है कभी अधिक (और इस ‘कम-ज़्यादा’ के पीछे कोई तर्क जुटा पाना असंभव है) और यद्यपि कहानियाँ वहीं रहती हैं, हर पाँच दस वर्ष बाद उनके प्रति दिलचस्पी का पेंडुलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूम जाता है। यदि हर पाँच वर्ष बाद मुझे अपनी प्रिय ‘‘कहानियाँ’ चुनने का मौका मिले तो शायद पहले की छूटी हुई कहानियाँ भीतर आ जाएँ और भीतर बैठी हुई कहानियाँ छूट जाएँ और। वह शायद ठीक भी है। और होना ऐसा ही चाहिए।
अपनी इन कहानियों को चुनने से पहले मैंने दुबारा पढ़ा था। पढ़ते समय मुझे बार-बार एक अँग्रेजी लेखक की बात याद आ रही,’ अर्से बाद अपनी पुरानी कहानियाँ पढ़ते हुए गहरा आश्चर्य होता कि मैंने ही उन्हें कभी लिखा था। बार-बार यह भ्रम होता है कि मैं किसी अजनबी लेखक की कहानियां पढ़ रहा हूँ जिसे मैं पहले कभी जानता था। साथ-साथ एक अजीब किस्म का सुखद विस्मय भी होता है कि ये कहानियाँ एक जमाने में उस व्यक्ति ने लिखी थीं, जो आज मैं हूँ।’’
मेरे लिए यह आश्चर्य गूंगी किस्म की सुन्न उदासी से जुड़ा है। एक तरह का बचकाना क्षोभ-क्योंकि यह सन्देह बराबर कहीं कोंचता है कि अच्छी हों या बुरी, ये कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ अब लिखना असम्भव है। थोड़ी-बहुत ख्याति मिल जाने पर (चाहे उसका कौड़ी-भर मूल्य न हो) हर लेखक अपनी शुरू-शुरू की निरीह कातरता (vulnerability) को खो देता है, जब लिखना छिपकर सिगरेट पीने की तरह या जुलाई की रातों में छतों पर जागने की तरह था-एक ख़ास किस्म की हिन्दुस्तानी व्यथा-जो न इधर है, न उधर। यों तो शायद हर देशी-विदेशी लेखक को देर-सवेरे अपना ‘कुंवारापन’ (Sense of innocence) खो देना पड़ता है, किन्तु मैं इस ख्याल को कभी नहीं निगल पाता कि एक बार खो देने के बाद उसे दुबारा पकड़ने का भ्रम भी हटा देना चाहिए। औरों की बात कहना अनुचित है, पर मेरे लिए खोये हुए ‘कुंवारेपन’ की मरीचिका बहुत जरूरी है जिसके पीछे जिन्दगी भर सूने मरुस्थल में भागा जा सके। यह जानते हुए भी कि वह हमेशा पकड़ के बाहर है-लेकिन हमेशा बाहर रहेगी, इसका विश्वास जरूरी नहीं।
इन कहानियों को दुबारा पढ़ते हुए मुझे लगा है कि मेरे लिए हर कहानी एक नाकाम-और कभी-कभी सौभाग्य के क्षणों में-लगभग सफल कोशिश रही है कि जंगल के अंतहीन सूनेपन उस घास के टु़कड़े तक लौट सकूँ जहाँ मैंने किसी अनजाने और मूर्खतापूर्ण क्षण में पहली बार जीने, सूँघने, रोने और देखने को खो दिया था। एक अपराधी की तरह मैं बार-बार उस ‘घटनास्थल’ तक पहुँचना चाहता हूँ। मेरे लिए ‘भोगे हुए यथार्थ’ को पुनर्जीवित करने की आकांक्षा कभी नहीं रही। अगर कभी आकांक्षा रही तो उस खाली वीरान, जगहों को भरने की जो भोगते हुए क्षण की बदहवासी और भुलाने को हड़बड़ाहट में अनछुए रह गए थे या जिन्हें छूने का साहस अपने-आपसे परे की बात लगा था।
यह वह बिन्दु है जहां लिखने का जोखिम करीब-करीब जीने के भ्रम के साथ जुड़ जाता है। यह मौका है दुबारा जीने का। चेखव की एक बहुत पुरानी कहानी है, जब गाँव की मास्टरानी एक शाम घर लौटते हुए लेविल-क्रासिंग पर रेल के गुज़र जाने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती है-शाम के धुंधलके में अपनी हताश, सूनी ज़िन्दगी में लिपटी हुई। कुछ देर बाद ट्रेन गुज़रती है – अचानक ट्रेन के एक डिब्बे में उसे एक ड़बड़बाया हुआ चेहरा दिखाई देता है, हूबहू अपनी माँ का चेहरा, हालाँकि उसकी माँ वर्षों पहले मर चुकी है-लेकिन चेहरा वही है, वही झुर्रियां हैं वही दो पहचानी आँखों का भीगा आलोक। तब एक क्षण-भर के लिए चमकीला-सा बोध होता है कि गँवई-गाँव की अकेली मास्टरनी की आँखों से खुद चेखव अपनी ज़िन्दगी दोहरा रही हों-एक गुज़रती हुई गाड़ी में माँ का चेहरा-उसकी एक टिमटिमाती झलक पकड़ पाना-यह उस मरीचिका की खोज है, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था।
वर्षों विदेश में रहने के कारण मेरी कुछ कहानियों में शायद एक वीराने किस्म का ‘प्रवासीपन’ चला आया है- मुझे नहीं मालूम यह कहानियों को अच्छा बनाता है या बुरा। कुछ भी हो, इन्हें ‘विदेशी कहानियाँ’ कहना शायद ठीक न होगा। यों भी मुझे कहानियों, कविताओं को भौगोलिक खण्डों में विभाजित करना अरुचिकर और बहुत हद तक अर्थहीन लगता रहा ग्राहम-ग्रीन ज़िन्दगी भर अपने उपन्यासों के कथानक ढूँढते रहे-लेकिन रहे शुरू से लेकर आख़िर तक ठेठ अंग्रेजी लेखक। क्या लारेन्स की कहानियों-उपन्यासों को देशी-विदेशी कटघरों में बाँटना हास्यास्द नहीं होगा ? मैं यहाँ यह चीज़ अपनी कहानियों को ‘बचाने’ के लिए नहीं (इसकी मुझे कोई लालसा नहीं) केवल एक सीधी-सी बात को सीधे ढंग से रखने की कोशिश में कह रहा हूँ ताकि हम निरर्थक बहसों से छुटकारा पा सकें। दरअसल किसी लेखक की पृष्ठभूमि विदेशी है या देशी, यह चीज़ बहुत ही गौण है। उसका महत्व है तो सिर्फ इसमें कि किस सीमा तक और कितनी गहराई से वह किसी खास स्थिति या नियति को खोल पाती है –बल्कि यूँ कहें, महत्व की कोई चीज़ है, तो सिर्फ यह ही-बाकी सब राख है।
आज सोचता हूँ तो मुझे स्वयं अपनी कहानियों की परिस्थिति (देशी या परदेशी) ज़्यादा स्पष्ट रूप से याद नहीं आतीं। केवल एक धुंधली–सी स्मृति छाया की तरह हर कहानी के साथ जुड़ी रह गयी है। ये कहानियाँ या इनमें से अधिकांश अलग-अलग टुकड़ों में काफी लम्बे अन्तरालों के बीच लिखी गई थीं। ‘परिन्दे’ और ‘अँधेरे में’ के बारे में कुछ भी कहना असंभव जान पड़ता है। पहाड़ी मकानों की एक खास निर्जन किस्म की भुतैली आभा होती है। इसे वह समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने अकेले सांय-सांय करते बचपन के हर्ष, बहुत-से वर्ष, एक साथ पहाड़ी स्टेशनों पर गुजा़रे हों।
कई परेशान और ज्वर-ग्रस्त कहानियाँ (‘डेढ़ इंच ऊपर या ‘इतनी बड़ी आकांक्षा’) उन शराबघरों के बारे में हैं। जहां मैं बारिश और ठंड से बचने के लिए घड़ी-दो-घड़ी बैठ जाता था या जब रात इतनी आगे बढ़ जाती थी कि घर लौटना कायरता जान पड़ता था। यूरोप के अलग-अलग शहरों की स्मृति एक तरह से इन रातों के झुरमुट में दबी है। मुझमें चाहे कोई आकर्षण न हो, लेकिन किसी लुटी-पिटी ‘बार या ‘पब’ में पियक्कड़ों को-या ऐसे ‘तलछटी’ प्राणियों को, जो बहुत गहरे में जा चुके हों-अपनी तरफ़ खींचने की अद्भुत क्षमता रही है। मुझे देखते ही वे मेरी मेंज़ के इर्द-गिर्द बैठ जाते थे। ‘‘You are a quiet Indian, aren’ t you ?’’ ( बाद में उनके बीच मैं लम्बे अर्से तक इसी नाम से प्रसिद्ध रहा) उनकी ऊपर से अनर्गल दीखने वाली आत्मकथाओं में मुझे पहली बार उन अँधेरे कोनों से साक्षात्कार हुआ, जिन्हें मैं छिपाकर रखता आया था। आज मैं जो कुछ हूं उसका एक हिस्सा इन आज्ञात लोगों की देन हैं-जो अब हमेशा के लिए दुनिया के अलग-अलग कोनों में खो गए हैं।
मुझे खुशी हैं, वे इन कहानियों को कभी नहीं पढ़ेंगे।, यदि उन्हें मालूम होता कि उनके साथ रात गुज़ारने वाला ‘कुआयट इण्डियन’ कहानियाँ लिखकर जीवन काटता है, तो उन्हें सचमुच निराशा होती।
कभी वह कम हो जाता है कभी अधिक (और इस ‘कम-ज़्यादा’ के पीछे कोई तर्क जुटा पाना असंभव है) और यद्यपि कहानियाँ वहीं रहती हैं, हर पाँच दस वर्ष बाद उनके प्रति दिलचस्पी का पेंडुलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूम जाता है। यदि हर पाँच वर्ष बाद मुझे अपनी प्रिय ‘‘कहानियाँ’ चुनने का मौका मिले तो शायद पहले की छूटी हुई कहानियाँ भीतर आ जाएँ और भीतर बैठी हुई कहानियाँ छूट जाएँ और। वह शायद ठीक भी है। और होना ऐसा ही चाहिए।
अपनी इन कहानियों को चुनने से पहले मैंने दुबारा पढ़ा था। पढ़ते समय मुझे बार-बार एक अँग्रेजी लेखक की बात याद आ रही,’ अर्से बाद अपनी पुरानी कहानियाँ पढ़ते हुए गहरा आश्चर्य होता कि मैंने ही उन्हें कभी लिखा था। बार-बार यह भ्रम होता है कि मैं किसी अजनबी लेखक की कहानियां पढ़ रहा हूँ जिसे मैं पहले कभी जानता था। साथ-साथ एक अजीब किस्म का सुखद विस्मय भी होता है कि ये कहानियाँ एक जमाने में उस व्यक्ति ने लिखी थीं, जो आज मैं हूँ।’’
मेरे लिए यह आश्चर्य गूंगी किस्म की सुन्न उदासी से जुड़ा है। एक तरह का बचकाना क्षोभ-क्योंकि यह सन्देह बराबर कहीं कोंचता है कि अच्छी हों या बुरी, ये कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ अब लिखना असम्भव है। थोड़ी-बहुत ख्याति मिल जाने पर (चाहे उसका कौड़ी-भर मूल्य न हो) हर लेखक अपनी शुरू-शुरू की निरीह कातरता (vulnerability) को खो देता है, जब लिखना छिपकर सिगरेट पीने की तरह या जुलाई की रातों में छतों पर जागने की तरह था-एक ख़ास किस्म की हिन्दुस्तानी व्यथा-जो न इधर है, न उधर। यों तो शायद हर देशी-विदेशी लेखक को देर-सवेरे अपना ‘कुंवारापन’ (Sense of innocence) खो देना पड़ता है, किन्तु मैं इस ख्याल को कभी नहीं निगल पाता कि एक बार खो देने के बाद उसे दुबारा पकड़ने का भ्रम भी हटा देना चाहिए। औरों की बात कहना अनुचित है, पर मेरे लिए खोये हुए ‘कुंवारेपन’ की मरीचिका बहुत जरूरी है जिसके पीछे जिन्दगी भर सूने मरुस्थल में भागा जा सके। यह जानते हुए भी कि वह हमेशा पकड़ के बाहर है-लेकिन हमेशा बाहर रहेगी, इसका विश्वास जरूरी नहीं।
इन कहानियों को दुबारा पढ़ते हुए मुझे लगा है कि मेरे लिए हर कहानी एक नाकाम-और कभी-कभी सौभाग्य के क्षणों में-लगभग सफल कोशिश रही है कि जंगल के अंतहीन सूनेपन उस घास के टु़कड़े तक लौट सकूँ जहाँ मैंने किसी अनजाने और मूर्खतापूर्ण क्षण में पहली बार जीने, सूँघने, रोने और देखने को खो दिया था। एक अपराधी की तरह मैं बार-बार उस ‘घटनास्थल’ तक पहुँचना चाहता हूँ। मेरे लिए ‘भोगे हुए यथार्थ’ को पुनर्जीवित करने की आकांक्षा कभी नहीं रही। अगर कभी आकांक्षा रही तो उस खाली वीरान, जगहों को भरने की जो भोगते हुए क्षण की बदहवासी और भुलाने को हड़बड़ाहट में अनछुए रह गए थे या जिन्हें छूने का साहस अपने-आपसे परे की बात लगा था।
यह वह बिन्दु है जहां लिखने का जोखिम करीब-करीब जीने के भ्रम के साथ जुड़ जाता है। यह मौका है दुबारा जीने का। चेखव की एक बहुत पुरानी कहानी है, जब गाँव की मास्टरानी एक शाम घर लौटते हुए लेविल-क्रासिंग पर रेल के गुज़र जाने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती है-शाम के धुंधलके में अपनी हताश, सूनी ज़िन्दगी में लिपटी हुई। कुछ देर बाद ट्रेन गुज़रती है – अचानक ट्रेन के एक डिब्बे में उसे एक ड़बड़बाया हुआ चेहरा दिखाई देता है, हूबहू अपनी माँ का चेहरा, हालाँकि उसकी माँ वर्षों पहले मर चुकी है-लेकिन चेहरा वही है, वही झुर्रियां हैं वही दो पहचानी आँखों का भीगा आलोक। तब एक क्षण-भर के लिए चमकीला-सा बोध होता है कि गँवई-गाँव की अकेली मास्टरनी की आँखों से खुद चेखव अपनी ज़िन्दगी दोहरा रही हों-एक गुज़रती हुई गाड़ी में माँ का चेहरा-उसकी एक टिमटिमाती झलक पकड़ पाना-यह उस मरीचिका की खोज है, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था।
वर्षों विदेश में रहने के कारण मेरी कुछ कहानियों में शायद एक वीराने किस्म का ‘प्रवासीपन’ चला आया है- मुझे नहीं मालूम यह कहानियों को अच्छा बनाता है या बुरा। कुछ भी हो, इन्हें ‘विदेशी कहानियाँ’ कहना शायद ठीक न होगा। यों भी मुझे कहानियों, कविताओं को भौगोलिक खण्डों में विभाजित करना अरुचिकर और बहुत हद तक अर्थहीन लगता रहा ग्राहम-ग्रीन ज़िन्दगी भर अपने उपन्यासों के कथानक ढूँढते रहे-लेकिन रहे शुरू से लेकर आख़िर तक ठेठ अंग्रेजी लेखक। क्या लारेन्स की कहानियों-उपन्यासों को देशी-विदेशी कटघरों में बाँटना हास्यास्द नहीं होगा ? मैं यहाँ यह चीज़ अपनी कहानियों को ‘बचाने’ के लिए नहीं (इसकी मुझे कोई लालसा नहीं) केवल एक सीधी-सी बात को सीधे ढंग से रखने की कोशिश में कह रहा हूँ ताकि हम निरर्थक बहसों से छुटकारा पा सकें। दरअसल किसी लेखक की पृष्ठभूमि विदेशी है या देशी, यह चीज़ बहुत ही गौण है। उसका महत्व है तो सिर्फ इसमें कि किस सीमा तक और कितनी गहराई से वह किसी खास स्थिति या नियति को खोल पाती है –बल्कि यूँ कहें, महत्व की कोई चीज़ है, तो सिर्फ यह ही-बाकी सब राख है।
आज सोचता हूँ तो मुझे स्वयं अपनी कहानियों की परिस्थिति (देशी या परदेशी) ज़्यादा स्पष्ट रूप से याद नहीं आतीं। केवल एक धुंधली–सी स्मृति छाया की तरह हर कहानी के साथ जुड़ी रह गयी है। ये कहानियाँ या इनमें से अधिकांश अलग-अलग टुकड़ों में काफी लम्बे अन्तरालों के बीच लिखी गई थीं। ‘परिन्दे’ और ‘अँधेरे में’ के बारे में कुछ भी कहना असंभव जान पड़ता है। पहाड़ी मकानों की एक खास निर्जन किस्म की भुतैली आभा होती है। इसे वह समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने अकेले सांय-सांय करते बचपन के हर्ष, बहुत-से वर्ष, एक साथ पहाड़ी स्टेशनों पर गुजा़रे हों।
कई परेशान और ज्वर-ग्रस्त कहानियाँ (‘डेढ़ इंच ऊपर या ‘इतनी बड़ी आकांक्षा’) उन शराबघरों के बारे में हैं। जहां मैं बारिश और ठंड से बचने के लिए घड़ी-दो-घड़ी बैठ जाता था या जब रात इतनी आगे बढ़ जाती थी कि घर लौटना कायरता जान पड़ता था। यूरोप के अलग-अलग शहरों की स्मृति एक तरह से इन रातों के झुरमुट में दबी है। मुझमें चाहे कोई आकर्षण न हो, लेकिन किसी लुटी-पिटी ‘बार या ‘पब’ में पियक्कड़ों को-या ऐसे ‘तलछटी’ प्राणियों को, जो बहुत गहरे में जा चुके हों-अपनी तरफ़ खींचने की अद्भुत क्षमता रही है। मुझे देखते ही वे मेरी मेंज़ के इर्द-गिर्द बैठ जाते थे। ‘‘You are a quiet Indian, aren’ t you ?’’ ( बाद में उनके बीच मैं लम्बे अर्से तक इसी नाम से प्रसिद्ध रहा) उनकी ऊपर से अनर्गल दीखने वाली आत्मकथाओं में मुझे पहली बार उन अँधेरे कोनों से साक्षात्कार हुआ, जिन्हें मैं छिपाकर रखता आया था। आज मैं जो कुछ हूं उसका एक हिस्सा इन आज्ञात लोगों की देन हैं-जो अब हमेशा के लिए दुनिया के अलग-अलग कोनों में खो गए हैं।
मुझे खुशी हैं, वे इन कहानियों को कभी नहीं पढ़ेंगे।, यदि उन्हें मालूम होता कि उनके साथ रात गुज़ारने वाला ‘कुआयट इण्डियन’ कहानियाँ लिखकर जीवन काटता है, तो उन्हें सचमुच निराशा होती।
दहलीज़
पिछली रात रूनी को लगा कि इतने बरसों बाद कोई पुराना सपना धीमे कदमों से
उनके पास चला आया है., वही बंगला था, अलग कोने में पत्तों से घिरा हुआ
धीरे-धीरे फाटक के भीतर घुसी है..... मौन की अथाह गहराई में लॉन डूबा है
.....शुरू मार्च की वासन्ती हवा घास को सिहरा-सहला जाती है..... बहुत
बरसों पहले के एक रिकार्ड की धुन छतरी के नीचे से आ रही है.... ताश के
पत्ते घास पर बिखरे हैं..... लगता है, जैसे शम्मी भाई अभी खिलखिलाकर हंस
देंगे और आपा (बरसों पहले, जिनका नाम जेली था) बंगले के पिछवाड़े
क्यारियों को खोदती हुई पूछेंगी-रूनी, जरा मेरे हाथों को तो देख, कितने
लाल हो गए हैं !
इतने बरसों बाद रूनी को लगा कि वह बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी बरसों पहले, मार्च के एक दिन की तरह था कुछ भी नहीं बदला, वही बंगला है। मार्च की खुश्क-गरम हवा सांय-सांय करती चली आ रही है, सूनी-सी दुपहर को परदे के रिंग धीमे-धीमे खनखना जाते हैं....और वह घास पर लेटी है.....बस, अब अगर मैं मर जाऊँ, उसने उस घड़ी सोचा था।
लेकिन वह दुपहर ऐसी न थी कि केवल चाहने-भर से कोई मर जाता। लॉन के कोने में तीन पेडो़ का एक झुरमुट, था ऊपर की फुनगियां एक-दूसरे से बार-बार उलझ जाती थीं। हवा चलने से उसके बीच आकांश की नीली फांक कभी मुद जाती थी, कभी खुल जाती थी, बंगले की छत पर लगे एरियल-पोल तार को देखो, (देखो, तो घास पर लेटकर अधमुंदी आँखों से रूनी ऐसे ही देखती है) तो लगता है, जैसे वह हिल रहा है, हौले-हौले ....अनझिप आंखों से देखो, (पलक बिलकुल न मूंदो, चाहे आँखों में आंसू भर जाएं तो भी.....रूनी ऐसे ही देखती है) तो लगता है, जैसे तार बीच में से कटता जा रहा है और दो कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की सतह पर हल्के-हल्के तैरने लगती है।....
इतने बरसों बाद रूनी को लगा कि वह बंगले के सामने खड़ी है और सब कुछ वैसा ही है जैसा कभी बरसों पहले, मार्च के एक दिन की तरह था कुछ भी नहीं बदला, वही बंगला है। मार्च की खुश्क-गरम हवा सांय-सांय करती चली आ रही है, सूनी-सी दुपहर को परदे के रिंग धीमे-धीमे खनखना जाते हैं....और वह घास पर लेटी है.....बस, अब अगर मैं मर जाऊँ, उसने उस घड़ी सोचा था।
लेकिन वह दुपहर ऐसी न थी कि केवल चाहने-भर से कोई मर जाता। लॉन के कोने में तीन पेडो़ का एक झुरमुट, था ऊपर की फुनगियां एक-दूसरे से बार-बार उलझ जाती थीं। हवा चलने से उसके बीच आकांश की नीली फांक कभी मुद जाती थी, कभी खुल जाती थी, बंगले की छत पर लगे एरियल-पोल तार को देखो, (देखो, तो घास पर लेटकर अधमुंदी आँखों से रूनी ऐसे ही देखती है) तो लगता है, जैसे वह हिल रहा है, हौले-हौले ....अनझिप आंखों से देखो, (पलक बिलकुल न मूंदो, चाहे आँखों में आंसू भर जाएं तो भी.....रूनी ऐसे ही देखती है) तो लगता है, जैसे तार बीच में से कटता जा रहा है और दो कटे हुए तारों के बीच आकाश की नीली फांक आंसू की सतह पर हल्के-हल्के तैरने लगती है।....
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i