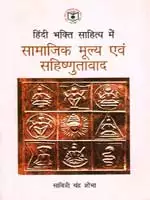|
भाषा एवं साहित्य >> हिन्दी भक्ति साहित्य में सामाजिक मूल्य एवं सहिष्णुतावाद हिन्दी भक्ति साहित्य में सामाजिक मूल्य एवं सहिष्णुतावादसावित्री चंद्र शोभा
|
46 पाठक हैं |
|||||||
इस पुस्तक में मुख्य रूप से हिंदी भक्ति और हिंदी लिखित सूफी प्रेमाख्यानों के माध्यम से मध्यकालीन भारत में ‘सामाजिक और उदारतावादी तत्वों को रेखांकित किया गया है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस पुस्तक में मुख्य रूप से हिंदी भक्ति और हिंदी लिखित सूफी
प्रेमाख्यानों के माध्यम से मध्यकालीन भारत में ‘सामाजिक और
उदारतावादी तत्वों को रेखांकित किया गया है। नामदेव और अमीर खुसरो के
सहिष्णुतावादी उदगारों के परिप्रेक्ष्य में मुल्ला दाऊद, कबीर, रैदास और
सूफी लेखक कुतबन, जायसी और मंझन की कृतियों का विष्लेषण इसी दृष्टिकोण से
किया गया है। नानक को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। मीरा, सूर,
तुलसी की रचनाओं के सामाजिक और सहिष्णुतावादी विचारों के साथ 17वीं -18वीं
शती में सगुण-निर्गुण भक्ति, सूफी प्रेमाख्यानों के साथ रीतिकालीन और
नीतिपरक काव्यों का विश्लेषण नई-दृष्टि से किया गया है। कवियों के
नारी-संबंधी विचारों पर भी नई दृष्टि डाली गई है।
भूमिका
उत्तरी भारत में चौदहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक फैली भक्ति की लहर समाज
के वर्ण, जाति, कुल और धर्म की सीमाएं लांघ कर सारे जनमानस की चेतना में
परिव्याप्त हो गई थी, जिसने एक जन-आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। भक्ति
आंदोलन का एक पक्ष था साधन या भक्त के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति अथवा
भगवान के साथ मिलन, चाहे भगवान का स्वरूप सगुण था या निर्गुण। दूसरा पक्ष
था समाज में स्थित असमानता का। ऊंच-नीच की भावना अथवा एक वर्ण, जाति या
धर्म के लोगों का दूसरे वर्ण व जाति या धर्म के लोगों के प्रति किए गए
अत्याचार, अन्याय और शोषण का विरोध। इस प्रकार संतो ने असहमति और विरोध का
नारा बुलंद किया।
साथ ही निर्गुण संतों ने भक्ति के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण, धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों के खोखलेपन का पर्दाफाश किया और समाज में एकात्मक्ता और भाईचारे की भावना को फैलाने का पुरजोर प्रयत्न किया। समानतावादी व्यवस्था में आस्था रखने वालों में कबीर, दाऊद, रज्जबदास, रैदास, सूरदास आदि आते ही हैं तो साथ ही सिख संप्रदाय के जन्मदाता नानक और उनके संप्रदाय को बढ़ाने वाले सिख गुरु भी शामिल हैं। सूफी धर्म मत से प्रभावित संत और मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और मंझन इत्यादि को भी विस्तृत भक्ति आंदोलन में शामिल रचना उचित है। उनके विचार से प्रेम की पीर के द्वारा अपनी माशूका अर्थात् प्रियतमा के साथ मिलन अर्थात फना हो जाना भगवद् भक्ति का ही दूसरा स्वरूप था।
मध्यकालीन भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता का झंडा लहराने वालों में सबसे पहले कबीर का नाम लिया जाता है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जिनका जन्म और प्रभ्रमण 1260-1350 का माना जाता है। और जिनके अभंग मराठी और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं—धार्मिक सहिष्णुता की उद्घोषणा करते हुए कहते हैं—
हिंदु मंदिर में पूजा करते हैं, मुलमान मस्जिद में, जो (भगवान का) नाम स्मरण करता है वहां न मंदिर है न मस्जिद।
नामदेव गोविंद या विट्ठलदेव के भक्त थे किंतु वे भगवान के लिए राम, विट्ठल, मुरारी, रहीम, करीम आदि नामों से पुकारते हैं।
चौदहवीं सदी में धार्मिक सहिष्णुता का नारा उठाने वालों में अमीर खुसरो का नाम अग्रणी है। यह बात उनके एक ही शेर से स्पष्ट की जा सकती है—
मैं यार (भगवान) क इश्क में काबा में रहूं या मंदिर में। यार (भगवान) के आशिक को (एक को) कुफ्र या (दूसरे को) ईमान कहने का काम नहीं।
दिलचस्प बात यह है कि जहां खुसरो ने ब्रह्मणों की विद्वता, निष्ठा और सादगी की प्रशंसा की है वहीं उन्होंने उल्माओं (मुल्ला का बहुवचन) को लालची, दगाबाज और पाखंडी बताया है।
खुसरो की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन में परिलक्षित होती है। चंदायन की रचना 14वीं सदी के उत्तरार्द्ध में की गई। अपने संरक्षक जौनाशाह जो सुल्तान फ़िरोजशाह तुगलक के वजीर थे, के न्याय की प्रशंसा करते हुए मुल्ला दाऊद कहते हैं कि हिंदू तुरक दुहू सम राखई हिंदुओं और तुर्कों अथवा मुसलमानों को समान मानता था। उसके यहां सिंह और शेर अर्थात् मुसलमान और हिंदू एक घाट पर पानी पीते थे। यही नहीं मुल्ला दाऊद ने पुराण को कुरान के समकक्ष माना है और पहिले चार ख़लीफ़ाओं को पंडित की उपाधि दी है।
इस प्रकार कबीर धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की भावना के जन्मदाता नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस प्रवृत्ति को जन-आंदोलन का रूप प्रदान किया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को अंधविश्वास फैलाने, जात-पांत और ऊंच-नीच का समर्थन करने और थोथा ज्ञान वाले ढोंगी की संज्ञा दी है। उन्होंने सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध असहमति और विरोध की भावना को अपनी व्यंग्य भरी वाणी के द्वारा जनता-जनार्दन तक पहुंचाया।
हिंदू-मुस्लिम भावात्मक एकता की बात इतनी बलवती हो गई थी कि कुतबन, मंझन और जायसी तथा उनके परिवर्ती सूफी कवियों ने एक नई प्रकार की रचनाएं लिखनी शुरू कर दीं। इन रचनाओं में जिन्हें प्रेमाख्यान कहा गया है और जो मसनवी परंपरा पर आधारित थीं, न केवल भक्ति और सूफी भावनाओं और विचारों को मिले-जुले रूप में प्रस्तुत किया गया है किंतु साथ ही हिंदू आचार-विचार, मान्यताओं देवी-देवताओं, संस्कार, उत्सव इत्यादि जिनको कठमुल्ला कुफ्र मानते थे, उदारतापूर्ण तथा संवेदनात्मक रूप में रेखांकित किया गया है।
सूफी कवि इस्लाम में दृढ़ विश्वास रखते थे, किंतु उनके ईश्वर जिसको वे सृजनहार कहते हैं और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कोई विशेष मतभेद नहीं थे। यही नहीं वह प्रेम द्वारा ईश्वर और जीव, आत्मा और परमात्मा के मिलने के आदर्श को भी रोचक रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। वह कुरान के साथ वेद पुरान को भी पवित्र ग्रंथ मानते हैं, और पहले चार खलीफाओं को पंडित की उपाधि देते हैं। इस प्रकार सूफी कवि हिंदू-मुस्लिम सामंजस्य और भाईचारे के दृढ़ समर्थक दिखाई देते हैं।
ये रचनाएं हिंदू और मुस्लिम जनता में लोकप्रिय थीं इसका एक उदाहरण यह है कि जुम्मे की नमाज़ में मीनार से चंदायन के कुछ अंश पढ़ जाते थे। सत्रहवीं सदी के जैन लेखक बनारसीदास ने अर्धकथा में सूफी ग्रंथ मधुमालती और मृगावती पढ़ने का उल्लेख किया है।
निर्गुण और सगुण भक्ति का भेद अस्वीकार करते हुए भी उन्हें अलग-अलग दिखाने की प्राचीन परिपाटी रही है। यहां तक कि नागरी प्रचारिणी सभा के प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास में निर्गुण और सगुण भक्ति साहित्य की समीक्षा अलग-अलग जिल्दों में की गई है। हमने निर्गुण और सगुण भक्ति को समानांतर धाराओं के रूप में देखने का प्रयास किया है।
16वीं सदी में भारत में संक्रमण का काल है। इस काल में निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों अबाध धाराओं के रूप में विकसित होती रही हैं। साथ ही सूफी प्रेमाख्यानक काव्य भी लिखे जाते रहे। इसी काल में नानक ने सिख संप्रदाय की नींव डाली और कबीर, रैदास इत्यादि के विचारों को एक नया स्वरूप दिया। नानक के सहिष्णुतावादी और मनुष्य में भाईचारे और समानता की भावना, और अहंभाव को त्याग कर निराकार ब्रह्म का नाम लेने के महत्त्व को इसी परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया गया है।
16वीं शती की उपर्युक्त धाराओं में कोई टकराव नहीं था। किंतु उन्होंने एक-दूसरे को किस हद तक प्रभावित किया, यह कहना कठिन है। न ही यह हमारी सोच का विषय है।
प्रस्तुत पुस्तक में मीरा, सूर, नानक, दादू और तुलसी के सामाजिक सहिष्णुतावादी और मानवतावादी तत्त्वों का विवेचन किया गया है। सोलहवीं सदी में चैतन्य ने पूर्वी भारत में, और उत्तर भारत में मीरा, सूर और तुलसी ने कृष्ण और राम की रास-लीलाओं और अनन्य भक्ति को ऐसे धरातल पर पहुंचा दिया कि उनकी वाणी आज भी जनमानस को प्रभावित करती है।
मीरा को आमतौर से दो रूपों में देखा जा सकता है—एक पितृसत्तात्मक परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली नारी, और दूसरा कृष्ण के प्रेम में विह्वल नृत्य करने वाली प्रेममार्ग को प्रश्रय देने वाली साध्वी नारी। मीरा पर राजा द्वारा पहरा बिठा देना, ताला जड़ देना ताकि मीरा बाहर न जाए। सास-ननद का लड़ना और ताना देना मीरा का अपना अनुभव था और साथ ही वे स्त्री-जाति की असहाय स्थिति की ओर संकेत करती हैं। मीरा का विद्रोह नारी स्वतंत्रता का प्रतीक था। सामंती कोटिबद्ध समाज की मान्यताओं पर जो जात-पांत के विभाजन पर आधारित थी एक प्रकार की चुनौती थी। मीरा की भक्ति के द्वार चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो खुले हुए थे।
उनके गीतों में धार्मिक ग्रंथों और कर्मकांडों की चर्चा की गई है। मीरा का प्रेम सहज-प्रेम है जिसमें सांप्रदायिकता या संकीर्णता का कहीं स्थान नहीं है। कृष्ण से बिछुड़ने की तड़पन सूफी काव्य में आत्मा रूप या राजा का परमात्मा रूपी परी या राजकुमारी के विरह में तड़पने के समान है।
सूरदास के लिए प्रेम या श्रीकृष्ण की माधुर्य भक्ति जिसमें उनकी लीलाओं का वर्णन है धर्म का सार है। वह सब प्रकार की सामाजिक और नैतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है। एक सच्चे भक्त के लिए वे वर्ण, जाति, या कुल-भेद को महत्त्व नहीं देते। फिर भी सूरदास समाज में वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और उच्च-वर्ण या ब्रह्मणों का शूद्रों या निम्नवर्ण के लोगों के साथ बैठकर भोजन करना, हंस और कौए या लहसुन और कपूर के योग के समान हैं।
सूर ने ब्रज में रहने वाले पशु पालक अहीरों के सादे और निश्छल जीवन तथा उसी क्षेत्र में रहने वाले किसानों के कठिन और अभावग्रस्त जीवन को चित्रित किया है। फिर भी सूरदास ब्रज को प्रेम और आनंद के काल्पनिक लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
सूरदास नारी को काम या वासना का प्रतीक नहीं मानते। वह मुख्यतः कोमलता, प्रेम, भक्ति और संवेदनाओं की मूर्ति है। सूरदास नारी के लिए भक्ति का मार्ग खोलते हैं जिसमें सामाजिक बंधन ढीले पड़ जाते हैं। किंतु मुख्य रूप से सूरदास नारी के लिए पति-सेवा को ही महत्त्व देते हैं।
समाज में एकता और हिंदू-मुसलमानों में समता और भाईचारे के विषय पर नानक और दादू के विचार बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। दादू और तुलसी दोनों का अकबर का समकालीन होना महत्त्वपूर्ण है। जिस तरह अकबर ने सुलह-कुल की नीति प्रतिपादित की, उसी तरह धार्मिक क्षेत्र में दादू ने निर्पख-साधना को प्रस्तुत किया।
उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को दोनों कान, हाथ और आंख बताते हुए उन्हे पखा-पखी छोड़कर एक ब्रह्म की भक्ति में लाने की मंत्रणा दी। आपसी विरोध का कारण उन्होंने दोनों धर्मों के ठेकेदार मुल्लाओं और ब्रह्मणों को बताया। रूढ़िवादी धार्मिक परम्पराओं और बाह्यचारों को छोड़ने के लिए उन्होंने यहां तक कहा कि वह न हिंद है, न मुसलमान, वह तो एक ब्रह्म या रहमान में ही रमते हैं।
तुलसीदास ने समसामयिक सामाजिक परिवेश, जीवन-मूल्य एवं मानदंडों की वास्तविकता पर अपनी रचनाओं से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार दुर्जनों और खलों की बहुसंख्या होने के कारण और उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक श्रेष्ठ राजा की आवाश्यकता होती ही है। साथ ही तुलसी की मान्यता थी कि समाज में अलग-अलग श्रेणियों और जातियों के लोगों में अपने-अपने कार्य धर्मों में लगे रहने और दूसरों के कार्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने से ही समाज में संतुलन स्थापित है। इसलिए वे वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार करते हैं अपितु इसको वे जन्म पर नहीं गुणों के ऊपर आधारित करते हैं। इस कार्य में राजा के साथ संत का भी सहयोग आवश्यक है। संत समाज में नैतिक गुण ही नहीं फैलाते अपितु उनके संसर्ग एवं सदप्रभाव से समाज में सज्जनों का समूह बनता है जो उसमें संतुलन स्थापित करने का एक महत कार्य करता है।
तुलसी की भक्ति पारमार्थिक या पारलौकिक या भौतिक दो स्पष्ट रूपों में अभिव्यक्त हुई है। भक्ति के पारमार्थिक या पारलोकिक रूप को भक्ति का आध्यात्मकि पक्ष भी कहा जा सकता है। भक्ति का लौकिक रूप भक्त पर संत को समाज के अभ्युत्थान के साथ-साथ अच्छे मानव बनने का मार्ग दिखाता है। यही तुलसी का मानवतावाद है।
तुलसी की भक्ति भावना और उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक सच्चे संत का मुख्य धर्म लोगों की सेवा और उनके दुखो का निवारण ही था। राम के दयालु चरित्र और दीन—हीनों के प्रति उनकी गहरी संवेदना के कारण ही अनेक स्थानो पर राम को गरीब-निवाज या बंदी-छोर कहा गया है। जिन वांछनीय गुणों को तुलसी ने श्रेष्ठ-जनों के लिए आवश्यक माना है, वे हैं धर्मनिर्पेक्षता और मानवतावाद।
तुलसी का समाज और समाज में संतुलन रखने के प्रयास ने उनकी नारी संबंधी अवधारणा को भी प्रभावित किया। पुरुषों की तरह समाज में अधम और खल नारियों की संख्या बहुत अधिक थी और उन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक था। यह नियंत्रण मुख्य रूप से मर्यादा पर आश्रित है, जिसके अनुसार उनको सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक नियमों का अतिक्रमण करना अनुचित था।
सत्रहवीं शती से सगुण और निर्गुण भक्ति और सूफी प्रेममार्गी विचारधारा बराबर चलती रही। सगुण भक्ति में तुलसीदास जैसा कोई मूर्धन्य विचारक और कवि तो हमें नहीं मिलता। तथापि वैष्णव भक्ति इतनी उदार थी कि रसखान और अब्दुर्रहीम खानेखाना को कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर भक्ति रस में बहकर अपने उदगार व्यक्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस काल का सगुण भक्ति आंदोलन कितना उदार था हमें इस बात से पता चलता है कि वैष्णव भक्ति की रचना करने वालों से मुसलमानों के साथ यादवेंद्र दास कुम्हार की वार्ता, विष्णुदास छीपी थी वार्ता, सूतार कारीगर की वार्ता, इत्यादि अवर्ण व्यक्तियों के नाम आते हैं।
निर्गुण भक्ति की सहिष्णुतावादी धारा 17वीं शताब्दी के अंत तक गरीबदास, सुंदरदास, धरणीदास, रैदास आदि की रचनाओं में निरंतर अभिव्यक्ति पाती रही। इन संतों की रचनाओं में सहिष्णुतावादी विचारधारा के तहत हिंदू-मुस्लिम एकता पर ही नहीं, वरन मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी-मानवों में एक ही ब्रह्मांश के होने के कारण समता, समानता और बराबरी का होने का भी प्रचार किया।
साथ ही निर्गुण संतों ने भक्ति के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, आर्थिक शोषण, धार्मिक अंधविश्वासों और कर्मकांडों के खोखलेपन का पर्दाफाश किया और समाज में एकात्मक्ता और भाईचारे की भावना को फैलाने का पुरजोर प्रयत्न किया। समानतावादी व्यवस्था में आस्था रखने वालों में कबीर, दाऊद, रज्जबदास, रैदास, सूरदास आदि आते ही हैं तो साथ ही सिख संप्रदाय के जन्मदाता नानक और उनके संप्रदाय को बढ़ाने वाले सिख गुरु भी शामिल हैं। सूफी धर्म मत से प्रभावित संत और मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और मंझन इत्यादि को भी विस्तृत भक्ति आंदोलन में शामिल रचना उचित है। उनके विचार से प्रेम की पीर के द्वारा अपनी माशूका अर्थात् प्रियतमा के साथ मिलन अर्थात फना हो जाना भगवद् भक्ति का ही दूसरा स्वरूप था।
मध्यकालीन भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता का झंडा लहराने वालों में सबसे पहले कबीर का नाम लिया जाता है। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जिनका जन्म और प्रभ्रमण 1260-1350 का माना जाता है। और जिनके अभंग मराठी और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं—धार्मिक सहिष्णुता की उद्घोषणा करते हुए कहते हैं—
हिंदू पूजै देहुरा, मुस्सलमान मसीत।
नामे कोई सेविया, जहं देहुरा न मसीत।।
नामे कोई सेविया, जहं देहुरा न मसीत।।
हिंदु मंदिर में पूजा करते हैं, मुलमान मस्जिद में, जो (भगवान का) नाम स्मरण करता है वहां न मंदिर है न मस्जिद।
नामदेव गोविंद या विट्ठलदेव के भक्त थे किंतु वे भगवान के लिए राम, विट्ठल, मुरारी, रहीम, करीम आदि नामों से पुकारते हैं।
चौदहवीं सदी में धार्मिक सहिष्णुता का नारा उठाने वालों में अमीर खुसरो का नाम अग्रणी है। यह बात उनके एक ही शेर से स्पष्ट की जा सकती है—
मा ब इश्क-ए यार अगर दर किब्ला गर दर बुतकदा
अशिकान-ए-दोस्त रा अज कुफ्र ओ इमान कार नीस्त।
अशिकान-ए-दोस्त रा अज कुफ्र ओ इमान कार नीस्त।
मैं यार (भगवान) क इश्क में काबा में रहूं या मंदिर में। यार (भगवान) के आशिक को (एक को) कुफ्र या (दूसरे को) ईमान कहने का काम नहीं।
दिलचस्प बात यह है कि जहां खुसरो ने ब्रह्मणों की विद्वता, निष्ठा और सादगी की प्रशंसा की है वहीं उन्होंने उल्माओं (मुल्ला का बहुवचन) को लालची, दगाबाज और पाखंडी बताया है।
खुसरो की धार्मिक सहिष्णुता की परंपरा मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन में परिलक्षित होती है। चंदायन की रचना 14वीं सदी के उत्तरार्द्ध में की गई। अपने संरक्षक जौनाशाह जो सुल्तान फ़िरोजशाह तुगलक के वजीर थे, के न्याय की प्रशंसा करते हुए मुल्ला दाऊद कहते हैं कि हिंदू तुरक दुहू सम राखई हिंदुओं और तुर्कों अथवा मुसलमानों को समान मानता था। उसके यहां सिंह और शेर अर्थात् मुसलमान और हिंदू एक घाट पर पानी पीते थे। यही नहीं मुल्ला दाऊद ने पुराण को कुरान के समकक्ष माना है और पहिले चार ख़लीफ़ाओं को पंडित की उपाधि दी है।
इस प्रकार कबीर धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की भावना के जन्मदाता नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस प्रवृत्ति को जन-आंदोलन का रूप प्रदान किया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को अंधविश्वास फैलाने, जात-पांत और ऊंच-नीच का समर्थन करने और थोथा ज्ञान वाले ढोंगी की संज्ञा दी है। उन्होंने सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध असहमति और विरोध की भावना को अपनी व्यंग्य भरी वाणी के द्वारा जनता-जनार्दन तक पहुंचाया।
हिंदू-मुस्लिम भावात्मक एकता की बात इतनी बलवती हो गई थी कि कुतबन, मंझन और जायसी तथा उनके परिवर्ती सूफी कवियों ने एक नई प्रकार की रचनाएं लिखनी शुरू कर दीं। इन रचनाओं में जिन्हें प्रेमाख्यान कहा गया है और जो मसनवी परंपरा पर आधारित थीं, न केवल भक्ति और सूफी भावनाओं और विचारों को मिले-जुले रूप में प्रस्तुत किया गया है किंतु साथ ही हिंदू आचार-विचार, मान्यताओं देवी-देवताओं, संस्कार, उत्सव इत्यादि जिनको कठमुल्ला कुफ्र मानते थे, उदारतापूर्ण तथा संवेदनात्मक रूप में रेखांकित किया गया है।
सूफी कवि इस्लाम में दृढ़ विश्वास रखते थे, किंतु उनके ईश्वर जिसको वे सृजनहार कहते हैं और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कोई विशेष मतभेद नहीं थे। यही नहीं वह प्रेम द्वारा ईश्वर और जीव, आत्मा और परमात्मा के मिलने के आदर्श को भी रोचक रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। वह कुरान के साथ वेद पुरान को भी पवित्र ग्रंथ मानते हैं, और पहले चार खलीफाओं को पंडित की उपाधि देते हैं। इस प्रकार सूफी कवि हिंदू-मुस्लिम सामंजस्य और भाईचारे के दृढ़ समर्थक दिखाई देते हैं।
ये रचनाएं हिंदू और मुस्लिम जनता में लोकप्रिय थीं इसका एक उदाहरण यह है कि जुम्मे की नमाज़ में मीनार से चंदायन के कुछ अंश पढ़ जाते थे। सत्रहवीं सदी के जैन लेखक बनारसीदास ने अर्धकथा में सूफी ग्रंथ मधुमालती और मृगावती पढ़ने का उल्लेख किया है।
निर्गुण और सगुण भक्ति का भेद अस्वीकार करते हुए भी उन्हें अलग-अलग दिखाने की प्राचीन परिपाटी रही है। यहां तक कि नागरी प्रचारिणी सभा के प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास में निर्गुण और सगुण भक्ति साहित्य की समीक्षा अलग-अलग जिल्दों में की गई है। हमने निर्गुण और सगुण भक्ति को समानांतर धाराओं के रूप में देखने का प्रयास किया है।
16वीं सदी में भारत में संक्रमण का काल है। इस काल में निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों अबाध धाराओं के रूप में विकसित होती रही हैं। साथ ही सूफी प्रेमाख्यानक काव्य भी लिखे जाते रहे। इसी काल में नानक ने सिख संप्रदाय की नींव डाली और कबीर, रैदास इत्यादि के विचारों को एक नया स्वरूप दिया। नानक के सहिष्णुतावादी और मनुष्य में भाईचारे और समानता की भावना, और अहंभाव को त्याग कर निराकार ब्रह्म का नाम लेने के महत्त्व को इसी परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत किया गया है।
16वीं शती की उपर्युक्त धाराओं में कोई टकराव नहीं था। किंतु उन्होंने एक-दूसरे को किस हद तक प्रभावित किया, यह कहना कठिन है। न ही यह हमारी सोच का विषय है।
प्रस्तुत पुस्तक में मीरा, सूर, नानक, दादू और तुलसी के सामाजिक सहिष्णुतावादी और मानवतावादी तत्त्वों का विवेचन किया गया है। सोलहवीं सदी में चैतन्य ने पूर्वी भारत में, और उत्तर भारत में मीरा, सूर और तुलसी ने कृष्ण और राम की रास-लीलाओं और अनन्य भक्ति को ऐसे धरातल पर पहुंचा दिया कि उनकी वाणी आज भी जनमानस को प्रभावित करती है।
मीरा को आमतौर से दो रूपों में देखा जा सकता है—एक पितृसत्तात्मक परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली नारी, और दूसरा कृष्ण के प्रेम में विह्वल नृत्य करने वाली प्रेममार्ग को प्रश्रय देने वाली साध्वी नारी। मीरा पर राजा द्वारा पहरा बिठा देना, ताला जड़ देना ताकि मीरा बाहर न जाए। सास-ननद का लड़ना और ताना देना मीरा का अपना अनुभव था और साथ ही वे स्त्री-जाति की असहाय स्थिति की ओर संकेत करती हैं। मीरा का विद्रोह नारी स्वतंत्रता का प्रतीक था। सामंती कोटिबद्ध समाज की मान्यताओं पर जो जात-पांत के विभाजन पर आधारित थी एक प्रकार की चुनौती थी। मीरा की भक्ति के द्वार चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो खुले हुए थे।
उनके गीतों में धार्मिक ग्रंथों और कर्मकांडों की चर्चा की गई है। मीरा का प्रेम सहज-प्रेम है जिसमें सांप्रदायिकता या संकीर्णता का कहीं स्थान नहीं है। कृष्ण से बिछुड़ने की तड़पन सूफी काव्य में आत्मा रूप या राजा का परमात्मा रूपी परी या राजकुमारी के विरह में तड़पने के समान है।
सूरदास के लिए प्रेम या श्रीकृष्ण की माधुर्य भक्ति जिसमें उनकी लीलाओं का वर्णन है धर्म का सार है। वह सब प्रकार की सामाजिक और नैतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है। एक सच्चे भक्त के लिए वे वर्ण, जाति, या कुल-भेद को महत्त्व नहीं देते। फिर भी सूरदास समाज में वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और उच्च-वर्ण या ब्रह्मणों का शूद्रों या निम्नवर्ण के लोगों के साथ बैठकर भोजन करना, हंस और कौए या लहसुन और कपूर के योग के समान हैं।
सूर ने ब्रज में रहने वाले पशु पालक अहीरों के सादे और निश्छल जीवन तथा उसी क्षेत्र में रहने वाले किसानों के कठिन और अभावग्रस्त जीवन को चित्रित किया है। फिर भी सूरदास ब्रज को प्रेम और आनंद के काल्पनिक लोक के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
सूरदास नारी को काम या वासना का प्रतीक नहीं मानते। वह मुख्यतः कोमलता, प्रेम, भक्ति और संवेदनाओं की मूर्ति है। सूरदास नारी के लिए भक्ति का मार्ग खोलते हैं जिसमें सामाजिक बंधन ढीले पड़ जाते हैं। किंतु मुख्य रूप से सूरदास नारी के लिए पति-सेवा को ही महत्त्व देते हैं।
समाज में एकता और हिंदू-मुसलमानों में समता और भाईचारे के विषय पर नानक और दादू के विचार बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। दादू और तुलसी दोनों का अकबर का समकालीन होना महत्त्वपूर्ण है। जिस तरह अकबर ने सुलह-कुल की नीति प्रतिपादित की, उसी तरह धार्मिक क्षेत्र में दादू ने निर्पख-साधना को प्रस्तुत किया।
उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को दोनों कान, हाथ और आंख बताते हुए उन्हे पखा-पखी छोड़कर एक ब्रह्म की भक्ति में लाने की मंत्रणा दी। आपसी विरोध का कारण उन्होंने दोनों धर्मों के ठेकेदार मुल्लाओं और ब्रह्मणों को बताया। रूढ़िवादी धार्मिक परम्पराओं और बाह्यचारों को छोड़ने के लिए उन्होंने यहां तक कहा कि वह न हिंद है, न मुसलमान, वह तो एक ब्रह्म या रहमान में ही रमते हैं।
तुलसीदास ने समसामयिक सामाजिक परिवेश, जीवन-मूल्य एवं मानदंडों की वास्तविकता पर अपनी रचनाओं से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार दुर्जनों और खलों की बहुसंख्या होने के कारण और उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक श्रेष्ठ राजा की आवाश्यकता होती ही है। साथ ही तुलसी की मान्यता थी कि समाज में अलग-अलग श्रेणियों और जातियों के लोगों में अपने-अपने कार्य धर्मों में लगे रहने और दूसरों के कार्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने से ही समाज में संतुलन स्थापित है। इसलिए वे वर्ण-व्यवस्था को स्वीकार करते हैं अपितु इसको वे जन्म पर नहीं गुणों के ऊपर आधारित करते हैं। इस कार्य में राजा के साथ संत का भी सहयोग आवश्यक है। संत समाज में नैतिक गुण ही नहीं फैलाते अपितु उनके संसर्ग एवं सदप्रभाव से समाज में सज्जनों का समूह बनता है जो उसमें संतुलन स्थापित करने का एक महत कार्य करता है।
तुलसी की भक्ति पारमार्थिक या पारलौकिक या भौतिक दो स्पष्ट रूपों में अभिव्यक्त हुई है। भक्ति के पारमार्थिक या पारलोकिक रूप को भक्ति का आध्यात्मकि पक्ष भी कहा जा सकता है। भक्ति का लौकिक रूप भक्त पर संत को समाज के अभ्युत्थान के साथ-साथ अच्छे मानव बनने का मार्ग दिखाता है। यही तुलसी का मानवतावाद है।
तुलसी की भक्ति भावना और उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर कहा जा सकता है कि एक सच्चे संत का मुख्य धर्म लोगों की सेवा और उनके दुखो का निवारण ही था। राम के दयालु चरित्र और दीन—हीनों के प्रति उनकी गहरी संवेदना के कारण ही अनेक स्थानो पर राम को गरीब-निवाज या बंदी-छोर कहा गया है। जिन वांछनीय गुणों को तुलसी ने श्रेष्ठ-जनों के लिए आवश्यक माना है, वे हैं धर्मनिर्पेक्षता और मानवतावाद।
तुलसी का समाज और समाज में संतुलन रखने के प्रयास ने उनकी नारी संबंधी अवधारणा को भी प्रभावित किया। पुरुषों की तरह समाज में अधम और खल नारियों की संख्या बहुत अधिक थी और उन पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक था। यह नियंत्रण मुख्य रूप से मर्यादा पर आश्रित है, जिसके अनुसार उनको सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक नियमों का अतिक्रमण करना अनुचित था।
सत्रहवीं शती से सगुण और निर्गुण भक्ति और सूफी प्रेममार्गी विचारधारा बराबर चलती रही। सगुण भक्ति में तुलसीदास जैसा कोई मूर्धन्य विचारक और कवि तो हमें नहीं मिलता। तथापि वैष्णव भक्ति इतनी उदार थी कि रसखान और अब्दुर्रहीम खानेखाना को कृष्ण भक्ति में सराबोर होकर भक्ति रस में बहकर अपने उदगार व्यक्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस काल का सगुण भक्ति आंदोलन कितना उदार था हमें इस बात से पता चलता है कि वैष्णव भक्ति की रचना करने वालों से मुसलमानों के साथ यादवेंद्र दास कुम्हार की वार्ता, विष्णुदास छीपी थी वार्ता, सूतार कारीगर की वार्ता, इत्यादि अवर्ण व्यक्तियों के नाम आते हैं।
निर्गुण भक्ति की सहिष्णुतावादी धारा 17वीं शताब्दी के अंत तक गरीबदास, सुंदरदास, धरणीदास, रैदास आदि की रचनाओं में निरंतर अभिव्यक्ति पाती रही। इन संतों की रचनाओं में सहिष्णुतावादी विचारधारा के तहत हिंदू-मुस्लिम एकता पर ही नहीं, वरन मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी-मानवों में एक ही ब्रह्मांश के होने के कारण समता, समानता और बराबरी का होने का भी प्रचार किया।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i