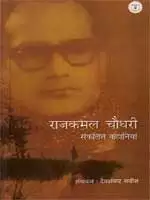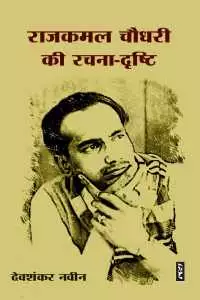|
कहानी संग्रह >> राजकमल चौधरी संकलित कहानियाँ राजकमल चौधरी संकलित कहानियाँदेवशंकर नवीन
|
288 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत हैं राजकमल चौधरी की संकलित कहानियाँ
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
हिन्दी में राजकमल चौधरी (13.12.1929 से 19.06.1967) की रचनाएं छठे दशक के
उत्तरार्ध में, अर्थात प्रकाश में आते ही चकाचौंध पैदा करने लगी थीं। उनकी
पहली हिन्दी कविता (बरसात रात प्रभात) सितंबर 1956 में ‘नई
धारा’ में पहली कहानी (सती धनुकराइन) मार्च 1958 में
‘कहानी’ में और पहला निबन्ध (भारतीय कला में सौन्दर्य- भावना)
जून 1959 में ज्ञानोदय में प्रकाशित हुआ। मैथिली में सन् 1954 से ही उनकी
रचनाएं छपने लगी थीं। सन् 1958 आते- आते वहां वे ख्यात तो हो ही चुके थे,
मैथिली की रुग्ण जर्जर एवं रूढ़िग्रस्त रचनाशीलता के लिए चुनौती बने रहे।
लेकिन, अप्रकाशित पांडुलिपियों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि सन्
1949-50 के आस-पास से ही वे सृजन में पर्याप्त सक्रिय थे। हिन्दी में उन
दिनों की उनकी अनेक रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि
हिन्दी में आने से पहले ही उनकी रचनात्मकता पर्याप्त समृद्ध हो चुकी थी।
हिन्दी और मैथिली-दोनों भाषाओं में लिखी-छपी उनकी रचनाओं में छठे दशक की सामाजिक रूढियों, पाखंडों, धर्माधताओं, कुरीतियों, अत्याचारों, राजनीतिक षड्यत्रों और बहुसंख्य साधारण जन के साथ किए जा रहे प्रवंचन, प्रपंच, धोखाधड़ी आदि के संबंध में उनकी नजर सावधान दिखती है। उनके लिए ऐसी एक भी हरकत सह्य नहीं थी, जिसकी परिणति जनहित से अलगाव रख रही हो। जनविरोधी उपक्रमों का विरोध उन्होंने ताऊम्र किसी एक्टिविस्ट की तरह किया; शुद्ध साहित्यिक लेखक की तरह कहानी, कविता, निबंध लिखकर अपना दायित्व पूर्ण समझ लेने वालों की सूची में उन्होंने अपने को सीमित नहीं रखा।
गागर में सागर भरने वाली राजकमल चौधरी की सारी कहानियां सन् 1967 से पहले ही लिखी गईं, मगर आज भी अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित करती हैं, और विमर्श की नई व्याख्याएं आमंत्रित करती हैं। नारी लेखन और नारी जीवन पर विश्व-साहित्य में आज जितनी भी बहसें हो रही हैं, उसके बहुत सारे संकेत राजकमल चौधरी के कथा लेखन में चार-पांच दशक पूर्व से मौजूद हैं। पुरुष मनोवृत्ति के बरक्स, स्त्री जीवन के इतने सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता हमें उन्हीं दिनों महसूस करनी चाहिए थी।
राजकमल चौधरी का संपूर्ण लेखन (कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, नाटक, पत्र, डायरी...) मानव जीवन की बुनियादी शर्त पर टिका है। उन्होंने मानव जीवन की तीन ही आदम प्रवृत्तियां स्वीकार कीं-आत्म बुभुक्षा, यौन पिपासा, आत्म सुरक्षा, अर्थात् रोटी सेक्स सुरक्षा। इन तीनों की पूर्ति में मनुष्य मर्यादा तोड़ता है, असभ्य और जंगली हो जाता है। इसके पटल एक बिंदु और है कि मनुष्य शक्ति चाहता है-पावर। भारतीय स्वाधीनता के गत साठ वर्षों में, और राजकमल चौधरी की मृत्यु तक के समय को लें तो कुल बीस वर्षों में इस पावर की व्याख्या मनुष्य को भ्रमित करती रही। मनुष्य का ‘पावर’ क्या है पैसा, पद, स्त्री, बंगला, गाड़ी, गद्दी क्या है मनुष्य का पावर ? एक से एक तानाशाह पल भर का उन्माद मिटाने के लिए अपने मातहत स्त्री के सामने घुटने टेक देता है, नंगा हो जाता है; पैसे कमाने के लिए ईमान और इज्जत बेच आता है। फिर पैसा कमाकर इज्जतदार बनना चाहता है। राजकमल चौधरी का जीवन-दर्शन इस सूत्र में भी झलकता है कि मनुष्य सब कुछ बेचकर पैसा खरीदता है और पैसे ले सब कुछ खरीद लेना चाहता है।
उनका नायक खरीद पाता है या नहीं-यह और बात है, इच्छा पूरी हो या न हो, मूल बात है कि वह इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसे ही नायकों, उपनायकों की रचना उनके साहित्य का अहम् हिस्सा है, और संभवतः इसी कारण ऐसे नायक के सर्जक को स्वेच्छाचारी कहा जाने लगा। वस्तुतः यह स्वेच्छाचार नहीं है। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि मनुष्य योनि की पहली अभिलाषा जिजीविषा है, अर्थात् जीने की इच्छा। और जीवन जीने की पहली शर्त है रोटी।....यह बात मान लेने की है कि भूख में निर्णय लेने की बड़ी ताकत होती है। भूखा व्यक्ति पाप-पुण्य की परिभाषा जानने की इच्छा नहीं रखता, उसके जीवन की प्रथम और परम नैतिकता रोटी होती है। स्वाधीनता के बाद के उन बीस वर्षों की वह कैसी नैतिकता रही होगी, जब किसी स्त्री को अपनी या अपने बाल-बच्चों की भूख मिटाने, तन ढकने के लिए किसी अनचाहे मर्द के सामने अपना तन उघारने को मजबूर होना पड़ता होगा। ...इसके ठीक विपरीत, वैसी स्त्री की मनोदशा भी याद रखने की है, जिसके मर्द पैसा बनाने के कार्यक्रमों में व्यस्त, अपनी जवान पत्नी बहन-बेटी के मनोभावों और उत्तेजनाओं से निरपेक्ष रहता होगा, खुद किराए के बिस्तरों की तलाश में लिप्त रहता होगा, और उसके घर की स्त्रियां पड़ोस में गिगोलो की तलाश करती होंगी। देह से अर्थोपार्जन और अर्थ बल से देह के सौदा का यह गोरखधंधा स्वाधीनता के बाद जिस चरम पर था, आज उससे कहीं ज्यादा है मगर यह सत्य है कि सामाजिक ढांचा उस समय ऐसा नहीं था। जीवन की इस विद्रूप परिस्थिति को राजकमल चौधरी ने सूक्ष्मता से पकड़ा।
भारत की जिस आजादी में सामान्य नागरिक का अस्तित्व संकटग्रस्त रहे, जिजीविषा खतरे में रहे; मान-स्वाभिमान, लालसा-अभिलाषा तो दूर, जीवन रक्षा की पहली जरूरत रोटी तक ठीक से उपलब्ध नहीं हो, उसके लिए कौन-सी नैतिकता कामयाब होगी ? अपनी कहानियों, कविताओं में राजकमल चौधरी ने जीवन के इसी मर्म को पकड़ने की सफलतम कोशिश की है। यहां एक बात गंभीरता से देखने की है कि मानव जीवन की महत्वपूर्ण क्रिया यौनाचार, सृष्टि का कारण है, मगर उनकी कहानियों में इस घटना का उल्लेख हर जगह शुद्ध व्यापार के रूप में हुआ है, इस क्रिया में लिप्त व्यक्ति कामगार की भूमिका में है, जैसे फैक्ट्री में जूता बनाता हुआ कारीगर, जूता नहीं बनाता है, जूता बनाते वक्त वह पैसा कमा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि एक जोड़े जूते तैयार करने के कितने पैसे मिलेंगे। इन दिनों एक शब्द प्रचलन में आया है यौनकर्मी (सेक्स वर्कर) यह शब्द अपने कोशीय अर्थ की पूरी दुनिया के साथ राजकमल चौधरी की कहानियों में है। यौनकर्म में लिप्त इनकी कहानियों के पात्र एक ही क्षण; एक ही कर्म में अलग-अलग जीवन जीते हैं। जिस देश का लोकतंत्र, नागरिक के जीवन में भूख मिटाने के लिए टुकड़ा भर सूखी रोटी और सो जाने के लिए बित्ते भर बिस्तर भी उपलब्ध न करा पाए उस देश की आजादी किस काम की ? राजकमल चौधरी की कहानियां, अपने तमाम समकालीन कहानियों के साथ इसी विडंबना का चार्ट बना रही थी। कागज पर लिखी हुई आजादी, या नारेबाजी की आजादी में उस समय के कथाकारों की कोई दिलचस्पी नहीं थी।
आजादी के बाद भारतीय समाज में पनपी कुछ दुरवस्थाओं, सियासी तिकड़मों, ठगे हुए नागरिकों की निराशाओं, आजादी के जश्न में मसरूफ राजनेताओं, राजनीतिक, मोहभंग, सीमा संघर्ष और पड़ोसी राष्ट्र की धोखेबाजी का चित्रण हिन्दी के रचनाकारों के लिए ज्वलन्त विषय रहे हैं। भारत का नागरिक जीवन बेतरह परेशान था। जीवन की बुनियादी सुविधा जुटाने में बदहबास नागरिक को मुश्किल से जुटाई हुई सुविधा भोग पाने की स्थिति नहीं दी जा रही थी। जीवन का यही त्रासद क्षण उसे नकार से भर रहा था, वह समाज व्यवस्था द्वारा निर्मित आचार संहिता को क्रूरता से कुचल डालना चाहता था। अभाव, उपेक्षा, दमन, शोषण, पराजय, अपमान, अलमूल्यन...से प्रताड़ित आजादी के बाद का नायक हिन्दी कहानी में कभी प्रतिक्रियावादी की तरह, कभी आन्दोलनकारी की तरह, कभी व्यथित पराजित समझौतावादी की तरह, कभी नकार भाव से परे स्वेच्छाकारी की तरह उपस्थित होता रहा।
स्वाधीन भारत का मनुष्य, सांस भर जिंदगी, पेट भर अन्न, लिप्सा भर प्यार, लाज भर वस्त्र प्राण भर सुरक्षा अर्थात् तिनका भर अभिलाषा की पूर्ति के लिए, धरती के इस छोरे से उस छोरे तक बेतहाशा भागता और निरंतर संघर्ष करता रहता है। जीवन और जीवन की इन्हीं आदिम आवश्यकताओं रोटी-सेक्स-सुरक्षा, प्रेम-प्रतिष्ठा-ऐश्वर्य, बल-बुद्धि-पराक्रम के इंतजाम में जुटा रहता है। इसी इंतजाम में कोई शेर और भेड़िया हो जाता है, जो अपनी सफलता के लिए दूसरों को खा जाता है; और कोई भेड़-बकरा-हिरण-खरगोश हो जाता है, जो शक्तिवानों के लिए आहार और उपकरण भर होकर रह जाता है। राजकमल चौधरी की रचनाएं समाज और व्यक्ति के जीवन में आ रहे ऐसे परिवर्तनों मशीन और मशीनीकरण, पश्चिमी देशों और पश्चिमी व्यवसायों, संस्कृतियों से प्रभावित संचालित आधुनिक भारतीय समाज और सभ्यता के जीवन संग्राम की अंदरूनी कथा कहती हैं। सुखानुभूति, जुगुप्सा और क्रोध-तमाम रचनाओं में ये तीन परिणतियां पाठकों के सामने बार-बार आती है। स्वातंत्र्योत्तर काल के भारत की जनता, सत्ता और जनतंत्र की कई गुत्थियां इनके यहां खोली गई हैं। कहा जाना चाहिए कि राजमकल चौधरी की रचनाएं आधुनिक सभ्यता की विकासमान दानवता के जबड़े में निरीह बैठे जनमानस को झकझोरने और उसे अपनी इस ताकत की याद दिलाने का गीत है, जिसे व्यवस्था की चकाचौंध रोशनी में या बेतहाशा शोरगुल में, जनता भूल गई है। भाषा में खिन्न और नाराज तेवरों के बावजूद सामाजिक अवसाद के सारे पहलुओं पर अत्यंत सावधान आयास यहां प्राप्त हैं।
स्वातंत्र्योत्तर काल में सत्ता की चमक-दमक में बड़े-बड़े सूरमाओं की आंखें चौंधियाने लगी थीं। तात्कालिक लाभ और चमत्कारिक उन्नति, बैभव-साधन, सुख-संपदा की प्राप्ति की लालसा में निरक्षर, साक्षर, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग सब सम्मोहित होने लगे और सत्ता की गलियों में भटकने लगे। समाज का व्यवस्था विखंडन हुआ, रूढ़िग्रस्त परंपराओं का निर्वाह करने वाला एक वर्ग अपने जातीय संस्कारों में उलझा रहा, श्रम और श्रमजीवी को हेय समझना उसके अहं का पर्याय-सा बन चुका था। संचित एवं स्थायी संपदाओं को बेचकर-खाना-भोगना उसके जीवनयापन की मजबूरी हो गई। रूढ़िग्रस्त जन्मजात संस्कारों की वजह से यह वर्ग श्रम एवं श्रमजीवियों के करीब जाने से कतराता था, और अपनी अक्षमता के कारण ऊपर वाले वर्ग में अपने को समाहित कर नहीं पा रहा था।
आजादी से मोहभंग भारतीय समाज की बड़ी और ऐतिहासिक घटना है। समतामूलक समाज का स्वरूप पूरा न होने से बेकारी- बरोजगारी, भूख-अभाव के सृजन का एक विशाल तंत्र बढ़ रहा था। नागरिक की दशा यह थी कि
सिर्फ अपनी बीवी
और सिर्फ अपनी दो सौ चालीस की नौकरी
बांधती थी उसे
अपने नागरिक व्यूह में
देश में नागरिक की इच्छा -आकांक्षा का कोई मतलब नहीं था। ऐसे में यदि राजकमल चौधरी का पात्र अंधेरे से ऊबते हुए कहता है कि ‘उजाला मैं भी नहीं मांगता हूं, मांगने से मिल सकेगा, मुझे विश्वास नहीं...उजाला तो एक स्थिति है, जिसे लाने के लिए अंधेरे की स्थितियों के खिलाफ जेहाद करना पड़ता है। मुझसे संभव नहीं है, यह जेहाद, क्रूसेड, मेरी तलवार की मूंठ टूटी हुई है, मेरे जिरह बख्तर को जंग के कीड़े खा गए हैं (देहगाथा/भूमिका) तो पूरे देश की अराजक स्थिति और अभाव अनाचार के अंधेरे में भटक रहे दिशाहारा भारतीय नागरिक की दशा स्पष्ट हो उठती है।
स्वाधीनता के कुछ वर्षों बाद स्थिति और भी नाजुक हो गई। सत्तासीन क्रूर विदेशी को विस्थापित कर गद्दी पर काबिज हुए भारतीयों की स्वार्थी नीतियों के कारण राजनीतिक पार्टियों की आतंरकि दशा बिगड़ने लगी। राजनीतिक दलों के अंतसंघर्ष स्वार्थों के टकराव और एक ही संसाधन पर लालायित होकर आक्रमण करने की हरकतों से बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेत-नियम भी संदिग्ध दिखने लगे। जनता समझने लगी कि साधारण जनता के हित की चिंता न तो सत्ताधारियों को है, न सत्ता विरोधियों को। यूनियनबाजी से लेकर जुलूस-नारा आंदोलन यहां तक कि लाठीचार्ज की हरकत तक में राजनीतिक पार्टियां ‘स्व’ के आस-पास घूमती हैं।
हिन्दी और मैथिली-दोनों भाषाओं में लिखी-छपी उनकी रचनाओं में छठे दशक की सामाजिक रूढियों, पाखंडों, धर्माधताओं, कुरीतियों, अत्याचारों, राजनीतिक षड्यत्रों और बहुसंख्य साधारण जन के साथ किए जा रहे प्रवंचन, प्रपंच, धोखाधड़ी आदि के संबंध में उनकी नजर सावधान दिखती है। उनके लिए ऐसी एक भी हरकत सह्य नहीं थी, जिसकी परिणति जनहित से अलगाव रख रही हो। जनविरोधी उपक्रमों का विरोध उन्होंने ताऊम्र किसी एक्टिविस्ट की तरह किया; शुद्ध साहित्यिक लेखक की तरह कहानी, कविता, निबंध लिखकर अपना दायित्व पूर्ण समझ लेने वालों की सूची में उन्होंने अपने को सीमित नहीं रखा।
गागर में सागर भरने वाली राजकमल चौधरी की सारी कहानियां सन् 1967 से पहले ही लिखी गईं, मगर आज भी अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित करती हैं, और विमर्श की नई व्याख्याएं आमंत्रित करती हैं। नारी लेखन और नारी जीवन पर विश्व-साहित्य में आज जितनी भी बहसें हो रही हैं, उसके बहुत सारे संकेत राजकमल चौधरी के कथा लेखन में चार-पांच दशक पूर्व से मौजूद हैं। पुरुष मनोवृत्ति के बरक्स, स्त्री जीवन के इतने सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता हमें उन्हीं दिनों महसूस करनी चाहिए थी।
राजकमल चौधरी का संपूर्ण लेखन (कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, नाटक, पत्र, डायरी...) मानव जीवन की बुनियादी शर्त पर टिका है। उन्होंने मानव जीवन की तीन ही आदम प्रवृत्तियां स्वीकार कीं-आत्म बुभुक्षा, यौन पिपासा, आत्म सुरक्षा, अर्थात् रोटी सेक्स सुरक्षा। इन तीनों की पूर्ति में मनुष्य मर्यादा तोड़ता है, असभ्य और जंगली हो जाता है। इसके पटल एक बिंदु और है कि मनुष्य शक्ति चाहता है-पावर। भारतीय स्वाधीनता के गत साठ वर्षों में, और राजकमल चौधरी की मृत्यु तक के समय को लें तो कुल बीस वर्षों में इस पावर की व्याख्या मनुष्य को भ्रमित करती रही। मनुष्य का ‘पावर’ क्या है पैसा, पद, स्त्री, बंगला, गाड़ी, गद्दी क्या है मनुष्य का पावर ? एक से एक तानाशाह पल भर का उन्माद मिटाने के लिए अपने मातहत स्त्री के सामने घुटने टेक देता है, नंगा हो जाता है; पैसे कमाने के लिए ईमान और इज्जत बेच आता है। फिर पैसा कमाकर इज्जतदार बनना चाहता है। राजकमल चौधरी का जीवन-दर्शन इस सूत्र में भी झलकता है कि मनुष्य सब कुछ बेचकर पैसा खरीदता है और पैसे ले सब कुछ खरीद लेना चाहता है।
उनका नायक खरीद पाता है या नहीं-यह और बात है, इच्छा पूरी हो या न हो, मूल बात है कि वह इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसे ही नायकों, उपनायकों की रचना उनके साहित्य का अहम् हिस्सा है, और संभवतः इसी कारण ऐसे नायक के सर्जक को स्वेच्छाचारी कहा जाने लगा। वस्तुतः यह स्वेच्छाचार नहीं है। मानव सभ्यता का इतिहास गवाह है कि मनुष्य योनि की पहली अभिलाषा जिजीविषा है, अर्थात् जीने की इच्छा। और जीवन जीने की पहली शर्त है रोटी।....यह बात मान लेने की है कि भूख में निर्णय लेने की बड़ी ताकत होती है। भूखा व्यक्ति पाप-पुण्य की परिभाषा जानने की इच्छा नहीं रखता, उसके जीवन की प्रथम और परम नैतिकता रोटी होती है। स्वाधीनता के बाद के उन बीस वर्षों की वह कैसी नैतिकता रही होगी, जब किसी स्त्री को अपनी या अपने बाल-बच्चों की भूख मिटाने, तन ढकने के लिए किसी अनचाहे मर्द के सामने अपना तन उघारने को मजबूर होना पड़ता होगा। ...इसके ठीक विपरीत, वैसी स्त्री की मनोदशा भी याद रखने की है, जिसके मर्द पैसा बनाने के कार्यक्रमों में व्यस्त, अपनी जवान पत्नी बहन-बेटी के मनोभावों और उत्तेजनाओं से निरपेक्ष रहता होगा, खुद किराए के बिस्तरों की तलाश में लिप्त रहता होगा, और उसके घर की स्त्रियां पड़ोस में गिगोलो की तलाश करती होंगी। देह से अर्थोपार्जन और अर्थ बल से देह के सौदा का यह गोरखधंधा स्वाधीनता के बाद जिस चरम पर था, आज उससे कहीं ज्यादा है मगर यह सत्य है कि सामाजिक ढांचा उस समय ऐसा नहीं था। जीवन की इस विद्रूप परिस्थिति को राजकमल चौधरी ने सूक्ष्मता से पकड़ा।
भारत की जिस आजादी में सामान्य नागरिक का अस्तित्व संकटग्रस्त रहे, जिजीविषा खतरे में रहे; मान-स्वाभिमान, लालसा-अभिलाषा तो दूर, जीवन रक्षा की पहली जरूरत रोटी तक ठीक से उपलब्ध नहीं हो, उसके लिए कौन-सी नैतिकता कामयाब होगी ? अपनी कहानियों, कविताओं में राजकमल चौधरी ने जीवन के इसी मर्म को पकड़ने की सफलतम कोशिश की है। यहां एक बात गंभीरता से देखने की है कि मानव जीवन की महत्वपूर्ण क्रिया यौनाचार, सृष्टि का कारण है, मगर उनकी कहानियों में इस घटना का उल्लेख हर जगह शुद्ध व्यापार के रूप में हुआ है, इस क्रिया में लिप्त व्यक्ति कामगार की भूमिका में है, जैसे फैक्ट्री में जूता बनाता हुआ कारीगर, जूता नहीं बनाता है, जूता बनाते वक्त वह पैसा कमा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि एक जोड़े जूते तैयार करने के कितने पैसे मिलेंगे। इन दिनों एक शब्द प्रचलन में आया है यौनकर्मी (सेक्स वर्कर) यह शब्द अपने कोशीय अर्थ की पूरी दुनिया के साथ राजकमल चौधरी की कहानियों में है। यौनकर्म में लिप्त इनकी कहानियों के पात्र एक ही क्षण; एक ही कर्म में अलग-अलग जीवन जीते हैं। जिस देश का लोकतंत्र, नागरिक के जीवन में भूख मिटाने के लिए टुकड़ा भर सूखी रोटी और सो जाने के लिए बित्ते भर बिस्तर भी उपलब्ध न करा पाए उस देश की आजादी किस काम की ? राजकमल चौधरी की कहानियां, अपने तमाम समकालीन कहानियों के साथ इसी विडंबना का चार्ट बना रही थी। कागज पर लिखी हुई आजादी, या नारेबाजी की आजादी में उस समय के कथाकारों की कोई दिलचस्पी नहीं थी।
आजादी के बाद भारतीय समाज में पनपी कुछ दुरवस्थाओं, सियासी तिकड़मों, ठगे हुए नागरिकों की निराशाओं, आजादी के जश्न में मसरूफ राजनेताओं, राजनीतिक, मोहभंग, सीमा संघर्ष और पड़ोसी राष्ट्र की धोखेबाजी का चित्रण हिन्दी के रचनाकारों के लिए ज्वलन्त विषय रहे हैं। भारत का नागरिक जीवन बेतरह परेशान था। जीवन की बुनियादी सुविधा जुटाने में बदहबास नागरिक को मुश्किल से जुटाई हुई सुविधा भोग पाने की स्थिति नहीं दी जा रही थी। जीवन का यही त्रासद क्षण उसे नकार से भर रहा था, वह समाज व्यवस्था द्वारा निर्मित आचार संहिता को क्रूरता से कुचल डालना चाहता था। अभाव, उपेक्षा, दमन, शोषण, पराजय, अपमान, अलमूल्यन...से प्रताड़ित आजादी के बाद का नायक हिन्दी कहानी में कभी प्रतिक्रियावादी की तरह, कभी आन्दोलनकारी की तरह, कभी व्यथित पराजित समझौतावादी की तरह, कभी नकार भाव से परे स्वेच्छाकारी की तरह उपस्थित होता रहा।
स्वाधीन भारत का मनुष्य, सांस भर जिंदगी, पेट भर अन्न, लिप्सा भर प्यार, लाज भर वस्त्र प्राण भर सुरक्षा अर्थात् तिनका भर अभिलाषा की पूर्ति के लिए, धरती के इस छोरे से उस छोरे तक बेतहाशा भागता और निरंतर संघर्ष करता रहता है। जीवन और जीवन की इन्हीं आदिम आवश्यकताओं रोटी-सेक्स-सुरक्षा, प्रेम-प्रतिष्ठा-ऐश्वर्य, बल-बुद्धि-पराक्रम के इंतजाम में जुटा रहता है। इसी इंतजाम में कोई शेर और भेड़िया हो जाता है, जो अपनी सफलता के लिए दूसरों को खा जाता है; और कोई भेड़-बकरा-हिरण-खरगोश हो जाता है, जो शक्तिवानों के लिए आहार और उपकरण भर होकर रह जाता है। राजकमल चौधरी की रचनाएं समाज और व्यक्ति के जीवन में आ रहे ऐसे परिवर्तनों मशीन और मशीनीकरण, पश्चिमी देशों और पश्चिमी व्यवसायों, संस्कृतियों से प्रभावित संचालित आधुनिक भारतीय समाज और सभ्यता के जीवन संग्राम की अंदरूनी कथा कहती हैं। सुखानुभूति, जुगुप्सा और क्रोध-तमाम रचनाओं में ये तीन परिणतियां पाठकों के सामने बार-बार आती है। स्वातंत्र्योत्तर काल के भारत की जनता, सत्ता और जनतंत्र की कई गुत्थियां इनके यहां खोली गई हैं। कहा जाना चाहिए कि राजमकल चौधरी की रचनाएं आधुनिक सभ्यता की विकासमान दानवता के जबड़े में निरीह बैठे जनमानस को झकझोरने और उसे अपनी इस ताकत की याद दिलाने का गीत है, जिसे व्यवस्था की चकाचौंध रोशनी में या बेतहाशा शोरगुल में, जनता भूल गई है। भाषा में खिन्न और नाराज तेवरों के बावजूद सामाजिक अवसाद के सारे पहलुओं पर अत्यंत सावधान आयास यहां प्राप्त हैं।
स्वातंत्र्योत्तर काल में सत्ता की चमक-दमक में बड़े-बड़े सूरमाओं की आंखें चौंधियाने लगी थीं। तात्कालिक लाभ और चमत्कारिक उन्नति, बैभव-साधन, सुख-संपदा की प्राप्ति की लालसा में निरक्षर, साक्षर, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग सब सम्मोहित होने लगे और सत्ता की गलियों में भटकने लगे। समाज का व्यवस्था विखंडन हुआ, रूढ़िग्रस्त परंपराओं का निर्वाह करने वाला एक वर्ग अपने जातीय संस्कारों में उलझा रहा, श्रम और श्रमजीवी को हेय समझना उसके अहं का पर्याय-सा बन चुका था। संचित एवं स्थायी संपदाओं को बेचकर-खाना-भोगना उसके जीवनयापन की मजबूरी हो गई। रूढ़िग्रस्त जन्मजात संस्कारों की वजह से यह वर्ग श्रम एवं श्रमजीवियों के करीब जाने से कतराता था, और अपनी अक्षमता के कारण ऊपर वाले वर्ग में अपने को समाहित कर नहीं पा रहा था।
आजादी से मोहभंग भारतीय समाज की बड़ी और ऐतिहासिक घटना है। समतामूलक समाज का स्वरूप पूरा न होने से बेकारी- बरोजगारी, भूख-अभाव के सृजन का एक विशाल तंत्र बढ़ रहा था। नागरिक की दशा यह थी कि
सिर्फ अपनी बीवी
और सिर्फ अपनी दो सौ चालीस की नौकरी
बांधती थी उसे
अपने नागरिक व्यूह में
देश में नागरिक की इच्छा -आकांक्षा का कोई मतलब नहीं था। ऐसे में यदि राजकमल चौधरी का पात्र अंधेरे से ऊबते हुए कहता है कि ‘उजाला मैं भी नहीं मांगता हूं, मांगने से मिल सकेगा, मुझे विश्वास नहीं...उजाला तो एक स्थिति है, जिसे लाने के लिए अंधेरे की स्थितियों के खिलाफ जेहाद करना पड़ता है। मुझसे संभव नहीं है, यह जेहाद, क्रूसेड, मेरी तलवार की मूंठ टूटी हुई है, मेरे जिरह बख्तर को जंग के कीड़े खा गए हैं (देहगाथा/भूमिका) तो पूरे देश की अराजक स्थिति और अभाव अनाचार के अंधेरे में भटक रहे दिशाहारा भारतीय नागरिक की दशा स्पष्ट हो उठती है।
स्वाधीनता के कुछ वर्षों बाद स्थिति और भी नाजुक हो गई। सत्तासीन क्रूर विदेशी को विस्थापित कर गद्दी पर काबिज हुए भारतीयों की स्वार्थी नीतियों के कारण राजनीतिक पार्टियों की आतंरकि दशा बिगड़ने लगी। राजनीतिक दलों के अंतसंघर्ष स्वार्थों के टकराव और एक ही संसाधन पर लालायित होकर आक्रमण करने की हरकतों से बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेत-नियम भी संदिग्ध दिखने लगे। जनता समझने लगी कि साधारण जनता के हित की चिंता न तो सत्ताधारियों को है, न सत्ता विरोधियों को। यूनियनबाजी से लेकर जुलूस-नारा आंदोलन यहां तक कि लाठीचार्ज की हरकत तक में राजनीतिक पार्टियां ‘स्व’ के आस-पास घूमती हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i