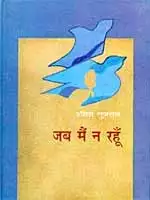|
कविता संग्रह >> जब मैं न रहूँ जब मैं न रहूँशीला गुजराल
|
204 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत कविता संग्रह में अतिवादों की वर्जना तो है ही,जीवन के सहज स्वस्थ रूप का स्वीकार भी है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
हिन्दी, पंजाबी और अँग्रेजी में समान रूप से लिखनेवाली प्रतिष्ठित
कवि-कथाकार श्रीमती शीला गुजराल की कविताओं का यह चौदहवाँ कविता संग्रह
है जब मैं न रहूँ, हिन्दी में आठवाँ। उनके पिछले संग्रहों की कविताओं से
इस संग्रह की कविताएँ कुछ भिन्न प्रकृति की हैं-शिल्प और अर्थ-विस्तार
दोनों ही दृष्टियों से, और निस्सन्देह काव्य की सौन्दर्यश्री, प्रभूत
कल्पना, भाव-सम्पदा और परिवेश की उपलब्धियों का समर्थ प्रतिनिधित्व करती
हैं। जब मैं न रहूँ की कविताओं में अतिवादों की वर्जना तो है ही, जीवन के
सहज स्वस्थ रूप का स्वीकार भी है। इन कविताओं में नवीन और प्राचीन भावना
और विज्ञान, अध्यात्म और भौतिकता तथा राजनीति और संस्कृति के बहुआयामी
यथार्थ को कलात्मक अभिव्यक्ति मिली है। राग-विराग, हर्ष और अवसाद को पूरी
हार्दिकता और सार्थकता के साथ शब्द देने वाली इन कविताओं को पढ़ना
काव्यप्रेमी पाठकों को निस्सन्देह आश्वस्त करेगा।
आत्म-निवेदन
किसी भी यात्रा पर बाहर निकलते समय कुछ विशेष
हिदायतें
देकर जाना हर गृहिणी के लिए स्वाभाविक ही है, और मैं नियमित रूप से ऐसा
करती आयी हूँ...
अचानक मन में विचार कौंधा कि आगामी सूचना मिले बिना यदि अन्तिम यात्रा के लिए प्रस्थान करना पड़ा तो अनुजों के लिए विदा-सन्देश देने का अवसर कब मिलेगा ?...
वैसे तो जिन्दगी का कारवाँ स्वमेव चलता रहता है। मेरे-जैसे सहस्रों सामान्य जन प्रति पल इस संसार से विदा लेते हैं। पर स्वभाव-वश मैं अपने मन से अन्तिम सन्देश का प्रलोभन निकाल नहीं पायी।...
अपना कर्तव्य निभा, आश्वस्त हो लेखन-कार्य में जुटी रहूँ, यही विश्वास सँजोये मैं यह पुस्तक ‘जब मैं न रहूँ ’ प्रस्तुत करती हूँ।
अचानक मन में विचार कौंधा कि आगामी सूचना मिले बिना यदि अन्तिम यात्रा के लिए प्रस्थान करना पड़ा तो अनुजों के लिए विदा-सन्देश देने का अवसर कब मिलेगा ?...
वैसे तो जिन्दगी का कारवाँ स्वमेव चलता रहता है। मेरे-जैसे सहस्रों सामान्य जन प्रति पल इस संसार से विदा लेते हैं। पर स्वभाव-वश मैं अपने मन से अन्तिम सन्देश का प्रलोभन निकाल नहीं पायी।...
अपना कर्तव्य निभा, आश्वस्त हो लेखन-कार्य में जुटी रहूँ, यही विश्वास सँजोये मैं यह पुस्तक ‘जब मैं न रहूँ ’ प्रस्तुत करती हूँ।
शीला गुजराल
जब मैं न रहूँ
जब मैं न रहूँ
तब तुम अपने हियांगन में
सृष्टि का सारा सौन्दर्य
सहेज लेना
जो मैं न सहेज पायी
जब मैं न रहूँ
तब तुम अपने नयनों से
प्रकृति का सारा पीयूष
पी लेना
जो मैं न पी पायी
जब मैं न रहूँ
तब तुम अपने हाथों से दीन दुखियों का सारा दर्द
मथ लेना
जो मैं मथ न पायी
जब मैं न रहूँ
तब तुम मृदुल मुस्कानों से
श्रान्त क्लान्त का सारा क्लेश
हर लेना
जो मैं न हर पायी ।
तब तुम अपने हियांगन में
सृष्टि का सारा सौन्दर्य
सहेज लेना
जो मैं न सहेज पायी
जब मैं न रहूँ
तब तुम अपने नयनों से
प्रकृति का सारा पीयूष
पी लेना
जो मैं न पी पायी
जब मैं न रहूँ
तब तुम अपने हाथों से दीन दुखियों का सारा दर्द
मथ लेना
जो मैं मथ न पायी
जब मैं न रहूँ
तब तुम मृदुल मुस्कानों से
श्रान्त क्लान्त का सारा क्लेश
हर लेना
जो मैं न हर पायी ।
औरत
औरत,
सदियों से
अनन्त परम्परा में अभिशप्त
यातनाएँ सहती
पल-पल ढहती
आक्रान्त होते हुए भी
सदा अखण्डित
पुरुष की वासना
निर्मम अत्याचार
सभी कुछ झेलती
काँटों से खेलती
स्वयं हो जाती भस्म,
सृष्टि थाती
सृजन बीज का
पोषण कर वह
भूमण्डल को
मानस गन्ध से
सदा रखे
सुमण्डित।
सदियों से
अनन्त परम्परा में अभिशप्त
यातनाएँ सहती
पल-पल ढहती
आक्रान्त होते हुए भी
सदा अखण्डित
पुरुष की वासना
निर्मम अत्याचार
सभी कुछ झेलती
काँटों से खेलती
स्वयं हो जाती भस्म,
सृष्टि थाती
सृजन बीज का
पोषण कर वह
भूमण्डल को
मानस गन्ध से
सदा रखे
सुमण्डित।
लाखों अरमान
अभावों की कारा में बन्द
अठारह वर्ष बीत गये
कभी एक जून खाने को मिलता
कभी वह भी नहीं,
पगडण्डियों पर गिरे
कच्चे पक्के आम
बेर-बेरियाँ
जो कुछ मिलता
खा कर
पेट की आग बुझाती,
साँझ ढले
ठण्डे फर्श पर
चटाई डाल, सो जाती।
एक दिन माँ ने
जिगर के टुकड़े को
बूढ़े दूल्हे की भेंट
साड़ी में लपेट,
आशीषों के कलशों को
भर-भर उँडेल
काँपते हाथों से
भेजा ससुराल-
बूढ़े दूल्हे की हवेली
करने आबाद।
गद्देदार पलंग
मीठे पकवान
बीसियों बाँदियाँ
नौकर दरबान-
कपड़े लत्ते
गहनों का अम्बार
पर बन्नो का मन
बीहड़, सुनसान !
बेचारी, बन्नो,
गर्म देगची से ढुलकी
अंगारों पर उतरी
भग्न हुए, ललना के
लाखों अरमान
अठारह वर्ष बीत गये
कभी एक जून खाने को मिलता
कभी वह भी नहीं,
पगडण्डियों पर गिरे
कच्चे पक्के आम
बेर-बेरियाँ
जो कुछ मिलता
खा कर
पेट की आग बुझाती,
साँझ ढले
ठण्डे फर्श पर
चटाई डाल, सो जाती।
एक दिन माँ ने
जिगर के टुकड़े को
बूढ़े दूल्हे की भेंट
साड़ी में लपेट,
आशीषों के कलशों को
भर-भर उँडेल
काँपते हाथों से
भेजा ससुराल-
बूढ़े दूल्हे की हवेली
करने आबाद।
गद्देदार पलंग
मीठे पकवान
बीसियों बाँदियाँ
नौकर दरबान-
कपड़े लत्ते
गहनों का अम्बार
पर बन्नो का मन
बीहड़, सुनसान !
बेचारी, बन्नो,
गर्म देगची से ढुलकी
अंगारों पर उतरी
भग्न हुए, ललना के
लाखों अरमान
पीढ़ी-दर-पीढ़ी
पर्वत की कोख में उपजी
एक अधखिली कली
पूर्ण विकसित होने से पहले ही
व्यभिचारी पर्यटक के हाथों
लुटी।
आज उसकी प्रतिकृति
शैशव की सीढ़ी लाँघ
चहलकदमी करते यात्रियों
की कामाग्नि बुझाने में है
जुटी।
एक अधखिली कली
पूर्ण विकसित होने से पहले ही
व्यभिचारी पर्यटक के हाथों
लुटी।
आज उसकी प्रतिकृति
शैशव की सीढ़ी लाँघ
चहलकदमी करते यात्रियों
की कामाग्नि बुझाने में है
जुटी।
उन्मुक्त
तरुणावस्था में पहुँचते ही
आभास हुआ
मानो
दुत्कारों का जंगल उभर आया हो।
प्रोत्साहन की कोमल मखमली घास
लांछन की समिधा में भस्म हो
धूम्र रेखा बन
धुन्ध-सी छा गयी।
दिशाहीन भटकते
पैरों में बिवाइयाँ
और समूचे तन-मन पर
फफोलों की फसल
उग आयी।
अर्धचेतन अवस्था में
श्रान्त क्लान्त
मुरझाई लता-सी
बरसों पड़ी रही
अचानक
हवा का एक झोंका आया
सजीवनी लाया
उसे सूँघते ही
जंगल फाँद
यौवन के आँगन में
आ पहुँची
जहाँ
सपनों का राजकुमार
उड़न-खटोला लिये
प्रतीक्षारत
खड़ा था।
आभास हुआ
मानो
दुत्कारों का जंगल उभर आया हो।
प्रोत्साहन की कोमल मखमली घास
लांछन की समिधा में भस्म हो
धूम्र रेखा बन
धुन्ध-सी छा गयी।
दिशाहीन भटकते
पैरों में बिवाइयाँ
और समूचे तन-मन पर
फफोलों की फसल
उग आयी।
अर्धचेतन अवस्था में
श्रान्त क्लान्त
मुरझाई लता-सी
बरसों पड़ी रही
अचानक
हवा का एक झोंका आया
सजीवनी लाया
उसे सूँघते ही
जंगल फाँद
यौवन के आँगन में
आ पहुँची
जहाँ
सपनों का राजकुमार
उड़न-खटोला लिये
प्रतीक्षारत
खड़ा था।
अलविदा
माँ की मौत के बाद
खाली घर छोड़
विदेश के लिए
जब उसने विदा ली
तो बाजुओं में सहेज
दो बूँद आँसू बहा
शीतलता प्रदान करने वाला
कोई न था,
और न ही
दरवाज़े पर ठिठका
रेशमी रूमाल हिला
‘अलविदा’ कहने वाला कोई था।
भारी तन मन
टैक्सी में बैठ
जब इधर उधर झाँका
तो देखा-
वायु से बतियाते
पेड़-पौधे
रेशमी रूमाल हिलाते
प्रभात की देवी को
अलविदा कह रहे थे
और विस्तृत हरा मैदान
उषा के ममतामयी
आँसुओं से ढँका था
कुछ आगे-
सड़क के उस पार
आँधी से उखड़े
शबनम से लथपथ
धराशायी वृक्ष को देखा-
मानो अपना ही प्रतिबिम्ब हो !
खाली घर छोड़
विदेश के लिए
जब उसने विदा ली
तो बाजुओं में सहेज
दो बूँद आँसू बहा
शीतलता प्रदान करने वाला
कोई न था,
और न ही
दरवाज़े पर ठिठका
रेशमी रूमाल हिला
‘अलविदा’ कहने वाला कोई था।
भारी तन मन
टैक्सी में बैठ
जब इधर उधर झाँका
तो देखा-
वायु से बतियाते
पेड़-पौधे
रेशमी रूमाल हिलाते
प्रभात की देवी को
अलविदा कह रहे थे
और विस्तृत हरा मैदान
उषा के ममतामयी
आँसुओं से ढँका था
कुछ आगे-
सड़क के उस पार
आँधी से उखड़े
शबनम से लथपथ
धराशायी वृक्ष को देखा-
मानो अपना ही प्रतिबिम्ब हो !
अभिशाप वापस लो
माँ !
अपना अभिशाप वापस लो
मुझे राम की सीता बन कर नहीं रहना
मुझे समाज की निष्ठुरता को नहीं सहना।
सामने देखो,
कितनी सीताएँ तिरस्कृत हो
एकाकी जीवन जी रही हैं
अपने लव-कुश सीने लगा
वेदनाओं के आँसू पी रही हैं
मुझे इस कतार में भर्ती नहीं होना माँ
मुझे नयी रोशनी में बढ़ने दो
मुझे अपने ढँग से जीने दो !
देखो चहुँ ओर,
तमाशबीन धोबियों की भरमार लगी है
कनसुनवे कमनौतियों की लाम जुटी है
मुझे नहीं चाहिए
मर्यादापुरुष राम, कठपुतले भगवान्
जो इनके बहकावे में आ
मुझे त्याग दे।
मुझे तो चाहिए, माँ
ऐसा इन्सान, सही विद्वान
जो समाज से शास्त्रार्थ कर
मेरी खामियों को नजर-अन्दाज कर
वार्तालाप का सेतु बाँध
दुर्गम परिस्थितियों में भी
आँख से आँख मिला सके।
मुझे नहीं चाहिए ऐसा भगवान
जो क्षणभंगुर उन्माद में
प्रसव बीज थोप
मिथ्यापवाद के भय से
परित्याग कर मुझे
नितान्त अकेला छोड़ दे।
मुझे चाहिए, माँ
सचेत सुशील साथी
जो जन्म-भर निर्भीक रहे
प्रीति में सटीक रहे
लोक लांछन दुत्कार
पत्नी को स्वीकार
निज दायित्व निभा सके।
अपना अभिशाप वापस लो
मुझे राम की सीता बन कर नहीं रहना
मुझे समाज की निष्ठुरता को नहीं सहना।
सामने देखो,
कितनी सीताएँ तिरस्कृत हो
एकाकी जीवन जी रही हैं
अपने लव-कुश सीने लगा
वेदनाओं के आँसू पी रही हैं
मुझे इस कतार में भर्ती नहीं होना माँ
मुझे नयी रोशनी में बढ़ने दो
मुझे अपने ढँग से जीने दो !
देखो चहुँ ओर,
तमाशबीन धोबियों की भरमार लगी है
कनसुनवे कमनौतियों की लाम जुटी है
मुझे नहीं चाहिए
मर्यादापुरुष राम, कठपुतले भगवान्
जो इनके बहकावे में आ
मुझे त्याग दे।
मुझे तो चाहिए, माँ
ऐसा इन्सान, सही विद्वान
जो समाज से शास्त्रार्थ कर
मेरी खामियों को नजर-अन्दाज कर
वार्तालाप का सेतु बाँध
दुर्गम परिस्थितियों में भी
आँख से आँख मिला सके।
मुझे नहीं चाहिए ऐसा भगवान
जो क्षणभंगुर उन्माद में
प्रसव बीज थोप
मिथ्यापवाद के भय से
परित्याग कर मुझे
नितान्त अकेला छोड़ दे।
मुझे चाहिए, माँ
सचेत सुशील साथी
जो जन्म-भर निर्भीक रहे
प्रीति में सटीक रहे
लोक लांछन दुत्कार
पत्नी को स्वीकार
निज दायित्व निभा सके।
गोपनीय भेद (एक)
नाती पोतों से घिरी
माया की डोर से जकड़ी
मुस्कराहट का मुखौटा पहन
सफलता का लिबास ओढ़
सौभाग्यवती, ममतामयी
प्रतिभाशाली, गौरवमयी
न जाने कितने उपनामों से
अलंकृत,
बरसों से निज भेद
मन में छिपाये
समता का भाषण देती
सुघड़ गृहिणी का अभिनय करती
व्यस्त हूँ
देखने में स्वस्थ हूँ।
पर आज तुझे बताती हूँ, मेरी बच्ची
मैं भीतर से कितनी खोखली हूँ
मंच पर भाषण देना सहज है
कर के दिखाना सुगम नहीं।
स्वेच्छा, सम-अधिकार, समता
आत्माभिमान, आत्मबल, आत्म-निर्भरता-
ये शब्द कितने सहज हैं
पर गृहस्थी के फन्दे में फँसते ही
वे मृगतृष्णा बन, दूर क्षितिज में मँडराते
मन को अकुलाते हैं।
समाज गढ़ित लक्ष्मण रेखा से निकल
क्रान्तिध्वज उठा,
संघर्ष पथ अपना,
दूभर स्थितियों से जूझने की क्षमता
विरलों में है, जो मुझे में नहीं।
तभी तो, मुस्कराहट का मुखौटा पहन
सफलता का लिबास ओढ़
भीतर से खोखली होते हुए भी, मंच पर भाषण देती
समाज सेविका और सुघड़ गृहिणी का अभिनय करने में
हर पल, हर क्षण व्यस्त हूँ।
माया की डोर से जकड़ी
मुस्कराहट का मुखौटा पहन
सफलता का लिबास ओढ़
सौभाग्यवती, ममतामयी
प्रतिभाशाली, गौरवमयी
न जाने कितने उपनामों से
अलंकृत,
बरसों से निज भेद
मन में छिपाये
समता का भाषण देती
सुघड़ गृहिणी का अभिनय करती
व्यस्त हूँ
देखने में स्वस्थ हूँ।
पर आज तुझे बताती हूँ, मेरी बच्ची
मैं भीतर से कितनी खोखली हूँ
मंच पर भाषण देना सहज है
कर के दिखाना सुगम नहीं।
स्वेच्छा, सम-अधिकार, समता
आत्माभिमान, आत्मबल, आत्म-निर्भरता-
ये शब्द कितने सहज हैं
पर गृहस्थी के फन्दे में फँसते ही
वे मृगतृष्णा बन, दूर क्षितिज में मँडराते
मन को अकुलाते हैं।
समाज गढ़ित लक्ष्मण रेखा से निकल
क्रान्तिध्वज उठा,
संघर्ष पथ अपना,
दूभर स्थितियों से जूझने की क्षमता
विरलों में है, जो मुझे में नहीं।
तभी तो, मुस्कराहट का मुखौटा पहन
सफलता का लिबास ओढ़
भीतर से खोखली होते हुए भी, मंच पर भाषण देती
समाज सेविका और सुघड़ गृहिणी का अभिनय करने में
हर पल, हर क्षण व्यस्त हूँ।
गोपनीय भेद (दो)
मामा की कड़ी निगरानी में
बरामदे की लक्ष्मण-रेखा में बन्द
सखी सहेलियों से कटी
बरसों से पड़ी हूँ।
सुबह-शाम
रोटी-साग, दाल-भात
यन्त्रबद्ध गले उतार
शरीर रूपी इंजन
रखती चलायमान।
निशा-काल
निंदिया की नौका में निश्चित विचरती
तारिकाओं से आँखमिचौली खेलती
चाँदनी के जाम उँडेल
नव स्फूर्ति पा
वापस आ लौटती।
मामा को क्या भान
प्रकृति पीयूष पीती
तेजी से बढ़ती
बावरी बिटिया
दीवारें फाँद
मेढ़ें लाँघ
एक दिन
अपने निर्धारित पथ पर
बढ़ती चली जायेगी
निश्चिन्त, निर्भीक, निश्शंक !
बरामदे की लक्ष्मण-रेखा में बन्द
सखी सहेलियों से कटी
बरसों से पड़ी हूँ।
सुबह-शाम
रोटी-साग, दाल-भात
यन्त्रबद्ध गले उतार
शरीर रूपी इंजन
रखती चलायमान।
निशा-काल
निंदिया की नौका में निश्चित विचरती
तारिकाओं से आँखमिचौली खेलती
चाँदनी के जाम उँडेल
नव स्फूर्ति पा
वापस आ लौटती।
मामा को क्या भान
प्रकृति पीयूष पीती
तेजी से बढ़ती
बावरी बिटिया
दीवारें फाँद
मेढ़ें लाँघ
एक दिन
अपने निर्धारित पथ पर
बढ़ती चली जायेगी
निश्चिन्त, निर्भीक, निश्शंक !
संशय
लाख चेष्टा की
तुझसे राहत पाने की
तुम हो कि दानव की तरह
मेरे पीछे लगे हो।
रात भर
सन्देह की सलाखों पर तड़पती
श्रान्त क्लान्त
मीठी नींद की गोद में
जब सोती
तो अकस्मात्
तुम मुझे
पाशविक पंजों से झपट
जटिल जाल में जकड़
वेदना के विष सागर में
डुबो देते।
मैंने तुर्प चाल निकाली-
अब, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले ही
बिस्तर त्याग
उपवन में जा
स्वच्छन्द पंछियों के
कलरव में डूब
तुम्हारी आँखों से ओझल
हो जाती हूँ।.........
व्यस्तता के दुर्ग में सुरक्षित हो
तुम से नजरें बचा
कर्मठा के कानन में
दिन भर घूमती हूँ
और फिर साँझ ढले
छलछलाते जाम उठा
सुरा के सुरों पर झूमती, मचलती
अलमस्त हो झूलती हूँ।
वहीं न जाने कैसे सेंध लगा
तुम आ टपकते हो
और मुझे क्रूरता से झकझोर
मेरा रंग रूप निचोड़
गर्म लावे में
पुन: उँडेल देते हो
और मैं
रात भर चीखती-चिल्लाती
बिलखती, कराहती
मुक्ति के उपाय ढूँढ़ती हूँ।
लाख चेष्टा की तुमसे राहत पाने की,
तुम हो कि दानव की तरह
मेरे पीछे लगे हो।
तुझसे राहत पाने की
तुम हो कि दानव की तरह
मेरे पीछे लगे हो।
रात भर
सन्देह की सलाखों पर तड़पती
श्रान्त क्लान्त
मीठी नींद की गोद में
जब सोती
तो अकस्मात्
तुम मुझे
पाशविक पंजों से झपट
जटिल जाल में जकड़
वेदना के विष सागर में
डुबो देते।
मैंने तुर्प चाल निकाली-
अब, मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले ही
बिस्तर त्याग
उपवन में जा
स्वच्छन्द पंछियों के
कलरव में डूब
तुम्हारी आँखों से ओझल
हो जाती हूँ।.........
व्यस्तता के दुर्ग में सुरक्षित हो
तुम से नजरें बचा
कर्मठा के कानन में
दिन भर घूमती हूँ
और फिर साँझ ढले
छलछलाते जाम उठा
सुरा के सुरों पर झूमती, मचलती
अलमस्त हो झूलती हूँ।
वहीं न जाने कैसे सेंध लगा
तुम आ टपकते हो
और मुझे क्रूरता से झकझोर
मेरा रंग रूप निचोड़
गर्म लावे में
पुन: उँडेल देते हो
और मैं
रात भर चीखती-चिल्लाती
बिलखती, कराहती
मुक्ति के उपाय ढूँढ़ती हूँ।
लाख चेष्टा की तुमसे राहत पाने की,
तुम हो कि दानव की तरह
मेरे पीछे लगे हो।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i