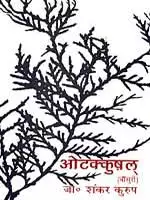|
कविता संग्रह >> ओटक्कुषल् ओटक्कुषल्जी.शंकर कुरुप
|
34 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत कविता में भारतीय अद्वैत भावना का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है..
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
ओटक्कुषल् (बाँसुरी) की कविताओं में भारतीय अद्वैत भावना का साक्ष्य है,
जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकवि जी, शंकर कुरूप ने प्रकृति के
विविध रूपों में प्रतिबिम्बित आत्मछवि की गहरी अनुभूति से अर्जित किया है,
केवल परम्परागत रहस्यवादी मान्यता को स्वीकार भर कर लेने से नहीं। चराचर
के साथ तादात्म्य की प्रतीति के कारण कवि के रूमानी गीतों में भी एक
आध्यात्मिक और उदात्त नैतिक स्वर मुखरित हुआ है। कुरूप बिम्बों और
प्रतीकों के कवि है। इनके माध्यम से परम्परागत छन्द-विधान और संस्कृतनिष्ठ
भाषा को परिमार्जित कर उन्होंने अपने चिन्तन को समर्थ अभिव्यक्ति दी है।
इसलिए कथ्य और शैली-शिल्प दोनों में ही उनकी कविता मलयालम साहित्य ही
नहीं, भारतीय साहित्य की एक उपलब्धि बनकर गूँज रही है।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति ‘ओटक्कुष़ल्’ के इस नये संस्करण का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के लिए गौरव की बात है।
‘‘हो सकता है कि कल यह वंशी, मूक होकर काल की लम्बी कूड़ेदानी में गिर जाये, या यह दीमकों का आहार बन जाये, या यह मात्र एक चुटकी राख के रूप में परिवर्तित हो जाये। तब कुछ ही ऐसे होंगे जो शोक निःश्वास लेकर गुणों की चर्चा करेंगे; लेकिन लोग तो प्रायः बुराइयों के ही गीत गायेंगे : जो भी हो, मेरा जीवन तो तेरे हाथों समर्पित होकर सदा के लिए आनन्द-लहरियों में तरंगित हो गया।’’
धन्य हो गया।’’
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति ‘ओटक्कुष़ल्’ के इस नये संस्करण का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के लिए गौरव की बात है।
‘‘हो सकता है कि कल यह वंशी, मूक होकर काल की लम्बी कूड़ेदानी में गिर जाये, या यह दीमकों का आहार बन जाये, या यह मात्र एक चुटकी राख के रूप में परिवर्तित हो जाये। तब कुछ ही ऐसे होंगे जो शोक निःश्वास लेकर गुणों की चर्चा करेंगे; लेकिन लोग तो प्रायः बुराइयों के ही गीत गायेंगे : जो भी हो, मेरा जीवन तो तेरे हाथों समर्पित होकर सदा के लिए आनन्द-लहरियों में तरंगित हो गया।’’
धन्य हो गया।’’
‘तू ने अपनी सांस की फूँक से
उत्पन्न कर दी है प्राणों की सिरहन
इस निःसार खोखली नली में।’...(जी.शंकर कुरु)
(मुख्य पृष्ठ की रचना करते हुए श्री अल्काज़ी ने वंशी-ध्वनि को चुना है एक छायाकृत पत्ती के रूप में, प्रकृति के बिखरे हुए अनेक उपादानों में से—कि वंशी का रूप चाहे जितना आधुनिक और सूक्ष्म क्यों न हो, उस कल्पनालोक तक नहीं पहुँचायेगा जो महाकवि कुरुप की गीतात्मक प्रकृति से सम्पन्न है और ‘ओटक्कुष़ल्’ का प्रतीक भी।’)
उत्पन्न कर दी है प्राणों की सिरहन
इस निःसार खोखली नली में।’...(जी.शंकर कुरु)
(मुख्य पृष्ठ की रचना करते हुए श्री अल्काज़ी ने वंशी-ध्वनि को चुना है एक छायाकृत पत्ती के रूप में, प्रकृति के बिखरे हुए अनेक उपादानों में से—कि वंशी का रूप चाहे जितना आधुनिक और सूक्ष्म क्यों न हो, उस कल्पनालोक तक नहीं पहुँचायेगा जो महाकवि कुरुप की गीतात्मक प्रकृति से सम्पन्न है और ‘ओटक्कुष़ल्’ का प्रतीक भी।’)
प्राक्कथन
मलयालम की यह काव्यकृति ‘ओटक्कुष़ल्’ भारतीय ज्ञानपीठ
द्वारा
प्रवर्तित एक लाख रुपये राशि से पुरस्कृत हुई है और दिल्ली में 11 नवम्बर,
1966 को आयोजित पुरस्कार-समर्पण-समारोह के अवसर पर हिन्दी-अनुवाद के रूप
में पाठकों के सामने आ रही है। इस काव्य-संग्रह का प्रकाशन भारतीय साहित्य
के इतिहास की बड़ी घटना है। इस अवसर पर यदि भारतीय ज्ञानपीठ को विशेष गर्व
और गौरव अनुभव हो, तो यह स्वाभाविक है।
इस घटना के कितने-कितने आयाम हैं। यह, कि समग्र भारतीय साहित्य को एक इकाई के रूप में देख कर उस मूल्यांकन का प्रयत्न देश में पहली बार हुआ है; कि एक निश्चित विधि-विधान के अन्तर्गत, भारतीय साहित्य की एक कृति को निर्धारित अवधि में प्रकाशित सर्जनात्मक साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धि घोषित कर देश का ध्यान उस कवि और उस कृति की ओर आकर्षित किया जा रहा है; कि, अपेक्षा है कि इस कृति का अनुवाद-प्रकाशन हिन्दी को वास्तविक अर्थ में देश की साहित्यिक उपलब्धियों के आदान-प्रदान का सार्थक माध्यम प्रमाणित करेगा; कि, इस प्रकाशन से यह प्रमाणित होगा कि दिल्ली में जनमा और बैठा हिन्दी भाषा-भाषी साहित्यकार (‘दिल्ली में’ इस लिए कि, यहाँ ही इस प्रकाशन का अनावरण पहली बार हो रहा है) मूल मलयालम की देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ कर देखेगा और विमुग्ध होगा कि जिस अखिल भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक स्पन्दन की बात कही जा रही है, साहित्य के क्षेत्र में वह कोरी कल्पना नहीं है, ठोस यथार्थ है। क्योंकि भाषा, छन्द-विधान, भाव-निधि इतने जाने-पहचाने लगते हैं जैसे उसकी अपनी भाषा की श्रेष्ठ कृतियों की भावभूमि मलयालम के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हो—यद्यपि कहाँ दिल्ली, और कहाँ केरल।
कृतिकार, महाकवि शंकर कुरूप का नाम इन पंक्तियों में अभी तक लिया नहीं गया है, केरल और दिल्ली के हृदयों के इस सम-स्वरीय स्पन्दन से विधाता वे हैं। ओटक्कुष़ल् का शाब्दिक अर्थ मलयालम में, ‘बांस की नली’ है, हिन्दी में हम ने उसे बांसुरी कहा है, अर्थात् ‘वंशी’-बाँस की बनी। कवि का नाम ‘शंकर’ और कृति का नाम ‘वंशी’—जैसे देश का सारा दार्शनिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक चित्र-फलक इस प्रकाश-बिन्दु के आलोक में जगमगा उठा।
पुरस्कार के लिए इस कृति का वरण ‘सर्वश्रेष्ठ’ है के रूप में प्रकाशन अवधि की सीमाओं से बाधित है, यह बात ध्यान में रख लेना आवश्यक है। पुरस्कार-विधान के अन्तर्गत, 1965 के पुरस्कार के लिए वे ही कृतियाँ विचारणीय थीं जिन के लेख जीवित हों, जो ‘सर्जनात्मक साहित्य’ की कोटि में आती हों और जिन का प्रकाशन सन् 1920 से 1958 के बीच हुआ हो। कृति के वरण की पद्धति यह है कि भारतीय संविधान-विहित 14 भाषाओं के लिए एक-एक ‘भाषा परामर्श समिति’ है जो अपनी भाषा की एक कृति को ‘सर्वश्रेष्ठ’ के रूप में चुन कर, भाषा-वर्ग समितियों के विचारार्थ प्रस्तुत करती है। भाषा-वर्ग समितियों का गठन इस प्रकार होता है कि परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों की दो-दो या तीन-तीन भाषाओं का एक वर्ग बनाया जाता है, क्योंकि (अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त पड़ोस के भाषांचल की भाषा जानने वाले समीक्षक सुविधापूर्वक मिल जाते हैं) जो सम्बन्धित भाषा-परामर्श समितियों द्वारा पुरस्कृत दो या तीन कृतियों पर विचार करते हैं और उनमें से एक ‘श्रेष्ठ’ को चुन लेते हैं। इस प्रथम पुरस्कार के सन्दर्भ में ऐसी 5 वर्ग समितियाँ भी थीं जिन्होंने एक-एक कृति को चुना, और अन्तिम निर्णायक मंडल—‘प्रवर परिषद्— के विचारार्थ प्रस्तुत किया।
‘प्रवर परिषद्’ ने द्वि-भाषी साहित्यिक समीक्षकों से कृतियों का पारस्परिक मूल्यांकन करवाया, एक विशेष आधार पर; इनका पुनर्मूल्यांकन करवाया गया। हिन्दी अनुवाद भी सामने प्रस्तुत रहा, अन्तिम निर्णय से पहले सम्बन्धित भाषा समितियों के संयोजकों और कृतियों के हिन्दी अनुवादकों को आमन्त्रित कर के प्रवर परिषद ने उन से अनुशंसित कृतियों के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया, प्रश्नोत्तर हुए, मूल कृतियों के चुने हुए अंशों के पाठ द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया कि अनुवाद में मूल के छन्द, स्वर, लय की जो प्रतिध्वनियाँ नहीं आ पायीं वे क्या हैं—आदि, आदि। इस प्रकार जो कृतियाँ अन्तिम चरण में विचारणीय थीं, उनसे प्रवर परिषद् ने सर्व-सम्मति से महाकवि कुरूप की इस कृति ‘ओटक्कुष़ल्’ का वरण सर्वश्रेष्ठ के रूप में किया।
प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया कि पुस्तक का वरण सर्वथा निष्पक्ष और प्रामाणिक रहे। हमें प्रसन्नता है कि भारतीय ज्ञानपीठ और प्रवर परिषद् की निष्पक्षता और प्रामाणिकता के विषय में कहीं कोई सन्देह नहीं रहा। कृति के वरण के विषय में कहीं कोई मत-भेद हो सकता है, वह प्रत्येक पुरस्कार के सम्बन्ध में सदा रहा है।
ओटक्कुष़ल’ के हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। अनुवाद का प्रमुख लक्ष्य यह था कि मूल का भाव यथा-सम्भव अक्षुण्ण रूप से आ जाये, ताकि, कवि के शब्दों में, ‘‘रिद्म’ (लय) की अपेक्षा ‘कॉण्टेण्ट’ (विषय-बोध, भाव-बोध) पर ध्यान दिया जाये।’’
ज्ञानपीठ श्री पी.एन. भट्टतिरि, सह-सम्पादक ‘भारतवाणी, श्री जी.नारायण पिल्लै, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय केन्द्र, एणार्कुलम, श्री के रविवर्मा, सम्पादक ‘युग प्रभात’ और श्री इलियटम् के प्रति आभारी है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुवाद के प्रारूप को आधार बनाकर रूपान्तर प्रस्तुत किया जा सका है। श्री भट्टरि ने अपने अनुवाद में हिन्दी की छन्द और लय ध्वनि देने का प्रयत्न किया। श्री.जी नारायण पिल्लै की लगन, उनकी क्षमता और श्रम बहुत सहायक रहे। वह दो बार कलकत्ता आये, कुछ दिन रहे और रूपान्तरण के लिए मूल शब्दों और भावों का स्पष्टीकरण किया। संग्रह की एक कविता ‘वन्दनम् परयुक’ का अनुवाद, ‘शतशः धन्यवाद’ श्री दिनकर ने रेडियो के दिल्ली केन्द्र द्वारा आयोजित सर्वभाषा आन्दोलन में प्रस्तुत किया था। उसे साभार सम्मिलित किया गया है। एक समर्थ कवि द्वारा प्रस्तुत अनुवाद को सम्मिलित करने का एक विशेष प्रयोजन यह भी था कि कवि की एक कविता का छन्दबद्ध प्रवाह नमूने के रूप में सामने आये और कवि की अन्य कृतियों के अनुवाद के लिए प्रेरणा मिले।
‘ओटक्कुष़ल्’ में संग्रहीत कविताओं का चयन कवि ने अपनी 1950 तक की रचित कविताओं में से ही किया था। इधर के 15 वर्षों में कवि की प्रतिभा ने कौन सी सामर्थ्य और कौन से आयाम प्राप्त किए हैं, जब तक वह सामने न आए, कवि कुरू के कृतित्व का ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं हो सकता। भारतीय ज्ञानपीठ ने ‘ओटक्कुष़ल्’ के प्रकाशन के साथ-साथ कवि की चुनी हुई परवर्ती दस कविताओं का एक दूसरा संकलन, उनकी कविता के आधार पर ‘एक और नचिकेता’ शीर्षक से प्रकाशित किया है जो इसी प्रथम पुरस्कार-समर्पण-समारोह के अवसर पर पुस्तकों को भेंट किया जा रहा है।
कवि कुरूप ने अपने काव्य-विकास के सम्बन्ध में जो वक्तव्य ‘ओटक्कुष़ल्’ की भूमिका के रूप में तैयार किया था उस का अनुवाद सम्मिलित है। हाँ, श्री गुप्तन नायर की विस्तृत, भावपूर्ण भूमिका का अनुवाद सम्मिलित नहीं किया गया है, विशेषकर इस लिए कि हिन्दी के पाठक और समीक्षक कृति का रसग्रहण और मूल्यांकन स्वयं करें।
महाकवि और उनकी कविता के सम्बन्ध में विशेष कुछ न कह कर यहाँ हम उस ‘प्रशस्ति’ को उद्धरित कर रहे हैं जो कवि के सम्मान में समर्पित है
‘‘भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रवर्तित एक लाख रुपये की राशि का यह साहित्यिक पुरस्कार श्री जी. शंकर कुरूप को उनके मलयालम काव्य-संग्रह ‘ओटक्कुष़ल्’ के लिए समर्पित है, जिसे पुरस्कार विधान के अन्तर्गत गठित प्रवर परिषद् ने सन् 1920 से 1958 के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत् सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया है।
‘ओटक्कुष़ल्’ का वरण यद्यपि सन् 1965 के लिए हुआ है, किन्तु इस का प्रकाशन वर्ष 1950 है। इस दृष्टि से यह कृति कवि के न केवल 1950 तक के सर्वश्रेष्ठ कृतित्व का प्रतिनिधित्व करती है, अपितु उनके अगले 15 वर्षों तक के अधिक समर्थ कृतित्व का पूर्व परिचय देती है। ‘ओटक्कुष़ल्’ की कविताओं में भारतीय अद्वैत भावना का साक्ष्य है जिसे कवि ने परम्परागत रहस्यवादी मान्यता के अंगीकरण द्वारा मान्य नहीं, प्रकृति के नानारूपों में प्रतिबिम्बित आत्म-छवि का वास्तविक अनुभूति द्वारा प्राप्त किया है। चराचर के साथ तादात्मय भाव की इस प्रतीति के कारण कवि कुरूप के रूमानी गीत-काव्य में भी एक आध्यात्मिक और नैतिक उदात्त स्वर है।
‘‘कवि की काव्य चेतना ने ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक युगबोध के प्रति सजग भाव रखा है और उत्तरोत्तर विकास पाया है। इस विकास-यात्रा में प्रकृति-प्रेम का स्थान यथार्थ ने, समाजवादी राष्ट्रीय चेतना का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मानवता ने ले लिया और इन सब की परिणति आध्यात्मिक विश्वचेतना में हुई जहाँ मानव विराट् विश्व की समष्टि से एकतान है; जहां मृत्यु भी विकास का चरण होने के कारण वरेण्य है।
‘‘कुरूप बिम्बों और प्रतीकों के कवि हैं। उन्होंने परम्परागत छन्द-विधान और संस्कृति-निष्ठ भाषा को अपनाया, परिमार्जित किया और अपने चिन्तन तथा काव्य-प्रतिबिम्बों के अनुरूप उन्हें अभिव्यक्ति की नयी सामर्थ्य से पुष्ट किया। इसीलिए कवि का कृतित्व कथ्य में भी शैली-शिल्प में भी मलयालम साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में ही नहीं भारतीय साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में ही नहीं, भारतीय साहित्य की एक उपलब्धि के रूप में भी सहज ग्राह्य है।
कवि दीर्घजीवी हों। शुभं भूयात् !’’
इस घटना के कितने-कितने आयाम हैं। यह, कि समग्र भारतीय साहित्य को एक इकाई के रूप में देख कर उस मूल्यांकन का प्रयत्न देश में पहली बार हुआ है; कि एक निश्चित विधि-विधान के अन्तर्गत, भारतीय साहित्य की एक कृति को निर्धारित अवधि में प्रकाशित सर्जनात्मक साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धि घोषित कर देश का ध्यान उस कवि और उस कृति की ओर आकर्षित किया जा रहा है; कि, अपेक्षा है कि इस कृति का अनुवाद-प्रकाशन हिन्दी को वास्तविक अर्थ में देश की साहित्यिक उपलब्धियों के आदान-प्रदान का सार्थक माध्यम प्रमाणित करेगा; कि, इस प्रकाशन से यह प्रमाणित होगा कि दिल्ली में जनमा और बैठा हिन्दी भाषा-भाषी साहित्यकार (‘दिल्ली में’ इस लिए कि, यहाँ ही इस प्रकाशन का अनावरण पहली बार हो रहा है) मूल मलयालम की देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ कर देखेगा और विमुग्ध होगा कि जिस अखिल भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक स्पन्दन की बात कही जा रही है, साहित्य के क्षेत्र में वह कोरी कल्पना नहीं है, ठोस यथार्थ है। क्योंकि भाषा, छन्द-विधान, भाव-निधि इतने जाने-पहचाने लगते हैं जैसे उसकी अपनी भाषा की श्रेष्ठ कृतियों की भावभूमि मलयालम के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हो—यद्यपि कहाँ दिल्ली, और कहाँ केरल।
कृतिकार, महाकवि शंकर कुरूप का नाम इन पंक्तियों में अभी तक लिया नहीं गया है, केरल और दिल्ली के हृदयों के इस सम-स्वरीय स्पन्दन से विधाता वे हैं। ओटक्कुष़ल् का शाब्दिक अर्थ मलयालम में, ‘बांस की नली’ है, हिन्दी में हम ने उसे बांसुरी कहा है, अर्थात् ‘वंशी’-बाँस की बनी। कवि का नाम ‘शंकर’ और कृति का नाम ‘वंशी’—जैसे देश का सारा दार्शनिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक चित्र-फलक इस प्रकाश-बिन्दु के आलोक में जगमगा उठा।
पुरस्कार के लिए इस कृति का वरण ‘सर्वश्रेष्ठ’ है के रूप में प्रकाशन अवधि की सीमाओं से बाधित है, यह बात ध्यान में रख लेना आवश्यक है। पुरस्कार-विधान के अन्तर्गत, 1965 के पुरस्कार के लिए वे ही कृतियाँ विचारणीय थीं जिन के लेख जीवित हों, जो ‘सर्जनात्मक साहित्य’ की कोटि में आती हों और जिन का प्रकाशन सन् 1920 से 1958 के बीच हुआ हो। कृति के वरण की पद्धति यह है कि भारतीय संविधान-विहित 14 भाषाओं के लिए एक-एक ‘भाषा परामर्श समिति’ है जो अपनी भाषा की एक कृति को ‘सर्वश्रेष्ठ’ के रूप में चुन कर, भाषा-वर्ग समितियों के विचारार्थ प्रस्तुत करती है। भाषा-वर्ग समितियों का गठन इस प्रकार होता है कि परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों की दो-दो या तीन-तीन भाषाओं का एक वर्ग बनाया जाता है, क्योंकि (अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त पड़ोस के भाषांचल की भाषा जानने वाले समीक्षक सुविधापूर्वक मिल जाते हैं) जो सम्बन्धित भाषा-परामर्श समितियों द्वारा पुरस्कृत दो या तीन कृतियों पर विचार करते हैं और उनमें से एक ‘श्रेष्ठ’ को चुन लेते हैं। इस प्रथम पुरस्कार के सन्दर्भ में ऐसी 5 वर्ग समितियाँ भी थीं जिन्होंने एक-एक कृति को चुना, और अन्तिम निर्णायक मंडल—‘प्रवर परिषद्— के विचारार्थ प्रस्तुत किया।
‘प्रवर परिषद्’ ने द्वि-भाषी साहित्यिक समीक्षकों से कृतियों का पारस्परिक मूल्यांकन करवाया, एक विशेष आधार पर; इनका पुनर्मूल्यांकन करवाया गया। हिन्दी अनुवाद भी सामने प्रस्तुत रहा, अन्तिम निर्णय से पहले सम्बन्धित भाषा समितियों के संयोजकों और कृतियों के हिन्दी अनुवादकों को आमन्त्रित कर के प्रवर परिषद ने उन से अनुशंसित कृतियों के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया, प्रश्नोत्तर हुए, मूल कृतियों के चुने हुए अंशों के पाठ द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया कि अनुवाद में मूल के छन्द, स्वर, लय की जो प्रतिध्वनियाँ नहीं आ पायीं वे क्या हैं—आदि, आदि। इस प्रकार जो कृतियाँ अन्तिम चरण में विचारणीय थीं, उनसे प्रवर परिषद् ने सर्व-सम्मति से महाकवि कुरूप की इस कृति ‘ओटक्कुष़ल्’ का वरण सर्वश्रेष्ठ के रूप में किया।
प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया कि पुस्तक का वरण सर्वथा निष्पक्ष और प्रामाणिक रहे। हमें प्रसन्नता है कि भारतीय ज्ञानपीठ और प्रवर परिषद् की निष्पक्षता और प्रामाणिकता के विषय में कहीं कोई सन्देह नहीं रहा। कृति के वरण के विषय में कहीं कोई मत-भेद हो सकता है, वह प्रत्येक पुरस्कार के सम्बन्ध में सदा रहा है।
ओटक्कुष़ल’ के हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। अनुवाद का प्रमुख लक्ष्य यह था कि मूल का भाव यथा-सम्भव अक्षुण्ण रूप से आ जाये, ताकि, कवि के शब्दों में, ‘‘रिद्म’ (लय) की अपेक्षा ‘कॉण्टेण्ट’ (विषय-बोध, भाव-बोध) पर ध्यान दिया जाये।’’
ज्ञानपीठ श्री पी.एन. भट्टतिरि, सह-सम्पादक ‘भारतवाणी, श्री जी.नारायण पिल्लै, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय केन्द्र, एणार्कुलम, श्री के रविवर्मा, सम्पादक ‘युग प्रभात’ और श्री इलियटम् के प्रति आभारी है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुवाद के प्रारूप को आधार बनाकर रूपान्तर प्रस्तुत किया जा सका है। श्री भट्टरि ने अपने अनुवाद में हिन्दी की छन्द और लय ध्वनि देने का प्रयत्न किया। श्री.जी नारायण पिल्लै की लगन, उनकी क्षमता और श्रम बहुत सहायक रहे। वह दो बार कलकत्ता आये, कुछ दिन रहे और रूपान्तरण के लिए मूल शब्दों और भावों का स्पष्टीकरण किया। संग्रह की एक कविता ‘वन्दनम् परयुक’ का अनुवाद, ‘शतशः धन्यवाद’ श्री दिनकर ने रेडियो के दिल्ली केन्द्र द्वारा आयोजित सर्वभाषा आन्दोलन में प्रस्तुत किया था। उसे साभार सम्मिलित किया गया है। एक समर्थ कवि द्वारा प्रस्तुत अनुवाद को सम्मिलित करने का एक विशेष प्रयोजन यह भी था कि कवि की एक कविता का छन्दबद्ध प्रवाह नमूने के रूप में सामने आये और कवि की अन्य कृतियों के अनुवाद के लिए प्रेरणा मिले।
‘ओटक्कुष़ल्’ में संग्रहीत कविताओं का चयन कवि ने अपनी 1950 तक की रचित कविताओं में से ही किया था। इधर के 15 वर्षों में कवि की प्रतिभा ने कौन सी सामर्थ्य और कौन से आयाम प्राप्त किए हैं, जब तक वह सामने न आए, कवि कुरू के कृतित्व का ठीक-ठीक मूल्यांकन नहीं हो सकता। भारतीय ज्ञानपीठ ने ‘ओटक्कुष़ल्’ के प्रकाशन के साथ-साथ कवि की चुनी हुई परवर्ती दस कविताओं का एक दूसरा संकलन, उनकी कविता के आधार पर ‘एक और नचिकेता’ शीर्षक से प्रकाशित किया है जो इसी प्रथम पुरस्कार-समर्पण-समारोह के अवसर पर पुस्तकों को भेंट किया जा रहा है।
कवि कुरूप ने अपने काव्य-विकास के सम्बन्ध में जो वक्तव्य ‘ओटक्कुष़ल्’ की भूमिका के रूप में तैयार किया था उस का अनुवाद सम्मिलित है। हाँ, श्री गुप्तन नायर की विस्तृत, भावपूर्ण भूमिका का अनुवाद सम्मिलित नहीं किया गया है, विशेषकर इस लिए कि हिन्दी के पाठक और समीक्षक कृति का रसग्रहण और मूल्यांकन स्वयं करें।
महाकवि और उनकी कविता के सम्बन्ध में विशेष कुछ न कह कर यहाँ हम उस ‘प्रशस्ति’ को उद्धरित कर रहे हैं जो कवि के सम्मान में समर्पित है
‘‘भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रवर्तित एक लाख रुपये की राशि का यह साहित्यिक पुरस्कार श्री जी. शंकर कुरूप को उनके मलयालम काव्य-संग्रह ‘ओटक्कुष़ल्’ के लिए समर्पित है, जिसे पुरस्कार विधान के अन्तर्गत गठित प्रवर परिषद् ने सन् 1920 से 1958 के बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओं के सर्जनात्मक साहित्य में विधिवत् सर्वश्रेष्ठ निर्णीत और घोषित किया है।
‘ओटक्कुष़ल्’ का वरण यद्यपि सन् 1965 के लिए हुआ है, किन्तु इस का प्रकाशन वर्ष 1950 है। इस दृष्टि से यह कृति कवि के न केवल 1950 तक के सर्वश्रेष्ठ कृतित्व का प्रतिनिधित्व करती है, अपितु उनके अगले 15 वर्षों तक के अधिक समर्थ कृतित्व का पूर्व परिचय देती है। ‘ओटक्कुष़ल्’ की कविताओं में भारतीय अद्वैत भावना का साक्ष्य है जिसे कवि ने परम्परागत रहस्यवादी मान्यता के अंगीकरण द्वारा मान्य नहीं, प्रकृति के नानारूपों में प्रतिबिम्बित आत्म-छवि का वास्तविक अनुभूति द्वारा प्राप्त किया है। चराचर के साथ तादात्मय भाव की इस प्रतीति के कारण कवि कुरूप के रूमानी गीत-काव्य में भी एक आध्यात्मिक और नैतिक उदात्त स्वर है।
‘‘कवि की काव्य चेतना ने ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक युगबोध के प्रति सजग भाव रखा है और उत्तरोत्तर विकास पाया है। इस विकास-यात्रा में प्रकृति-प्रेम का स्थान यथार्थ ने, समाजवादी राष्ट्रीय चेतना का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय मानवता ने ले लिया और इन सब की परिणति आध्यात्मिक विश्वचेतना में हुई जहाँ मानव विराट् विश्व की समष्टि से एकतान है; जहां मृत्यु भी विकास का चरण होने के कारण वरेण्य है।
‘‘कुरूप बिम्बों और प्रतीकों के कवि हैं। उन्होंने परम्परागत छन्द-विधान और संस्कृति-निष्ठ भाषा को अपनाया, परिमार्जित किया और अपने चिन्तन तथा काव्य-प्रतिबिम्बों के अनुरूप उन्हें अभिव्यक्ति की नयी सामर्थ्य से पुष्ट किया। इसीलिए कवि का कृतित्व कथ्य में भी शैली-शिल्प में भी मलयालम साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में ही नहीं भारतीय साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में ही नहीं, भारतीय साहित्य की एक उपलब्धि के रूप में भी सहज ग्राह्य है।
कवि दीर्घजीवी हों। शुभं भूयात् !’’
-लक्ष्मीचन्द्र जैन
मेरी कविता
प्रकृति की कनिष्ठा सन्तान होने के कारण विश्व की अपेक्षा मनुष्य आयु में
बहुत छोटा है। आज भी उसका जीवन शिशु-सहज कौतुकों से भरा है। रूप, नाद, रस,
गन्ध तथा स्पर्श द्वारा उस की ज्ञानेन्द्रियाँ निरन्तर जागरूक हैं। ये
ज्ञानेन्द्रियाँ हृदय तथा आत्मा को मोहित करनेवाला वृत्तान्त मनुष्य को
सदा सुनाती आयी हैं। यह वृत्तान्त कितना भी लम्बा क्यों न हो, मनुष्य की
आत्मा को वह कभी बुरा नहीं लगता। आत्मा को तो इस बात का दुःख रहता है कि
नयी अनुभूतियों के वृत्तान्त लाने के लिए मनुष्य के पास नयी इन्द्रियाँ
नहीं हैं। आत्मा में इस कारण एक प्रकार की असंतृप्ति बनी रहती है।
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अवगत होनेवाला मनुष्य हृदय में एक कौतुकपूर्ण जिज्ञासा जाग्रत करता है। जब कल्पना, चिन्तन आदि मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रकृति का प्रतिबिम्ब आत्मा पर पड़ता होता है, तब मनुष्य हृदय में जाग्रत जिज्ञासा, उस प्रतिबिम्ब का विश्लेषण करने तथा उसको संचय करके एक कथावस्तु के रूप में प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाती है। विश्व, विज्ञान तथा कला का यह सजीव स्रोत किसी के भीतर निरन्तर बहता रहता है तो किसी में तुषार कण की तरह प्रकट होकर विलीन हो जाता है। मेरी आत्मा के किसी उच्च स्तर पर आज भी बहने वाले उस स्रोत ने ही कदाचित मेरे हृदय में प्रकृति एवं मनुष्य जीवन को ध्यान से देखने तथा उनका अध्ययन व आस्वादन करने का कौतुक उत्पन्न किया हो। यह आत्मीयता का भाव ही मेरी अकिंचन तथा अपूर्ण कविता का उद्गम है।
कुछ लोगों का मन्तव्य है कि वैज्ञानिक अभिज्ञता बढ़ने के साथ विलक्षणता कम होने लगती है तथा चिन्तन शक्ति के प्रहार से कल्पना का प्रसाद ढह जाता है। मुझे यह मान्यता ठीक नहीं लगती। सूर्य-मण्डल के सम्बन्ध में मनुष्य की वैज्ञानिक जानकारी बहुत बढ़ गयी है। क्या उस जानकारी के कारण पृथ्वी तथा ग्रह मनुष्य की दृष्टि में और भी अधिक रम्य नहीं बने हैं ? अपने प्रसन्न मुख पर प्रेम की ऊष्मता लिए अनन्त आकाश से कभी झुककर और कभी सीधे निर्निमेष देखने वाला नित्य प्रेमी सूर्य तथा ऋतु-परिवर्तन की विचित्रता लिये अपनी तिमिर केशराशि को पीठ पर फैलाये विविध रंगों में सजकर विविध शब्दों के साथ स्वयं घूम-घूम कर नृत्य करने वाली पृथ्वी—इन सब के भव्य काल्पनिक चित्र मेरे लिए आज भी दर्शनीय हैं। एक क्षुद्र ‘सेल’ रमणीय सुन्दरी शकुन्तला के रूप में विकसित हो जाता है। क्या इस वैज्ञानिक सत्य में कल्पना की उड़ान के लिए स्थान नहीं है ? वास्तव में विज्ञान की कल्पना का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा कौतुक बढ़ता है। बचपन के दिनों की बात है। इडव1 मास की अँधेरी रातों में जब मैं अपने छोटे घर के बरामदे में बैठकर, घने बादलों की गोद से निकल कर उसी में छिप जाने वाली बिजली को देखता तो न जाने क्यों, उछल पड़ता। आज मैं बिजली से अनभिज्ञ नहीं हूँ। वह मेरे परिवार का ही अंग बन गयी है और इस समय मेरी मेज के पास खड़ी होकर, पतले काँच के झीने अवगुंठन के भीतर से मेरी लेखनी उसे देख-देख कर मुस्करा रही है। फिर भी विद्युत की अप्सरा के प्रति तथा उसको बाँध कर रखने वाले मनुष्य के प्रति मेरा कौतुक रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। अपने शरीर पर हाथ लगाने की अविवेकी कृत्य करने वालों को भष्म कर देने वाली बिजली क्या चरित्रगुण में दमयन्ती से कम है ? वैज्ञानिक अभिज्ञता कवि कल्पना के पंखों को सत्य की रक्त शिरायें प्रदान करती है और उनमें उड़ान की शक्ति भर देती है।
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा अवगत होनेवाला मनुष्य हृदय में एक कौतुकपूर्ण जिज्ञासा जाग्रत करता है। जब कल्पना, चिन्तन आदि मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रकृति का प्रतिबिम्ब आत्मा पर पड़ता होता है, तब मनुष्य हृदय में जाग्रत जिज्ञासा, उस प्रतिबिम्ब का विश्लेषण करने तथा उसको संचय करके एक कथावस्तु के रूप में प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाती है। विश्व, विज्ञान तथा कला का यह सजीव स्रोत किसी के भीतर निरन्तर बहता रहता है तो किसी में तुषार कण की तरह प्रकट होकर विलीन हो जाता है। मेरी आत्मा के किसी उच्च स्तर पर आज भी बहने वाले उस स्रोत ने ही कदाचित मेरे हृदय में प्रकृति एवं मनुष्य जीवन को ध्यान से देखने तथा उनका अध्ययन व आस्वादन करने का कौतुक उत्पन्न किया हो। यह आत्मीयता का भाव ही मेरी अकिंचन तथा अपूर्ण कविता का उद्गम है।
कुछ लोगों का मन्तव्य है कि वैज्ञानिक अभिज्ञता बढ़ने के साथ विलक्षणता कम होने लगती है तथा चिन्तन शक्ति के प्रहार से कल्पना का प्रसाद ढह जाता है। मुझे यह मान्यता ठीक नहीं लगती। सूर्य-मण्डल के सम्बन्ध में मनुष्य की वैज्ञानिक जानकारी बहुत बढ़ गयी है। क्या उस जानकारी के कारण पृथ्वी तथा ग्रह मनुष्य की दृष्टि में और भी अधिक रम्य नहीं बने हैं ? अपने प्रसन्न मुख पर प्रेम की ऊष्मता लिए अनन्त आकाश से कभी झुककर और कभी सीधे निर्निमेष देखने वाला नित्य प्रेमी सूर्य तथा ऋतु-परिवर्तन की विचित्रता लिये अपनी तिमिर केशराशि को पीठ पर फैलाये विविध रंगों में सजकर विविध शब्दों के साथ स्वयं घूम-घूम कर नृत्य करने वाली पृथ्वी—इन सब के भव्य काल्पनिक चित्र मेरे लिए आज भी दर्शनीय हैं। एक क्षुद्र ‘सेल’ रमणीय सुन्दरी शकुन्तला के रूप में विकसित हो जाता है। क्या इस वैज्ञानिक सत्य में कल्पना की उड़ान के लिए स्थान नहीं है ? वास्तव में विज्ञान की कल्पना का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा कौतुक बढ़ता है। बचपन के दिनों की बात है। इडव1 मास की अँधेरी रातों में जब मैं अपने छोटे घर के बरामदे में बैठकर, घने बादलों की गोद से निकल कर उसी में छिप जाने वाली बिजली को देखता तो न जाने क्यों, उछल पड़ता। आज मैं बिजली से अनभिज्ञ नहीं हूँ। वह मेरे परिवार का ही अंग बन गयी है और इस समय मेरी मेज के पास खड़ी होकर, पतले काँच के झीने अवगुंठन के भीतर से मेरी लेखनी उसे देख-देख कर मुस्करा रही है। फिर भी विद्युत की अप्सरा के प्रति तथा उसको बाँध कर रखने वाले मनुष्य के प्रति मेरा कौतुक रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। अपने शरीर पर हाथ लगाने की अविवेकी कृत्य करने वालों को भष्म कर देने वाली बिजली क्या चरित्रगुण में दमयन्ती से कम है ? वैज्ञानिक अभिज्ञता कवि कल्पना के पंखों को सत्य की रक्त शिरायें प्रदान करती है और उनमें उड़ान की शक्ति भर देती है।
कला-कविताः
कौतुक से सजीव कल्पना विश्व तथा मनुष्य जीवन को अपनी ओर खींचने तथा अपने
बाहुपाश में करने के लिए हाथ बढ़ाती रहती है। इसलिए उसके हाथ बलिष्ट होते
हैं और उसकी पहुँच दूर तक होती है। मन में बिजली-जैसी उठने वाली प्रक्रिया
जब मनुष्य हृदय में और विश्व-हृदय में भी अपनी प्रति-ध्वनि सुनने के लिए
मचलने लगती है तब हमें सर्वव्यापी एकता की अनुभूति होने लगती है। कल्पना
तथा मानसिक प्रक्रिया का यह कार्य जितना शक्तिशाली होता है उतना ही कलाकार
का महत्त्व भी बढ़ता है। कवि हृदय एवं प्रकृति के बीच, मधुर कल्पना तथा
आर्द भाव-युक्त संयोग से उत्पन्न होने वाली अनुभूति का घनीभूत रूप ही
कथावस्तु है। कल्पना कथावस्तु का प्राण है तो मानसिक प्रक्रिया है उसकी
शिराओं में दौड़ने वाला जीव-रक्त ! कल्पना-सुरभित तथा भाव-निर्मित इन
कथा-वस्तुओं में प्रकृति तथा मानव आत्मा की छाप स्पष्ट रूप से देख सकते
हैं। यह छाप ही कलाकार का व्यक्तित्व है। कथा-वस्तुओं का प्रकाश ही कला
है। अपने कलात्मक जीवन की अनुभूतियों से कविता के सम्बन्ध में यही कुछ समझ
पाया हूँ।
——————————————
1.ऋषभ राशि का तद्भव रूप। केरल के महीने का नाम।
मेरे लिए कविता आत्मा का प्रकाश मात्र है। जैसे धूसर क्षितिज पर सन्ध्या की छवि प्रतिबिम्बित होती है वैसे ही बन्धुर छन्दों के पदबन्धों में कवि का हृदय प्रतिबिम्बित होता है। इस आत्म-प्रकाश से और कुछ बने या न बने, किन्तु एक कलाकार के लिए यह परमानन्द का कारण तो है ही। जैसे मन्द पवन हंस के पंखों को ऊपर उड़ा ले जाता है वैसे ही परमानन्द की यह अनुभूति एक कलाकार की आत्मा को भीतर शरीर से परे उठा ले जाती है। प्राचीन मनुष्य द्वारा गुहा-भित्ति पर अंकित हिरन के चित्र को ही लीजिए। जब मनुष्य के हृदय से निकल कर वह हिरन अचल शिला पर दौड़ने लगा तब उसके साथ उस मनुष्य की आत्मा ने कितनी उड़ाने भरी होंगी। उस मनुष्य की अनुभूति का वह प्रतीक जब उसके मित्रों के हृदयों को भी पुलकित करने लगा तब यो भी उसके निकट खिंच आने लगे। इस प्रकार जो केवल एक व्यक्ति की आत्मा का प्रकाश था उस का एक सामाजिक मूल्य उत्पादन हो गया। एक कवि के होने के कारण अपनी अनुभूतियों का प्रकाश ही मेरे लिए परमानन्द का विषय है। और यदि उस आनन्द का आस्वादन अन्य लोगों को भी करा सका तो वह मेरी विजय होगी। उस से मेरी कला को सामाजिक आधार मिलेगा। लोगों का उत्कर्ष अन्य लोगों के द्वारा हो अथवा मेरे द्वारा ! यह अनुभूति कैसी वांछनीय है, और कितनी आत्म-संतृप्ति है उसमें।
कविता व्यक्तिगत अनुभवों का प्रकाश है। ‘मुत्तकळ्’ नामक अपने कविता-संग्रह में मैंने अपनी यह धारणा प्रकट की थी। जीवन के यथार्थ अनुभवों के आघात से हृदय में उत्पन्न होने वाली मधुर संवेदनाओं की कल्पना का आवरण पहना कर प्रकट करना ही रचना है। उसमें व्यक्ति की प्रधानता रहती है। ‘इल्युजन ऐण्ड रियलिटी’ नामक एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। उस पुस्तक में उपर्युक्त कथन का प्रतिवादन यह प्रमाणित करने के लिए किया गया था कि कला व्यक्ति की नहीं समाज की सृष्टि है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती हैं। किन्तु वास्तव में हैं एक ही सत्य के दो पहलू। क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव सामाजिक अनुभवों का अंग है और व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपज है। मेरे गाँव के हरे मैदान, सुनहरे खेत, ग्राम्य हृदय में मस्तक ऊँचा किये खड़ा रहने वाला प्राचीन मन्दिर, दरिद्रता में डूबा हुआ प्रतिवंश, कवि कल्पना को अपने पास बुलाने वाली पहाड़ियाँ इन्हीं सब ने मेरे हृदय को स्वप्नों से भर दिया था और फिर उन स्वप्नों को विविध रंगों से सजाया तथा वाणी देकर सजीव बनाया था। वह खेत जिसमें कंगन-हंसियों की चमक दिखाई देती है, सिर पर धान का बोझा लिये चलने में हाँफती हुई वे कृषक कन्याएँ, अपनी झोपड़ी की ड्योढ़ियों पर बैठे रहनेवाले पुलयर1, सन्ध्या के शान्ति पूर्ण वातावरण में मधुरता फैलाता हुआ मन्दिर से आने वाला शंखनाद—इन सब से मेरे कल्पना-समुद्र में अव्यक्त एवं विचित्र तरंगें उठी हैं।
मरणोन्मुख सामन्तशाही तथा पाखण्डी पुरोहितों के अत्याचार के कारण गाँव का जीवन विकृत हो रहा है, यह बात बचपन के उन दिनों में मैं नहीं समझता था। तो भी सामन्ती पाखण्डियों तथा उनके नियमों के प्रति मेरे हृदय में लेशमात्र आदर नहीं था। मेरे हृदय में जब मेरा व्यक्तित्व अंकुरित हुआ तब उसकी वायु तथा प्रकाश का आहार मिला, मेरे गाँव के वातावरण से। इसलिए मेरी कविता भी उस ग्राम-हृदय का एक अंग है। उसके बाद जब अध्यापक का काम करने लगा तब एक और गाँव का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा। ‘तिरुविल्वामला’ का विशाल हृदय की तरह फैला हुआ स्वप्न-सान्द्र मैदान, टीलों-वनों में आँखमिचौनी खेलती हुई संकेत स्थान पर आ मिलनेवाली नदियाँ, हाथों में जल कुम्भ लिए खड़े रहने वाले मेघ, तराई के मार्ग पर मन्दगति से जानेवाली बैलगाड़ियाँ ये सब दृश्य हैं जिनके कारण एकान्त में भी मैं एकाकी नहीं था। वे दृष्य मेरे व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहे। ‘एकादशी’ के पर्व के अवसर पर दयालुओं की उदारता की आशा में मार्ग पर मिट्टी की थाली रख कर दूर जा खड़े होनेवाले नायाड़ियों2 को देख कर मुझे दारिद्रय, तथा छूत-छात क्रूरता के साथ-साथ किसी समय स्थापित हुए आर्यों के उपनिवेश का स्मरण हो आता तो भी मनुष्य को प्रकृति चित्र के कतिपय बिन्दुओं की तरह ही मैं देख सका था। सम्भव है उस समय प्रकृति चित्र को संवेदनाओं के उत्ताप से सजीव बनाने के लिए ही मेरा मन मनुष्य को ढूढ़ता था। किन्तु आज मैं प्रकृति-चित्र से भिन्न मनुष्य के आदर्शमय अस्तित्व का वास्तविक चित्र देखता हूँ।
——————————————
1.ऋषभ राशि का तद्भव रूप। केरल के महीने का नाम।
मेरे लिए कविता आत्मा का प्रकाश मात्र है। जैसे धूसर क्षितिज पर सन्ध्या की छवि प्रतिबिम्बित होती है वैसे ही बन्धुर छन्दों के पदबन्धों में कवि का हृदय प्रतिबिम्बित होता है। इस आत्म-प्रकाश से और कुछ बने या न बने, किन्तु एक कलाकार के लिए यह परमानन्द का कारण तो है ही। जैसे मन्द पवन हंस के पंखों को ऊपर उड़ा ले जाता है वैसे ही परमानन्द की यह अनुभूति एक कलाकार की आत्मा को भीतर शरीर से परे उठा ले जाती है। प्राचीन मनुष्य द्वारा गुहा-भित्ति पर अंकित हिरन के चित्र को ही लीजिए। जब मनुष्य के हृदय से निकल कर वह हिरन अचल शिला पर दौड़ने लगा तब उसके साथ उस मनुष्य की आत्मा ने कितनी उड़ाने भरी होंगी। उस मनुष्य की अनुभूति का वह प्रतीक जब उसके मित्रों के हृदयों को भी पुलकित करने लगा तब यो भी उसके निकट खिंच आने लगे। इस प्रकार जो केवल एक व्यक्ति की आत्मा का प्रकाश था उस का एक सामाजिक मूल्य उत्पादन हो गया। एक कवि के होने के कारण अपनी अनुभूतियों का प्रकाश ही मेरे लिए परमानन्द का विषय है। और यदि उस आनन्द का आस्वादन अन्य लोगों को भी करा सका तो वह मेरी विजय होगी। उस से मेरी कला को सामाजिक आधार मिलेगा। लोगों का उत्कर्ष अन्य लोगों के द्वारा हो अथवा मेरे द्वारा ! यह अनुभूति कैसी वांछनीय है, और कितनी आत्म-संतृप्ति है उसमें।
कविता व्यक्तिगत अनुभवों का प्रकाश है। ‘मुत्तकळ्’ नामक अपने कविता-संग्रह में मैंने अपनी यह धारणा प्रकट की थी। जीवन के यथार्थ अनुभवों के आघात से हृदय में उत्पन्न होने वाली मधुर संवेदनाओं की कल्पना का आवरण पहना कर प्रकट करना ही रचना है। उसमें व्यक्ति की प्रधानता रहती है। ‘इल्युजन ऐण्ड रियलिटी’ नामक एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। उस पुस्तक में उपर्युक्त कथन का प्रतिवादन यह प्रमाणित करने के लिए किया गया था कि कला व्यक्ति की नहीं समाज की सृष्टि है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती हैं। किन्तु वास्तव में हैं एक ही सत्य के दो पहलू। क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव सामाजिक अनुभवों का अंग है और व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपज है। मेरे गाँव के हरे मैदान, सुनहरे खेत, ग्राम्य हृदय में मस्तक ऊँचा किये खड़ा रहने वाला प्राचीन मन्दिर, दरिद्रता में डूबा हुआ प्रतिवंश, कवि कल्पना को अपने पास बुलाने वाली पहाड़ियाँ इन्हीं सब ने मेरे हृदय को स्वप्नों से भर दिया था और फिर उन स्वप्नों को विविध रंगों से सजाया तथा वाणी देकर सजीव बनाया था। वह खेत जिसमें कंगन-हंसियों की चमक दिखाई देती है, सिर पर धान का बोझा लिये चलने में हाँफती हुई वे कृषक कन्याएँ, अपनी झोपड़ी की ड्योढ़ियों पर बैठे रहनेवाले पुलयर1, सन्ध्या के शान्ति पूर्ण वातावरण में मधुरता फैलाता हुआ मन्दिर से आने वाला शंखनाद—इन सब से मेरे कल्पना-समुद्र में अव्यक्त एवं विचित्र तरंगें उठी हैं।
मरणोन्मुख सामन्तशाही तथा पाखण्डी पुरोहितों के अत्याचार के कारण गाँव का जीवन विकृत हो रहा है, यह बात बचपन के उन दिनों में मैं नहीं समझता था। तो भी सामन्ती पाखण्डियों तथा उनके नियमों के प्रति मेरे हृदय में लेशमात्र आदर नहीं था। मेरे हृदय में जब मेरा व्यक्तित्व अंकुरित हुआ तब उसकी वायु तथा प्रकाश का आहार मिला, मेरे गाँव के वातावरण से। इसलिए मेरी कविता भी उस ग्राम-हृदय का एक अंग है। उसके बाद जब अध्यापक का काम करने लगा तब एक और गाँव का प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा। ‘तिरुविल्वामला’ का विशाल हृदय की तरह फैला हुआ स्वप्न-सान्द्र मैदान, टीलों-वनों में आँखमिचौनी खेलती हुई संकेत स्थान पर आ मिलनेवाली नदियाँ, हाथों में जल कुम्भ लिए खड़े रहने वाले मेघ, तराई के मार्ग पर मन्दगति से जानेवाली बैलगाड़ियाँ ये सब दृश्य हैं जिनके कारण एकान्त में भी मैं एकाकी नहीं था। वे दृष्य मेरे व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहे। ‘एकादशी’ के पर्व के अवसर पर दयालुओं की उदारता की आशा में मार्ग पर मिट्टी की थाली रख कर दूर जा खड़े होनेवाले नायाड़ियों2 को देख कर मुझे दारिद्रय, तथा छूत-छात क्रूरता के साथ-साथ किसी समय स्थापित हुए आर्यों के उपनिवेश का स्मरण हो आता तो भी मनुष्य को प्रकृति चित्र के कतिपय बिन्दुओं की तरह ही मैं देख सका था। सम्भव है उस समय प्रकृति चित्र को संवेदनाओं के उत्ताप से सजीव बनाने के लिए ही मेरा मन मनुष्य को ढूढ़ता था। किन्तु आज मैं प्रकृति-चित्र से भिन्न मनुष्य के आदर्शमय अस्तित्व का वास्तविक चित्र देखता हूँ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i