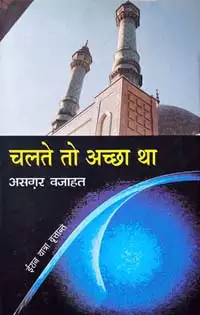|
राजनैतिक >> कैसी आगी लगाई कैसी आगी लगाईअसगर वजाहत
|
391 पाठक हैं |
|||||||
एक श्रेष्ठ उपन्यास
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
उपन्यास का महत्त्व दरअसल आजकल भी इसलिए बना हुआ है कि उपन्यास एक
समानान्तर जीवन की परिकल्पना करते हैं। इस संदर्भ में असगर वजाहत के
उपन्यास ‘कैसी आग लगाई’ में जीवन की विशद व्याख्या है, जीवन
का विस्तार है और तमाम अन्तर्विरोधों के बीच से मानव-गरिमा और श्रेष्ठता
के कलात्मक संकेत मिलते हैं।
पिछले तीस साल से कहानियाँ और उपन्यासों के माध्यम से अपनी विशेष पहचान बना चुके असग़र वजाहत ने ‘कैसी आग लगाई’ में विविधताओं से भरा एक जीवन हमारे सामने रखा है। यह जीवन बिना किसी शर्त पाठक के सामने खुलता चला जाता है। कहीं-कहीं बहुत संवेदनशील और वर्जित माने जानेवाले क्षेत्रों में उपन्यासकार पाठक को बड़ी कलात्मकता और सतर्कता से ले जाता है और कुछ ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जो सम्भवतः हिन्दी उपन्यास में इससे पहले नहीं आए हैं।
उपन्यास का ढाँचा परम्परागत है लेकिन दर्शक के सामने विभिन्न प्रसंग जिस तरह खुलते हैं, वह अत्यन्त कलात्मक है, एक व्यापक जीवन में लेखक जिस प्रसंग को उठाता है उसे जीवन्त बना देता है।
‘कैसी आगी लगाई’ में साम्प्रदायिकता, छात्र-जीवन, स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति, सामन्तवाद, वामपन्थी राजनीति, मुस्लिम समाज, छोटे शहरों का जीवन और महानगर की आपाधापी के साथ-साथ सामाजिक अन्तर्विरोधों से जन्मा वैचारिक संघर्ष भी हमारे सामने आता है। उपन्यास मानवीय सरोकारों और मानवीय गरिमा के कई पक्षों को उद्घाटित करता है। जीवन और जगत् के विभिन्न कार्य-व्यापारों के बीच कथा-सूत्र एक ऐसा रोचक ताना-बाना बुनते हैं कि पाठक उसमें डूबता चला जाता है।
‘कैसी आगी लगाई’ उन पाठकों के लिए आवश्यक है जो उपन्यास विधा से अतिरिक्त आशाएँ रखते हैं।
जिस तरह युद्ध में हारे हुए सिपाही घर लौटते हैं उसी तरह जख्मी, अपमानित भूखा, निराश आस्था और भविष्यहीन मैं अपने घर लौटा। न किसी को देने के लिए कोई तोहफा और न बताने के लिए कोई बात। न पिछले एक साल की कोई ऐसी याद जो ताजा करती रहे। बस एक आवाज है जो चिपक गई है...हार गए...पराजित हो गए...शिकस्त हो गई...डिफीट हो गई...खाट खड़ी हो गई...क्या पाने गए थे यह भी याद नहीं...यही अच्छा है जान बच गई...ख़ैर से बुद्धु घर को आए...दिल्ली में दर्जनों लावारिस कुचलकर रोज मर जाते हैं दैत्याकार द्रुतगामी यान्त्रिक आकृतियों के नीचे। कहीं एक बूँद खून का निशान भी नहीं मिलता।...
राजनीति में, उद्योग में और अपराधजगत में कोई ‘सोर्स’ नहीं है। मैं किसी को खुश करने की कला नहीं जानता और थोड़ी-बहुत शर्म भी है जो आड़े आती है। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि दूसरों का निवाला छीनकर खा जाऊँ और इतना कमजोर भी नहीं बन सका कि अपने को कीड़ा समझकर जी लेता। इसलिए मैं हार गया। खुलकर कहो कि चालाकी और मक्कारी से, बेईमानी और धोखेधड़ी से, चतुराई और कमीनेपन से, स्वार्थ और धृष्टता से, छल और छद्म से, चोरी और सीनाजोरी से, अन्याय और अत्याचार से हार गया...हार गया...सौ बार कहो, कमाल का एक शे’र याद आया....
पिछले तीस साल से कहानियाँ और उपन्यासों के माध्यम से अपनी विशेष पहचान बना चुके असग़र वजाहत ने ‘कैसी आग लगाई’ में विविधताओं से भरा एक जीवन हमारे सामने रखा है। यह जीवन बिना किसी शर्त पाठक के सामने खुलता चला जाता है। कहीं-कहीं बहुत संवेदनशील और वर्जित माने जानेवाले क्षेत्रों में उपन्यासकार पाठक को बड़ी कलात्मकता और सतर्कता से ले जाता है और कुछ ऐसे प्रसंग सामने आते हैं जो सम्भवतः हिन्दी उपन्यास में इससे पहले नहीं आए हैं।
उपन्यास का ढाँचा परम्परागत है लेकिन दर्शक के सामने विभिन्न प्रसंग जिस तरह खुलते हैं, वह अत्यन्त कलात्मक है, एक व्यापक जीवन में लेखक जिस प्रसंग को उठाता है उसे जीवन्त बना देता है।
‘कैसी आगी लगाई’ में साम्प्रदायिकता, छात्र-जीवन, स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति, सामन्तवाद, वामपन्थी राजनीति, मुस्लिम समाज, छोटे शहरों का जीवन और महानगर की आपाधापी के साथ-साथ सामाजिक अन्तर्विरोधों से जन्मा वैचारिक संघर्ष भी हमारे सामने आता है। उपन्यास मानवीय सरोकारों और मानवीय गरिमा के कई पक्षों को उद्घाटित करता है। जीवन और जगत् के विभिन्न कार्य-व्यापारों के बीच कथा-सूत्र एक ऐसा रोचक ताना-बाना बुनते हैं कि पाठक उसमें डूबता चला जाता है।
‘कैसी आगी लगाई’ उन पाठकों के लिए आवश्यक है जो उपन्यास विधा से अतिरिक्त आशाएँ रखते हैं।
जिस तरह युद्ध में हारे हुए सिपाही घर लौटते हैं उसी तरह जख्मी, अपमानित भूखा, निराश आस्था और भविष्यहीन मैं अपने घर लौटा। न किसी को देने के लिए कोई तोहफा और न बताने के लिए कोई बात। न पिछले एक साल की कोई ऐसी याद जो ताजा करती रहे। बस एक आवाज है जो चिपक गई है...हार गए...पराजित हो गए...शिकस्त हो गई...डिफीट हो गई...खाट खड़ी हो गई...क्या पाने गए थे यह भी याद नहीं...यही अच्छा है जान बच गई...ख़ैर से बुद्धु घर को आए...दिल्ली में दर्जनों लावारिस कुचलकर रोज मर जाते हैं दैत्याकार द्रुतगामी यान्त्रिक आकृतियों के नीचे। कहीं एक बूँद खून का निशान भी नहीं मिलता।...
राजनीति में, उद्योग में और अपराधजगत में कोई ‘सोर्स’ नहीं है। मैं किसी को खुश करने की कला नहीं जानता और थोड़ी-बहुत शर्म भी है जो आड़े आती है। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि दूसरों का निवाला छीनकर खा जाऊँ और इतना कमजोर भी नहीं बन सका कि अपने को कीड़ा समझकर जी लेता। इसलिए मैं हार गया। खुलकर कहो कि चालाकी और मक्कारी से, बेईमानी और धोखेधड़ी से, चतुराई और कमीनेपन से, स्वार्थ और धृष्टता से, छल और छद्म से, चोरी और सीनाजोरी से, अन्याय और अत्याचार से हार गया...हार गया...सौ बार कहो, कमाल का एक शे’र याद आया....
भले से हारे जो हारे हमीं तो हार गए
लो आप जीत गए कजकुलाह कर लीजिए।
लो आप जीत गए कजकुलाह कर लीजिए।
-इसी पुस्तक से
एक अनपढ़ का विलाप
आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान रहता हूँ। परेशानी से बचने के लिए काम
शुरू कर देता हूँ। लोग समझते हैं काम कर रहा हूँ जबकि मैं तो सिर्फ
परेशानी से बच रहा होता हूँ। परेशानी यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर झूठ
बोला जा रहा है। आप कहेंगे मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। मैं कहूँगा
बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारा झूठ बोले जाने का फर्क हमारे ऊपर पड़ता है
क्योंकि सच्चाई धुँधलाने लगती है। चीजें समझ में नहीं आतीं और
‘कन्फ्युजन’ वाली स्थिति पैदा हो जाती है। पाकिस्तानी
अणु
वैज्ञानिक डॉ. खान को सजा दी जा रही है कि उसने परमाणु टेक्नॉलोजी ईरान और
सीरिया को दी है, तो जनाब बाकी दूसरे देशों को यह तकनीक कहां से मिली, मैं
एटमबम आदि का कट्टर विरोधी हूँ। अमेरिका ने सबसे पहले एटमबम बनाया और
जापान पर गिराया। यानी अणु तकनीक सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुई फिर
रूस यानी उस जमाने के सोवियत यूनियन में। संसार के अधिकतर देश जिन्होंने
अणु बम बनाया वे कहीं न कहीं अमेरिका और रूस के ऋणी हैं। अब सवाल ये है कि
अमेरिका या रूस अणुबम बनाने की तकनीक किसी देश को देते हैं तो वह मानवता
के लिए खतरा नहीं होता। पर जैसे ही यह काम कुछ अन्य देश करने लगते हैं, यह
मानवता के लिए खतरा बन जाता है। क्यों ? लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा
है।
अमेरिका कहता है कि एटम बम सामूहिक नरसंहार का हथियार है। इसलिए वह उसका कट्टर विरोधी है।
अब सवाल यह है कि सामूहिक नरसंहार हथियारों से मतलब क्या है ? एटम बम से हजारों, लाखों लोग मर सकते हैं लेकिन टैंक, फाइटर प्लेन आदि से सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। उसके हथियारों से सामूहिक नरसंहार नहीं होता; पर नरसंहार तो होता है और नरसंहार अगर लगातार किया जाए तो सामूहिक नरसंहार जैसा ही नुकसान हो सकता है। क्या अमेरिका ने मध्य एशिया में सामूहिक नरसंहार नहीं किए थे ? पर उस समय सामूहिक नरसंहार के विरोध में वह वातावरण क्यों नहीं बन पाया था जो आज है ? या उन हथियारों के खिलाफ विश्व जनमत क्यों नहीं बन रहा है जो अमेरिका बेचता रहता है ? इसलिए मेरी समझ में यह नहीं आता कि सामूहिक नरसंहार के हथियार कौन-से हैं ? और नरसंहारी कौन है ? मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का केवल यह मतलब क्यों है कि एक देश को दूसरे देश में जाकर व्यापार करने की छूट है तथा वहाँ अपना सामान बेचेने की अनुमति है। ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का यह अर्थ क्यों नहीं लगाया जाता है कि एशियाई मजदूर अपनी मेहनत संसार में जहाँ चाहे जाकर बेच सकता है। एशियाई, अफ्रीकी, लातीनी अमरीकी और अरबी जहाँ चाहें जाकर काम करते हैं ? उदारीकरण और पेटेन्ट का क्या सम्बन्ध है ? उदारीकरण का मतलब तो यह है कि सब कुछ सबके लिए खुला है...संसार उदार हो गया है, एकाधिकार नहीं है। लेकिन पेटेन्ट का मतलब तो उदार होना नहीं है। मान लीजिए भारत ‘शून्य’ को पेटेन्ट करा ले ? मान लीजिए अमेरिका टेलीफोन पेटेन्ट करा ले ? मतलब यह कि उदारीकरण और पेटेन्ट की और पेटेन्ट की वकालत एक साथ करने का मतलब क्या है ?
यह भी अजीब रहस्य है कि एक ही राजनीतिक दल एक तरफ तो कहता है कि हम विश्व को बिरादरी मानते हैं, दूसरी तरफ वही राजनीतिक दल किसी भारतीय को इसलिए भारतीय स्वीकार नहीं करता कि उसका पिता या माता विदेशी थे। विश्व की बिरादरी मानने वाला राजनीतिक दल अपने ही देशवासियों का नरसंहार करा देता है। फिर भी विश्व को कुटुम्ब मानता रहता है। एक भी ऐसा राजनीतिक दल मेरी समझ में नहीं आता जो पड़ोसी देश से मित्रता करना चाहता है और देशवासियों के एक बड़े समूह को देशद्रोही मानता है, उनके खिलाफ घृणा का प्रचार करता है, उनको बरबाद कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि देश से प्रेम करने वाले लोग देश की सम्मति विदेशियों को बेच डालें ? यह भी रहस्य ही है कि चुनाव के पहले पूरे देश को घूस दी जाए और घूस देने की प्रशंसा भी हो। घूस देनेवाली सत्ता नैतिकता की बातें भी करती है।
दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाज में आदमियों के पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन की कोई विधि विकसित नहीं हुई है। यदि सिर्फ मोटे तौर पर ही देखा जाए तो हमारे देश में आदमी आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज दहेज के लिए औरतों को जला देना सहज है, दंगाइयों का प्रिय खेल आदमियों, औरतों, बच्चों को आग में जला डालना है, क्योंकि वे जानते हैं इस अपराध को हमारा सभ्य समाज अपराध ही नहीं मानता और उसकी सजा ही नहीं है। आपराधिक मामले छोड़ भी दें तो समाज में धर्मगत, जातिगत, सेक्सगत हिंसा इतनी अधिक है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।चलती ट्रेन में हत्याएँ, बलात्कार, अपराध अपहरण-यह सब क्यों हो रहा है ? सब कुछ इतना उग्र क्यों हो गया है ? कारण यह है कि हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो झूठ पर आधारित और जीवित है। सब कुछ झूठ है और सब जानते हैं कि सब झूठ है, सब मानते हैं कि झूठ है, सबको यह लगता है कि सब झूठ है। न्याय व्यवस्था ऐसी है जहाँ मजिस्ट्रेट को पैसा खिलाकर कुछ भी किया जा सकता है। पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी हर तरह के आरोपों में फँसे हैं, राजनेता-उनके बारे में सब जानते हैं-पत्रकार और मीडियाकर्मी-कुछ बेचारे चीखते रहते हैं पर एक बड़े अनुशासन में बँधे हैं कि व्यवस्था को इतना बुरा मत कहो कि वह गिर जाए-क्योंकि तुम भी इसी व्यवस्था की पैदावार हो, यह गिर जाएगी तो तुम भी गिर जाओगे।
आदमी के सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज उसकी जान की कीमत शून्य है। और हम कहते हैं कि देश के खजाने लबालब भरे हैं। प्रगति के आँकड़े आसमान छू रहे हैं। सबको अच्छा लग रहा है, या लगना चाहिए लेकिन दुःख की बात है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता संसार के सबसे कमजोर आदमी से है।
मेरी परेशानी की एक वजह प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण भी है। हमारे देश में यह बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारे यहाँ पहले दो क्षेत्रों में उद्योग थे। एक निजी क्षेत्र में और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र बड़ी-बड़ी कम्पनियों जैसे बिड़ला, टाटा, डालमिया आदि के उपक्रम थे और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी-बड़ी सरकारी कम्पनियाँ थीं जो सरकार के पैसे से यानी करदाताओं के पैसे से बनाई गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में जो पैसा लगा था वह जनता का पैसा था। अब सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को बेचा जा रहा है और उसे प्राइवेट कम्पनियाँ खरीद रही हैं इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है। क्या सार्वजनिक कम्पनियों में प्राइवेट लोगों (जनता) का पैसा नहीं लगा था ? यानी सार्वजनिक क्षेत्र तो पहले से ही प्राइवेट क्षेत्र था उसे और अधिक प्राइवेट क्यों किया जा रहा है ? मेरी समझ में यह नहीं आता। जनता का अरबों, खरबों रुपया लगाकर जो कम्पनियाँ बनाई गईं उन्हें सरकारी अधिकारियों ने चलाया; इस तरह चलाया कि बुरी तरह लूटा, खाया और जब वे दीवालिया होने के कगार पर हैं तो कहा जा रहा है इन्हें रखना सरकार को महँगा पड़ता है और प्राइवेटाइजेशन की जा रही हैं, बेची जा रही है। कहा जा रहा है सरकार का काम उद्योग धन्धे चलाना नहीं है। तो क्या सरकार ने सभी धन्धों से हाथ खींच लिया है ? नहीं तो क्या सरकार प्रतीक्षा में है कि कौन सा धन्धा चौपट हो और उसे बेच दिया जाए-प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए ?
थोड़ा सोचिए, सरकार ने जनता के पैसे से जो पब्लिक सेक्टर बनाया था। वह लाभ में चलता तो क्या होता ? मान लीजिए जिस तरह प्राइवेट सेक्टर ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है उसी तरह पब्लिक सेक्टर भी तरक्की करता तो क्या होता ? जनता का एक रुपया आज एक लाख रुपए के बराबर होता उसी तरह जैसे पचास साल पहले अम्बानी का एक रुपया आज एक लाख के बराबर है। थोड़ा सोचिए, सरकार को पब्लिक सेक्टर से इतनी आमदनी होती तो वह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार आदि पर लगता है और आज देश में वैसी ही प्रगति दर्ज होती जैसी एशिया के कुछ देशों में देखी जा सकती है।
सवाल यह है कि अम्बानी का एक रुपया आज एक लाख हो गया पर हमारा जनता का पैसा क्यों नहीं हो पाया ? और नहीं हो पाया तो इसका जिम्मेदार कौन है ? ऐसा तो नहीं है कि हमें, आपको यानी जनता को धोखा दिया गया तो ? जनता को धोखा देनेवाले देशप्रेमी हो सकते हैं ?
मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि इराक की जनता को मुक्त कराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने युद्ध किया था और अब इराक की जनता उनका विरोध कर रही है। यह भी समझ में नहीं आता कि इराक की जनता की भावनाओं से ब्रिटेन के प्रधामन्त्री टोनी ब्लेयर जितने परिचित हैं उतना और कोई दूसरा नहीं है।
हमार देश के चुनाव होने वाले हैं और सरकार ने अपने खजाने के मुँह खोल दिए हैं। हर वर्ग को लाभ शुद्ध लाभ पहुँचाने की योजनाएँ घोषित हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या योजनाएँ घोषित करने वालों को पहले से यह पता न था कि समस्याएँ क्या हैं ? ऐसा नहीं हो सकता, समस्याओं की जानकारी सरकार को ही नहीं दरबान तक को होती है। तब फिर आजकल की लाभकारी योजनाएँ क्यों लागू की जा रही हैं ? क्या सरकार को योजनाएँ घोषित करने के समय की जानकारी न थी ? पर यह कैसे हो सकता है कि चुनाव से पहले सब की सब राहत योजनाएँ एक साथ घोषित हो रही हैं ? तुम्हें ये मिल जाएगा मोबाइल सस्ते हो जाएँगे नौकरी मिलेगी, आरक्षण होगा, आयात कर सकोगे निर्यात में भी छूट मिलेगी। इन सब योजनाओं से पब्लिक को लाभ होगा। लाभ का सीधा मतलब है अधिक पैसा। और अधिक पैसा और अधिक पैसा; जितना ज़्यादा पैसा जनता को मिलेगा या बचेगा जनता उतना ही खुश होगी..तो क्या हमारी जनता लालची है ? नहीं, नहीं हमारी जनता लालची नहीं है। ठीक है, लालची नहीं है तो उसे लालची बनाया जा राह है ?....और अगर जनता लालची बनाई जा रही है तो जनता को क्या संस्कार दिए जा रहे हैं ?
जनता को सीधे-सीधे संस्कार दिए जा रहे हैं-‘बाप बड़ा, न भइया सबसे बड़ा रुपइया।’ जनता के यह संस्कार हैं या दिए जा रहे हैं और जनता पैसे के लिए नवविवाहिता लड़कियों को जला रही है तो क्या बुरा कर रही है ? भाई साहब आप एक बहू को जला देंगे...दूसरी लाएँगे तो दहेज दो गुना हो जाएगा। हत्याएँ कीजिए, पैसा अपहरण कीजिए पैसा जनता में लालच के संस्कार बढ़ते हैं और भ्रष्टाचार को सार्वजनिक मान्यता मिलती है तो क्या बुरा है ? हमारी सरकार ने ही यह तय किया है कि रुपया, पैसा, धन, दौलत बड़ी चीजें हैं-चाहे वोट देने से मिले चाहे वोट देने के बाद मिले। भ्रष्टाचार का रोना दिखावा नहीं तो क्या है जबकि सरकार ही प्रत्यक्ष रूप से उसे बढ़ावा दे रही है। वे प्रान्त जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ केन्द्र पैसा देगा, जहाँ नहीं हैं वहाँ नहीं देगा। मतलब नियम कोई नहीं है। हमारे साथ हो तो फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान उठाओ।
पिछले पचास साल में हमने देश को कितना बनाया है, मैं नहीं जानता...लेकिन लोगों को बिगाड़ा है। बूढ़ों को बिगाड़ा है, जवानों और बच्चों को बिगाड़ा है। बिगाड़ने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और आज जो भाषा है-मीडिया की भाषा-संचार की भाषा उस पर राजनीति की काली छाया है।
शब्दों पर जब राजनीति या कहिए अवसरवादी, छद्म राजनीति की काली छाया पड़ने लगे तो लेखक को बड़ी बेचैनी होती है और वह शब्दों को बचाने के लिए बेचैन हो जाता है। वह जानता है शब्द ही न रहेंगे-यानी अर्थवान शब्द ही न रहेंगे तो मनुष्य ही न रहेगा, समाज ही न रहेगा। इसलिए लेखक लिखता है। शब्दों को अर्थ देने या अर्थवान बनाए रखने के लिए।
इन दिनों से पहले कभी यह नहीं लगा कि लिखना कितना जरूरी है। वजह, और सबसे बड़ी वजह यही है कि लेखक जो सोचता है, कहना चाहता है उसके लिए साहित्य को छोड़कर कोई और मंच नहीं बचा है। हर जगह स्पेस की कमी है। राजनीति और मनोरंजन ने सूचना तन्त्र पर लगभग अपना एकाधिकार जमा लिया है। ऐसी स्थिति में यदि लेखक अपनी बात कहना चाहता तो कहाँ कहे ? लेखक यदि इस समाज व्यवस्था के समान्तर कोई दूसरी व्यवस्था देना चाहता है तो कहाँ दे। कौन सा ऐसा मंच है ? क्या राजनीतिक मंच पर हम लेखक अपनी बात कह सकते हैं ? हरगिज नहीं। पर क्या मीडिया, टेलीविजन, रेडियो या पत्र पत्रिकाएँ हमारी चिन्ताओं में शामिल होंगे ? शायद नहीं, क्योंकि उनका काम हमारी चिन्ताओं में शामिल होना नहीं बल्कि अपनी तरह का व्यापार करना है, ले दे कर कागज़ और कलम ही हैं जो हमें शरण देते हैं। शब्द हमारे काम आते हैं।
अमेरिका कहता है कि एटम बम सामूहिक नरसंहार का हथियार है। इसलिए वह उसका कट्टर विरोधी है।
अब सवाल यह है कि सामूहिक नरसंहार हथियारों से मतलब क्या है ? एटम बम से हजारों, लाखों लोग मर सकते हैं लेकिन टैंक, फाइटर प्लेन आदि से सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। उसके हथियारों से सामूहिक नरसंहार नहीं होता; पर नरसंहार तो होता है और नरसंहार अगर लगातार किया जाए तो सामूहिक नरसंहार जैसा ही नुकसान हो सकता है। क्या अमेरिका ने मध्य एशिया में सामूहिक नरसंहार नहीं किए थे ? पर उस समय सामूहिक नरसंहार के विरोध में वह वातावरण क्यों नहीं बन पाया था जो आज है ? या उन हथियारों के खिलाफ विश्व जनमत क्यों नहीं बन रहा है जो अमेरिका बेचता रहता है ? इसलिए मेरी समझ में यह नहीं आता कि सामूहिक नरसंहार के हथियार कौन-से हैं ? और नरसंहारी कौन है ? मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का केवल यह मतलब क्यों है कि एक देश को दूसरे देश में जाकर व्यापार करने की छूट है तथा वहाँ अपना सामान बेचेने की अनुमति है। ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का यह अर्थ क्यों नहीं लगाया जाता है कि एशियाई मजदूर अपनी मेहनत संसार में जहाँ चाहे जाकर बेच सकता है। एशियाई, अफ्रीकी, लातीनी अमरीकी और अरबी जहाँ चाहें जाकर काम करते हैं ? उदारीकरण और पेटेन्ट का क्या सम्बन्ध है ? उदारीकरण का मतलब तो यह है कि सब कुछ सबके लिए खुला है...संसार उदार हो गया है, एकाधिकार नहीं है। लेकिन पेटेन्ट का मतलब तो उदार होना नहीं है। मान लीजिए भारत ‘शून्य’ को पेटेन्ट करा ले ? मान लीजिए अमेरिका टेलीफोन पेटेन्ट करा ले ? मतलब यह कि उदारीकरण और पेटेन्ट की और पेटेन्ट की वकालत एक साथ करने का मतलब क्या है ?
यह भी अजीब रहस्य है कि एक ही राजनीतिक दल एक तरफ तो कहता है कि हम विश्व को बिरादरी मानते हैं, दूसरी तरफ वही राजनीतिक दल किसी भारतीय को इसलिए भारतीय स्वीकार नहीं करता कि उसका पिता या माता विदेशी थे। विश्व की बिरादरी मानने वाला राजनीतिक दल अपने ही देशवासियों का नरसंहार करा देता है। फिर भी विश्व को कुटुम्ब मानता रहता है। एक भी ऐसा राजनीतिक दल मेरी समझ में नहीं आता जो पड़ोसी देश से मित्रता करना चाहता है और देशवासियों के एक बड़े समूह को देशद्रोही मानता है, उनके खिलाफ घृणा का प्रचार करता है, उनको बरबाद कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि देश से प्रेम करने वाले लोग देश की सम्मति विदेशियों को बेच डालें ? यह भी रहस्य ही है कि चुनाव के पहले पूरे देश को घूस दी जाए और घूस देने की प्रशंसा भी हो। घूस देनेवाली सत्ता नैतिकता की बातें भी करती है।
दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाज में आदमियों के पारस्परिक सम्बन्धों के अध्ययन की कोई विधि विकसित नहीं हुई है। यदि सिर्फ मोटे तौर पर ही देखा जाए तो हमारे देश में आदमी आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज दहेज के लिए औरतों को जला देना सहज है, दंगाइयों का प्रिय खेल आदमियों, औरतों, बच्चों को आग में जला डालना है, क्योंकि वे जानते हैं इस अपराध को हमारा सभ्य समाज अपराध ही नहीं मानता और उसकी सजा ही नहीं है। आपराधिक मामले छोड़ भी दें तो समाज में धर्मगत, जातिगत, सेक्सगत हिंसा इतनी अधिक है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।चलती ट्रेन में हत्याएँ, बलात्कार, अपराध अपहरण-यह सब क्यों हो रहा है ? सब कुछ इतना उग्र क्यों हो गया है ? कारण यह है कि हमने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो झूठ पर आधारित और जीवित है। सब कुछ झूठ है और सब जानते हैं कि सब झूठ है, सब मानते हैं कि झूठ है, सबको यह लगता है कि सब झूठ है। न्याय व्यवस्था ऐसी है जहाँ मजिस्ट्रेट को पैसा खिलाकर कुछ भी किया जा सकता है। पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी हर तरह के आरोपों में फँसे हैं, राजनेता-उनके बारे में सब जानते हैं-पत्रकार और मीडियाकर्मी-कुछ बेचारे चीखते रहते हैं पर एक बड़े अनुशासन में बँधे हैं कि व्यवस्था को इतना बुरा मत कहो कि वह गिर जाए-क्योंकि तुम भी इसी व्यवस्था की पैदावार हो, यह गिर जाएगी तो तुम भी गिर जाओगे।
आदमी के सम्मान की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज उसकी जान की कीमत शून्य है। और हम कहते हैं कि देश के खजाने लबालब भरे हैं। प्रगति के आँकड़े आसमान छू रहे हैं। सबको अच्छा लग रहा है, या लगना चाहिए लेकिन दुःख की बात है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता संसार के सबसे कमजोर आदमी से है।
मेरी परेशानी की एक वजह प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण भी है। हमारे देश में यह बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारे यहाँ पहले दो क्षेत्रों में उद्योग थे। एक निजी क्षेत्र में और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र बड़ी-बड़ी कम्पनियों जैसे बिड़ला, टाटा, डालमिया आदि के उपक्रम थे और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी-बड़ी सरकारी कम्पनियाँ थीं जो सरकार के पैसे से यानी करदाताओं के पैसे से बनाई गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में जो पैसा लगा था वह जनता का पैसा था। अब सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को बेचा जा रहा है और उसे प्राइवेट कम्पनियाँ खरीद रही हैं इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जा रहा है। क्या सार्वजनिक कम्पनियों में प्राइवेट लोगों (जनता) का पैसा नहीं लगा था ? यानी सार्वजनिक क्षेत्र तो पहले से ही प्राइवेट क्षेत्र था उसे और अधिक प्राइवेट क्यों किया जा रहा है ? मेरी समझ में यह नहीं आता। जनता का अरबों, खरबों रुपया लगाकर जो कम्पनियाँ बनाई गईं उन्हें सरकारी अधिकारियों ने चलाया; इस तरह चलाया कि बुरी तरह लूटा, खाया और जब वे दीवालिया होने के कगार पर हैं तो कहा जा रहा है इन्हें रखना सरकार को महँगा पड़ता है और प्राइवेटाइजेशन की जा रही हैं, बेची जा रही है। कहा जा रहा है सरकार का काम उद्योग धन्धे चलाना नहीं है। तो क्या सरकार ने सभी धन्धों से हाथ खींच लिया है ? नहीं तो क्या सरकार प्रतीक्षा में है कि कौन सा धन्धा चौपट हो और उसे बेच दिया जाए-प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए ?
थोड़ा सोचिए, सरकार ने जनता के पैसे से जो पब्लिक सेक्टर बनाया था। वह लाभ में चलता तो क्या होता ? मान लीजिए जिस तरह प्राइवेट सेक्टर ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है उसी तरह पब्लिक सेक्टर भी तरक्की करता तो क्या होता ? जनता का एक रुपया आज एक लाख रुपए के बराबर होता उसी तरह जैसे पचास साल पहले अम्बानी का एक रुपया आज एक लाख के बराबर है। थोड़ा सोचिए, सरकार को पब्लिक सेक्टर से इतनी आमदनी होती तो वह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार आदि पर लगता है और आज देश में वैसी ही प्रगति दर्ज होती जैसी एशिया के कुछ देशों में देखी जा सकती है।
सवाल यह है कि अम्बानी का एक रुपया आज एक लाख हो गया पर हमारा जनता का पैसा क्यों नहीं हो पाया ? और नहीं हो पाया तो इसका जिम्मेदार कौन है ? ऐसा तो नहीं है कि हमें, आपको यानी जनता को धोखा दिया गया तो ? जनता को धोखा देनेवाले देशप्रेमी हो सकते हैं ?
मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि इराक की जनता को मुक्त कराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने युद्ध किया था और अब इराक की जनता उनका विरोध कर रही है। यह भी समझ में नहीं आता कि इराक की जनता की भावनाओं से ब्रिटेन के प्रधामन्त्री टोनी ब्लेयर जितने परिचित हैं उतना और कोई दूसरा नहीं है।
हमार देश के चुनाव होने वाले हैं और सरकार ने अपने खजाने के मुँह खोल दिए हैं। हर वर्ग को लाभ शुद्ध लाभ पहुँचाने की योजनाएँ घोषित हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या योजनाएँ घोषित करने वालों को पहले से यह पता न था कि समस्याएँ क्या हैं ? ऐसा नहीं हो सकता, समस्याओं की जानकारी सरकार को ही नहीं दरबान तक को होती है। तब फिर आजकल की लाभकारी योजनाएँ क्यों लागू की जा रही हैं ? क्या सरकार को योजनाएँ घोषित करने के समय की जानकारी न थी ? पर यह कैसे हो सकता है कि चुनाव से पहले सब की सब राहत योजनाएँ एक साथ घोषित हो रही हैं ? तुम्हें ये मिल जाएगा मोबाइल सस्ते हो जाएँगे नौकरी मिलेगी, आरक्षण होगा, आयात कर सकोगे निर्यात में भी छूट मिलेगी। इन सब योजनाओं से पब्लिक को लाभ होगा। लाभ का सीधा मतलब है अधिक पैसा। और अधिक पैसा और अधिक पैसा; जितना ज़्यादा पैसा जनता को मिलेगा या बचेगा जनता उतना ही खुश होगी..तो क्या हमारी जनता लालची है ? नहीं, नहीं हमारी जनता लालची नहीं है। ठीक है, लालची नहीं है तो उसे लालची बनाया जा राह है ?....और अगर जनता लालची बनाई जा रही है तो जनता को क्या संस्कार दिए जा रहे हैं ?
जनता को सीधे-सीधे संस्कार दिए जा रहे हैं-‘बाप बड़ा, न भइया सबसे बड़ा रुपइया।’ जनता के यह संस्कार हैं या दिए जा रहे हैं और जनता पैसे के लिए नवविवाहिता लड़कियों को जला रही है तो क्या बुरा कर रही है ? भाई साहब आप एक बहू को जला देंगे...दूसरी लाएँगे तो दहेज दो गुना हो जाएगा। हत्याएँ कीजिए, पैसा अपहरण कीजिए पैसा जनता में लालच के संस्कार बढ़ते हैं और भ्रष्टाचार को सार्वजनिक मान्यता मिलती है तो क्या बुरा है ? हमारी सरकार ने ही यह तय किया है कि रुपया, पैसा, धन, दौलत बड़ी चीजें हैं-चाहे वोट देने से मिले चाहे वोट देने के बाद मिले। भ्रष्टाचार का रोना दिखावा नहीं तो क्या है जबकि सरकार ही प्रत्यक्ष रूप से उसे बढ़ावा दे रही है। वे प्रान्त जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ केन्द्र पैसा देगा, जहाँ नहीं हैं वहाँ नहीं देगा। मतलब नियम कोई नहीं है। हमारे साथ हो तो फायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान उठाओ।
पिछले पचास साल में हमने देश को कितना बनाया है, मैं नहीं जानता...लेकिन लोगों को बिगाड़ा है। बूढ़ों को बिगाड़ा है, जवानों और बच्चों को बिगाड़ा है। बिगाड़ने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और आज जो भाषा है-मीडिया की भाषा-संचार की भाषा उस पर राजनीति की काली छाया है।
शब्दों पर जब राजनीति या कहिए अवसरवादी, छद्म राजनीति की काली छाया पड़ने लगे तो लेखक को बड़ी बेचैनी होती है और वह शब्दों को बचाने के लिए बेचैन हो जाता है। वह जानता है शब्द ही न रहेंगे-यानी अर्थवान शब्द ही न रहेंगे तो मनुष्य ही न रहेगा, समाज ही न रहेगा। इसलिए लेखक लिखता है। शब्दों को अर्थ देने या अर्थवान बनाए रखने के लिए।
इन दिनों से पहले कभी यह नहीं लगा कि लिखना कितना जरूरी है। वजह, और सबसे बड़ी वजह यही है कि लेखक जो सोचता है, कहना चाहता है उसके लिए साहित्य को छोड़कर कोई और मंच नहीं बचा है। हर जगह स्पेस की कमी है। राजनीति और मनोरंजन ने सूचना तन्त्र पर लगभग अपना एकाधिकार जमा लिया है। ऐसी स्थिति में यदि लेखक अपनी बात कहना चाहता तो कहाँ कहे ? लेखक यदि इस समाज व्यवस्था के समान्तर कोई दूसरी व्यवस्था देना चाहता है तो कहाँ दे। कौन सा ऐसा मंच है ? क्या राजनीतिक मंच पर हम लेखक अपनी बात कह सकते हैं ? हरगिज नहीं। पर क्या मीडिया, टेलीविजन, रेडियो या पत्र पत्रिकाएँ हमारी चिन्ताओं में शामिल होंगे ? शायद नहीं, क्योंकि उनका काम हमारी चिन्ताओं में शामिल होना नहीं बल्कि अपनी तरह का व्यापार करना है, ले दे कर कागज़ और कलम ही हैं जो हमें शरण देते हैं। शब्द हमारे काम आते हैं।
मेरे शेर हैं मेरी सल्तनत, इसी फन में है मुझे आफियन
मेरे कास-एक-शबो-रोज़ तेरे काम की कोई शय नहीं
मेरे कास-एक-शबो-रोज़ तेरे काम की कोई शय नहीं
नासिर काज़मी शायरी में एक पूरी सल्तनत रचते हैं। यानी वे जो दुनिया बनाना
चाहते हैं, वे जैसी व्यवस्था चाहते हैं जैसा निजाम चाहते हैं वह शेरों में
है। इसी कला में यानी शायरी में शायर सुरक्षित है। कलाकार कला से बाहर आता
है तो मर जाता है। अपनी कला में ही वह समानान्तर जीवन और जगत रचता है। यह
रचना निश्चित रूप से ऐसे लोगों के काम की नहीं है जो यथास्थिति के पक्षधर
हैं।
यह सब लिखते हुए ध्यान आया कि सामाजिक परिवर्तन की माँग जब कलाकार, लेखक करते हैं तो यह कहा जाता है कि अरे यह तो कोरी कल्पना है ऐसा कहाँ होता है। जबकि सच्चाई यह है की मानव समाज के विकास का हर चरण एक समय मात्र कोरी कल्पना हुआ करता था। जैसे चाँद पर पहुँच जाना, आकाश में उड़ना लोकतन्त्र या समाजवाद यह सब कभी बिल्कुल कोरी कल्पनाएँ लगा करती होंगी, पर आज नहीं है। और आज अगर हम लोग एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे हैं जहाँ गरीबी नहीं होगी, अत्याचार नहीं होंगे, शोषण नहीं होगा, हर आदमी को शिक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो यह कोई कल्पना नहीं है। यह होगा और अवश्य होगा।
आज की तारीख में सोचना इस देश में सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन कृपया ज़रूर सोचिए।
अब कुछ इस उपन्यास ‘कैसी आगी लगाई’ के बारे में। यह एक उपन्यास त्रयी है। इसका प्रथम भाग जो आपके हाथों में है, वह 1996-1997 के दौरान बुदापैश्त, हंगरी में लिखा गया था। यह सौभाग्य ही कहा जाएगा कि मैं वहाँ जा सका और लगभग ढाई हज़ार पृष्ठ लिख सका। मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने मेरी मदद की थी।
इस उपन्यास त्रयी के दो भाग और प्रकाशित होंगे।
अपने काम की प्रशंसा या निन्दा तो मूर्खता होगी। अब यह आपके हाथों में है और आप ही इसके पारखी हैं।
यह सब लिखते हुए ध्यान आया कि सामाजिक परिवर्तन की माँग जब कलाकार, लेखक करते हैं तो यह कहा जाता है कि अरे यह तो कोरी कल्पना है ऐसा कहाँ होता है। जबकि सच्चाई यह है की मानव समाज के विकास का हर चरण एक समय मात्र कोरी कल्पना हुआ करता था। जैसे चाँद पर पहुँच जाना, आकाश में उड़ना लोकतन्त्र या समाजवाद यह सब कभी बिल्कुल कोरी कल्पनाएँ लगा करती होंगी, पर आज नहीं है। और आज अगर हम लोग एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे हैं जहाँ गरीबी नहीं होगी, अत्याचार नहीं होंगे, शोषण नहीं होगा, हर आदमी को शिक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो यह कोई कल्पना नहीं है। यह होगा और अवश्य होगा।
आज की तारीख में सोचना इस देश में सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन कृपया ज़रूर सोचिए।
अब कुछ इस उपन्यास ‘कैसी आगी लगाई’ के बारे में। यह एक उपन्यास त्रयी है। इसका प्रथम भाग जो आपके हाथों में है, वह 1996-1997 के दौरान बुदापैश्त, हंगरी में लिखा गया था। यह सौभाग्य ही कहा जाएगा कि मैं वहाँ जा सका और लगभग ढाई हज़ार पृष्ठ लिख सका। मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने मेरी मदद की थी।
इस उपन्यास त्रयी के दो भाग और प्रकाशित होंगे।
अपने काम की प्रशंसा या निन्दा तो मूर्खता होगी। अब यह आपके हाथों में है और आप ही इसके पारखी हैं।
31 दिसम्बर 2003
दिल्ली जनवरी
दिल्ली जनवरी
-असग़र वजाहत
1
ये नई बात है। आमतौर पर सायरन सुबह पौने आठ बजे बजता है। क्लास आठ बजे से
शुरू होते हैं। लेकिन आज कोई साढ़े दस बजे सायरन बजने लगा। और बजने भी इस
तरह लगा जैसे करुण आवाज में कोई दैत्य रो रहा हो। सायरन की आवाज सुनकर जो
जहाँ था वहाँ से निकलकर भाग रहा था। पता नहीं, कहाँ ? मैंने किसी से पूछा
कि ये क्या है और सब किधर जा रहे हैं तो जवाब मिला था जल्दी करो, ये
इमरजेन्सी का सायरन है, सब लोग एस.एस. हॉल की तरफ जा रहे हैं। और ज्यादा
पूछने का मौका नहीं था क्योंकि बताने वाला भी बहुत जल्दी में था। वह शायद
कोई सीनियर लड़का था जिसे यूनीवर्सिटी के क़ायदे-कानून पता थे। मैं तो
पिछले ही साल आया था।
एस.एस हॉल में अन्दर जानेवाला लोहे का बड़ा फाटक बन्द था और छोटीवाली खिड़की खुली थी। सब उसी खिड़की से अन्दर जा रहे थे। फाटक के बाहर प्राक्टर और कुछ सीनियर प्रोफेसर खड़े थे, वे सबसे जल्दी अन्दर जाने के लिए कह रहे थे। मुझे पता न था कि अन्दर क्या हो रहा है या होगा ? लेकिन मैं भी अन्दर घुस गया। अन्दर जाकर पता चला कि लगभग पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के यहाँ मौजूद हैं। मुझे अहमद जल्दी ही मिल गया। वह लॉन में कुछ लड़कों के साथ बैठा था। मुझे देखकर वह मेरे पास आ गया।
‘‘ये क्या है यार ?’’ मैंने उससे पूछा।
‘‘पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पर हमला होनेवाला है ?’’
‘‘हमला ? कैसा हमला।’’
‘‘शहर से हिन्दू गुंडों का एक बड़ा गिरोह आ रहा है।’’
‘‘ये तुम्हें किसने बताया ?’’
‘‘सब यही बातें कर रहे हैं।’’
उन दिनों शहर में हिन्दू-मुस्लिम फसाद की फिजा़ बनी हुई थी। दो दिन पहले चाकू मारकर किसी हिन्दू की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मुसलमानों की कुछ दुकानें लुटी थीं। शहर के एक इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था और शहर यूनीवर्सिटी के लड़कों के लिए ‘आउट ऑफ बाउंड’ हो गया था। प्राक्टर का ऐसा नोटिस मैंने देखा था।
फिर अचानक कुछ लड़के छत तक पहुँच गए और ये खबर तेज़ी से फैल गई कि शमशाद मार्केट के ऊपर से धुआँ उठ रहा है। शमशाद मार्केट जल रही है और लूटी जा रही है, ये सुनते ही डर, खौफ़ और ‘न जाने क्या हो’ वाली भावना एकदम गुस्से में बदल गई थी। लड़के बड़े फाटक को खोलने पर जोर दे रहे थे। फाटक के बाहर दूसरी तरफ वाइस चांसलर, प्राक्टर और दूसरे लोग उन्हें समझा रहे थे कि फाटक क्यों नहीं खोला जा सकता। ज़ाहिर है कि अगर कई हज़ार लड़के गुस्से में बाहर निकलते तो उन्हें कौन क्या करने से रोक सकता था ? यह भी नहीं तय था कि बाहर निकलने पर वे सिर्फ़ शमशाद मार्केट तक ही जाएँगे और आगे नहीं बढ़ेंगे।
‘अथारटीज़’ और लड़कों में बातचीत लड़कों की तरफ से इतनी गर्म हो गई थी कि वे वाइस चांसलर को मोटी-मोटी गालियाँ देने लगे। वाइस चांसलर किसी भी कीमत पर फाटक खुलवाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ शमशाद मार्केट के ऊपर से उठने वाला धुआँ एक काला विशाल बादल जैसा बन गया और छत पर जाए बगै़र ही नज़र आने लगा।
कुछ ही देर में पता चला कि लड़कों ने एक कमरे की खिड़की की सलाखें तोड़ डाली हैं और बाहर जाने का रास्ता बन गया है। ये खबर फैलते ही लड़के उस तरफ झटके। मैं और अहमद भी आगे। कमरे के अन्दर की खिड़की से कूद-कूदकर लड़के बाहर निकल रहे थे। हम लोग भी बाहर आ गए। सब शमशाद मार्केट की तरफ भाग रहे थे। अचानक हमें रास्ते में जूलॉजी के लेक्चरर मिले। वे हमें पढ़ाते थे। हम दोनों को देखकर चीखे-खाली हाथ मत जाओ।’ फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से मच्छरदानी का एक बाँस हमें पकड़ा दिया जिसे तोड़कर हमने दो कर लिए। एक टुकड़ा मैंने ले लिया और एक अहमद ने झपट लिया।
शमशाद मार्केट में खालू का होटल धुआँधार जल रहा था। खालू सामने खड़ा था। हमें देखकर बोला-‘तुम लोग अब आए हो। देखो, सारे बर्तन तोड़ गए। कुर्सियाँ बेंचे अन्दर डालकर आग लगा दी। मैं तो कसम से बर्बाद हो गया।’ खालू के होटल के बाद ‘नगीना रेस्टोरेंट’ भी जल रहा था।
एस.एस हॉल में अन्दर जानेवाला लोहे का बड़ा फाटक बन्द था और छोटीवाली खिड़की खुली थी। सब उसी खिड़की से अन्दर जा रहे थे। फाटक के बाहर प्राक्टर और कुछ सीनियर प्रोफेसर खड़े थे, वे सबसे जल्दी अन्दर जाने के लिए कह रहे थे। मुझे पता न था कि अन्दर क्या हो रहा है या होगा ? लेकिन मैं भी अन्दर घुस गया। अन्दर जाकर पता चला कि लगभग पूरी यूनिवर्सिटी के लड़के यहाँ मौजूद हैं। मुझे अहमद जल्दी ही मिल गया। वह लॉन में कुछ लड़कों के साथ बैठा था। मुझे देखकर वह मेरे पास आ गया।
‘‘ये क्या है यार ?’’ मैंने उससे पूछा।
‘‘पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पर हमला होनेवाला है ?’’
‘‘हमला ? कैसा हमला।’’
‘‘शहर से हिन्दू गुंडों का एक बड़ा गिरोह आ रहा है।’’
‘‘ये तुम्हें किसने बताया ?’’
‘‘सब यही बातें कर रहे हैं।’’
उन दिनों शहर में हिन्दू-मुस्लिम फसाद की फिजा़ बनी हुई थी। दो दिन पहले चाकू मारकर किसी हिन्दू की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मुसलमानों की कुछ दुकानें लुटी थीं। शहर के एक इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था और शहर यूनीवर्सिटी के लड़कों के लिए ‘आउट ऑफ बाउंड’ हो गया था। प्राक्टर का ऐसा नोटिस मैंने देखा था।
फिर अचानक कुछ लड़के छत तक पहुँच गए और ये खबर तेज़ी से फैल गई कि शमशाद मार्केट के ऊपर से धुआँ उठ रहा है। शमशाद मार्केट जल रही है और लूटी जा रही है, ये सुनते ही डर, खौफ़ और ‘न जाने क्या हो’ वाली भावना एकदम गुस्से में बदल गई थी। लड़के बड़े फाटक को खोलने पर जोर दे रहे थे। फाटक के बाहर दूसरी तरफ वाइस चांसलर, प्राक्टर और दूसरे लोग उन्हें समझा रहे थे कि फाटक क्यों नहीं खोला जा सकता। ज़ाहिर है कि अगर कई हज़ार लड़के गुस्से में बाहर निकलते तो उन्हें कौन क्या करने से रोक सकता था ? यह भी नहीं तय था कि बाहर निकलने पर वे सिर्फ़ शमशाद मार्केट तक ही जाएँगे और आगे नहीं बढ़ेंगे।
‘अथारटीज़’ और लड़कों में बातचीत लड़कों की तरफ से इतनी गर्म हो गई थी कि वे वाइस चांसलर को मोटी-मोटी गालियाँ देने लगे। वाइस चांसलर किसी भी कीमत पर फाटक खुलवाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ शमशाद मार्केट के ऊपर से उठने वाला धुआँ एक काला विशाल बादल जैसा बन गया और छत पर जाए बगै़र ही नज़र आने लगा।
कुछ ही देर में पता चला कि लड़कों ने एक कमरे की खिड़की की सलाखें तोड़ डाली हैं और बाहर जाने का रास्ता बन गया है। ये खबर फैलते ही लड़के उस तरफ झटके। मैं और अहमद भी आगे। कमरे के अन्दर की खिड़की से कूद-कूदकर लड़के बाहर निकल रहे थे। हम लोग भी बाहर आ गए। सब शमशाद मार्केट की तरफ भाग रहे थे। अचानक हमें रास्ते में जूलॉजी के लेक्चरर मिले। वे हमें पढ़ाते थे। हम दोनों को देखकर चीखे-खाली हाथ मत जाओ।’ फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से मच्छरदानी का एक बाँस हमें पकड़ा दिया जिसे तोड़कर हमने दो कर लिए। एक टुकड़ा मैंने ले लिया और एक अहमद ने झपट लिया।
शमशाद मार्केट में खालू का होटल धुआँधार जल रहा था। खालू सामने खड़ा था। हमें देखकर बोला-‘तुम लोग अब आए हो। देखो, सारे बर्तन तोड़ गए। कुर्सियाँ बेंचे अन्दर डालकर आग लगा दी। मैं तो कसम से बर्बाद हो गया।’ खालू के होटल के बाद ‘नगीना रेस्टोरेंट’ भी जल रहा था।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i