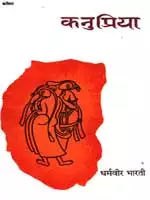|
कविता संग्रह >> कनुप्रिया कनुप्रियाधर्मवीर भारती
|
325 पाठक हैं |
|||||||
भारती जी की श्रेष्ठ कविताएँ...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
ऐसे तो क्षण होते ही हैं जब लगता है कि इतिहास की दुर्दान्त
शक्तियाँ अपनी निर्मम गति से बढ़ रही हैं, जिन में कभी हम अपने को विवश
पाते हैं, कभी विक्षुब्ध, कभी विद्रोही और प्रतिशोधयुक्त, कभी वल्गाएँ हाथ
में लेकर गतिनायक या व्याख्याकार, तो कभी चुपचाप शाप या सलीब स्वीकार करते
हुए आत्मबलिदानी उद्धारक या त्राता.....लेकिन ऐसे भी क्षण होते हैं जब
हमें लगता है कि यह सब जो बाहर का उद्वेग है-महत्त्व उसका नहीं है-महत्त्व
उसका है जो हमारे अन्दर साक्षात्कृत होता है-चरम तन्मयता का क्षण जो एक
स्तर पर सारे बाह्म इतिहास की प्रक्रिया से ज्यादा मूल्यवान् सिद्ध होता
है, जो क्षण हमें सीपी की तरह खोल गया है-इस तरह कि समस्त बाह्म-अतीत,
वर्तमान और भविष्य-सिमट कर उस क्षण में पूँजीभूत हो गया है, और हम हम नहीं
रहे !
प्रयास तो कई बार यह हुआ कि कोई ऐसा मूल्यस्तर खोजा जा सके जिस पर ये दोनों ही स्थितियाँ अपनी सार्थकता पा सकें-पर इस खोज को कठिन पा कर दूसरे आसान समाधान खोज लिये गये हैं-मसलन इन दोनों के बीच एक अमिट पार्थक्य रेखा खींच देना-और फिर इस बिन्दु से खड़े होकर उस बिन्दु को, और उस बिन्दु से खड़े होकर इस बिन्दु को मिथ्या भ्रम घोषित करना।......या दूसरी पद्धति यह रही है कि पहले वह स्थिति जी लेना, उस की तन्मयता को सर्वोपरि मानना- और बाद में दूसरी स्थिति का सामना करना, उस के समाधान की खोज में पहली को बिलकुल भूल जाना। इस तरह पहली को भूलकर दूसरी और दूसरी से अब फिर पहली की ओर निरन्तर घटते-बढ़ते रहना-धीरे-धीरे इस असंगति के प्रति न केवल अभ्यस्त हो जाना-वरन् इसी असंगति को महानता का आधार मान लेना। (यह घोषित करना कि अमुक मनुष्य या प्रभु का व्यक्तित्व ही इसीलिए असाधारण है कि वह दोनों विरोधी स्थितियाँ बिना किसी सामंजस्य के जी सकने में समर्थ हैं।)
लेकिन वह क्या करे जिसने अपने सहज मन से जीवन जिया है, तन्मयता के क्षणों में डूब कर सार्थकता पायी है, और जो अब उद्धघोषित महानताओं से अभिभूत और आतंकित नहीं होता बल्कि आग्रह करता है कि वह उसी सहज की कसौटी पर समस्त को कसेगा।
ऐसा ही आग्रह है कनुप्रिया का !
लेकिन उस का यह प्रश्न और आग्रह उस की प्रारम्भिक कैशोर्य-सुलभ मनःस्थितियों से ही उपज कर धीरे-धीरे विकसित होता गया है। इस कृति का काव्यबोध भी उन विकास स्थितियों को उन की ताजगी में ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करता चलता है। पूर्वराग और मंजरी-परिणय उस विकास का प्रथम चरण, सृष्टि-संकल्प, द्वितीय चरण तथा महाभारत काल से जीवन के अन्त तक शासक, कूटनीतिज्ञ व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास-निर्माण को कनुप्रिया की दृष्टि से देखने वाले खण्ड-इतिहास तथा समापन इस विकास का तृतीय चरण चित्रित करते हैं।
लेखक के पिछले दृश्यकाव्य में एक बिन्दु से इस समस्या पर दृष्टिपात किया जा चुका है-गान्धारी, युयुत्सु और अश्वत्थामा के माध्यम से। कनुप्रिया उनसे सर्वथा पृथक-बिलकुल दूसरे बिन्दु से चल कर उसी समस्या तक पहुँचती है, उसी प्रक्रिया को दूसरे भावस्तर से देखती है और अपने अनजान में ही प्रश्न के ऐसे सन्दर्भ उद्घाटित करती है जो पूरक सिद्ध होते हैं। पर यह सब उस के अनजान में में होता है क्योंकि उस की मूलवृत्ति संशय या जिज्ञासा नहीं, भावाकुल तन्मयता है।
कनुप्रिया की सारी प्रतिक्रियाएँ उसी तन्मयता की विभिन्न स्थितियाँ हैं।
प्रयास तो कई बार यह हुआ कि कोई ऐसा मूल्यस्तर खोजा जा सके जिस पर ये दोनों ही स्थितियाँ अपनी सार्थकता पा सकें-पर इस खोज को कठिन पा कर दूसरे आसान समाधान खोज लिये गये हैं-मसलन इन दोनों के बीच एक अमिट पार्थक्य रेखा खींच देना-और फिर इस बिन्दु से खड़े होकर उस बिन्दु को, और उस बिन्दु से खड़े होकर इस बिन्दु को मिथ्या भ्रम घोषित करना।......या दूसरी पद्धति यह रही है कि पहले वह स्थिति जी लेना, उस की तन्मयता को सर्वोपरि मानना- और बाद में दूसरी स्थिति का सामना करना, उस के समाधान की खोज में पहली को बिलकुल भूल जाना। इस तरह पहली को भूलकर दूसरी और दूसरी से अब फिर पहली की ओर निरन्तर घटते-बढ़ते रहना-धीरे-धीरे इस असंगति के प्रति न केवल अभ्यस्त हो जाना-वरन् इसी असंगति को महानता का आधार मान लेना। (यह घोषित करना कि अमुक मनुष्य या प्रभु का व्यक्तित्व ही इसीलिए असाधारण है कि वह दोनों विरोधी स्थितियाँ बिना किसी सामंजस्य के जी सकने में समर्थ हैं।)
लेकिन वह क्या करे जिसने अपने सहज मन से जीवन जिया है, तन्मयता के क्षणों में डूब कर सार्थकता पायी है, और जो अब उद्धघोषित महानताओं से अभिभूत और आतंकित नहीं होता बल्कि आग्रह करता है कि वह उसी सहज की कसौटी पर समस्त को कसेगा।
ऐसा ही आग्रह है कनुप्रिया का !
लेकिन उस का यह प्रश्न और आग्रह उस की प्रारम्भिक कैशोर्य-सुलभ मनःस्थितियों से ही उपज कर धीरे-धीरे विकसित होता गया है। इस कृति का काव्यबोध भी उन विकास स्थितियों को उन की ताजगी में ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करता चलता है। पूर्वराग और मंजरी-परिणय उस विकास का प्रथम चरण, सृष्टि-संकल्प, द्वितीय चरण तथा महाभारत काल से जीवन के अन्त तक शासक, कूटनीतिज्ञ व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास-निर्माण को कनुप्रिया की दृष्टि से देखने वाले खण्ड-इतिहास तथा समापन इस विकास का तृतीय चरण चित्रित करते हैं।
लेखक के पिछले दृश्यकाव्य में एक बिन्दु से इस समस्या पर दृष्टिपात किया जा चुका है-गान्धारी, युयुत्सु और अश्वत्थामा के माध्यम से। कनुप्रिया उनसे सर्वथा पृथक-बिलकुल दूसरे बिन्दु से चल कर उसी समस्या तक पहुँचती है, उसी प्रक्रिया को दूसरे भावस्तर से देखती है और अपने अनजान में ही प्रश्न के ऐसे सन्दर्भ उद्घाटित करती है जो पूरक सिद्ध होते हैं। पर यह सब उस के अनजान में में होता है क्योंकि उस की मूलवृत्ति संशय या जिज्ञासा नहीं, भावाकुल तन्मयता है।
कनुप्रिया की सारी प्रतिक्रियाएँ उसी तन्मयता की विभिन्न स्थितियाँ हैं।
पहला गीत
ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक-वृक्ष
तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में
जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे तुम को क्या मालूम कि
मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए-धूल में मिली हूँ
धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे
तु्म्हारे कठोर तने के रेशों में कलियाँ बन, कोंपल बन,सौरभ बन,लाली बन-
चुपके से सो गयी हूँ
कि कब मधुमास आये और तुम कब मेरे
प्रस्फुटन से छा जाओ !
फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, नहीं आया,
तब तुम को मेरे इन जावक-रचित पाँवों ने
केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्हीं में हूँ
तुम्हारे ही रेशे-रेशे में सोयी हुई-
और अब समय आ गया कि
मैं तुम्हारी नस-नस में पंख पसार कर उडूँगी
और तुम्हारी डाल-डाल में गुच्छे-गुच्छे लाल-लाल
कलियाँ बन खिलूँगी !
ओ पथ के किनारे खड़े
छायादार पावन अशोक-वृक्ष
तुम यह क्यों कहते हो कि
तुम मेरी ही प्रतीक्षा में
कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे !
तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में
जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे तुम को क्या मालूम कि
मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए-धूल में मिली हूँ
धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे
तु्म्हारे कठोर तने के रेशों में कलियाँ बन, कोंपल बन,सौरभ बन,लाली बन-
चुपके से सो गयी हूँ
कि कब मधुमास आये और तुम कब मेरे
प्रस्फुटन से छा जाओ !
फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, नहीं आया,
तब तुम को मेरे इन जावक-रचित पाँवों ने
केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्हीं में हूँ
तुम्हारे ही रेशे-रेशे में सोयी हुई-
और अब समय आ गया कि
मैं तुम्हारी नस-नस में पंख पसार कर उडूँगी
और तुम्हारी डाल-डाल में गुच्छे-गुच्छे लाल-लाल
कलियाँ बन खिलूँगी !
ओ पथ के किनारे खड़े
छायादार पावन अशोक-वृक्ष
तुम यह क्यों कहते हो कि
तुम मेरी ही प्रतीक्षा में
कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे !
दूसरा गीत
यह जो अकस्मात्
आज मेरे जिस्म के सितार के
एक-एक तार में तुम झंकार उठे हो-
सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत
तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे।
सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को-
पोर-पोर को अवगुण्ठन में ढँक कर तुम्हारे सामने गयी
मुझे तुम से कितनी लाज आती थी,
मैं ने अक्सर अपनी हथेलियों में
अपना लाज से आरक्त मुँह छिपा लिया है
मुझे तुम से कितनी लाज आती थी
मैं अक्सर तुम से केवल तम के प्रगाढ़ परदे में मिली
जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था
मुझे तुम से कितनी लाज आती थी,
पर हाय मुझे क्या मालूम था
कि इस वेला जब अपने को
अपने से छिपाने के लिए मेरे पास
कोई आवरण नहीं रहा
तुम मेरे जिस्म के एक-एक तार से
झकार उठोगे
सुनो ! सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत
इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम
कब से मुझ में छिपे सो रहे थे।
आज मेरे जिस्म के सितार के
एक-एक तार में तुम झंकार उठे हो-
सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत
तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे।
सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को-
पोर-पोर को अवगुण्ठन में ढँक कर तुम्हारे सामने गयी
मुझे तुम से कितनी लाज आती थी,
मैं ने अक्सर अपनी हथेलियों में
अपना लाज से आरक्त मुँह छिपा लिया है
मुझे तुम से कितनी लाज आती थी
मैं अक्सर तुम से केवल तम के प्रगाढ़ परदे में मिली
जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था
मुझे तुम से कितनी लाज आती थी,
पर हाय मुझे क्या मालूम था
कि इस वेला जब अपने को
अपने से छिपाने के लिए मेरे पास
कोई आवरण नहीं रहा
तुम मेरे जिस्म के एक-एक तार से
झकार उठोगे
सुनो ! सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत
इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम
कब से मुझ में छिपे सो रहे थे।
तीसरा गीत
घाट से लौटते हुए
तीसरे पहर की अलसायी बेला में
मैं ने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे
चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया
मैं न कोई अज्ञात वनदेवता समझ
कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया
पर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल!
तुम ने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं !
दिन पर दिन बीतते गये
और मैं ने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया
पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही
अटूट बन्धन बन कर
मेरी प्रणाम-बद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह
लिपट जायेगी कि कभी खुल ही नहीं पायेगी।
और मुझे क्या मालूम था कि
तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे
तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति
इस तरह भा गयी कि
तुम मेरे एक-एक अंग की एक-एक गति को
पूरी तरह बाँध लोगे
इस सम्पूर्ण के लोभी तुम
भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते ?
और मुझ पगली को देखो कि मैं
तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो
कितने निर्लिप्त !
तीसरे पहर की अलसायी बेला में
मैं ने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे
चुपचाप ध्यानमग्न खड़े पाया
मैं न कोई अज्ञात वनदेवता समझ
कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया
पर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त, वीतराग, निश्चल!
तुम ने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं !
दिन पर दिन बीतते गये
और मैं ने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया
पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही
अटूट बन्धन बन कर
मेरी प्रणाम-बद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह
लिपट जायेगी कि कभी खुल ही नहीं पायेगी।
और मुझे क्या मालूम था कि
तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे
तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति
इस तरह भा गयी कि
तुम मेरे एक-एक अंग की एक-एक गति को
पूरी तरह बाँध लोगे
इस सम्पूर्ण के लोभी तुम
भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते ?
और मुझ पगली को देखो कि मैं
तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो
कितने निर्लिप्त !
चौथा गीत
यह जो दोपहर के सन्नाटे में
यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र
किनारे रख
मैं घण्टों जल में निहारती हूँ
क्या तुम समझते हो कि मैं
इस भाँति अपने को देखती हूँ ?
नहीं, मेरे साँवरे !
यमुना के नीले जल में
मेरा यह वेतसलता-सा काँपता तन-बिम्ब, और उस के चारों
ओर साँवली गहराई का अथाह प्रसार जानते हो
कैसा लगता है-
मानो यह यमुना की साँवली गहराई नहीं है
यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर
मुझे चारों ओर से कण-कण, रोम-रोम
अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर-पोर
कसे हुए हो !
यह क्या तुम समझते हो
घण्टों-जल में-मैं अपने को निहारती हूँ
नहीं, मेरे साँवरे !
यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र
किनारे रख
मैं घण्टों जल में निहारती हूँ
क्या तुम समझते हो कि मैं
इस भाँति अपने को देखती हूँ ?
नहीं, मेरे साँवरे !
यमुना के नीले जल में
मेरा यह वेतसलता-सा काँपता तन-बिम्ब, और उस के चारों
ओर साँवली गहराई का अथाह प्रसार जानते हो
कैसा लगता है-
मानो यह यमुना की साँवली गहराई नहीं है
यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर
मुझे चारों ओर से कण-कण, रोम-रोम
अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर-पोर
कसे हुए हो !
यह क्या तुम समझते हो
घण्टों-जल में-मैं अपने को निहारती हूँ
नहीं, मेरे साँवरे !
पाँचवाँ गीत
यह जो मैं गृहकाज से अलसा कर अक्सर
इधर चली आती हूँ
और कदम्ब की छाँह में शिथिल, अस्तव्यस्त
अनमनी-सी पड़ी रहती हूँ....
यह पछतावा अब मुझे हर क्षण
सालता रहता है कि
मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आयी ?
जो चरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर
तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा दे कर नाचते रहे
वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाये
मैं उस दिन लौटी क्यों-
कण-कण अपने को तुम्हें दे कर रीत क्यों नहीं गयी ?
तुम ने तो उस रास की रात
जिसे अंशत: भी आत्मसात् किया
उसे सम्पूर्ण बना कर
वापस अपने-अपने घर भेज दिया
पर हाय वही सम्पूर्णता तो
इस जिस्म के एक-एक कण में
बराबर टीसती रहती है,
तुम्हारे लिए !
कैसे हो जी तुम ?
जब मैं जाना ही नहीं चाहती
तो बाँसुरी के एक गहरे अलाप से
मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो
और जब वापस नहीं आना चाहती
तब मुझे अंशत: ग्रहण कर
सम्पूर्ण बना कर लौटा देते हो !
इधर चली आती हूँ
और कदम्ब की छाँह में शिथिल, अस्तव्यस्त
अनमनी-सी पड़ी रहती हूँ....
यह पछतावा अब मुझे हर क्षण
सालता रहता है कि
मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आयी ?
जो चरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर
तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा दे कर नाचते रहे
वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाये
मैं उस दिन लौटी क्यों-
कण-कण अपने को तुम्हें दे कर रीत क्यों नहीं गयी ?
तुम ने तो उस रास की रात
जिसे अंशत: भी आत्मसात् किया
उसे सम्पूर्ण बना कर
वापस अपने-अपने घर भेज दिया
पर हाय वही सम्पूर्णता तो
इस जिस्म के एक-एक कण में
बराबर टीसती रहती है,
तुम्हारे लिए !
कैसे हो जी तुम ?
जब मैं जाना ही नहीं चाहती
तो बाँसुरी के एक गहरे अलाप से
मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो
और जब वापस नहीं आना चाहती
तब मुझे अंशत: ग्रहण कर
सम्पूर्ण बना कर लौटा देते हो !
मंजरी-परिणय
आम्र-बौर का गीत
यह जो मैं कभी-कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में
बिलकुल जड़ और निस्पन्द हो जाती हूँ
इस का मर्म तुम समझते क्यों नहीं साँवरे !
तुम्हारी जन्म-जन्मान्तर की रहस्यमयी लीला की
एकान्त-संगिनी मैं
इन क्षणों में अकस्मात्
तुम से पृथक् नहीं हो जाती मेरे प्राण,
तुम यह क्यों नहीं समझ पाते कि लाज
सिर्फ जिस्म की नहीं होती
मन की भी होती है
एक मधुर भय
एक अनजाना संशय,
एक आग्रह भरा गोपन,
एक निर्व्याख्या वेदना; उदासी,
जो मुझे बार-बार चरम सुख के क्षणों में भी
अभिभूत कर लेती है।
भय, संशय, गोपन, उदासी
ये सभी ढीठ, चंचल, सरचढ़ी सहेलियों की तरह
मुझे घेर लेती हैं
और मैं कितना चाह कर भी तुम्हारे पास ठीक उसी समय
नहीं पहुँच पाती जब आम्र मंजरियों के नीचे
अपनी बाँसुरी में मेरा नाम भर कर तुम बुलाते हो !
उस दिन तुम उस बौर लदे आम की
झुकी डालियों से टिके कितनी देर मुझे वंशी से टेरते रहे
ढलते सूरज की उदास काँपती किरणें
तुम्हारे माथे के मोरपंखों
से बेबस विदा माँगने लगीं-
मैं नहीं आयी
गायें कुछ क्षण तुम्हें अपनी भोली आँखों से
मुँह उठाये देखती रहीं और फिर
धीरे-धीरे नन्दगाँव की पगडण्डी पर
बिना तुम्हारे अपने-आप मुड़ गयीं-
मैं नहीं आयी
यमुना के घाट पर
मछुओं ने अपनी नावें बाँध दीं
और कन्धों पर पतवारें रख चले गये-
मैं नहीं आयी
तुम ने वंशी होठों से हटा ली थी
और उदास, मौन, तुम आम्र-वृक्ष की जड़ों से टिक कर
बैठ गये थे
और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे
मैं नहीं आयी, नहीं आयी, नहीं आयी
तुम अन्त में उठे
एक झुकी डाल पर खिला एक बौर तुम ने तोड़ा
और धीरे-धीरे चल दिये
अनमने तुम्हारे पाँव पगडण्डी पर चल रहे थे
पर जानते हो तुम्हारे अनजान में ही तुम्हारी उँगलियाँ
क्या कर रही थीं !
वे उस आम्र मंजरी को चूर-चूर कर
श्यामल बनघासों में बिछी उस माँग-सी उजली पगडण्डी पर
बिखेर रही थीं....
यह तुम ने क्या किया प्रिय !
क्या अपने अनजाने में ही
उस आम के बौर से मेरी क्वाँरी उजली पवित्र माँग
भर रहे थे साँवरे ?
पर मुझे देखो कि मैं उस समय भी तो माथा नीचा कर
इस अलौकिक सुहाग से प्रदीप्त हो कर
माथे पर पल्ला डाल कर
झुक कर तुम्हारी चरणधूलि ले कर
तुम्हें प्रणाम करने-
नहीं आयी, नहीं आयी,नहीं आयी !
पर मेरे प्राण
यह क्यों भूल जाते हो कि मैं वही
बावली लड़की हूँ न जो-कदम्ब के नीचे बैठ कर
जब तुम पोई की जंगली लतरों के पके फलों को
तोड़ कर, मसल कर, उन की लाली से मेरे पाँवों को
महावर रचने के लिए अपनी गोद में रखते हो
तो मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती हूँ
और अपने पाँव पूरे बल से समेट कर खींच लेती हूँ
अपनी दोनों बाँहों में अपने घुटने कस
मुँह फेर कर निश्चल बैठ जाती हूँ
पर शाम को जब घर आती हूँ तो
निभृत एकान्त में दीपक के मन्द आलोक में
अपने उन्हीं चरणों को
अपलक निहारती हूँ
बावली सी उन्हें बार-बार प्यार करती हूँ
जल्दी-जल्दी में अधबनी उन महावर की रेखाओं को
चारों ओर देख कर धीमे-से
चूम लेती हूँ।
रात गहरा आयी है
और तुम चले गये हो
और मैं कितनी देर तक बाँह से
उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही हूँ
जिस पर टिक कर तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो
और मैं लौट रही हूँ,
हताश, और निष्फल
और ये आम के बौर के कण-कण
मेरे पाँवों में बुरी तरह साल रहे हैं।
पर तुम्हें यह कौन बतायेगा साँवरे
कि देर ही में सही
पर मैं तुम्हारे पुकारने पर आ तो गयी
और माँग-सी उजली पगडण्डी पर बिखरे
ये मंजरी-कण भी अगर मेरे चरणों में गड़ते हैं तो
इसी लिए न कि कितना लम्बा रास्ता
कितनी जल्दी-जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा है
और काँटों और काँकरियों से
मेरे पाँव किस बुरी तरह घायल हो गये हैं !
यह कैसे बताऊँ तुम्हें
कि चरम साक्षात्कार के ये अनूठे क्षण भी
जो कभी-कभी मेरे हाथ से छूट जाते हैं
तुम्हारी मर्म-पुकार जो कभी-कभी मैं नहीं सुन पाती
तुम्हारी भेंट का अर्थ जो नहीं समझ पाती
तो मेरे साँवरे-
लाज मन की भी होती है
एक अज्ञात भय,
अपरिचित संशय,
आग्रह भरा गोपन,
और सुख के क्षण
में भी घिर आने वाली निर्व्याख्या उदासी-
फिर भी उसे चीर कर
देर में ही आऊँगी प्राण,
तो क्या तुम मुझे अपनी लम्बी,
चन्दन-बाँहों में भर कर बेसुध नहीं
कर दोगे ?
बिलकुल जड़ और निस्पन्द हो जाती हूँ
इस का मर्म तुम समझते क्यों नहीं साँवरे !
तुम्हारी जन्म-जन्मान्तर की रहस्यमयी लीला की
एकान्त-संगिनी मैं
इन क्षणों में अकस्मात्
तुम से पृथक् नहीं हो जाती मेरे प्राण,
तुम यह क्यों नहीं समझ पाते कि लाज
सिर्फ जिस्म की नहीं होती
मन की भी होती है
एक मधुर भय
एक अनजाना संशय,
एक आग्रह भरा गोपन,
एक निर्व्याख्या वेदना; उदासी,
जो मुझे बार-बार चरम सुख के क्षणों में भी
अभिभूत कर लेती है।
भय, संशय, गोपन, उदासी
ये सभी ढीठ, चंचल, सरचढ़ी सहेलियों की तरह
मुझे घेर लेती हैं
और मैं कितना चाह कर भी तुम्हारे पास ठीक उसी समय
नहीं पहुँच पाती जब आम्र मंजरियों के नीचे
अपनी बाँसुरी में मेरा नाम भर कर तुम बुलाते हो !
उस दिन तुम उस बौर लदे आम की
झुकी डालियों से टिके कितनी देर मुझे वंशी से टेरते रहे
ढलते सूरज की उदास काँपती किरणें
तुम्हारे माथे के मोरपंखों
से बेबस विदा माँगने लगीं-
मैं नहीं आयी
गायें कुछ क्षण तुम्हें अपनी भोली आँखों से
मुँह उठाये देखती रहीं और फिर
धीरे-धीरे नन्दगाँव की पगडण्डी पर
बिना तुम्हारे अपने-आप मुड़ गयीं-
मैं नहीं आयी
यमुना के घाट पर
मछुओं ने अपनी नावें बाँध दीं
और कन्धों पर पतवारें रख चले गये-
मैं नहीं आयी
तुम ने वंशी होठों से हटा ली थी
और उदास, मौन, तुम आम्र-वृक्ष की जड़ों से टिक कर
बैठ गये थे
और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे
मैं नहीं आयी, नहीं आयी, नहीं आयी
तुम अन्त में उठे
एक झुकी डाल पर खिला एक बौर तुम ने तोड़ा
और धीरे-धीरे चल दिये
अनमने तुम्हारे पाँव पगडण्डी पर चल रहे थे
पर जानते हो तुम्हारे अनजान में ही तुम्हारी उँगलियाँ
क्या कर रही थीं !
वे उस आम्र मंजरी को चूर-चूर कर
श्यामल बनघासों में बिछी उस माँग-सी उजली पगडण्डी पर
बिखेर रही थीं....
यह तुम ने क्या किया प्रिय !
क्या अपने अनजाने में ही
उस आम के बौर से मेरी क्वाँरी उजली पवित्र माँग
भर रहे थे साँवरे ?
पर मुझे देखो कि मैं उस समय भी तो माथा नीचा कर
इस अलौकिक सुहाग से प्रदीप्त हो कर
माथे पर पल्ला डाल कर
झुक कर तुम्हारी चरणधूलि ले कर
तुम्हें प्रणाम करने-
नहीं आयी, नहीं आयी,नहीं आयी !
पर मेरे प्राण
यह क्यों भूल जाते हो कि मैं वही
बावली लड़की हूँ न जो-कदम्ब के नीचे बैठ कर
जब तुम पोई की जंगली लतरों के पके फलों को
तोड़ कर, मसल कर, उन की लाली से मेरे पाँवों को
महावर रचने के लिए अपनी गोद में रखते हो
तो मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती हूँ
और अपने पाँव पूरे बल से समेट कर खींच लेती हूँ
अपनी दोनों बाँहों में अपने घुटने कस
मुँह फेर कर निश्चल बैठ जाती हूँ
पर शाम को जब घर आती हूँ तो
निभृत एकान्त में दीपक के मन्द आलोक में
अपने उन्हीं चरणों को
अपलक निहारती हूँ
बावली सी उन्हें बार-बार प्यार करती हूँ
जल्दी-जल्दी में अधबनी उन महावर की रेखाओं को
चारों ओर देख कर धीमे-से
चूम लेती हूँ।
रात गहरा आयी है
और तुम चले गये हो
और मैं कितनी देर तक बाँह से
उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही हूँ
जिस पर टिक कर तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो
और मैं लौट रही हूँ,
हताश, और निष्फल
और ये आम के बौर के कण-कण
मेरे पाँवों में बुरी तरह साल रहे हैं।
पर तुम्हें यह कौन बतायेगा साँवरे
कि देर ही में सही
पर मैं तुम्हारे पुकारने पर आ तो गयी
और माँग-सी उजली पगडण्डी पर बिखरे
ये मंजरी-कण भी अगर मेरे चरणों में गड़ते हैं तो
इसी लिए न कि कितना लम्बा रास्ता
कितनी जल्दी-जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा है
और काँटों और काँकरियों से
मेरे पाँव किस बुरी तरह घायल हो गये हैं !
यह कैसे बताऊँ तुम्हें
कि चरम साक्षात्कार के ये अनूठे क्षण भी
जो कभी-कभी मेरे हाथ से छूट जाते हैं
तुम्हारी मर्म-पुकार जो कभी-कभी मैं नहीं सुन पाती
तुम्हारी भेंट का अर्थ जो नहीं समझ पाती
तो मेरे साँवरे-
लाज मन की भी होती है
एक अज्ञात भय,
अपरिचित संशय,
आग्रह भरा गोपन,
और सुख के क्षण
में भी घिर आने वाली निर्व्याख्या उदासी-
फिर भी उसे चीर कर
देर में ही आऊँगी प्राण,
तो क्या तुम मुझे अपनी लम्बी,
चन्दन-बाँहों में भर कर बेसुध नहीं
कर दोगे ?
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i